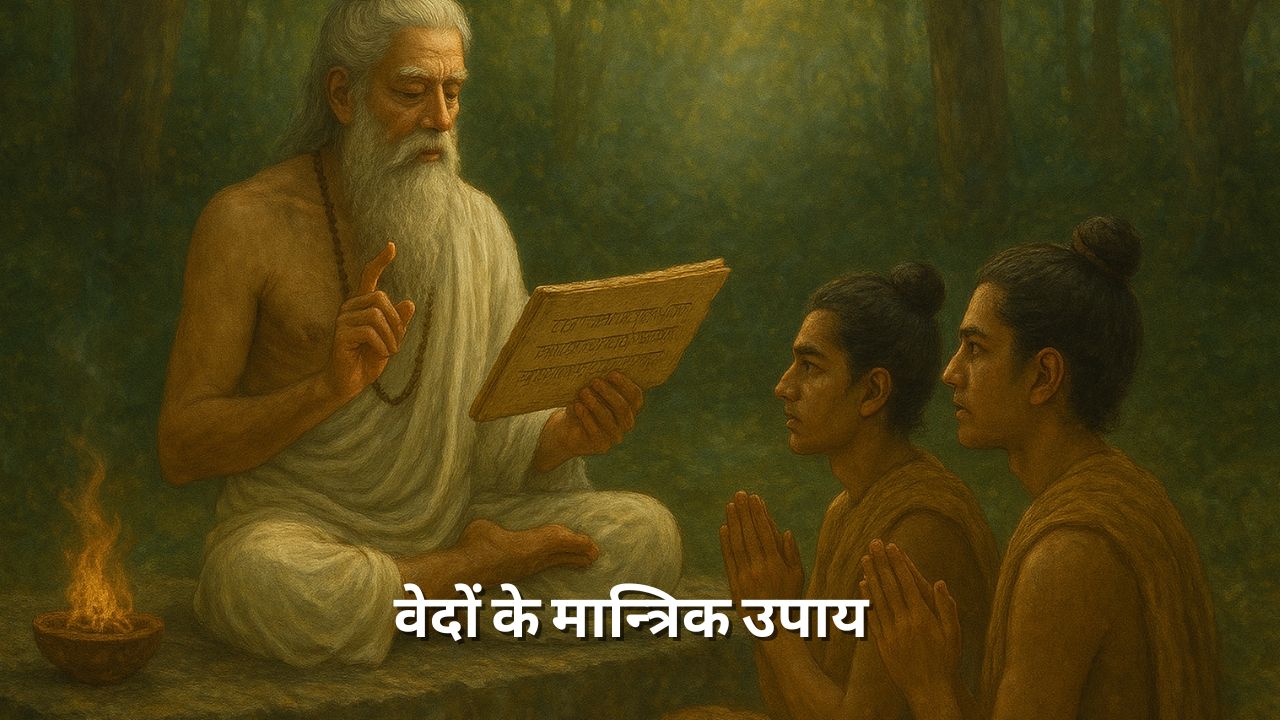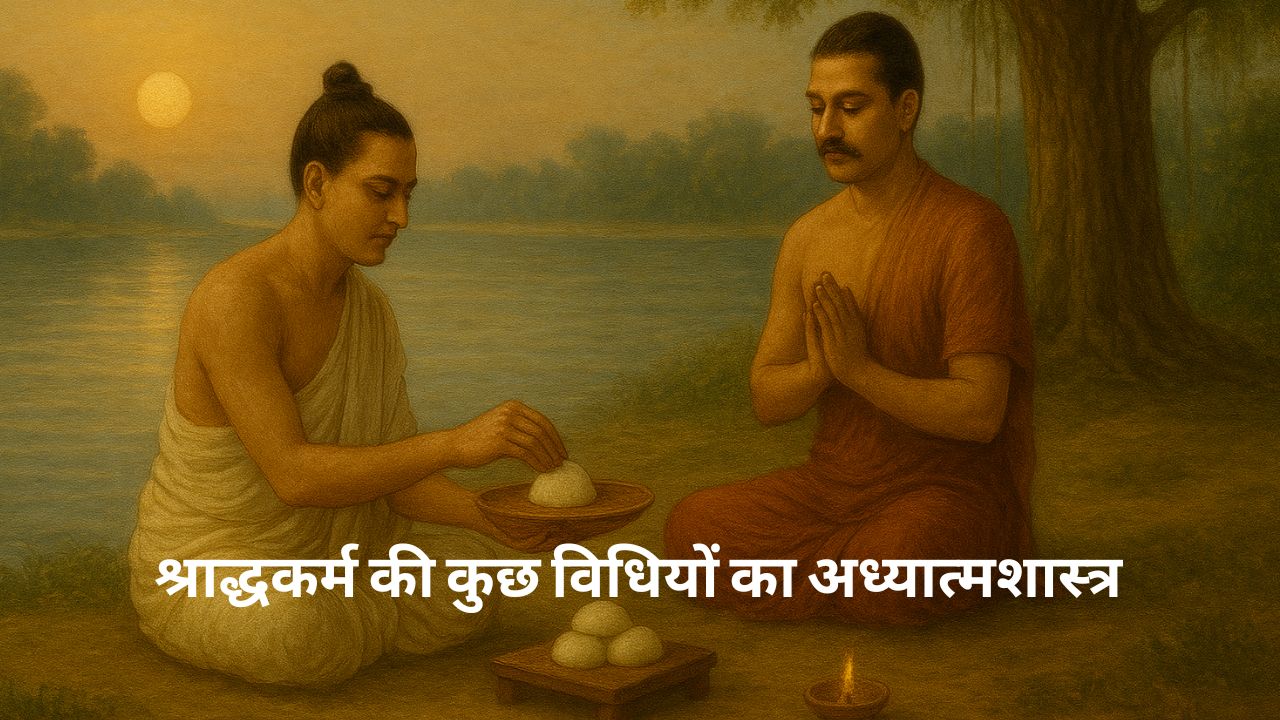- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
प्रचंड प्रद्योत(धर्मज्ञ)- पृथ्वी से देखने पर सूर्य जिस पथ में दिखते हैं वह क्रान्तिवृत्त (ecliptic) है। क्रान्तिवृत्त के उत्तर व दक्षिण ९-९ अंशों के विस्तार से बनी पट्टी को भचक्र (zodiac) कहते हैं। भचक्र में ही समस्त ग्रह गतिशील हैं। भचक्र में २७ नक्षत्र अवस्थित हैं। भचक्र के १२ भाग हैं जो राशि कहलाते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके क्रमश: नाम हैं – मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ व मीन।
पृथ्वी एवं उसके परिक्रमण-पथ द्वारा आकाश पर बने प्रक्षेप की संज्ञा “विष्णु” है। इस प्रक्षेप के अनेक रूप हैं किन्तु “चतुर्भुज रूप” को “विष्णु का स्वरूप” कहा जाता है। भचक्र भी विष्णु का एक रूप है। समस्त तारों सहित सम्पूर्ण आकाश भी विष्णु ही है।
क्रान्तिवृत्त के क्रमश: ४ बिन्दुओं १. दक्षिणायनान्त (पैर), २. उत्तरगोलारम्भ (बायाँ करतल) ३. उत्तरायणान्त (सिर) व ४. दक्षिणगोलारम्भ (दायाँ करतल) को मिलाने से बना चतुर्भुज “विष्णु” है। इस चतुर्भुज के केन्द्र को “ब्रह्म-स्थान” कहा गया है जहाँ सूर्य प्रतिष्ठित हैं।
यह चतुर्भुज ब्रह्म-स्थान रूपी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा है। उपर्युक्त चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के मध्य ३-३ ऋतुमास होते हैं – प्रथम व द्वितीय के मध्य तपस् , तपस्य व मधु। द्वितीय व तृतीय के मध्य माधव, शुक्र व शुचि। तृतीय व चतुर्थ के मध्य नभस् , नभस्य व इष। चतुर्थ व प्रथम के मध्य ऊर्ज, सहस् व सहस्य। इस चतुर्भुज-पुरुष (विष्णु) के करतलों को मिलाने वाली रेखा “कर्ण” है। जब कर्ण के बाएँ सिरे पर सूर्य दृष्टिगोचर होते हैं तब “मधु” मास का अन्त हो जाता है तथा जब कर्ण के दाएँ सिरे पर सूर्य दृष्टिगोचर होते हैं तब “इष” मास का अन्त हो जाता है अथवा वसन्त संपात होने पर मधु मास का अन्त होता है तथा शरद् संपात होने पर इष मास का अन्त हो जाता है। इसी प्रकार जब विष्णु के सिर पर सूर्य दृष्टिगोचर होते हैं तब शुचि मास का अन्त होता है तथा जब विष्णु के पैर पर सूर्य दृष्टिगोचर होते हैं तब सहस्य मास का अन्त हो जाता है।
कथा के अनुसार मधु-कैटभ ने ब्रह्मा पर आक्रमण किया था अर्थात् मधु व कैटभ को मिलाने वाली रेखा ब्रह्म-स्थान से होकर जाती थी अर्थात् कैटभ की स्थिति मधु से १८०° पर थी अर्थात् कैटभ में इष का अन्त हो रहा था। अर्थात् वृष में मधु का अन्त हो रहा था। कथा के अनुसार कैटभ “विष्णुकर्णमलोद्भूत” (विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न) था। वस्तुत: यह विशेषण पाठान्तरित है। मौलिक पाठ “विष्णुकर्णमूलोद्भूत” है क्योंकि “कीट अथवा कैटभ” संज्ञा वृश्चिक राशि की है और वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र की उपाधि “कुड्य” अथवा “कर्णकुण्डल” है जिसकी पूर्व दिशा में मूल नक्षत्र है।
अत: मधु-कैटभ के विष्णुकर्णमूलोद्भूत होने का तात्पर्य हुआ कि “तब मूल नक्षत्र (निरयण रेखांश २४०° ४३’ ४३”) में इषान्त (शरद् संपात) होता था।” सम्प्रति कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण (निरयण रेखांश १५६° १८’ १३”) में इषान्त हो रहा है। अत: इस कथा में वर्णित स्थिति से अब तक चतुर्भुज के कर्ण का दायाँ सिरा मूल नक्षत्र से पश्चिम की ओर लगभग ८५° घूम चुका है। १° घूर्णन में लगभग ७१ वर्ष लगते हैं। तदनुसार ८५° घूर्णन में लगभग ६००० वर्ष लगे अर्थात् मधु-कैटभ की कथा लगभग ६००० वर्ष प्राचीन है।
इसी प्रकार लगभग १७०० वर्ष पूर्व दक्षिणायनगत सूर्य का “कुमारी” (कन्या) राशि में प्रवेश होने पर वे भारतवर्ष के दक्षिणतम बिन्दु (८° उत्तर) पर लम्बवत् होते थे जिसके कारण उक्त स्थान को “कुमारी तीर्थ” कहा गया। कुमारी तीर्थ का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में है। इसी प्रकार उत्तरायणान्त रेखा (२४° उत्तर) को “कर्क रेखा” कहे जाने का कारण भी यही है कि तब सूर्य के पृथ्वी की उत्तरायणान्त रेखा पर लम्बवत् होने पर आकाश में वे (सूर्य) कर्क राशि में प्रवेश करते थे। अत: खगोल व भूगोल के समन्वय के आधार पर निम्नोक्त अक्षांशों के १७०० वर्ष प्राचीन नाम दृष्टव्य हैं। २४° उत्तर = कर्क रेखा १६° उत्तर = मिथुन-सिंह रेखा ८° उत्तर = वृष-कन्या रेखा ०° = मेष-तुला रेखा ८° दक्षिण = मीन-वृश्चिक रेखा १६° दक्षिण = कुम्भ-धनु रेखा २४° दक्षिण = मकर रेखा पृथ्वी के उपर्युक्त ६ अक्षांशीय खण्डों को कूट रूप में “द्वादश-दल-कमल” द्वारा भी प्रकट किया जाता रहा है।
इसी प्रकार द्वादश-दल-कमल द्वादश ऋतुमासों को भी प्रकट करता है। इस द्वादश-दल-कमल के भीतर ऊर्ध्वमुख त्रिकोण व अधोमुख त्रिकोण का युग्म होता है। इस युग्म में छ: कोण होते हैं। इस युग्म के दो आसन्न कोणों के मध्य एक ऋतु अवस्थित होती है तथा केन्द्र में सूर्य (सौर-मण्डल)! लगभग २५८०० वर्षों में संपात-बिन्दु भचक्र की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं जिसे मन्वन्तर कहा जाता है। अत: १७०० वर्ष पूर्व ही नहीं अपितु लगभग २७५०० वर्ष पूर्व भी उत्तरायणान्त रेखा का नाम कर्क रेखा था और उसके भी लगभग २५८०० वर्ष पूर्व भी यही था। इसी प्रकार मधु-कैटभ की कथा ६००० वर्ष पूर्व ही नहीं अपितु ३१८०० वर्ष पूर्व के लिए भी सही है। इन दोनों और ऐसी ही अन्य अनेक बातों व कथाओं के विषय में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वे इसी मन्वन्तर की हैं अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य मन्वन्तर की। इसी कारण कहा गया है – मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्ग: संहार एव च। क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुन: पुन: ॥ (मनुस्मृति १-८०)
चित्रबोध हेतु संकेत
१. बाह्य वृत्त राशिचक्र अथवा भचक्र (zodiac) का द्योतक है जो ‘अचल’ है।
२. पृथ्वी से सूर्य की ओर देखने पर सूर्य की राशीय स्थित को जाना जा सकता है।
३. भचक्र के निकट बना वृत्त आदित्य-चक्र अथवा ऋतुमास-चक्र का द्योतक है जो ब्रह्म-स्थान के परित: पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन व परिक्रमण कर रही है। अत: किसी राशि का पश्चिमी शीर्ष उसका आरम्भ है तथा पूर्वी शीर्ष उसका अन्त।
४. आदित्य-चक्र के एक घूर्णन में २५८०० वर्ष लगते हैं जो पृथ्वी के अक्ष-डोलन पर आधारित है। यदि राशि का मध्यम मान भचक्र का ३०° माना जाय तो आदित्य-चक्र का कोई बिन्दु एक राशि को पार करने में प्राय: २१५० वर्ष लेता है।
५. पृथ्वी के अक्ष को उत्तर की ओर बढ़ा हुआ कल्पित करने पर वह आकाश में जिस बिन्दु को स्पर्श करता प्रतीत होता है वह “विष्णु का परमपद” कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष डोल रहा है जिससे उत्तरी ध्रुव द्वारा उत्तरी आकाश में एक काल्पनिक वृत्त बनता है। वर्तमान गति के अनुसार इस डोलन में २५८०० वर्ष लगते हैं।
इस वृत्त की परिधि के अतिनिकट ३ सुदृश्य तारे स्थित हैं – ध्रुव (Polaris), अभिजित् (Vega) व Deneb । ध्रुव व अभिजित् इस वृत्त की परिधि पर प्राय: आमने-सामने हैं। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जिस तारे के अतिनिकट आ जाता है वही तत्कालीन ध्रुवतारा कहलाता है। अर्थात् जिस तारे के अतिनिकट “विष्णु का परमपद” पड़ता है वही ध्रुवतारा कहलाता है।
दक्षिणी ध्रुव द्वारा दक्षिणी आकाश पर बनाए गए काल्पनिक वृत्त की परिधि के अतिनिकट प्राय: कोई सुदृश्य तारा नहीं है।
६. आदित्य-चक्र में बना चतुर्भुज उसी का एक भाग है।
७. भचक्र के सापेक्ष आदित्य-चक्र की चित्रित स्थिति १७०० वर्ष पूर्व की है जब मेष राशि के आरम्भ में मधु का अन्त अथवा सूर्य का उत्तरगोलारम्भ होता था। उत्तरगोलारम्भ वाली राशि को प्रथम राशि माना जाता है। अब मीन राशि के ६° में उत्तरगोलारम्भ हो रहा है। ५०० वर्ष उपरान्त कुम्भ राशि में उत्तरगोलारम्भ होने लगेगा।
८. कथा में वर्णित मधु की अपेक्षा चित्रगत मधु दो राशियाँ पार कर चुका है अर्थात् यह चित्र कथा से ४३०० वर्ष (२ × २१५० वर्ष) उपरान्त का है। इसमें १७०० वर्ष और जोड़ने पर ६००० वर्ष होते हैं। अस्तु , धर्मद्रोही यदि समझकर भी समझना न चाहें तो वे कह सकते हैं कि भारत नक्षत्रों को तो जानता था किन्तु राशियों को नहीं जानता था! किन्तु उन्हें कौन समझाए कि राशियाँ स्थूल हैं जबकि नक्षत्र सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म के ज्ञाता स्थूल को नहीं जानते थे, ऐसा आग्रह मूर्ख ही कर सकते हैं! भचक्र के जिस तारे के निकट एक पूर्णिमा होती है उससे पूर्व दिशा के किसी तारे के निकट अगली पूर्णिमा होती है। पहले तारे से दूसरे तारे तक के क्षेत्र का विस्तार ३०° से कुछ न्यून होता है। ऐसे १२ क्षेत्र अवश्य बनेंगे। इन्हीं क्षेत्रों से राशियों का उद्भव हुआ था। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् !
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.