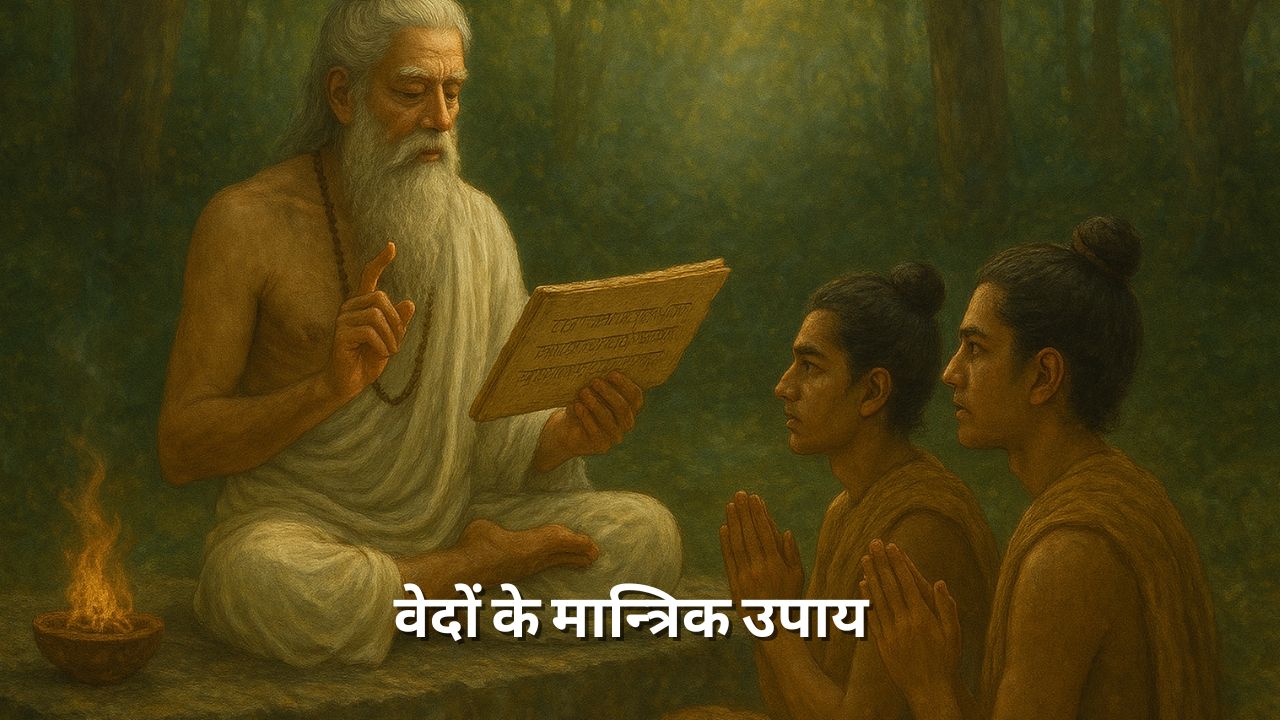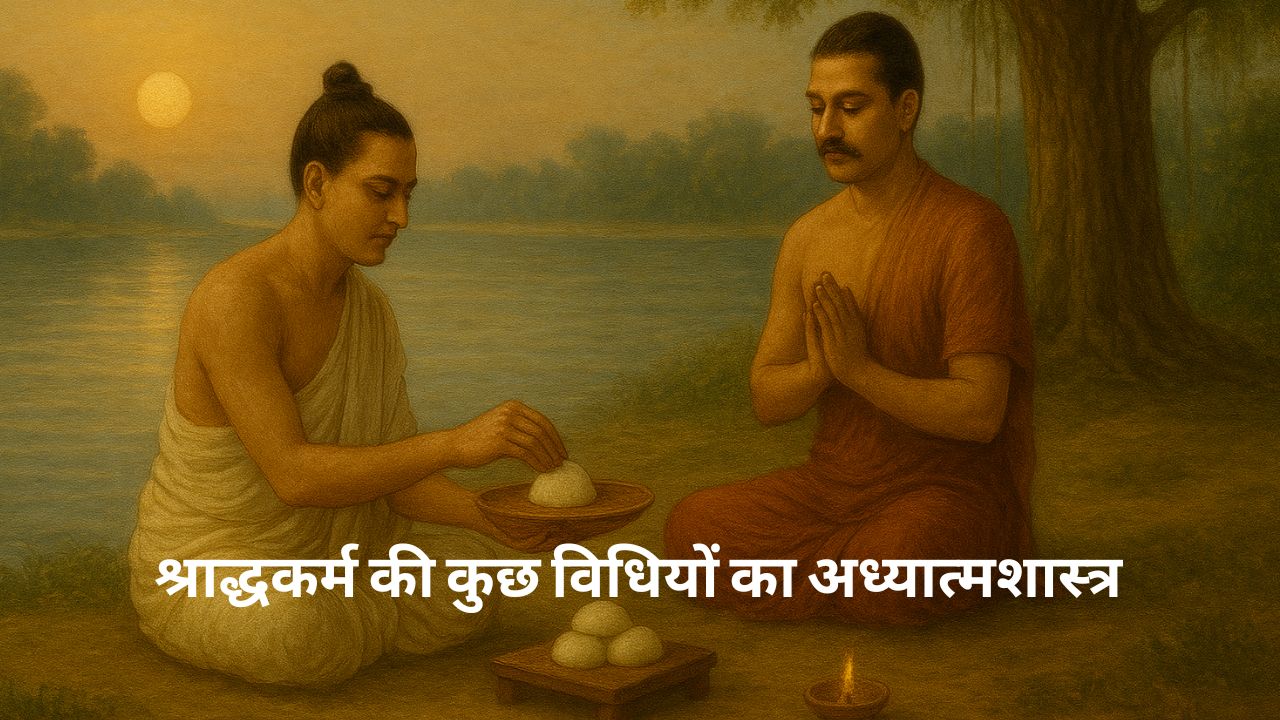- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
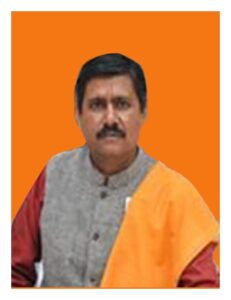 डॉ. दिलीप कुमार नाथाणी विद्यावाचस्पति-
Mystic power - पितृ विषय पर बहुत ही वाद—विवाद करते हुये हिन्दू धर्मद्रोहियों ने पितरों से सम्बन्धित वेद वचनों को भी मिथ्या करने का कुत्सित प्रयास किया है। वे सभी स्वयं केा वेद का संरक्षक, वेदवादी कहने वाले हैं। किसी म्लेच्छ ने ये दुराग्रह कभी नहीं किया उनको इससे कोई मतलब नहीं था। दुष्ट एव हठधर्मी तो हमारे ही भीतर हैं। किसी अन्य को कहने से क्या तात्पर्य, दुर्भाग्य है कि ऐसा कुत्सित कार्य किसी म्लेच्छ धर्मावलम्बियों ने नहीं वरन् स्वयं को वेदोपासक कहने वाले हमारे ही अन्तद्रोहियों वेद के स्वयम्भू ठेकेदारों का कुकर्म रहा है।
डॉ. दिलीप कुमार नाथाणी विद्यावाचस्पति-
Mystic power - पितृ विषय पर बहुत ही वाद—विवाद करते हुये हिन्दू धर्मद्रोहियों ने पितरों से सम्बन्धित वेद वचनों को भी मिथ्या करने का कुत्सित प्रयास किया है। वे सभी स्वयं केा वेद का संरक्षक, वेदवादी कहने वाले हैं। किसी म्लेच्छ ने ये दुराग्रह कभी नहीं किया उनको इससे कोई मतलब नहीं था। दुष्ट एव हठधर्मी तो हमारे ही भीतर हैं। किसी अन्य को कहने से क्या तात्पर्य, दुर्भाग्य है कि ऐसा कुत्सित कार्य किसी म्लेच्छ धर्मावलम्बियों ने नहीं वरन् स्वयं को वेदोपासक कहने वाले हमारे ही अन्तद्रोहियों वेद के स्वयम्भू ठेकेदारों का कुकर्म रहा है।
 आज से मेरा प्रयास रहेगा कि पितरों से सम्बन्धित वैदिक परम्परा को प्रमाणिक रूप से रखते हुये उसके वैदिक विज्ञान को समझाऊँ। इसके लिये परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय वेद वाचस्पति श्री मधुसूदन ओझा जी के द्वारा निरूपित वैदिक व्याख्या पद्धति का अनुसरण करते हुये उन्हीं के लेखन को सरलीकृत करके आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। उनकी दो अत्यन्त ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं *''पितृसमीक्षा'' एवं ''आशौच—पंजिका'' इन दोनों ही पुस्तकों में महामहोपाध्याय पण्डित मधुसूदन ओझा जी ने धर्म को वैदिक विज्ञान के सन्दर्भ में बहुत ही अच्छे से समझाया है। हम उन्हीं का ही अनुसरण करेंगे। साथ ही पण्डित मधुसूदन ओझा के पट्ट शिष्य पण्डितमोती लाल शास्त्री जी कि श्राद्ध विज्ञान के आधार पर इस आलेख का विस्तार करूँगा।
वेद विज्ञान के अनुसार ब्रह्म का वितान यानि विस्तार ही चराचर जगत् है। ब्रह्म का विकास पाँच प्रकार से होता है। यह विकास (1) ऋषिरूप, (2) पितृरूप, (3) देवरूप, (4) असुररूप, (5) गन्धर्वरूप। भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी ने गीता में पितृतत्व की स्थापना करते हुये स्वयं को जगत् का पिता पितामह बताते हुये कहा—
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामह:।
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च।। गीता 9.17
मैं इस जगत् का पिता हूँ। माता, धाता और पितामह भी मैं ही हूँ। जो सबसे पावन ज्ञेय (ब्रह्म) है ओमकार, ऋक्, साम और यजुष् भी में हूँ। अब यदि हमें पितरों के स्वरूप को जानना है तो मूल सत्ता के स्वरूप को, ऋषि एवं मनु के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा। इस विषय का वेद में सविस्तार प्रतिपादन भी किया गया है।
वेद का उद्घोष यही है कि आत्मा से मन, प्राण, इन्द्रियाँ एवं उनके विषयरूप में दिखाई देने वाले तीनों लोक उत्पन्न होते हैं, अतएव उस सच्चित्सुखस्वरूप आत्मा को जानने से सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को जानने लेने से उसमें से बने हुये विभिन्न आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के मूल आधार सच्चिदानंद आत्मा को जानने से सारी सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। उसी परम सत्ता से ही सभी का आविर्भाव हुआ है मुण्डकोपनिषत् में कहा है—
गता: कला: पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु।
भूतानि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति।। मुण्डकोपनिषत् 3.2.7
आदिपुरुष का सोलह कलाओं वाला शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होता है। यहाँ सूक्ष्म से तात्पर्य परिमाण या आकार में छोटा होना नहीं है सूक्ष्म से तात्पर्य है कि जो अत्यन्त अगम्य हो। हमारी भौतिक इन्द्रियों से जिसे नहीं जाना जा सके उसे ही सूक्ष्म कहते हैं। उस सोलह कला परिपूर्ण आदिपुरुष से यह आदि पुरुष आनन्द एवं विज्ञानात्मक है। इससे प्रथम तीन धाराएँ निकलती हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक। प्रथम धारा आधिदैविक धारा है जिसमें आनन्द तथा विज्ञान की स्थिति से आगे निकल कर प्राणनामक कला दिखाई देती है। यह प्राणात्मक ऊर्जा ही ऋषि व देवता के सूक्ष्म भावों में प्रकट होती है।
यह क्रम सतत् चलते हुये आकाश के गुण वाक् रूप में तथा आकाशादि पाँच महाभूतों व उनकी सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में परिणत होती है, उसे आधिभौतिक धारा कहा गया है। एवं इस आधिभौतिक धारा का बाह्यभ्यन्तर विस्तार ही आध्यात्मिक धारा कहा गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार असंख्य विराट् पिण्ड उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्राणी शरीर कहा जाता है। इन शरीर में जो रहता है, वह चैतन्य है उसे ईश्वर या जीव कहते हैं। इस प्रकार जितने भी ब्रह्माण्ड अथवा प्राणियों के शरीर रूप उत्पन्न होते हैं उन सबमें अव्यय, अक्षर एवं क्षर की कुल सोलह कलाएँ होती हैं। ये संक्षिप्त में ब्रह्म की एवं उसकी सृष्टि विकास के क्रम की व्याख्या यहाँ दी गई। अब इस आलेख का मूल विषय पितर है तो उस पर चर्चा करते हैं।
पितर एक प्राणात्मक तत्त्व है वेद में पितर का तात्पर्य केवल मात्र पूर्वज भाव नहीं है प्रेत, पितर आदि से अग्र अन्य भाव भी पितर है। इस सम्बन्ध में वेद के मंत्र प्रमाण स्वरूप हैं—
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा: पितर: सोम्यास:।
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो5वन्तु पितरो हवेषु।। ऋक् 10.1.1
प्रथम, मध्यम व उत्तम श्रेणि के पितर हमारे लिये सौम्य (अनुग्रह करने वाले) बनते हुये हमारी उन्नति का कारण बनें। ऋतु को पहचानने वाले अहिंसकर पितर प्राण प्रदाता हैं। ऐसे वे पितर हमारी प्रार्थना सुनें, हमारी रक्षा करें।
इस मंत्र से यह अर्थ निकलता है कि पितर, कोई तत्त्व विशेष है, प्राणविशेष है। पितर प्राण का सोम तत्त्व से सम्बन्ध है। साथ ही में यह तत्त्व प्राणशक्ति का प्रदाता है। यहाँ कोर्इ् पितर शब्द से जीवित पिता आदि अर्थ लगाता है तो उनमें प्रथम—मध्यम—उत्तम इस प्रकार कर लौकिक श्रेणिविभाग करना असंगत है।
प्राणशक्ति के रूप में पितरों का वर्णन—
त इद्देवानां सधमाद आसनृतावान: कवय: पूर्व्यास:।
गूलहं ज्योति: पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजयन्नुषासम्।। ऋक् 7.76.4
ऋत मार्ग के अनुयायी, भृगुवंशी पूर्वकालिक वे अंगिरा नाम के पितर ही देवताओं के साथ प्रेम करने में समर्थ हुये। गुहानिहित ज्येाति अर्थात् सूर्य को इन्होंने ही प्रकट किया। सत्यब्रह्म के उपासक, किंवा सत्यमंत्र मूर्त्ति इन पितरों ने ही उषा को उत्पन्न किया। पुन: इस मंत्र में प्रकाश उषा आदि तत्त्व प्राकृति है जो पितर इन प्राकृति तत्त्वों के उत्पादक माने हैं उनका जीवित पितरों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। अवश्य ही पितर प्राण आधिदैविक जगत् की कोई विशेष एवं मौलिक प्राणात्मक तत्त्व विशेष है।
सरस्वति या सरथं यथाथ स्वधामिर्देवि पितृभिर्मदन्ती।
आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा इष आधेह्यस्मै। ऋक् 10.17.8
पितरों के साथ रथ पर आरूढ होती हुई एवं स्वधा नामक अन्न से मोदमान होती हुई सरस्वती देवी! इस यज्ञ में विराजमान होकर आप प्रसन्नमूर्त्ति बनिए, हमें एवं हमारे अन्नों को निर्दोष कीजिये।
इस मंत्र में सरस्वती नाम की वाग् देवता के साथ पितरों का सम्बन्ध बतलाया है। परमेष्ठी के सरस्वान् समुद्र से ही इस सरस्वती वाक् का विनिर्गम है। उसी सौम्य परमेष्ठी मण्डल में सौम्य प्राणरूप पितरतत्त्व प्रतिष्ठित है। ऐसी स्थिति में पितर शब्द पितादि परक मानना शास्त्रसम्मत कदापि नहीं है।
प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्दैवै: पितृभि: संविदान:।
शिवा: सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया संमदेम।। ऋक् 10,169.4।।
विश्वेदेव नाम पारमेष्ठ्य देवता, एवं पितरों के साथ संयुक्त होते हुये प्रजापति (परमेष्ठी) मेरे लिये गौसंपत्ति प्रदान करते हैं। वह प्रजापति देवता कल्याकारिणी बनती हुई, उन गायों को हमारे गोस्थान के सन्निकट करें, एवं उन गौसंतानओं से अर्थात् गोवंश से हमें प्रसन्न करे।
स्पष्ट रूप से सर्वविदित है कि सोम परमेष्ठी की ही वस्तु है। विश्वेदेव एवं पितरा दोनों ही प्राणों की प्रत्तिष्ठा सौम्य परमेष्ठी ही है। परमेष्ठी ही सहस्रा विभक्त होकर गोतत्त्व उत्पन्न होता है। इसी गौप्रवर्त्तक पारमेष्ठ्य सौम्य प्राण को पितर शब्द से संबोधित किया गया है।
आज से मेरा प्रयास रहेगा कि पितरों से सम्बन्धित वैदिक परम्परा को प्रमाणिक रूप से रखते हुये उसके वैदिक विज्ञान को समझाऊँ। इसके लिये परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय वेद वाचस्पति श्री मधुसूदन ओझा जी के द्वारा निरूपित वैदिक व्याख्या पद्धति का अनुसरण करते हुये उन्हीं के लेखन को सरलीकृत करके आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। उनकी दो अत्यन्त ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं *''पितृसमीक्षा'' एवं ''आशौच—पंजिका'' इन दोनों ही पुस्तकों में महामहोपाध्याय पण्डित मधुसूदन ओझा जी ने धर्म को वैदिक विज्ञान के सन्दर्भ में बहुत ही अच्छे से समझाया है। हम उन्हीं का ही अनुसरण करेंगे। साथ ही पण्डित मधुसूदन ओझा के पट्ट शिष्य पण्डितमोती लाल शास्त्री जी कि श्राद्ध विज्ञान के आधार पर इस आलेख का विस्तार करूँगा।
वेद विज्ञान के अनुसार ब्रह्म का वितान यानि विस्तार ही चराचर जगत् है। ब्रह्म का विकास पाँच प्रकार से होता है। यह विकास (1) ऋषिरूप, (2) पितृरूप, (3) देवरूप, (4) असुररूप, (5) गन्धर्वरूप। भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी ने गीता में पितृतत्व की स्थापना करते हुये स्वयं को जगत् का पिता पितामह बताते हुये कहा—
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामह:।
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च।। गीता 9.17
मैं इस जगत् का पिता हूँ। माता, धाता और पितामह भी मैं ही हूँ। जो सबसे पावन ज्ञेय (ब्रह्म) है ओमकार, ऋक्, साम और यजुष् भी में हूँ। अब यदि हमें पितरों के स्वरूप को जानना है तो मूल सत्ता के स्वरूप को, ऋषि एवं मनु के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा। इस विषय का वेद में सविस्तार प्रतिपादन भी किया गया है।
वेद का उद्घोष यही है कि आत्मा से मन, प्राण, इन्द्रियाँ एवं उनके विषयरूप में दिखाई देने वाले तीनों लोक उत्पन्न होते हैं, अतएव उस सच्चित्सुखस्वरूप आत्मा को जानने से सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को जानने लेने से उसमें से बने हुये विभिन्न आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के मूल आधार सच्चिदानंद आत्मा को जानने से सारी सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। उसी परम सत्ता से ही सभी का आविर्भाव हुआ है मुण्डकोपनिषत् में कहा है—
गता: कला: पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु।
भूतानि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति।। मुण्डकोपनिषत् 3.2.7
आदिपुरुष का सोलह कलाओं वाला शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होता है। यहाँ सूक्ष्म से तात्पर्य परिमाण या आकार में छोटा होना नहीं है सूक्ष्म से तात्पर्य है कि जो अत्यन्त अगम्य हो। हमारी भौतिक इन्द्रियों से जिसे नहीं जाना जा सके उसे ही सूक्ष्म कहते हैं। उस सोलह कला परिपूर्ण आदिपुरुष से यह आदि पुरुष आनन्द एवं विज्ञानात्मक है। इससे प्रथम तीन धाराएँ निकलती हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक। प्रथम धारा आधिदैविक धारा है जिसमें आनन्द तथा विज्ञान की स्थिति से आगे निकल कर प्राणनामक कला दिखाई देती है। यह प्राणात्मक ऊर्जा ही ऋषि व देवता के सूक्ष्म भावों में प्रकट होती है।
यह क्रम सतत् चलते हुये आकाश के गुण वाक् रूप में तथा आकाशादि पाँच महाभूतों व उनकी सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में परिणत होती है, उसे आधिभौतिक धारा कहा गया है। एवं इस आधिभौतिक धारा का बाह्यभ्यन्तर विस्तार ही आध्यात्मिक धारा कहा गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार असंख्य विराट् पिण्ड उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्राणी शरीर कहा जाता है। इन शरीर में जो रहता है, वह चैतन्य है उसे ईश्वर या जीव कहते हैं। इस प्रकार जितने भी ब्रह्माण्ड अथवा प्राणियों के शरीर रूप उत्पन्न होते हैं उन सबमें अव्यय, अक्षर एवं क्षर की कुल सोलह कलाएँ होती हैं। ये संक्षिप्त में ब्रह्म की एवं उसकी सृष्टि विकास के क्रम की व्याख्या यहाँ दी गई। अब इस आलेख का मूल विषय पितर है तो उस पर चर्चा करते हैं।
पितर एक प्राणात्मक तत्त्व है वेद में पितर का तात्पर्य केवल मात्र पूर्वज भाव नहीं है प्रेत, पितर आदि से अग्र अन्य भाव भी पितर है। इस सम्बन्ध में वेद के मंत्र प्रमाण स्वरूप हैं—
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा: पितर: सोम्यास:।
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो5वन्तु पितरो हवेषु।। ऋक् 10.1.1
प्रथम, मध्यम व उत्तम श्रेणि के पितर हमारे लिये सौम्य (अनुग्रह करने वाले) बनते हुये हमारी उन्नति का कारण बनें। ऋतु को पहचानने वाले अहिंसकर पितर प्राण प्रदाता हैं। ऐसे वे पितर हमारी प्रार्थना सुनें, हमारी रक्षा करें।
इस मंत्र से यह अर्थ निकलता है कि पितर, कोई तत्त्व विशेष है, प्राणविशेष है। पितर प्राण का सोम तत्त्व से सम्बन्ध है। साथ ही में यह तत्त्व प्राणशक्ति का प्रदाता है। यहाँ कोर्इ् पितर शब्द से जीवित पिता आदि अर्थ लगाता है तो उनमें प्रथम—मध्यम—उत्तम इस प्रकार कर लौकिक श्रेणिविभाग करना असंगत है।
प्राणशक्ति के रूप में पितरों का वर्णन—
त इद्देवानां सधमाद आसनृतावान: कवय: पूर्व्यास:।
गूलहं ज्योति: पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजयन्नुषासम्।। ऋक् 7.76.4
ऋत मार्ग के अनुयायी, भृगुवंशी पूर्वकालिक वे अंगिरा नाम के पितर ही देवताओं के साथ प्रेम करने में समर्थ हुये। गुहानिहित ज्येाति अर्थात् सूर्य को इन्होंने ही प्रकट किया। सत्यब्रह्म के उपासक, किंवा सत्यमंत्र मूर्त्ति इन पितरों ने ही उषा को उत्पन्न किया। पुन: इस मंत्र में प्रकाश उषा आदि तत्त्व प्राकृति है जो पितर इन प्राकृति तत्त्वों के उत्पादक माने हैं उनका जीवित पितरों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। अवश्य ही पितर प्राण आधिदैविक जगत् की कोई विशेष एवं मौलिक प्राणात्मक तत्त्व विशेष है।
सरस्वति या सरथं यथाथ स्वधामिर्देवि पितृभिर्मदन्ती।
आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा इष आधेह्यस्मै। ऋक् 10.17.8
पितरों के साथ रथ पर आरूढ होती हुई एवं स्वधा नामक अन्न से मोदमान होती हुई सरस्वती देवी! इस यज्ञ में विराजमान होकर आप प्रसन्नमूर्त्ति बनिए, हमें एवं हमारे अन्नों को निर्दोष कीजिये।
इस मंत्र में सरस्वती नाम की वाग् देवता के साथ पितरों का सम्बन्ध बतलाया है। परमेष्ठी के सरस्वान् समुद्र से ही इस सरस्वती वाक् का विनिर्गम है। उसी सौम्य परमेष्ठी मण्डल में सौम्य प्राणरूप पितरतत्त्व प्रतिष्ठित है। ऐसी स्थिति में पितर शब्द पितादि परक मानना शास्त्रसम्मत कदापि नहीं है।
प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्दैवै: पितृभि: संविदान:।
शिवा: सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया संमदेम।। ऋक् 10,169.4।।
विश्वेदेव नाम पारमेष्ठ्य देवता, एवं पितरों के साथ संयुक्त होते हुये प्रजापति (परमेष्ठी) मेरे लिये गौसंपत्ति प्रदान करते हैं। वह प्रजापति देवता कल्याकारिणी बनती हुई, उन गायों को हमारे गोस्थान के सन्निकट करें, एवं उन गौसंतानओं से अर्थात् गोवंश से हमें प्रसन्न करे।
स्पष्ट रूप से सर्वविदित है कि सोम परमेष्ठी की ही वस्तु है। विश्वेदेव एवं पितरा दोनों ही प्राणों की प्रत्तिष्ठा सौम्य परमेष्ठी ही है। परमेष्ठी ही सहस्रा विभक्त होकर गोतत्त्व उत्पन्न होता है। इसी गौप्रवर्त्तक पारमेष्ठ्य सौम्य प्राण को पितर शब्द से संबोधित किया गया है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.