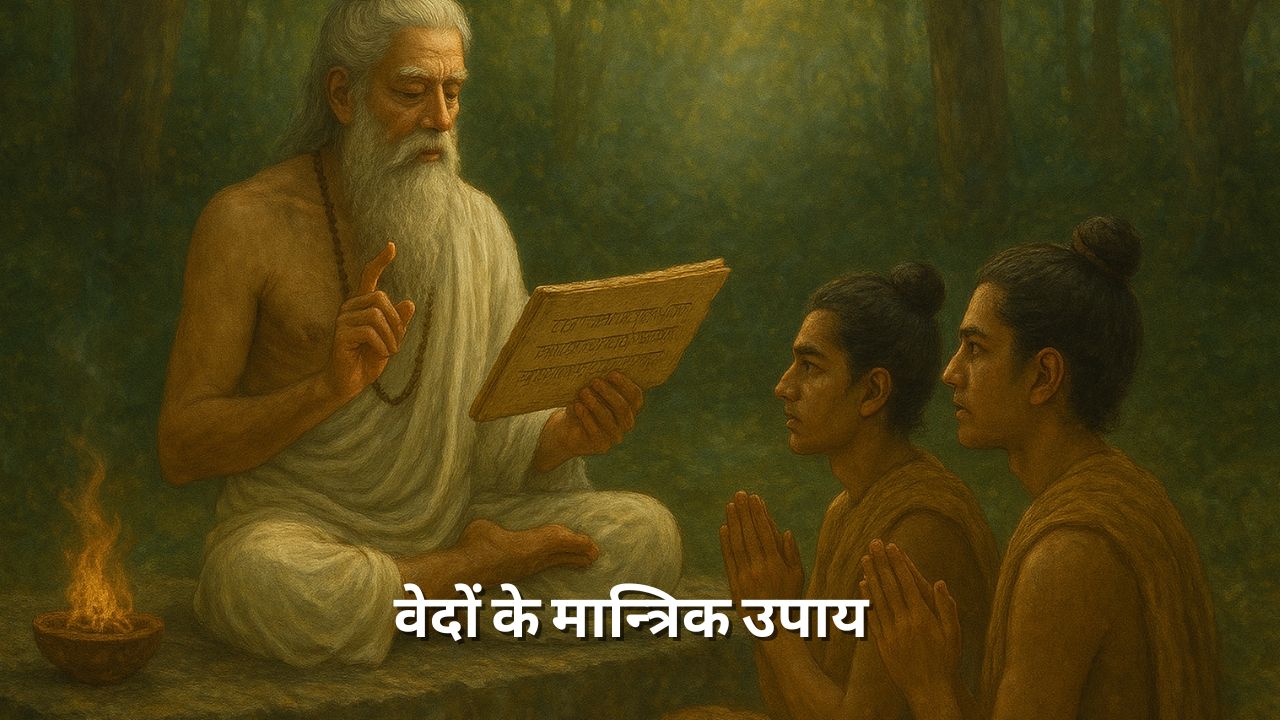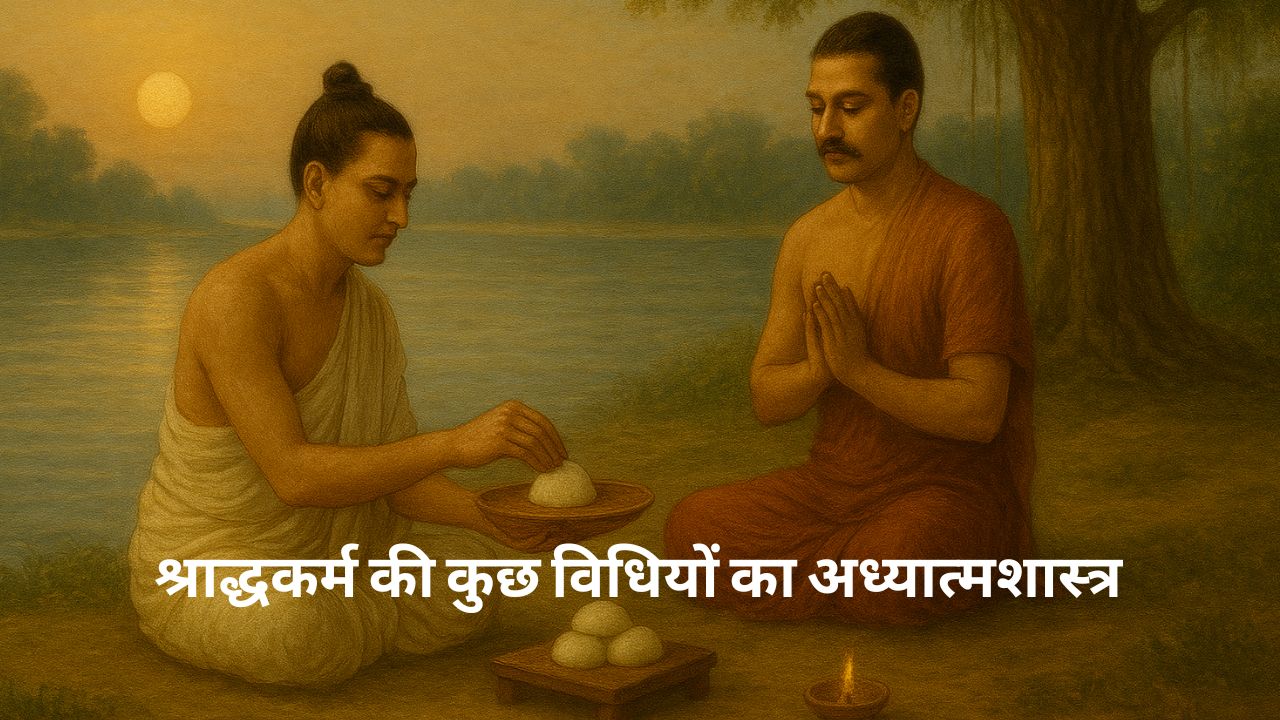- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 डॉ. दीनदयाल मणि त्रिपाठी (प्रबंध संपादक)- लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर श्रीकृष्ण का सम्पूर्ण ‘जीवन चरित्र’ अनेक अद्भुत और दिव्य कथाओं से परिपूर्ण है, तथापि उनके बालजीवन की कथाएँ ‘लालित्य से परिपूर्ण एवं प्रतिबोधात्मक’ रूप में विश्रुत हैं। अतः विविध बाललीलाओं और ‘गीता ज्ञानोपदेश’ के आधारपर उन्हें जन-जन द्वारा स्मरण किया जाता है । बोध भरे मनोरंजन हेतु लोकजीवन में स्मृत है ।
भारतीय दार्शनिक मान्यता में श्रीकृष्ण को ‘पूर्णब्रह्म’ जाना गया है । उन्हें ‘षोडशकला पुरुष’ कहा गया है । अतः उनका सम्पूर्ण जीवन-चरित्र इस जगत के धारणकर्ता रह्स्य को प्रकट करने वाला है । अतः चिरस्मृति का आधार बना हुआ है । भारतीय धार्मिक मान्यताओं में एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण जीवन-चरित्र “सगुण ब्रह्म” श्रीराम का है, जिन्हें “मर्यादा पुरुषोत्तम” रूप में जाना गया है ।
सगुणब्रह्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ‘जीवन-चरित्र’ जहाँ युवामानस् और विवाहित जीवन के लिये आदर्श माना जाकर भारतीय जीवन का नियमन करने वाला बना हुआ है, वहीं पूर्णब्रह्म, षोडशकला पुरुष, योगेश्वर श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र अपनी विविध बाल लीलाओं और ‘गीताज्ञानोपदेश’ तथा ‘महाभारत युद्ध’ में नेतृत्व के आधार पर प्रमुखता लिये हुए है । मनीषी पुरुषों के लिये विचार करने हेतु यह विपुल सामग्री लिये हुए है । इस प्रकार ये दोनों ही जीवन-चरित्र ‘भारतीय-जीवन-पद्धति’ का नियमन करने वाले हो गये हैं ।
ये बालमन के मनोरंजन, युवामन के लिये कर्म का आदर्श, विवाहित जीवन के लिये संयम और प्रोढ़मन के लिये विचार की विपुल सामग्री प्रदान करनेवाले हो गये हैं । ये इस जगत् में ‘शिक्षा प्राप्ति’ का आधार और ‘कर्म का आदर्श’ प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण जीवन के लिये आदर्शरूप हो गये हैं ।
भारतीय ज्ञान परम्परा में ‘सगुणब्रह्म श्रीराम’ का जीवन-चरित्र ‘धर्म के पालनकर्ता’ का प्रकट रूप है’ । अतः उन्हें ‘धर्म का मूर्तिमान स्वरूप’ जाना गया है – *“रामो विग्रहवान्धर्मः ।”* तथा श्रीकृष्ण का ‘जीवन’ लीलामय है, उन्हें ‘योगेश्वर’ कहा गया है । अतः उनका जीवन-चरित्र इस ‘जगत के धारणकर्ता रहस्य’ को प्रकट करने के साथ-साथ ‘योगमार्ग’ को प्रकट करने वाला हो गया है तथा उनके बालजीवन से जुडी हुई घटनाएँ ‘योग-क्रिया’ आधारित ‘साधना मार्ग’ को प्रकट करने वाली हो गयी हैं; शिक्षारूप हो गयी हैं ।
ये ‘बालकथाएँ’ आख्यान रूप में प्रतीकार्थ को धारण करने वाली तथा ‘लौकिक जीवन’ में मार्गबोध प्रदान करने वाली होना जानी गयी हैं । ये बालकथाएँ भारतीय लोकजीवन में ‘अबोध बालमन’ के लिये तो मनोरंजन करने वाली किंतु अध्यात्म प्रेमी विज्ञजनों के लिये जागतिक जीवन में दिशा-निर्देश प्रदान करने वाली हो गयी हैं । ‘ज्ञान के आलोक’ में ये ‘जीवनपथ’ को आलोकित करने वाली और ‘योग-शिक्षा’ का आधार होना जानी गयी हैं ।
अतः लौकिक जीवन की आपाधापी में योगेश्वर श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का ‘कथा रहस्य’ जानने हेतु प्रथमतः हमारे द्वारा यह जान लेना आवश्योक है कि उपनिषद्वाणी में श्रुति ‘वय’ अर्थात् ‘आयु’ को ‘ज्येष्ठता’ या ‘प्रोढ़ता’ का आधार मानती नहीं है । श्रुति तो ‘अपरा विद्या’ और ‘परा विद्या’ के भेद आधार पर ‘अपरा विद्या’ में पारंगत व्यक्ति के लिये “बालाः” सम्बोधन को अपनाती है । उसे वयस्क होने पर भी ‘बालबुद्धि’ को धारण करने वाला कथन करती है – *“अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: ।”* (मुण्ड.उप. 1.2.9)
अर्थात् –
“अविद्या अर्थात् ‘अपरा विद्या’ में स्थित रहकर बहुत प्रकार से (भलीभांति) आचरण करने वाले जो पुरुष स्वयं को कृतार्थ मान लेते हैं, (अर्थात् स्वयं को विद्वान् होना मान लेते हैं) वे तो बालकों के सदृश, बालबुद्धि को धारण करने वाले होते हैं ।”
‘अपरा विद्या’ (अविद्या) में स्वयं को पारंगत (विद्वान्) मान लेना या ‘इतना ही ज्ञान है’ यह मान लेना तो मूर्खता को अपनाना होता है । (कठ.उप. १.२.५) अतः जो लोग ‘परा विद्या’ को जानने वाले या वेदऋचा के ‘छन्द रहस्य’ को जानने वाले हैं, अर्थात् जो वेदऋचा के ‘ऋषि संदेश’ को जानते हैं, उन्हें ही “ज्येष्ठ” होना कथन करती है, उन्हें ‘प्रोढ़’ (= ज्येष्ठ और श्रेष्ठ) मानती है, फिर भले ही वह ‘अल्पायु’ अथवा ‘वय’ में छोटा ही क्यों न हो । अतः श्रीमद्भागवतपुराण में महर्षि वेदव्यास का वचन है कि – “वेदज्ञान को छोड़कर केवल आयु का अधिक होना ही किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का कारण नहीं है । ” – “छन्दोरभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्यैष्ठस्य कारणम् ।” (श्रीमद्भागवत 6.7.33) इस प्रकार वैदिक ऋचा-छन्द के ‘ऋषि सन्देश’ का बोध प्राप्त कर लेना ही इस जगत में ज्येष्ठता का एकमेव आधार अथवा कारण होता है ।
इस मानव जीवन में बोध प्राप्ति हेतु वेदवाणी में श्रुति कथन आया है कि – “इस लोक में ‘बोध’ एवं ‘प्रतिबोध’ नाम के ‘दो ऋषि’ हैं । वे दोनों ही दिवस और रात्री में सब लोगों के लिये बोध प्राप्ति का आधार एवं प्राणों की रक्षा करने वाले हैं ।” :-
*ऋषी बोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्चा जागृविः ।*
*तौ ते प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तं च जागृताम्॥ (अथर्ववेद 5.30.10)*
अर्थात् – “बोध और प्रतिबोध नाम के दो ऋषि हैं; वे स्वप्नावस्था में तथा जो जागृत अवस्था है उसमें (अर्थात् ‘अहोरात्र’ आधारित इस सृष्टिचक्र में रात और दिन आधारित जो उभयरूप अवस्था है, उसमें) वे संतुष्ट करने वाले हैं । वे दोनों ही तुम सब लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले रात में और दिन में जागते रहें (अर्थात् हम सब लोग इन दोनों को अपनाने वाले बने रहें) ।”
इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बोधावस्था को अपनाकर जीवनयापन करने वाला होता है । वह अपनी बोधावस्था के अनुसार ही आचरण करता और परस्पर जागतिक व्यवहार को अपनाता है । तथा जागतिक व्यवहार के आधारपर ही कोई व्यक्ति इस जगत में सुख या दुःख, मित्रता या विरोध, प्रसन्न्ता या क्लेश आधारित चित्त की स्वस्थ या अस्वस्थ अवस्था को प्राप्त करने वाला हो जाता है तथा इनके अनुसार ही वह दीर्घायु या अल्पायु को प्राप्त करने वाला जाना जाता है । अतः किसी भी व्यक्ति के लेये उसके द्वारा धारण की गयी बोधावस्था ही सुख-दुःख की प्राप्ति और अल्पायु या दीर्घ जीवन का कारण होती है । यह लोकसम्मान का आधार बनाती है ।
डॉ. दीनदयाल मणि त्रिपाठी (प्रबंध संपादक)- लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर श्रीकृष्ण का सम्पूर्ण ‘जीवन चरित्र’ अनेक अद्भुत और दिव्य कथाओं से परिपूर्ण है, तथापि उनके बालजीवन की कथाएँ ‘लालित्य से परिपूर्ण एवं प्रतिबोधात्मक’ रूप में विश्रुत हैं। अतः विविध बाललीलाओं और ‘गीता ज्ञानोपदेश’ के आधारपर उन्हें जन-जन द्वारा स्मरण किया जाता है । बोध भरे मनोरंजन हेतु लोकजीवन में स्मृत है ।
भारतीय दार्शनिक मान्यता में श्रीकृष्ण को ‘पूर्णब्रह्म’ जाना गया है । उन्हें ‘षोडशकला पुरुष’ कहा गया है । अतः उनका सम्पूर्ण जीवन-चरित्र इस जगत के धारणकर्ता रह्स्य को प्रकट करने वाला है । अतः चिरस्मृति का आधार बना हुआ है । भारतीय धार्मिक मान्यताओं में एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण जीवन-चरित्र “सगुण ब्रह्म” श्रीराम का है, जिन्हें “मर्यादा पुरुषोत्तम” रूप में जाना गया है ।
सगुणब्रह्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ‘जीवन-चरित्र’ जहाँ युवामानस् और विवाहित जीवन के लिये आदर्श माना जाकर भारतीय जीवन का नियमन करने वाला बना हुआ है, वहीं पूर्णब्रह्म, षोडशकला पुरुष, योगेश्वर श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र अपनी विविध बाल लीलाओं और ‘गीताज्ञानोपदेश’ तथा ‘महाभारत युद्ध’ में नेतृत्व के आधार पर प्रमुखता लिये हुए है । मनीषी पुरुषों के लिये विचार करने हेतु यह विपुल सामग्री लिये हुए है । इस प्रकार ये दोनों ही जीवन-चरित्र ‘भारतीय-जीवन-पद्धति’ का नियमन करने वाले हो गये हैं ।
ये बालमन के मनोरंजन, युवामन के लिये कर्म का आदर्श, विवाहित जीवन के लिये संयम और प्रोढ़मन के लिये विचार की विपुल सामग्री प्रदान करनेवाले हो गये हैं । ये इस जगत् में ‘शिक्षा प्राप्ति’ का आधार और ‘कर्म का आदर्श’ प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण जीवन के लिये आदर्शरूप हो गये हैं ।
भारतीय ज्ञान परम्परा में ‘सगुणब्रह्म श्रीराम’ का जीवन-चरित्र ‘धर्म के पालनकर्ता’ का प्रकट रूप है’ । अतः उन्हें ‘धर्म का मूर्तिमान स्वरूप’ जाना गया है – *“रामो विग्रहवान्धर्मः ।”* तथा श्रीकृष्ण का ‘जीवन’ लीलामय है, उन्हें ‘योगेश्वर’ कहा गया है । अतः उनका जीवन-चरित्र इस ‘जगत के धारणकर्ता रहस्य’ को प्रकट करने के साथ-साथ ‘योगमार्ग’ को प्रकट करने वाला हो गया है तथा उनके बालजीवन से जुडी हुई घटनाएँ ‘योग-क्रिया’ आधारित ‘साधना मार्ग’ को प्रकट करने वाली हो गयी हैं; शिक्षारूप हो गयी हैं ।
ये ‘बालकथाएँ’ आख्यान रूप में प्रतीकार्थ को धारण करने वाली तथा ‘लौकिक जीवन’ में मार्गबोध प्रदान करने वाली होना जानी गयी हैं । ये बालकथाएँ भारतीय लोकजीवन में ‘अबोध बालमन’ के लिये तो मनोरंजन करने वाली किंतु अध्यात्म प्रेमी विज्ञजनों के लिये जागतिक जीवन में दिशा-निर्देश प्रदान करने वाली हो गयी हैं । ‘ज्ञान के आलोक’ में ये ‘जीवनपथ’ को आलोकित करने वाली और ‘योग-शिक्षा’ का आधार होना जानी गयी हैं ।
अतः लौकिक जीवन की आपाधापी में योगेश्वर श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का ‘कथा रहस्य’ जानने हेतु प्रथमतः हमारे द्वारा यह जान लेना आवश्योक है कि उपनिषद्वाणी में श्रुति ‘वय’ अर्थात् ‘आयु’ को ‘ज्येष्ठता’ या ‘प्रोढ़ता’ का आधार मानती नहीं है । श्रुति तो ‘अपरा विद्या’ और ‘परा विद्या’ के भेद आधार पर ‘अपरा विद्या’ में पारंगत व्यक्ति के लिये “बालाः” सम्बोधन को अपनाती है । उसे वयस्क होने पर भी ‘बालबुद्धि’ को धारण करने वाला कथन करती है – *“अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: ।”* (मुण्ड.उप. 1.2.9)
अर्थात् –
“अविद्या अर्थात् ‘अपरा विद्या’ में स्थित रहकर बहुत प्रकार से (भलीभांति) आचरण करने वाले जो पुरुष स्वयं को कृतार्थ मान लेते हैं, (अर्थात् स्वयं को विद्वान् होना मान लेते हैं) वे तो बालकों के सदृश, बालबुद्धि को धारण करने वाले होते हैं ।”
‘अपरा विद्या’ (अविद्या) में स्वयं को पारंगत (विद्वान्) मान लेना या ‘इतना ही ज्ञान है’ यह मान लेना तो मूर्खता को अपनाना होता है । (कठ.उप. १.२.५) अतः जो लोग ‘परा विद्या’ को जानने वाले या वेदऋचा के ‘छन्द रहस्य’ को जानने वाले हैं, अर्थात् जो वेदऋचा के ‘ऋषि संदेश’ को जानते हैं, उन्हें ही “ज्येष्ठ” होना कथन करती है, उन्हें ‘प्रोढ़’ (= ज्येष्ठ और श्रेष्ठ) मानती है, फिर भले ही वह ‘अल्पायु’ अथवा ‘वय’ में छोटा ही क्यों न हो । अतः श्रीमद्भागवतपुराण में महर्षि वेदव्यास का वचन है कि – “वेदज्ञान को छोड़कर केवल आयु का अधिक होना ही किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का कारण नहीं है । ” – “छन्दोरभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्यैष्ठस्य कारणम् ।” (श्रीमद्भागवत 6.7.33) इस प्रकार वैदिक ऋचा-छन्द के ‘ऋषि सन्देश’ का बोध प्राप्त कर लेना ही इस जगत में ज्येष्ठता का एकमेव आधार अथवा कारण होता है ।
इस मानव जीवन में बोध प्राप्ति हेतु वेदवाणी में श्रुति कथन आया है कि – “इस लोक में ‘बोध’ एवं ‘प्रतिबोध’ नाम के ‘दो ऋषि’ हैं । वे दोनों ही दिवस और रात्री में सब लोगों के लिये बोध प्राप्ति का आधार एवं प्राणों की रक्षा करने वाले हैं ।” :-
*ऋषी बोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्चा जागृविः ।*
*तौ ते प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तं च जागृताम्॥ (अथर्ववेद 5.30.10)*
अर्थात् – “बोध और प्रतिबोध नाम के दो ऋषि हैं; वे स्वप्नावस्था में तथा जो जागृत अवस्था है उसमें (अर्थात् ‘अहोरात्र’ आधारित इस सृष्टिचक्र में रात और दिन आधारित जो उभयरूप अवस्था है, उसमें) वे संतुष्ट करने वाले हैं । वे दोनों ही तुम सब लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले रात में और दिन में जागते रहें (अर्थात् हम सब लोग इन दोनों को अपनाने वाले बने रहें) ।”
इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बोधावस्था को अपनाकर जीवनयापन करने वाला होता है । वह अपनी बोधावस्था के अनुसार ही आचरण करता और परस्पर जागतिक व्यवहार को अपनाता है । तथा जागतिक व्यवहार के आधारपर ही कोई व्यक्ति इस जगत में सुख या दुःख, मित्रता या विरोध, प्रसन्न्ता या क्लेश आधारित चित्त की स्वस्थ या अस्वस्थ अवस्था को प्राप्त करने वाला हो जाता है तथा इनके अनुसार ही वह दीर्घायु या अल्पायु को प्राप्त करने वाला जाना जाता है । अतः किसी भी व्यक्ति के लेये उसके द्वारा धारण की गयी बोधावस्था ही सुख-दुःख की प्राप्ति और अल्पायु या दीर्घ जीवन का कारण होती है । यह लोकसम्मान का आधार बनाती है ।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.