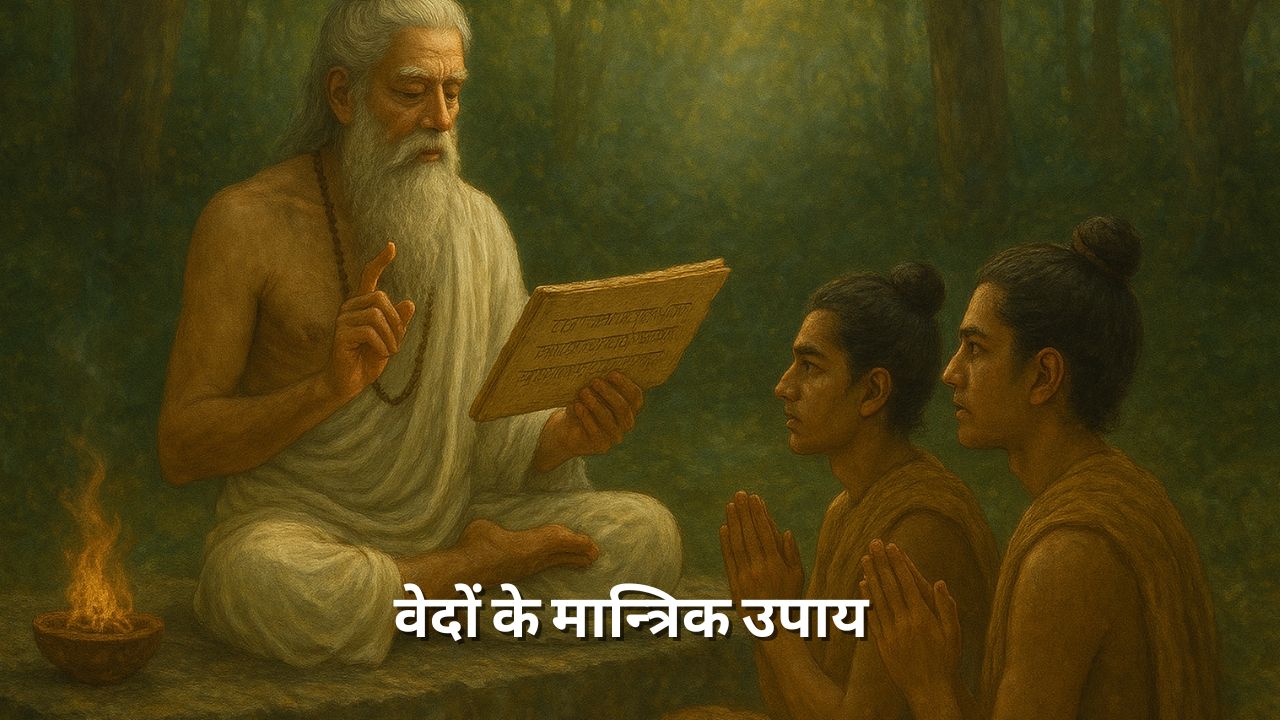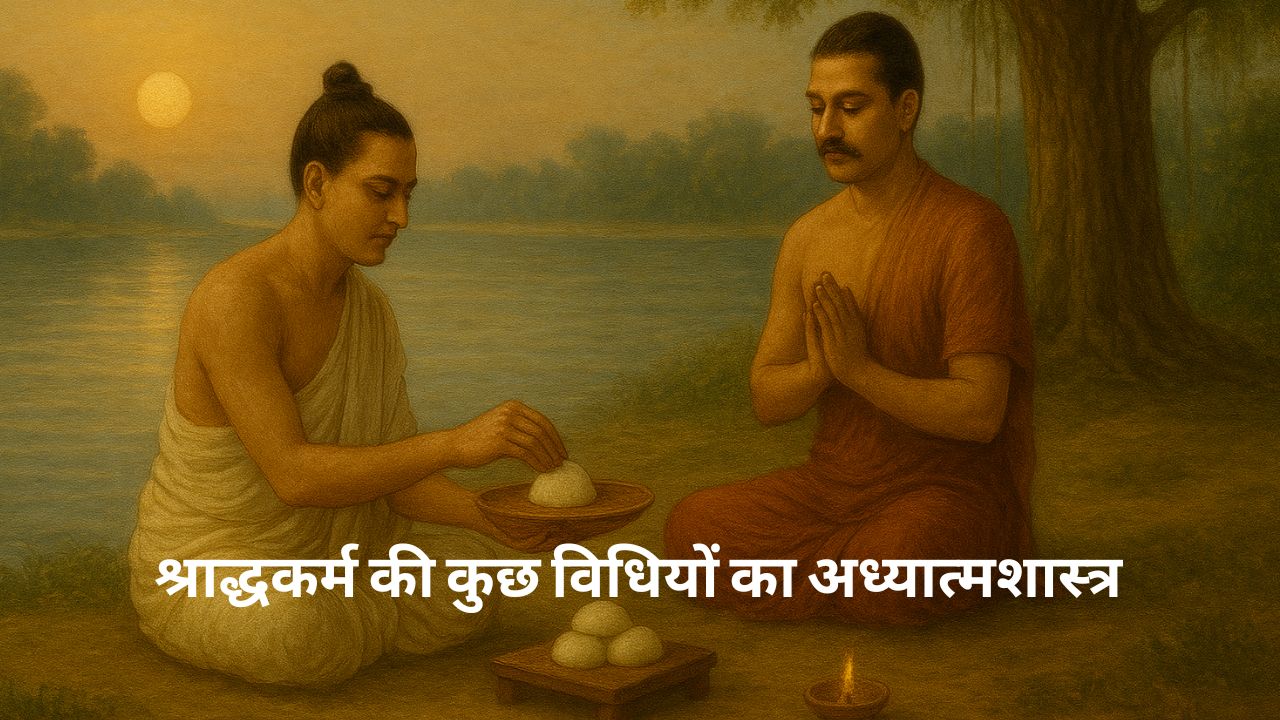- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
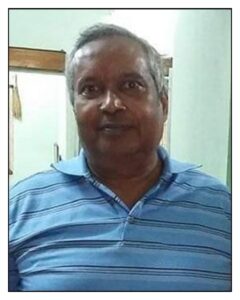 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
mystic power - १. वेद के ४ स्तर- १. संहिता (ऋषियों के मन्त्र का संग्रह), ब्राह्मण (व्याख्या), आरण्यक (प्रयोग), उपनिषद् (स्थिर सिद्धान्त-निषाद = बैठना )। इसमें अन्य भागों में केवल आदि में शान्तिपाठ होता है। उपनिषद् में आदि और अन्त दोनों में शान्ति पाठ होता है। इसका कारण है कि सिद्धान्त स्थिर करने के पहले मन शान्त होना चाहिये। सिद्धान्त का बाद में हर स्थिति में प्रयोग होता है अतः उसके भी विधिवत् लाभदायक प्रयोग के लिये मन शान्त होना चाहिये।
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
mystic power - १. वेद के ४ स्तर- १. संहिता (ऋषियों के मन्त्र का संग्रह), ब्राह्मण (व्याख्या), आरण्यक (प्रयोग), उपनिषद् (स्थिर सिद्धान्त-निषाद = बैठना )। इसमें अन्य भागों में केवल आदि में शान्तिपाठ होता है। उपनिषद् में आदि और अन्त दोनों में शान्ति पाठ होता है। इसका कारण है कि सिद्धान्त स्थिर करने के पहले मन शान्त होना चाहिये। सिद्धान्त का बाद में हर स्थिति में प्रयोग होता है अतः उसके भी विधिवत् लाभदायक प्रयोग के लिये मन शान्त होना चाहिये।
 https://mycloudparticles.com/
२. मांगलिक शब्द- हर मन्त्रके पहले ॐ का उच्चारण किया जाता है-
मनुस्मृति (२/७४)-ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा। स्रवत्यमोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति॥
ॐ और अथ इन दो शब्दों का ब्रह्मा ने सबसे पहले उच्चारण किया था अतः इनको माङ्गलिक कहा जाता है-
ॐकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा।
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ॥
(नारद पुराण, ५१/१०)
https://mycloudparticles.com/
२. मांगलिक शब्द- हर मन्त्रके पहले ॐ का उच्चारण किया जाता है-
मनुस्मृति (२/७४)-ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा। स्रवत्यमोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति॥
ॐ और अथ इन दो शब्दों का ब्रह्मा ने सबसे पहले उच्चारण किया था अतः इनको माङ्गलिक कहा जाता है-
ॐकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा।
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकावुभौ॥
(नारद पुराण, ५१/१०)
 ३. शान्तिपाठ के भेद- हर वेद के लिये अलग अलग शान्ति पाठ हैं। ४ वेदों में यजुर्वेद २ प्रकार का है-शुक्ल और कृष्ण। अतः कुल ५ प्रकार के शान्ति पाठ हैं जो इन वेदों के उपनिषदों के लिये प्रयुक्त होते हैं।
महा वाक्य रत्नावली में शान्तिपाठ का क्रम संक्षेप में है-
वाक्पूर्णसहनाप्यायन्भद्रं कर्णेभिरेव च।
पञ्च शान्तीः पठित्वादौ पठेद्वाक्यान्यनन्तरम्॥
इसका मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार स्पष्टीकरण है-
ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यवेदेषु द्विविधो मतः।
यजुर्वेदः शुक्लकृष्णविभेदेनात एव च॥१॥
शान्तयः पञ्चधा प्रोक्ता वेदानुक्रमणेन वै।
वाङ्मे मनसि शान्त्यैव त्वैतरेयं प्रपठ्यते॥२॥
ईशं पूर्णमदेनैव बृहदारण्यकं तथा।
सह नाविति शान्त्या च तैत्तिरीयं कठं च वै॥३॥
आप्यायन्त्विति शान्त्यैव केनच्छान्दोग्यसंज्ञके।
भद्रं कर्णेति मन्त्रेण प्रश्नमाण्डूक्यमुण्डकम्॥४॥
इति क्रमेण प्रत्युपनिषद् आदावन्ते च शान्तिं पठेत्।
इनके अनुसार वेदानुसार उपनिषदों के शान्तिपाठ हैं-
ऋग्वेद शान्तिपाठ-
ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधिवेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रात्संदधाम्यृतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्। अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
शुक्ल यजुर्वेदीय शान्ति पाठ-
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
कृष्ण यजुर्वेदीय शान्ति पाठ-
ॐ सह नाववतु॥ सह नौ भुनक्तु॥ सह वीर्यं करवावहै॥ तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
सामवेदीय शान्तिपाठ-
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
अथर्ववेदीय शान्ति पाठ-
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
४. वेद विभाजन- मूल एक ही वेद था जिसे ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को पढ़ाया था। बाद में इसका परा (एकत्व) तथा अपरा (वर्गीकरण-विज्ञान) में विभाजन हुआ। अपरा से ४ वेद और ६ अङ्ग हुए।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव,
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा-
मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह॥१॥
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा ऽथर्वा तां पुरो वाचाङ्गिरे ब्रह्म-विद्याम्। स भरद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भरद्वाजो ऽङ्गिरसे परावराम्॥२॥ (मुण्डकोपनिषद्,१/१/१,२ )।
द्वे विद्ये वेदितव्ये- ... परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डकोपनिषद्, १/१/४,५)
विभाजन के बाद अविभाज्य अंश ब्रह्म रूप अथर्व वेद में रह गया-
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। (गीता, १३/१६)
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। (गीता, १८/२०)
अतः त्रयी का अर्थ १ मूल + ३ शाखा = ४ वेद होता है। इसका प्रतीक पलास दण्ड है जिससे ३ पत्ते निकलते है। यह वेद निर्माता ब्रह्मा के प्रतीक रूप में वेदारम्भ संस्कार (यज्ञोपवीत) में प्रयुक्त होता है।
ब्रह्म वै पलाशः। (शतपथ ब्राह्मण, १/३/३/१९, ५/२/४/१८, ६/६/३/७)
ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशम् (पर्णम्) (शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/८)
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः। (ऐतरेय ब्राह्मण २/१)
यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः।
अत्रा नो विश्यतिः पिता पुराणां अनु वेनति॥
(ऋक् १०/१३५/१)
ब्राह्मणो बैल्व पालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ।
पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हति धर्मतः॥ (मनु स्मृति, २/४५)
बिल्व (बेल) तथा पलाश दोनों में ३ पत्ते होते हैं।
त्रयी विभाजन का आधार है, ऋक् = मूर्ति, यजु = गति, साम = महिमा या प्रभाव, अथर्व = अविभक्त ब्रह्म। इसी को मनुस्मृति आदि में अग्नि (सघन ताप या पदार्थ), वायु (गति) तथा रवि (तेज) भी कहा गया है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः,
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्,
सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम्॥
(मनु स्मृति, १/२३)
गति २ प्रकार की है-शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल गति प्रकाश युक्त अर्थात् दीखती है। कृष्ण गति अन्धकार युक्त अर्थात् भीतर छिपी हुयी है। शुक्ल गति ३ प्रकार की है-निकट आना, दूर जाना, सम दूरी पर रहना (वृत्ताकार कक्षा)। वस्तु का आन्तरिक प्रसारण या संकोच मिला कर ५ गति कही गयी है।
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। --- धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। (गीता, ८/२४-२५)
उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि। (वैशेषिक सूत्र, १/१/७)
शरीर या किसी पिण्ड के भीतर की गति दीखता नहीं है। वह कृष्ण गति १७ प्रकार की है, इस अर्थ में प्रजापति या पुरुष को १७ प्रकार का कहा गया है। समाज (विट् = समाज, वैश्य) भी १७ प्रकार है। विट् सप्तदशः। (ताण्ड्य महाब्राह्मण १८/१०/९) विशः सप्तदशः (ऐतरेय ब्राह्मण, ८/४)
सप्तदशो वै पुरुषो दश प्राणाश्चत्वार्यङ्गान्यात्मा पञ्चदशो ग्रीवाः षोडश्च्यः शिरः सप्तदशम्। (शतपथ ब्राह्मण, ६/२/२/९)
राष्ट्रं सप्तदशः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/८/८/५)
सर्व्वः सप्तदशो भवति। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १७/९/४)
सप्तदश एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रजात्यै। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १२/६/१३)
तस्माऽएतस्मै सप्तदशाय प्रजापतये। एतत् सप्तदशमन्नं समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश कला एते ते षोडशर्त्विजः (शतपथ ब्राह्मण, १०/४/१/१९)
अर्थात्, व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के अंगों का आन्तरिक समन्वय १७ प्रकार से है जो दीखता नहीं है। वह कृष्ण गति है। एक समतल को किसी चिह्न (ठप्पा) द्वारा १७ प्रकार से भरा जा सकता है। इसे आधुनिक बीजगणित में समतल स्फटिक सिद्धान्त कहते हैं। (Modern algebra by Michael Artin, Prentice-Hall, page 172-174) ५ महाभूतों की शुक्ल गति ५ x ३ =१५ प्रकार की होगी आन्तरिक गति १७ x ५ = ८५ प्रकार की है। अतः शुक्ल यजुर्वेद की १५ शाखा तथा कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा ( १ अगति या यथा स्थिति मिलाकर) हैं। समतल चादर की तरह मेघ भी पृथ्वी सतह को ढंक कर रखता है अतः ज्योतिष में १७ के लिये मेघ, घन आदि शब्दों का प्रयोग होता है।
५. शान्ति पाठ विभाजन- (१) ऋग्वेद स्थूल शरीर या मूर्ति का वेद है। अतः स्थूल शरीर में मन, वाक् आदि प्रतिष्ठित हों यह कामना करते हैं। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता----
(२) यजुर्वेद- गति का वेद है। जिस गति से उपयोगी कर्म होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। बाह्य यज्ञ ३ प्रकार के विश्व रूपों में देखते हैं-पूर्ण विश्व की स्थिति, पूर्ण विश्व गति रूप, पूरण विश्व निर्माण या यज्ञ रूप। ये तीनों अनन्त हैं। अतः हम कहते हैं कि पूर्ण विश्व से पूर्ण गति रूप निकाल देने पर भी निर्माण या परिवर्तन रूप यज्ञ बचा रहता है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं----
(३) कृष्ण यजुर्वेद-यह समाज या देश की आन्तरिक रचना है। इसके लिये हमारी कामना है कि सभी एक साथ रह कर एक दूसरे की सहायता करें। यज्ञों का उद्देश्य भी यही कहा है कि एक यज्ञ द्वारा दूसरा यज्ञ सम्पन्न हो तभी उन्नति की जा सकती है। ॐ सह नाववतु॥ सह नौ भुनक्तु---
ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति । (गीता ४/२५)
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (पुरुष-सूक्त, यजुर्वेद ३१/१६)
(४) साम वेद-यह बाहरी अदृश्य प्रभाव या महिमा है। उससे हमारे मन शरीर आप्यायित हों यह हमारी कामना है। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि-----। यही गायत्री मन्त्र का तृतीय पद भी है-धियो यो नः प्रचोदयात्।
(५) अथर्ववेद-यह सनातन ब्रह्म का स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं है। थर्व = थरथराना, अथर्व = स्थिर, स्थायी। अतः हमारी कामना है कि हमारा शरीर स्थिर रहे, सब तरफ शान्ति हो, चारों दिशाओं में स्वस्ति हो। इन्द्र, पूषा, तार्क्ष्य, बृहस्पति-ये ४ दिशाओं के ४ नक्षत्रों के स्वामी हैं-ज्येष्ठा, रेवती, गोविन्द (विष्णु), पुष्य। इसका प्रतीक स्वस्तिक चिह्न है। अन्य प्रकार से ये ४ पुरुषार्थों के कारक हैं-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्द्र राजा है, बृहस्पति गुरु, पूषा पोषण देने वाला तथा विष्णु पालन कर्त्ता। रक्षक राजा, ज्ञानदायक गुरु, पालन कर्त्ता विष्णु और पोषक पूषा कल्याण करें। अतः दोनों कहते हैं-स्थिरैरङ्गैः---, या स्वस्ति न इन्द्रो---।
६. ईशोपनिषद् का शान्तिपाठ-यह उपनिषद् शुक्ल यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय है। वाजसनेयि और काण्व शाखा के पाठ में थोड़ा अन्तर है, पर अर्थ एक ही हैं। अतः इसमें शुक्ल यजुर्वेद का शान्तिपाठ पढ़ा जाता है।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥
इसका सामान्य अर्थ कहते हैं कि विश्व अनन्त है, और अनन्त से अनन्त को घटाने पर अनन्त ही बचता है। शून्य से शून्य घाटाने पर भी वही बचता है। वेद में ४ प्रकार के अनन्तों की चर्चा है-
(१) वेदों के ३ अनन्त-भरद्वाजो ह वै त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्य्यमुवास । तं ह जीर्णि स्थविरं शयानं इन्द्र उपब्रज्य उवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुर्दद्यां, किमेनेन कुर्य्या इति ? ब्रह्मचर्य्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच । तं ह त्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयाञ्चकार। तेषां हैकैकस्मान्मुष्टिमाददे । स होवाच, भरद्वाजेत्यमन्त्र्य । वेदा वा एते । “अनन्ता वै वेदाः” । एतद्वा एतैस्त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचथाः । अथ त इतरदनूक्तमेव । (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१०/११)
यहां वेद और अनन्त दोनों बहुवचन हैं अतः २ से अधिक हैं। अनन्त की परिभाषा आधुनिक बीज गणित और कैलकुलस (कलन) में है कि यह किसी भी बड़ी संख्या से बड़ा है। इसके विपरीत बीजगणित में किसी संख्या से उसी को घटाने से शून्य होता है। किन्तु कैलकुलस की परिभाषा है कि यह किसी भी छोटी संख्या से छोटा है। कैलकुलस की दोनों परिभाषायें उपनिषद् में हैं-
अणोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्।
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः॥
(कठोपनिषद्, १/२/२०, श्वेताश्वतर उपनिषद्, ३/२०)
कैण्टर की सेट थिओरी (१८८०) में अनन्तों की २ श्रेणियों की व्याख्या है-एक वह जो गिना जा सके। १,२,३,..... आदि संख्याओं का क्रम भी अनन्त है। इन संख्याओं से सभी वस्तुओं को १-१ कर मिलाया जा सके तो यह प्रथम प्रकार का अनन्त है। भिन्न संख्यायें भी इससे एक विधि द्वारा गिनी जा सकती हैं। पर कुछ संख्यायें ऐसी हैं जो इससे नहीं गिनी जा सकती हैं, जैसे ० और १ के बीच की सभी संख्या या किसी रेखा खण्ड के विन्दुओं की संख्या। यह बड़ा अनन्त है जिसको २ के अनन्त घात से सूचित किया जाता है। एक अन्य अनन्त भी हो सकता है, जो २ के दूसरे अनन्त घात के बराबर होगा। ऋग्वेद मूर्त्ति रूप है, वह गिना जा सकता है-प्रथम प्रकार का अनन्त जो १,२,३, .... क्रम के बराबर है। यजुर्वेद का क्रिया या गति रूप अनन्त वही है जो विन्दु की गति से बने रेखा में होगा, यह दूसरा अनन्त है। साम उसकी महिमा तीसरा अनन्त है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः,
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्,
सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
दूसरा अनन्त भी २ प्रकार का है, जो गणित सूत्रों द्वारा व्यक्त हो सके वह परिमेय या प्रमेय, जो उससे व्यक्त नहीं हो सके वह अप्रमेय है । विष्णु सहस्रनाम में अनन्त के लिये ३ शब्द हैं-अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय। इसके अनुसार प्रथम संख्येय अनन्त है। असंख्येय अनन्त २ प्रकार का है, प्रमेय और अप्रमेय। उसके बाद परात्पर अनन्त ब्रह्मरूप अथर्व वेद है।
यज्ञ सम्बन्धी अर्थ है कि स्थिति रूप जगत् का एक अंश कर्म या क्रिया रूप जगत् है, क्रिया का एक भाग यज्ञ है जिससे चक्रीय क्रम में उपयोगी वस्तु का उत्पादन होत है। ये तीनों ही पूर्ण तथा अनन्त हैं तथा एक दूसरे के अंश है।
अन्य अर्थ भी वैसा ही है। सबसे पहले अव्यक्त परात्पर पुरुष था जिसके ४ पाद में केवल एक पाद से दृश्य जगत् बना। मूल परात्पर बड़ा है या दृश्य विश्व के पिण्डों का आधार भी बड़ा है, अतः इनको पूरुष (दीर्घ पू) कहा है। विराट् पुरुष में कई प्रकार के यज्ञ हैं जिनका आरम्भ पुरुष रूपी पशु से हुआ जिसे यज्ञ पुरुष कहते हैं। अतः पूरुष, विराट् पुरुष तथा यज्ञ पुरुष क्रमशः पूर्व के अंश हैं तथा सभी पूर्ण हैं।
(पुरुष सूक्त, वाज. यजु, अध्याय ३१)-
एतावान् अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥३॥
= इतनी इसकी (भूत, वर्तमान् भविष्य जगत् रूप पुरुष की) महिमा है। इससे भी बड़ा या अधिक (ज्यायान्) पूरुष है। पूरा विश्व और भूत इसका १ ही पाद है, बाकी ३ पाद आकाश में अमृत (ज्यों का त्यों, अक्षय) है।
ततो विराट् अजायत, विराजो अधि पूरुषः।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः॥५॥
= उससे (एक पाद विश्व-रूप पुरुष, अज-एकपाद) विराट् (विशेष राजित, अव्यक्त तुलना में प्रत्यक्ष) विश्व उत्पन्न हुआ। विराट् से अधि-पूरुष (इसका आधार) उत्पन्न हुआ।
सप्तास्यासन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः।
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥१५॥
= इसकी ७ परिधि (७ लोकों की सीमा) थी तथा ३ x ७ समिधा (निर्माण सामग्री, जिसके हवन से नयी वस्तु उत्पन्न होति है) थी। देवों ने पुरुष रूप पशु को ही बान्ध कर विश्व निर्माण यज्ञ आरम्भ किया। (ब्रह्म ही हवि, निर्माण क्रिया, निर्मित पदार्थ अदि सब कुछ है-गीता, ४/२४)
इस अर्थ का निर्देश उपनिषद् के प्रथम श्लोक में भी है। वहां पूर्ण का क्रम है-विश्व (रचना), जगत् (गतिशील), जगत्यां जगत् (चक्रीय क्रम में उत्पादन)।
अदः का अर्थ दूर का निर्देश अर्थात् प्रथम पूर्ण, इदं निकटवर्ती या अन्तिम पूर्ण है।
३. शान्तिपाठ के भेद- हर वेद के लिये अलग अलग शान्ति पाठ हैं। ४ वेदों में यजुर्वेद २ प्रकार का है-शुक्ल और कृष्ण। अतः कुल ५ प्रकार के शान्ति पाठ हैं जो इन वेदों के उपनिषदों के लिये प्रयुक्त होते हैं।
महा वाक्य रत्नावली में शान्तिपाठ का क्रम संक्षेप में है-
वाक्पूर्णसहनाप्यायन्भद्रं कर्णेभिरेव च।
पञ्च शान्तीः पठित्वादौ पठेद्वाक्यान्यनन्तरम्॥
इसका मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार स्पष्टीकरण है-
ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यवेदेषु द्विविधो मतः।
यजुर्वेदः शुक्लकृष्णविभेदेनात एव च॥१॥
शान्तयः पञ्चधा प्रोक्ता वेदानुक्रमणेन वै।
वाङ्मे मनसि शान्त्यैव त्वैतरेयं प्रपठ्यते॥२॥
ईशं पूर्णमदेनैव बृहदारण्यकं तथा।
सह नाविति शान्त्या च तैत्तिरीयं कठं च वै॥३॥
आप्यायन्त्विति शान्त्यैव केनच्छान्दोग्यसंज्ञके।
भद्रं कर्णेति मन्त्रेण प्रश्नमाण्डूक्यमुण्डकम्॥४॥
इति क्रमेण प्रत्युपनिषद् आदावन्ते च शान्तिं पठेत्।
इनके अनुसार वेदानुसार उपनिषदों के शान्तिपाठ हैं-
ऋग्वेद शान्तिपाठ-
ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधिवेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रात्संदधाम्यृतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्। अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
शुक्ल यजुर्वेदीय शान्ति पाठ-
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
कृष्ण यजुर्वेदीय शान्ति पाठ-
ॐ सह नाववतु॥ सह नौ भुनक्तु॥ सह वीर्यं करवावहै॥ तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
सामवेदीय शान्तिपाठ-
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
अथर्ववेदीय शान्ति पाठ-
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
४. वेद विभाजन- मूल एक ही वेद था जिसे ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को पढ़ाया था। बाद में इसका परा (एकत्व) तथा अपरा (वर्गीकरण-विज्ञान) में विभाजन हुआ। अपरा से ४ वेद और ६ अङ्ग हुए।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव,
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा-
मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह॥१॥
अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा ऽथर्वा तां पुरो वाचाङ्गिरे ब्रह्म-विद्याम्। स भरद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भरद्वाजो ऽङ्गिरसे परावराम्॥२॥ (मुण्डकोपनिषद्,१/१/१,२ )।
द्वे विद्ये वेदितव्ये- ... परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डकोपनिषद्, १/१/४,५)
विभाजन के बाद अविभाज्य अंश ब्रह्म रूप अथर्व वेद में रह गया-
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। (गीता, १३/१६)
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। (गीता, १८/२०)
अतः त्रयी का अर्थ १ मूल + ३ शाखा = ४ वेद होता है। इसका प्रतीक पलास दण्ड है जिससे ३ पत्ते निकलते है। यह वेद निर्माता ब्रह्मा के प्रतीक रूप में वेदारम्भ संस्कार (यज्ञोपवीत) में प्रयुक्त होता है।
ब्रह्म वै पलाशः। (शतपथ ब्राह्मण, १/३/३/१९, ५/२/४/१८, ६/६/३/७)
ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशम् (पर्णम्) (शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/८)
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः। (ऐतरेय ब्राह्मण २/१)
यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः।
अत्रा नो विश्यतिः पिता पुराणां अनु वेनति॥
(ऋक् १०/१३५/१)
ब्राह्मणो बैल्व पालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ।
पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हति धर्मतः॥ (मनु स्मृति, २/४५)
बिल्व (बेल) तथा पलाश दोनों में ३ पत्ते होते हैं।
त्रयी विभाजन का आधार है, ऋक् = मूर्ति, यजु = गति, साम = महिमा या प्रभाव, अथर्व = अविभक्त ब्रह्म। इसी को मनुस्मृति आदि में अग्नि (सघन ताप या पदार्थ), वायु (गति) तथा रवि (तेज) भी कहा गया है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः,
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्,
सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम्॥
(मनु स्मृति, १/२३)
गति २ प्रकार की है-शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल गति प्रकाश युक्त अर्थात् दीखती है। कृष्ण गति अन्धकार युक्त अर्थात् भीतर छिपी हुयी है। शुक्ल गति ३ प्रकार की है-निकट आना, दूर जाना, सम दूरी पर रहना (वृत्ताकार कक्षा)। वस्तु का आन्तरिक प्रसारण या संकोच मिला कर ५ गति कही गयी है।
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। --- धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। (गीता, ८/२४-२५)
उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि। (वैशेषिक सूत्र, १/१/७)
शरीर या किसी पिण्ड के भीतर की गति दीखता नहीं है। वह कृष्ण गति १७ प्रकार की है, इस अर्थ में प्रजापति या पुरुष को १७ प्रकार का कहा गया है। समाज (विट् = समाज, वैश्य) भी १७ प्रकार है। विट् सप्तदशः। (ताण्ड्य महाब्राह्मण १८/१०/९) विशः सप्तदशः (ऐतरेय ब्राह्मण, ८/४)
सप्तदशो वै पुरुषो दश प्राणाश्चत्वार्यङ्गान्यात्मा पञ्चदशो ग्रीवाः षोडश्च्यः शिरः सप्तदशम्। (शतपथ ब्राह्मण, ६/२/२/९)
राष्ट्रं सप्तदशः। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/८/८/५)
सर्व्वः सप्तदशो भवति। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १७/९/४)
सप्तदश एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रजात्यै। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १२/६/१३)
तस्माऽएतस्मै सप्तदशाय प्रजापतये। एतत् सप्तदशमन्नं समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश कला एते ते षोडशर्त्विजः (शतपथ ब्राह्मण, १०/४/१/१९)
अर्थात्, व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के अंगों का आन्तरिक समन्वय १७ प्रकार से है जो दीखता नहीं है। वह कृष्ण गति है। एक समतल को किसी चिह्न (ठप्पा) द्वारा १७ प्रकार से भरा जा सकता है। इसे आधुनिक बीजगणित में समतल स्फटिक सिद्धान्त कहते हैं। (Modern algebra by Michael Artin, Prentice-Hall, page 172-174) ५ महाभूतों की शुक्ल गति ५ x ३ =१५ प्रकार की होगी आन्तरिक गति १७ x ५ = ८५ प्रकार की है। अतः शुक्ल यजुर्वेद की १५ शाखा तथा कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा ( १ अगति या यथा स्थिति मिलाकर) हैं। समतल चादर की तरह मेघ भी पृथ्वी सतह को ढंक कर रखता है अतः ज्योतिष में १७ के लिये मेघ, घन आदि शब्दों का प्रयोग होता है।
५. शान्ति पाठ विभाजन- (१) ऋग्वेद स्थूल शरीर या मूर्ति का वेद है। अतः स्थूल शरीर में मन, वाक् आदि प्रतिष्ठित हों यह कामना करते हैं। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता----
(२) यजुर्वेद- गति का वेद है। जिस गति से उपयोगी कर्म होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। बाह्य यज्ञ ३ प्रकार के विश्व रूपों में देखते हैं-पूर्ण विश्व की स्थिति, पूर्ण विश्व गति रूप, पूरण विश्व निर्माण या यज्ञ रूप। ये तीनों अनन्त हैं। अतः हम कहते हैं कि पूर्ण विश्व से पूर्ण गति रूप निकाल देने पर भी निर्माण या परिवर्तन रूप यज्ञ बचा रहता है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं----
(३) कृष्ण यजुर्वेद-यह समाज या देश की आन्तरिक रचना है। इसके लिये हमारी कामना है कि सभी एक साथ रह कर एक दूसरे की सहायता करें। यज्ञों का उद्देश्य भी यही कहा है कि एक यज्ञ द्वारा दूसरा यज्ञ सम्पन्न हो तभी उन्नति की जा सकती है। ॐ सह नाववतु॥ सह नौ भुनक्तु---
ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति । (गीता ४/२५)
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (पुरुष-सूक्त, यजुर्वेद ३१/१६)
(४) साम वेद-यह बाहरी अदृश्य प्रभाव या महिमा है। उससे हमारे मन शरीर आप्यायित हों यह हमारी कामना है। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि-----। यही गायत्री मन्त्र का तृतीय पद भी है-धियो यो नः प्रचोदयात्।
(५) अथर्ववेद-यह सनातन ब्रह्म का स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं है। थर्व = थरथराना, अथर्व = स्थिर, स्थायी। अतः हमारी कामना है कि हमारा शरीर स्थिर रहे, सब तरफ शान्ति हो, चारों दिशाओं में स्वस्ति हो। इन्द्र, पूषा, तार्क्ष्य, बृहस्पति-ये ४ दिशाओं के ४ नक्षत्रों के स्वामी हैं-ज्येष्ठा, रेवती, गोविन्द (विष्णु), पुष्य। इसका प्रतीक स्वस्तिक चिह्न है। अन्य प्रकार से ये ४ पुरुषार्थों के कारक हैं-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्द्र राजा है, बृहस्पति गुरु, पूषा पोषण देने वाला तथा विष्णु पालन कर्त्ता। रक्षक राजा, ज्ञानदायक गुरु, पालन कर्त्ता विष्णु और पोषक पूषा कल्याण करें। अतः दोनों कहते हैं-स्थिरैरङ्गैः---, या स्वस्ति न इन्द्रो---।
६. ईशोपनिषद् का शान्तिपाठ-यह उपनिषद् शुक्ल यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय है। वाजसनेयि और काण्व शाखा के पाठ में थोड़ा अन्तर है, पर अर्थ एक ही हैं। अतः इसमें शुक्ल यजुर्वेद का शान्तिपाठ पढ़ा जाता है।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥
इसका सामान्य अर्थ कहते हैं कि विश्व अनन्त है, और अनन्त से अनन्त को घटाने पर अनन्त ही बचता है। शून्य से शून्य घाटाने पर भी वही बचता है। वेद में ४ प्रकार के अनन्तों की चर्चा है-
(१) वेदों के ३ अनन्त-भरद्वाजो ह वै त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्य्यमुवास । तं ह जीर्णि स्थविरं शयानं इन्द्र उपब्रज्य उवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुर्दद्यां, किमेनेन कुर्य्या इति ? ब्रह्मचर्य्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच । तं ह त्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयाञ्चकार। तेषां हैकैकस्मान्मुष्टिमाददे । स होवाच, भरद्वाजेत्यमन्त्र्य । वेदा वा एते । “अनन्ता वै वेदाः” । एतद्वा एतैस्त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचथाः । अथ त इतरदनूक्तमेव । (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१०/११)
यहां वेद और अनन्त दोनों बहुवचन हैं अतः २ से अधिक हैं। अनन्त की परिभाषा आधुनिक बीज गणित और कैलकुलस (कलन) में है कि यह किसी भी बड़ी संख्या से बड़ा है। इसके विपरीत बीजगणित में किसी संख्या से उसी को घटाने से शून्य होता है। किन्तु कैलकुलस की परिभाषा है कि यह किसी भी छोटी संख्या से छोटा है। कैलकुलस की दोनों परिभाषायें उपनिषद् में हैं-
अणोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्।
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः॥
(कठोपनिषद्, १/२/२०, श्वेताश्वतर उपनिषद्, ३/२०)
कैण्टर की सेट थिओरी (१८८०) में अनन्तों की २ श्रेणियों की व्याख्या है-एक वह जो गिना जा सके। १,२,३,..... आदि संख्याओं का क्रम भी अनन्त है। इन संख्याओं से सभी वस्तुओं को १-१ कर मिलाया जा सके तो यह प्रथम प्रकार का अनन्त है। भिन्न संख्यायें भी इससे एक विधि द्वारा गिनी जा सकती हैं। पर कुछ संख्यायें ऐसी हैं जो इससे नहीं गिनी जा सकती हैं, जैसे ० और १ के बीच की सभी संख्या या किसी रेखा खण्ड के विन्दुओं की संख्या। यह बड़ा अनन्त है जिसको २ के अनन्त घात से सूचित किया जाता है। एक अन्य अनन्त भी हो सकता है, जो २ के दूसरे अनन्त घात के बराबर होगा। ऋग्वेद मूर्त्ति रूप है, वह गिना जा सकता है-प्रथम प्रकार का अनन्त जो १,२,३, .... क्रम के बराबर है। यजुर्वेद का क्रिया या गति रूप अनन्त वही है जो विन्दु की गति से बने रेखा में होगा, यह दूसरा अनन्त है। साम उसकी महिमा तीसरा अनन्त है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः,
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्,
सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
दूसरा अनन्त भी २ प्रकार का है, जो गणित सूत्रों द्वारा व्यक्त हो सके वह परिमेय या प्रमेय, जो उससे व्यक्त नहीं हो सके वह अप्रमेय है । विष्णु सहस्रनाम में अनन्त के लिये ३ शब्द हैं-अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय। इसके अनुसार प्रथम संख्येय अनन्त है। असंख्येय अनन्त २ प्रकार का है, प्रमेय और अप्रमेय। उसके बाद परात्पर अनन्त ब्रह्मरूप अथर्व वेद है।
यज्ञ सम्बन्धी अर्थ है कि स्थिति रूप जगत् का एक अंश कर्म या क्रिया रूप जगत् है, क्रिया का एक भाग यज्ञ है जिससे चक्रीय क्रम में उपयोगी वस्तु का उत्पादन होत है। ये तीनों ही पूर्ण तथा अनन्त हैं तथा एक दूसरे के अंश है।
अन्य अर्थ भी वैसा ही है। सबसे पहले अव्यक्त परात्पर पुरुष था जिसके ४ पाद में केवल एक पाद से दृश्य जगत् बना। मूल परात्पर बड़ा है या दृश्य विश्व के पिण्डों का आधार भी बड़ा है, अतः इनको पूरुष (दीर्घ पू) कहा है। विराट् पुरुष में कई प्रकार के यज्ञ हैं जिनका आरम्भ पुरुष रूपी पशु से हुआ जिसे यज्ञ पुरुष कहते हैं। अतः पूरुष, विराट् पुरुष तथा यज्ञ पुरुष क्रमशः पूर्व के अंश हैं तथा सभी पूर्ण हैं।
(पुरुष सूक्त, वाज. यजु, अध्याय ३१)-
एतावान् अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥३॥
= इतनी इसकी (भूत, वर्तमान् भविष्य जगत् रूप पुरुष की) महिमा है। इससे भी बड़ा या अधिक (ज्यायान्) पूरुष है। पूरा विश्व और भूत इसका १ ही पाद है, बाकी ३ पाद आकाश में अमृत (ज्यों का त्यों, अक्षय) है।
ततो विराट् अजायत, विराजो अधि पूरुषः।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः॥५॥
= उससे (एक पाद विश्व-रूप पुरुष, अज-एकपाद) विराट् (विशेष राजित, अव्यक्त तुलना में प्रत्यक्ष) विश्व उत्पन्न हुआ। विराट् से अधि-पूरुष (इसका आधार) उत्पन्न हुआ।
सप्तास्यासन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः।
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥१५॥
= इसकी ७ परिधि (७ लोकों की सीमा) थी तथा ३ x ७ समिधा (निर्माण सामग्री, जिसके हवन से नयी वस्तु उत्पन्न होति है) थी। देवों ने पुरुष रूप पशु को ही बान्ध कर विश्व निर्माण यज्ञ आरम्भ किया। (ब्रह्म ही हवि, निर्माण क्रिया, निर्मित पदार्थ अदि सब कुछ है-गीता, ४/२४)
इस अर्थ का निर्देश उपनिषद् के प्रथम श्लोक में भी है। वहां पूर्ण का क्रम है-विश्व (रचना), जगत् (गतिशील), जगत्यां जगत् (चक्रीय क्रम में उत्पादन)।
अदः का अर्थ दूर का निर्देश अर्थात् प्रथम पूर्ण, इदं निकटवर्ती या अन्तिम पूर्ण है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.