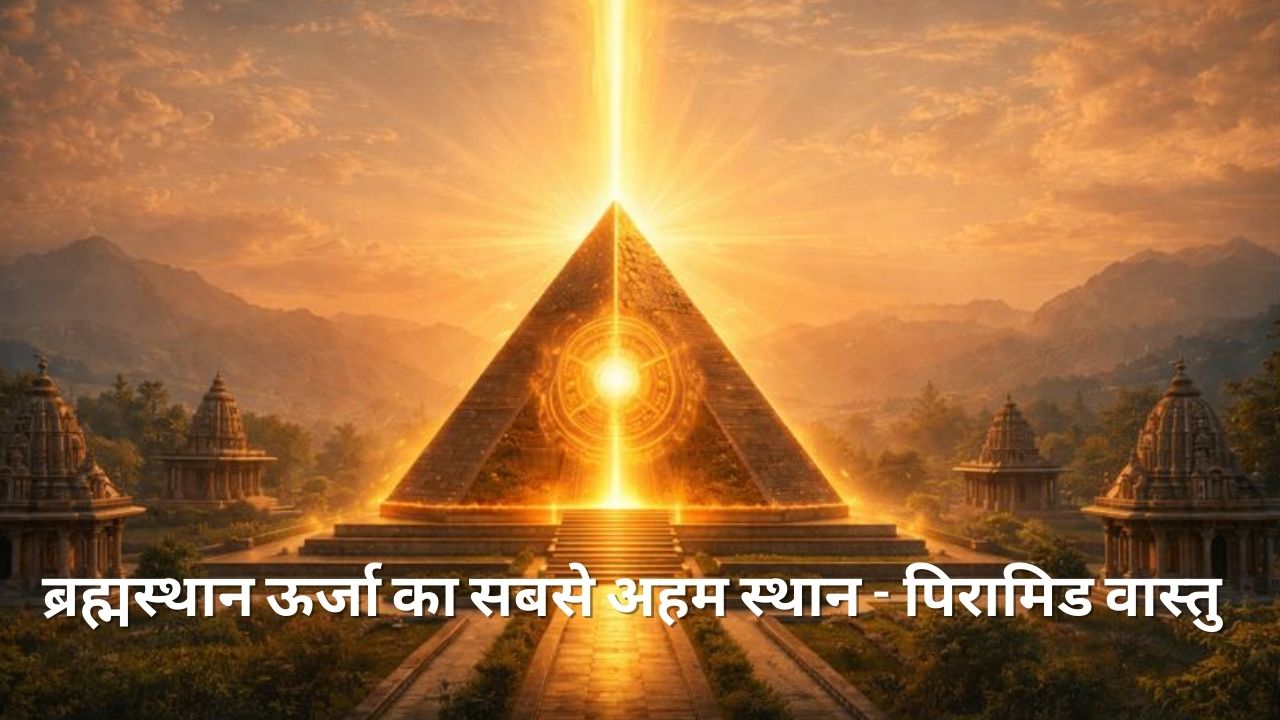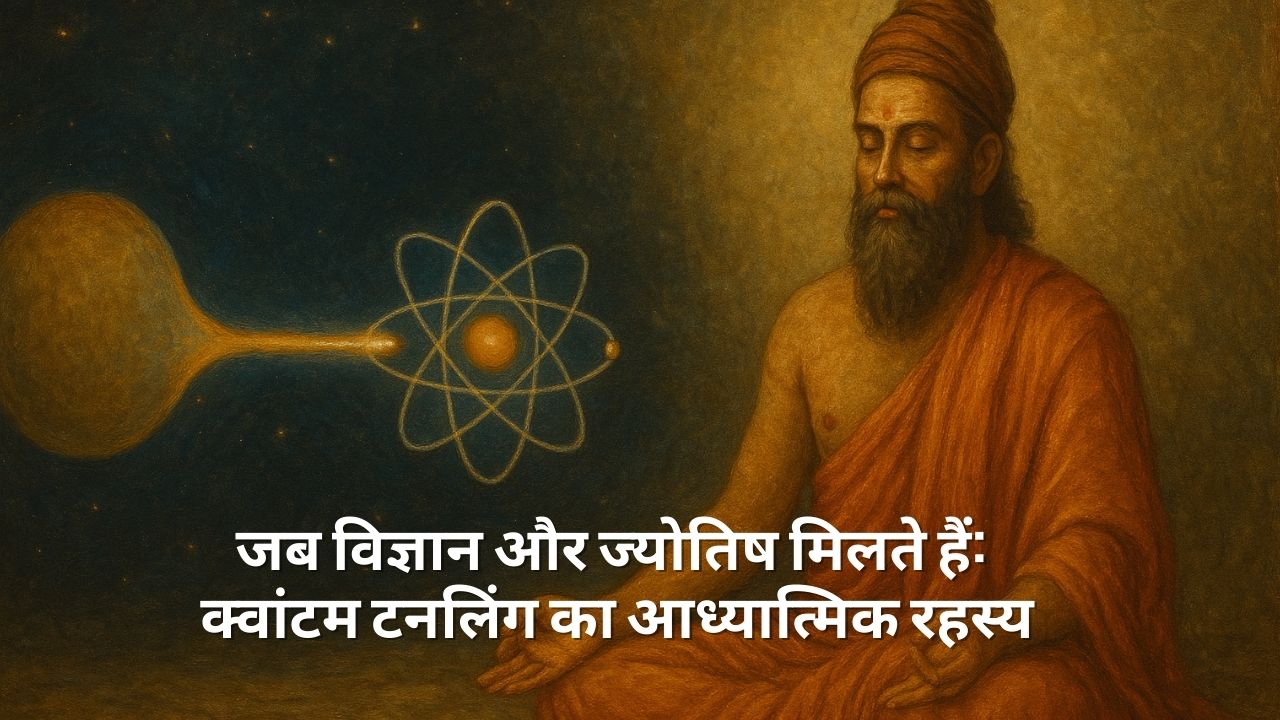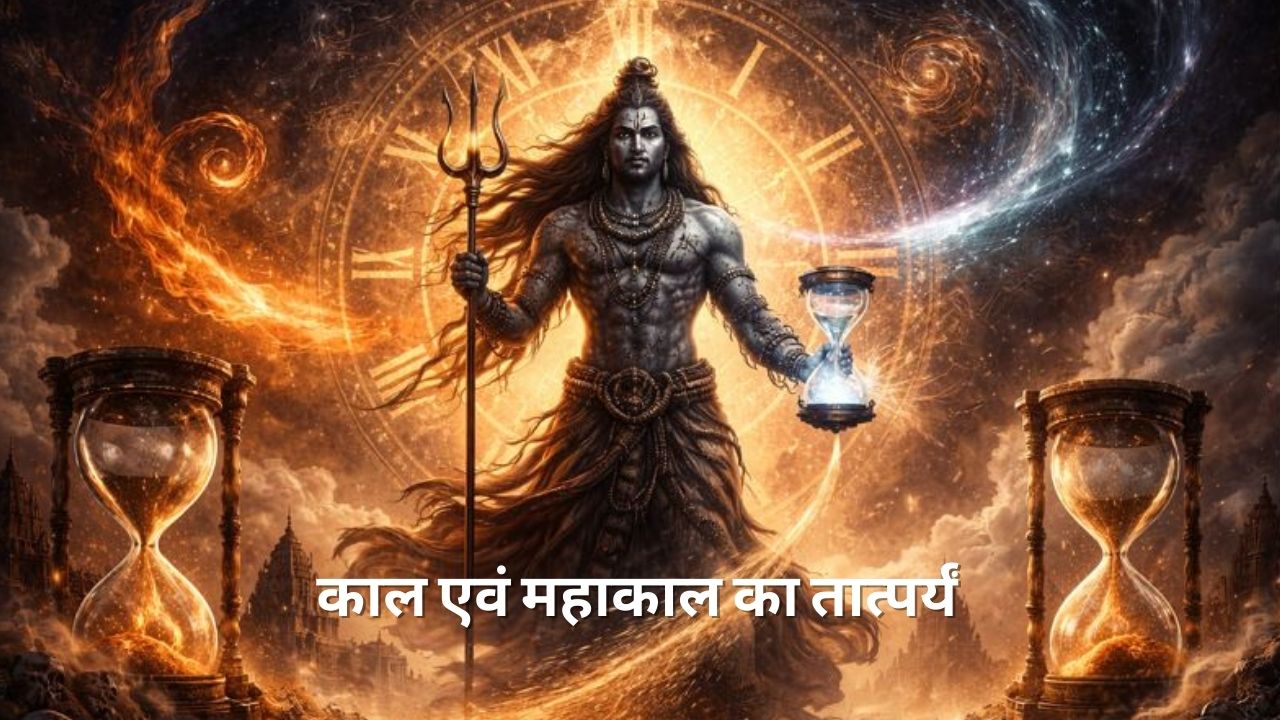- ज्योतिष विज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 शशांक शेखर शुल्ब (धर्मज्ञ)-
mysticpower-सृष्टि के दो सूत्र हैं- सूर्य और प्रकृति । सूर्य ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत (सूत्र) है। प्रकृति ही गुणों (सत्, रज, तम) का स्रोत (स्थान) है। द्योतते इति ज्योतिः। जिसमें चमक है, वह ज्योति है। सूर्यो ज्योति:- यह वेदवचन है। ज्योतिरेव ज्योतिषः । ज्योति और ज्योतिष में अभेद है, जैसे सूर्य एवं उसके प्रकाश में। इसी प्रकार प्रकृति एवं उसके गुण अभिन्न हैं। जो सूर्य को जानता है, वह ज्योतिषी है और जो प्रकृति को जानता है, वह भी ज्योतिषी है। सूर्य में ज्योति है । चन्द्रमा में ज्योत्स्ना है। स्वस्फूर्त प्रकाश को ज्योति और परस्फूर्त प्रकाश को ज्योत्स्ना कहते हैं। ज्योति - ज्ञान । ज्योति से तमका नाश होता है। ज्ञानसे अज्ञान दूर होता है। ज्योति णिनि ज्योतिषी ज्ञानी, प्रकाशयुक्त सूर्य परम ज्योतिषी है। इस सूर्यका उदय जिसके हृदयाकाश में हुआ है, वही ज्ञानी या ज्योतिषी है।
शशांक शेखर शुल्ब (धर्मज्ञ)-
mysticpower-सृष्टि के दो सूत्र हैं- सूर्य और प्रकृति । सूर्य ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत (सूत्र) है। प्रकृति ही गुणों (सत्, रज, तम) का स्रोत (स्थान) है। द्योतते इति ज्योतिः। जिसमें चमक है, वह ज्योति है। सूर्यो ज्योति:- यह वेदवचन है। ज्योतिरेव ज्योतिषः । ज्योति और ज्योतिष में अभेद है, जैसे सूर्य एवं उसके प्रकाश में। इसी प्रकार प्रकृति एवं उसके गुण अभिन्न हैं। जो सूर्य को जानता है, वह ज्योतिषी है और जो प्रकृति को जानता है, वह भी ज्योतिषी है। सूर्य में ज्योति है । चन्द्रमा में ज्योत्स्ना है। स्वस्फूर्त प्रकाश को ज्योति और परस्फूर्त प्रकाश को ज्योत्स्ना कहते हैं। ज्योति - ज्ञान । ज्योति से तमका नाश होता है। ज्ञानसे अज्ञान दूर होता है। ज्योति णिनि ज्योतिषी ज्ञानी, प्रकाशयुक्त सूर्य परम ज्योतिषी है। इस सूर्यका उदय जिसके हृदयाकाश में हुआ है, वही ज्ञानी या ज्योतिषी है।
 https://www.mycloudparticles.com/
व्यक्ताव्यक्त प्रकृति महामाया जगन्माता विश्वात्मिका- द्वारा प्रतिपल ज्योतिषशास्त्र का उत्सर्जन नाना भाँति होता रहता है। प्रकृति की भाषा क्रियात्मक है। प्रकृति के अवयव पंचभूतादि के माध्यम से घटित होने वाली घटनाओं का परिज्ञान अनेकों जनों, मुनियों, मनीषियों को हुआ। इन्होंने उसे सम्यक् रूपसे प्रस्तुत किया। इसे ज्योतिषशास्त्र का नाम दिया गया है। जिससे लोगोंके मन-बुद्धिपर शासन किया जाय, उसका नाम शास्त्र है। ज्योतिषशास्त्र सर्वाधिक प्रभावशाली होने से समस्त शास्त्रों में सर्वोपरि एवं अग्रगण्य है। इसकी अनेक विधाएँ शाखाएँ हैं।
https://www.mycloudparticles.com/
व्यक्ताव्यक्त प्रकृति महामाया जगन्माता विश्वात्मिका- द्वारा प्रतिपल ज्योतिषशास्त्र का उत्सर्जन नाना भाँति होता रहता है। प्रकृति की भाषा क्रियात्मक है। प्रकृति के अवयव पंचभूतादि के माध्यम से घटित होने वाली घटनाओं का परिज्ञान अनेकों जनों, मुनियों, मनीषियों को हुआ। इन्होंने उसे सम्यक् रूपसे प्रस्तुत किया। इसे ज्योतिषशास्त्र का नाम दिया गया है। जिससे लोगोंके मन-बुद्धिपर शासन किया जाय, उसका नाम शास्त्र है। ज्योतिषशास्त्र सर्वाधिक प्रभावशाली होने से समस्त शास्त्रों में सर्वोपरि एवं अग्रगण्य है। इसकी अनेक विधाएँ शाखाएँ हैं।
 इतिहास, पुराण, रामायण, तन्त्र एवं इतर ग्रन्थोंमें एतत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि के प्रत्यक्ष गोचर तथा राहु- केतुके अप्रत्यक्ष प्रभाव की संयुक्त विधा से ग्रहनक्षत्रजन्य ज्योतिष का आविष्कार हमारे पूर्वजोंने किया। इस ज्योतिषवृक्षका मूल सिद्धान्त है, तना संहिता है, फल भविष्यकथन है। जैसे फलहीन वृक्ष व्यर्थ है, वैसे ही फलितशास्त्र (परिणामवाचन) के बिना ज्योतिष बुद्धिका बोझ है। फलित मनुष्यका मार्गदर्शक है। समाज फलितज्ञ आदरणीय है। शुष्क ज्ञान, जिसका जीवनमें उपयोग नहीं है, त्याज्य है। जीवन के संवर्धन, मार्गदर्शन हेतु उपयोगी समस्त ज्ञान ज्योतिष की परिधि में आता है। यह ज्योतिषीय ज्ञान व्यावहारिक होने से वरेण्य एवं वर्ण्य है। इसीका वर्णन ज्योतिर्विद महर्षियों ने किया है।
माताके गर्भ से बाहर आनेवाला शरीरधारी जीव जातक कहलाता है। समयसापेक्ष ग्रह-नक्षत्रोंकी स्थितिसे जातकके विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसकी सत्यता का आधार सिद्धान्त एवं लोकव्यवहार से युक्त उहा एवं सत्यनिष्ठा है। असत्यमें प्रतिष्ठित व्यक्तिका ज्ञान अफल होता है, वाणी विफल होती है. क्रिया निष्फल होती है। ज्योतिषी सत्यके प्रति दृढ़- संलग्न होता है, वह सत्यचर्या में रहता है और निर्भय तथा निर्लोभ होता है।
नवग्रह, द्वादश भाव एवं द्वादश राशियोंकि त्र्यम्बकमे ज्योतिष- पुरुषका शरीर बनता है। यह ज्योतिषपुरुष ही काल है। इसका ज्ञाता कालज्ञ कहलाता है। सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु नवग्रह है। ये सभी उदय एवं अस्त होते रहते हैं उदय दृश्य। अस्त अदृश्य राहु-केतु उदयास्त से परे हैं, छाया ग्रह हैं। होना मात्र इनकी वास्तविकता है। अति प्रभावशाली होनेसे ये सतत मान्य हैं। इनका कोई अपना घर नहीं है। ये किरायेके घरमें अथवा बलात् दूसरेके घरमें रहते हैं। ये सदैव वामावर्त (वक्री) रहते हैं। ये स्थिर गति से चलते हैं तथा प्रत्येक राशिमें १८ महीने रहते हैं। सूर्य सदैव स्थिर स्वभावका तथा चन्द्रमा अस्थिर स्वभावका है। बुध और बृहस्पति नित्य द्विस्वभावके हैं। शुक्र, शनि, मंगल- ये तीनों कभी स्थिर और कभी अस्थिर स्वभाव रखते हैं राहु-केतुका अपना कोई स्वभाव नहीं ये जिस राशिमें रहते हैं, उसीके स्वभावको अपना लेते हैं।
नवग्रहोंमें दो वर्ग हैं-देव, दैत्य। सूर्य, मंगल, शुक्लपक्षका चन्द्रमा, बृहस्पति, केतु देववर्गमें आते हैं। शुक्र, शनि, बुध, राहु, कृष्णपक्षका चन्द्रमा दैत्यवर्गमें आते हैं। किसीसे वैर न रखनेवाला चन्द्रमा दोनों पक्षोंमें मान्य है। चन्द्रमा मन प्रत्येक व्यक्तिका मन कभी देव तो कभी दैत्यके गुणोंवाला होता है। वृद्धिको प्राप्त चन्द्रमा देव है। ह्रासमाण चन्द्रमा दैत्य है। मेष-वृश्चिक, धनु मीन, कर्क- सिंह राशियाँ देववर्गकी हैं। वृष-तुला, मिथुन- कन्या, मकर कुम्भ राशियाँ दैत्यवर्गकी हैं। कर्कराशिवाला व्यक्ति शुक्लपक्षी होनेपर देववर्गमें तथा कृष्णपक्षी होनेपर दैत्यवर्गमें गिना जाता है। स्वभाव-निर्धारणमें यह विशेष ध्यातव्य है। राहु-केतु कुटिल ग्रह हैं। लग्न या चन्द्रमाके साथ रहनेपर ये स्वभावनियन्ता होते हैं। केतु प्रकाश है। राहु अन्धकार है। उच्चतर ज्ञान केतु है। निम्नतर विद्या राहु है। दोनों गूढ ग्रह हैं तथा अपने- अपने वर्गमें बलिष्ठ हैं। मंगलका पोष्य केतु है। शनिका पोष्य राहु है। शरीरमें कटिके ऊपरका भाग केतु है, नाभिके नीचेका भाग राहु है। सिरके केश केतु हैं, अधो स्थानके बाल राहु हैं। व्यक्तिको भूमिपर पड़ती छाया राहु है तथा पानी या दर्पणमें पड़ती छाया केतु है। राहु सदा अधोगामी मूल है तो केतु उपरिगामी तना। केतु दिन है। राहु रात्रि है। केतु आत्मगौरव है। राहु आत्माभिमान है। राहु-केतुके इस भेदको जो जाने, वही ज्योतिष में निष्णात है।
स्वयंको जानना ही ज्योतिषशास्त्रका लक्ष्य है। बाह्य ऐश्वर्यके लिये ज्योतिष नहीं है, स्वयंमें निहित आन्तरिक ऐश्वर्यके दर्शनके लिये ज्योतिष है। सुपात्रको सब कुछ मिलता है, कुपात्रको कुछ नहीं मिलता। इस सत्यघोषको कौन नकारेगा? व्यक्तिको सर्वप्रथम अपना लग्न जानना चाहिये। लग्न जन्मसमय-पूर्वी क्षितिजमें उदित राशि। १२ राशियाँ होनेसे १२ लग्न हैं। इसे भूलग्न कहते हैं। चन्द्रमा जन्मसमयमें जिस राशिमें होता है, उसे चन्द्रलग्न कहते हैं। राशि चक्रकी आदिराशि मेष है। इसकी ब्रह्मलग्न संज्ञा है। प्रकृति महत्तत्त्व/मस्तिष्कसंरचनाका ज्ञान हाँसे होता है। इन तीन लग्नोंके समयेत अध्ययन व्यक्तिको अपनी प्रकृतिका बोध होता है बोधके पश्चात् तदनुकूल कर्म करनेसे मोक्षका मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ ज्योतिषीय ज्ञानकी सार्थकता है। ज्योतिषमें आत्मनिष्ठा सर्वोपरि है, वस्तुनिष्ठा गौण है। जो स्वयं अन्धा है, वह दूसरेको क्या दिशानिर्देश देगा? स्वयंके लिये ज्योतिष अपनाना साधु है, परार्थ असाधु है।
प्रत्येक ग्रहक्ष के भाव या राशि जन्य बारह फल हैं। नवग्रहों एवं चारह भावों या राशियों के योग से १२×९=१०८ फल या परिणाम होते हैं। जिसे इसका पूर्ण ज्ञान है, उसे श्री१०८ के अलंकरण को भूषित माना जाता है। ज्योतिष के व्यापारी एवं ज्योतिष के आचारी अलग-अलग है। दोनों का कोई मेल नहीं। ज्योतिष फलकथनों पारपद्धति सर्वतोमुख एवं विश्वमान्य है। विंशेत्तरीदशापद्धति का विज्ञान अत्यन्त गूढ़ है। २७ नक्षत्रोंपर ९ ग्रहोंका स्वामित्व तथा प्रत्येक ग्रहकी दशावर्षसंख्या बौद्धिक तर्क से परे है। सटीक फल देनेसे यह सुमान्य है। यह सर्वविदित एवं प्रायोगिक सत्य है। दशान्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा, सूक्ष्मदशा प्राणदशापर्यन्त गणना केवल विंशोत्तरी प्रणाली में है। इससे व्यवस्थामें अव्यवस्था तथा अव्यवस्थायें व्यवस्थाका परिज्ञान होता है। प्रत्येक शुभ अशुभ तथा अशुभ शुभका होना इसका प्रमाण है। निश्चितता में अनिश्चितता तथा अनिश्चितताएँ निश्चितता अथवा अप्रत्याशित फलका होना ज्योतिषसे प्रमाणित है। प्रत्येक जातक को अकालमृत्युका सामना करना पड़ता है। प्रत्येक जातककी मृत्यु चन्द्रमाको प्राणदशामें होती है। यह घटी-पलात्मक होती है। इसमें वेदवाक्य प्रमाण हैं- चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः (अथर्व० १४।१।२४ एवं ७ । ८५ । २) । चन्द्रमाके द्वारा दीर्घायुका उल्लंघन - नाश किया जाता है। अर्थात् चन्द्रमा अकालमृत्युका कारक है। चन्द्रमा (मन) प्रतिक्षण क्षीण या वृद्धिको प्राप्त होता रहता है। इसलिये यह आयुका हारक अथवा कारक है। जातककी मृत्यु तो निश्चित है, आयु निश्चित नहीं है। आयुका संकोच एवं विस्तार जातकके अधिकारमें है। आयु (जीवन-विस्तार) का आधार उसके पूर्वजन्मके कर्मफल हैं। हम अपने एवं अपने लोगोंके वर्तमान कमसे अपनी आयुका नाशन एवं वर्धन करते रहते हैं। विकर्मसे आयुका संकोच होता है। सुकर्मसे आयुका विस्तार होता है। इस सत्यसे जो परिचित है, वही सच्चा ज्योतिषी है।
आयुकी सूक्ष्म गणना करना व्यर्थ किंवा सुमूर्खता है। स्थूलरूपसे दीर्घायु मध्यायु एवं अल्पायुका ज्ञान ही पर्याप्त है। तन्यका परिमापन करनेसे क्या लाभ? विषादसे आयु क्षीण होती है, प्रसादसे आयु बढ़ती है। विषाद एवं प्रसादका वासस्थान मन है। 'चन्द्रमा मनसो जातः' (अथर्व० १९।६।७) । मनसे स्थूल शरीर प्रभावित होता है। स्थूल शरीर या लग्नका कारक सूर्य है। सूर्य आत्मा (शरीर प्राण) है कथन है-'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' (यजु० १३। ४६) । इसलिये कुण्डलीमें चन्द्रमा एवं सूर्यकी स्थिति एवं बलका आकलनकर आयुकी उहा करनी चाहिये। महर्षि पराशर के अनुसार कलियुगमें मनुष्यकी सामान्य आयु १२० वर्ष है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित आयु देता है। सूर्य ६ वर्ष, चन्द्रमा १० वर्ष, मंगल ७ वर्ष, राहु १८ वर्ष, गुरु १६ वर्ष, शनि १९ वर्ष, बुध १७ वर्ष, केतु ७ वर्ष, शुक्र २० वर्ष है। सबका योग १२० वर्ष है। इसपर क्यों कहना अनुचित है। यह है और ध्रुव सत्य है।
वैवाहिक सम्बन्धोंमें कुण्डली मिलान एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। आधुनिक समयमें कुल एवं गुणको प्रधानता न देकर अर्थ एवं स्वार्थको वरीयता दी जा रही है। विवाहमें अवरोध डालनेके लिये कुण्डलीका उपयोग हो रहा है। विवाह अब क्रय-विक्रयका सेतु एवं पाखण्डका प्रतीक है। कन्याके विवाहके सन्दर्भमें नाडीका विचार किया जाता है, किंतु अब कन्याका विवाह होता कहाँ है? इसलिये वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण एवं भकूटपर्यन्त गुणोंका विचार करना समीचीन है। यहाँतक २८ गुण ही बनते हैं। नाड़ी के स्थानपर द्विजों को गोत्र का विचार करना चाहिये समगोत्रके विवाहसे उत्पन्न जातक वर्णसंकर होता है और वह श्राद्धके अयोग्य होता हैं। इससे कुलमें पितृदोषको सृष्टि होती है। इससे कुलधर्म नष्ट होता है। विवाह कुलधर्मको रक्षाके लिये किया जाता है। विवाह मात्र दो शरीरोंका मिलन नहीं, अपितु दो अन्तःकरणोंका या संस्कारोंका मिलन है। विवाह केवल उत्सव नहीं, संस्कार या पाणिग्रहण (आजीवन सहयोगनिर्वाहकी प्रतिज्ञा) है। इस पवित्र बन्धन (जो अग्निके साक्ष्यमें होता है) का हमें सम्मान करना चाहिये। ज्योतिष इस में सहायक है।
अपकृष्ट ज्योतिषियों ने कालसर्प योग नाम से एक भय रचा है, जो वस्तुत: है नहीं। यह अविचार्य है। कुज (मंगल) दोष का विचार विवाह पूर्व कन्या के विवाह के प्रसंग में देखा जाता है। जब कोई कन्या रही नहीं तो ऐसी वयस्का के विवाह हेतु यह भी अब अविचार्य ही प्रतीत होता है। दाम्पत्यजीवनमें जो घटित होता है, वह होकर ही रहेगा। इसका निवारण नहीं है। इसके समाधानहेतु प्रशस्त उपाय करनेमें क्या जाता है ? जो जब, जहाँ होना है, वह पूर्वनिश्चित है। यह सब कुण्डलीगत ग्रहोंक अनुसार होगा। अतएव सब कुछ सहज होते देना चाहिये जीवनमें ज्योतिषका उपयोग दालमें नमकके समान स्वादवर्धनार्थ है, न कि उदरभरणार्थ दाम्पत्यका निर्वाह सन्तोष, सहनशीलता, सदाचरणसे होता है। दाम्पत्यक्लेश स्वार्थपरता, सेवाहीनता एवं पारस्परिक हिन्द्रान्वेषणसे होता है। कुण्डलीसे समाधान नहीं है। भाग्यका विधान अटल है। युगल-दम्पती यदि अपनेको एक घंटे (ईश्वर- इष्ट) से बाँध लें तो शुभ घटित होता है। जितने भी ज्योतिषीय उपाय हैं, वे सब तात्कालिक हैं। उग्र पुरुषार्थसे अभीष्ट सिद्धि होती है। मनुष्य स्वयं भाग्यविधाता है, काल इसका प्रस्तोता है।
प्रत्येक कुण्डली गुणदोषयुक्त होती है। कुण्डली में पाँच ग्रहोंके उच्च में होनेका जो फल है, वही फल पाँच ग्रहों के नीच में होने का भी है। दोनों स्थितियों में जीवन कण्टकाकीर्ण होता है तथा प्रशस्तिपूर्ण भी एकपक्षीय दृष्टि से कुण्डली पर कभी विचार नहीं करना चाहिये, हर कोण से कुण्डली को देखना है। कारण का ज्ञान होने पर ही निवारणका प्रयास करना साधु है। कुण्डली में सदैव आशा की किरण खोजनी चाहिये। यह किरण नहीं है तो इसे उत्पन्न करना चाहिये। सकारात्मक दृष्टि लभ्य एवं प्रशस्त्य है। प्रश्न पूछा जाता है। उसका उत्तर दिया जाता है। प्रकृति पूछती है, प्रकृति उत्तर देती है। प्रकृतिके उत्तर में समाधान होता है। ऐसा तब होता है, जब दोनों कुटिल न हों। 'संत सरल चित जगत हित' (रा०च०मा० (१ । ३ ख ) । सन्त सदैव समाधान देता है। किसे ? जो उसकी शरणमें जाता है। अहंकारी कभी शरणमें नहीं जाता। शरणागतका उद्धार होता है, अभिमानीका पतन । ज्योतिषी क्या करेगा? मानवकृत समस्याका समाधान मानुषज्योतिषीके पास है। प्राकृतिक समस्याका हल केवल प्राकृतिक सन्तके पास है।
लोकमें प्रश्न पूछा जाता है। समाधानयुक्त उत्तरके लिये लोकमें प्राच्य प्रचलित अनेक साधन हैं। यथा-
१- जन्मकुण्डलीके ग्रहोंके आधारपर ।
२- प्रश्न लग्नकी कुण्डली बनाकर ।
३- शारीरिक संरचनाको ध्यानमें रखकर ।
४-आंगिक चेष्टाओंका अवलोकनकर।
५- मुखमण्डलपर उपस्थित भावको पढ़कर। ६- हाथकी रेखाओंको अच्छी तरह देखकर । ७- व्यक्तिकी वेषभूषा एवं अलंकरणसे।
८- व्यक्तिकी स्वाभाविक चाल या गतिसे । ९- व्यक्तिकी नाड़ी की गतिको जानकर । १०- व्यक्तिके मुख से निकले हुए वाक्य से। ११- व्यक्तिके आवास एवं तद्धृत वस्तुओं को देखकर |
१२- तात्कालिक शकुन या प्राकृतिक घटनाओं से ।
१३- स्वयं के श्वास-प्रश्वास या स्वरज्ञान से। १४- स्वप्न में घटित दृश्योंके आधार पर । १५- अदृश्य शक्तियों के संवाद से ।
१६- कालदर्शनकी सिद्धिसे ।
१७- सहज अनुभूत अन्तर्ज्ञानसे ।
शिवजी आदि ज्योतिषी (ज्ञानी) हैं। पार्वतीजी आदि प्रष्टा हैं। गरुड़जी महाज्ञानी हैं। काकभुशुण्डिजी अज्ञानभंजक हैं। ये गरुड़के प्रश्नोंका उत्तर देते हैं। गरुडका समाधान हो जाता है। पार्वतीजीका भी समाधान होता है। वे कहती हैं- 'नाथ कृपाँ मम गत संदेहा' (रा०च०मा० ७ ।१२९ । ८) । शिवजी वास्तविक ज्योतिषी (ज्ञानी) हैं। काकभुशुण्डिजी परम सन्त हैं। ये दोनों सूर्यरूप हैं अर्थात् सकल विश्वके अवलोकनकर्ता- द्रष्टा, बेता हैं। इन्हें हम सादर नमन करते हैं।
ज्योति भीतर है। ज्योति बाहर है। बाहरकी ज्योति भीतरकी ज्योतिको प्रकट करनेके लिये उत्प्रेरकमात्र है। ज्योतिका मूल ऊपर है। इसकी शाखाएँ (किरणें) नीचेतक फैली हैं। इतनामात्र ज्योतिष है-
"ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥"
(गीता १५।१)
ज्योतिका मूल सूर्य ऊपर है। इस सूर्यकी शाखाएँ (किरणें) नीचे भूमितक फैली हैं। यह सूर्य अश्वत्थ (अश्नाति अन्धकारम्) अर्थात् अन्धकारका अशन- भक्षण करनेवाला शाश्वत है। पृथ्वीको आच्छादित करनेवाले चन्द्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि आदि ग्रह पर्ण (रक्षक) हैं। जो इस तथ्यको जाने, उसे ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। अन्य प्रकारसे ज्ञानका मूलस्रोत मस्तिष्कदेहोपरि सिरमें है। इससे निकली हुई तन्त्रिकाएँ देहांगोंमें नीचेतक फैली हुई हैं। संवेदनाका भक्षण करनेसे यह मस्तिष्क अश्वत्थ है। यह आजीवन अक्षीण रहता है। शरीरमें फैली समस्त ग्रन्थियाँ इसकी पोषक (पूर्ण) हैं। इसका बोध जिसे है, वह वेदज्ञ ज्योतिषी है। यह शरीर वेद है। इसका कारक लग्नपति सूर्य है। इसका मूल सिर है, दोनों हाथ एवं दोनों पैर इसकी शाखाएँ हैं। यह देह सन्ततिप्रवाहके कारण अव्यय / अविनाशी है। त्वचा, नख, केश, रोमादि इसके पर्ण हैं। इसका ज्ञाता ब्रह्मज्ञ है। ज्योतिष-पुरुषका वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं-
"नमो द्विशीर्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे ।
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥"
(श्रीमद्भा० ८। १६ । ३१)
जिसके दो सिर (उत्तरायण, दक्षिणायन) हैं, उस पुरुषको नमस्कार। उस पुरुषके तीन पैर (ब्रह्मलोकको छूनेवाला, अन्तरिक्षमें फैलनेवाला, भूलोकतक आनेवाला प्रकाश) हैं। उसके चार सींगें (प्रातः कालीन, मध्याह्निक, सायंकालीन, आर्धरात्रिक- निशीथ स्थितियाँ) हैं। वह तन्तुमान् (सर्वव्यापी) है। उसके सात हाथ (सप्तवर्णक्रम इन्द्रचापरूप) हैं। वह यज्ञस्वरूप (सहजप्रकाशदाता) है। वह सदैव त्रयीविद्यात्मक है। (सत्, रज, तमसे उपवीत) है। यह ज्योतिपुरुष सूर्य ही है। वेद इसका उद्घोष इस प्रकार करता है-
"चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्योंँ आ विवेश ॥"
(ऋ० ४।५८।३)
परमात्मा सूर्य एकमात्र ज्योतिपुरुष है। यह चार सींगोंवाला है-चारों दिशाओंके अन्धकारका छेदन करता रहता है। इसके तीन पैर हैं- इसकी किरणें भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोकतक गतिशील हैं। यह दो शीर्षवाला है-छः मास उत्तरगोलमें तथा छः मास दक्षिणगोलमें रहता है। इसके सात हाथ हैं- इसका प्रकाश सप्त वर्णोंवाला है। यह ज्योतिपुरुष त्रिधावद्ध है-चर, अचर एवं द्विस्वभावराशियों में विचरता है अथवा पूर्वी क्षितिजसे उदित होता है तथा पश्चिमी क्षितिजमें समा जाता है और आकाशके मध्यमें चरमको प्राप्त होता है। यह पुरुष वृषभ है- वर्षाका कारक है तथा प्रकाशमान । इसके आगमनका स्वागत करनेके लिये खगगण शब्द करते या चहचहाते हैं। यह ज्योतिपुरुष महान् देवता है। यह सभी मर्त्यो अथवा प्राणियों में सतत प्रविष्ट है। जो इस ज्योतिपुरुष सूर्यको नहीं जानता, वह श्रेष्ठ ज्योतिषी नहीं है।
अधिकांश विख्यात ज्योतिषी अपने ज्योतिष-व्यवसायमें तन्त्रका आश्रय लेते हैं। ज्योतिष विद्या है, तन्त्र विज्ञान है। टोना-टोटका भी विज्ञान है। प्रेतविद्याका प्रयोग भी विज्ञान है। इन मायावी विद्याओंका ज्योतिषके स्थानपर या ज्योतिष नामसे प्रयोग किया जाता है। यह सब अद्भुत, किंतु सत्य तथा बुद्धिको चमत्कृत करनेवाला है। इसके व्यापार में कुटिलता एवं दाँव-पेच अधिक है। समस्त अपकर्म, कुकर्म इनकी छायामें किये जाते हैं। ऐसे क्षुद्र लोग आध्यात्मिक पुरुष या सिद्धके रूपमें पूजे जाते हैं। इनमेंसे अपवादरूपमें कुछ अच्छे होते हैं। इन विद्याओंसे सम्पन्न लोग काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मद, लोभसे ग्रसित होकर जघन्य निन्द्य कर्मोंमें संलग्न रहकर ज्योतिषदूषणके रूपमें जी रहे हैं। इन छद्म ज्योतिषियों से सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवनके अन्त्यभाग में ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इनके वंशों का उच्छेद होना देखा जाता है। पापकर्मसे प्राप्त धन एवं कीर्ति दोनों उनके लिये अशुभ होते हैं।
सुकृति से सौभाग्य, दुष्कृतिसे दुर्भाग्यका होना सहज है। ज्योतिषी जब अपना भाग्य नहीं सुधार सकता तो औरोंका क्या ठीक करेगा? दुःखके बीजसे सुखका अंकुर फूटता है। सुखके फलमें दुःखकी गुठली होती है। दुःख-सुख दोनों सहजात एवं अन्योन्याश्रित हैं। दुःखसे बचना सम्भव नहीं। सुख पानेके उपक्रममें दुःख मिलता है। दुःख बिना प्रयत्न किये ही मिलता है। कुण्डलीमें छः भाव सुखके तथा छः भाव दुःखके हैं। जीवनके सन्तुलनके लिये यह प्राकृतिक व्यवस्था है। सुख प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिलता। जैसे बिना प्रयत्न दुःख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न सुख मिलता है। इसे जानना चाहिये और जानकर शान्त रहना चाहिये। 'चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च' जो हम बोते या भूमिको देते हैं, वह हमें कई गुना होकर मिलता- वापस लौटता है। इस न्यायसे सुख दूसरोंको बाँटेंगे तो वह कई गुना होकर हमारे पास आयेगा। यदि हम दूसरोंको दुःख देंगे तो वह भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। यही वास्तवमें ज्योतिष है। हम अपने सुख-दुःख, सौभाग्य- दुर्भाग्यके स्वयं उत्तरदायी हैं। विधाता या अन्य किसीपर आरोप मढ़ना असमीचीन है-
"सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ।
अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥"
(अध्यात्मरामायण २।६।६)
स्वकर्मसूत्र से हमारी जन्मकुण्डली बनी है। इस बात को गोस्वामीजी इस प्रकार कहते हैं-
"काहुन कोउ सुख दुख कर दाता।
निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥"
(रा०च०मा० २।९२।४)
"जनम मरन सब दुख सुख भोगा।
हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥
काल करम बस होहिं गोसाईं ।
बरबस राति दिवस की नाई ॥"
(रा०च०मा० २ । १५०/५-६ )
"करम प्रधान बिस्व करि राखा ।
जो जस करड़ सो तस फल चाखा ॥" (रा०च०मा० २।२१९ । ४)
ज्योतिषशास्त्र कर्मफलसूचक शास्त्र है। कर्मफल अटल एवं भोग्य हैं। इसे बिना भोगे छुटकारा नहीं है।
भले ही किसी एक जातकका कर्मफल दूसरा भोगे, पर बलात् नहीं स्वेच्छा से। सन्तजन ऐसा करते हैं। इसलिये कर्म को भोग के कारण के रूप में जानना चाहिये। यद्यपि इसकी गति बड़ी गहन है-'कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं ..... गहना कर्मणो गतिः'। (गीता ४।१७)
किस जन्मका कर्मफल भोगा है ? किस कारण यह कर्म हुआ? यह सब जानना कठिन है। कर्मविपाक प्रारब्ध है।
ज्योतिष सत् - शास्त्र है, धर्मसे संवलित एवं मर्यादित है। ज्योतिषी धर्मज्ञ होता है। धर्मनिरपेक्ष धर्मकी अवहेलना करता है। धर्मनिरपेक्षता पापकी जननी है। ज्योतिष धर्मसापेक्ष शास्त्र है। इस शास्त्रको हमारा सहस्र नमस्कार ।
सबको अपना भविष्य जाननेकी इच्छा होती है । ज्योतिष जिज्ञासुके लिये है। जातकको स्वयंके बारेमें जाननेका उद्योग करना स्वाभाविक है। कुण्डलीमें भूतसे भविष्यपर्यन्त सम्पूर्ण वृत्त समाहित है। आत्मज्ञान ज्योतिष है। आत्मज्ञानीके सम्मुख मैं सतत विनत एवं प्रणत हूँ- यस्मै कस्मै तस्मै ज्योतिषे नमः ।
इतिहास, पुराण, रामायण, तन्त्र एवं इतर ग्रन्थोंमें एतत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि के प्रत्यक्ष गोचर तथा राहु- केतुके अप्रत्यक्ष प्रभाव की संयुक्त विधा से ग्रहनक्षत्रजन्य ज्योतिष का आविष्कार हमारे पूर्वजोंने किया। इस ज्योतिषवृक्षका मूल सिद्धान्त है, तना संहिता है, फल भविष्यकथन है। जैसे फलहीन वृक्ष व्यर्थ है, वैसे ही फलितशास्त्र (परिणामवाचन) के बिना ज्योतिष बुद्धिका बोझ है। फलित मनुष्यका मार्गदर्शक है। समाज फलितज्ञ आदरणीय है। शुष्क ज्ञान, जिसका जीवनमें उपयोग नहीं है, त्याज्य है। जीवन के संवर्धन, मार्गदर्शन हेतु उपयोगी समस्त ज्ञान ज्योतिष की परिधि में आता है। यह ज्योतिषीय ज्ञान व्यावहारिक होने से वरेण्य एवं वर्ण्य है। इसीका वर्णन ज्योतिर्विद महर्षियों ने किया है।
माताके गर्भ से बाहर आनेवाला शरीरधारी जीव जातक कहलाता है। समयसापेक्ष ग्रह-नक्षत्रोंकी स्थितिसे जातकके विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसकी सत्यता का आधार सिद्धान्त एवं लोकव्यवहार से युक्त उहा एवं सत्यनिष्ठा है। असत्यमें प्रतिष्ठित व्यक्तिका ज्ञान अफल होता है, वाणी विफल होती है. क्रिया निष्फल होती है। ज्योतिषी सत्यके प्रति दृढ़- संलग्न होता है, वह सत्यचर्या में रहता है और निर्भय तथा निर्लोभ होता है।
नवग्रह, द्वादश भाव एवं द्वादश राशियोंकि त्र्यम्बकमे ज्योतिष- पुरुषका शरीर बनता है। यह ज्योतिषपुरुष ही काल है। इसका ज्ञाता कालज्ञ कहलाता है। सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु नवग्रह है। ये सभी उदय एवं अस्त होते रहते हैं उदय दृश्य। अस्त अदृश्य राहु-केतु उदयास्त से परे हैं, छाया ग्रह हैं। होना मात्र इनकी वास्तविकता है। अति प्रभावशाली होनेसे ये सतत मान्य हैं। इनका कोई अपना घर नहीं है। ये किरायेके घरमें अथवा बलात् दूसरेके घरमें रहते हैं। ये सदैव वामावर्त (वक्री) रहते हैं। ये स्थिर गति से चलते हैं तथा प्रत्येक राशिमें १८ महीने रहते हैं। सूर्य सदैव स्थिर स्वभावका तथा चन्द्रमा अस्थिर स्वभावका है। बुध और बृहस्पति नित्य द्विस्वभावके हैं। शुक्र, शनि, मंगल- ये तीनों कभी स्थिर और कभी अस्थिर स्वभाव रखते हैं राहु-केतुका अपना कोई स्वभाव नहीं ये जिस राशिमें रहते हैं, उसीके स्वभावको अपना लेते हैं।
नवग्रहोंमें दो वर्ग हैं-देव, दैत्य। सूर्य, मंगल, शुक्लपक्षका चन्द्रमा, बृहस्पति, केतु देववर्गमें आते हैं। शुक्र, शनि, बुध, राहु, कृष्णपक्षका चन्द्रमा दैत्यवर्गमें आते हैं। किसीसे वैर न रखनेवाला चन्द्रमा दोनों पक्षोंमें मान्य है। चन्द्रमा मन प्रत्येक व्यक्तिका मन कभी देव तो कभी दैत्यके गुणोंवाला होता है। वृद्धिको प्राप्त चन्द्रमा देव है। ह्रासमाण चन्द्रमा दैत्य है। मेष-वृश्चिक, धनु मीन, कर्क- सिंह राशियाँ देववर्गकी हैं। वृष-तुला, मिथुन- कन्या, मकर कुम्भ राशियाँ दैत्यवर्गकी हैं। कर्कराशिवाला व्यक्ति शुक्लपक्षी होनेपर देववर्गमें तथा कृष्णपक्षी होनेपर दैत्यवर्गमें गिना जाता है। स्वभाव-निर्धारणमें यह विशेष ध्यातव्य है। राहु-केतु कुटिल ग्रह हैं। लग्न या चन्द्रमाके साथ रहनेपर ये स्वभावनियन्ता होते हैं। केतु प्रकाश है। राहु अन्धकार है। उच्चतर ज्ञान केतु है। निम्नतर विद्या राहु है। दोनों गूढ ग्रह हैं तथा अपने- अपने वर्गमें बलिष्ठ हैं। मंगलका पोष्य केतु है। शनिका पोष्य राहु है। शरीरमें कटिके ऊपरका भाग केतु है, नाभिके नीचेका भाग राहु है। सिरके केश केतु हैं, अधो स्थानके बाल राहु हैं। व्यक्तिको भूमिपर पड़ती छाया राहु है तथा पानी या दर्पणमें पड़ती छाया केतु है। राहु सदा अधोगामी मूल है तो केतु उपरिगामी तना। केतु दिन है। राहु रात्रि है। केतु आत्मगौरव है। राहु आत्माभिमान है। राहु-केतुके इस भेदको जो जाने, वही ज्योतिष में निष्णात है।
स्वयंको जानना ही ज्योतिषशास्त्रका लक्ष्य है। बाह्य ऐश्वर्यके लिये ज्योतिष नहीं है, स्वयंमें निहित आन्तरिक ऐश्वर्यके दर्शनके लिये ज्योतिष है। सुपात्रको सब कुछ मिलता है, कुपात्रको कुछ नहीं मिलता। इस सत्यघोषको कौन नकारेगा? व्यक्तिको सर्वप्रथम अपना लग्न जानना चाहिये। लग्न जन्मसमय-पूर्वी क्षितिजमें उदित राशि। १२ राशियाँ होनेसे १२ लग्न हैं। इसे भूलग्न कहते हैं। चन्द्रमा जन्मसमयमें जिस राशिमें होता है, उसे चन्द्रलग्न कहते हैं। राशि चक्रकी आदिराशि मेष है। इसकी ब्रह्मलग्न संज्ञा है। प्रकृति महत्तत्त्व/मस्तिष्कसंरचनाका ज्ञान हाँसे होता है। इन तीन लग्नोंके समयेत अध्ययन व्यक्तिको अपनी प्रकृतिका बोध होता है बोधके पश्चात् तदनुकूल कर्म करनेसे मोक्षका मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ ज्योतिषीय ज्ञानकी सार्थकता है। ज्योतिषमें आत्मनिष्ठा सर्वोपरि है, वस्तुनिष्ठा गौण है। जो स्वयं अन्धा है, वह दूसरेको क्या दिशानिर्देश देगा? स्वयंके लिये ज्योतिष अपनाना साधु है, परार्थ असाधु है।
प्रत्येक ग्रहक्ष के भाव या राशि जन्य बारह फल हैं। नवग्रहों एवं चारह भावों या राशियों के योग से १२×९=१०८ फल या परिणाम होते हैं। जिसे इसका पूर्ण ज्ञान है, उसे श्री१०८ के अलंकरण को भूषित माना जाता है। ज्योतिष के व्यापारी एवं ज्योतिष के आचारी अलग-अलग है। दोनों का कोई मेल नहीं। ज्योतिष फलकथनों पारपद्धति सर्वतोमुख एवं विश्वमान्य है। विंशेत्तरीदशापद्धति का विज्ञान अत्यन्त गूढ़ है। २७ नक्षत्रोंपर ९ ग्रहोंका स्वामित्व तथा प्रत्येक ग्रहकी दशावर्षसंख्या बौद्धिक तर्क से परे है। सटीक फल देनेसे यह सुमान्य है। यह सर्वविदित एवं प्रायोगिक सत्य है। दशान्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा, सूक्ष्मदशा प्राणदशापर्यन्त गणना केवल विंशोत्तरी प्रणाली में है। इससे व्यवस्थामें अव्यवस्था तथा अव्यवस्थायें व्यवस्थाका परिज्ञान होता है। प्रत्येक शुभ अशुभ तथा अशुभ शुभका होना इसका प्रमाण है। निश्चितता में अनिश्चितता तथा अनिश्चितताएँ निश्चितता अथवा अप्रत्याशित फलका होना ज्योतिषसे प्रमाणित है। प्रत्येक जातक को अकालमृत्युका सामना करना पड़ता है। प्रत्येक जातककी मृत्यु चन्द्रमाको प्राणदशामें होती है। यह घटी-पलात्मक होती है। इसमें वेदवाक्य प्रमाण हैं- चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः (अथर्व० १४।१।२४ एवं ७ । ८५ । २) । चन्द्रमाके द्वारा दीर्घायुका उल्लंघन - नाश किया जाता है। अर्थात् चन्द्रमा अकालमृत्युका कारक है। चन्द्रमा (मन) प्रतिक्षण क्षीण या वृद्धिको प्राप्त होता रहता है। इसलिये यह आयुका हारक अथवा कारक है। जातककी मृत्यु तो निश्चित है, आयु निश्चित नहीं है। आयुका संकोच एवं विस्तार जातकके अधिकारमें है। आयु (जीवन-विस्तार) का आधार उसके पूर्वजन्मके कर्मफल हैं। हम अपने एवं अपने लोगोंके वर्तमान कमसे अपनी आयुका नाशन एवं वर्धन करते रहते हैं। विकर्मसे आयुका संकोच होता है। सुकर्मसे आयुका विस्तार होता है। इस सत्यसे जो परिचित है, वही सच्चा ज्योतिषी है।
आयुकी सूक्ष्म गणना करना व्यर्थ किंवा सुमूर्खता है। स्थूलरूपसे दीर्घायु मध्यायु एवं अल्पायुका ज्ञान ही पर्याप्त है। तन्यका परिमापन करनेसे क्या लाभ? विषादसे आयु क्षीण होती है, प्रसादसे आयु बढ़ती है। विषाद एवं प्रसादका वासस्थान मन है। 'चन्द्रमा मनसो जातः' (अथर्व० १९।६।७) । मनसे स्थूल शरीर प्रभावित होता है। स्थूल शरीर या लग्नका कारक सूर्य है। सूर्य आत्मा (शरीर प्राण) है कथन है-'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' (यजु० १३। ४६) । इसलिये कुण्डलीमें चन्द्रमा एवं सूर्यकी स्थिति एवं बलका आकलनकर आयुकी उहा करनी चाहिये। महर्षि पराशर के अनुसार कलियुगमें मनुष्यकी सामान्य आयु १२० वर्ष है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित आयु देता है। सूर्य ६ वर्ष, चन्द्रमा १० वर्ष, मंगल ७ वर्ष, राहु १८ वर्ष, गुरु १६ वर्ष, शनि १९ वर्ष, बुध १७ वर्ष, केतु ७ वर्ष, शुक्र २० वर्ष है। सबका योग १२० वर्ष है। इसपर क्यों कहना अनुचित है। यह है और ध्रुव सत्य है।
वैवाहिक सम्बन्धोंमें कुण्डली मिलान एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। आधुनिक समयमें कुल एवं गुणको प्रधानता न देकर अर्थ एवं स्वार्थको वरीयता दी जा रही है। विवाहमें अवरोध डालनेके लिये कुण्डलीका उपयोग हो रहा है। विवाह अब क्रय-विक्रयका सेतु एवं पाखण्डका प्रतीक है। कन्याके विवाहके सन्दर्भमें नाडीका विचार किया जाता है, किंतु अब कन्याका विवाह होता कहाँ है? इसलिये वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण एवं भकूटपर्यन्त गुणोंका विचार करना समीचीन है। यहाँतक २८ गुण ही बनते हैं। नाड़ी के स्थानपर द्विजों को गोत्र का विचार करना चाहिये समगोत्रके विवाहसे उत्पन्न जातक वर्णसंकर होता है और वह श्राद्धके अयोग्य होता हैं। इससे कुलमें पितृदोषको सृष्टि होती है। इससे कुलधर्म नष्ट होता है। विवाह कुलधर्मको रक्षाके लिये किया जाता है। विवाह मात्र दो शरीरोंका मिलन नहीं, अपितु दो अन्तःकरणोंका या संस्कारोंका मिलन है। विवाह केवल उत्सव नहीं, संस्कार या पाणिग्रहण (आजीवन सहयोगनिर्वाहकी प्रतिज्ञा) है। इस पवित्र बन्धन (जो अग्निके साक्ष्यमें होता है) का हमें सम्मान करना चाहिये। ज्योतिष इस में सहायक है।
अपकृष्ट ज्योतिषियों ने कालसर्प योग नाम से एक भय रचा है, जो वस्तुत: है नहीं। यह अविचार्य है। कुज (मंगल) दोष का विचार विवाह पूर्व कन्या के विवाह के प्रसंग में देखा जाता है। जब कोई कन्या रही नहीं तो ऐसी वयस्का के विवाह हेतु यह भी अब अविचार्य ही प्रतीत होता है। दाम्पत्यजीवनमें जो घटित होता है, वह होकर ही रहेगा। इसका निवारण नहीं है। इसके समाधानहेतु प्रशस्त उपाय करनेमें क्या जाता है ? जो जब, जहाँ होना है, वह पूर्वनिश्चित है। यह सब कुण्डलीगत ग्रहोंक अनुसार होगा। अतएव सब कुछ सहज होते देना चाहिये जीवनमें ज्योतिषका उपयोग दालमें नमकके समान स्वादवर्धनार्थ है, न कि उदरभरणार्थ दाम्पत्यका निर्वाह सन्तोष, सहनशीलता, सदाचरणसे होता है। दाम्पत्यक्लेश स्वार्थपरता, सेवाहीनता एवं पारस्परिक हिन्द्रान्वेषणसे होता है। कुण्डलीसे समाधान नहीं है। भाग्यका विधान अटल है। युगल-दम्पती यदि अपनेको एक घंटे (ईश्वर- इष्ट) से बाँध लें तो शुभ घटित होता है। जितने भी ज्योतिषीय उपाय हैं, वे सब तात्कालिक हैं। उग्र पुरुषार्थसे अभीष्ट सिद्धि होती है। मनुष्य स्वयं भाग्यविधाता है, काल इसका प्रस्तोता है।
प्रत्येक कुण्डली गुणदोषयुक्त होती है। कुण्डली में पाँच ग्रहोंके उच्च में होनेका जो फल है, वही फल पाँच ग्रहों के नीच में होने का भी है। दोनों स्थितियों में जीवन कण्टकाकीर्ण होता है तथा प्रशस्तिपूर्ण भी एकपक्षीय दृष्टि से कुण्डली पर कभी विचार नहीं करना चाहिये, हर कोण से कुण्डली को देखना है। कारण का ज्ञान होने पर ही निवारणका प्रयास करना साधु है। कुण्डली में सदैव आशा की किरण खोजनी चाहिये। यह किरण नहीं है तो इसे उत्पन्न करना चाहिये। सकारात्मक दृष्टि लभ्य एवं प्रशस्त्य है। प्रश्न पूछा जाता है। उसका उत्तर दिया जाता है। प्रकृति पूछती है, प्रकृति उत्तर देती है। प्रकृतिके उत्तर में समाधान होता है। ऐसा तब होता है, जब दोनों कुटिल न हों। 'संत सरल चित जगत हित' (रा०च०मा० (१ । ३ ख ) । सन्त सदैव समाधान देता है। किसे ? जो उसकी शरणमें जाता है। अहंकारी कभी शरणमें नहीं जाता। शरणागतका उद्धार होता है, अभिमानीका पतन । ज्योतिषी क्या करेगा? मानवकृत समस्याका समाधान मानुषज्योतिषीके पास है। प्राकृतिक समस्याका हल केवल प्राकृतिक सन्तके पास है।
लोकमें प्रश्न पूछा जाता है। समाधानयुक्त उत्तरके लिये लोकमें प्राच्य प्रचलित अनेक साधन हैं। यथा-
१- जन्मकुण्डलीके ग्रहोंके आधारपर ।
२- प्रश्न लग्नकी कुण्डली बनाकर ।
३- शारीरिक संरचनाको ध्यानमें रखकर ।
४-आंगिक चेष्टाओंका अवलोकनकर।
५- मुखमण्डलपर उपस्थित भावको पढ़कर। ६- हाथकी रेखाओंको अच्छी तरह देखकर । ७- व्यक्तिकी वेषभूषा एवं अलंकरणसे।
८- व्यक्तिकी स्वाभाविक चाल या गतिसे । ९- व्यक्तिकी नाड़ी की गतिको जानकर । १०- व्यक्तिके मुख से निकले हुए वाक्य से। ११- व्यक्तिके आवास एवं तद्धृत वस्तुओं को देखकर |
१२- तात्कालिक शकुन या प्राकृतिक घटनाओं से ।
१३- स्वयं के श्वास-प्रश्वास या स्वरज्ञान से। १४- स्वप्न में घटित दृश्योंके आधार पर । १५- अदृश्य शक्तियों के संवाद से ।
१६- कालदर्शनकी सिद्धिसे ।
१७- सहज अनुभूत अन्तर्ज्ञानसे ।
शिवजी आदि ज्योतिषी (ज्ञानी) हैं। पार्वतीजी आदि प्रष्टा हैं। गरुड़जी महाज्ञानी हैं। काकभुशुण्डिजी अज्ञानभंजक हैं। ये गरुड़के प्रश्नोंका उत्तर देते हैं। गरुडका समाधान हो जाता है। पार्वतीजीका भी समाधान होता है। वे कहती हैं- 'नाथ कृपाँ मम गत संदेहा' (रा०च०मा० ७ ।१२९ । ८) । शिवजी वास्तविक ज्योतिषी (ज्ञानी) हैं। काकभुशुण्डिजी परम सन्त हैं। ये दोनों सूर्यरूप हैं अर्थात् सकल विश्वके अवलोकनकर्ता- द्रष्टा, बेता हैं। इन्हें हम सादर नमन करते हैं।
ज्योति भीतर है। ज्योति बाहर है। बाहरकी ज्योति भीतरकी ज्योतिको प्रकट करनेके लिये उत्प्रेरकमात्र है। ज्योतिका मूल ऊपर है। इसकी शाखाएँ (किरणें) नीचेतक फैली हैं। इतनामात्र ज्योतिष है-
"ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥"
(गीता १५।१)
ज्योतिका मूल सूर्य ऊपर है। इस सूर्यकी शाखाएँ (किरणें) नीचे भूमितक फैली हैं। यह सूर्य अश्वत्थ (अश्नाति अन्धकारम्) अर्थात् अन्धकारका अशन- भक्षण करनेवाला शाश्वत है। पृथ्वीको आच्छादित करनेवाले चन्द्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि आदि ग्रह पर्ण (रक्षक) हैं। जो इस तथ्यको जाने, उसे ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। अन्य प्रकारसे ज्ञानका मूलस्रोत मस्तिष्कदेहोपरि सिरमें है। इससे निकली हुई तन्त्रिकाएँ देहांगोंमें नीचेतक फैली हुई हैं। संवेदनाका भक्षण करनेसे यह मस्तिष्क अश्वत्थ है। यह आजीवन अक्षीण रहता है। शरीरमें फैली समस्त ग्रन्थियाँ इसकी पोषक (पूर्ण) हैं। इसका बोध जिसे है, वह वेदज्ञ ज्योतिषी है। यह शरीर वेद है। इसका कारक लग्नपति सूर्य है। इसका मूल सिर है, दोनों हाथ एवं दोनों पैर इसकी शाखाएँ हैं। यह देह सन्ततिप्रवाहके कारण अव्यय / अविनाशी है। त्वचा, नख, केश, रोमादि इसके पर्ण हैं। इसका ज्ञाता ब्रह्मज्ञ है। ज्योतिष-पुरुषका वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं-
"नमो द्विशीर्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे ।
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥"
(श्रीमद्भा० ८। १६ । ३१)
जिसके दो सिर (उत्तरायण, दक्षिणायन) हैं, उस पुरुषको नमस्कार। उस पुरुषके तीन पैर (ब्रह्मलोकको छूनेवाला, अन्तरिक्षमें फैलनेवाला, भूलोकतक आनेवाला प्रकाश) हैं। उसके चार सींगें (प्रातः कालीन, मध्याह्निक, सायंकालीन, आर्धरात्रिक- निशीथ स्थितियाँ) हैं। वह तन्तुमान् (सर्वव्यापी) है। उसके सात हाथ (सप्तवर्णक्रम इन्द्रचापरूप) हैं। वह यज्ञस्वरूप (सहजप्रकाशदाता) है। वह सदैव त्रयीविद्यात्मक है। (सत्, रज, तमसे उपवीत) है। यह ज्योतिपुरुष सूर्य ही है। वेद इसका उद्घोष इस प्रकार करता है-
"चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्योंँ आ विवेश ॥"
(ऋ० ४।५८।३)
परमात्मा सूर्य एकमात्र ज्योतिपुरुष है। यह चार सींगोंवाला है-चारों दिशाओंके अन्धकारका छेदन करता रहता है। इसके तीन पैर हैं- इसकी किरणें भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोकतक गतिशील हैं। यह दो शीर्षवाला है-छः मास उत्तरगोलमें तथा छः मास दक्षिणगोलमें रहता है। इसके सात हाथ हैं- इसका प्रकाश सप्त वर्णोंवाला है। यह ज्योतिपुरुष त्रिधावद्ध है-चर, अचर एवं द्विस्वभावराशियों में विचरता है अथवा पूर्वी क्षितिजसे उदित होता है तथा पश्चिमी क्षितिजमें समा जाता है और आकाशके मध्यमें चरमको प्राप्त होता है। यह पुरुष वृषभ है- वर्षाका कारक है तथा प्रकाशमान । इसके आगमनका स्वागत करनेके लिये खगगण शब्द करते या चहचहाते हैं। यह ज्योतिपुरुष महान् देवता है। यह सभी मर्त्यो अथवा प्राणियों में सतत प्रविष्ट है। जो इस ज्योतिपुरुष सूर्यको नहीं जानता, वह श्रेष्ठ ज्योतिषी नहीं है।
अधिकांश विख्यात ज्योतिषी अपने ज्योतिष-व्यवसायमें तन्त्रका आश्रय लेते हैं। ज्योतिष विद्या है, तन्त्र विज्ञान है। टोना-टोटका भी विज्ञान है। प्रेतविद्याका प्रयोग भी विज्ञान है। इन मायावी विद्याओंका ज्योतिषके स्थानपर या ज्योतिष नामसे प्रयोग किया जाता है। यह सब अद्भुत, किंतु सत्य तथा बुद्धिको चमत्कृत करनेवाला है। इसके व्यापार में कुटिलता एवं दाँव-पेच अधिक है। समस्त अपकर्म, कुकर्म इनकी छायामें किये जाते हैं। ऐसे क्षुद्र लोग आध्यात्मिक पुरुष या सिद्धके रूपमें पूजे जाते हैं। इनमेंसे अपवादरूपमें कुछ अच्छे होते हैं। इन विद्याओंसे सम्पन्न लोग काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मद, लोभसे ग्रसित होकर जघन्य निन्द्य कर्मोंमें संलग्न रहकर ज्योतिषदूषणके रूपमें जी रहे हैं। इन छद्म ज्योतिषियों से सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवनके अन्त्यभाग में ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इनके वंशों का उच्छेद होना देखा जाता है। पापकर्मसे प्राप्त धन एवं कीर्ति दोनों उनके लिये अशुभ होते हैं।
सुकृति से सौभाग्य, दुष्कृतिसे दुर्भाग्यका होना सहज है। ज्योतिषी जब अपना भाग्य नहीं सुधार सकता तो औरोंका क्या ठीक करेगा? दुःखके बीजसे सुखका अंकुर फूटता है। सुखके फलमें दुःखकी गुठली होती है। दुःख-सुख दोनों सहजात एवं अन्योन्याश्रित हैं। दुःखसे बचना सम्भव नहीं। सुख पानेके उपक्रममें दुःख मिलता है। दुःख बिना प्रयत्न किये ही मिलता है। कुण्डलीमें छः भाव सुखके तथा छः भाव दुःखके हैं। जीवनके सन्तुलनके लिये यह प्राकृतिक व्यवस्था है। सुख प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिलता। जैसे बिना प्रयत्न दुःख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न सुख मिलता है। इसे जानना चाहिये और जानकर शान्त रहना चाहिये। 'चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च' जो हम बोते या भूमिको देते हैं, वह हमें कई गुना होकर मिलता- वापस लौटता है। इस न्यायसे सुख दूसरोंको बाँटेंगे तो वह कई गुना होकर हमारे पास आयेगा। यदि हम दूसरोंको दुःख देंगे तो वह भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। यही वास्तवमें ज्योतिष है। हम अपने सुख-दुःख, सौभाग्य- दुर्भाग्यके स्वयं उत्तरदायी हैं। विधाता या अन्य किसीपर आरोप मढ़ना असमीचीन है-
"सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ।
अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥"
(अध्यात्मरामायण २।६।६)
स्वकर्मसूत्र से हमारी जन्मकुण्डली बनी है। इस बात को गोस्वामीजी इस प्रकार कहते हैं-
"काहुन कोउ सुख दुख कर दाता।
निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥"
(रा०च०मा० २।९२।४)
"जनम मरन सब दुख सुख भोगा।
हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥
काल करम बस होहिं गोसाईं ।
बरबस राति दिवस की नाई ॥"
(रा०च०मा० २ । १५०/५-६ )
"करम प्रधान बिस्व करि राखा ।
जो जस करड़ सो तस फल चाखा ॥" (रा०च०मा० २।२१९ । ४)
ज्योतिषशास्त्र कर्मफलसूचक शास्त्र है। कर्मफल अटल एवं भोग्य हैं। इसे बिना भोगे छुटकारा नहीं है।
भले ही किसी एक जातकका कर्मफल दूसरा भोगे, पर बलात् नहीं स्वेच्छा से। सन्तजन ऐसा करते हैं। इसलिये कर्म को भोग के कारण के रूप में जानना चाहिये। यद्यपि इसकी गति बड़ी गहन है-'कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं ..... गहना कर्मणो गतिः'। (गीता ४।१७)
किस जन्मका कर्मफल भोगा है ? किस कारण यह कर्म हुआ? यह सब जानना कठिन है। कर्मविपाक प्रारब्ध है।
ज्योतिष सत् - शास्त्र है, धर्मसे संवलित एवं मर्यादित है। ज्योतिषी धर्मज्ञ होता है। धर्मनिरपेक्ष धर्मकी अवहेलना करता है। धर्मनिरपेक्षता पापकी जननी है। ज्योतिष धर्मसापेक्ष शास्त्र है। इस शास्त्रको हमारा सहस्र नमस्कार ।
सबको अपना भविष्य जाननेकी इच्छा होती है । ज्योतिष जिज्ञासुके लिये है। जातकको स्वयंके बारेमें जाननेका उद्योग करना स्वाभाविक है। कुण्डलीमें भूतसे भविष्यपर्यन्त सम्पूर्ण वृत्त समाहित है। आत्मज्ञान ज्योतिष है। आत्मज्ञानीके सम्मुख मैं सतत विनत एवं प्रणत हूँ- यस्मै कस्मै तस्मै ज्योतिषे नमः ।
Related Posts
- ज्योतिष विज्ञान
- |
- 07 December 2025
जब विज्ञान और ज्योतिष मिलते हैं: क्वांटम टनलिंग का आध्यात्मिक रहस्य
0 Comments
Comments are not available.