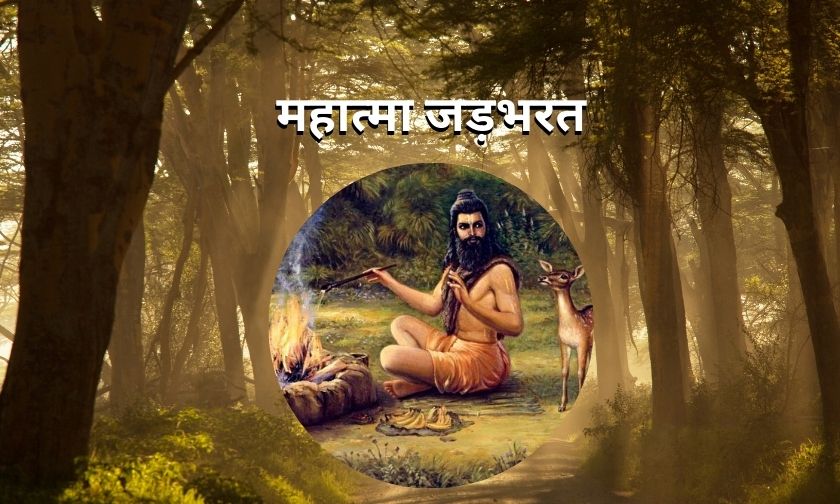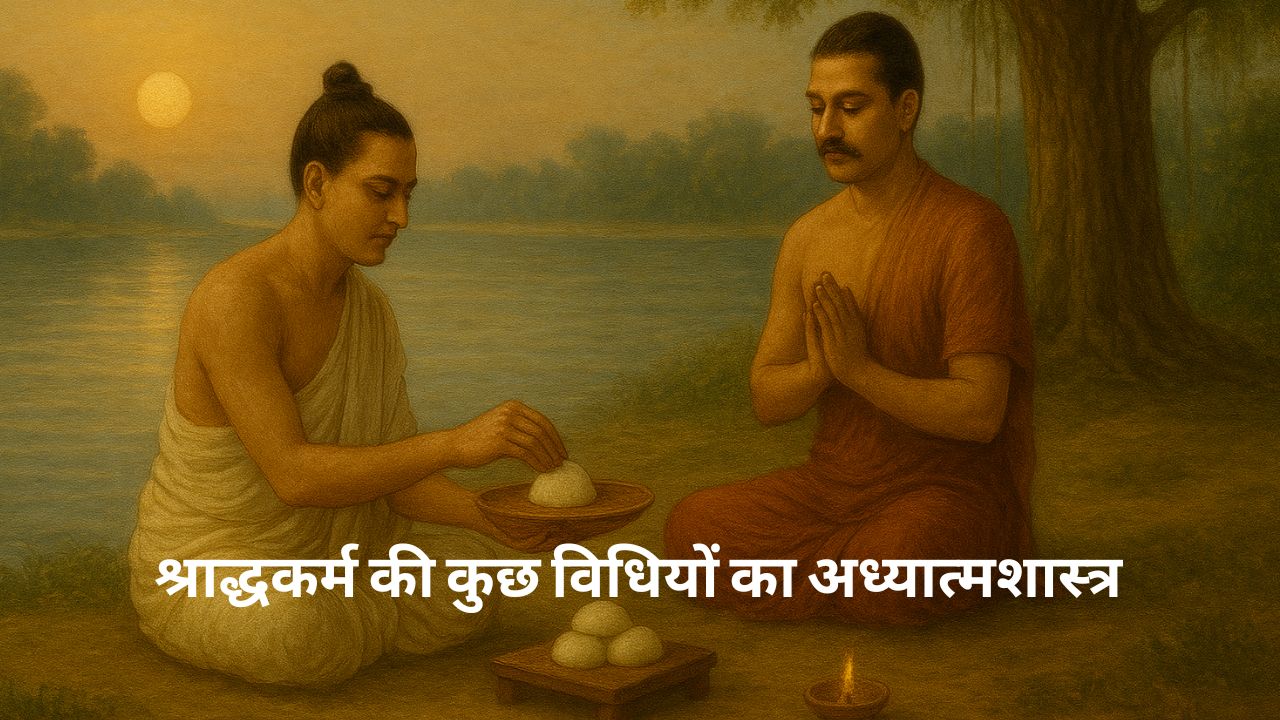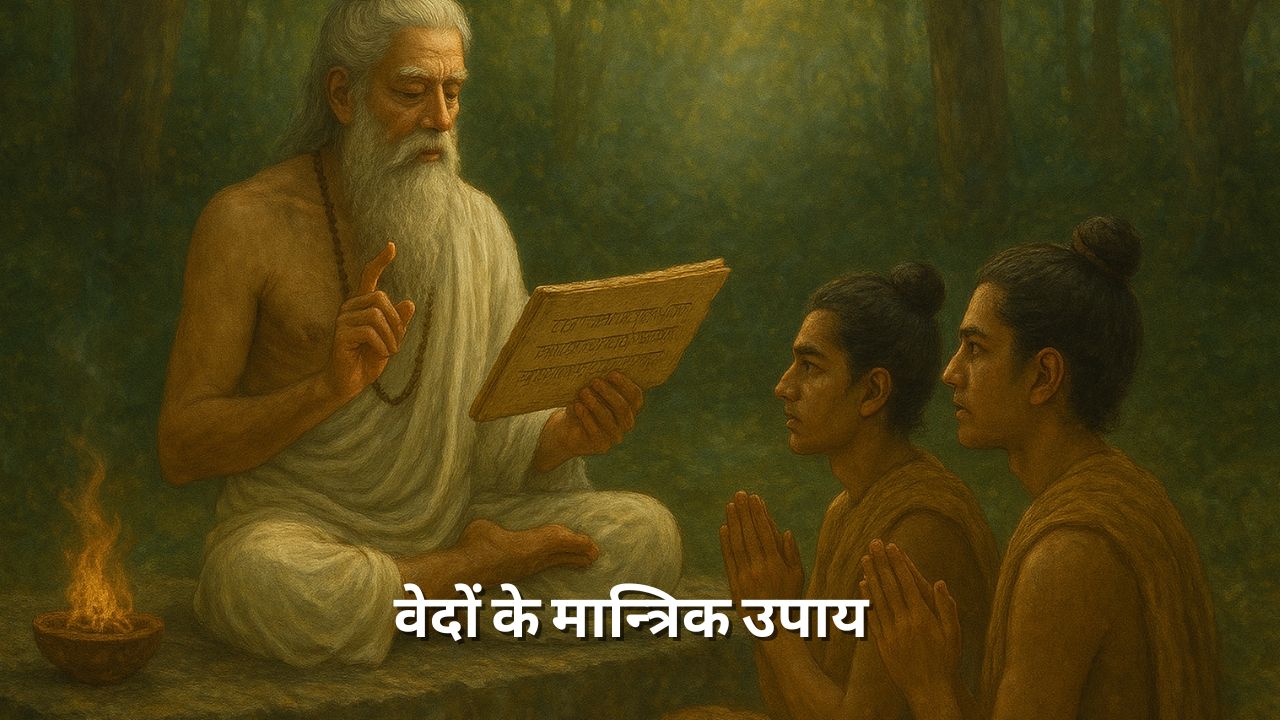- NA
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
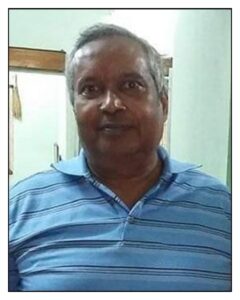 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
Mystic Power - नाग का सामान्य अर्थ सर्प है, किन्तु वेद तथा पुराणों में इसका कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। यह मनुष्य जाति है जिसके भारत तथा विदेशों में कई विभाग हैं। भारत में ब्राह्मणों की एक उपाधि है, कई क्षत्रिय राजा नागेश्वर गोत्र के हैं। वैश्यों में अग्रवाल नाग जाति के हैं, अन्य माहेश्वरी हैं।
भारत के बाहर भी आन्तरिक तथा समुद्री व्यापार करने वाले नाग थे जिनके नाम अभी तक जापान, मेक्सिको, अफ्रीका, मध्य एशिया आदि में सुरक्षित हैं। आठ दिशाओं के नाग ८ महाद्वीपों की सीमा हैं (अनन्त = अण्टार्कटिक सहित)। नग = गति नहीं करने वाला, पर्वत। उसके निवासी भी नाग हैं, जैसे नागालैण्ड।
भारत के ९ खण्डों में एक खण्ड नागद्वीप है जो अण्डमान से सुमात्रा, यवद्वीप तक है। आकाश में ब्रह्माण्ड आदि की सीमा नाग है। ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा भी नाग है, जिसका बाहरी छोर अश्लेषा नक्षत्र है, उसका देवता नाग है। सर्पाकार भुजा का क्षेत्र महः लोक है जिसकी पृथ्वी पर प्रतिमा चीन है (महः के निवासियों को ब्रह्मा ने महान् या हान कहा था) अतः चीन भी नाग क्षेत्र है। नाग या वृत्र आठवां आयाम है, जो कण से लेकर ब्रह्माण्ड तक को घेरने वाली सीमा है। शरीर के भीतर एक उपप्राण वायु नाग है अतः नाग शब्द का व्यवहार ८ संख्या के लिए होता है।
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
Mystic Power - नाग का सामान्य अर्थ सर्प है, किन्तु वेद तथा पुराणों में इसका कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। यह मनुष्य जाति है जिसके भारत तथा विदेशों में कई विभाग हैं। भारत में ब्राह्मणों की एक उपाधि है, कई क्षत्रिय राजा नागेश्वर गोत्र के हैं। वैश्यों में अग्रवाल नाग जाति के हैं, अन्य माहेश्वरी हैं।
भारत के बाहर भी आन्तरिक तथा समुद्री व्यापार करने वाले नाग थे जिनके नाम अभी तक जापान, मेक्सिको, अफ्रीका, मध्य एशिया आदि में सुरक्षित हैं। आठ दिशाओं के नाग ८ महाद्वीपों की सीमा हैं (अनन्त = अण्टार्कटिक सहित)। नग = गति नहीं करने वाला, पर्वत। उसके निवासी भी नाग हैं, जैसे नागालैण्ड।
भारत के ९ खण्डों में एक खण्ड नागद्वीप है जो अण्डमान से सुमात्रा, यवद्वीप तक है। आकाश में ब्रह्माण्ड आदि की सीमा नाग है। ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा भी नाग है, जिसका बाहरी छोर अश्लेषा नक्षत्र है, उसका देवता नाग है। सर्पाकार भुजा का क्षेत्र महः लोक है जिसकी पृथ्वी पर प्रतिमा चीन है (महः के निवासियों को ब्रह्मा ने महान् या हान कहा था) अतः चीन भी नाग क्षेत्र है। नाग या वृत्र आठवां आयाम है, जो कण से लेकर ब्रह्माण्ड तक को घेरने वाली सीमा है। शरीर के भीतर एक उपप्राण वायु नाग है अतः नाग शब्द का व्यवहार ८ संख्या के लिए होता है।
 https://mycloudparticles.com/
१. सर्प-विषधर तथा बिना विष के कई प्रकार के नाग हैं जिनका आयुर्वेद ग्रन्थों में वर्णन है। सामान्यतः वनस्पतियों, खनिजों के लिए नाग तथा जन्तुओं के लिए सर्प शब्द का व्यवहार है। सुश्रुत संहिता, कल्प स्थान, अध्याय ४, ५ में विस्तार से वर्गीकरण दिया है।५ प्रकार के सर्प हैं-(१) दर्वीकर= फण वाले २६ प्रकार के, (२) मण्डली = बिना फण के, विविध मण्डलों से चित्रित, २२ प्रकार के, (३) राजिमन्त = रेखायुक्त, बिना फण के, पुण्डरीक आदि कम विष वाले, १० प्रकार के, (४) निर्विष = गल-लोमी, शूकपत्र आदि १२ प्रकार के, (५) वैकरञ्ज = अन्य जातियों के ३ प्रकार के।
२. नाग वनस्पति-सर्प तथा नाग में अन्तर है यद्यपि इनका समान अर्थ में व्यवहार होता है। गीता (१०/२८-२९) में भगवान् ने अपने को सर्पों में वासुकि तथा नागों में अनन्त कहा है।
आयुर्वेद सन्दर्भ में नाग वनस्पति तथा खनिज ओषधियों के नाम हैं- नाग खनिज, सीसा (रसरत्नसमुच्चय, १/४१), वनस्पति नागकेसर (सुश्रुत सूत्र, ४५/१२, रसर. २१/२५-२८), ताम्बूल (र, २४/१३६), एरण्द (र. २१/२५-२८), सल्लकी (अष्टांग सं, शा, ४/३८), ग्रह भुजंगम (सुश्रुत उत्तर, ६०/३६) देवयोनि वासुकि आदि (सुश्रुत सूत्र, ५/२१), पशुगज (सुश्रुत, चिकित्सा, २८/२६), नाग केसर (सुश्रुत, सूत्र, ४६/२८७), (२) नागा-नाकुली वनस्पति (रस, २१/२९), नागकन्द, हस्तिकन्द, नाग करण्डक, नागकर्ण, नागकुमारी, नागकुमारिका, नागकेसर, नागगन्धा, नागगर्भ, नागचपल, नागचम्पक, नागच्छत्रा, नागज (सिन्दूर), नागतुम्बी (भूतुम्बी, राजनिघण्टु, ७/२४१), नागदन्ती, नागदमनी, नाग पुष्प, नागबला, नागदमनी, नागवल्ली (ताम्बूल), नागराति (वन्ध्याकर्कोटकी), नागेन्दु, नागदन्ती आदि।
https://mycloudparticles.com/
१. सर्प-विषधर तथा बिना विष के कई प्रकार के नाग हैं जिनका आयुर्वेद ग्रन्थों में वर्णन है। सामान्यतः वनस्पतियों, खनिजों के लिए नाग तथा जन्तुओं के लिए सर्प शब्द का व्यवहार है। सुश्रुत संहिता, कल्प स्थान, अध्याय ४, ५ में विस्तार से वर्गीकरण दिया है।५ प्रकार के सर्प हैं-(१) दर्वीकर= फण वाले २६ प्रकार के, (२) मण्डली = बिना फण के, विविध मण्डलों से चित्रित, २२ प्रकार के, (३) राजिमन्त = रेखायुक्त, बिना फण के, पुण्डरीक आदि कम विष वाले, १० प्रकार के, (४) निर्विष = गल-लोमी, शूकपत्र आदि १२ प्रकार के, (५) वैकरञ्ज = अन्य जातियों के ३ प्रकार के।
२. नाग वनस्पति-सर्प तथा नाग में अन्तर है यद्यपि इनका समान अर्थ में व्यवहार होता है। गीता (१०/२८-२९) में भगवान् ने अपने को सर्पों में वासुकि तथा नागों में अनन्त कहा है।
आयुर्वेद सन्दर्भ में नाग वनस्पति तथा खनिज ओषधियों के नाम हैं- नाग खनिज, सीसा (रसरत्नसमुच्चय, १/४१), वनस्पति नागकेसर (सुश्रुत सूत्र, ४५/१२, रसर. २१/२५-२८), ताम्बूल (र, २४/१३६), एरण्द (र. २१/२५-२८), सल्लकी (अष्टांग सं, शा, ४/३८), ग्रह भुजंगम (सुश्रुत उत्तर, ६०/३६) देवयोनि वासुकि आदि (सुश्रुत सूत्र, ५/२१), पशुगज (सुश्रुत, चिकित्सा, २८/२६), नाग केसर (सुश्रुत, सूत्र, ४६/२८७), (२) नागा-नाकुली वनस्पति (रस, २१/२९), नागकन्द, हस्तिकन्द, नाग करण्डक, नागकर्ण, नागकुमारी, नागकुमारिका, नागकेसर, नागगन्धा, नागगर्भ, नागचपल, नागचम्पक, नागच्छत्रा, नागज (सिन्दूर), नागतुम्बी (भूतुम्बी, राजनिघण्टु, ७/२४१), नागदन्ती, नागदमनी, नाग पुष्प, नागबला, नागदमनी, नागवल्ली (ताम्बूल), नागराति (वन्ध्याकर्कोटकी), नागेन्दु, नागदन्ती आदि।
 ३. सर्प विद्या-वेद का सर्पविद्या अंग लुप्त होने के कारण इसे ठीक से समझना सम्भव नहीं है। पर नीचे दिये कुछ उद्धरणों के आधार पर इसके कुछ अर्थ दिये जा रहे हैं।
रज्जुरिव हि सर्पाः कूपा इव हि सर्पाणां आयतनानि अस्ति वै मनुष्याणां च सर्पाणां च विभ्रातृव्यम् (शतपथ ब्राह्मण, ४/४/५/३)
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ (यजु, वाजसनेयि १३/६)
ते (देवाः) एतानि सर्पनामान्यपश्यन्। तैरुपातिष्ठन्त तैरस्माऽइमांल्लोकानस्थापयम्स्तैरनमयन्यदनमयंस्तस्मात् सर्पनामानि। (शतपथ ब्राह्मण, ७/४/१/२६)
इयं वै पृथिवी सर्पराज्ञी (ऐतरेय ब्राह्मण ५/३३, तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/४/६/६, शतपथ ब्राह्मण २/१/४/३०, ४/६/९/१७)
देव वै सर्पाः। तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी। (तैत्तिरीय ब्राह्मण २/२/६/२)
सर्पराज्ञा ऋग्भिः स्तुवन्ति। अर्ब्बुदः सर्प एताभिर्मृतां त्वचमपाहत मृतामेवैताभिस्त्वचमपघ्नते। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, ९/८/७-८)
अर्बुदः काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विशः... सर्पविद्या वेदः... सर्पव्द्याया एकं पर्व व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्। (शतपथ ब्राह्मण, १३/४/३/९)
ते देवाः सर्पेभ्य आश्रेषाभ्य आज्ये करंभं निरवपन्। तान् (असुरान्) एताभिरेव देवताभिरुपानयन्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१/४/७)
४. वेद में सर्प- सर्प के वेद में कई अर्थ हैं-
(१) आकाश का ८वां आयाम। इसको वृत्र, अहि, नाग भी कहा गया है। इस अर्थ में नाग, अहि, सर्प आदि का ८ संख्या के लिये व्यवहार होता है। यान्त्रिक विश्व के ५ आयाम हैं-रेखा, पृष्ठ, आयतन, पदार्थ, काल। चेतना या चिति करने वाला पुरुष तत्त्व ६ठा आयाम है। दो पिण्डों या कणों के बीच सम्बन्ध ऋषि (रस्सी) ७वां आयाम है। पिण्डों को सीमा के भीतर घेरने वाला वृत्र या अहि है।
वृत्रो ह वाऽ इदं सर्वं वृत्वा शिश्ये। यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी स यदिदं सर्वं वृत्वा शिश्ये तस्माद् वृत्रो नाम। (शतपथ ब्राह्मण, १/१/३/४)
स यद्वर्त्तमानः समभवत्। तस्माद् वृत्रः (शतपथ ब्राह्मण, १/६/३/९)
(२) आकाश गंगा (ब्रह्माण्ड) की सर्पाकार भुजा अहिर्बुध्न्य (बुध्न्य = बाढ़, ब्रह्माण्ड का द्रव जैसा फैला पदार्थ, अप्; उसमें सर्प जैसी भुजा अहिः, पुराण का शेषनाग), इसमें सूर्य के चारों तरफ भुजा की मोटाई का गोला महर्लोक है जिसके १००० तारा शेष के १००० सिर हैं जिनमें एक पर कण के समान पृथ्वी स्थित है।
(३) पृथ्वी की वक्र परिधि सतह सर्पराज्ञी है। ७ द्वीपों को जोड़ने वाले ८ दिङ्नाग हैं।
(४) समुद्री यात्रा मार्ग मुख्यतः उत्तर गोलार्ध में था। पृथ्वी पर वह मार्ग तथा उसके समान्तर आकाश का मार्ग नाग वीथी है।
(५) व्यापार के लिये वस्तुओं का परिवहन करने वाले नाग हैं जो पूरे विश्व में फैले हैं। केन्द्रीय वितरक माहेश्वरी हैं। यह अग्रवालों में बड़े माने जाते हैं।
(६) नाग पूजा पृथ्वी तथा उसके ऊपर मनुष्य रूप नागों के कार्य में सहयोग के लिये शक्ति देना है जिससे वे विश्व का भरण पोषण कर सकें। इसे देवों द्वारा दिया गया आज्य कहा है। आज्य का स्रोत दूध है जो प्रतीक रूप में दिया जाता है। इसकी व्याख्या वेदों की सर्पविद्या में थी जो लुप्त है।
(७) आश्लेषा (तैत्तिरीय में आश्रेषा भी) के देवता सर्प हैं। यह नक्षत्र मुख्यतः ब्रह्माण्ड की सर्पिल भुज के मध्य में है। श्रावण मास में सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में रहता है, मुख्यतः शुक्ल पञ्चमी तिथि के निकट। पूर्णिमा को चन्द्रमा इसके विपरीत श्रवण नक्षत्र में रहेगा जिसका देवता सर्प का विपरीत गरुड़ है। अतः इस समय नाग पूजा होती है।
वृत्रशङ्कुं दक्षिणतोऽधस्यैवानत्ययाय। (शतपथ ब्राह्मण, १३/८/४/१)
सूर्य जब पृथ्वी सतह पर सबसे दक्षिण रहता है तब वह श्रवण (३ तारा, तार्क्ष्य = गरुड़) नक्षत्र में होता है। उसके बाद उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में वृत्र = रात्रि का मान कम होने लगता है। अतः श्रवण का देवता गरुड़ है।
(८) पृथ्वी की नाग (गोलाकार पृष्ठ) सीमा के भीतर रहने वाले सर्पाकार जीव भी सर्प हैं।
(९) चीन-आकाश में ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा में सूर्य केन्द्रित गोल महः लोक है, जो ७ लोकों का मध्य है। आकाश के लोकों की तरह पृथ्वी के उत्तर गोल के भारत वाले पाद में भी विषुव से उत्तर ध्रुव तक ७ लोक हैं, जिनमें मध्य चीन भाग महः लोक है। यहां के लोगों को ब्रह्मा ने महान् कहा था, जिसका हान नाम प्रचलित है। महर्लोक में सर्प नक्षत्र आश्लेषा है, अतः चीन को भी सर्प भाग (ड्रैगन) कहते हैं। ब्रह्माण्ड पुराण उपसंहार पाद, अध्याय २ (३/४/२)-
लोकाख्यानि तु यानि स्युर्येषां तिष्ठन्ति मानवाः॥८॥भूरादयस्तु सत्यान्ताः सप्तलोकाः कृतास्त्विह॥९॥
पृथिवीचान्तरिक्षं च दिव्यं यच्च महत् स्मृतम्। स्थानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्यावर्णकानि च॥११॥
जनस्तपश्च सत्यं च स्थान्यान्येतानि त्रीणि तु। एकान्तिकानि तानि स्युस्तिष्ठंतीहाप्रसंयमात्॥१३॥
भूर्लोकः प्रथमस्तेषां द्वितीयस्तु भुवः स्मृतः।१४॥
स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो वै महः स्मृतः जनस्तु पञ्चमो लोकस्तपः षष्ठो विभाव्यते॥१५॥
सत्यस्तु सप्तमो लोको निरालोकस्ततः परम्।१६।महेति व्याहृतेनैव महर्लोकस्ततोऽभवत्॥२१॥
यामादयो गणाः सर्वे महर्लोक निवासिनः।५१॥
(१०) कुण्डलिनी-शरीर में मेरुदण्ड के नीचे मूलाधार के केन्द्र में साढ़े ३ चक्र की कुण्डलिनी है जिसे सर्प कहा है।
कन्दोर्ध्वे कुण्डली शक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः (योगचूडामणि उपनिषद्, ३६, ४४)
(११) नाग वायु-शरीर में ५ प्राण तथा ५ उप-प्राण हैं। नाग उप-प्राण है जिसे सर्प की तरह लिपटे हुए आन्त्र से वायु निकलती है।
प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायवः॥२२॥
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः।
हृदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले॥२३॥
समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः।
व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्चवायवः॥२४॥
उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने तथा।
कृकरः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे॥२५॥
न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनञ्जयः।
(योगचूडामणि उपनिषद्)
५. विश्व मूल कुण्डलिनी-शरीर और विश्व दोनों की जननी कुण्डलिनी कहा है, जो साढ़े ३ चक्र बना कर अपने मुंह में पूंछ लिये हुए है।
पश्चिमाभिमुखी योनिर्गुदमेढ्रान्तरालगा।
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा॥७९॥
संवेष्ट्य सकला नाडीः सार्द्धत्रि कुटिलाकृतिः।
मुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्णा विवरे स्थिता॥८०॥
सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ति प्रभया स्वया।
अहिवत् सन्धि संस्थाना वाग्देवी बीजसंज्ञिका॥८१॥
(शिवसंहिता, पटल, ५)
= गुदा-मेढ्र के बीच योनि स्थान में पीछे की तरफ कन्द में कुण्डलिनी साढ़े ३ फेरा कर अपने मुंह में पुच्छ ले कर सुषुम्णा विवर में स्थित है। यह सर्प के समान प्रभा युक्त हो कर सन्धि स्थान में सोई है। यह वाग्देवी और बीज (उत्पत्ति स्रोत) है। अत्रास्ते शिशु सूर्य सोदर कला चन्द्रस्य सा षोडशी,
शुद्धा नीरज सूक्ष्म तन्तु शतधा भागैक रूपा परा॥४६॥
एतस्या मध्य देशेविलसति परमापूर्व निर्वाण शक्तिः,
कोट्यादित्य प्रकाशा त्रिभुवन जननी कोटि भागैकरूपा।
केशाग्रस्यातिसूक्ष्मा निरवधि विगलत् प्रेमधाराधरा सा,
सर्वेषां जीव भूता मुनि-मनसि मुदा तत्त्वबोधं वहन्ति॥४८॥
(षट्चक्र निरूपण)
कन्द में कुण्डलिनी केशाग्र का १ कोटि भाग में है तथा उसके तन्तु उसका भी १०० भाग है। केशाग्र = १ माइक्रोन = १० घात (-६) मीटर। उसके कोटि भाग का १०० भाग = १० घात (-१५) मीटर। यह परमाणु की नाभि का आकार है। यह त्रिभुवन जननी है अर्थात् मनुष्य आदि जीव, सभी भुवनों को जन्म देने वाली। यह धारा रूप में पूर्व जन्म के संस्कार का वहन करती है।इसके कई अर्थ हैं-
(१) सूक्ष्म रूप में परमाणु नाभि आकार की कुण्डलिनी से शरीर के गुण सूत्र निर्धारित होते हैं। यह डीएनए की भी रचना है जिसमें मरोड़ी हुयी ३ सीढ़ियों के मिलन जैसी रचना है। इससे शरीर के सभी गुण निर्धारित होते हैं, यह आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। किन्तु पूर्व जन्म के संस्कार इस माध्यम से कैसे आते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। इस बीज रूप से सृष्टि क्रम चलता रहता है जैसे वृक्ष मूल से शाखा फल होते हैं और उनके बीज से पुनः वैसा ही बीज उत्पन्न होता है। अतः शुक्र द्वारा सृष्टि को अमृत कहा गया है।
ऊर्ध्वमूलोऽवाक् शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।
तस्मुँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन॥ एतद् वै तत्॥
(कठोपनिषद्, २/३/१)
(२) सृष्टि चक्र-सृष्टि के ९ सर्ग तथा अव्यक्त को मिलाकर १० सर्ग हैं। हर चक्र का सृष्टि-प्रलय क्रम है जिनसे ९ प्रकार के माप योग्य काल मान हैं (सूर्य सिद्धान्त, १४/१)। इसके लिए ब्रह्म के ३ रूपों के प्रतीक ३ वृक्ष हैं। त्रिगुण मयी प्रकृति या वेदत्रयी का प्रतीक पलास वृक्ष स्रष्टा रूप ब्रह्मा का चिह्न है। पलास की शाखा से ३ पत्र निकलते हैं, मूल भी बचा रहता है। इसी प्रकार वेद की ३ शाखा हुयी-मूर्ति रूप ऋक्, गति रूप यजु, महिमा रूप साम वेद। उसके बाद भी ब्रह्म या आधार रूप अथर्व बचा रहा। अतः त्रयी का अर्थ ४ वेद हैं। इसी प्रकार ३ गुणों से सृष्टि होने पर भी गुणातीत परम प्रकृति रह जाती है। सृष्टि का क्रम वट वृक्ष है, यही गुरुशिष्य परम्परा भी है और शिव का चिह्न है। वट वृक्ष अपनी शाखा नीचे जमीन पर गिरा कर वैसा ही वृक्ष उत्पन्न करता है। गुरु भी शिष्य को ज्ञान दे कर अपने जैसा मनुष्य बनाता है। इस चक्र के भीतर जो सृष्टि है वह पिछली सृष्टि के अन्त (पूंछ या पैर) से आरम्भ हुई। आरम्भ को मुख कहते हैं। अतः वट वृक्ष के आश्रय में भगवान् कृष्ण अपना पैर मुंह में रखे हुए हैं। इस प्रकार सृष्टि की निरन्तरता अविनाशी अश्वत्थ है, जो विष्णु का प्रतीक है। वेद में वट के परस्पर मिले हुए वृक्षों को प्रघन कहा है। निर्माण स्रोत को वृषभ (जो वर्षा करे) कहा गया है, यह शिव का वाहन हुआ। पिण्डों का आवरण कपर्द (जटा, कपड़ा) है जिसे बनाने वाला कपर्दी शिव है।
न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एन ममेहयन् वृषभं मध्य आजेः।
तेन सूभर्वं शतवत् सहस्रं गवां मुद्गलः प्रघने जिगाय॥५॥
शुनमष्ट्राव्यचरत् कपर्दी वरत्रायां दार्वानह्यमानः॥८॥
इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानम्॥९॥ (ऋक्, १०/१०२)
कः स्विद् वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नाधितः पर्यषस्वजत्।
पर्णा मृगस्य पतरोरिवारभ उदश्विना ऊहथुः श्रोमताय कम्॥ (ऋक्, १/१८२/७)
पलास रूप ब्रह्मा-यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः। अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति॥ (ऋक्, १०/१३५/१)
सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां योनिर्यत् पलासः। (स्वायम्भुव ब्रह्मरूपत्त्वात्) तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः-ऐतरेय ब्राह्मण २/१)
ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशम् (= पर्णम्)। (शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/८)
मुख से पैर तक का सृष्टि चक्र-करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥
(बालमुकुन्दाष्टक, भागवत अध्याय १२/९ के अनुसार)
स्रोत सूर्य, अन्त यम है, इन दोनों के चक्र से सृष्टि चल रही है-
पूषन् एकर्षे यम-सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह (ईशावास्योपनिषद्, वाज. सं. ४०/१६)
(२) त्रिभाग व्यवस्था-विश्व को समझने के लिए कई प्रकार से ३ भाग करते हैं। हर बार कुछ छूट जाता है। उस अज्ञात को अर्ध मात्रा या चक्र कहते हैं।
ॐ के ३ खण्ड हैं-अ, उ, म। उसके बाद अनुस्वार की गूंज रह जाती है। यह अर्ध मात्रा परा प्रकृति है।सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।
अर्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः (दुर्गा सप्तशती, १/७४)।
इसके भी क्रमशः अर्ध भाग ९ बार होते हैं, जो सृष्टि के ९ सर्गों या ९ दुर्गा के रूप हैं।
परब्रह्म का कार्य, कारण समझ में नहीं आता, अतः उसे ज्ञान, बल, क्रिया रूप में समझते हैं- ज्ञानघन जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा।
न तस्य कार्यं करणं न विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
गायत्री मन्त्र भी कुण्डलिनी का ही रूप है। उसके ३ पाद ब्रह्म के स्रष्टा, क्रिया, ज्ञान रूप का वर्णन करते हैं। उसके बाद भी अदर्शित परोरजा (लोक से परे) रूप रह जाता है।
कुण्डलिन्या समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी (योगचूडामणि उपनिषद्, ३५)
परोरजसेऽसावदोम् (बृहदारण्यक, ५/१४/७), परोरजा य एष तपति (बृहदारण्यक, ५/१४/३)
(३) अन्य त्रिक-कई प्रकार के त्रिक हैं,जिनके माध्यम से विश्व को जानते हैं, पर कुछ बाकी रह जाता है। वह साढ़े ३ चक्र भुवनों (मनुष्य तथा लोक) का रेत (शुक्र, बीज) है।
सत्-चित्-आनन्द= सर्वव्यापी आनन्द हर चित् या विन्दु आकाश में है, उसमें जो अनुभव गम्य है, वह सत् है।
शंकर = खं ब्रह्म (शून्य आकाश) + कं ब्रह्म (कर्ता, करतार), रं ब्रह्म (गतिशील प्राण)
ॐ तत्-सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः (गीता, १७/२३)
ॐ का गति रूप रं है, तत् को नाम से कहते हैं। अतः प्राण निकलने पर कहते हैं-राम नाम सत्।
अतः त्रैगुण्य रूप वेद या विश्व जानने के बाद उससे परे की भी कल्पना करनी चाहिए।
त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन (गीता, २/४५)
विश्व मूल कुण्डलिनी-
सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि।
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवति विश्वतः॥ (ऋक्, १/१६४/३६)
६. अनन्त-
(१) अनन्त वेद-तैत्तिरीय ब्राह्मण (३/१०/११/३-४) के अनुसार भरद्वाज ने ३ आयु तक वेदाध्ययन किया पर पूरा नहीं हुआ। इन्द्र से एक और जीवन मांगा तो इन्द्र ने ३ विशाल पर्वत दिखाये जो ३ वेदों के स्वरूप थे। कहा-अनन्ताः वै वेदाः। उन पर्वतों से १-१ मुठ्ठी वेद ही पढ़ सके थे। यहां अनन्त बहुवचन में है, अतः कम से कम ३ प्रकार के अनन्त हैं। विष्णु सहस्रनाम में इन तीनों का उल्लेख हुआ है-अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय।
संख्येय अनन्त वह है जिसकी गणना १, २, ३, --- आदि क्रम से किया जा सके। इन संख्याओं आ क्रम भी अनन्त है। सभी भिन्न संख्याओं को भी क्रमबद्ध कर गिना जा सकता है। (कैण्टर सेट थिओरी)
असंख्येय अनन्त को संख्या क्रम में नहीं रख सकते न गिन सकते हैं। किसी भी रेखा में विन्दुओं की संख्या किसी क्रम में नहीं गिन सकते। यह २ प्रकार का है-
प्रमेय अनन्त संख्या को गणित सूत्र या परिभाषा द्वारा समझ सकते हैं जैसे परिधि/व्यास अनुपात।
अप्रमेय अनन्त को गणित या किसी सिद्धान्त से नहीं समझ सकते।
असंख्येय अनन्तों के भी विभिन्न प्रकार के समूह और बड़े अनन्त हैं।
मूर्ति रूप ऋग्वेद संख्येय है। गति रूप यजुर्वेद विन्दु की रेखा गति जैसा है और असंख्येय है। सामवेद में हर विन्दु तथा उसकी महिमा-दो प्रकार से असंख्येय हैं। इनका आधार या स्रोत अथर्व या ब्रह्म वेद इन सभी अनन्तों के समूह रूप हैं।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
वाक् में अनन्त के क्रमशः बड़े स्तर हैं-वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा।
(२) अनन्त विश्व-दृश्य जगत् के सभी स्तर पुरुष हैं। इनका आधार या अव्यक्त स्रोत पूरुष हैं। पूरुष के ४ भागों में १ ही भाग का प्रयोग हुआ। बाकी ३ भाग बचे रह गये जो उच्छिष्ट (भोजन से बचा जूठा) या ज्यायान् (भोजपुरी में जियान = बेकार, अनुपयुक्त) हैं। दृश्य या निर्मित जगत् का अव्यक्त आधार ही अनन्त है जिसने अपने सहस्र शीर्ष (स्रोत) में जगत् का धारण किया है।
दृश्य जगत् को गिन सकते हैं। जिसकी गणना हो सके वह गणेश है। विश्व निर्माण के बाद बचा ३ भाग उच्छिष्ट गणपति है। १०० अरब ब्रह्माण्ड, हमारे ब्रह्माण्ड में १०० अरब तारा, उसकी प्रतिमा मनुष्य मस्तिष्क में कलिल (लोमगर्त्त) हैं। मुहूर्त्त को ७ बार १५-१५ से भाग देने पर लोमगर्त्त होता है, १ सेकण्ड का प्रायः ७५,००० भाग। वर्ष में जितने लोमगर्त्त हैं, उतने ही आकाश में नक्षत्र हैं, अर्थात् १०० अरब। (शतपथ ब्राह्मण, १२/३/२/५, १०/४/४/२)। विश्व का कण या चूर्ण (खर्व) रूप में यही मान है। अतः खर्व = १०० अरब (खर्व स्थूलतनुं गजेन्द्र वदनम्)। खर्व का अन्य अर्थ नाटा है।
१०० अरब ब्रह्माण्डों का समूह महा गणपति तथा १०० अरब तारा समूह का हमारा ब्रह्माण्ड गणपति है। इसकी माप जगती छन्द में है। पृथ्वी को २४ बार २ गुणा करने पर सौर मण्डल-या गायत्री गुणा है। पुनः २४ बार २ गुणा करने पर ब्रह्माण्ड है। इन क्रमशः बड़े क्षेत्रों को अहर्गण कहते हैं। ब्रह्माण्ड सीमा तक ४९ अहर्गण हैं जिसमें कणों की गति ४९ प्रकार के मरुत् हैं। हमारा ब्रह्माण्ड अन्य खर्व ब्रह्माण्डों के आकर्षण से टिका है जो शेष या अनन्त है।
ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा वेद का अहिर्बुध्न्य (बुध्न्य अर्थात् बाढ़, अहि = सर्प) या पुराण का शेष नाग है। इसमें जहां सूर्य है, वहां भुजा की मोटाई के गोल (१४०० प्रकाश वर्ष व्यास) में १००० तारा हैं जो शेष के १००० सिर हैं। सूर्य रूपी विष्णु इसी शेष पर सोये हैं जो आकाश गंगा (ब्रह्माण्ड) के समुद्र में है। १००० सिरों में १ सिर सूर्य पर पृथ्वी कण मात्र है।
इस महर्लोक समुद्र में भी सौर मण्डल तैर रहा है। सूर्य ने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है (पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवि त्वं विष्णुना धृता)। सौर मण्डल का केन्द्र या नाभि सूर्य है जिससे आकर्षण रूपी कमल नाल पर पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर मर्त्य ब्रह्मा द्वारा सृष्टि है।
(३) पार्थिव अनन्त-उत्तरी गोल का नक्शा ४ भागों में बनता था जिनको भू-पद्म का ४ दल कहा है। इसी प्रकार दक्षिण गोल में भी बनता था। गोल पृथ्वी का समतल नक्शा बनाने के लिए १ लाख योजन ऊंचे ४ पार्श्वके मेरु पर प्रक्षेप करते थे। इसमें ध्रुव विन्दु पर अनन्त गुणा आकार हो जाता है। उत्तर ध्रुव जल में है अतः वहां कोई समस्या नहीं होती। पर दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है, उसका आकार अनन्त हो जाता है। अतः इसे अनन्त द्वीप कहते थे जिसका अलग से नवम नक्शा बनाना पड़ता था। (आर्यभटीय, ४/१२, लल्ल, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र, १७/३-४)। इसके २ भू-खण्ड (यम = यमल, जोड़ा) अतः इसे यम द्वीप भी कहते थे। नक्शा में दक्षिण भाग नीचे दिखाते हैं अतः इस अनन्त पर ही पृथ्वी टिकी है तथा नाग की तरह अक्ष पर गोल घूम रही है।
७. मनुष्य नाग-नाग जातियों का वर्णन महाभारत, उद्योग पर्व, अध्याय १०३ में है। अर्जुन ने खाण्डव प्रस्थ को तक्षक के अधिकार से छुड़ा कर वहां इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान दिल्ली) का निर्माण किया (महाभारत, आदि पर्व, २२२-२२६ अध्याय)। वह अपने मूल स्थान तक्षशिला चला गया। पाण्डवों से शत्रुता के कारण इसकी दुर्योधन से मैत्री हुई तथा परीक्षित की हत्या की थी (महाभारत, आदि पर्व, अध्याय, ४३, ५०)। जनमेजय ने इसे मारने के लिए नाग यज्ञ किया। नागों के २ नगरों को श्मशान बना दिया जिनके नाम मोइन-जो-दरो (मृतक स्थान) तथा हड़प्पा (हड्डियों का ढेर) हुए। यह वर्णन गुरु गोविन्द सिंह ने एक राम मन्दिर की दीवाल पर लिखवाया था। दुर्योधन ने तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसमें ३०,००० छात्र रहते थे (एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का पारसी अनुवाद मज़्मा ए तवारीख)। तक्षक का एक नगर कश्मीर में भी था, जो वितस्ता नाम से प्रसिद्ध हुआ (पद्म पुराण, ३/२५/२)। पुरुवंश से तक्षशिला की शत्रुता सिकन्दर काल तक चलती रही। सभी तक्षक एक ही नहीं थे। तक्षक जाति कद्रू की सन्तान या काद्रवेय थी। तक्षक जाति का एक भवन सुतल (जापान आदि) में था (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२०/२४) में था। वहां नागासाकी नगर है। नागाशी वास्तव में नाग-शत्रु गरुड़ की सन्तान थी (महाभारत, उद्योग पर्व, १०१/९)। इस जाति का निवास निषध पर्वत पर भी था (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/१७/३४)। अफ्रीका से जो तक्षक जाति के लोग समुद्र मन्थन के लिए झारखण्ड आये थे, उनका निवास स्थान कडरू (कद्रू) है।
समुद्र मन्थन या खनिज दोहन में समन्वय वासुकि नाग ने किया था जो मूलतः पाताल लोक या उत्तर अमेरिका के थे (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२०/३९-४१)। मन्थन कामुख्य स्रोत मन्दार पर्वत था जो मथानी के आकार में सिंहभूमि से भागलपुर में गंगा तट तक चला गया। है। वहां वासुकिनाथ मन्दिर है। भागलपुर नाम भी नागों की भोगवती पुरी के नाम पर है। वासुकि की भोगवती पुरी प्रयाग में भी थी (अग्नि पुराण, १११/१०)।
नागों का नरसंहार रोकने के लिए वासुकि नाग ने अपनी बहन जरत्कारु के पुत्र आस्तीक को भेजा था (देवी भागवत, २/११)। अतः आस्तीक भी उत्तर अमेरिका ए ही थे जिनको आजकल मेक्सिको में एज्टेक कहते हैं। पुरुवंश के नहुष भी ऋषि शाप से पाताल चले गये थे और नाग हुए (महाभारत, उद्योग पर्व, १७/१४-१८)। उनके वंशज मेक्सिको के नहुआ हैं। नहुष नागों को भी कद्रु का पुत्र कहा गया है (महाभारत, आदि पर्व, ३५/९)।
नाग तथा सर्प एक ही जाति के है। भारत की शत्रु जातियों को सर्प कहते थे जिनके विरुद्ध गरुड़ का अभियान चलता रहता था। वासुकि के नागाधिप व तक्षक के सर्पाधिप बनने का उल्लेख है (मत्स्य पुराण, ८/७, वायु पुराण, ६९/३२२)। तक्षक कॊ भी प्रायः नाग ही कहा गया है।
रांगेय राघव ने ’महागाथा-यात्रा’ में भारत में नाग जाति के स्थानों का उल्लेख किया है जो सर्पों के नाम पर हैं-नागपुर, अहिच्छत्र, अहिगृह (आगरा), नागपट्टनम्, अहोबिल, भोगल (फोगला), भागलपुर, भोगवती। यह अलग जाति नहीं थी। व्यापार के लिए सामान ले जाने वाले नाग थे। इन्द्र के सहायक नाग थे तथा तक्षक से उनकी मैत्री थी (आदि पर्व, २२२/७)। इन्द्र को अच्युत-च्युतः कहा गया है (ऋक्, २/१२/९) अर्थात् जो अपराजित को भी पराजित कर सके। इन्द्र पूर्व के लोकेपाल थे अतः पूर्व में असम के राजा को च्युत या चूतिता कहते थे। इनका नागपुर चुतिया-नागपुर था जो अंग्रेजी माध्यम से छोटानागपुर हो गया। आज भी रांची में चुतिया मोड़ है।
अहिगृह वालों को अघरिया कहते हैं जो पश्चिम ओड़िशा, छत्तीसगढ़ का व्यापारी वर्ग है। इनकी उपाधि पटेल है। एक तक्षक सौराष्ट्र में रैवत राजा बना था जिसके वंशज नागर हैं (लक्ष्मीनारायण संहिता, १/४९९/११, २/२८/१६)।
अग्रवाल नाम अहिगृह से नहीं है जैसा रांगेय राघव का अनुमान था। वेद में नेता को अग्नि या अग्रि (अग्रणी) कहा गया है।
अग्ने नय सुपथा राये (ईशावास्योपनिषद्) = अग्नि! हमें अच्छॆ मार्ग पर ले चलो (नय से नेता हुआ है)।
भारत का अग्नि विश्व का भरण पोषण करता था इससे उसको भरत तथा इस देश को भारत कहा गया। यही अग्नि या अग्रि लोकभाषा में अग्रसेन है तथा उनके सहयोगी अग्रवाल।
स यदस्य सर्वस्याग्र सृजत तस्मादग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम्। शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/११)
= सबसे प्रथम उत्पन्न होने के कारण यह अग्रि (नेता) हुआ, इसे परोक्ष में अग्नि कहा जाता है।
अग्नेर्महाँ ब्राह्मण भारतेति । एष हि देवेभ्य हव्यं भरति । (तैत्तिरीय संहिता, २/५/९/१, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/५/३/१, शतपथ ब्राह्मण, १/४/१/१)
= ब्रह्मा ने भारत के अग्नि को महान् कहा था क्योंकि यह देवों को भोजन देता है।
भरणात्प्रजनाच्चैष मनुर्भरत उच्यते । एतन्निरुक्त वचनाद् वर्षं तद् भारतं स्मृतम् ।
यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तिर्यगग्यामः प्रकीर्तितः । य एनं जयते कृत्स्नं स सम्राडिति कीर्तितः ।
(मत्स्य पुराण, ११४/५,६, वायु पुराण, ४५/७६)
= लोकों के भरण तथा पालन के कारण इस देश का मनु (शासक) भरत कहा जाता है। निरुक्त परिभाषा के अनुसार भी इस देश को भारत कहा गया है।
विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत आस होई॥ (राम चरित मानस, बालकाण्ड, ९६/५)
३. सर्प विद्या-वेद का सर्पविद्या अंग लुप्त होने के कारण इसे ठीक से समझना सम्भव नहीं है। पर नीचे दिये कुछ उद्धरणों के आधार पर इसके कुछ अर्थ दिये जा रहे हैं।
रज्जुरिव हि सर्पाः कूपा इव हि सर्पाणां आयतनानि अस्ति वै मनुष्याणां च सर्पाणां च विभ्रातृव्यम् (शतपथ ब्राह्मण, ४/४/५/३)
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ (यजु, वाजसनेयि १३/६)
ते (देवाः) एतानि सर्पनामान्यपश्यन्। तैरुपातिष्ठन्त तैरस्माऽइमांल्लोकानस्थापयम्स्तैरनमयन्यदनमयंस्तस्मात् सर्पनामानि। (शतपथ ब्राह्मण, ७/४/१/२६)
इयं वै पृथिवी सर्पराज्ञी (ऐतरेय ब्राह्मण ५/३३, तैत्तिरीय ब्राह्मण, १/४/६/६, शतपथ ब्राह्मण २/१/४/३०, ४/६/९/१७)
देव वै सर्पाः। तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी। (तैत्तिरीय ब्राह्मण २/२/६/२)
सर्पराज्ञा ऋग्भिः स्तुवन्ति। अर्ब्बुदः सर्प एताभिर्मृतां त्वचमपाहत मृतामेवैताभिस्त्वचमपघ्नते। (ताण्ड्य महाब्राह्मण, ९/८/७-८)
अर्बुदः काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विशः... सर्पविद्या वेदः... सर्पव्द्याया एकं पर्व व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्। (शतपथ ब्राह्मण, १३/४/३/९)
ते देवाः सर्पेभ्य आश्रेषाभ्य आज्ये करंभं निरवपन्। तान् (असुरान्) एताभिरेव देवताभिरुपानयन्। (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१/४/७)
४. वेद में सर्प- सर्प के वेद में कई अर्थ हैं-
(१) आकाश का ८वां आयाम। इसको वृत्र, अहि, नाग भी कहा गया है। इस अर्थ में नाग, अहि, सर्प आदि का ८ संख्या के लिये व्यवहार होता है। यान्त्रिक विश्व के ५ आयाम हैं-रेखा, पृष्ठ, आयतन, पदार्थ, काल। चेतना या चिति करने वाला पुरुष तत्त्व ६ठा आयाम है। दो पिण्डों या कणों के बीच सम्बन्ध ऋषि (रस्सी) ७वां आयाम है। पिण्डों को सीमा के भीतर घेरने वाला वृत्र या अहि है।
वृत्रो ह वाऽ इदं सर्वं वृत्वा शिश्ये। यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी स यदिदं सर्वं वृत्वा शिश्ये तस्माद् वृत्रो नाम। (शतपथ ब्राह्मण, १/१/३/४)
स यद्वर्त्तमानः समभवत्। तस्माद् वृत्रः (शतपथ ब्राह्मण, १/६/३/९)
(२) आकाश गंगा (ब्रह्माण्ड) की सर्पाकार भुजा अहिर्बुध्न्य (बुध्न्य = बाढ़, ब्रह्माण्ड का द्रव जैसा फैला पदार्थ, अप्; उसमें सर्प जैसी भुजा अहिः, पुराण का शेषनाग), इसमें सूर्य के चारों तरफ भुजा की मोटाई का गोला महर्लोक है जिसके १००० तारा शेष के १००० सिर हैं जिनमें एक पर कण के समान पृथ्वी स्थित है।
(३) पृथ्वी की वक्र परिधि सतह सर्पराज्ञी है। ७ द्वीपों को जोड़ने वाले ८ दिङ्नाग हैं।
(४) समुद्री यात्रा मार्ग मुख्यतः उत्तर गोलार्ध में था। पृथ्वी पर वह मार्ग तथा उसके समान्तर आकाश का मार्ग नाग वीथी है।
(५) व्यापार के लिये वस्तुओं का परिवहन करने वाले नाग हैं जो पूरे विश्व में फैले हैं। केन्द्रीय वितरक माहेश्वरी हैं। यह अग्रवालों में बड़े माने जाते हैं।
(६) नाग पूजा पृथ्वी तथा उसके ऊपर मनुष्य रूप नागों के कार्य में सहयोग के लिये शक्ति देना है जिससे वे विश्व का भरण पोषण कर सकें। इसे देवों द्वारा दिया गया आज्य कहा है। आज्य का स्रोत दूध है जो प्रतीक रूप में दिया जाता है। इसकी व्याख्या वेदों की सर्पविद्या में थी जो लुप्त है।
(७) आश्लेषा (तैत्तिरीय में आश्रेषा भी) के देवता सर्प हैं। यह नक्षत्र मुख्यतः ब्रह्माण्ड की सर्पिल भुज के मध्य में है। श्रावण मास में सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में रहता है, मुख्यतः शुक्ल पञ्चमी तिथि के निकट। पूर्णिमा को चन्द्रमा इसके विपरीत श्रवण नक्षत्र में रहेगा जिसका देवता सर्प का विपरीत गरुड़ है। अतः इस समय नाग पूजा होती है।
वृत्रशङ्कुं दक्षिणतोऽधस्यैवानत्ययाय। (शतपथ ब्राह्मण, १३/८/४/१)
सूर्य जब पृथ्वी सतह पर सबसे दक्षिण रहता है तब वह श्रवण (३ तारा, तार्क्ष्य = गरुड़) नक्षत्र में होता है। उसके बाद उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में वृत्र = रात्रि का मान कम होने लगता है। अतः श्रवण का देवता गरुड़ है।
(८) पृथ्वी की नाग (गोलाकार पृष्ठ) सीमा के भीतर रहने वाले सर्पाकार जीव भी सर्प हैं।
(९) चीन-आकाश में ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा में सूर्य केन्द्रित गोल महः लोक है, जो ७ लोकों का मध्य है। आकाश के लोकों की तरह पृथ्वी के उत्तर गोल के भारत वाले पाद में भी विषुव से उत्तर ध्रुव तक ७ लोक हैं, जिनमें मध्य चीन भाग महः लोक है। यहां के लोगों को ब्रह्मा ने महान् कहा था, जिसका हान नाम प्रचलित है। महर्लोक में सर्प नक्षत्र आश्लेषा है, अतः चीन को भी सर्प भाग (ड्रैगन) कहते हैं। ब्रह्माण्ड पुराण उपसंहार पाद, अध्याय २ (३/४/२)-
लोकाख्यानि तु यानि स्युर्येषां तिष्ठन्ति मानवाः॥८॥भूरादयस्तु सत्यान्ताः सप्तलोकाः कृतास्त्विह॥९॥
पृथिवीचान्तरिक्षं च दिव्यं यच्च महत् स्मृतम्। स्थानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्यावर्णकानि च॥११॥
जनस्तपश्च सत्यं च स्थान्यान्येतानि त्रीणि तु। एकान्तिकानि तानि स्युस्तिष्ठंतीहाप्रसंयमात्॥१३॥
भूर्लोकः प्रथमस्तेषां द्वितीयस्तु भुवः स्मृतः।१४॥
स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो वै महः स्मृतः जनस्तु पञ्चमो लोकस्तपः षष्ठो विभाव्यते॥१५॥
सत्यस्तु सप्तमो लोको निरालोकस्ततः परम्।१६।महेति व्याहृतेनैव महर्लोकस्ततोऽभवत्॥२१॥
यामादयो गणाः सर्वे महर्लोक निवासिनः।५१॥
(१०) कुण्डलिनी-शरीर में मेरुदण्ड के नीचे मूलाधार के केन्द्र में साढ़े ३ चक्र की कुण्डलिनी है जिसे सर्प कहा है।
कन्दोर्ध्वे कुण्डली शक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः (योगचूडामणि उपनिषद्, ३६, ४४)
(११) नाग वायु-शरीर में ५ प्राण तथा ५ उप-प्राण हैं। नाग उप-प्राण है जिसे सर्प की तरह लिपटे हुए आन्त्र से वायु निकलती है।
प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायवः॥२२॥
नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः।
हृदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले॥२३॥
समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः।
व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्चवायवः॥२४॥
उद्गारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने तथा।
कृकरः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे॥२५॥
न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनञ्जयः।
(योगचूडामणि उपनिषद्)
५. विश्व मूल कुण्डलिनी-शरीर और विश्व दोनों की जननी कुण्डलिनी कहा है, जो साढ़े ३ चक्र बना कर अपने मुंह में पूंछ लिये हुए है।
पश्चिमाभिमुखी योनिर्गुदमेढ्रान्तरालगा।
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा॥७९॥
संवेष्ट्य सकला नाडीः सार्द्धत्रि कुटिलाकृतिः।
मुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्णा विवरे स्थिता॥८०॥
सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ति प्रभया स्वया।
अहिवत् सन्धि संस्थाना वाग्देवी बीजसंज्ञिका॥८१॥
(शिवसंहिता, पटल, ५)
= गुदा-मेढ्र के बीच योनि स्थान में पीछे की तरफ कन्द में कुण्डलिनी साढ़े ३ फेरा कर अपने मुंह में पुच्छ ले कर सुषुम्णा विवर में स्थित है। यह सर्प के समान प्रभा युक्त हो कर सन्धि स्थान में सोई है। यह वाग्देवी और बीज (उत्पत्ति स्रोत) है। अत्रास्ते शिशु सूर्य सोदर कला चन्द्रस्य सा षोडशी,
शुद्धा नीरज सूक्ष्म तन्तु शतधा भागैक रूपा परा॥४६॥
एतस्या मध्य देशेविलसति परमापूर्व निर्वाण शक्तिः,
कोट्यादित्य प्रकाशा त्रिभुवन जननी कोटि भागैकरूपा।
केशाग्रस्यातिसूक्ष्मा निरवधि विगलत् प्रेमधाराधरा सा,
सर्वेषां जीव भूता मुनि-मनसि मुदा तत्त्वबोधं वहन्ति॥४८॥
(षट्चक्र निरूपण)
कन्द में कुण्डलिनी केशाग्र का १ कोटि भाग में है तथा उसके तन्तु उसका भी १०० भाग है। केशाग्र = १ माइक्रोन = १० घात (-६) मीटर। उसके कोटि भाग का १०० भाग = १० घात (-१५) मीटर। यह परमाणु की नाभि का आकार है। यह त्रिभुवन जननी है अर्थात् मनुष्य आदि जीव, सभी भुवनों को जन्म देने वाली। यह धारा रूप में पूर्व जन्म के संस्कार का वहन करती है।इसके कई अर्थ हैं-
(१) सूक्ष्म रूप में परमाणु नाभि आकार की कुण्डलिनी से शरीर के गुण सूत्र निर्धारित होते हैं। यह डीएनए की भी रचना है जिसमें मरोड़ी हुयी ३ सीढ़ियों के मिलन जैसी रचना है। इससे शरीर के सभी गुण निर्धारित होते हैं, यह आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। किन्तु पूर्व जन्म के संस्कार इस माध्यम से कैसे आते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। इस बीज रूप से सृष्टि क्रम चलता रहता है जैसे वृक्ष मूल से शाखा फल होते हैं और उनके बीज से पुनः वैसा ही बीज उत्पन्न होता है। अतः शुक्र द्वारा सृष्टि को अमृत कहा गया है।
ऊर्ध्वमूलोऽवाक् शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।
तस्मुँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन॥ एतद् वै तत्॥
(कठोपनिषद्, २/३/१)
(२) सृष्टि चक्र-सृष्टि के ९ सर्ग तथा अव्यक्त को मिलाकर १० सर्ग हैं। हर चक्र का सृष्टि-प्रलय क्रम है जिनसे ९ प्रकार के माप योग्य काल मान हैं (सूर्य सिद्धान्त, १४/१)। इसके लिए ब्रह्म के ३ रूपों के प्रतीक ३ वृक्ष हैं। त्रिगुण मयी प्रकृति या वेदत्रयी का प्रतीक पलास वृक्ष स्रष्टा रूप ब्रह्मा का चिह्न है। पलास की शाखा से ३ पत्र निकलते हैं, मूल भी बचा रहता है। इसी प्रकार वेद की ३ शाखा हुयी-मूर्ति रूप ऋक्, गति रूप यजु, महिमा रूप साम वेद। उसके बाद भी ब्रह्म या आधार रूप अथर्व बचा रहा। अतः त्रयी का अर्थ ४ वेद हैं। इसी प्रकार ३ गुणों से सृष्टि होने पर भी गुणातीत परम प्रकृति रह जाती है। सृष्टि का क्रम वट वृक्ष है, यही गुरुशिष्य परम्परा भी है और शिव का चिह्न है। वट वृक्ष अपनी शाखा नीचे जमीन पर गिरा कर वैसा ही वृक्ष उत्पन्न करता है। गुरु भी शिष्य को ज्ञान दे कर अपने जैसा मनुष्य बनाता है। इस चक्र के भीतर जो सृष्टि है वह पिछली सृष्टि के अन्त (पूंछ या पैर) से आरम्भ हुई। आरम्भ को मुख कहते हैं। अतः वट वृक्ष के आश्रय में भगवान् कृष्ण अपना पैर मुंह में रखे हुए हैं। इस प्रकार सृष्टि की निरन्तरता अविनाशी अश्वत्थ है, जो विष्णु का प्रतीक है। वेद में वट के परस्पर मिले हुए वृक्षों को प्रघन कहा है। निर्माण स्रोत को वृषभ (जो वर्षा करे) कहा गया है, यह शिव का वाहन हुआ। पिण्डों का आवरण कपर्द (जटा, कपड़ा) है जिसे बनाने वाला कपर्दी शिव है।
न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एन ममेहयन् वृषभं मध्य आजेः।
तेन सूभर्वं शतवत् सहस्रं गवां मुद्गलः प्रघने जिगाय॥५॥
शुनमष्ट्राव्यचरत् कपर्दी वरत्रायां दार्वानह्यमानः॥८॥
इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानम्॥९॥ (ऋक्, १०/१०२)
कः स्विद् वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नाधितः पर्यषस्वजत्।
पर्णा मृगस्य पतरोरिवारभ उदश्विना ऊहथुः श्रोमताय कम्॥ (ऋक्, १/१८२/७)
पलास रूप ब्रह्मा-यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः। अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति॥ (ऋक्, १०/१३५/१)
सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां योनिर्यत् पलासः। (स्वायम्भुव ब्रह्मरूपत्त्वात्) तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः-ऐतरेय ब्राह्मण २/१)
ब्रह्म वै पलाशस्य पलाशम् (= पर्णम्)। (शतपथ ब्राह्मण, २/६/२/८)
मुख से पैर तक का सृष्टि चक्र-करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्।
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥
(बालमुकुन्दाष्टक, भागवत अध्याय १२/९ के अनुसार)
स्रोत सूर्य, अन्त यम है, इन दोनों के चक्र से सृष्टि चल रही है-
पूषन् एकर्षे यम-सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह (ईशावास्योपनिषद्, वाज. सं. ४०/१६)
(२) त्रिभाग व्यवस्था-विश्व को समझने के लिए कई प्रकार से ३ भाग करते हैं। हर बार कुछ छूट जाता है। उस अज्ञात को अर्ध मात्रा या चक्र कहते हैं।
ॐ के ३ खण्ड हैं-अ, उ, म। उसके बाद अनुस्वार की गूंज रह जाती है। यह अर्ध मात्रा परा प्रकृति है।सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।
अर्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः (दुर्गा सप्तशती, १/७४)।
इसके भी क्रमशः अर्ध भाग ९ बार होते हैं, जो सृष्टि के ९ सर्गों या ९ दुर्गा के रूप हैं।
परब्रह्म का कार्य, कारण समझ में नहीं आता, अतः उसे ज्ञान, बल, क्रिया रूप में समझते हैं- ज्ञानघन जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा।
न तस्य कार्यं करणं न विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
गायत्री मन्त्र भी कुण्डलिनी का ही रूप है। उसके ३ पाद ब्रह्म के स्रष्टा, क्रिया, ज्ञान रूप का वर्णन करते हैं। उसके बाद भी अदर्शित परोरजा (लोक से परे) रूप रह जाता है।
कुण्डलिन्या समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी (योगचूडामणि उपनिषद्, ३५)
परोरजसेऽसावदोम् (बृहदारण्यक, ५/१४/७), परोरजा य एष तपति (बृहदारण्यक, ५/१४/३)
(३) अन्य त्रिक-कई प्रकार के त्रिक हैं,जिनके माध्यम से विश्व को जानते हैं, पर कुछ बाकी रह जाता है। वह साढ़े ३ चक्र भुवनों (मनुष्य तथा लोक) का रेत (शुक्र, बीज) है।
सत्-चित्-आनन्द= सर्वव्यापी आनन्द हर चित् या विन्दु आकाश में है, उसमें जो अनुभव गम्य है, वह सत् है।
शंकर = खं ब्रह्म (शून्य आकाश) + कं ब्रह्म (कर्ता, करतार), रं ब्रह्म (गतिशील प्राण)
ॐ तत्-सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः (गीता, १७/२३)
ॐ का गति रूप रं है, तत् को नाम से कहते हैं। अतः प्राण निकलने पर कहते हैं-राम नाम सत्।
अतः त्रैगुण्य रूप वेद या विश्व जानने के बाद उससे परे की भी कल्पना करनी चाहिए।
त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन (गीता, २/४५)
विश्व मूल कुण्डलिनी-
सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि।
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवति विश्वतः॥ (ऋक्, १/१६४/३६)
६. अनन्त-
(१) अनन्त वेद-तैत्तिरीय ब्राह्मण (३/१०/११/३-४) के अनुसार भरद्वाज ने ३ आयु तक वेदाध्ययन किया पर पूरा नहीं हुआ। इन्द्र से एक और जीवन मांगा तो इन्द्र ने ३ विशाल पर्वत दिखाये जो ३ वेदों के स्वरूप थे। कहा-अनन्ताः वै वेदाः। उन पर्वतों से १-१ मुठ्ठी वेद ही पढ़ सके थे। यहां अनन्त बहुवचन में है, अतः कम से कम ३ प्रकार के अनन्त हैं। विष्णु सहस्रनाम में इन तीनों का उल्लेख हुआ है-अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय।
संख्येय अनन्त वह है जिसकी गणना १, २, ३, --- आदि क्रम से किया जा सके। इन संख्याओं आ क्रम भी अनन्त है। सभी भिन्न संख्याओं को भी क्रमबद्ध कर गिना जा सकता है। (कैण्टर सेट थिओरी)
असंख्येय अनन्त को संख्या क्रम में नहीं रख सकते न गिन सकते हैं। किसी भी रेखा में विन्दुओं की संख्या किसी क्रम में नहीं गिन सकते। यह २ प्रकार का है-
प्रमेय अनन्त संख्या को गणित सूत्र या परिभाषा द्वारा समझ सकते हैं जैसे परिधि/व्यास अनुपात।
अप्रमेय अनन्त को गणित या किसी सिद्धान्त से नहीं समझ सकते।
असंख्येय अनन्तों के भी विभिन्न प्रकार के समूह और बड़े अनन्त हैं।
मूर्ति रूप ऋग्वेद संख्येय है। गति रूप यजुर्वेद विन्दु की रेखा गति जैसा है और असंख्येय है। सामवेद में हर विन्दु तथा उसकी महिमा-दो प्रकार से असंख्येय हैं। इनका आधार या स्रोत अथर्व या ब्रह्म वेद इन सभी अनन्तों के समूह रूप हैं।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
वाक् में अनन्त के क्रमशः बड़े स्तर हैं-वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा।
(२) अनन्त विश्व-दृश्य जगत् के सभी स्तर पुरुष हैं। इनका आधार या अव्यक्त स्रोत पूरुष हैं। पूरुष के ४ भागों में १ ही भाग का प्रयोग हुआ। बाकी ३ भाग बचे रह गये जो उच्छिष्ट (भोजन से बचा जूठा) या ज्यायान् (भोजपुरी में जियान = बेकार, अनुपयुक्त) हैं। दृश्य या निर्मित जगत् का अव्यक्त आधार ही अनन्त है जिसने अपने सहस्र शीर्ष (स्रोत) में जगत् का धारण किया है।
दृश्य जगत् को गिन सकते हैं। जिसकी गणना हो सके वह गणेश है। विश्व निर्माण के बाद बचा ३ भाग उच्छिष्ट गणपति है। १०० अरब ब्रह्माण्ड, हमारे ब्रह्माण्ड में १०० अरब तारा, उसकी प्रतिमा मनुष्य मस्तिष्क में कलिल (लोमगर्त्त) हैं। मुहूर्त्त को ७ बार १५-१५ से भाग देने पर लोमगर्त्त होता है, १ सेकण्ड का प्रायः ७५,००० भाग। वर्ष में जितने लोमगर्त्त हैं, उतने ही आकाश में नक्षत्र हैं, अर्थात् १०० अरब। (शतपथ ब्राह्मण, १२/३/२/५, १०/४/४/२)। विश्व का कण या चूर्ण (खर्व) रूप में यही मान है। अतः खर्व = १०० अरब (खर्व स्थूलतनुं गजेन्द्र वदनम्)। खर्व का अन्य अर्थ नाटा है।
१०० अरब ब्रह्माण्डों का समूह महा गणपति तथा १०० अरब तारा समूह का हमारा ब्रह्माण्ड गणपति है। इसकी माप जगती छन्द में है। पृथ्वी को २४ बार २ गुणा करने पर सौर मण्डल-या गायत्री गुणा है। पुनः २४ बार २ गुणा करने पर ब्रह्माण्ड है। इन क्रमशः बड़े क्षेत्रों को अहर्गण कहते हैं। ब्रह्माण्ड सीमा तक ४९ अहर्गण हैं जिसमें कणों की गति ४९ प्रकार के मरुत् हैं। हमारा ब्रह्माण्ड अन्य खर्व ब्रह्माण्डों के आकर्षण से टिका है जो शेष या अनन्त है।
ब्रह्माण्ड की सर्पाकार भुजा वेद का अहिर्बुध्न्य (बुध्न्य अर्थात् बाढ़, अहि = सर्प) या पुराण का शेष नाग है। इसमें जहां सूर्य है, वहां भुजा की मोटाई के गोल (१४०० प्रकाश वर्ष व्यास) में १००० तारा हैं जो शेष के १००० सिर हैं। सूर्य रूपी विष्णु इसी शेष पर सोये हैं जो आकाश गंगा (ब्रह्माण्ड) के समुद्र में है। १००० सिरों में १ सिर सूर्य पर पृथ्वी कण मात्र है।
इस महर्लोक समुद्र में भी सौर मण्डल तैर रहा है। सूर्य ने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है (पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवि त्वं विष्णुना धृता)। सौर मण्डल का केन्द्र या नाभि सूर्य है जिससे आकर्षण रूपी कमल नाल पर पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर मर्त्य ब्रह्मा द्वारा सृष्टि है।
(३) पार्थिव अनन्त-उत्तरी गोल का नक्शा ४ भागों में बनता था जिनको भू-पद्म का ४ दल कहा है। इसी प्रकार दक्षिण गोल में भी बनता था। गोल पृथ्वी का समतल नक्शा बनाने के लिए १ लाख योजन ऊंचे ४ पार्श्वके मेरु पर प्रक्षेप करते थे। इसमें ध्रुव विन्दु पर अनन्त गुणा आकार हो जाता है। उत्तर ध्रुव जल में है अतः वहां कोई समस्या नहीं होती। पर दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है, उसका आकार अनन्त हो जाता है। अतः इसे अनन्त द्वीप कहते थे जिसका अलग से नवम नक्शा बनाना पड़ता था। (आर्यभटीय, ४/१२, लल्ल, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र, १७/३-४)। इसके २ भू-खण्ड (यम = यमल, जोड़ा) अतः इसे यम द्वीप भी कहते थे। नक्शा में दक्षिण भाग नीचे दिखाते हैं अतः इस अनन्त पर ही पृथ्वी टिकी है तथा नाग की तरह अक्ष पर गोल घूम रही है।
७. मनुष्य नाग-नाग जातियों का वर्णन महाभारत, उद्योग पर्व, अध्याय १०३ में है। अर्जुन ने खाण्डव प्रस्थ को तक्षक के अधिकार से छुड़ा कर वहां इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान दिल्ली) का निर्माण किया (महाभारत, आदि पर्व, २२२-२२६ अध्याय)। वह अपने मूल स्थान तक्षशिला चला गया। पाण्डवों से शत्रुता के कारण इसकी दुर्योधन से मैत्री हुई तथा परीक्षित की हत्या की थी (महाभारत, आदि पर्व, अध्याय, ४३, ५०)। जनमेजय ने इसे मारने के लिए नाग यज्ञ किया। नागों के २ नगरों को श्मशान बना दिया जिनके नाम मोइन-जो-दरो (मृतक स्थान) तथा हड़प्पा (हड्डियों का ढेर) हुए। यह वर्णन गुरु गोविन्द सिंह ने एक राम मन्दिर की दीवाल पर लिखवाया था। दुर्योधन ने तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसमें ३०,००० छात्र रहते थे (एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का पारसी अनुवाद मज़्मा ए तवारीख)। तक्षक का एक नगर कश्मीर में भी था, जो वितस्ता नाम से प्रसिद्ध हुआ (पद्म पुराण, ३/२५/२)। पुरुवंश से तक्षशिला की शत्रुता सिकन्दर काल तक चलती रही। सभी तक्षक एक ही नहीं थे। तक्षक जाति कद्रू की सन्तान या काद्रवेय थी। तक्षक जाति का एक भवन सुतल (जापान आदि) में था (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२०/२४) में था। वहां नागासाकी नगर है। नागाशी वास्तव में नाग-शत्रु गरुड़ की सन्तान थी (महाभारत, उद्योग पर्व, १०१/९)। इस जाति का निवास निषध पर्वत पर भी था (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/१७/३४)। अफ्रीका से जो तक्षक जाति के लोग समुद्र मन्थन के लिए झारखण्ड आये थे, उनका निवास स्थान कडरू (कद्रू) है।
समुद्र मन्थन या खनिज दोहन में समन्वय वासुकि नाग ने किया था जो मूलतः पाताल लोक या उत्तर अमेरिका के थे (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/२०/३९-४१)। मन्थन कामुख्य स्रोत मन्दार पर्वत था जो मथानी के आकार में सिंहभूमि से भागलपुर में गंगा तट तक चला गया। है। वहां वासुकिनाथ मन्दिर है। भागलपुर नाम भी नागों की भोगवती पुरी के नाम पर है। वासुकि की भोगवती पुरी प्रयाग में भी थी (अग्नि पुराण, १११/१०)।
नागों का नरसंहार रोकने के लिए वासुकि नाग ने अपनी बहन जरत्कारु के पुत्र आस्तीक को भेजा था (देवी भागवत, २/११)। अतः आस्तीक भी उत्तर अमेरिका ए ही थे जिनको आजकल मेक्सिको में एज्टेक कहते हैं। पुरुवंश के नहुष भी ऋषि शाप से पाताल चले गये थे और नाग हुए (महाभारत, उद्योग पर्व, १७/१४-१८)। उनके वंशज मेक्सिको के नहुआ हैं। नहुष नागों को भी कद्रु का पुत्र कहा गया है (महाभारत, आदि पर्व, ३५/९)।
नाग तथा सर्प एक ही जाति के है। भारत की शत्रु जातियों को सर्प कहते थे जिनके विरुद्ध गरुड़ का अभियान चलता रहता था। वासुकि के नागाधिप व तक्षक के सर्पाधिप बनने का उल्लेख है (मत्स्य पुराण, ८/७, वायु पुराण, ६९/३२२)। तक्षक कॊ भी प्रायः नाग ही कहा गया है।
रांगेय राघव ने ’महागाथा-यात्रा’ में भारत में नाग जाति के स्थानों का उल्लेख किया है जो सर्पों के नाम पर हैं-नागपुर, अहिच्छत्र, अहिगृह (आगरा), नागपट्टनम्, अहोबिल, भोगल (फोगला), भागलपुर, भोगवती। यह अलग जाति नहीं थी। व्यापार के लिए सामान ले जाने वाले नाग थे। इन्द्र के सहायक नाग थे तथा तक्षक से उनकी मैत्री थी (आदि पर्व, २२२/७)। इन्द्र को अच्युत-च्युतः कहा गया है (ऋक्, २/१२/९) अर्थात् जो अपराजित को भी पराजित कर सके। इन्द्र पूर्व के लोकेपाल थे अतः पूर्व में असम के राजा को च्युत या चूतिता कहते थे। इनका नागपुर चुतिया-नागपुर था जो अंग्रेजी माध्यम से छोटानागपुर हो गया। आज भी रांची में चुतिया मोड़ है।
अहिगृह वालों को अघरिया कहते हैं जो पश्चिम ओड़िशा, छत्तीसगढ़ का व्यापारी वर्ग है। इनकी उपाधि पटेल है। एक तक्षक सौराष्ट्र में रैवत राजा बना था जिसके वंशज नागर हैं (लक्ष्मीनारायण संहिता, १/४९९/११, २/२८/१६)।
अग्रवाल नाम अहिगृह से नहीं है जैसा रांगेय राघव का अनुमान था। वेद में नेता को अग्नि या अग्रि (अग्रणी) कहा गया है।
अग्ने नय सुपथा राये (ईशावास्योपनिषद्) = अग्नि! हमें अच्छॆ मार्ग पर ले चलो (नय से नेता हुआ है)।
भारत का अग्नि विश्व का भरण पोषण करता था इससे उसको भरत तथा इस देश को भारत कहा गया। यही अग्नि या अग्रि लोकभाषा में अग्रसेन है तथा उनके सहयोगी अग्रवाल।
स यदस्य सर्वस्याग्र सृजत तस्मादग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम्। शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/११)
= सबसे प्रथम उत्पन्न होने के कारण यह अग्रि (नेता) हुआ, इसे परोक्ष में अग्नि कहा जाता है।
अग्नेर्महाँ ब्राह्मण भारतेति । एष हि देवेभ्य हव्यं भरति । (तैत्तिरीय संहिता, २/५/९/१, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/५/३/१, शतपथ ब्राह्मण, १/४/१/१)
= ब्रह्मा ने भारत के अग्नि को महान् कहा था क्योंकि यह देवों को भोजन देता है।
भरणात्प्रजनाच्चैष मनुर्भरत उच्यते । एतन्निरुक्त वचनाद् वर्षं तद् भारतं स्मृतम् ।
यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तिर्यगग्यामः प्रकीर्तितः । य एनं जयते कृत्स्नं स सम्राडिति कीर्तितः ।
(मत्स्य पुराण, ११४/५,६, वायु पुराण, ४५/७६)
= लोकों के भरण तथा पालन के कारण इस देश का मनु (शासक) भरत कहा जाता है। निरुक्त परिभाषा के अनुसार भी इस देश को भारत कहा गया है।
विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत आस होई॥ (राम चरित मानस, बालकाण्ड, ९६/५)
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.