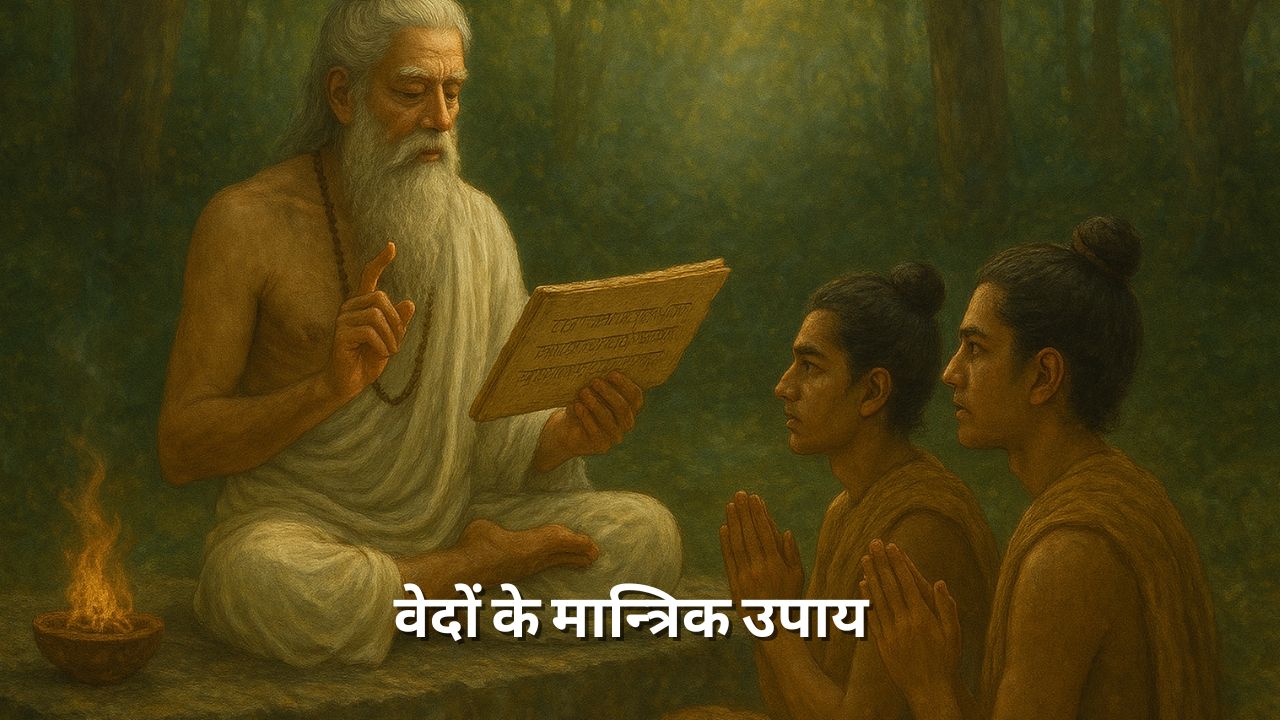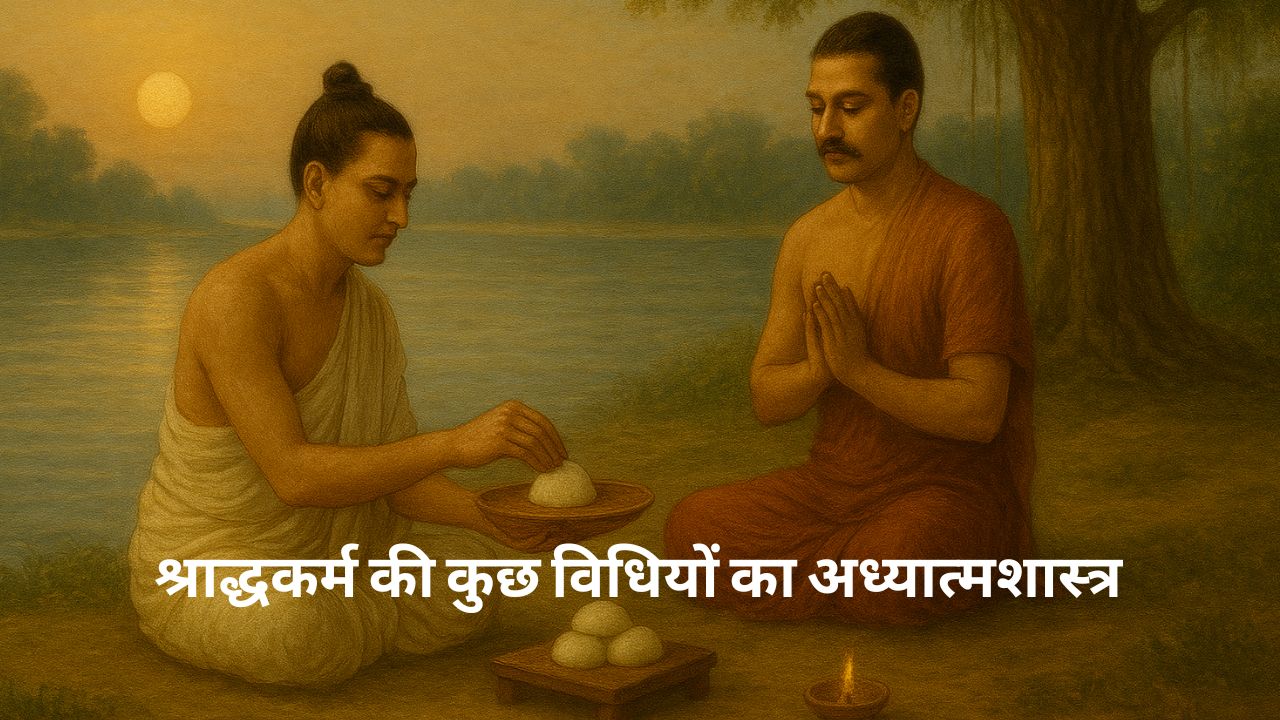- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 अनिल गोविंद बोकील ।
नाथसंप्रदाय मे पूर्णाभिषिक्त और तंत्र मार्ग मे काली कुल मे पूर्णाभिषिक्त के बाद साम्राज्याभिषिक्त ।
"राम" शब्द अत्यन्त विलक्षण है । बीजमन्त्र के रूप मे इसके प्रयोग साधको द्वारा प्राचीन काल से होते आ रहे है । कई साधक तो परमपद तक पहुंच गये है ।
"राम" बोलते ही हमारे सामने दशरथ पुत्र धनुर्धारी राम ही आते है । पर यह शब्द तो इसके पहले भी था ही । इसलिए गुरू वसिष्ठजी द्वारा प्रथम दशरथ पुत्र को यह सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया गया ।
समस्त धार्मिक परंपराओ मे " राम " तथा " ओम " प्रतिकात्मक है । और इसके अलावा ; " राम " ; सार्थक भी है । अगर कोई प्रश्न करे कि ; " राम " शब्द मे ऐसा क्या है ? तो इसका उत्तर होगा एक प्रतिप्रश्न ( Counter questioning ) कि ; राम मे क्या नहीं है ? अब थोडा विचार करेंगे ।
राम शब्द मे तीन वर्ण ( अक्षर ) है ।
र + अ + म = राम ।
इन्ही तीन अक्षरो को हम ६ प्रकार से लिख सकते है ।
( १ ) र + अ + म = राम ।
( २ ) र + म + अ = रमा ।
( ३ ) म + अ + र = मार ।
( ४ ) म + र + अ = मरा ।
( ५ ) अ + म + र = अमर ।
( ६ ) अ + र + म = अरम ।
इस प्रकार से देखा तो ; ध्यान मे आता है कि ; इन तीन अक्षरो मे ; सृष्टी के अंतर्गत ; उत्पत्ति-सृजन-विलय सबकुछ समाविष्ट हुआ है । और सिर्फ इतना ही नहीं ; तो यह भी स्पष्ट ( प्रकट ) होता है कि ; परस्परविरोधी प्रतीत होनेवाला ( दिखनेवाला ) जो भी है - सब एक ही है । हमे सिर्फ आभास होता रहता है विरोध का ।। अब जरा विस्तार से देखते है ।
अब जो विवेचन आप लोग पढेंगे उसमे ; प्रकृति व पुरुष शब्द तत्व-रूप मे जाने -- और इन्ही के सगुण रूप राम और रमा जाने ।
जो राम " पुरुष " है ; उसीकी स्त्री प्रकृति है " रमा " ! पुरुष रूप मे राम समस्त विश्वब्रह्माण्ड सृष्टी का " कारण " है ; आक्रमक बल है ; और प्रकृति जो " रमा " ; वही स्त्री-रूप मे संग्राहक है ; सृजन का निर्माण-कर्ती है । यहांतक समझ गये हम लोग । अब एक एक युग्म ( जोडी ) का अर्थ देखेंगे हम ।
" राम " पुरु बल प्रधान है ; और " रमा " है संवेदना प्रधान !! राम बुद्धीमान है ; संश्लेषणात्मक है - बुद्धी हमेशा मार्गनिर्देश करती है ; और भावना ( चित्त ) द्वारा उसे स्थायित्व प्रदान किया जाता है । और सृजन के लिए तो यही दो आधार होते है ना ? क्योंकि जबतक राम और रमा ; अलग रहेंगे – तब तक सृजन की संभावना ही नहीं रहेगी । अगर उपमा देनी हो तो यू कहा जा सकता है कि ; राम और रमा तो दो किनारे ( तीर ) है नदी के । और उन्हे संयुक्त किया जा सकता है / जोडा जा सकता है / एकत्रित लाया जा सकता है वह - " म + अ + र = मार " ( या काम ) द्वारा ही । भ. बुद्ध तो इस " मार " पर विजय की बहुत ही प्रशंसा करते है ।
हमारे ऋषि-मुनीयो के लिए भी यह काम-विजय आदर्श रहा है । " नारद-मोह " नामक संपूर्ण आख्यान तो बहुत ही सारगर्भित है । अब आगे चलते है - यह " मार " है ; इसलिए तो उसके भी पार जाकर ;परमपद / एकत्व प्राप्त किया जा सकता है । अन्यथा क्या होगा ? होगा ये कि ; राम और रमा - दोनो मार द्वारा एकत्र आकर प्रचंड सृष्टी फैलाते रहेंगे । पुरुष व प्रकृति भिन्न नहीं है यह सत्य हैही ; साथ ही उनके परस्पर संबंधो की कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है । अद्वैत दृष्टी से जो राम है ; वही रमा है ; वही मार है ।
अब अगला युग्म देखेंगे ।
जो " अमर " है ; वही " मरा " है । वैसे तात्विक दृष्टी से देखा जाय तो ; अमरत्व और मरण-धर्मिता ; शाश्वतता और क्षणभंगुरत्व- अलग अलग बिलकुल नहीं होते । ये तो एक दूसरे के सापेक्ष ( Dependable ) ही तो है ना ? अत: एक बात समझ मे आएगी कि ; हम जिसे क्षणभंगुर कहते है -- वो वास्तव मे " सदैव परिवर्तनशील " ही होता है । ( Physics का नियम याद आया या नहीं ? ) और वही " अमर " होता है । मृत्यु या परिवर्तन; मात्र आभास है । मृत्यु कभी भी किसी की भी होती ही नहीं - जो होता है वह सिर्फ परिवर्तन ही होता है । मृत्यु जैसा झूठ अन्य कुछ भी नहीं । हां; जब तक हमे मृत्यु " वास्तव " लगता है; तब तक " मरा " है ही । कहां जीवित है वो?
इस प्रकार दोनो पक्ष ( विचारधारा ) आपके समक्ष रखे है । इन्हे समझ लेने का प्रयास अवश्य करे ।
यह " अमर व मरा " मे ही -- अर्थात
" राम " मे ही निहित ( Included ) होते है । साथ ही यह भी सत्य है कि ; ये दोनो सदैव ; एक ही समय ; एकत्रित उपस्थित रहते है । हरेक बात का / चीज का ; चरम यथार्थ --- शाश्वत ; नित्य ; अपरिवर्तनशील ; अमर ; अनादि तथा अनंत - ऐसा ही तो है । इसी के साथ इसका विवर्त ( आभासी ) स्वरूप क्षणभंगुर ; अनित्य ; सदैव परिवर्तनशीलता ; मरण-धर्मा ; तथा समित है ।
थोडासा मनन चिंतन करनेपर यह पक्का समझ मे जरूर आएगा ।
जय श्रीराम ! अब ६ वा शब्द है - अ + र + म = अरम ।अरम याने जिस मे रमा नहीं जा सकता ( रमा = रमना या रममाण होना । )।
कितनी विचित्र बात है ना ? जहां विदवज्जन ; गुणीजन कहते है कि ; सर्वत्र " रमा " है --- तो फिर ये अरम हुआ ही कैसे ? यही तो फर्क है -- विद्वान और सिद्ध मे ! विद्वान " उस " को देखता है ; समझ लेने का प्रयास करता है । और सिद्ध ? सिद्ध तो उसकी अनुभूती लेकर उसी मे एकरूप ( अद्वैत ) हो जाता है । संत तुलसीदासजी कहते है -
" जानत तुमहिं ; तुमहिं हो जाई "
ओ$हो$$हो पानी की बुंद गिर गयी सागर मे ; और खुद ही सागर बन गयी । बुंद का अस्तित्व तो मिट गया । पर दूसरे अर्थ से वो महाजीवन को प्राप्त हुई ना ? जहां बुंद ही बची नहीं ; वहां रमेगा कौन ? और कैसे ? तो यही परासत्ता ; यही परम-वास्तव ; यही परब्रह्म - अरम हो सकता है ना ?
रामचरितमानसकार कहते है -
" सोई जाने जेहि देहु जनाई "
और ऐसे ही इस प्रकार के अर्थ की वजह से ही तो रामनाम बन गया है महामन्त्रराज ! इसी के निरंतर स्मरण से / जप से ; उसके अंतर्गत का निहित सार ; समस्त गूढ रहस्य ; अर्थ ; और साथ ही सृष्टी के सभी रहस्य - साधको को जीवनमुक्ती का परमपद बहाल करा देते है ।
अब नाथपंथी अर्थ भी देखे ।
रा = ब्रह्म । और म = माया । " राम " का उच्चारण करते ही ब्रह्म व माया अलग अलग महसूस होना चाहिये । यही होगा पूर्ण सत्य और वास्तव राम-दर्शन !
श्रीरामरक्षा स्तोत्र मे कहा गया ही है ना -
" सहस्रनाम ततुल्यम रामनाम वरानने "
क्यों कहा गया है ऐसा ? यह अब ध्यान मे आया होगा । जय श्रीराम ।
विवेचन पूरा हुआ है - ऐसा तो नहीं कह सकता । बहुत कुछ शेष भी है । बस्स ! इतनी ही अपेक्षा लिखते समय रखी थी कि कम से कम इस दिशा मे विचारमंथन तो शुरू होगा । अब कुछ और बिंदू आपके विचारार्थ रखता हूँ ।
इस प्रदीर्घ प्रस्तुति मे ; राम और रमा ; बिलकुल अलग प्रकार से ; कामेश व कामेश्वरी के संदर्भ मे आये हुए है ।
अमर व मरा = सहज ; सुरेख स्वप्नविश्व दर्पण नगरी ।। " सत्य और भासात्मक सत्य " इस युग्म को Physics का नियम लगाकर यह Theory मेरे द्वारा लिखी गयी है ।
अरम मे से एकरूपत्व आ गया । रमनेवाला ; रमा लेनेवाला और जिस मे रमना है वो इन मे अलगपन शेष ही नहीं रहा और एक बात आप जैसे अभ्यास को के चिंतन हेतु दे रहा हूँ कि -
इन तीन अक्षरोपर आधारित तथा इसी त्रयी के पार ले जानेवाला नाम भी -
" र + आ + म + अ = तेज है -- जो माया को दूर ( नष्ट ) करता है । भास - आभास को ही उडा देता है ।
सर्वप्रथम किये गये उल्लेख के अनुसार ; अगर ; र अ म ; बीजमन्त्र ; चक्रोपर के स्थान आदिपर भी सोचा जाय तो ; अत्यन्त परिपूर्ण अर्थ मिलेगा । अर्थात अभी का परसेप्शन अलग है - इसलिए नहीं लिखा है इस प्रस्तुति मे । फिर भी अभ्यासको के विचारो को इस से अधिक गहरापन आएगा और ; उसका उपयोग साधक कर सकेंगे । इसीलिए यहां सिर्फ संक्षेप मे उल्लेख करके ; बस्स करता हूँ । क्योंकि मै संपूर्ण तंत्रमार्ग खुला नहीं कर सकता । तो मेरे दोस्तो यहांपर इस प्रस्तुति को पूर्ण-विराम देते है ।
नमो आदेश !
अनिल गोविंद बोकील ।
नाथसंप्रदाय मे पूर्णाभिषिक्त और तंत्र मार्ग मे काली कुल मे पूर्णाभिषिक्त के बाद साम्राज्याभिषिक्त ।
"राम" शब्द अत्यन्त विलक्षण है । बीजमन्त्र के रूप मे इसके प्रयोग साधको द्वारा प्राचीन काल से होते आ रहे है । कई साधक तो परमपद तक पहुंच गये है ।
"राम" बोलते ही हमारे सामने दशरथ पुत्र धनुर्धारी राम ही आते है । पर यह शब्द तो इसके पहले भी था ही । इसलिए गुरू वसिष्ठजी द्वारा प्रथम दशरथ पुत्र को यह सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया गया ।
समस्त धार्मिक परंपराओ मे " राम " तथा " ओम " प्रतिकात्मक है । और इसके अलावा ; " राम " ; सार्थक भी है । अगर कोई प्रश्न करे कि ; " राम " शब्द मे ऐसा क्या है ? तो इसका उत्तर होगा एक प्रतिप्रश्न ( Counter questioning ) कि ; राम मे क्या नहीं है ? अब थोडा विचार करेंगे ।
राम शब्द मे तीन वर्ण ( अक्षर ) है ।
र + अ + म = राम ।
इन्ही तीन अक्षरो को हम ६ प्रकार से लिख सकते है ।
( १ ) र + अ + म = राम ।
( २ ) र + म + अ = रमा ।
( ३ ) म + अ + र = मार ।
( ४ ) म + र + अ = मरा ।
( ५ ) अ + म + र = अमर ।
( ६ ) अ + र + म = अरम ।
इस प्रकार से देखा तो ; ध्यान मे आता है कि ; इन तीन अक्षरो मे ; सृष्टी के अंतर्गत ; उत्पत्ति-सृजन-विलय सबकुछ समाविष्ट हुआ है । और सिर्फ इतना ही नहीं ; तो यह भी स्पष्ट ( प्रकट ) होता है कि ; परस्परविरोधी प्रतीत होनेवाला ( दिखनेवाला ) जो भी है - सब एक ही है । हमे सिर्फ आभास होता रहता है विरोध का ।। अब जरा विस्तार से देखते है ।
अब जो विवेचन आप लोग पढेंगे उसमे ; प्रकृति व पुरुष शब्द तत्व-रूप मे जाने -- और इन्ही के सगुण रूप राम और रमा जाने ।
जो राम " पुरुष " है ; उसीकी स्त्री प्रकृति है " रमा " ! पुरुष रूप मे राम समस्त विश्वब्रह्माण्ड सृष्टी का " कारण " है ; आक्रमक बल है ; और प्रकृति जो " रमा " ; वही स्त्री-रूप मे संग्राहक है ; सृजन का निर्माण-कर्ती है । यहांतक समझ गये हम लोग । अब एक एक युग्म ( जोडी ) का अर्थ देखेंगे हम ।
" राम " पुरु बल प्रधान है ; और " रमा " है संवेदना प्रधान !! राम बुद्धीमान है ; संश्लेषणात्मक है - बुद्धी हमेशा मार्गनिर्देश करती है ; और भावना ( चित्त ) द्वारा उसे स्थायित्व प्रदान किया जाता है । और सृजन के लिए तो यही दो आधार होते है ना ? क्योंकि जबतक राम और रमा ; अलग रहेंगे – तब तक सृजन की संभावना ही नहीं रहेगी । अगर उपमा देनी हो तो यू कहा जा सकता है कि ; राम और रमा तो दो किनारे ( तीर ) है नदी के । और उन्हे संयुक्त किया जा सकता है / जोडा जा सकता है / एकत्रित लाया जा सकता है वह - " म + अ + र = मार " ( या काम ) द्वारा ही । भ. बुद्ध तो इस " मार " पर विजय की बहुत ही प्रशंसा करते है ।
हमारे ऋषि-मुनीयो के लिए भी यह काम-विजय आदर्श रहा है । " नारद-मोह " नामक संपूर्ण आख्यान तो बहुत ही सारगर्भित है । अब आगे चलते है - यह " मार " है ; इसलिए तो उसके भी पार जाकर ;परमपद / एकत्व प्राप्त किया जा सकता है । अन्यथा क्या होगा ? होगा ये कि ; राम और रमा - दोनो मार द्वारा एकत्र आकर प्रचंड सृष्टी फैलाते रहेंगे । पुरुष व प्रकृति भिन्न नहीं है यह सत्य हैही ; साथ ही उनके परस्पर संबंधो की कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है । अद्वैत दृष्टी से जो राम है ; वही रमा है ; वही मार है ।
अब अगला युग्म देखेंगे ।
जो " अमर " है ; वही " मरा " है । वैसे तात्विक दृष्टी से देखा जाय तो ; अमरत्व और मरण-धर्मिता ; शाश्वतता और क्षणभंगुरत्व- अलग अलग बिलकुल नहीं होते । ये तो एक दूसरे के सापेक्ष ( Dependable ) ही तो है ना ? अत: एक बात समझ मे आएगी कि ; हम जिसे क्षणभंगुर कहते है -- वो वास्तव मे " सदैव परिवर्तनशील " ही होता है । ( Physics का नियम याद आया या नहीं ? ) और वही " अमर " होता है । मृत्यु या परिवर्तन; मात्र आभास है । मृत्यु कभी भी किसी की भी होती ही नहीं - जो होता है वह सिर्फ परिवर्तन ही होता है । मृत्यु जैसा झूठ अन्य कुछ भी नहीं । हां; जब तक हमे मृत्यु " वास्तव " लगता है; तब तक " मरा " है ही । कहां जीवित है वो?
इस प्रकार दोनो पक्ष ( विचारधारा ) आपके समक्ष रखे है । इन्हे समझ लेने का प्रयास अवश्य करे ।
यह " अमर व मरा " मे ही -- अर्थात
" राम " मे ही निहित ( Included ) होते है । साथ ही यह भी सत्य है कि ; ये दोनो सदैव ; एक ही समय ; एकत्रित उपस्थित रहते है । हरेक बात का / चीज का ; चरम यथार्थ --- शाश्वत ; नित्य ; अपरिवर्तनशील ; अमर ; अनादि तथा अनंत - ऐसा ही तो है । इसी के साथ इसका विवर्त ( आभासी ) स्वरूप क्षणभंगुर ; अनित्य ; सदैव परिवर्तनशीलता ; मरण-धर्मा ; तथा समित है ।
थोडासा मनन चिंतन करनेपर यह पक्का समझ मे जरूर आएगा ।
जय श्रीराम ! अब ६ वा शब्द है - अ + र + म = अरम ।अरम याने जिस मे रमा नहीं जा सकता ( रमा = रमना या रममाण होना । )।
कितनी विचित्र बात है ना ? जहां विदवज्जन ; गुणीजन कहते है कि ; सर्वत्र " रमा " है --- तो फिर ये अरम हुआ ही कैसे ? यही तो फर्क है -- विद्वान और सिद्ध मे ! विद्वान " उस " को देखता है ; समझ लेने का प्रयास करता है । और सिद्ध ? सिद्ध तो उसकी अनुभूती लेकर उसी मे एकरूप ( अद्वैत ) हो जाता है । संत तुलसीदासजी कहते है -
" जानत तुमहिं ; तुमहिं हो जाई "
ओ$हो$$हो पानी की बुंद गिर गयी सागर मे ; और खुद ही सागर बन गयी । बुंद का अस्तित्व तो मिट गया । पर दूसरे अर्थ से वो महाजीवन को प्राप्त हुई ना ? जहां बुंद ही बची नहीं ; वहां रमेगा कौन ? और कैसे ? तो यही परासत्ता ; यही परम-वास्तव ; यही परब्रह्म - अरम हो सकता है ना ?
रामचरितमानसकार कहते है -
" सोई जाने जेहि देहु जनाई "
और ऐसे ही इस प्रकार के अर्थ की वजह से ही तो रामनाम बन गया है महामन्त्रराज ! इसी के निरंतर स्मरण से / जप से ; उसके अंतर्गत का निहित सार ; समस्त गूढ रहस्य ; अर्थ ; और साथ ही सृष्टी के सभी रहस्य - साधको को जीवनमुक्ती का परमपद बहाल करा देते है ।
अब नाथपंथी अर्थ भी देखे ।
रा = ब्रह्म । और म = माया । " राम " का उच्चारण करते ही ब्रह्म व माया अलग अलग महसूस होना चाहिये । यही होगा पूर्ण सत्य और वास्तव राम-दर्शन !
श्रीरामरक्षा स्तोत्र मे कहा गया ही है ना -
" सहस्रनाम ततुल्यम रामनाम वरानने "
क्यों कहा गया है ऐसा ? यह अब ध्यान मे आया होगा । जय श्रीराम ।
विवेचन पूरा हुआ है - ऐसा तो नहीं कह सकता । बहुत कुछ शेष भी है । बस्स ! इतनी ही अपेक्षा लिखते समय रखी थी कि कम से कम इस दिशा मे विचारमंथन तो शुरू होगा । अब कुछ और बिंदू आपके विचारार्थ रखता हूँ ।
इस प्रदीर्घ प्रस्तुति मे ; राम और रमा ; बिलकुल अलग प्रकार से ; कामेश व कामेश्वरी के संदर्भ मे आये हुए है ।
अमर व मरा = सहज ; सुरेख स्वप्नविश्व दर्पण नगरी ।। " सत्य और भासात्मक सत्य " इस युग्म को Physics का नियम लगाकर यह Theory मेरे द्वारा लिखी गयी है ।
अरम मे से एकरूपत्व आ गया । रमनेवाला ; रमा लेनेवाला और जिस मे रमना है वो इन मे अलगपन शेष ही नहीं रहा और एक बात आप जैसे अभ्यास को के चिंतन हेतु दे रहा हूँ कि -
इन तीन अक्षरोपर आधारित तथा इसी त्रयी के पार ले जानेवाला नाम भी -
" र + आ + म + अ = तेज है -- जो माया को दूर ( नष्ट ) करता है । भास - आभास को ही उडा देता है ।
सर्वप्रथम किये गये उल्लेख के अनुसार ; अगर ; र अ म ; बीजमन्त्र ; चक्रोपर के स्थान आदिपर भी सोचा जाय तो ; अत्यन्त परिपूर्ण अर्थ मिलेगा । अर्थात अभी का परसेप्शन अलग है - इसलिए नहीं लिखा है इस प्रस्तुति मे । फिर भी अभ्यासको के विचारो को इस से अधिक गहरापन आएगा और ; उसका उपयोग साधक कर सकेंगे । इसीलिए यहां सिर्फ संक्षेप मे उल्लेख करके ; बस्स करता हूँ । क्योंकि मै संपूर्ण तंत्रमार्ग खुला नहीं कर सकता । तो मेरे दोस्तो यहांपर इस प्रस्तुति को पूर्ण-विराम देते है ।
नमो आदेश !
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.