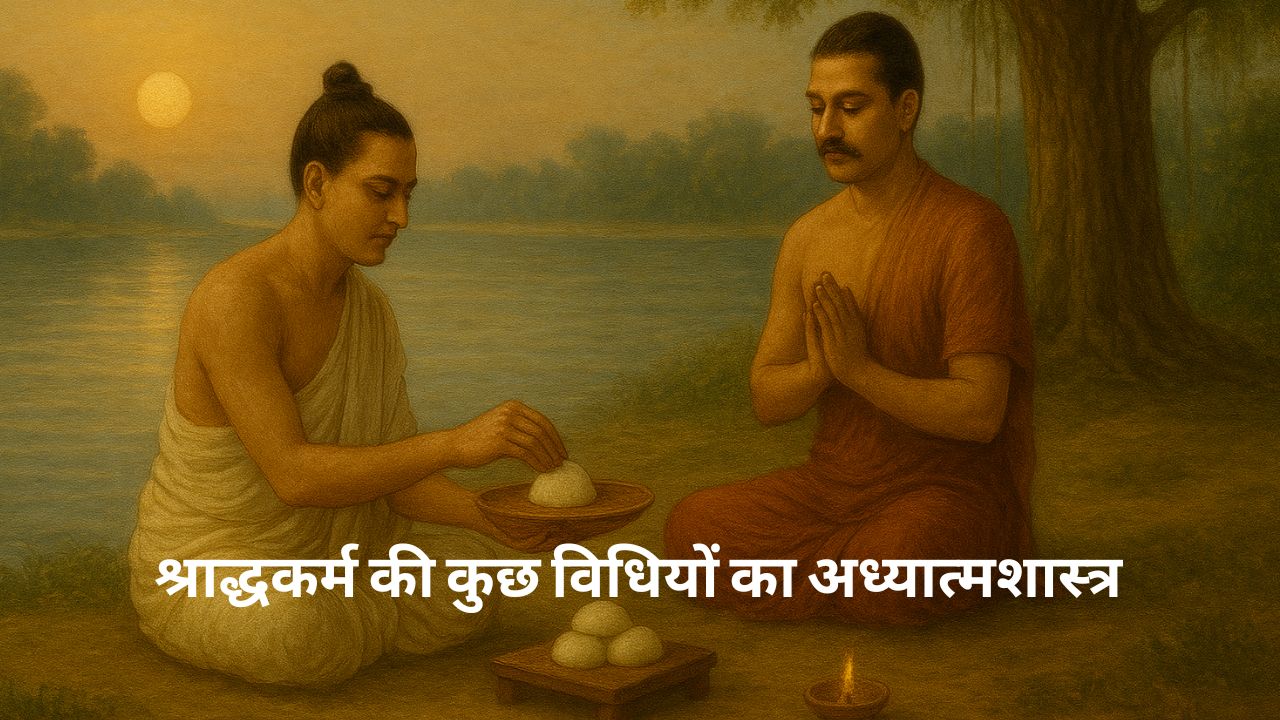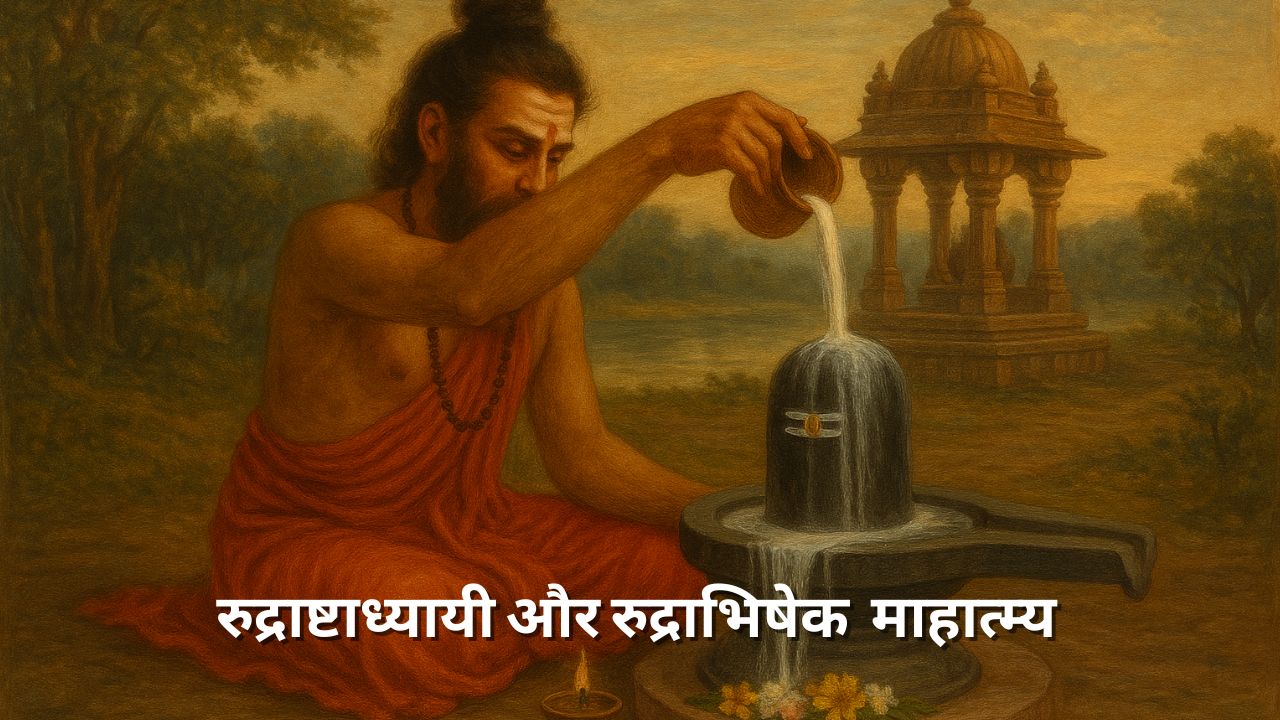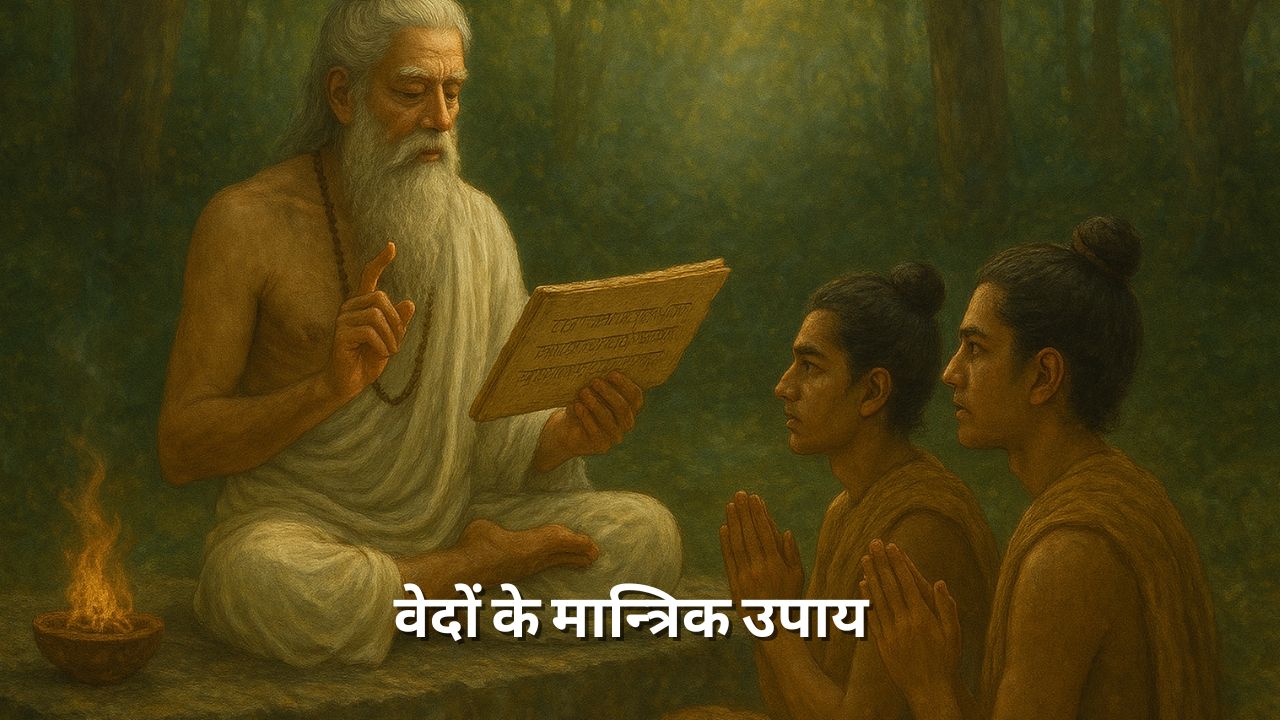- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
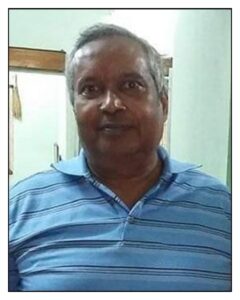 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
Mystic Power- १. वेद भूमिका-
हर लेखक अपनी रचना को स्पष्ट करने के लिए एक भूमिका लिखता है। वेद संहिताओं का वर्तमान रूप २८वें व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया। उसे अपने समय के इतिहास द्वारा स्पष्ट करने केलिए महाभारत लिखा जो वेदानुरूप होने के कारण पञ्चम वेद कहा जाता है।
सपादलक्षं च तथा भारतं मुनिना कृतम्।
इतिहास इति प्रोक्तं पञ्चमं वेदसम्मतम्॥
(देवीभागवत पुराण, २/२६)
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)
Mystic Power- १. वेद भूमिका-
हर लेखक अपनी रचना को स्पष्ट करने के लिए एक भूमिका लिखता है। वेद संहिताओं का वर्तमान रूप २८वें व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया। उसे अपने समय के इतिहास द्वारा स्पष्ट करने केलिए महाभारत लिखा जो वेदानुरूप होने के कारण पञ्चम वेद कहा जाता है।
सपादलक्षं च तथा भारतं मुनिना कृतम्।
इतिहास इति प्रोक्तं पञ्चमं वेदसम्मतम्॥
(देवीभागवत पुराण, २/२६)
 वेद ब्रह्म का शब्द रूप है-
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे (ब्रह्मणी वेदितव्ये) शब्द ब्रह्म परं च यत्।
शब्द (शाब्दे) ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥
(मैत्रायणी उपनिषद्, ६/२२)
वेद ब्रह्म का शब्द रूप है-
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे (ब्रह्मणी वेदितव्ये) शब्द ब्रह्म परं च यत्।
शब्द (शाब्दे) ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥
(मैत्रायणी उपनिषद्, ६/२२)
 अव्यक्त ब्रह्म न पुरुष है, न स्त्री-
स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान न जन्तुः।
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः॥
(गजेन्द्र मोक्ष, भागवत पुराण, ८/३/२४)
सृष्टि के लिए ब्रह्म २ रूप धारण करता है-चेतन तत्त्व को पुरुष तथा पदार्थ तत्त्व को प्रकृति या देवी कहा है। अतः २ रूपों को स्पष्ट करने के लिए २ ग्रन्थ लिखे-भागवत तथा देवी भागवत पुराण।
पूर्व काल में २४वें व्यास ऋक्ष या वाल्मीकि ने भी वेद को स्पष्ट करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र लिखा-
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे।
वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना।
तस्माद् रामायणं देवि वेद एव न संशयः॥
(अगस्त्य संहिता का श्लोक नीलकण्ठ कृत मन्त्र रामायण प्रथम श्लोक के स्वोपज्ञ भाष्य में उद्धृत)
बाद में सायण ने अपने वेद भाष्य के आरम्भ में वेद भाष्य भूमिका लिखी।
१७३० में बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूत्र के गोविन्द भाष्य के आरम्भ में वेद व्याख्या के लिए भागवत माहात्म्य लिखा-
उक्तं च गारुडे-
अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां, भारतार्थ विनिर्णयः।
गायत्री भाष्य रूपोऽसौ, वेदार्थ परिवृंहणः॥
सनातन वैदिक परम्परा को नष्ट करने के लिए विलियम जोन्स तथा पार्जिटर नियन्त्रित पुराण प्रकाशन में गरुड पुराण के इस श्लोक को हटाया गया। अंग्रेजों ने पुराण तथा वर्णाश्रम धर्म की निन्दा को प्रश्रय दिया तथा वैसे समाज बनवाये। यह अभी तक चल रहा है।
२. मङ्गलाचरण-
इसके ३ श्लोक वेद के सार रूप हैं तथा भागवत पुराण का उद्देश्य और विषय स्पष्ट करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो ऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, सत्यं परं धीमहि॥१॥
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां,
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, ताप-त्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परैरीश्वरः,
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥२॥
निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।
पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥३॥
प्रथम श्लोक अर्थ के ४ श्लोक देवीभागवत (२/५-८) में हैं। इनमें प्रथम श्लोक-
सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं, शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम्।
संहृत्य कल्प समये रमते तथैका, तां विश्वजननीं मनसा स्मरामि॥
द्वितीय श्लोक के समानार्थ देवीभागवत (३/३४-३८) हैं। प्रथम २ श्लोक हैं-
कृष्णद्वैपायनात् प्रोक्तं पुराणं च मया श्रुतम्।
श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखौघनाशनम्॥३४॥
कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थ परिबृंहितम्।
सर्वागमरसारामं मुमूक्षूणां सदा प्रियम्॥३५॥
तृतीय श्लोक के समानार्थक (देवीभागवत, ३/३९-४३) है। इनमें प्रथम श्लोक-
श्रीमद्भागवतामरांघ्रिप फलास्वादादरः सत्तमाः,
संसारार्णव दुर्विगाह्य सलिलं सन्तर्तुकामः शुकः।
नानाख्यान रसालयं श्रुतिपुटैः प्रेम्णाशृणोदद्भुतं,
तच्छृत्वा न विमुच्यते कलिभयादेवंविधः कः क्षितौ॥३९॥
३. प्रथम मन्त्र की वेदता-
(पुरी गोवर्धन पीठाधीश स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती की पुस्तक शुक-सुधा के आधार पर)
अर्थ-इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिस परमात्मा से है, जो कार्य प्रपञ्च में प्रविष्ट तथा उससे व्यतिरिक्त भी होने से स्वतः सिद्ध, सर्वज्ञ, स्वप्रकाश है; जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया, जिसमें विचारकुशल विद्वान् भी मोहित होते हैं; तेज, जल, मिट्टी का जैसे परस्पर विनिमय (आभास) होता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणात्मक जगत् सत्य जैसा दीखता है, अपने स्वरूप वैभव से माया को दूर हटाने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
ब्रह्म-सूत्र से समतुल्यता-
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (१/१/१) = निरस्त कुह कं सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य यतः (१/१/२)= वही है।
तत्तु समन्वयात् (१/१/४) = (अर्थेषु) अन्वयात्।
ईक्षतेर्नाशब्दम् (१/१/५) = अर्थेष्वभिज्ञः।
एतेन सर्वे व्याख्याता (१/४/२९) आदि समन्वय नामक प्रथम अध्याय = मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तदनन्यत्वमा रम्भणशब्दादिभ्यः (२/१/१४) सूचित द्वितीय अविरोध अध्याय = तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।
सह कार्यान्तर विधिः वक्षेण तद्वतो विध्यादिवत् (३/४/४७) सूचित तृतीय साधनाध्याय = सत्यं परं धीमहि।
परं जैमिनिर्मुख्यत्वात् (४/३/१२) सूचित चतुर्थ फलाध्याय = धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुह कं सत्यं परं।
गायत्री मन्त्र से समतुल्यता-
तत् सवितुः देवस्य = जन्माद्यस्य यतः।
भर्गो देवस्य = अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
धियो यो नः प्रचोदयात् = सत्यं परं धीमहि (ध्यायेम)
४. वेद सन्दर्भ-
ये बहुत विस्तार से हैं। कुछ का निर्देश। मुह्यन्ति यत् सूरयः - नासदीय सूक्त (१०/१२९/१-७) = सृष्टि के आरम्भ में देव भी नहीं थे, मूल पदार्थ सत् था या असत्-आदि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। सूक्त के ’किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्’ की तरह भागवत में ’निरस्त कुह कं" है।
धाम्ना- धाम का कई प्रकार से विभाजन है। बड़े धाम सृष्टि क्रम अनुसार हैं-परम (अनन्त विश्व), मध्यम (ब्रह्माण्ड, आकाशगंगा), अवम (सौर मण्डल)।
या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा। (ऋग्वेद, १०/८१/४)
इन धामों में भूमि-अन्तरिक्ष-द्यौ विभाग से ९ भाग हुए, बीच के २ भाग समान होने से ७ लोक हैं जिनकी माप केवल भागवत आदि पुराणों में है (विष्णु पुराण, २/७ अध्याय आदि)। ये माप ६ प्रकार से दिये हैं तथा आधुनिक मापों से अधिक शुद्ध हैं।
तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीरुत द्यून्त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम् ।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारु ॥ (ऋग्वेद, २/२७/८)
देवी रूप में वर्णन-यह श्री सूक्त, रुद्राध्यायी तथा अनेक उपनिषदों में है। इनके ३-३ विभाजन को तिस्रः त्रेधा कहा है-
(१) इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। (ऋक्, १/१३/९, ५/११/८)
(२) भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये॥ (ऋक्, १/१८८/८)
(३) शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती। इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः। (ऋक्, १/१४२/९)
(४) भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही। इमं नो यज्ञमागमन् तिस्रो देवीः सुपेशसः। (ऋक्, ९/५/८)
पुर तथा पुरुष रूप में वर्णन पुरुष सूक्त में है।
अव्यक्त ब्रह्म न पुरुष है, न स्त्री-
स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान न जन्तुः।
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः॥
(गजेन्द्र मोक्ष, भागवत पुराण, ८/३/२४)
सृष्टि के लिए ब्रह्म २ रूप धारण करता है-चेतन तत्त्व को पुरुष तथा पदार्थ तत्त्व को प्रकृति या देवी कहा है। अतः २ रूपों को स्पष्ट करने के लिए २ ग्रन्थ लिखे-भागवत तथा देवी भागवत पुराण।
पूर्व काल में २४वें व्यास ऋक्ष या वाल्मीकि ने भी वेद को स्पष्ट करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र लिखा-
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे।
वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना।
तस्माद् रामायणं देवि वेद एव न संशयः॥
(अगस्त्य संहिता का श्लोक नीलकण्ठ कृत मन्त्र रामायण प्रथम श्लोक के स्वोपज्ञ भाष्य में उद्धृत)
बाद में सायण ने अपने वेद भाष्य के आरम्भ में वेद भाष्य भूमिका लिखी।
१७३० में बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूत्र के गोविन्द भाष्य के आरम्भ में वेद व्याख्या के लिए भागवत माहात्म्य लिखा-
उक्तं च गारुडे-
अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां, भारतार्थ विनिर्णयः।
गायत्री भाष्य रूपोऽसौ, वेदार्थ परिवृंहणः॥
सनातन वैदिक परम्परा को नष्ट करने के लिए विलियम जोन्स तथा पार्जिटर नियन्त्रित पुराण प्रकाशन में गरुड पुराण के इस श्लोक को हटाया गया। अंग्रेजों ने पुराण तथा वर्णाश्रम धर्म की निन्दा को प्रश्रय दिया तथा वैसे समाज बनवाये। यह अभी तक चल रहा है।
२. मङ्गलाचरण-
इसके ३ श्लोक वेद के सार रूप हैं तथा भागवत पुराण का उद्देश्य और विषय स्पष्ट करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो ऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, सत्यं परं धीमहि॥१॥
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां,
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, ताप-त्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परैरीश्वरः,
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥२॥
निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।
पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥३॥
प्रथम श्लोक अर्थ के ४ श्लोक देवीभागवत (२/५-८) में हैं। इनमें प्रथम श्लोक-
सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं, शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम्।
संहृत्य कल्प समये रमते तथैका, तां विश्वजननीं मनसा स्मरामि॥
द्वितीय श्लोक के समानार्थ देवीभागवत (३/३४-३८) हैं। प्रथम २ श्लोक हैं-
कृष्णद्वैपायनात् प्रोक्तं पुराणं च मया श्रुतम्।
श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखौघनाशनम्॥३४॥
कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थ परिबृंहितम्।
सर्वागमरसारामं मुमूक्षूणां सदा प्रियम्॥३५॥
तृतीय श्लोक के समानार्थक (देवीभागवत, ३/३९-४३) है। इनमें प्रथम श्लोक-
श्रीमद्भागवतामरांघ्रिप फलास्वादादरः सत्तमाः,
संसारार्णव दुर्विगाह्य सलिलं सन्तर्तुकामः शुकः।
नानाख्यान रसालयं श्रुतिपुटैः प्रेम्णाशृणोदद्भुतं,
तच्छृत्वा न विमुच्यते कलिभयादेवंविधः कः क्षितौ॥३९॥
३. प्रथम मन्त्र की वेदता-
(पुरी गोवर्धन पीठाधीश स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती की पुस्तक शुक-सुधा के आधार पर)
अर्थ-इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिस परमात्मा से है, जो कार्य प्रपञ्च में प्रविष्ट तथा उससे व्यतिरिक्त भी होने से स्वतः सिद्ध, सर्वज्ञ, स्वप्रकाश है; जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया, जिसमें विचारकुशल विद्वान् भी मोहित होते हैं; तेज, जल, मिट्टी का जैसे परस्पर विनिमय (आभास) होता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणात्मक जगत् सत्य जैसा दीखता है, अपने स्वरूप वैभव से माया को दूर हटाने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
ब्रह्म-सूत्र से समतुल्यता-
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (१/१/१) = निरस्त कुह कं सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य यतः (१/१/२)= वही है।
तत्तु समन्वयात् (१/१/४) = (अर्थेषु) अन्वयात्।
ईक्षतेर्नाशब्दम् (१/१/५) = अर्थेष्वभिज्ञः।
एतेन सर्वे व्याख्याता (१/४/२९) आदि समन्वय नामक प्रथम अध्याय = मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तदनन्यत्वमा रम्भणशब्दादिभ्यः (२/१/१४) सूचित द्वितीय अविरोध अध्याय = तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।
सह कार्यान्तर विधिः वक्षेण तद्वतो विध्यादिवत् (३/४/४७) सूचित तृतीय साधनाध्याय = सत्यं परं धीमहि।
परं जैमिनिर्मुख्यत्वात् (४/३/१२) सूचित चतुर्थ फलाध्याय = धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुह कं सत्यं परं।
गायत्री मन्त्र से समतुल्यता-
तत् सवितुः देवस्य = जन्माद्यस्य यतः।
भर्गो देवस्य = अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
धियो यो नः प्रचोदयात् = सत्यं परं धीमहि (ध्यायेम)
४. वेद सन्दर्भ-
ये बहुत विस्तार से हैं। कुछ का निर्देश। मुह्यन्ति यत् सूरयः - नासदीय सूक्त (१०/१२९/१-७) = सृष्टि के आरम्भ में देव भी नहीं थे, मूल पदार्थ सत् था या असत्-आदि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। सूक्त के ’किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्’ की तरह भागवत में ’निरस्त कुह कं" है।
धाम्ना- धाम का कई प्रकार से विभाजन है। बड़े धाम सृष्टि क्रम अनुसार हैं-परम (अनन्त विश्व), मध्यम (ब्रह्माण्ड, आकाशगंगा), अवम (सौर मण्डल)।
या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा। (ऋग्वेद, १०/८१/४)
इन धामों में भूमि-अन्तरिक्ष-द्यौ विभाग से ९ भाग हुए, बीच के २ भाग समान होने से ७ लोक हैं जिनकी माप केवल भागवत आदि पुराणों में है (विष्णु पुराण, २/७ अध्याय आदि)। ये माप ६ प्रकार से दिये हैं तथा आधुनिक मापों से अधिक शुद्ध हैं।
तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीरुत द्यून्त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम् ।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारु ॥ (ऋग्वेद, २/२७/८)
देवी रूप में वर्णन-यह श्री सूक्त, रुद्राध्यायी तथा अनेक उपनिषदों में है। इनके ३-३ विभाजन को तिस्रः त्रेधा कहा है-
(१) इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। (ऋक्, १/१३/९, ५/११/८)
(२) भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये॥ (ऋक्, १/१८८/८)
(३) शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती। इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः। (ऋक्, १/१४२/९)
(४) भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही। इमं नो यज्ञमागमन् तिस्रो देवीः सुपेशसः। (ऋक्, ९/५/८)
पुर तथा पुरुष रूप में वर्णन पुरुष सूक्त में है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.