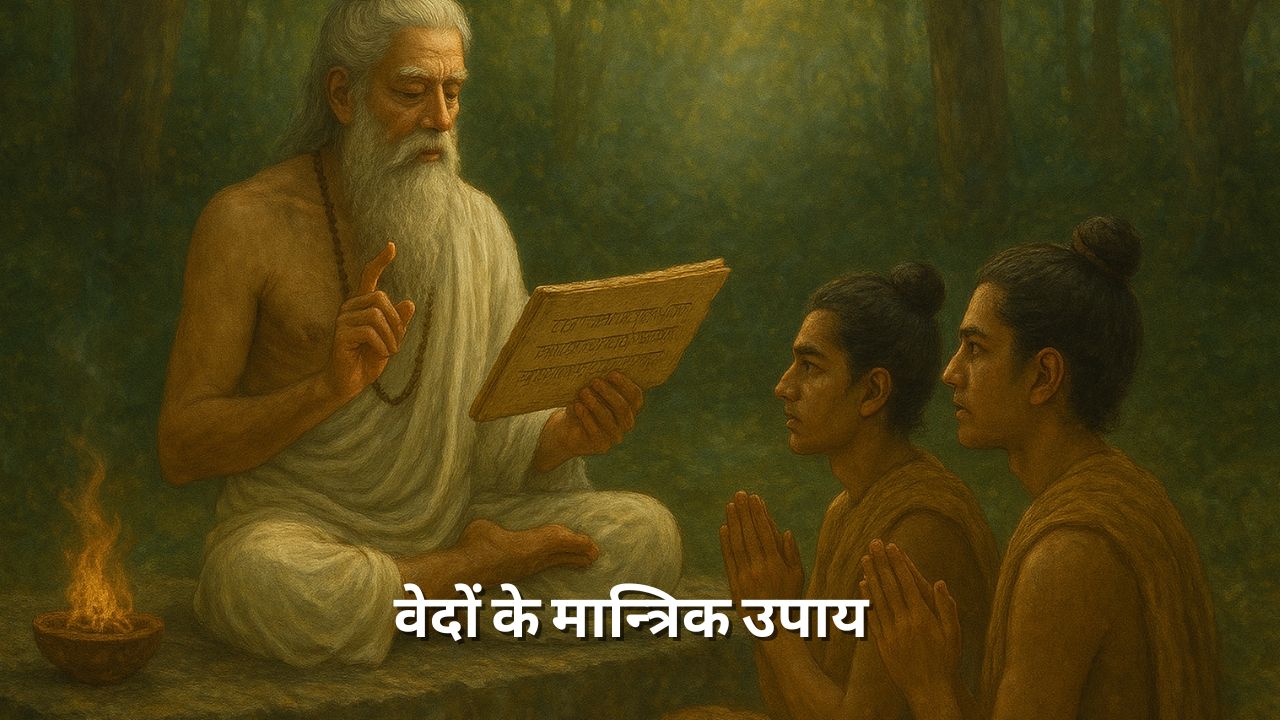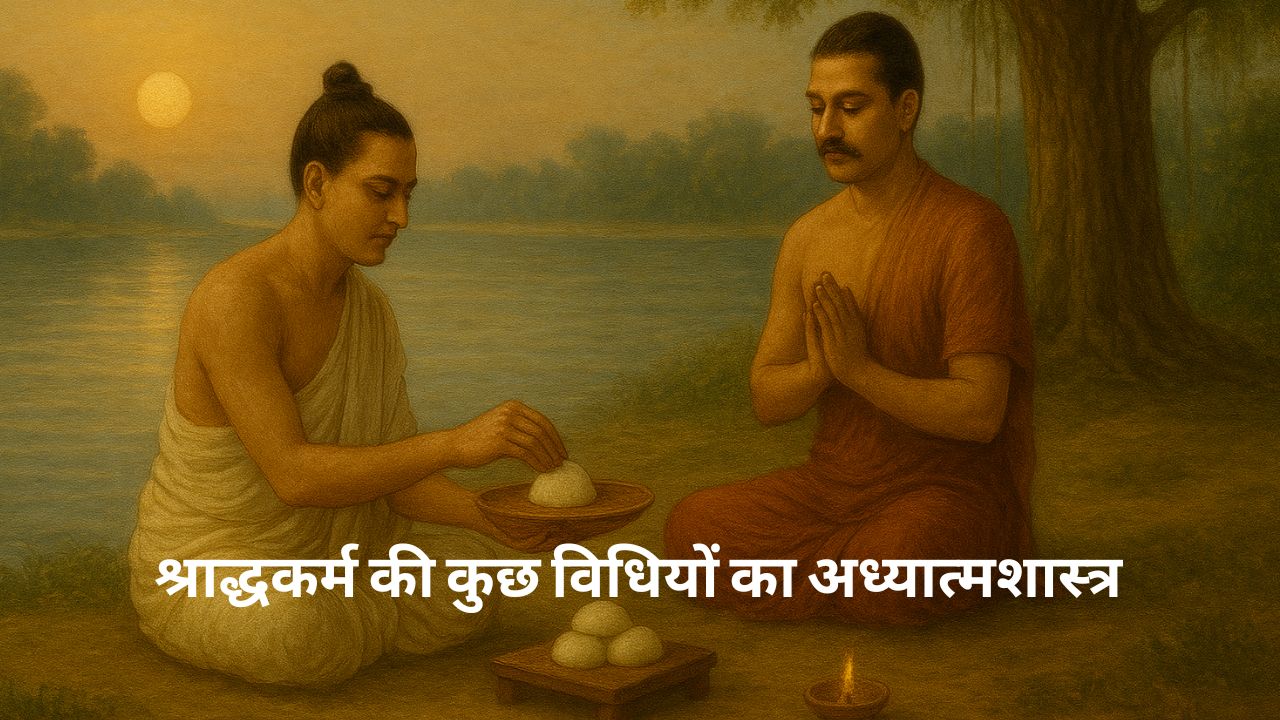- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
श्री पेमा तेनजिन-
Mystic Power- तिब्बत में पूर्वानूदित बौद्ध सूत्र तन्त्रों की अध्ययन एवं साधना परम्परा को जिया अथवा प्राचीन परम्परा कहा जाता है। यह परम्परा तिब्बत में बौद्धधर्म के संस्थापक रहे आचार्य शान्तरक्षित, आचार्य पद्मसम्भव, विमलमित्र, कमलशील आदि की देन है। यदि यहाँ मध्य में बौद्धशासन का हास नहीं हुआ होता और तिब्बत सत्तर से अस्सी वर्षों तक अंधकारयुग के संकट से न गुजरा होता, तो शायद ही जिमा का नामकरण हुआ होता और उक्त आचार्यों की परम्परा अविच्छिन्न रूप से पूर्णतया फल-फूल रही होती। वहाँ पुनः बौद्धशासन की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं हुई होती।
 प्रस्तुत लेख में तिब्बत की प्राचीन सिमा परम्परा के मूलभूत सिद्धान्तों एवं दृष्टि एवं चर्या भावना का परिचय देने के क्रम में इसके अन्तर्गत आए नौ यानों में से तीन बाह्ययान एवं तीन बाह्यतन्त्रों पर विमर्श किया गया है। इस क्रम में प्रारम्भ में तिब्बत में पूर्वापर बौद्धशासन का विकास, जिमा परम्परा की प्रामाणिकता, परवर्ती बौद्धशासन काल में विकसित नवीन परम्पराओं एवं चित्त की प्रधानता आदि विषयों की भी चर्चा की गई है।
तिब्बत में बौद्धशासन
तिब्बत में बौद्धधर्म की नींव सातवीं शताब्दी में राजा सोडचन गम्पो (617-698 ई०) के शासनकाल में ही पड़ चुकी थी, किन्तु वस्तुतः बौद्धधर्म की स्थापना वहाँ राजा द्विसोइ देउचन (742-797 ई०) के शासनकाल में उनके निमन्त्रण पर उपाध्याय शान्तरक्षित एवं आचार्य पद्मसम्भव के सहयोग से सुप्रसिद्ध समये महाविहार के निर्माण के साथ हुई। वहाँ महान लोचावा वैरोचन, अक ज्ञानकुमार के व पलचेंग, चोगरी लुइ लखन येथे-दे आदि एक सौ आठ वरिष्ठ एवं एक हजार कनिष्ठ लोचावा एकत्रित हुए और सम्पूर्ण महायान बौद्ध वाङ्मय के विनय, अभिधर्म सहित विभिन्न सूत्र एवं तन्त्रव बुद्धवचनों का संस्कृत भाषा में तिब्बतों में अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया गया। इतना ही नहीं, इन शास्त्रों की श्रवण, चिन्तन एवं भावना आदि के क्रम से प्रतिपादित भी किया गया। आचार्य पद्मसम्भव द्वारा सर्वप्रथम असाधनमण्डल' को उद्घाटित किये जाने पर उनके प्रधान पच्चीस शिष्य (जेनेरडा) आदि सिद्धि प्राप्त अपरिमित योगियों का प्रादुर्भाव हुआ आचार्य ने बाह्य एवं आभ्यन्तर सभी प्रकार के तन्त्रों का तथा विशेष रूप से अतियोग्य का प्रचार किया। इसी प्रकार महापण्डित विमलमित्र महान अनुवादक वैरोचन, पण्डित विद्याम आदि ने भी अतियोग के सूत्र अनुत्तर तन्त्रों से सम्बन्धित तन्त्र ग्रन्थों का न केवल अनुवाद एवं सम्पादन किया, अपितु पूर्णरूपेण अभिषेक, आगम, अववाद आदि द्वारा सूत्र एवं तन्त्र शासन को वहाँ फैलाया।
पूर्वापर बौद्धशासन का विकास तिब्बत में बौद्धशासन का विकास दो चरणों में हुआ अर्थात् आठवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी पर्यन्त तथा ग्यारहवीं के पश्चात्, जिसके कारण वहाँ पूर्ववर्ती काल में विकसित परम्परा को ञिङ्मा (प्राचीन) और परवर्ती काल में विकसित परम्पराओं को नवीन परम्परा के रूप में विभाजित किया गया। भोटदेशीय बौद्ध परम्परा में जिङ्मा एवं सरमा का भेद सूत्र के आधार पर नहीं किया गया है, क्योंकि सूत्र प्रणाली के सन्दर्भ में इनमें कोई भेद नहीं है। अतः इनका विभाजन गुहातन्त्रों की साधना परम्परा के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार आठवीं शताब्दी में बौद्धधर्म की स्थापना से लेकर पण्डित स्मृतिज्ञानकीर्ति के पूर्व तक अनूदित तन्त्रों की व्याख्यान एवं अनुष्ठान की परम्परा को प्राचीन अथवा ञिङ्मा कहा गया है। अनुवादक वैरोचन, विमलमित्र, अक्- ज्ञानकुमार आदि ने अतियोग के अन्तर्गत अनेक तन्त्र ग्रन्थों का अनुवाद किया। इन तन्त्रों का आगम, अभिषेक, उपदेश द्वारा अनुष्ठान करने वाली परम्परा को ञिङ्मा कहा जाता है।
महान् अनुवादक रिन्छेन जो एवं ग्यारहवीं शताब्दी में बौद्धधर्म को पुनः स्थापना से लेकर पञ्चाद्वर्ती तन्त्रों के अनुवादों तथा उनके श्रवण, चिन्तन एवं मनन करने वाली परम्परा को नवीन परम्परा अर्थात् सरमा कहा गया। परवर्ती शासनकाल में महान् अनुवादक रिन्छेन जो आदि अनुवादकों ने पितृतन्त्र, मातृतन्त्र एवं अद्वयतन्त्र के गुह्यसमाजतन्त्र, चक्रसंवरतन्त्र, कालचक्रतन्त्र आदि तन्त्रों का अनुवाद किया और आगम, अभिषेक एवं उपदेश द्वारा उनका अनुष्ठान किया, जिसे सरमा (नवीन) परम्परा कहा जाता है।
पूर्वानृदित प्राचीन (जिमा) परम्परा की प्रामाणिकता
चौदहवीं शताब्दी में तिब्बत के महान् विद्वान् चौखापा ने अपने जीवन वृत्तान्त में उल्लेख किया है कि बिड्मा के मूल सिद्धान्त उचित, प्रामाणिक तथा तत्त्वपरक है। उन्होंने सिमा सिद्धान्तों के अध्ययनार्थ ल्हो डक के त्रि ड मा के परमविद्वान् नमखा ग्यलछ्न को अपना गुरु बनाया और दर्शन से सम्बन्धित अनेक शंकाओं के समाधान के लिए भारत न जाकर उनसे इनका समाधान प्राप्त किया।
वास्तव में नवीन अनूदित शासन के विकास के पूर्व तिब्बत में अनेक विद्वान् तथा विशेषज्ञ विद्यमान थे। जैसे- गुरु पद्मसम्भव एवं उनके पच्चीस शिष्य आदि, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही जिङ्मा शिक्षाओं में विशेषज्ञता अर्जित कर ली थी और सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली थी। तब नवीन अनूदित परवर्ती शासन का आविर्भाव भी नहीं हुआ था। आज भी अनेक ऐसे साधक हैं, जो ञिङ्मा मार्ग-साधना द्वारा ही अध्यात्म के उच्च शिखरों को प्राप्त हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि ञिइमा परम्परा की महासन्धि (जोग-छेन) चर्या उच्चतम अनुत्तरयोगतन्त्र चर्या से सम्बन्धित एक विशुद्ध प्रणाली है।
मन्त्र-सम्बद्ध अनुवाद की इस प्राचीन पद्धति की वास्तविकता बिलकुल भिन्न है। शुरू में तिब्बत के धार्मिक नरेश ने स्वर्ण मुद्राओं के साथ वैरोचन, मयंक आदि पाँच विश्वसनीय भिक्षुओं को भारत भेजा। वहाँ उन्होंने महामुद्रा जैसे अद्भुत गुह्यमन्त्र सिद्धान्तों को ऐसे विज्ञजनों से प्राप्त किया, जो महासिद्ध एवं गुह्य साधक थे। तत्पश्चात् उन्होंने उनका अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त पद्मसम्भव, विमलमित्र, बुद्धगुह्य तथा अन्य विद्वानों को तिब्बत में आमन्त्रित किया गया, उन्होंने वहाँ महायान की उत्कृष्ट शिक्षाओं को प्रतिपादित किया।
ञिङ्मा परम्परा का जन्म तिब्बत में बौद्धधर्म की स्थापना एवं सर्वप्रथम समये महाविहार के निर्माण के साथ ही माना जाता है। ञिङ्मा परम्परा में विनय, सूत्र, तन्त्र एवं गुप्तनिधिकोश आदि के श्रवण चिन्तन एवं भावना की मिश्रित व्यवस्था है। ञिङ्मा आचार्यों की आगम परम्परा आदिबुद्ध समन्तभद्र से प्रारम्भ होती है, जिसमें आचार्यों के माध्यम से चली आ रही सिद्धान्त, शास्त्र, तन्त्र, साधना, कर्मकाण्ड एवं अधिगम आदि की अविच्छिन्न परम्परा निहित है। फलस्वरूप, छिम्फू में पच्चीस सिद्ध हुए, डग यङजोड़ में पचपन योगी साधक हुए, शेलडग में तीस गृहस्थ साधक हुए, येरपा एवं छुवोरि में एक सौ आठ साधक हुए तथा पच्चीस महिला साधिकाएं हुई, जिन्होंने मरणोपरान्त ऋद्धिकार्य प्राप्त किया अर्थात् उनका शरीर इन्द्रधनुष की भाँति प्रकाश में विलीन हो गया। उन्होंने तीन प्रकार के मार्गाभ्यास को आगे बढ़ाया, जो इस प्रकार है- बाह्य विनय मार्ग, आभ्यन्तर बोधिसत्त्व मार्ग तथा गुह्य वज्रयान मार्ग। गुह्यमार्ग एवं साधना तीन बाह्य तन्त्रों तथा तीन आभ्यन्तर तन्त्रों पर आधारित है, जिसमें से ञिइमा परम्परा तीन आभ्यन्तर तन्त्रों पर विशेष जोर देता है। इसे ही महायोगतन्त्र, अनुयोगतन्त्र एवं अतियोगतन्त्र कहा जाता है।
पहले ये परम्पराएं भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही होग ऐसा संस्कृत में उपलब्ध अनेक तन्त्र ग्रन्थों से भी स्पष्ट हो जाता है। कृष्णयमारितन्त्र महायोग, अनुयोग एवं अतियोग का बहुत स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। समये महाविहार प्राचीन अनुवाद पद्धति के अनेक भारतीय ग्रन्थों की प्रतियाँ अब भी शेष बचे हैं। ज तिब्बती अनुवादकर्ता भारत गये, उनका कहना था कि गुह्यगर्भ एवं पञ्चागमनिर्देश आदि मगध में उपलब्ध थे 2 आचार्य अतीश जब समये महाविहार में पहुँचे, तब उन्हें 'पे-कर द्वीप' (श्वेतकमल-द्वीप) में ठहराया गया। वहाँ उन्होंने दो अनुवादकों के साथ पञ्चविंशतिसाहस्रिकालोक एवं आचार्य वसुबन्धु कृत महायानसम्परिग्रह-टीका आदि अनेक ग्रन्थों का तिब्बती में अनुवाद किया। वहाँ संस्कृत भाषा में विद्यमान विशाल भारतीय ग्रन्थराशि को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने अनेक ऐसे ग्रन्थों को भी देखा, जो भारत से लुप्त हो चुके थे। उनके मुँह से अनायास निकल पड़ा कि पूर्व में तिब्बत में बौद्धशासन का जितना विकास हुआ उतना शायद भारत में भी मुश्किल है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत में भी अप्राप्त इन ग्रन्थों को आचार्य पद्मसम्भव ने अवश्य ही अमनुष्य-लोक से प्राप्त किया होगा। 3
परवर्ती बौद्ध शासनकाल में विकसित नवीन परम्पराएं
तिब्बत में बौद्ध शासन के विकास के उत्तरकाल में जिन तन्त्रों का प्रचार-प्रसार हुआ, वे सभी शाक्यमुनि गौतमबुद्ध द्वारा सम्भोगकाय के रूप में उपदिष्ट हैं। नवीन तन्त्रों के आधार पर उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है-तीन यान अर्थात् श्रावकयान, प्रत्येकबुद्धयान, बोधिसत्त्वयान। चार मन्त्रयान अर्थात् क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र तथा अनुत्तरतन्त्र। अनुत्तरतन्त्र के भी तीन भेद किये गये हैं--पितृतन्त्र, मातृतन्त्र एवं अद्वयतन्त्र ।
इस प्रकार तिब्बत में प्रमुख रूप से बिमा, कग्युद, साक्य एवं गेलुग परम्पराएं विकसित हुई। इनमें से बिइमा परम्परा को तान्त्रिक प्रस्थान माना गया है, किन्तु पश्चाद्वर्ती अनूदित शासनकाल में अन्य तीन परम्पराओं में भी नवीन तन्त्रों का विकास हुआ। कग्युद परम्परा की स्थापना महानुवादक मारपा लोचावा ( 1012-1099 ई०) ने की, साक्य परम्परा की स्थापना खोन कोनछोग ग्यलपो (1034-1102 ई०) ने तथा गेलुग परम्परा की स्थापना जे चोडखा पा (1357-1419 ई०) ने की।
आर्यावर्त (भारत) से लाये गये ग्रन्थों के अनुवाद के काल की विविधता एवं विकास के क्रम में तिब्बत में विभिन्न परम्पराओं का विकास हुआ, किन्तु सूत्रपक्ष को लेकर प्राचीन व नवीन परम्परा में कोई मतभेद नहीं है। सभी माध्यमिक दर्शन को मानते हैं, चर्या की दृष्टि से सभी बोधिसत्त्वयान का अनुसरण करते हैं। इसके अतिरिक्त भी चारों परम्पराओं में सूत्र एवं तन्त्र के अभ्यास की व्यवस्था विद्यमान है। प्रत्येक परम्परा में बुद्ध की शिक्षाओं के विशिष्ट लक्षणों सहित एक ही जीवन में बुद्धत्व प्राप्ति के आवश्यक उपाय तथा शिक्षाएं निहित हैं।
बौद्धधर्म के तिब्बत में विकास के समय भारत के विभिन्न विख्यात बौद्ध शिक्षा केन्द्रों से सांस्कृतिक निर्देशों सहित जो असाधारण धरोहर पहुँची उसमें तिब्बतियों की पूर्ण सहभागिता रही। वहाँ नागार्जुन के दर्शन तथा माध्यमिक प्रस्थान का एकछत्र राज रहा। चारों तिब्बती बौद्ध परम्पराएं इसे परमोत्कृष्ट दार्शनिक दृष्टि मानती है। बुद्धवचनों में तन्त्र को सर्वश्रेष्ठ मानने तथा उनकी साधना करने वाले बहुत से प्रकाण्ड भारतीय आचार्यों ने तिब्बत की यात्राएं कीं और उसका वहाँ प्रचार-प्रसार किया। इसलिए यदि तिब्बती बौद्धधर्मानुयायी भी तन्त्रवचनों को श्रेष्ठ मानकर उनकी साधना करता है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दूसरे बौद्ध धर्मावलम्बी देशों में ऐसी बात नहीं है। तिब्बत की अपेक्षा अन्य थेरवादी बौद्ध देशों में तान्त्रिक साधना एवं पद्धति प्रचलित नहीं हुई। लेकिन चीन एवं जापान जैसे बौद्ध देशों में तन्त्र की साधना को कुछ हद तक स्वीकार किया गया तथा कर्मकाण्ड एवं अनुष्ठानों के अवसर पर उसके प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। फिर भी, वहां तिब्बत की भाँति अनुत्तर योगतन्त्र की साधना प्रचलित नहीं हुई।
प्रस्तुत लेख में तिब्बत की प्राचीन सिमा परम्परा के मूलभूत सिद्धान्तों एवं दृष्टि एवं चर्या भावना का परिचय देने के क्रम में इसके अन्तर्गत आए नौ यानों में से तीन बाह्ययान एवं तीन बाह्यतन्त्रों पर विमर्श किया गया है। इस क्रम में प्रारम्भ में तिब्बत में पूर्वापर बौद्धशासन का विकास, जिमा परम्परा की प्रामाणिकता, परवर्ती बौद्धशासन काल में विकसित नवीन परम्पराओं एवं चित्त की प्रधानता आदि विषयों की भी चर्चा की गई है।
तिब्बत में बौद्धशासन
तिब्बत में बौद्धधर्म की नींव सातवीं शताब्दी में राजा सोडचन गम्पो (617-698 ई०) के शासनकाल में ही पड़ चुकी थी, किन्तु वस्तुतः बौद्धधर्म की स्थापना वहाँ राजा द्विसोइ देउचन (742-797 ई०) के शासनकाल में उनके निमन्त्रण पर उपाध्याय शान्तरक्षित एवं आचार्य पद्मसम्भव के सहयोग से सुप्रसिद्ध समये महाविहार के निर्माण के साथ हुई। वहाँ महान लोचावा वैरोचन, अक ज्ञानकुमार के व पलचेंग, चोगरी लुइ लखन येथे-दे आदि एक सौ आठ वरिष्ठ एवं एक हजार कनिष्ठ लोचावा एकत्रित हुए और सम्पूर्ण महायान बौद्ध वाङ्मय के विनय, अभिधर्म सहित विभिन्न सूत्र एवं तन्त्रव बुद्धवचनों का संस्कृत भाषा में तिब्बतों में अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया गया। इतना ही नहीं, इन शास्त्रों की श्रवण, चिन्तन एवं भावना आदि के क्रम से प्रतिपादित भी किया गया। आचार्य पद्मसम्भव द्वारा सर्वप्रथम असाधनमण्डल' को उद्घाटित किये जाने पर उनके प्रधान पच्चीस शिष्य (जेनेरडा) आदि सिद्धि प्राप्त अपरिमित योगियों का प्रादुर्भाव हुआ आचार्य ने बाह्य एवं आभ्यन्तर सभी प्रकार के तन्त्रों का तथा विशेष रूप से अतियोग्य का प्रचार किया। इसी प्रकार महापण्डित विमलमित्र महान अनुवादक वैरोचन, पण्डित विद्याम आदि ने भी अतियोग के सूत्र अनुत्तर तन्त्रों से सम्बन्धित तन्त्र ग्रन्थों का न केवल अनुवाद एवं सम्पादन किया, अपितु पूर्णरूपेण अभिषेक, आगम, अववाद आदि द्वारा सूत्र एवं तन्त्र शासन को वहाँ फैलाया।
पूर्वापर बौद्धशासन का विकास तिब्बत में बौद्धशासन का विकास दो चरणों में हुआ अर्थात् आठवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी पर्यन्त तथा ग्यारहवीं के पश्चात्, जिसके कारण वहाँ पूर्ववर्ती काल में विकसित परम्परा को ञिङ्मा (प्राचीन) और परवर्ती काल में विकसित परम्पराओं को नवीन परम्परा के रूप में विभाजित किया गया। भोटदेशीय बौद्ध परम्परा में जिङ्मा एवं सरमा का भेद सूत्र के आधार पर नहीं किया गया है, क्योंकि सूत्र प्रणाली के सन्दर्भ में इनमें कोई भेद नहीं है। अतः इनका विभाजन गुहातन्त्रों की साधना परम्परा के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार आठवीं शताब्दी में बौद्धधर्म की स्थापना से लेकर पण्डित स्मृतिज्ञानकीर्ति के पूर्व तक अनूदित तन्त्रों की व्याख्यान एवं अनुष्ठान की परम्परा को प्राचीन अथवा ञिङ्मा कहा गया है। अनुवादक वैरोचन, विमलमित्र, अक्- ज्ञानकुमार आदि ने अतियोग के अन्तर्गत अनेक तन्त्र ग्रन्थों का अनुवाद किया। इन तन्त्रों का आगम, अभिषेक, उपदेश द्वारा अनुष्ठान करने वाली परम्परा को ञिङ्मा कहा जाता है।
महान् अनुवादक रिन्छेन जो एवं ग्यारहवीं शताब्दी में बौद्धधर्म को पुनः स्थापना से लेकर पञ्चाद्वर्ती तन्त्रों के अनुवादों तथा उनके श्रवण, चिन्तन एवं मनन करने वाली परम्परा को नवीन परम्परा अर्थात् सरमा कहा गया। परवर्ती शासनकाल में महान् अनुवादक रिन्छेन जो आदि अनुवादकों ने पितृतन्त्र, मातृतन्त्र एवं अद्वयतन्त्र के गुह्यसमाजतन्त्र, चक्रसंवरतन्त्र, कालचक्रतन्त्र आदि तन्त्रों का अनुवाद किया और आगम, अभिषेक एवं उपदेश द्वारा उनका अनुष्ठान किया, जिसे सरमा (नवीन) परम्परा कहा जाता है।
पूर्वानृदित प्राचीन (जिमा) परम्परा की प्रामाणिकता
चौदहवीं शताब्दी में तिब्बत के महान् विद्वान् चौखापा ने अपने जीवन वृत्तान्त में उल्लेख किया है कि बिड्मा के मूल सिद्धान्त उचित, प्रामाणिक तथा तत्त्वपरक है। उन्होंने सिमा सिद्धान्तों के अध्ययनार्थ ल्हो डक के त्रि ड मा के परमविद्वान् नमखा ग्यलछ्न को अपना गुरु बनाया और दर्शन से सम्बन्धित अनेक शंकाओं के समाधान के लिए भारत न जाकर उनसे इनका समाधान प्राप्त किया।
वास्तव में नवीन अनूदित शासन के विकास के पूर्व तिब्बत में अनेक विद्वान् तथा विशेषज्ञ विद्यमान थे। जैसे- गुरु पद्मसम्भव एवं उनके पच्चीस शिष्य आदि, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही जिङ्मा शिक्षाओं में विशेषज्ञता अर्जित कर ली थी और सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली थी। तब नवीन अनूदित परवर्ती शासन का आविर्भाव भी नहीं हुआ था। आज भी अनेक ऐसे साधक हैं, जो ञिङ्मा मार्ग-साधना द्वारा ही अध्यात्म के उच्च शिखरों को प्राप्त हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि ञिइमा परम्परा की महासन्धि (जोग-छेन) चर्या उच्चतम अनुत्तरयोगतन्त्र चर्या से सम्बन्धित एक विशुद्ध प्रणाली है।
मन्त्र-सम्बद्ध अनुवाद की इस प्राचीन पद्धति की वास्तविकता बिलकुल भिन्न है। शुरू में तिब्बत के धार्मिक नरेश ने स्वर्ण मुद्राओं के साथ वैरोचन, मयंक आदि पाँच विश्वसनीय भिक्षुओं को भारत भेजा। वहाँ उन्होंने महामुद्रा जैसे अद्भुत गुह्यमन्त्र सिद्धान्तों को ऐसे विज्ञजनों से प्राप्त किया, जो महासिद्ध एवं गुह्य साधक थे। तत्पश्चात् उन्होंने उनका अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त पद्मसम्भव, विमलमित्र, बुद्धगुह्य तथा अन्य विद्वानों को तिब्बत में आमन्त्रित किया गया, उन्होंने वहाँ महायान की उत्कृष्ट शिक्षाओं को प्रतिपादित किया।
ञिङ्मा परम्परा का जन्म तिब्बत में बौद्धधर्म की स्थापना एवं सर्वप्रथम समये महाविहार के निर्माण के साथ ही माना जाता है। ञिङ्मा परम्परा में विनय, सूत्र, तन्त्र एवं गुप्तनिधिकोश आदि के श्रवण चिन्तन एवं भावना की मिश्रित व्यवस्था है। ञिङ्मा आचार्यों की आगम परम्परा आदिबुद्ध समन्तभद्र से प्रारम्भ होती है, जिसमें आचार्यों के माध्यम से चली आ रही सिद्धान्त, शास्त्र, तन्त्र, साधना, कर्मकाण्ड एवं अधिगम आदि की अविच्छिन्न परम्परा निहित है। फलस्वरूप, छिम्फू में पच्चीस सिद्ध हुए, डग यङजोड़ में पचपन योगी साधक हुए, शेलडग में तीस गृहस्थ साधक हुए, येरपा एवं छुवोरि में एक सौ आठ साधक हुए तथा पच्चीस महिला साधिकाएं हुई, जिन्होंने मरणोपरान्त ऋद्धिकार्य प्राप्त किया अर्थात् उनका शरीर इन्द्रधनुष की भाँति प्रकाश में विलीन हो गया। उन्होंने तीन प्रकार के मार्गाभ्यास को आगे बढ़ाया, जो इस प्रकार है- बाह्य विनय मार्ग, आभ्यन्तर बोधिसत्त्व मार्ग तथा गुह्य वज्रयान मार्ग। गुह्यमार्ग एवं साधना तीन बाह्य तन्त्रों तथा तीन आभ्यन्तर तन्त्रों पर आधारित है, जिसमें से ञिइमा परम्परा तीन आभ्यन्तर तन्त्रों पर विशेष जोर देता है। इसे ही महायोगतन्त्र, अनुयोगतन्त्र एवं अतियोगतन्त्र कहा जाता है।
पहले ये परम्पराएं भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही होग ऐसा संस्कृत में उपलब्ध अनेक तन्त्र ग्रन्थों से भी स्पष्ट हो जाता है। कृष्णयमारितन्त्र महायोग, अनुयोग एवं अतियोग का बहुत स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। समये महाविहार प्राचीन अनुवाद पद्धति के अनेक भारतीय ग्रन्थों की प्रतियाँ अब भी शेष बचे हैं। ज तिब्बती अनुवादकर्ता भारत गये, उनका कहना था कि गुह्यगर्भ एवं पञ्चागमनिर्देश आदि मगध में उपलब्ध थे 2 आचार्य अतीश जब समये महाविहार में पहुँचे, तब उन्हें 'पे-कर द्वीप' (श्वेतकमल-द्वीप) में ठहराया गया। वहाँ उन्होंने दो अनुवादकों के साथ पञ्चविंशतिसाहस्रिकालोक एवं आचार्य वसुबन्धु कृत महायानसम्परिग्रह-टीका आदि अनेक ग्रन्थों का तिब्बती में अनुवाद किया। वहाँ संस्कृत भाषा में विद्यमान विशाल भारतीय ग्रन्थराशि को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने अनेक ऐसे ग्रन्थों को भी देखा, जो भारत से लुप्त हो चुके थे। उनके मुँह से अनायास निकल पड़ा कि पूर्व में तिब्बत में बौद्धशासन का जितना विकास हुआ उतना शायद भारत में भी मुश्किल है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत में भी अप्राप्त इन ग्रन्थों को आचार्य पद्मसम्भव ने अवश्य ही अमनुष्य-लोक से प्राप्त किया होगा। 3
परवर्ती बौद्ध शासनकाल में विकसित नवीन परम्पराएं
तिब्बत में बौद्ध शासन के विकास के उत्तरकाल में जिन तन्त्रों का प्रचार-प्रसार हुआ, वे सभी शाक्यमुनि गौतमबुद्ध द्वारा सम्भोगकाय के रूप में उपदिष्ट हैं। नवीन तन्त्रों के आधार पर उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है-तीन यान अर्थात् श्रावकयान, प्रत्येकबुद्धयान, बोधिसत्त्वयान। चार मन्त्रयान अर्थात् क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र तथा अनुत्तरतन्त्र। अनुत्तरतन्त्र के भी तीन भेद किये गये हैं--पितृतन्त्र, मातृतन्त्र एवं अद्वयतन्त्र ।
इस प्रकार तिब्बत में प्रमुख रूप से बिमा, कग्युद, साक्य एवं गेलुग परम्पराएं विकसित हुई। इनमें से बिइमा परम्परा को तान्त्रिक प्रस्थान माना गया है, किन्तु पश्चाद्वर्ती अनूदित शासनकाल में अन्य तीन परम्पराओं में भी नवीन तन्त्रों का विकास हुआ। कग्युद परम्परा की स्थापना महानुवादक मारपा लोचावा ( 1012-1099 ई०) ने की, साक्य परम्परा की स्थापना खोन कोनछोग ग्यलपो (1034-1102 ई०) ने तथा गेलुग परम्परा की स्थापना जे चोडखा पा (1357-1419 ई०) ने की।
आर्यावर्त (भारत) से लाये गये ग्रन्थों के अनुवाद के काल की विविधता एवं विकास के क्रम में तिब्बत में विभिन्न परम्पराओं का विकास हुआ, किन्तु सूत्रपक्ष को लेकर प्राचीन व नवीन परम्परा में कोई मतभेद नहीं है। सभी माध्यमिक दर्शन को मानते हैं, चर्या की दृष्टि से सभी बोधिसत्त्वयान का अनुसरण करते हैं। इसके अतिरिक्त भी चारों परम्पराओं में सूत्र एवं तन्त्र के अभ्यास की व्यवस्था विद्यमान है। प्रत्येक परम्परा में बुद्ध की शिक्षाओं के विशिष्ट लक्षणों सहित एक ही जीवन में बुद्धत्व प्राप्ति के आवश्यक उपाय तथा शिक्षाएं निहित हैं।
बौद्धधर्म के तिब्बत में विकास के समय भारत के विभिन्न विख्यात बौद्ध शिक्षा केन्द्रों से सांस्कृतिक निर्देशों सहित जो असाधारण धरोहर पहुँची उसमें तिब्बतियों की पूर्ण सहभागिता रही। वहाँ नागार्जुन के दर्शन तथा माध्यमिक प्रस्थान का एकछत्र राज रहा। चारों तिब्बती बौद्ध परम्पराएं इसे परमोत्कृष्ट दार्शनिक दृष्टि मानती है। बुद्धवचनों में तन्त्र को सर्वश्रेष्ठ मानने तथा उनकी साधना करने वाले बहुत से प्रकाण्ड भारतीय आचार्यों ने तिब्बत की यात्राएं कीं और उसका वहाँ प्रचार-प्रसार किया। इसलिए यदि तिब्बती बौद्धधर्मानुयायी भी तन्त्रवचनों को श्रेष्ठ मानकर उनकी साधना करता है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दूसरे बौद्ध धर्मावलम्बी देशों में ऐसी बात नहीं है। तिब्बत की अपेक्षा अन्य थेरवादी बौद्ध देशों में तान्त्रिक साधना एवं पद्धति प्रचलित नहीं हुई। लेकिन चीन एवं जापान जैसे बौद्ध देशों में तन्त्र की साधना को कुछ हद तक स्वीकार किया गया तथा कर्मकाण्ड एवं अनुष्ठानों के अवसर पर उसके प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। फिर भी, वहां तिब्बत की भाँति अनुत्तर योगतन्त्र की साधना प्रचलित नहीं हुई।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.