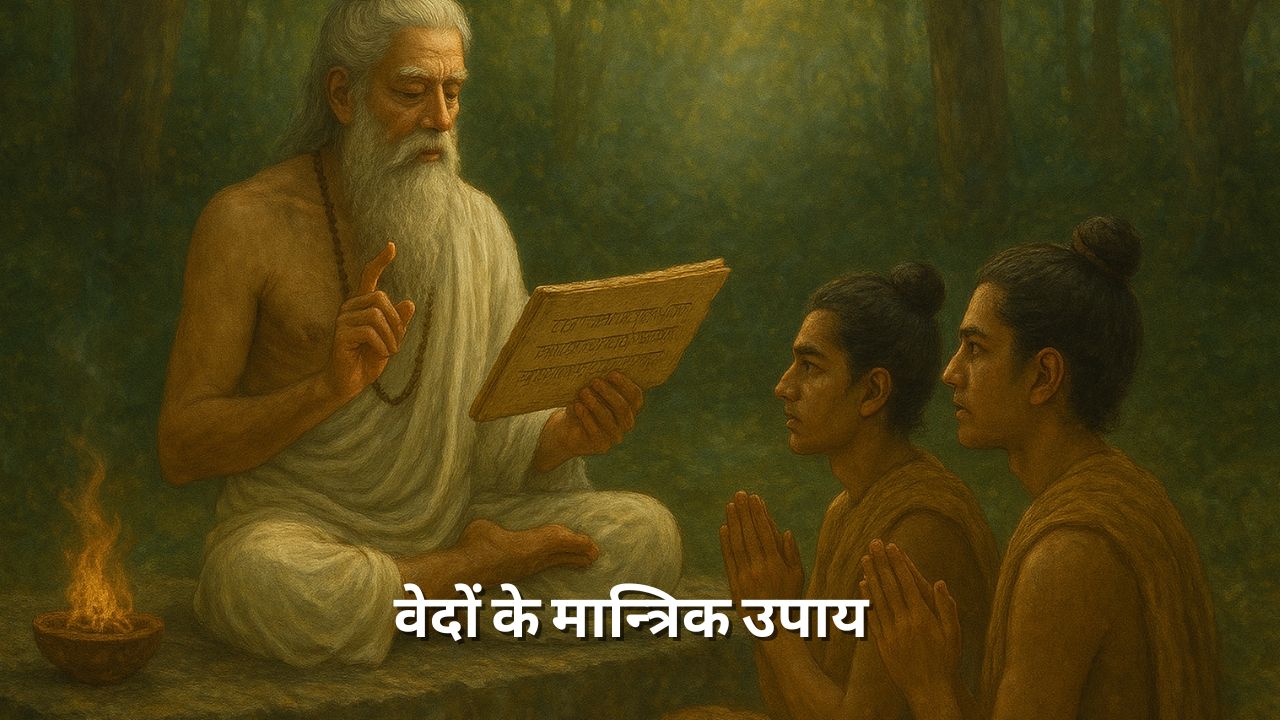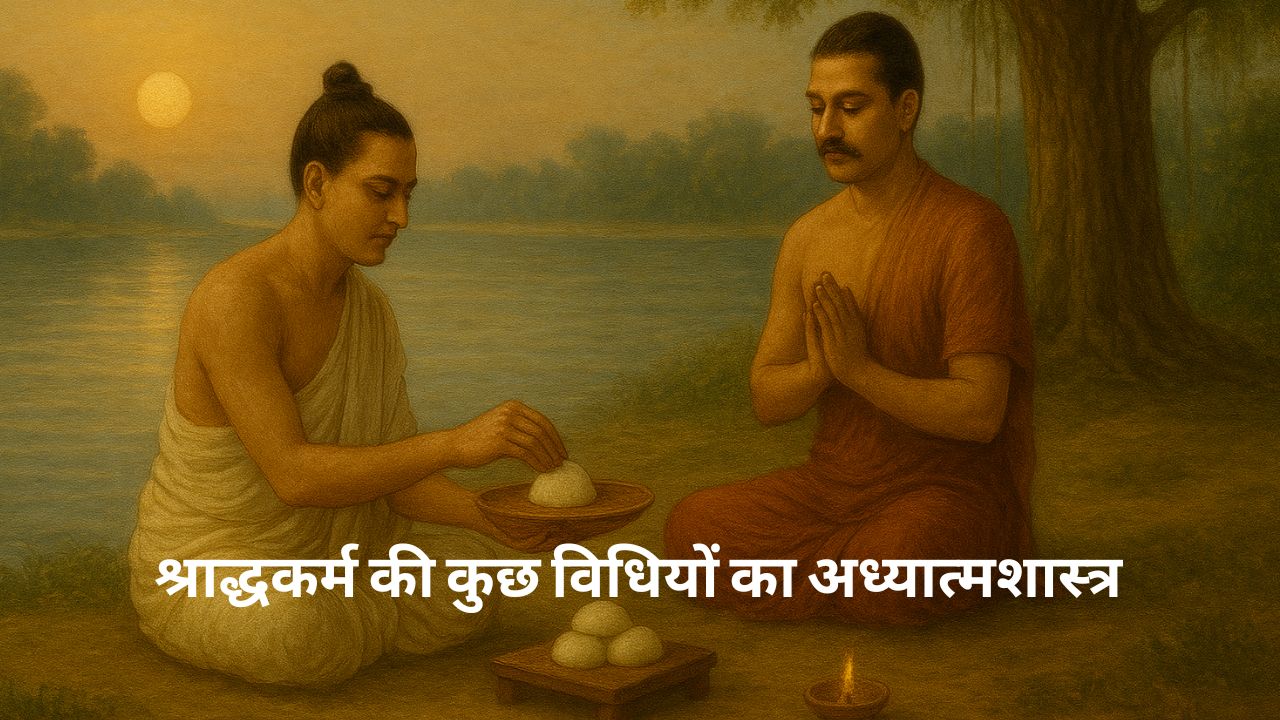- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
लेखक :श्री योगेंद्र जोशी
Mystic Power- वर्णाश्रम हिन्दुओं में प्रचलित एक ऐसी प्राचीन समाजिक व्यवस्था है जिसे आज की सामाजिक वास्तविकता के परिप्रेक्ष में समझ पाना कठिन है । इस व्यवस्था के दो पक्ष रहे हैं, पहला है श्रम अथवा कार्य विभाजन के आधार पर सामुदायिक स्तर के दायित्वों की 4 श्रेणियों का निर्धारण करना । इसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है । दूसरा है वह पहलू जिसका संबंध इन बातों से रहता है कि मनुष्य अपनी उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर किन दायित्वों को निभाए, कैसी दिनचर्या अपनाए, और कैसे जीवन के अपरिहार्य अवसान के लिए स्वयं को तैयार करे । ये बातें 4 कालखंडों की आश्रम व्यवस्था से संबंधित रहती हैं । मैं इस स्थल पर ऋग्वेद की उस ऋचा का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें चारों वर्णों की बात की गई है:
 "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायतः ॥"
(ऋग्वेद संहिता, मण्डल 10, सूक्त 90, ऋचा 12)
यदि शब्दों के अनुसार देखें तो इस ऋचा का अर्थ यों समझा जा सकता है:
सृष्टि के मूल उस परम ब्रह्म का मुख ब्राह्ण था, बाहु क्षत्रिय के कारण बने, उसकी जंघाएं वैश्य बने और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ ।
"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायतः ॥"
(ऋग्वेद संहिता, मण्डल 10, सूक्त 90, ऋचा 12)
यदि शब्दों के अनुसार देखें तो इस ऋचा का अर्थ यों समझा जा सकता है:
सृष्टि के मूल उस परम ब्रह्म का मुख ब्राह्ण था, बाहु क्षत्रिय के कारण बने, उसकी जंघाएं वैश्य बने और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ ।
 क्या उक्त ऋचा की व्याख्या इतने सरल एवं नितांत शाब्दिक तरीके से किया जाना चाहिए ? या यह बौद्धिक तथा दैहिक श्रम-विभाजन पर आधारित एक अधिक सार्थक सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा करती है ? मैं आगे अपना मत व्यक्त करूं उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि किंचित् अंतर के साथ इस ऋचा से साम्य रखने वाला श्लोक मनुस्मृति में भी उपलब्ध है:
"लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरूपादतः ।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥"
(मनुस्मृति, अध्याय 1, श्लोक 31)
(लोकानां तु विवृद्धि-अर्थम् मुख-बाहू-ऊरू-पादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्-अवर्तयत् ।)
शाब्दिक अर्थ: समाज की वृद्धि के उद्येश्य से उसने (ब्रह्म ने) मुख, बाहुओं, जंघाओं एवं पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का निर्माण किया ।
मेरी अपनी धारणा है कि उक्त चार वर्णों के पुरूषों का शरीरतः जन्म ब्रह्मा के चार कथित अंगों से हुआ है ऐसा मंतव्य उल्लिखित ऋग्वैदिक ऋचा में निहित नहीं होना चाहिए । मैं समझता हूं कि ये चार अंग श्रम विभाजन के चार श्रेणियों को व्यक्त करते हैं । ध्यान दें कि मनुष्य का मुख लोगों को शिक्षित करने, उन्हें उचितानुचित की बातें बताने, उन्हें अध्यात्म एवं दर्शन का जानकारी देने जैसे कार्य की भूमिका निभाता है । तदनुसार मुख ब्राह्मणोचित बौद्धिक कार्यों में संलग्नता का द्योतक है, जिसमें शारीरिक श्रम गौण होता है । इसी प्रकार भुजाओं को राज्य की बाह्य आक्रांताओं से रक्षा करने, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने, समाज-विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखने जैसी भूमिका का द्योतक समझा जाना चाहिए । ये ऐसे कार्य हैं जिनमें अच्छी शारीरिक सामर्थ्य के साथ प्रत्युत्पन्नमतिता की बाद्धिक क्षमता की आवश्यकता अनुभव की जाती है । प्राचीन ग्रंथों में इनको क्षत्रियोचित कार्य कहा गया है ।
ऋचा में उल्लिखित शब्द जंघाओं (जांघों) को मैं तीसरी श्रेणी के कार्यों से जोड़ता हूं । ये कार्य हैं नागरिकों के भोजन हेतु कृषि कार्य में लगना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करना, वाणिज्यिक कार्यों को संपन्न करना आदि । इन कार्यों में व्यापार विशेष के योग्य सामान्य बुद्धि की भूमिका प्रमुख रहती है और शारीरिक श्रम की विशेष आवश्यकता नहीं होती । इन्हें वैश्यों के कार्य कहा गया है । इन सब के विपरीत वे कार्य भी समाज में आवश्यक रहे हैं, जिनमें अतिसामान्य प्रकार की बौद्धिक क्षमता पर्याप्त रहती है और जिनमें शारीरिक श्रम ही प्रायः आवश्यक होता है । मनुष्य के पांव श्रमिकोचित कार्य के द्योतक के तौर पर देखे जा सकते हैं । हाथों का कार्य प्रायः हस्तकौशल के साथ संपादित किए जाते हैं, किंतु पांव से कार्य लेना सामान्यतः मात्र श्रमसाध्य होते हैं । दूसरों को विविध सेवाएं देने वाले इस वर्ग के लोगों को शूद्र कहा गया ।
समाज में बौद्धिक एवं दैहिक श्रम के उपयोग को मोटे तौर पर उपर्युक्त प्रकार से विभाजित किया जा सकता है । हम कह सकते हैं कि ब्रह्म अर्थात् परमात्मा ने इस विभाजन के साथ ही मानव समाज की रचना की है ।
इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज हिन्दू समाज में सैकड़ों प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं । ऐसे जातीय विभाजन का जिक्र प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता । कदाचित् इस विभाजन को समय के साथ समाज में घर कर गई विकृति के तौर पर देखा जाना चाहिए । प्राचीन भारत में समाज चार वर्णों में विभक्त था और उसी का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है ।
जिस प्रकार के कार्य में किसी परिवार के सदस्य संलग्न हों कदाचित् वही आगे की पीढ़ियां भी सीखती होंगी । ऐसा समाज में आज भी कुछ हद तक देखने को मिलता है । कुछ समय पहले तक कई व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे हैं । अब स्थितियां कुछ बदल गई हैं । शायद समय के साथ वर्ण विशेष परिवारों की विशिष्टता बन गया हो और ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण आदि की परंपरा ने जन्म लिया हो ।
क्या उक्त ऋचा की व्याख्या इतने सरल एवं नितांत शाब्दिक तरीके से किया जाना चाहिए ? या यह बौद्धिक तथा दैहिक श्रम-विभाजन पर आधारित एक अधिक सार्थक सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा करती है ? मैं आगे अपना मत व्यक्त करूं उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि किंचित् अंतर के साथ इस ऋचा से साम्य रखने वाला श्लोक मनुस्मृति में भी उपलब्ध है:
"लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरूपादतः ।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥"
(मनुस्मृति, अध्याय 1, श्लोक 31)
(लोकानां तु विवृद्धि-अर्थम् मुख-बाहू-ऊरू-पादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्-अवर्तयत् ।)
शाब्दिक अर्थ: समाज की वृद्धि के उद्येश्य से उसने (ब्रह्म ने) मुख, बाहुओं, जंघाओं एवं पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का निर्माण किया ।
मेरी अपनी धारणा है कि उक्त चार वर्णों के पुरूषों का शरीरतः जन्म ब्रह्मा के चार कथित अंगों से हुआ है ऐसा मंतव्य उल्लिखित ऋग्वैदिक ऋचा में निहित नहीं होना चाहिए । मैं समझता हूं कि ये चार अंग श्रम विभाजन के चार श्रेणियों को व्यक्त करते हैं । ध्यान दें कि मनुष्य का मुख लोगों को शिक्षित करने, उन्हें उचितानुचित की बातें बताने, उन्हें अध्यात्म एवं दर्शन का जानकारी देने जैसे कार्य की भूमिका निभाता है । तदनुसार मुख ब्राह्मणोचित बौद्धिक कार्यों में संलग्नता का द्योतक है, जिसमें शारीरिक श्रम गौण होता है । इसी प्रकार भुजाओं को राज्य की बाह्य आक्रांताओं से रक्षा करने, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने, समाज-विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखने जैसी भूमिका का द्योतक समझा जाना चाहिए । ये ऐसे कार्य हैं जिनमें अच्छी शारीरिक सामर्थ्य के साथ प्रत्युत्पन्नमतिता की बाद्धिक क्षमता की आवश्यकता अनुभव की जाती है । प्राचीन ग्रंथों में इनको क्षत्रियोचित कार्य कहा गया है ।
ऋचा में उल्लिखित शब्द जंघाओं (जांघों) को मैं तीसरी श्रेणी के कार्यों से जोड़ता हूं । ये कार्य हैं नागरिकों के भोजन हेतु कृषि कार्य में लगना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करना, वाणिज्यिक कार्यों को संपन्न करना आदि । इन कार्यों में व्यापार विशेष के योग्य सामान्य बुद्धि की भूमिका प्रमुख रहती है और शारीरिक श्रम की विशेष आवश्यकता नहीं होती । इन्हें वैश्यों के कार्य कहा गया है । इन सब के विपरीत वे कार्य भी समाज में आवश्यक रहे हैं, जिनमें अतिसामान्य प्रकार की बौद्धिक क्षमता पर्याप्त रहती है और जिनमें शारीरिक श्रम ही प्रायः आवश्यक होता है । मनुष्य के पांव श्रमिकोचित कार्य के द्योतक के तौर पर देखे जा सकते हैं । हाथों का कार्य प्रायः हस्तकौशल के साथ संपादित किए जाते हैं, किंतु पांव से कार्य लेना सामान्यतः मात्र श्रमसाध्य होते हैं । दूसरों को विविध सेवाएं देने वाले इस वर्ग के लोगों को शूद्र कहा गया ।
समाज में बौद्धिक एवं दैहिक श्रम के उपयोग को मोटे तौर पर उपर्युक्त प्रकार से विभाजित किया जा सकता है । हम कह सकते हैं कि ब्रह्म अर्थात् परमात्मा ने इस विभाजन के साथ ही मानव समाज की रचना की है ।
इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज हिन्दू समाज में सैकड़ों प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं । ऐसे जातीय विभाजन का जिक्र प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता । कदाचित् इस विभाजन को समय के साथ समाज में घर कर गई विकृति के तौर पर देखा जाना चाहिए । प्राचीन भारत में समाज चार वर्णों में विभक्त था और उसी का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है ।
जिस प्रकार के कार्य में किसी परिवार के सदस्य संलग्न हों कदाचित् वही आगे की पीढ़ियां भी सीखती होंगी । ऐसा समाज में आज भी कुछ हद तक देखने को मिलता है । कुछ समय पहले तक कई व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे हैं । अब स्थितियां कुछ बदल गई हैं । शायद समय के साथ वर्ण विशेष परिवारों की विशिष्टता बन गया हो और ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण आदि की परंपरा ने जन्म लिया हो ।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.