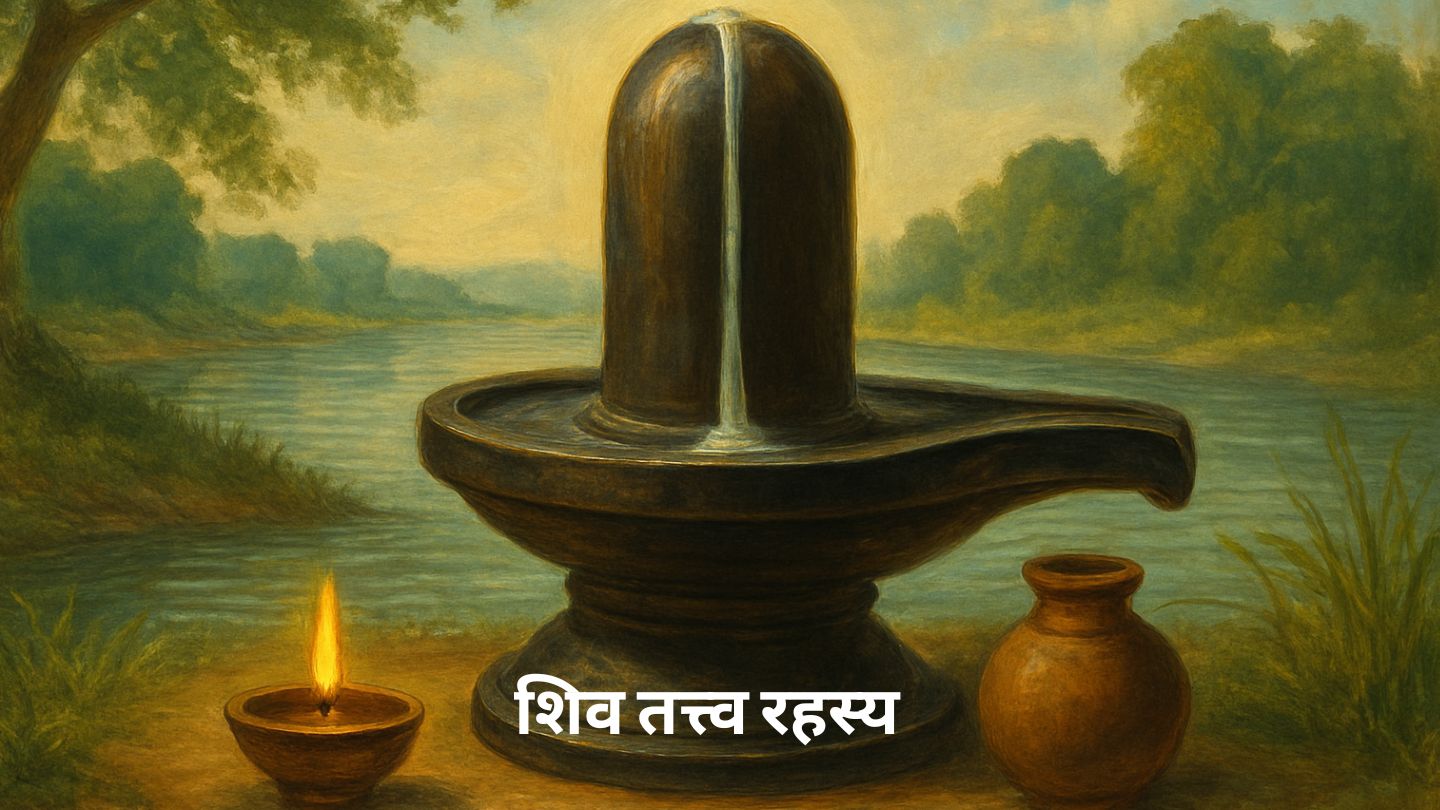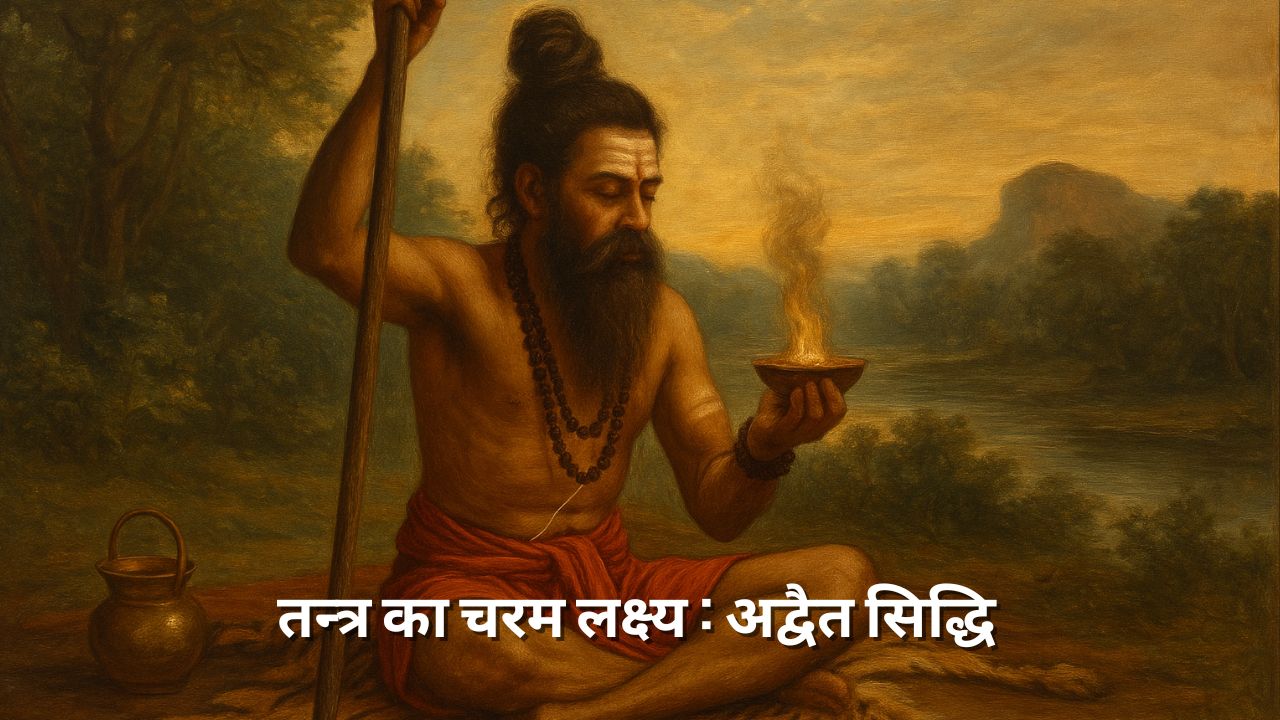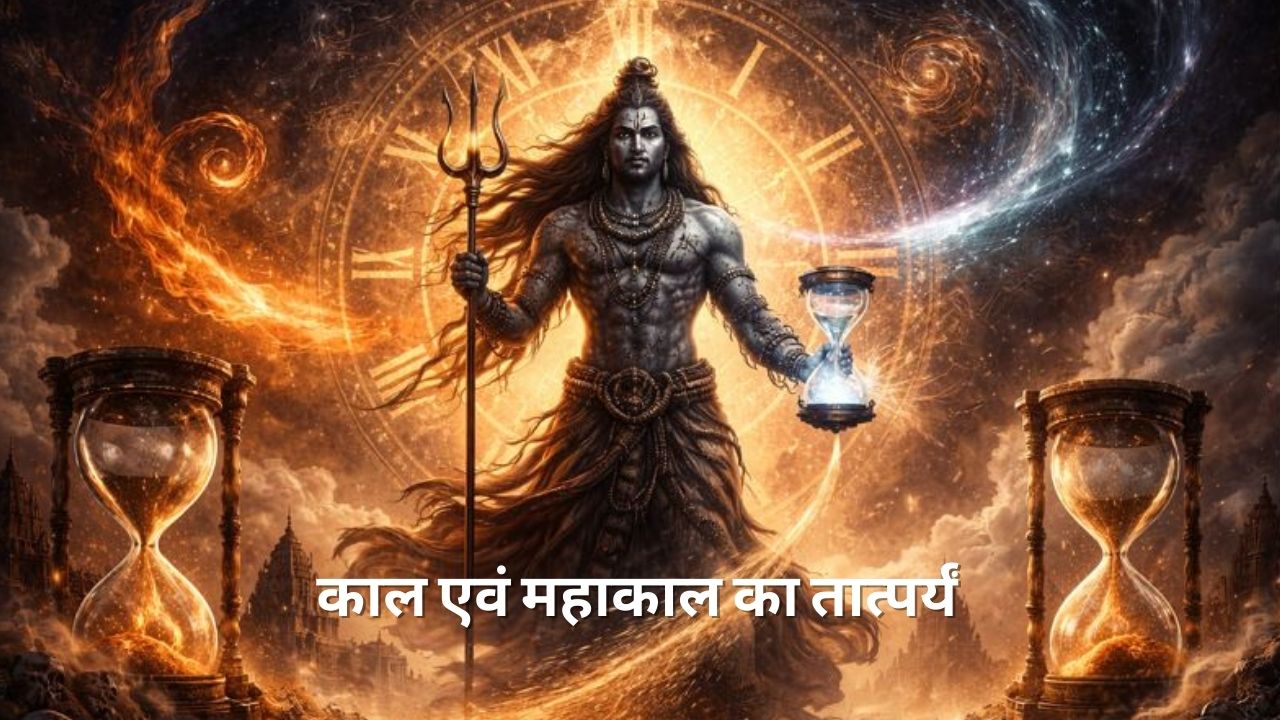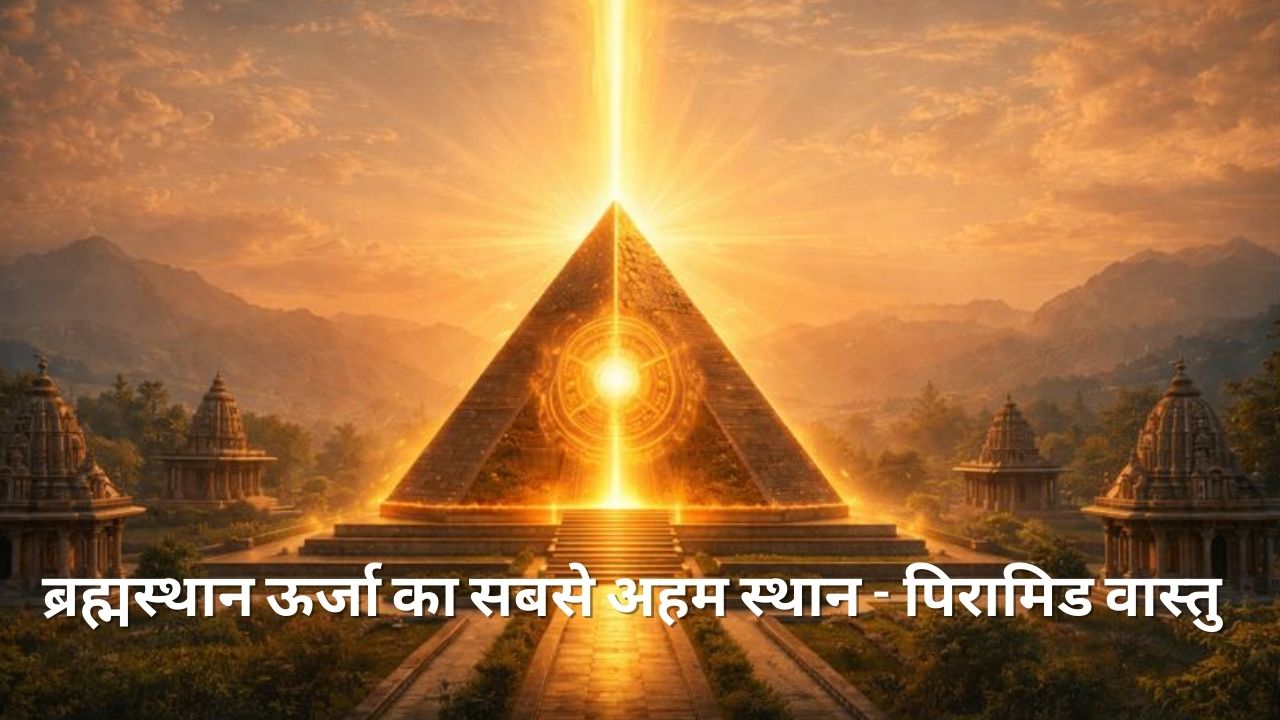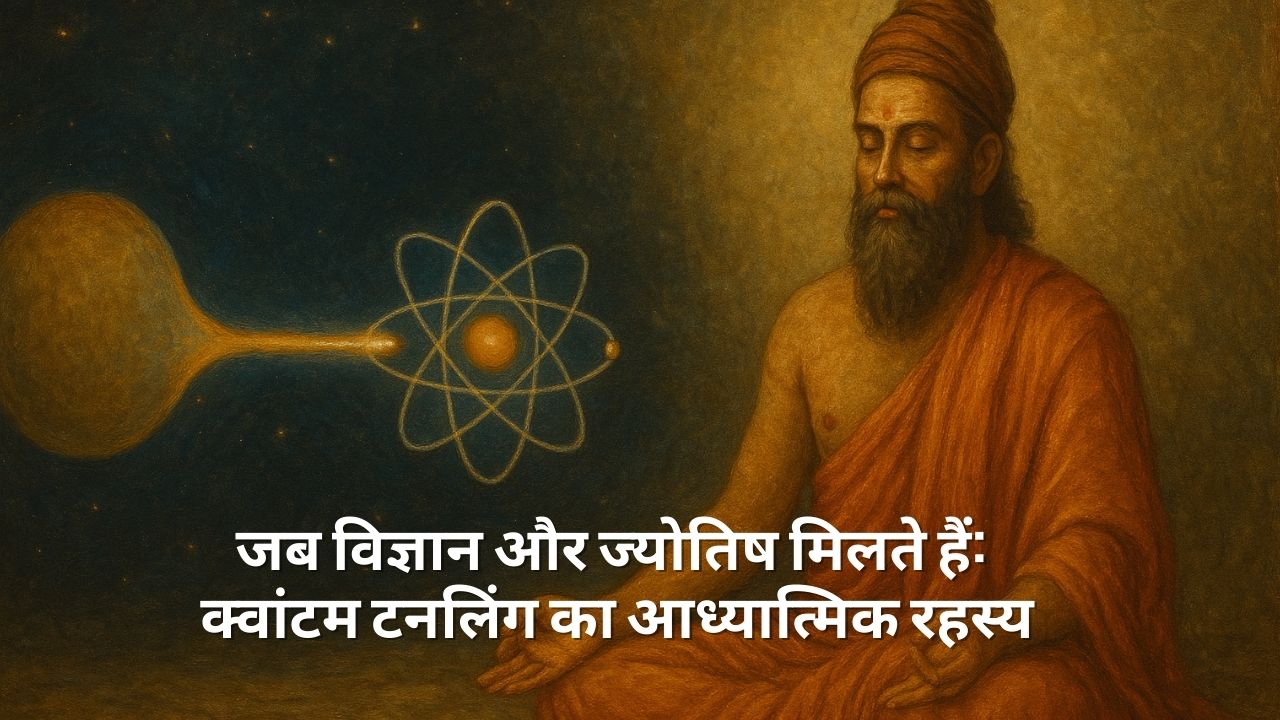- तंत्र शास्त्र
- |
- 01 January 2025
- |
- 0 Comments
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
ॐ मणिपद्मे हुँ। बौद्ध धर्म का साधना मन्त्र है जो विशेषकर हिमालय क्षेत्रों में प्रचलित है।
मनुष्य शरीर की क्रिया या विश्व स्वरूप एक ही है। अतः बौद्ध दर्शन भी इन तत्त्वों का प्रायः वही वर्णन करता है जो सनातन धर्म में है। कुछ भिन्न पारिभाषिक शब्द हैं या एक ही शब्द के भिन्न नाम हैं। तन्त्र में एक मूल प्रकृति के ३ भाग होते हैं-महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती। इनके पुनः ३-३ भाग होने से ९ भाग होते हैं, तथा मूल अज्ञात काली तत्त्व को मिला कर १० महाविद्या होती हैं।
तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा। तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम्॥ (वाज. यजु. २०/६३)
= सरस्वती, इळा, भारती (अश्विन् द्वारा)-ये ३ देवियां पुनः ३-३ में विभाजित हैं। इनको सोम अर्पण से इन्द्र (या इन्द्रिय) की पुष्टि होती है।
बौद्ध साहित्य में १० महाविद्या को १० प्रज्ञा-पारमिता कहा गया है। महा-विद्या = विद्या का महः (महर्, महल, आवरण क्षेत्र)। प्रज्ञा = मन द्वारा बाह्य तत्त्व का ज्ञान। इसे वेद में प्रज्ञान-आत्मा कहा गया है-
यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥
(शिव सङ्कल्प सूक्त, वाज. यजु. ३४/३)
= जो विशेष प्रकार के ज्ञान का कारण है, जो सामान्य ज्ञान का कारण है, जो धैर्य रूप है, जो समस्त प्रजा के हृदय में रह कर उसकी समस्त इन्द्रियों को प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर भी अमर रहता है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी (शिव) सङ्कल्प से युक्त हो।
मन ५ ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान लेता है, ५ कर्मेन्द्रियों द्वारा शरीर चलाता है। ज्ञान कर्म के सम्बन्ध रूप में मन प्रज्ञान है। मन में अनन्त विचार आते रहते हैं, यह प्रज्ञान है। उनका व्यवस्थित रूप बुद्धि है। जिस इच्छा द्वारा कर्म की योजना बने वह सङ्कल्प है-सङ्कल्प मूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्प सम्भवाः (मनु स्मृति, २/३)।
मन की क्रिया का महः या निकट आकाश में जो विस्तार है वह महाविद्या या प्रज्ञापारमिता है।
महाविद्या का उपदेश सुमेधा ऋषि ने परशुराम को दिया था, जब वे जनक के धनुषयज्ञ के बाद तप के लिए महेन्द्र पर्वत पर गये थे। यह उपदेश त्रिपुरा रहस्य के ३ विशाल खण्डों में है-ज्ञान खण्ड, माहात्म्य खण्ड, कर्म खण्ड (तृतीय उपलब्ध नहीं है)। यही सुमेधा ऋषि चण्डी पाठ के उपदेशक हैं। इनको बौद्ध साहित्य में सुमेधा बुद्ध कहा गया है। महेन्द्र पर्वत पर इनका स्थान ओड़िशा बा बौध जिला है। परशुराम के देहान्त के बाद ६१७७ ईपू में कलम्ब संवत् आरम्भ हुआ था। उन्होंने कर्णाटक तट पर शूर्पारक (बौद्ध साहित्य का सोपारा) नगर बनाया था जिसमें समुद्री जहाज लगाने के लिये सूप (शूर्प) की तरह तट की खुदाई की गयी था। उसकी पत्थर की ३० किमी. लम्बी दीवाल आज भी समुद्र में है, जिसे ८,००० वर्ष पुराना अनुमानित किया गया है। वननिधि समुद्र के जहाजों का घर होने के अर्थ में यह बन्दरगाह है। यहां लंगर का पतन होने से पत्तन है। गोलीय त्रिकोणमिति में ऊपर विन्दु को कदम्ब, निम्न विन्दु को कलम्ब कहते हैं। अतः बन्दरगाह को कलम्ब कहा गया (जैसे श्रीलंका का कोलम्बो) और परशुराम संवत् को कलम्ब संवत् (केरल का कोल्लम)।
१० महाविद्या में तारा की उपासना हिमालय क्षेत्रों में प्रचलित है, जिनको तिब्बत में डोलमा कहते हैं। तारा का कई प्रकार से वर्णन है, बौद्ध समाज में उनको चिकित्सा की देवी रूप में पूजा होती है- रोग से तारण या मुक्त करने वाली।
शाब्दिक तर्क रूप में बौद्ध दर्शन अनादि काल से है, जब भाषा की उत्पत्ति हुई। इसे सूत्र-बद्ध करने वाले को गौतम कहा गया। मन के भीतर वाक् के ३ पद हैं-परा, पश्यन्ती, मध्यमा। इनको गौ (ग = ३, तृतीय व्यञ्जन) कहते हैं, जिसका अर्थ वाक् या वाणी भी है। वाक् जब मन से बाहर कथन या लेखन रूप में निकलती है, उसे वैखरी कहते हैं। मन के भीतर के विचार को पूरी तरह शब्द में प्रकट नहीं कर सकते-भाषा, ज्ञान, या उपयुक्त शब्द उपलब्ध नहीं है। इसे तम (अन्धकार) कहते हैं। गौ तथा तम के भीतर सम्बन्ध को गौतम दर्शन कहते हैं। इस पद्धति से बौद्ध ज्ञान की व्याख्या करने वाले को भी गौतम बुद्ध कहते हैं। इस दर्शन में २ ही विकल्प हैं-सत्य, असत्य। गणित या विज्ञान में कई विकल्प हैं, उनके लिए अनेकान्त (जैन) या एकत्व (वेदान्त) दर्शन हुए।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.