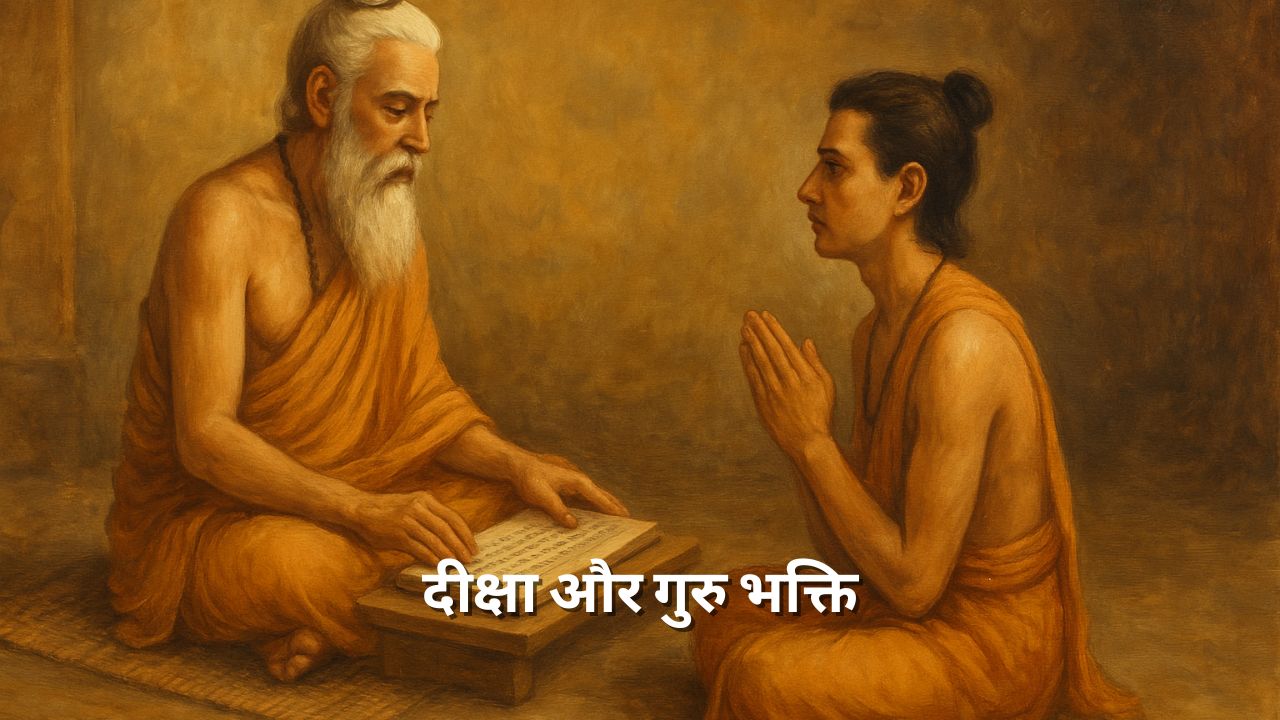- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
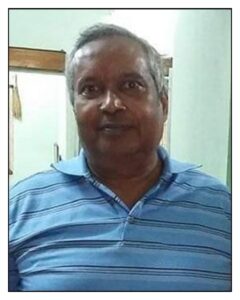
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)- हर व्यक्ति के लिए माता प्रथम गुरु है। उसके बाद पिता से सांसारिक शिक्षा मिलती है। इनकी भक्ति का यह अर्थ नहीं है कि जीवन भर माता की गोद में बैठ कर भोजन करें, या पिता की अंगुली पकड़ कर चलें। दोनों की शिक्षा का उद्देश्य था कि हम स्वतन्त्र हो कर अपना मार्ग चुनें तथा उनसे भी आगे बढ़ें।
हर गुरु का यही उद्देश्य है कि शिष्य उससे आगे निकले तथा उनकी भूलों का भी सुधार करें।
सर्वत्र जयमिच्छेत, पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। गीता (४/२८) में इसी को ज्ञान यज्ञ कहा है। ज्ञान यज्ञ समाज में ज्ञान परम्परा की रक्षा तथा विस्तार करता है। स्वाध्याय यज्ञ व्यक्तिगत ज्ञान तथा योग्यता का वितार करता है। गुरु से आगे निकलने में गुरु का सम्मान है।
अर्जुन सदा गर्व सहित अपने को द्रोण-शिष्य कहते थे। मेरे विद्यालय के एक शिक्षक मेरे परीक्षाफल पर सदा मुझसे अधिक प्रसन्न होते थे तथा उसकी गर्व सहित १ महीने तक चर्चा करते थे। मुझे स्वयं कष्ट होता था कि कुछ छूट गया नहीं तो अधिक अच्छा परिणाम होता।
योग-ध्यान की शिक्षा- दीक्षा मैंने कई स्रोतों से ली है-स्वामी निगमानन्द सरस्वती, सत्यानन्द योग विद्यालय, महेश योगी, क्रिया योग, पुरी शंकराचार्य। इसके अतिरिक्त शक्तिपात दीक्षा के लिए ऋषिकेश के योगश्री पीठ भी गया था। उन्होंने कहा कि उनकी दीक्षा मेरे लिए उपयुक्त नहीं है तथा क्रिया योग की सलाह दी। क्रिया योग में भी जिनके पास गया उन्होंने अन्य के पास जाने की सलाह दी जिनसे उनका कोर्ट में विवाद चल रहा था तथा परस्पर बातचीत नहीं थी। उनके विरोधी ने पूछा कि किसने उनके पास भेजा तो उत्तर सुन कर स्तब्ध रह गये। ३ वर्ष में ३ बार दीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि भारतीय शास्त्रों के लिए मैं ही उनका एक गुरु हूं। जब वे छात्र थे तो एक पुस्तक दूकान पर गीता खोज रहे थे। एक अंग्रेजी टीका दिखा कर मुझसे पूछा कि यह कैसी है। मैंने कहा कि अंग्रेजी में पढ़ने से ७ जन्म में भी गीता नही आयेगी। उनको यह वाक्य स्मरण था तथा इसका पालन किया।
शंकराचार्य तथा रामानुज परम्परा-दोनों में दीक्षा ली है। दोनों गुरुओं को पता था कि मैं अन्य से भी दीक्षा ले रहा हूं, पर कभी विवाद नहीं हुआ। वैदिक साहित्य की प्रथम दीक्षा पिताजी से ली। मैं प्रायः विरोध करने के लिए अलग अर्थ करता था, पर वे प्रसन्न हो जाते थे कि कोष के लिए नया अर्थ मिला। नवीन वैकल्पिक अर्थ जानने की प्रसन्नता ज्ञान का स्रोत है, जो जिज्ञासा का ही एक रूप है। हर दर्शन का सूत्र ग्रन्थ जिज्ञासा से ही आरम्भ हुआ है।
मैं वैदिक साहित्य के लिए प्रायः पण्डित मधुसूदन ओझा तथा उनके शिष्य मोतीलाल शर्मा की पुस्तकें पढ़ता हूं। मूल सन्दर्भ तथा अर्थ के लिए आर्यसमाज के विद्वानों भगवद्दत्त, सातवलेकर तथा हरिशरण जी की पुस्तकें देखता हूं। कुछ विदुओं पर हर व्यक्ति से मेरा मतभेद है जैसे पण्डित मधुसूदन ओझा से लोकों की अहर्गण माप तथा उनके प्रकार, या वेदार्थ में प्रायः प्रसंग अनुसार मूल लेखकों से अलग अर्थ करता हूं। पर अलग अर्थ भी सातवलेकर जी या हरिशरण जी की कृपा से ही हो रहा है।
सप्तर्षि वर्ष के दो अर्थों का समन्वय किया तो कई लोगों ने एक मास तक झगड़ा किया कि मैं आर्य समाज तथा भगवद्दत्त का विरोधी हूं। उस प्रसंग पर स्वयं भगवद्दत्त ने लिखा था कि इस विषय पर अधिक शोध की आवश्यकता है। इसी प्रकार मधुसूदन ओझा तथा भगवद्दत्त-दोनों के अनुसार ब्रह्मा का काल १३००० विक्रम पूर्व है, पर उनसे मेरा मत भिन्न है। पर यह विरोध नहीं है-दोनों ने लिखा था कि इससे बाद का काल नहीं हो सकता है।
ब्रह्म सूत्र के आरम्भ में ही ज्ञान के ३ स्रोत कहे हैं-जिज्ञासा, शास्त्र, समन्वय। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्रयोनित्वात्, तत्तु समन्वयात्। यदि मन के भीतर विरोध होने लगे तो ज्ञान नहीं हो सकता, शरीर भी नष्ट हो सकता है-संशयात्मा विनश्यति। जैसे कम्प्यूटर में वायरस से उसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है वैसे ही अन्तर्विरोध से शरीर व्यवस्था नष्ट होती है। समन्वय से देखने पर मुझे वेद, पुराण, जैन ज्योतिष, सूर्य सिद्धान्त आदि में कहीं विरोध नहीं दीखता है, सबने एक ही बात भिन्न प्रकार से कही है। मतवाद का विवाद ऐसा है है जैसे कोई कहे कि गणित ठीक है, भौतिक या रसायन विज्ञान गलत है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.