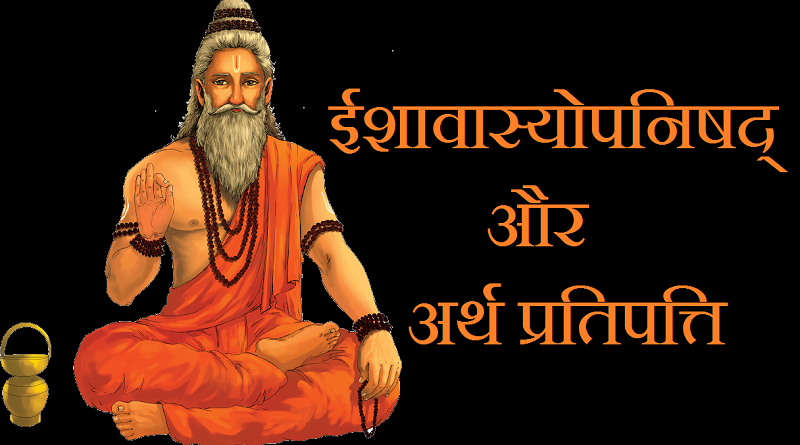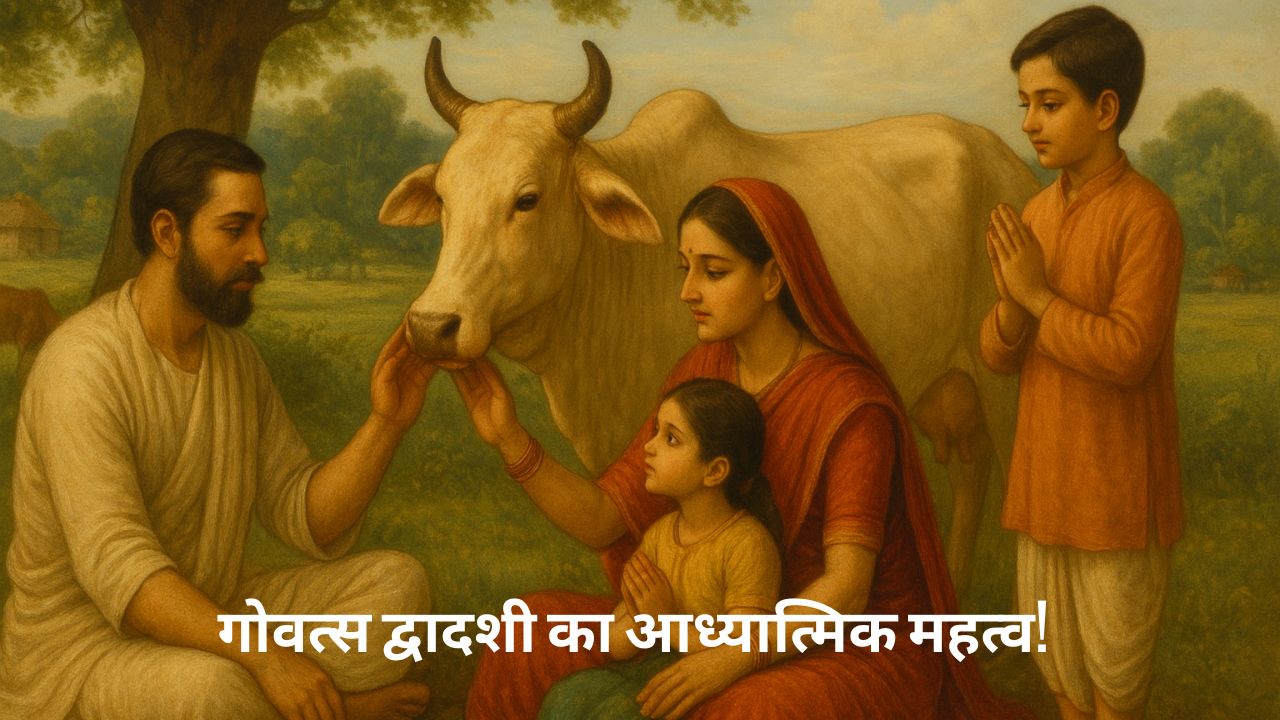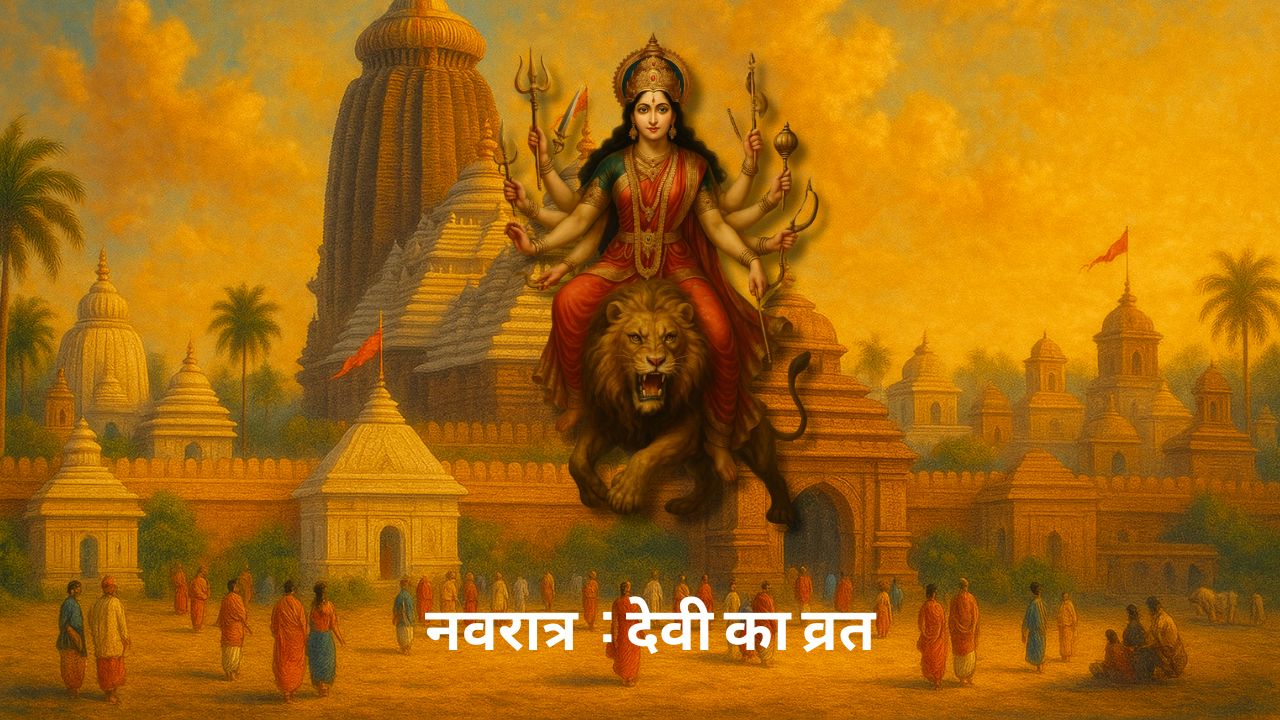- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
श्री अरुण उपाध्याय (धर्म शास्त्र विशेषज्ञ)-ईशावास्योपनिषद्, ८ में वाक्-अर्थ की दो प्रकार से प्रतिपत्ति है जिसको कालिदास ने रघुवंश आरम्भ में पार्वती परमेश्वर का रूप कहा है।
स पर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू,याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।
वाग्र्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ॥
इसी को तुलसीदास ने सीता-राम कहा है या सांख्य में पुरुष-प्रकृति कहा है- गिरा अरथ जल-वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। वन्दौं सीताराम पद, जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न।।
अव्यक्त अखन्ड परात्पर ब्रह्म ही दृश्य जगत् के रूप में प्रकट होता है। पुरुष सूक्त ३,४ के अनुसार भूत, भविष्य, वर्तमान का दृश्य जगत् पुरुष का एक ही पाद है। बाकी ३ पाद आकाश में अमृत (सनातन) हैं। चारों पाद मिला कर पूरुष कहा गया है।
मानव मस्तिष्क के अव्यक्त विचार भी तीन पाद हैं, तथा व्यक्त विचार (लेख, शब्द आदि द्वारा) चतुर्थ पाद हैं। जब अव्यक्त विचार को ज्यों का त्यों (याथातथ्य) व्यक्त किया जाय तो वह शाश्वत होता है। किसी एक घटना का वाक् द्वारा वर्णन वाक्य है। उसी के शाश्वत रूप में वर्णन काव्य है।
वाल्मीकि ने कामातुर क्रौञ्च युगल में एक का वध (रावण-मन्दोदरी में रावण वध जैसा) वर्णन किया तो राम कथा माध्यम से वह शाश्वत संघर्ष की कथा हो गयी। इस प्रकार शाश्वत काव्य की रचना के कारण वाल्मिकी को आदि कवि कहा गया, नहीँ तो अनुष्टुप आदि छन्दों का ज्ञान पहले से था जिसका उल्लेख रामायण के उस अध्याय में है।
दृश्य या मूर्त जगत् में वाक्-अर्थ प्रतिपत्ति विपरीत प्रकार से है। सभी वस्तुओं का ब्रह्मा ने नाम दिया था।
मनुस्मृति में- सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्। वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे॥ इनको पहले ऋण (रेखा) तथा चिद् ऋण (रेखा का सूक्ष्म भाग विन्दु) द्वारा प्रकट किया गया। (ऋग्वेद, १०/७१)। शब्द इतने अधिक हो गये कि उनको जीवन काल में स्मरण करना असम्भव हो गया। अतः इन्द्र-मरुत् ने उनको मूल ध्वनियों में व्याकृत (खण्डित) किया जिसे व्याकरण कहा गया।
ब्रह्म सूत्र के प्रथम ४ सूत्रों के अनुसार जिज्ञासा तथा शास्त्र को समन्वय से पढ़ने से ब्रह्म का ज्ञान होता है, पूरे विश्व के प्रति घृणा भाव रख कर नहीँ- अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जन्माद्यस्य यतः। (यहाँ अस्य का अर्थ मूर्त जगत् है) शास्त्र योनित्वात्। तत्तु समन्वयात्। यहाँ तत् का अर्थ दोनो है-अव्यक्त ब्रह्म तथा उसका वर्णन करने वाले व्यक्त शब्द या विश्व। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, शब्द ब्रह्म परं च यत्। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति॥ (मैत्रायणी आरण्यक, ६/२२) मूर्तियों तथा उनके प्रतिपादक मूर्त शब्दों के माध्यम से ही परम ब्रह्म का ज्ञान होता है, अमूर्त शब्द, सादा कागज या शून्य आकाश से नहीँ।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.