- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
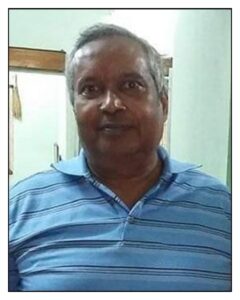
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )- Mystic Power -
१. चातुर्मास-आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहते हैं, जब देव या हरि (भगवान्) सोते हैं। इसके बाद ४ मास-श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्त्तिक- में शयन करते हैं। बीच में भाद्र शुक्ल एकादशी को पार्श्व परिवर्तन करते हैं। चातुर्मास पूर्ण होने के समय कार्त्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान् उठते हैं जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इन चार मास में कम यात्रा होती है। परिव्राजक (सदा चलने वाले) संन्यासी इन ४ मासों में एक स्थान पर विश्राम करते हैं, जिसे चातुर्मास नियम कहते हैं। वर्षा के कारण बाहरी यात्रा या व्यायाम नहीं हो सकता है। अतः घर के भीतर ही व्यायाम होता है। यह आषाढ़ मास से आरम्भ होता है, अतः व्यायाम स्थान को आषाढ़ (अखाड़ा) कहते हैं। मनुष्य २४ घण्टे में ८ घण्टा सोता है, उस अनुपात में १२ मास के दिव्य दिन में ४ मास शयन है।
२. कर्त्ता ब्रह्म-इसे संक्षेप में ’क’ कहा गया है। निर्माण के लिए कुछ पदार्थों की हवि या उपभोग होता है, अतः ’क’ (कर्त्ता) केलिए हवि देते हैं-
कस्मै देवाय हविषा विधेम (ऋक्, १०/१२१/१)
निर्विशेष व्रह्म अज्ञेय है, अवर्णनीय है। कर्त्ता के २ भाग हैं- एक रूप में केवल द्रष्टा हैं, अन्य रूप में विश्व के सञ्चालक। इनको साक्षी और भोक्ता सुपर्ण रूप कहते हैं। व्यक्ति शरीर में इनको आत्मा और जीव कहते हैं। ब्रह्म की शक्तियां ७ ऋषि रूप में हैं, जिनके समन्वय को पक्षी रूप में व्यक्त करते हैं। इसके चित्र को सुपर्ण चिति कहते हैं। सृष्टि के ४ मूल बल चौकोर शरीर हैं, २ पक्ष समरूपता है, नियन्त्रक या तेज सिर है, विषमता पुच्छ है। इनसे अग्नि (पदार्थ पिण्ड) का चयन होता है, जिससे विभिन्न निर्माण होते हैं।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकषीति॥ (मुण्डक उप. ३/१/१, श्वेताश्वतर उप. ४/६, ऋक्, १/१६४/२०, अथर्व, ९/९/२०) सुषुम्ना चेतना या ज्ञान का वृक्ष है। उसके मध्य (आज्ञा चक्र) में २ सुपर्ण (हंस, पक्षी) रहते हैं (परिषस्वजाते-पड़ोस में)। उनमें अन्य (एक) पिप्पल (पिब् + फल = जिस फल में आसक्ति हो) को स्वाद सहित खाता है। अन्य (दूसरा) बिना खाये (बिना आसक्ति = अनश्नन्) केवल देखभाल करता है।
त इद्धाः सप्त नाना पुरुषानसृजन्त। स एतान् सप्त पुरुषानेकं पुरुषमकुर्वन्-यदूर्ध्वं नाभेस्तौ द्वौ समौब्जन्, यदवाङ् नाभेस्तौ द्वौ। पक्षः पुरुषः, पक्षः पुरुषः। प्रतिष्ठैक आसीत्। अथ या एतेषां पुरुषाणां श्रीः, यो रस आसीत्-तमूर्ध्व समुदौहन्। तदस्य शिरोऽभवत्। स एवं पुरुषः प्रजापतिरभवत्। स यः सः पुरुषः-प्रजापतिरभवत्, अयमेव सः, योऽयमग्निश्चीयते(कायरूपेण-शरीररूपेण-मूर्त्तिपिण्डरूपेण-भूतपिण्डरूपेण)। स वै सप्तपुरुषो भवति। सप्तपुरुषो ह्ययं, पुरुषः-यच्चत्वार आत्मा, त्रयः पशुपुच्छानि। (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/२-६)
३. पार्थिव सुपर्ण-पृथ्वी पर सूर्य की गति २ प्रकार की है। वार्षिक गति उत्तरायण (मकर से कर्क रेखा तक) तथा उसके विपरीत दक्षिणायन है। यही सुपर्ण का विस्तार है। मकर रेखा पर सूर्य ३ तारा (तार्क्ष्य, ऋक्ष = तारा, भालू) वाले श्रवण नक्षत्र में रहता है (विक्रमादित्य काल में जब शून्य अयनांश था)।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ (यजु, २५/१९) यह आकाश के वृत्त (पृथ्वी कक्षा) की ४ दिशा हैं-ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी इन्द्र, रेवती का पूषा, श्रवण का गोविन्द जो अरिष्ट की नेमि या सीमा (दूर करने वाले) हैं, तथा पुष्य का बृहस्पति। दक्षिण में सूर्य रहने पर हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात्रि तथा शीत होता है अतः यह अरिष्टनेमि है। उत्तरी सीमा के कर्क रेखा को केवल नेमि कहते हैं।
उत्तर -दक्षिण दिशा में यह सूर्य की धुरी (नेमि) है। पृथ्वी अक्ष का झुकाव २२ से २६ अंश तक घटता बढ़ता है। कर्क रेखा की सीमा या नेमि का स्थान नैमिषारण्य है (कूर्म पुराण, २/४३/७, पद्म १/१, वराह, ११/१०७, वायु, १२५/२७, शिव, ७/१/३/५३)। इक्ष्वाकु काल में मिथिला की सीमा पर कर्क रेखा थी अतः वहां के राजा इक्ष्वाकु पुत्र को निमि कहते थे। उनकी निमि (पलक) नहीं गिरती थी। सूर्य चक्षु है, विषुव रेखा पर वह बन्द रहता है, कर्क, मकर रेखा पर पूरी तरह खुल जाता है। (भागवत पुराण, ९/१३, विष्णु, ४/५ आदि)।
आज भी मिथिला में सूर्य के कर्क रेखा पर स्थित होने पर पञ्चाङ्ग आरम्भ होता है। इस सूर्य गति के भी छन्द हैं। यहां गरुड़ संवत्सर रूप है।
अथ ह वाऽ एष महासुपर्ण एव स्यात्संवत्सरः। तस्य यान्पुरस्ताद्विषुवतः षण्मासानुपश्यन्ति सोऽन्यतरः पक्षो ऽथ यान्षड् उपरिष्टात् सः अन्यतरः। आत्मा विषुवान्। (शतपथ ब्राह्मण, १२/२/३/७)
यह वर्गीकरण ब्रह्मा के स्थान पुष्कर (अभी बुखारा) के अनुसार है, जो उज्जैन से १२ अंश पश्चिम है (विष्णु पुराण, २/२८)। वेदाङ्ग ज्योतिष के अनुसार सबसे बड़ा दिन १६ घण्टे का था। सबसे छोटा दिन ८ घण्टे का होगा, उसका आधा। अतः इनको गायत्री (२४ अक्षर) से जगती (४८ अक्षर) तक बांटा गया है। विषुव के उत्तर तथा दक्षिण में १२, २०, २४ अंश के अक्षांश वृत्तों से ये वीथियां बनती थीं। ३४० उत्तर अक्षांश का दिनमान सूर्य की इन रेखाओं पर स्थिति के अनुसार ८ से १६ घण्टा तक होगा। अतः दक्षिण से इन वृत्तों को गायत्री (६ x ४ अक्षर) से जगती छन्द (१२ x ४ अक्षर) तक का नाम दिया गया। इसकी चर्चा ऋग्वेद (१/१६४/१-३, १२, १३, १/११५/३, ७/५३/२, १०/१३०/४), अथर्व वेद (८/५/१९-२०), वायु पुराण, अध्याय २, ब्रह्माण्ड पुराण अध्याय (१/२२), विष्णु पुराण (अ. २/८-१०) आदि में है। इनके आधार पर पं. मधुसूदन ओझा ने आवरणवाद में इसकी व्याख्या की है (श्लोक १२३-१३२)। बाइबिल के इथिओपियन संस्करण में इनोक की पुस्तक के अध्याय ८२ में भी यही वर्णन है।
४. दिव्य दिन-ऋतु चक्र के अनुसार सौर वर्ष को दिव्य दिन कहा गया है। इसमें मकर रेखा से कर्क रेखा तक सूर्य गति (जहां सूर्य किरण लम्ब हो) या उत्तरायण देवों का दिन और कर्क से मकर तक की गति देवों की रात्रि है। असुरों के लिए यह विपरीत है।
ऐन्दवस्तिथिभिः तद्वत् सङ्क्रान्त्या सौर उच्यते। मासैर्द्वादशभिर्वर्ष दिव्यं तदह उच्यते॥१३॥ सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्। षट् षष्टिसङ्गुणं दिव्यं वर्षमासुरमेव च॥१४॥ (सूर्य सिद्धान्त, अध्याय १) अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायनम्॥२४॥ धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्॥२५॥ (गीता, अध्याय, ८)
सौर संक्रान्ति से चान्द्र मास का आरम्भ नहीं होता है। यदि विषुव संक्रान्ति से चैत्र मास का आरम्भ मानें तो- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ -उत्तरायण का द्वितीय अर्ध-विषुव से कर्क तक। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद- कर्क से विषुव तक-दक्षिणायन का प्रथम अर्ध। आश्विन, कार्त्तिक, मार्गशीर्ष-दक्षिणायन का द्वितीय अर्ध। पौष, माघ, फाल्गुन - उत्तरायण का प्रथम अर्ध। दक्षिणायन के प्रथम अर्ध अन्त होने के समय (प्रायः भाद्र शुक्ल एकादशी को) सूर्य विषुव रेखा को पार करते हैं, या पृथ्वी के उत्तर गोल से दक्षिण गोल जाते हैं। इसे पार्श्व परिवर्तन कहा गया है।
अहोरात्रिश्च ते पार्श्वे (वाज. यजुर्वेद, ३१/२२)
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.






