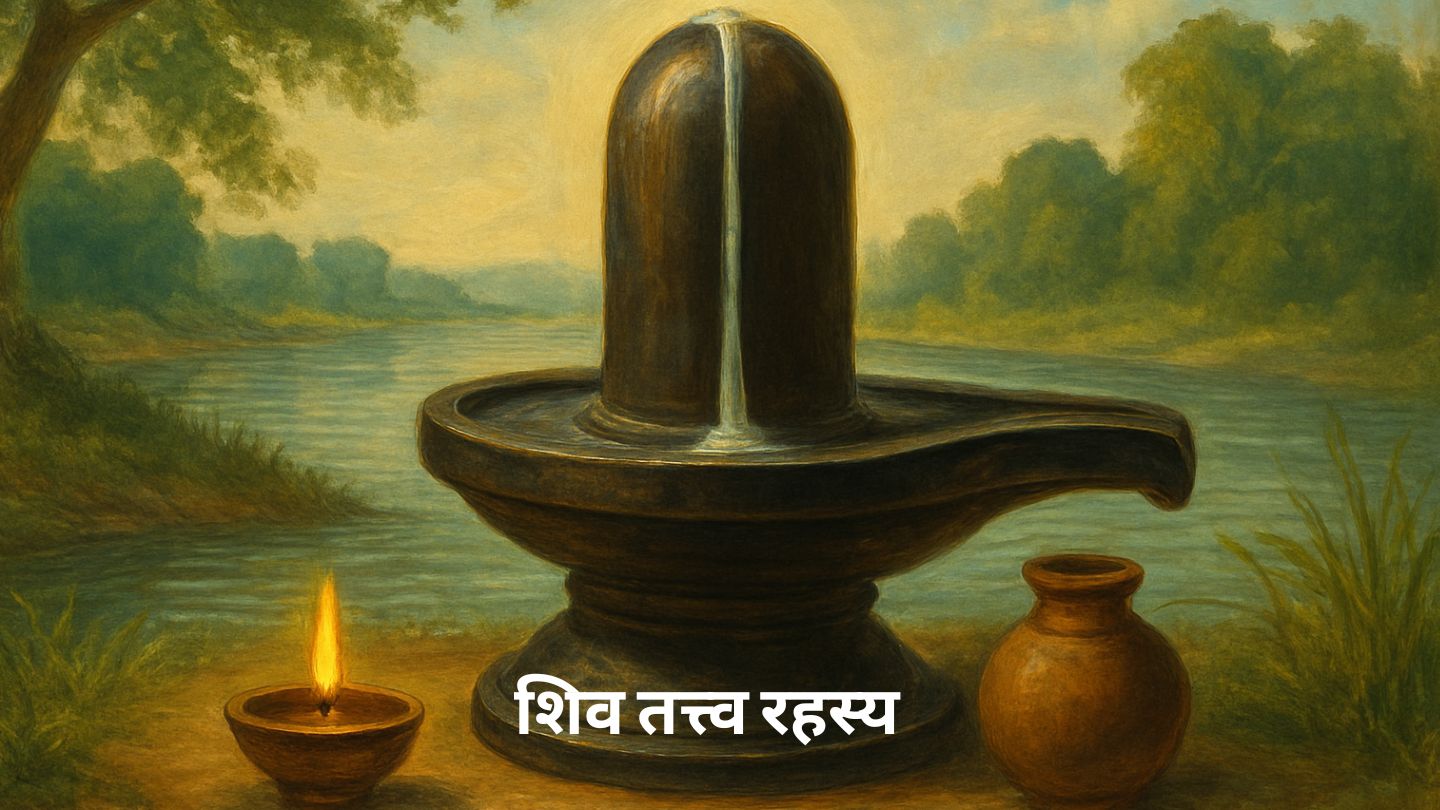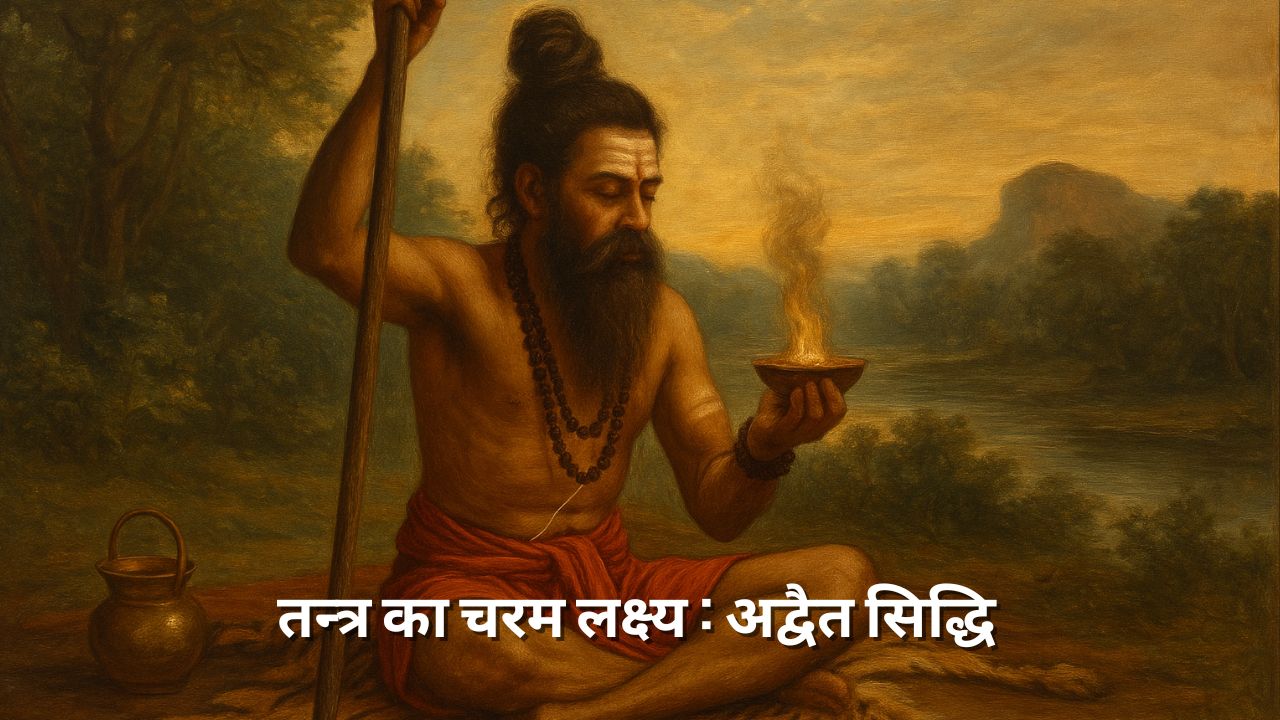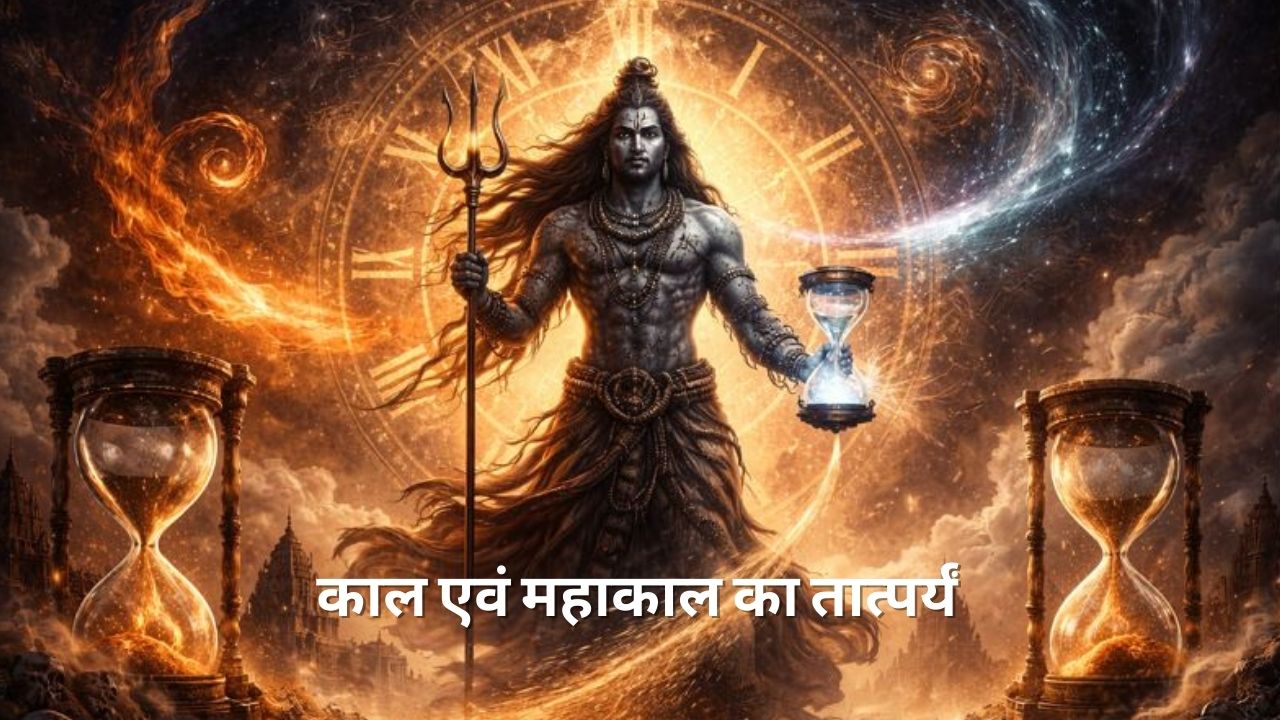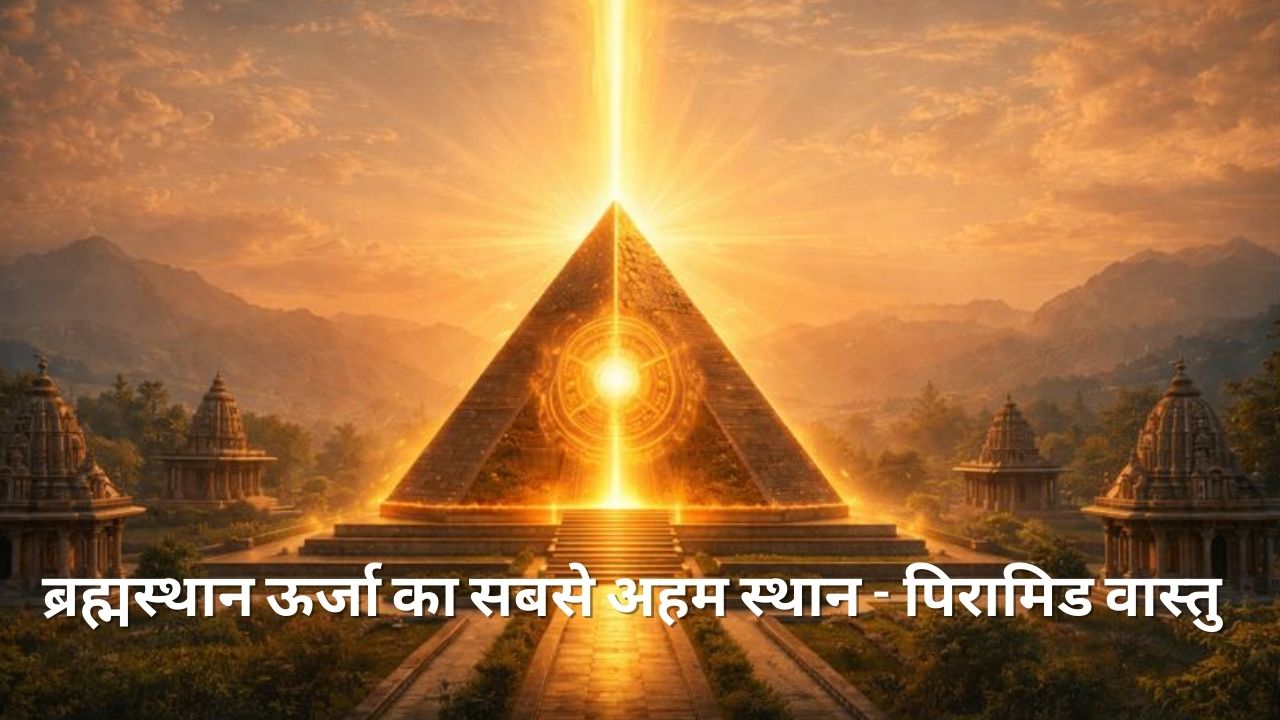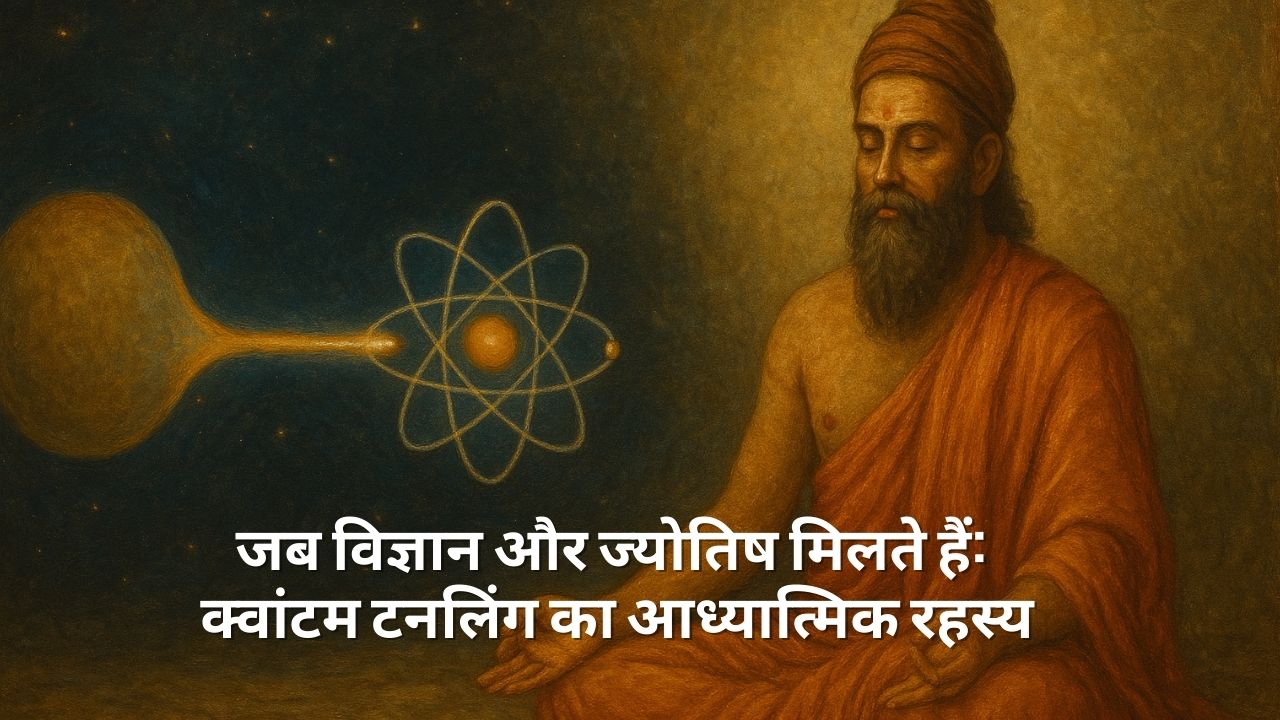- तंत्र शास्त्र
- |
- 15 April 2025
- |
- 0 Comments
तन्त्र में भाव बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है। कौलावली तन्त्र के ग्यारहवें उल्लास में बताया गया है कि 'भावपदार्थ' मन का धर्म विशेष है। वह शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल दिङ् मात्र होता है। जिस तरह गुड़ की मिठास जिह्वा से जानी जाती है, वाणी से नहीं, उसी प्रकार भाव का विभाव केवल मन से ही अनुभव करने योग्य होता है, शब्दों द्वारा नहीं।
महाभाव उपाधि-भेद और विषय भेद से अनेक प्रकार का होता है। भाव अपनी प्रगाढ़ावस्था में जब होता है, तो उससे उत्पन्न समस्त भेद महाभाव में विलीन हो जाते हैं। वस्तुतः भाव ही आनन्दधन-सन्दोह प्रभु है। भाव ही प्रकृति का रूप धारण करता है, भाव ही रसरूपी आत्मा है। भाव ही परम महान् है।"
तन्त्र-मन्त्र की सिद्धि में भाव ही कारण होता है। लाखों-करोड़ों की संख्या में जप किया जाए, होम किया जाए, शारीरिक कष्ट भोग कर साधना की जाए, किन्तु
१. भावस्तु मानसोधर्मः स हि शब्दः कथं भवेत् । तस्मात् भावो न वक्तव्यो दिङमात्न समुदाहृतम् ।।
यबेक्षुगुडमाधुर्य जिह्वाया ज्ञायते सदा । तस्माद् भावो विभावस्तु मनसा परिभाव्यते ।।
२. एक एव महाभावो नानात्वं भजते यतः । उपाधिभेदभावेन भावभेदो भविष्यति ।।
आनन्दघनसन्दोहः प्रभुः प्रकृतिरूपधृक् । रसरूपः स एवात्मा स प्रभुः परमोमहान् ।
बिना भाव के तन्त्र-मन्त्र की सिद्धि फलप्रद नहीं होती है। ज्ञान की विशेष अवस्था ही भाव है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भेद से भाव या ज्ञानावस्था क्रमशः दिव्य, वीर और पशु-तीन प्रकार को होती है। इसी को उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा जाता है। मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के अनुसार साधक के उपर्युक्त भाव तीन प्रकार के माने जाते हैं। जैसी जिस साधक की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही उसकी साधना भी उत्तम, मध्यम, अधम होती है। यदि साधक तमोगुणी स्वभाव का हो और वह दिव्य या वीर भाव की साधना करता है तो उसकी साधना निष्फल होती है। साधना का नियम यह है कि साधक पहले पणुभाव से साधना करके सिद्धि प्राप्त कर बीरभाव में प्रवेश करे। वीरभाव के बाद वह साधना द्वारा दिवभाव की प्राप्ति करे यथा दिव्य-भाव प्राप्त होने पर साधना द्वारा भावातीत्रत अवस्था को प्राप्त करे। तन्त्रशास्त्र का तर्कवचात मन है कि सामान्यतया मनुष्य सोत्रह वर्ष की अवस्था तक मनोवृत्ति को ज्ञानावस्था के कारण पचुनाव प्रधान रहता है। सत्रह वर्ष की अवस्था से लेकर पचास वर्ष की अवस्था तक उत्तेजित मनोवृति के कारण उसमें वीरभाव रहता है और इक्यावन वर्ष की अवस्था से लेकर वृद्धावस्या तक उसकी परिपक्व ज्ञान स्थिति होने से
वह दिव्यभाव सम्पन्न होता है।" तीनों प्रकार के भावों की स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार समझी जा सकती है-
पशुनाव- जिन मनुष्यों में अविद्या का आवरण होने से परिपूर्ण अद्वैत ज्ञान का उदव नहीं होता है, उनकी मानसिक अवस्था तमोगुगी होने के कारण उनमें पशुभाव रहता है। वे पशुओं की तरह अज्ञानान्धकार से आउत संसार से बंधे रहते हैं।
उत्तम और अवन भेद से पशुभाव दो प्रकार का होता है। संसार के मोहजाल में फैना हुआ जीव अधम पशु है और सत्कर्मपरावण भगवद्विश्वासी जीव उत्तम पशु है। अबम और उत्तम दोनों प्रकार के पशुनावों से सम्पन्न प्राणी द्वैतबुद्धि रखने के कारण दोनों पशु ही मारे जाते है। 'वधु' यह एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका तात्पर्य है-अज्ञानी । भगवान् शिव जीवों के पशुभाव (अज्ञान) को दूर करते हैं, इसलिए बह पशुरति' कहे जाते हैं। यजुर्वेद में 'पधूनांपतयेनेः' कह कर पशुपति भगवान शिव की स्तुति की गई है। वेदसार शिवस्तोत्र में भी भगवान् शिव को पापनाशक पशुपति कह कर उनकी स्तुति की गई है- 'पशूनां पतिवापनाशंवरेशन्' ।
बोरनाव- जो साबक अत ज्ञानामृत से परिपूर्ग सरोवर के एक बूंद का भी आस्वाइन कर लेता है, वह वीर पुरुष की नौति अज्ञात रज्जु को तोड़ने में सफल होता है और अमृत सरोवर का सन्चान करने के लिए तत्पर हो जाता है। तब वह वीरभाव-सम्पन्न साधक बन जाता है। वीरवावसान साधक की मनोवृत्ति रजोगुण
१. बहु जरात् तथा होमनात् कावक्तातु विस्तिरैः । न भावेन विना चैव तन्त्र-मन्त्राः फलप्रदाः ।।
२. सर्वे च पशवः सन्ति तलवत् भूतलेन राः ।
तेवो ज्ञान प्रकाशाव वीरभावः प्रकाशितः ।। वीरभावं सदा प्राध्य क्रमेण देवताभवे त् ।- रुद्रयामलतन्य
प्रधान होती है। वह समस्त जागतिक पदार्थों को शिव और शक्ति की विभूति मान-कर धारण करने का प्रयत्न करता है। इस वीरभाव की अवस्था में साधक द्वैतभावना से ऊपर अद्वैतभावना की ओर बढ़ता है।
विव्य-भाव- जब साधक वीरभाव से परिपुष्ट होकर द्वैतभाव को निरस्त कर अपने उपास्य देवता से तादात्म्यभाव रखने में समर्थ हो जाता है, अद्वैतानन्द अमृतपाननिरत ब्रह्ममय हो जाता है, तब वह दिव्य कहा जाने लगता है। उसकी मानसिक अवस्था पूर्णतया सात्विक हो जाती है। उसमें दिव्यभाव का उदय हो जाता है। दिव्यभाव साधक ब्रह्मज्ञानी परमहंस पद प्राप्त करता है।
पण्डित देवदत्त शास्त्री
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.