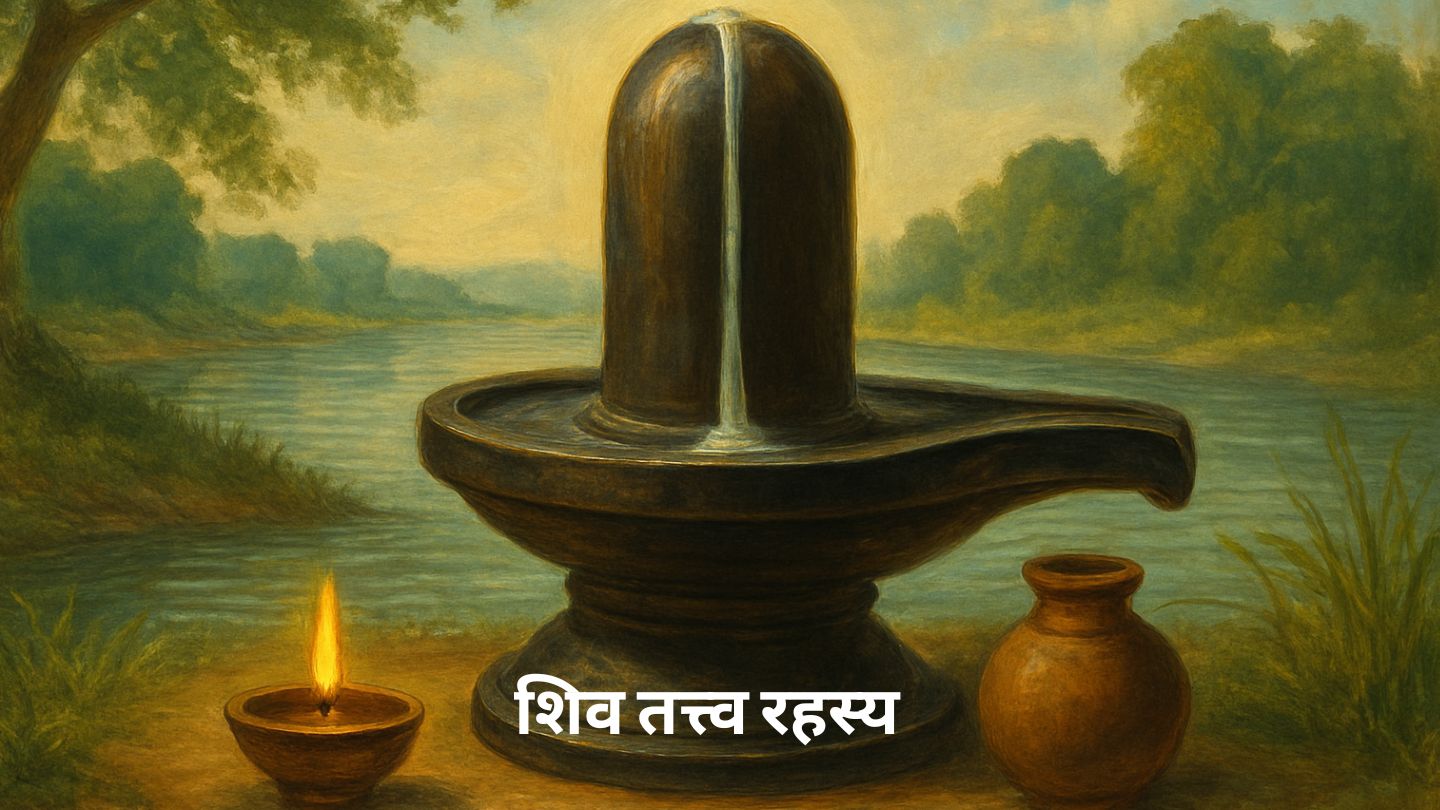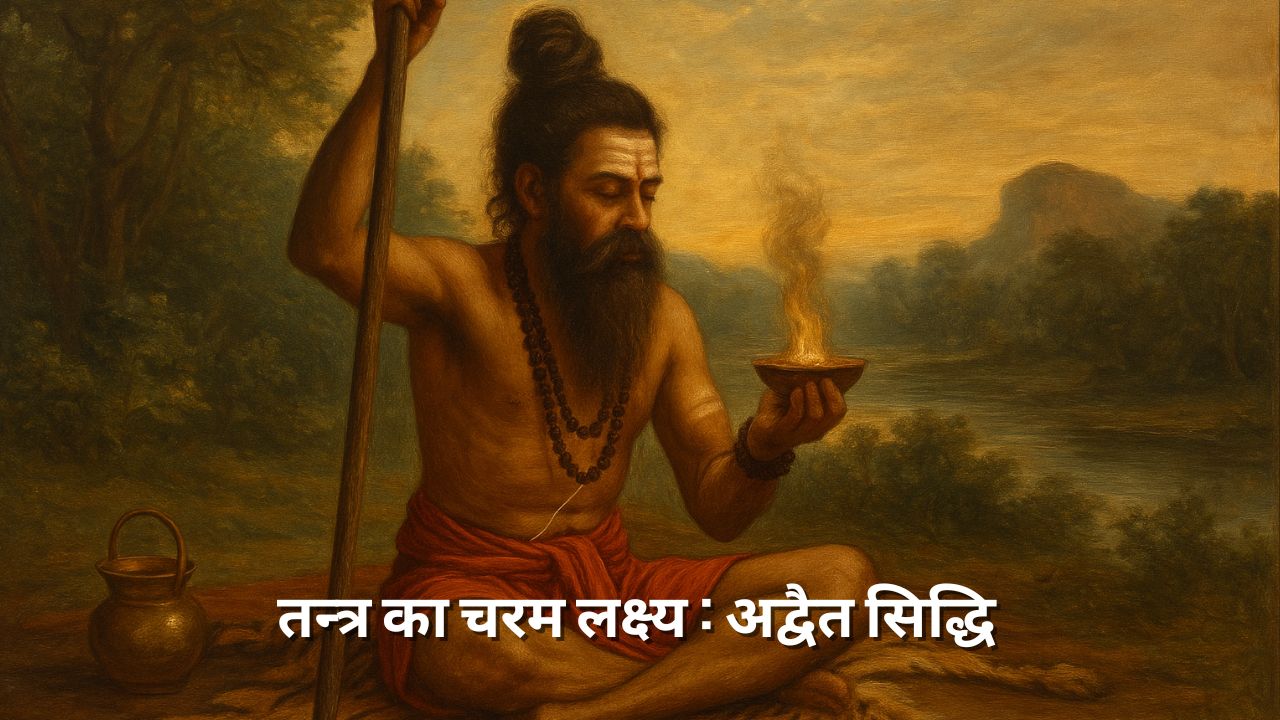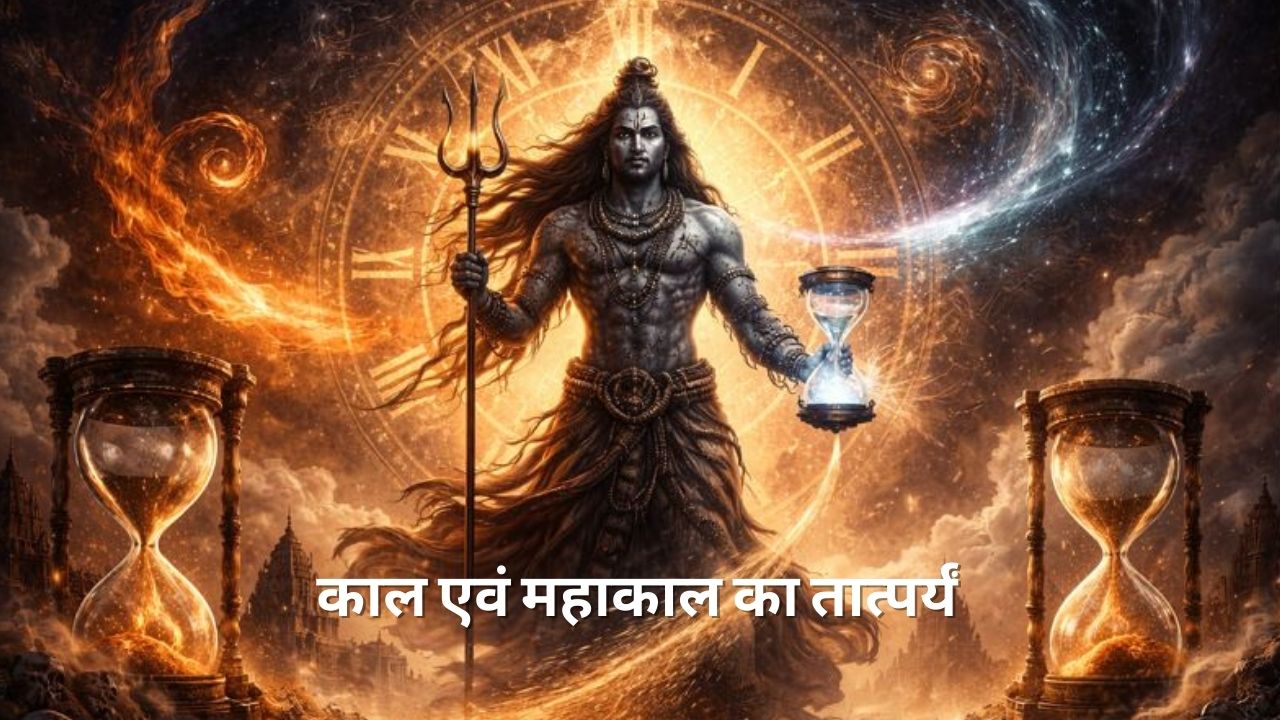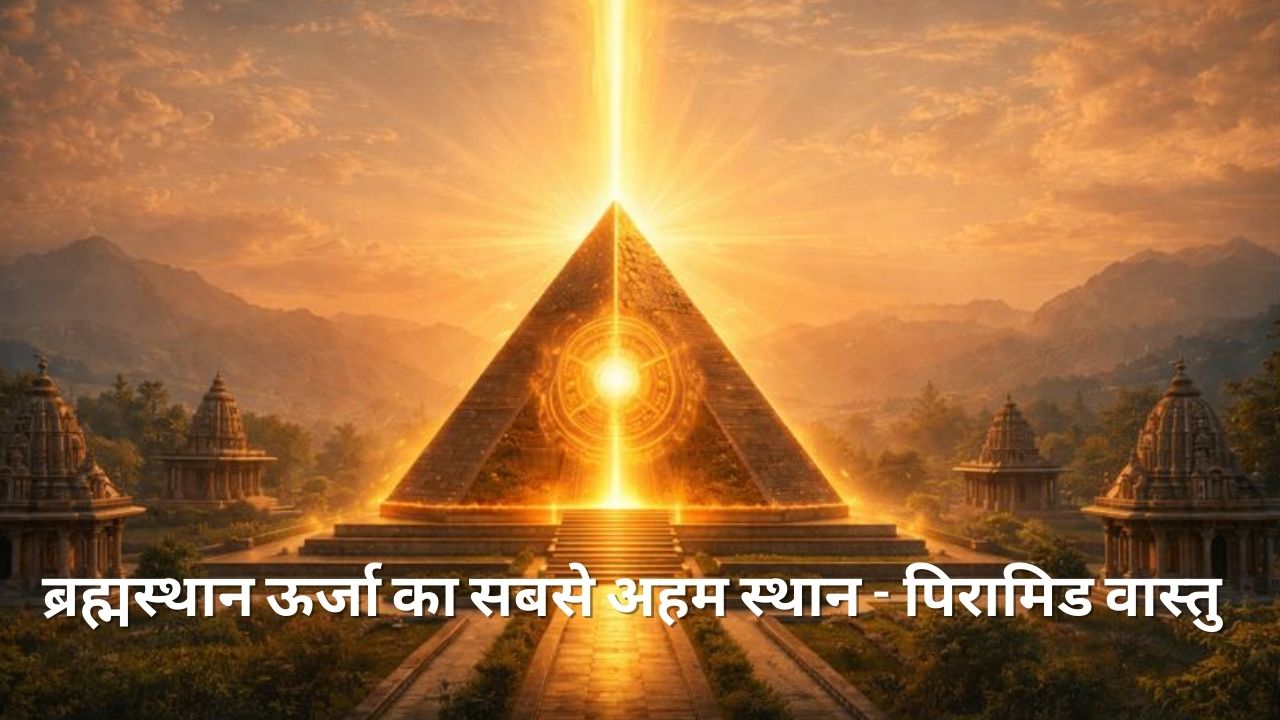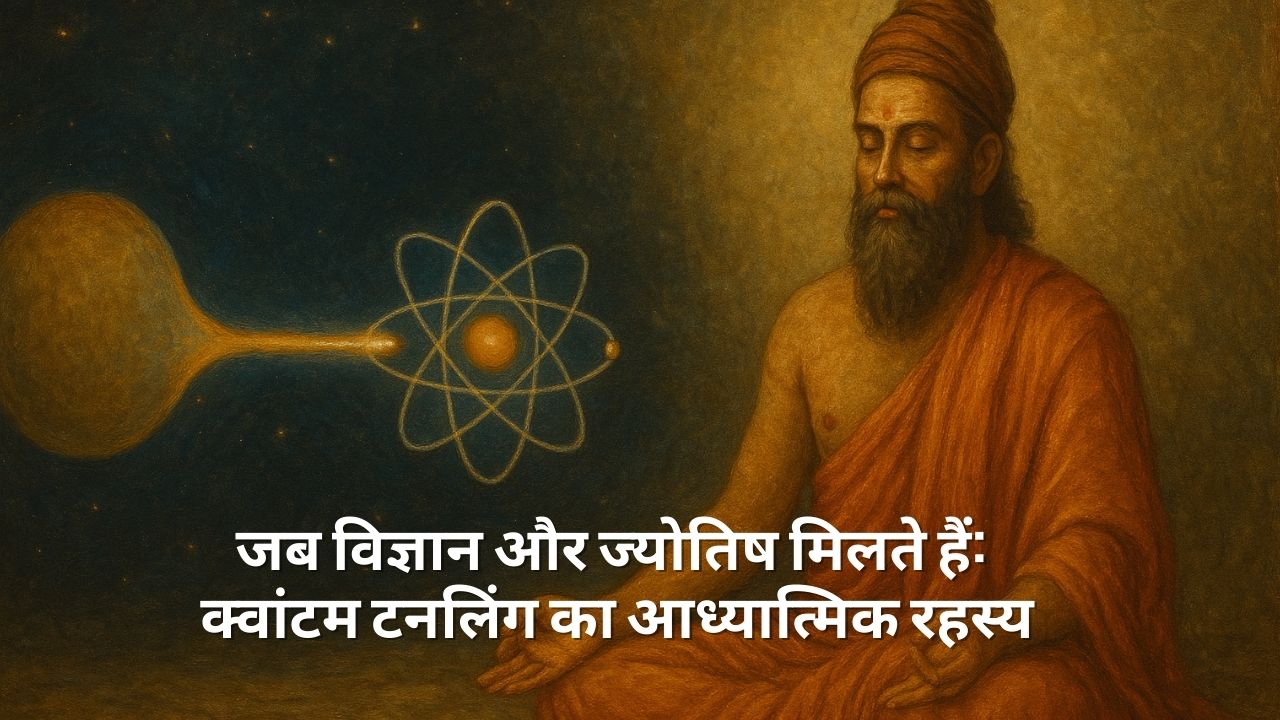- तंत्र शास्त्र
- |
- 31 March 2025
- |
- 1 Comments
डॉ. दीनदयाल मणि त्रिपाठी (प्रबंध संपादक )
तंत्र शब्द को लेकर भारतीय दर्शन एवं धर्म में अनेक भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसका मुख्य कारण है तन्त्र के रहस्य को न जानना। तंत्र का अर्थ है वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाये एवँ जो त्राण प्राप्ति में सहायक हो। वस्तुतः तंत्र में धर्म के साथ अर्थ और काम आदि मूल्यों का समन्वय करने का प्रयास किया गया है।
धर्म पारलौकिक सुख को महत्व देता है। यज्ञानुष्ठान आदि पारलौकिक सुख के निमित्त किये जाते हैं, जबकि तंत्र इहलौकिक सुख को प्राथमिकता देता है। धार्मिक व्यक्ति अपना सम्पूर्ण जीवन पारलौकिक सुखों की कामना करने एवं उसी के निमित्त अपने कर्मों का संचय करने में व्यतीत करता है, जबकि तंत्र का समर्थक स्वयं में देवत्व की अनुभूति करता हुआ इस पृथ्वी को स्वर्ग सदृश्य समझते हुए अपना बहुमूल्य जीवन व्यतीत करता है। तंत्र वेद का पूरक है। जो बात वेदों में सूक्ष्म रूप से कही गयी है। तंत्र उसे ही पूर्णरूप से प्रकाशित करता है। तंत्र का दूसरा नाम 'आगम' है। जिसमें भोग एवं मोक्ष दोनों समाहित है। वैदिक ग्रन्थों में वर्णित ज्ञान का क्रियात्मक रूप तंत्र का मुख्य विषय है। वृहदारण्यक आदि उपनिषदों में जो सूत्र मात्र सैद्धान्तिक रूप में वर्णित है, तंत्रों में इसे ही क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कर्म, उपासना और ज्ञान के स्वरूप को 'निगम' कहते हैं तथा इनके साधन भूत उपायों को 'आगम' या 'तंत्र' कहते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि तंत्र क्या हैं? इसका व्याख्यान इस प्रकार है- सांसारिक सकल कामनाओं के साधक चतुःषष्टि तंत्रों का प्रतिपादन कर देने के बाद पराम्बा भगवती पार्वती ने भूतभावन विश्वनाथ से पूछा- भगवन्! इन तंत्रों की साधना से जीव के आधि-व्याधि, शोक-संताप, दीन- हीनता आदि क्लेश तो दूर हो जाएगें, किन्तु गर्भवास और मरण के असह्य दुःखों की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपया इस दुःख की निवृत्ति एवं मोक्षरूप परमपद की प्राप्ति का कोई उपाय बतायें।
परिणामस्वरूप परम कल्याणमयी पुत्रवत्सला पराम्बा के साग्रह अनुरोध पर भगवान् शंकर ने इस श्रीविद्या साधना प्रणाली का प्राकट्य किया। इसी प्रसंग को आचार्य शंकर भगवत्पाद 'सौन्दर्य लहरी' में प्रकट करते हुए कहते हैं- पशुपतिभगवान् शंकर सिद्धिप्रद चौंसठ तंत्रों के द्वारा साधकों की जो स्वाभिमत सिद्धि है; उन सबका वर्णन करके विरत हो गये। पुनः आपके निर्बन्ध अर्थात् आग्रह पर उन्होंने सकल पुरुषार्थों अर्थात् धर्म, अर्थ, काम एवंमोक्ष को प्रदान करने वाले इस श्रीविद्या साधना तंत्र को प्राकट्य किया-
चतुःषष्टया तन्त्रैः सकलमतिसंधाय भुवनं स्थितस्तत्तत्स्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः । पुगस्त्वन्निर्बन्धादखिल पुरुषार्थेक घटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलभवातीतरदिदम् ।।
(सौन्दर्यलहरी)
श्रीविद्या साधना में परमराध्या, श्री ललिता महात्रिपुर सुन्दरी भगवती को परमतत्त्व के रूप में माना गया है। तत्रायं सिद्धान्तः - 'षटत्रिंशतत्त्वानि विश्वम्', 'शरीर कञ्चकितः शिवो जीवो निष्कञ्चकः परमः शिवः', 'स्वविमर्श-पुरुषार्थः', 'वर्मात्मका, नित्याः शब्दाः', 'मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता', सर्वसिद्धिः आदि श्रीपरशुराम कल्पसूत्र के इन सूत्रों में त्रैपुर सिद्धान्त का सारभूत संक्षिप्त ज्ञान भरा हुआ है।रामेश्वरवृत्ति में भी इसकी व्याख्या की गई है। सूत्रानुक्रम से वहीं पर श्रीचक्राधिष्ठात्री श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका महाषोडशी की उपासना के लिए क्रमपूर्वक पूजा पद्धति का विधान वर्णित है।
भारतीय आध्यात्मिक महार्णव से समुद्भूत षोडशकलापूर्ण सुधाकर के समान श्रीविद्या नाम समस्त आध्यात्मिक जगत् को आलोकित करता है। यही ब्रह्मविद्या है। 'परा विद्या' भी यही हैं इस विद्या की अधिष्ठात्री देवी संविदात्मिका महाशक्ति श्रीललिता। महात्रिपुरसुन्दरी है। इसकी उपासना का अपरिमित महत्त्व है। 'श्रीपरमशुराम कल्पूसत्र', 'योगिनी हृदय', 'त्रिपुररार्णव' तन्त्रराज आदि त्रैपुर सिद्धान्त के प्रमाणिक ग्रन्थ हैं। इसमें क्रमानुसार हेमोपादेयता से न्यूनाधिक्य रूप से स्थूल, सूक्ष्म और पर इस त्रिविध साधना का विधान वर्णित हैयोगिनीहृदय में परा, परापरा, अपरा पूजा के नाम से वर्णित है। अपरा स्थूलोपासना, परापरा सूक्ष्मोपासना, परपरा उपासना की विधि एवं महत्त्व का समीचीन प्रतिपादन है। भास्करराय अमृतानन्द योगी आदि श्रीविद्यानिष्णात आचार्यों की टीका से यह मणिकाञ्चन योग हो गया है।
त्रिपुरारहस्यम् के त्रिखण्ड (महात्मखण्ड, ज्ञानखण्ड, एवं चर्या खण्ड) में भगवती के महात्म्य एवं परमत्त्व की प्राप्ति के साधनों का विस्तृत वर्णन है। चर्याखण्ड अनुपलब्ध है
यह विद्या सभी मनोरचों को पूर्ण करने वाली है, तथा अभ्युदय और निःश्रेयस् प्रदान करने वाली है। इसमें इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों कल्याण निहित हैं। यह सभी विद्याओं में उत्तम है। अतः इसे श्रीविद्या कहते हैं। तांत्रिक साधना का चरमलक्ष्य अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति है। भगवान् आदि शंकराचार्य ने अद्वैतमत की स्थापना की और 'यावत् व्यवहारो न विरमेत', तावद् अद्वैतं नैव सिद्धेत को दृष्टिगत करके कराल कलिकाल में व्यवहार कीनिवृत्ति सुदर्लभ है। अतः व्यवहार में रहते हुए भी अद्वैत सिद्धि हो जाए, इसके लिये त्रैपुरसिद्धान्तसारसर्वस्व 'सौन्दर्य लहरी' स्तोत्र की रचना करके आगमपोसना का मार्ग प्रशस्त किया एवं अपने पाँच सन्यासी और नौगृहस्थ शिष्यों से प्रचार-प्रसार करवा के दिव्य समयाचार सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। इसका 'श्रीविद्यार्णव' में विस्तृत वर्णन है। शाक्तदर्शन में अद्वैत मत ही मुख्य है।
Related Posts
1 Comments