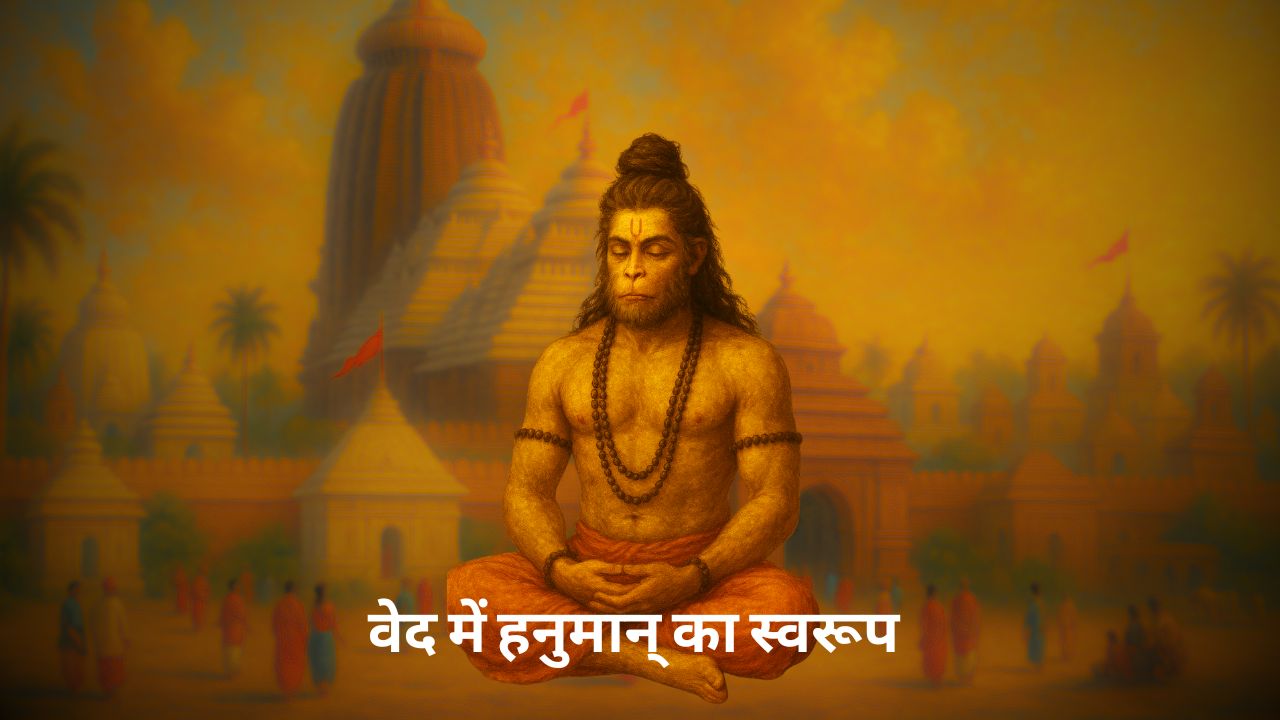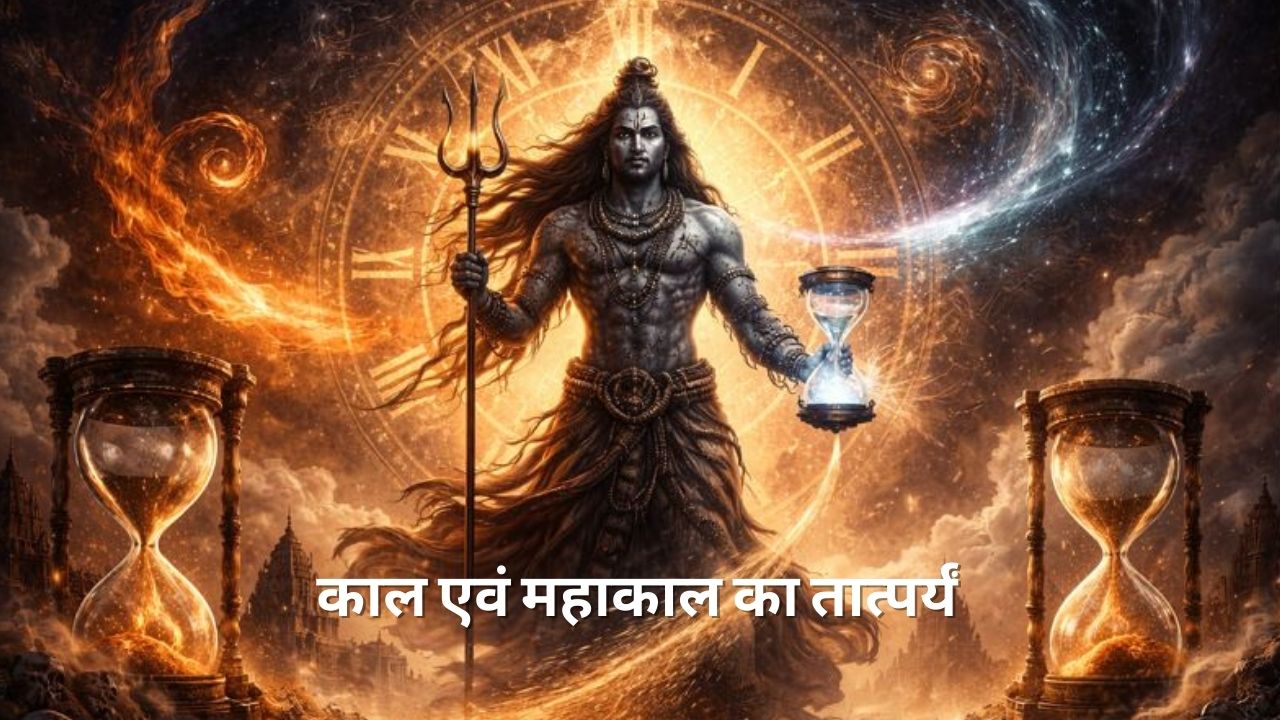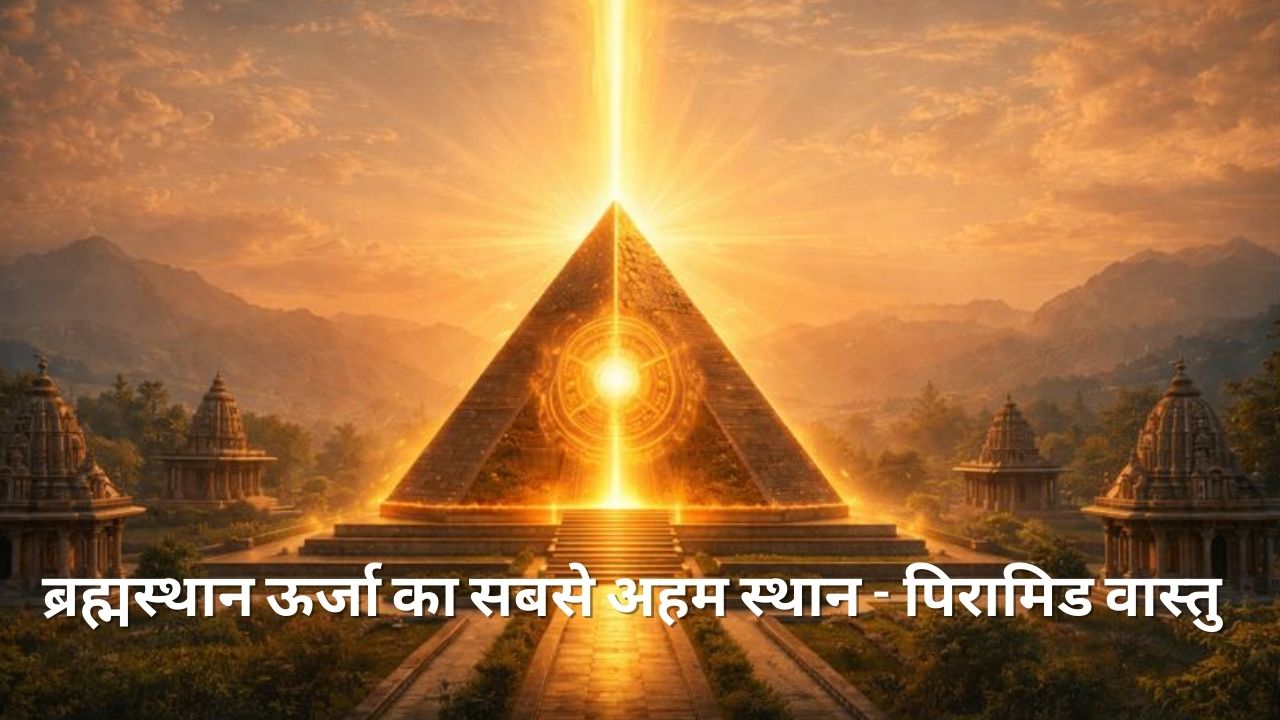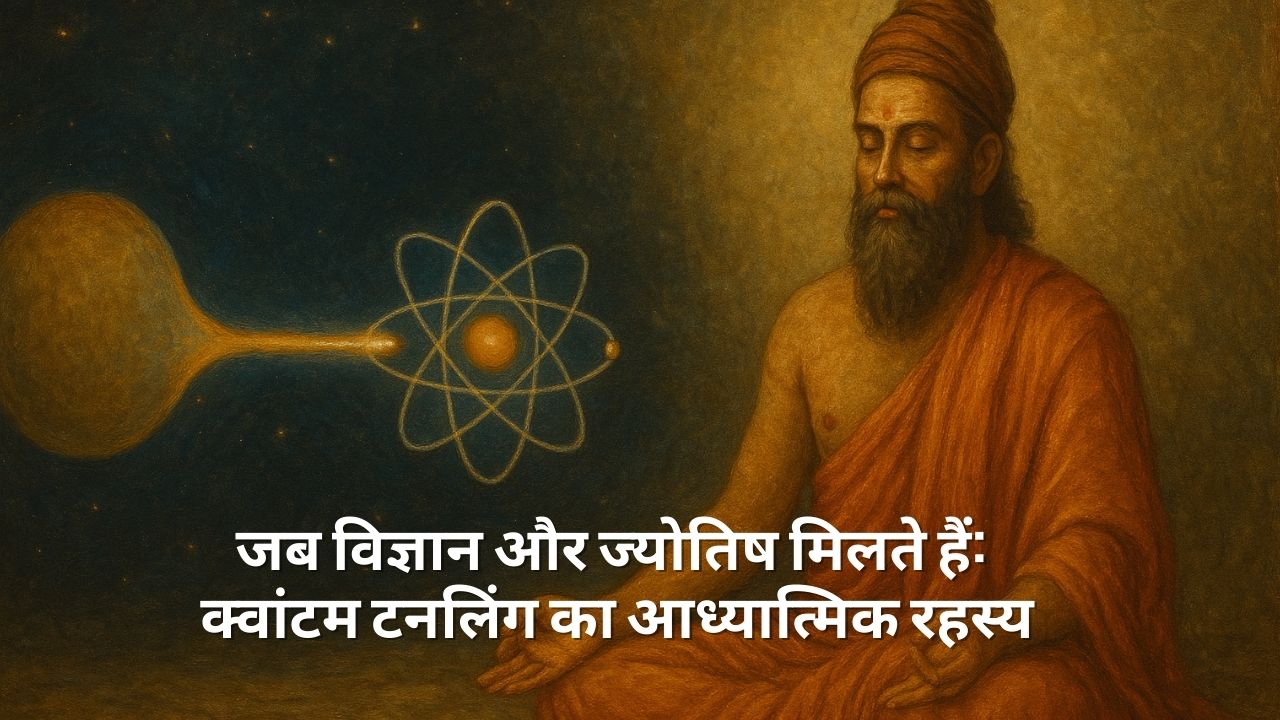- महापुरुष
- |
- 08 November 2025
- |
- 0 Comments
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
वैदिक वर्णन-वेद में तत्त्व रूप वर्णन हैं जिनके मूलतः आधिदैविक अर्थ हैं। इनका विस्तार आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक अर्थों में भी है। शब्द रचना मूलतः भौतिक पदार्थों के कर्म और गुण अनुसार हुई थी (मनुस्मृति, १/२१), उनके अर्थ का विस्तार आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रूपों में हुआ। इसे भागवत माहात्म्य में ज्ञान की वृद्धि कहा गया है और उस क्षेत्र को कर्णाटक (कर्ण द्वारा वेद या श्रुति का ग्रहण) कहा गया-उत्पन्ना द्रविड़े साऽहं वृद्धिं कर्णाटके गता (पद्म पुराण, उत्तर, १९३/४८)। वेद शब्दों की परिभाषा व्याख्या ब्राह्मण भाग में है। उनका भौतिक वर्णन इतिहास-पुराण में है-इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्॥२६७॥ बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति। (महाभारत, १/१)
https://mysticpower.in/dev-pujan/home.php
अतः तीनों को मिला कर पढ़ने से ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है।
जगन्नाथ के विषय में भी पाश्चात्य प्रचार था कि वे अशिक्षित वनवासियों के टोटेम (प्रतीक, देवता मानने से कष्ट होता है) थे, अतः उनकी मूर्त्ति के हाथ-पैर नहीं बनते (Gayacharan Tripathi, Hermann Kulke-Jagannath Cult)। इस दुष्प्रचार के लिए हरमन कुल्के को पद्मविभूषण मिला। बाद में और प्रचार होने लगा कि पूर्व तट ओड़िशा के प्रत्येक अंचल में जगन्नाथ की अलग अलग धारणा थी-जगन्नाथ को जगत् स्वरूप के बदले हर ग्राम का अलग स्वरूप करने का षड्यन्त्र। किन्तु भाषण देने के समय त्रिपाठी जी ने कहा कि जगन्नाथ परब्रह्म और वेद स्वरूप हैं (२००४ में दिल्ली में डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता में सम्मेलन)। मैंने कहा कि आप पुस्तक तथा लेखों में बिल्कुल उलटा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह मेरा विचार था, अब ठीक से लिखूंगा। पर वैसा लेख कभी नहीं लिखा जैसा भाषण करते थे, क्योंकि पाश्चात्य धारणा की प्रशंसा द्वारा पद लेना था। अधिकांश प्राध्यापक भाषण में वेद को अपौरुषेय, अनादि आदि कहते रहते हैं किन्तु पुस्तकों में लिखते हैं कि वैदिक युग १५०० ईपू में आरम्भ हुआ। अतः मैंने जगन्नाथ की वैदिक व्याख्या के लिए पुस्तक लिखी जिसका घोर विरोध हुआ। मैंने अन्तिम तर्क दिया कि स्वयं भगवान् कह रहे हैं कि वेद में उनका ही वर्णन है, आप कौन होते हैं उसका विरोधकरने वाले। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यं (गीता, १५/१५)।
विष्णु के जगन्नाथ या पुरुष रूप में जो कहा है, वही हनुमान् के वृषाकपि रूप विषय में भी है-
तत्र गत्त्वा जगन्नाथं वासुदेवं वृषाकपिम्।
पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिताः॥ (भागवत पुराण, १०/१/२०)
ततो विभुः प्रवर वराह रूपधृक् वृषाकपिः प्रसभमथैकदंष्ट्रया। (हरिवंश पुराण, ३/३४/४८)
शुक्ल यजुर्वेदीय तारसारोपनिषद् में हनुमान् का परब्रह्म रूप वर्णित है।
कल्याण के श्रीहनुमान अङ्क (१९७५) में कुछ लेख हनुमान के वेद वर्णन विषय में हैं। आरम्भ में हनुमान गायत्री सहित ऋक् (५/३/३,९/६९/१, ९/७१/२, ९/७२/५, १०/५/७) तथा साम (११/३/१/२) मन्त्र दिये हैं। स्वामी गंगेश्वरानन्द जी ने ऋग्वेद के कई मन्त्रों की हनुमान् चरित्र सम्बन्धित व्याख्या की है-ऋक (१/१२/१) में अग्नि अर्थात् अग्रि के दूत, विश्ववेदस (सर्वशास्त्रज्ञ), यज्ञ के सुक्रतु रूप में वर्णन है। ऋक् के प्रथम मन्त्र के चान्द्र भाष्य अनुसार अग्नि को वायुपुत्र हनुमान् तथा रत्न-धातम (राम की मुद्रिका, सीता की चूड़ामणि धारण करने वाले), पुरोहित (सबके आगे रह कर हित करने वाले), होतारं (लंका तथा असुरों को अग्नि और युद्ध में हवन करने वाले हैं। हनु भग्न होने का उल्लेख ऋक् (४/१७/९) में है। हनुमान् शब्द का हन्मन रूप वेद वर्णित है। ऋग्वेद में दूत शब्द ९० बार, हनू शब्द ४ बार तथा हन्मना शब्द ५ बार प्रयुक्त हुआ है। हनुमान् के लिए अपां-नपात् शब्द कई स्थानों पर है (ऋक् सूक्त २/३५, १/, ७, ९, १०, १३, १०/३०/३-४)। आकाश से वायु (तैत्तिरीय उपनिषद्, २/१), वायु से हनुमान् होने से वह आकाश या अन्तरिक्ष स्थित अप् के पौत्र (अपां-नपात्) हैं। ऋक् (२/३५/१०) में अपां-नपात् को कई प्रकार से हिरण्य रूप कहा है जिस रूप में हनुमान् की स्तुति है-अतुलितबलधामं हेमशैलाभ देहं। (रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, मंगलाचरण)
अशोभत मुखं तस्य जृम्भमाणस्य धीमतः।
अम्बरीषमिवादीप्तं विधूम इव पावकः॥ (रामायण, ४/६७/७)
ऋक् (१/१९) सूक्त के सभी ९ मन्त्रों के अन्त में ’मरुद्भिरग्न आ गहि’ कहा है। यहां मध्यम मरुत् स्थान् की अग्नि का अर्थ हनुमान् है।
स्वामी जी की व्याख्या के अतिरिक्त ऋक् (१/१९) के हर मन्त्र में में रामायण के हनुमत् चरित्र के कई घटनाओं का उल्लेख है तथा इसे हनुमान् सूक्त कहा जा सकता है-
(१) आक्रमण के समय जोर से हू शब्द करते हैं-प्र हूयसे। ननाद भीम निर्ह्रादो रक्षसां जनयन् भयम् (रामायण, ५/४३/१२)
(२) कोई देव या मर्त्य उनकी बराबरी नहीं कर सकता-नहि देवो न मर्त्यो महस्तव।
(३) सर्व शास्त्र जानने वाले-ये महो रजसो विदुः। - सर्वासु विद्यासु तपोनिधाने, प्रस्पर्धतेऽयं हि गुरुं सुराणाम्।
सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता, ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्॥ (वा. रामायण, ७/३६/४७)
(४) अजेय-अनाधृष्टास ओजसा।- न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलो भवेत् (रामायण, ५/४३/१०)
(५) प्रचण्ड तेजस्वी तथा असुर नाशक-ये शुभ्रा घोर वर्पसः, सुक्षत्रासो रिशादसः।
(६) स्वर्ग देव शिव अवतार-ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते।
(७) पर्वत ले जाने वाले (पर्वत से प्रहार, संजीवनी पर्वत उठा कर उड़ने वाले) तथा समुद्र पार करने वाले-य ईङ्खयन्ति पर्वतान्, तिरः समुद्रम् अर्णवम्।
(८) शरीर विस्तार से समुद्र जैसे-आ ये तन्वन्ति रश्मिभिः, तिरः समुद्र ओजसा।
(९) मधु सोम या लड्डू भोग-अभि त्वां पूर्व पीतये, सृजामि सोम्यं मधु।
इसके अतिरिक्त हनुमान के प्रणव रूप तथा नीलकण्ठ के मन्त्र रामायण में उल्लिखित हनुमत् चरित्र सम्बन्धी वेद मन्त्रों का संकलन कुछ लोगों ने किया है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.