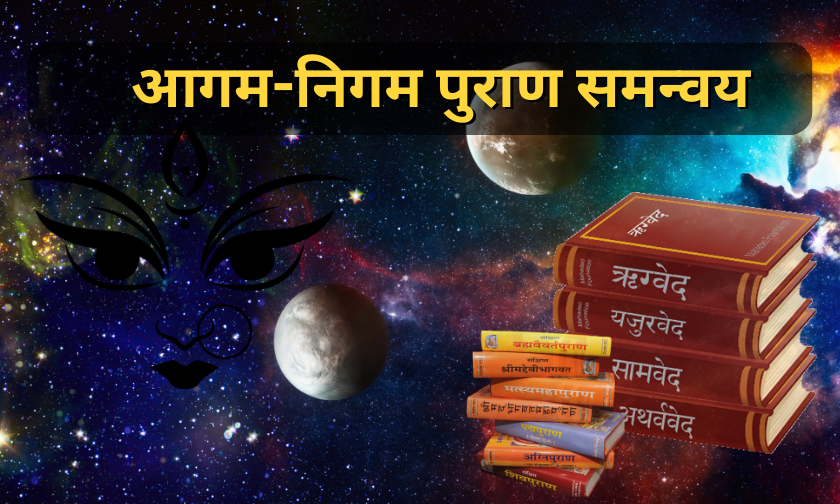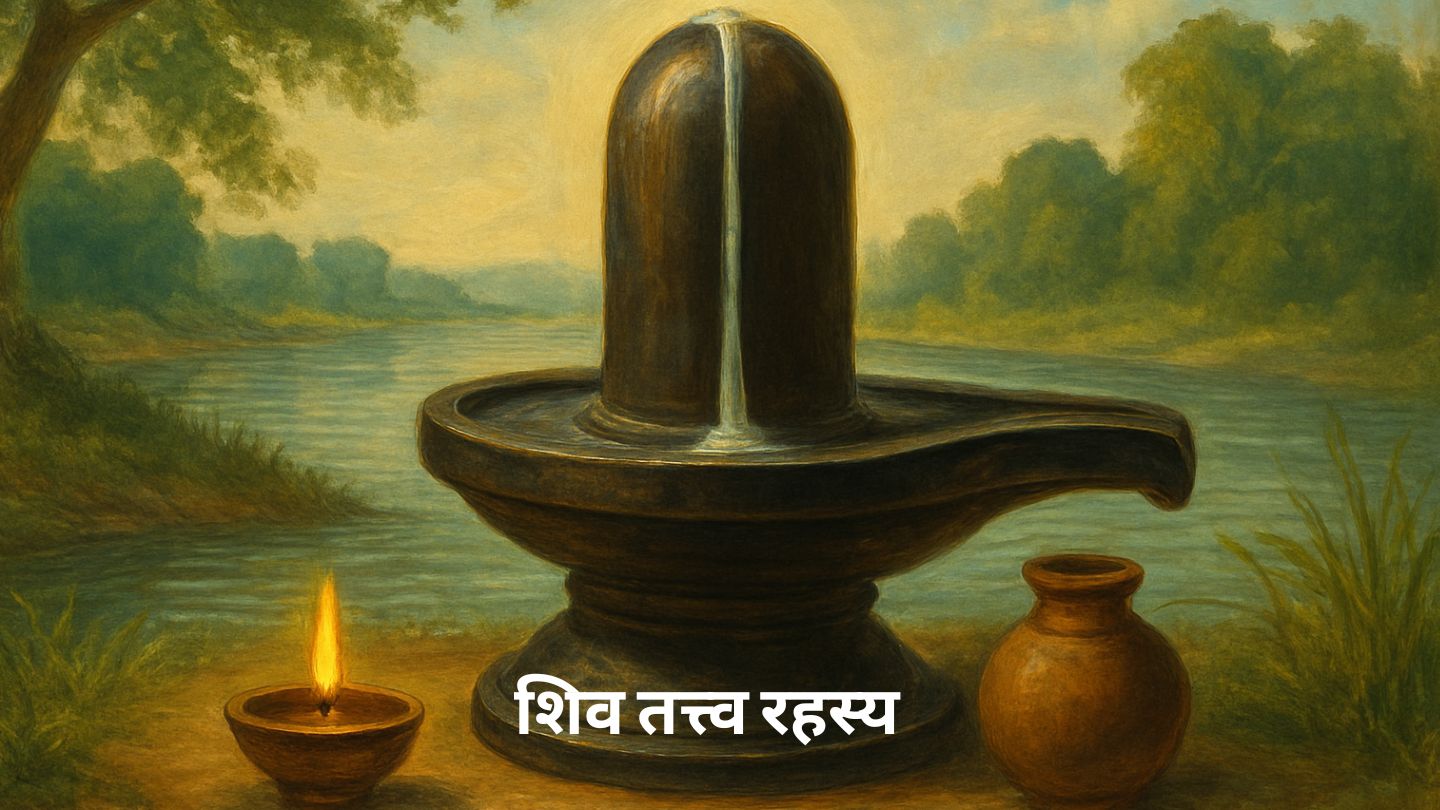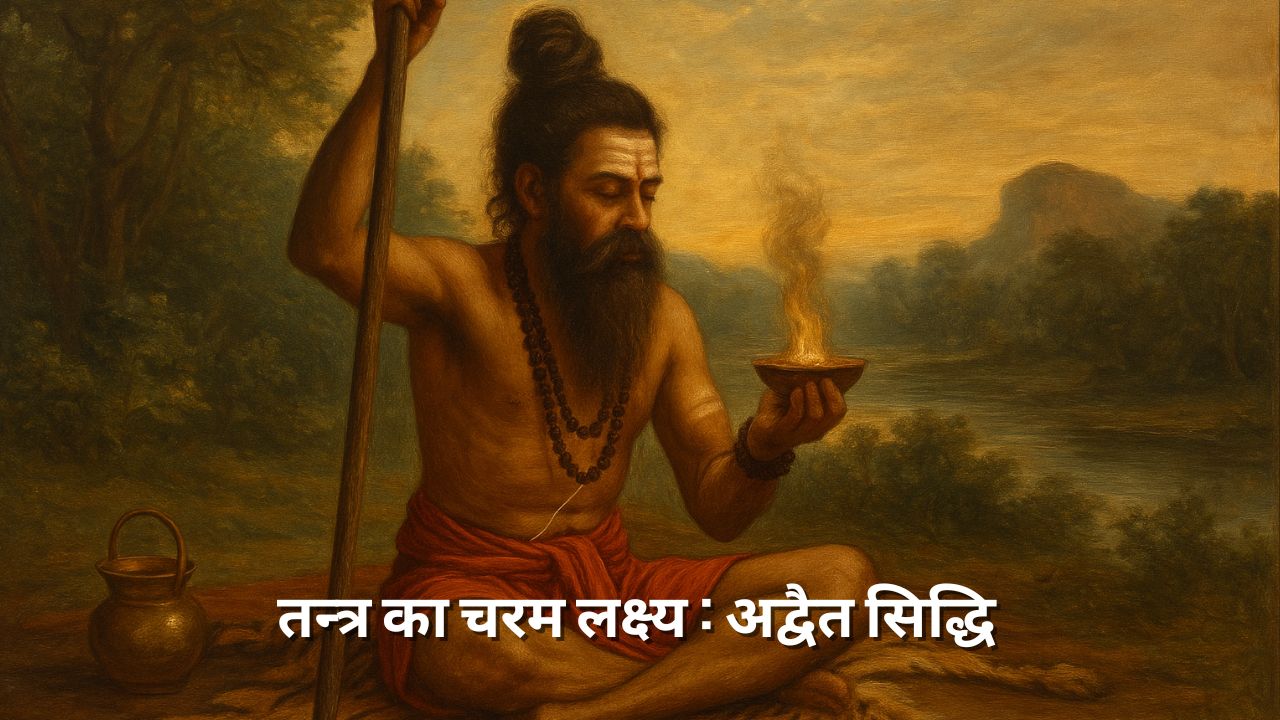- तंत्र शास्त्र
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
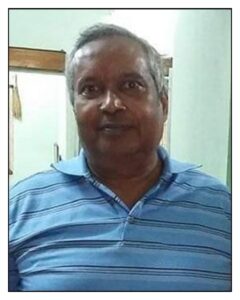 श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
Mystic Power- १. आगमों का पूरक रूप-आगम निगम पुराण इन तीनों को आदि काल से चले आने के कारण आगम कहते हैं।
(क) निसर्ग- या उससे प्राप्त ज्ञान का शब्द रूप को वेद कहते हैं। सृष्टि वेद को वेद पुरुष तथा उसका शब्द रूप में वर्णन शब्द या श्रीवेद है।
शब्दात्मिकां सुविमलर्ग्यजुषां निधानं, उद्गीथ रम्य पदपाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय, वार्ता समस्त जगतां परमार्ति हन्त्री॥ (चण्डी पाठ, ४/१०)
सृष्टि वेद- अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम् ॥(मनु स्मृति, १/२३)
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ )-
Mystic Power- १. आगमों का पूरक रूप-आगम निगम पुराण इन तीनों को आदि काल से चले आने के कारण आगम कहते हैं।
(क) निसर्ग- या उससे प्राप्त ज्ञान का शब्द रूप को वेद कहते हैं। सृष्टि वेद को वेद पुरुष तथा उसका शब्द रूप में वर्णन शब्द या श्रीवेद है।
शब्दात्मिकां सुविमलर्ग्यजुषां निधानं, उद्गीथ रम्य पदपाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय, वार्ता समस्त जगतां परमार्ति हन्त्री॥ (चण्डी पाठ, ४/१०)
सृष्टि वेद- अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम् ॥(मनु स्मृति, १/२३)
 चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भवच्चैव सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति ॥ (मनु स्मृति, १२/९७)
ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते ।
तमोमारेणैवायतेनान्येति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं च॥ (प्रश्नोपनिषत्, ५/७)
निसर्ग का ज्ञान श्रुति आदि ५ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिये इसे श्रुति कहते हैं। यह ३ अर्थों में अपौरुषेय है-
ऋषि द्वारा साम्यावस्था में ज्ञान, जब वह क्रोध, द्वेष आदि से मुक्त हो। निन्दा प्रवृत्ति रहने पर वेद ज्ञान सम्भव नहीं है।
विभिन्न देश-काल के कई ऋषियों के ज्ञान का संकलन।
५ ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त २ प्रकार के अतीन्द्रिय ज्ञान-परोरजा प्राण से (बृहदारण्यक उपनिषद्, ५/१४/७), असत् ऋषि प्राण (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/१) से।
(ख) पुराण- वेद एक काल का अनुभव है, परिवर्तन कब और कैसे हुआ इसे जानने के लिए कई बार अध्ययन की आवश्यकता है। पुराना कैसे और कितना नया हुआ इसका ज्ञान पुराण से होता है (पुरा + नवति, यास्क निरुक्त, ३/१९)
(ग) आगम या तन्त्र-इन ज्ञानों से व्यावहारिक कर्म कैसे करें, या विश्व की संस्थाओं का संचालन कैसे हो, उसे तन्त्र कहते हैं। आयुर्वेद के शालाक्य तन्त्र, राज्य में शासन तन्त्र, राज तन्त्र, अभिचार तन्त्र आदि।
प्राप्ति क्रम से ज्ञान के ३ स्तर हैं-श्रुति ज्ञान (वेद), अवधि ज्ञान (पुराण), केवल या अनन्त ज्ञान।
गीता के अनुसार-ज्ञान (अनन्त ज्ञान), ज्ञेय (जिसका प्रभाव या साम हम तक पहुंचता है, उसे ही जान सकते हैं), परिज्ञाता- ज्ञेय में भी अपनी क्षमता या साधन के अनुसार ही जान सकते हैं। (ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना-गीता, १८/१८)
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भवच्चैव सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति ॥ (मनु स्मृति, १२/९७)
ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते ।
तमोमारेणैवायतेनान्येति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं च॥ (प्रश्नोपनिषत्, ५/७)
निसर्ग का ज्ञान श्रुति आदि ५ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिये इसे श्रुति कहते हैं। यह ३ अर्थों में अपौरुषेय है-
ऋषि द्वारा साम्यावस्था में ज्ञान, जब वह क्रोध, द्वेष आदि से मुक्त हो। निन्दा प्रवृत्ति रहने पर वेद ज्ञान सम्भव नहीं है।
विभिन्न देश-काल के कई ऋषियों के ज्ञान का संकलन।
५ ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त २ प्रकार के अतीन्द्रिय ज्ञान-परोरजा प्राण से (बृहदारण्यक उपनिषद्, ५/१४/७), असत् ऋषि प्राण (शतपथ ब्राह्मण, ६/१/१/१) से।
(ख) पुराण- वेद एक काल का अनुभव है, परिवर्तन कब और कैसे हुआ इसे जानने के लिए कई बार अध्ययन की आवश्यकता है। पुराना कैसे और कितना नया हुआ इसका ज्ञान पुराण से होता है (पुरा + नवति, यास्क निरुक्त, ३/१९)
(ग) आगम या तन्त्र-इन ज्ञानों से व्यावहारिक कर्म कैसे करें, या विश्व की संस्थाओं का संचालन कैसे हो, उसे तन्त्र कहते हैं। आयुर्वेद के शालाक्य तन्त्र, राज्य में शासन तन्त्र, राज तन्त्र, अभिचार तन्त्र आदि।
प्राप्ति क्रम से ज्ञान के ३ स्तर हैं-श्रुति ज्ञान (वेद), अवधि ज्ञान (पुराण), केवल या अनन्त ज्ञान।
गीता के अनुसार-ज्ञान (अनन्त ज्ञान), ज्ञेय (जिसका प्रभाव या साम हम तक पहुंचता है, उसे ही जान सकते हैं), परिज्ञाता- ज्ञेय में भी अपनी क्षमता या साधन के अनुसार ही जान सकते हैं। (ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना-गीता, १८/१८)
 २. समन्वय से ज्ञान-ब्रह्म सूत्र चतुः सूत्री
(१) अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। (२) जन्माद्यस्य यतः, (३) शास्त्रयोनित्वात्, (४) तत् तु समन्वयात्।
वेद में कई ऋषियों के मत में भिन्नता दीखने के कारण उनमें समन्वय दिखाने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गयी।
मनुस्मृति में भी वेद में परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख है-
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्, तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ।
उभावपि हि तौ धर्मौ, सम्यगुक्तौ मनीषिभिः॥१४॥
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। (३ विचार)
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः॥१५॥
(मनुस्मृति, अध्याय, २)
वेद में मतान्तर-इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥ (ऋक्, १/१६४/४६, अथर्व, ९/१०/२८)
सत्य ३ या ७ प्रकार के हैं-
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः॥१॥ (अथर्व, शौनक संहिता)
सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः।
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। (पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, ३१/१५)
यही बात भागवत पुराण में है, जिसका खण्डन कर लोग वेद भक्ति दिखाते हैं-
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये।
सत्यस्य सत्यं ऋत-सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये॥ (भागवत पुराण, १०/२/२६)
३. वेद-पुराण की पूरकता-
(१) बिना इतिहास पुराण पढ़े वेद नहीं समझा जा सकता। पुराण नहीं जानने वाले से वेद भी डरता है कि वह मुझे समाप्त कर देगा।
इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्॥२६७॥ बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।
(महाभारत, १/१/२६७-६८)
स्वयं वेद में पुराण का उल्लेख है, क्योंकि उससे ही वेद समझा जा सकता है-
ऋच सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिता। (अथर्व, ११/७/२५)
(२) वेद में लोकों तथा धाम का उल्लेख है, उनकी माप केवल पुराणों में है। पुराणों की माप इकाई की व्याख्या जैन ग्रन्थों त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति तथा अनुयोगद्वार सूत्र में है। जैन ग्रन्थों के माप की परिभाषा यजुर्वेद (विशेष कर काण्व संहिता) में है।
(३) ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे सृष्टि करें। तब उन्होंने पुराण का स्मरण किया जिससे पता चला कि पूर्व कल्प में कैसे सृष्टि हुई थी। उसके अनुसार नये कल्प में भी वैसी ही सृष्टि की।
पुराणं सर्व शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥ (मत्स्य पुराण, ५३/३)
वेद में भी यही लिखा है कि पहले जैसी (यथापूर्वं) सृष्टि की गयी-
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वं अकल्पयत्। (ऋक्, १०/१९०/३)
(४) भगवद्दत्त जी ने भारतवर्ष का बृहत् इतिहास, खण्ड, १, पृष्ठ १८५ पर लिखा है-
"पं. विश्वबन्धु जी की भूल- वैदिक पदानुक्रम कोष में विश्वबन्धु जी ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के असुर सन्तान कायाधव प्रह्लाद का अर्थ कयाधु का पुत्र लिखा है। पुराण न जानने से ही विश्वबन्धु जी ने यह भूल की है। भागवत पुराण में लिखा है-
हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधूर्नाम दानवी (६/१८/१२)"
जो पुराण नहीं पढ़ने के साथ उसके विरोध करने के लिए अर्थ का अनर्थ कर उसे नैरुक्त प्रक्रिया कहता है, उसका कैसा ज्ञान होगा?
(५) वेद संहिता का रचना क्रम, ऋषियों का परिचय और उनका काल केवल पुराणों से ही पता चलता है। स्वायम्भुव मनु (२९१०० ईपू) से कृष्ण द्वैपायन व्यास (३२०० ईपू) तक २८ व्यासों ने वेद संहिता का संकलन किया। इनकी सूची कूर्म पुराण, अध्याय (१/५२), देवी भागवत (अध्याय १/२-३), ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/३५), लिंग पुराण (१/७/११, १/२४), वायु पुराण (१/२३/११६-२१८), विष्णु पुराण (३/३), शिव पुराण (अध्याय ३/४-६) में है।
ऋषभदेव ११वें व्यास थे, जिनका सूक्त ऋग्वेद (१०/१६६) है। स्पष्टतः उनके पूर्व व्यासों की संहिताओं में यह सूक्त सम्भव नहीं है। इसी प्रकार विश्वामित्र, वसिष्ठ, भरद्वाज, दीर्घतमा आदि अधिकांश ऋषि स्वायम्भुव मनु के समय नहीं थे। इनके सूक्त मूल वेद में नहीं हो सकते जो एक ही संहिता थी। इसका ४ वेद और ६ अंगों में विभाजन आंगिरस भरद्वाज ने किया (मुण्डक उपनिषद्, १/१/१-५)।
(६) दिवोदास आदि के वर्णन पूर्ण रूप में पुराणों में ही हैं, जिनसे आयुर्वेद इतिहास का भी पता चलता है।
(७) शब्द वेद सृष्टि के आरम्भ में नहीं था। सृष्टि का आरम्भ अनिश्चित है, यह स्वयं नासदीय सूक्त (ऋक्, १०/१२९/१-७) में कहा गया है, जहां १० अनुमान किये गये हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने वस्तुओं के नाम रखे (ऋक्, १०/७१/१-४, महाभारत, १२/२३२/२४-२६, मनुस्मृति, १/२१)। उसके बाद उनका अक्षर में विभाजन हुआ (ऐन्द्रवायव व्याकरण, तैत्तिरीय सं, ६/४/७, मैत्रायणी सं, ४/५/८)। उसके बाद माहेश्वर सूत्र से व्याकरण परम्परा आरम्भ हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत आदि द्वारा लोकों की माप हुई, पृथु आदि के समय खनिजों का दोहन हुआ। इनके बाद ही विज्ञान सम्मत वेद सूक्त का दर्शन और कथन सम्भव है। सृष्टि के आरम्भ में जब पृथ्वी या मनुष्य नहीं थे तब कौन मनुष्य ऋषि हुआ और भाषा के अभाव में कैसे सूक्त का दर्शन किया?
४. पुराण समझने के लिए वेद-
वेद में कोई सूक्त विषय क्रम से नहीं है। उनको व्यवस्थित रूप में पुराण से ही समझा जा सकता है। पुराण के भी कई ऐसे प्रसंग हैं जिनका वास्तविक अर्थ वेद से ही स्पष्ट होता है।
(१) रास नृत्य- इस नृत्य में एक केन्द्रीय व्यक्ति के चारों तरफ अन्य व्यक्ति नृत्य करते हैं। गरबा में भी इसी प्रकार वृत्त में लोग घूमते हैं। यह सृष्टि क्रिया के विभिन्न स्तरों का प्रतीक है। आकाश में ब्रह्माण्ड अपने केन्द्र के चारों तरफ घूम रहा है। उसके १०० अरब ताराओं में एक सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी आदि ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी का अक्ष भी चन्द्र तथा सूर्य आकर्षण से लट्टू की तरह घूम रहा है। इन गतियों का उल्लेख वेद में है तथा उनकी चक्र गति की माप पुराणों में है। पुराण में भी मूल रास का ब्रह्माण्ड में ही वर्णन है।
तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् .... दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः।
तदिन्द्राग्नी कृणुतां तद्विशाखे, तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम्।
नक्षत्राणां अधिपत्नी विशाखे, श्रेष्ठाविन्द्राग्नी भुवनस्य गोपौ॥११॥
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तात्, उन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय।
तस्यां देवा अधिसंवसन्तः, उत्तमे नाक इह मादयन्ताम्॥१२॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१/१)
= देव कामना पूर्ण करते हैं, इन्द्राग्नि (कृत्तिका) से विशाखा (नक्षत्रों की पत्नी) तक बढ़ते हैं। तब वे पूर्ण होते हैं, जो पूर्णमासी है। तब विपरीत गति आरम्भ होती है। यह गति नाक के चारो तरफ है।
इसे ब्रह्माण्ड पुराण में मन्वन्तर काल कहा है, जो इतिहास का मन्वन्तर है।
ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/९)-स वै स्वायम्भुवः पूर्वम् पुरुषो मनुरुच्यते॥३६॥ तस्यैक सप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥३७॥
ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/२९)-त्रीणि वर्ष शतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु। दिव्यः संवत्सरो ह्येष मानुषेण प्रकीर्त्तितः॥१६॥
त्रीणि वर्ष सहस्राणि मानुषाणि प्रमाणतः। त्रिंशदन्यानि वर्षाणि मतः सप्तर्षिवत्सरः॥१७॥
षड्विंशति सहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु। वर्षाणां युगं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः॥१९॥
पृथ्वी पर भी वार्षिक रास कार्त्तिक पूर्णिमा से आरम्भ होता है। यह ऋतु चक्र का वह समय है जब सभी समुद्री तूफान शान्त हो जाते हैं और समुद्री यात्रा आरम्भ हो सकती है। अतः सोमनाथ के समुद्र तट पर कार्त्तिकादि विक्रम सम्वत् का आरम्भ हुआ था।
देवी भागवत पुराण, स्कन्ध ९, अध्याय १-३ में सृष्टि प्रक्रिया के क्रमों के रूप में पार्वती (वेद वर्णित सृष्टि के ५ पर्व), महालक्ष्मी (दृश्य जगत्), सरस्वती (अदृश्य अप् या रस के स्तर), सावित्री (गायत्री माप अनुसार लोकों का क्रमशः बढ़ता आकार, विष्णु पुराण, २/७/३-४), राधा (५ तन्मात्रा रूप, ५ प्राणों की अधिष्ठात्री देवी), षडूर्वी या षष्ठी देवी (ऋक्, १०/१२८/२-५ आदि) का वर्णन है। षष्ठात् पञ्चाधिनिर्मिता (अथर्व, ८/९/४) = पञ्च-प्राणाधिदेवी के बाद षष्ठी निर्मिता। देवक्षेत्रं वै षष्टमहः (गोपथ ब्रा. उत्तर, ६/१०, ऐतरेय ब्रा, ५/९), पुरुष एव षष्टमहः (कौषीतकि ब्रा, २३/४)
वेद पुराण विरोधी इनको अश्लील नाच करने वाली कहते हैं।
(२) ब्रह्मा और सरस्वती-पुराणों का वर्णन अश्लील कह कर उसकी निन्दा की जाती है। ऋग्वेद (१०/६१/५-७) के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सहित सम्भोग किया। पुराणों से पता चलता है कि यह अश्लील नहीं है, बल्कि सृष्टि क्रिया है। प्रकृति ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई जिसमें ब्रह्म ने बीज वपन किया।
मम योनिर्महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्व भूतानां ततो भवति भारत॥३॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता॥४॥
(गीता, अध्याय १४)
पुराण में वर्णन-वामन पुराण (७१/२९-३६), गरुड़ पुराण (३/१६/८१-८२)-यहां सूर्य सिद्धान्त (१२/१२-१७) तथा पुरुष सूक्त क्रम के अनुसार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सृष्टि क्रम हैं, मनुष्यों के नाम नहीं। यह प्रसंग पुराण, शतपथ ब्राह्मण (२/१/२/६-१०), ऐतरेय ब्राह्मण (१३/९) को मिला कर स्पष्ट होता है।
(३) मृत्यु उपरान्त गति- इसको पौराणिक पाखण्ड कह कर गाली दी जाती है तथा श्राद्ध करने वाले को शव खाने वाला कहते हैं। गरुड़ (वेद का १, २, ३ सुपर्ण, गरुत्मान्, यजुर्वेद अध्याय १५ का मूर्धा वयः छन्द) आत्मा के वाहक हैं, जिनका लाक्षणिक रूप में गरुड़ पुराण में वर्णन है। पर उसकी विस्तृत व्याख्या अथर्व वेद, काण्ड १६ के ४ विस्तृत अध्यायों में ही है। उसमें सूक्ष्म आत्मा की गति को सूर्य किरण द्वारा कहा गया है। पृथ्वी कक्षा से बाहर की तरफ मंगल के २ उपग्रहों, अवान्तर ग्रह का वर्णन है। उसके बाद शनि वलय के ३ खण्डों को पीलुमती, उदन्वती, प्रद्यौ, कहा गया है (अथर्व, १८/२/४८)। सौर मण्डल से बाहर की गति के लिए गया श्राद्ध भी वेदों में ही वर्णित है।
(४) वेद सारांश को वेद विरुद्ध कहना- भागवत खण्डनम् (दयानन्द) में भागवत के प्रथम २ श्लोकों को वेद विरुद्ध और वेद निन्दा कहा गया है। स्पष्टतः यह वेद समझने की चेष्टा के बदले केवल निन्दा की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये श्लोक वेदों का सारांश कह रहे हैं। स्वयं वेद संकलन करने वाले कृष्ण द्वैपायन अपने प्रिय ग्रन्थ भागवत पुराण में वेद निन्दा कैसे कर सकते हैं?
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो ऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, सत्यं परं धीमहि॥१॥
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां,
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, ताप-त्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परैरीश्वरः,
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥२॥
निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।
पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥३॥
प्रथम मन्त्र का अर्थ-इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिस परमात्मा से है, जो कार्य प्रपञ्च में प्रविष्ट तथा उससे व्यतिरिक्त भी होने से स्वतः सिद्ध, सर्वज्ञ, स्वप्रकाश है; जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया, जिसमें विचारकुशल विद्वान् भी मोहित होते हैं; तेज, जल, मिट्टी का जैसे परस्पर विनिमय (आभास) होता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणात्मक जगत् सत्य जैसा दीखता है, अपने स्वरूप वैभव से माया को दूर हटाने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
ब्रह्म-सूत्र से समतुल्यता-
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (१/१/१) = निरस्त कुह कं सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य यतः (१/१/२)= वही है।
तत्तु समन्वयात् (१/१/४) = (अर्थेषु) अन्वयात्।
ईक्षतेर्नाशब्दम् (१/१/५) = अर्थेष्वभिज्ञः।
एतेन सर्वे व्याख्याता (१/४/२९) आदि समन्वय नामक प्रथम अध्याय = मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तदनन्यत्वमा रम्भणशब्दादिभ्यः (२/१/१४) सूचित द्वितीय अविरोध अध्याय = तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।
सह कार्यान्तर विधिः वक्षेण तद्वतो विध्यादिवत् (३/४/४७) सूचित तृतीय साधनाध्याय = सत्यं परं धीमहि।
परं जैमिनिर्मुख्यत्वात् (४/३/१२) सूचित चतुर्थ फलाध्याय = धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुह कं सत्यं परं।
गायत्री मन्त्र से समतुल्यता-
तत् सवितुः देवस्य = जन्माद्यस्य यतः।
भर्गो देवस्य = अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
धियो यो नः प्रचोदयात् = सत्यं परं धीमहि (ध्यायेम)
५. पुराण संकलन-२८ व्यासों ने वेदों के साथ पुराणों का भी संकलन किया था।
द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा। वेदमेकं स बहुधा कुरुते हित काम्यया॥१९॥
अल्पायुषोऽल्पबुद्धींश्च विप्राञ्ज्ञात्वा कलावथ। पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे॥२०॥
(देवीभागवत पुराण, १/३)-(यहां वेद और पुराण को सम्बन्धित या पूरक कहा है।)
महाभारत के बाद ज्ञान लुप्त होने के कारण वेद संकलन बन्द हो गया। किन्तु नैमिषारण्य में पुराण संकलन १००० वर्ष चला और उसके बाद विक्रमादित्य काल में बेताल भट्ट की अध्यक्षता में संकलन हुआ। अतः पुराणों में उत्तरायण आदि क्रम उसी काल का है तथा उसके पूर्व तक के राजाओं का ही वर्णन है।
नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः।
सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत॥ (भागवत पुराण, १/१/४)
कलौ सहस्रमब्दानामधुना प्रगतं द्विज। परीक्षितो जन्मकालात् समाप्तिं नीयतां मखः॥
(पद्म पुराण, उत्तर खण्ड, १९६/७२)
एवं द्वापरसन्ध्याया अन्ते सूतेन वर्णितम्। सूर्यचन्द्रान्वयाख्यानं तन्मया कथितम् तव॥१॥
विशालायां पुनर्गत्वा वैतालेन विनिर्मितम्। कथयिष्यति सूतस्तमितिहाससमुच्चयम्॥२॥
तन्मया कथितं सर्वं हृषीकोत्तम पुण्यदम्। पुनर्विक्रमभूपेन भविष्यति समाह्वयः॥३॥
नैमिषारण्यमासाद्य श्रावयिष्यति वै कथाम्। पुनरुक्तानि यान्येव पुराणाष्टादशानि वै।।४॥
तानि चोपपुराणानि भविष्यन्ति कलौ युगे। तेषां चोपपुराणानां द्वादशाध्यायमुत्तमम्॥५॥
(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व ४, अध्याय १)
हर शास्त्र में यही होता है। नयी खोज होने पर कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं। इतिहास में अधिक पुरानी घटनायें संक्षिप्त या लुप्त हो जाती हैं, नयी घटनाओं का विस्तार से वर्णन होता है। किन्तु पुराणों में या सूर्य सिद्धान्त आदि ज्योतिष ग्रन्थों में सृष्टि वर्णन महाभारत के बहुत पूर्व का है। महाभारत के बाद अमेरिका से कोई सम्पर्क नहीं था पर पुराण और ज्योतिष ग्रन्थों में अमेरिका तथा पश्चिम अफ्रीका के स्थानों के देशान्तर दिये हैं तथा आकाश के ग्रहों, गैलेक्सी आदि की सही माप दी है जो महाभारत के बाद सम्भव नहीं था।
२. समन्वय से ज्ञान-ब्रह्म सूत्र चतुः सूत्री
(१) अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। (२) जन्माद्यस्य यतः, (३) शास्त्रयोनित्वात्, (४) तत् तु समन्वयात्।
वेद में कई ऋषियों के मत में भिन्नता दीखने के कारण उनमें समन्वय दिखाने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गयी।
मनुस्मृति में भी वेद में परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख है-
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्, तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ।
उभावपि हि तौ धर्मौ, सम्यगुक्तौ मनीषिभिः॥१४॥
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। (३ विचार)
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः॥१५॥
(मनुस्मृति, अध्याय, २)
वेद में मतान्तर-इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥ (ऋक्, १/१६४/४६, अथर्व, ९/१०/२८)
सत्य ३ या ७ प्रकार के हैं-
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः॥१॥ (अथर्व, शौनक संहिता)
सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः।
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। (पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, ३१/१५)
यही बात भागवत पुराण में है, जिसका खण्डन कर लोग वेद भक्ति दिखाते हैं-
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये।
सत्यस्य सत्यं ऋत-सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये॥ (भागवत पुराण, १०/२/२६)
३. वेद-पुराण की पूरकता-
(१) बिना इतिहास पुराण पढ़े वेद नहीं समझा जा सकता। पुराण नहीं जानने वाले से वेद भी डरता है कि वह मुझे समाप्त कर देगा।
इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्॥२६७॥ बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।
(महाभारत, १/१/२६७-६८)
स्वयं वेद में पुराण का उल्लेख है, क्योंकि उससे ही वेद समझा जा सकता है-
ऋच सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिता। (अथर्व, ११/७/२५)
(२) वेद में लोकों तथा धाम का उल्लेख है, उनकी माप केवल पुराणों में है। पुराणों की माप इकाई की व्याख्या जैन ग्रन्थों त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति तथा अनुयोगद्वार सूत्र में है। जैन ग्रन्थों के माप की परिभाषा यजुर्वेद (विशेष कर काण्व संहिता) में है।
(३) ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे सृष्टि करें। तब उन्होंने पुराण का स्मरण किया जिससे पता चला कि पूर्व कल्प में कैसे सृष्टि हुई थी। उसके अनुसार नये कल्प में भी वैसी ही सृष्टि की।
पुराणं सर्व शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥ (मत्स्य पुराण, ५३/३)
वेद में भी यही लिखा है कि पहले जैसी (यथापूर्वं) सृष्टि की गयी-
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वं अकल्पयत्। (ऋक्, १०/१९०/३)
(४) भगवद्दत्त जी ने भारतवर्ष का बृहत् इतिहास, खण्ड, १, पृष्ठ १८५ पर लिखा है-
"पं. विश्वबन्धु जी की भूल- वैदिक पदानुक्रम कोष में विश्वबन्धु जी ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के असुर सन्तान कायाधव प्रह्लाद का अर्थ कयाधु का पुत्र लिखा है। पुराण न जानने से ही विश्वबन्धु जी ने यह भूल की है। भागवत पुराण में लिखा है-
हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधूर्नाम दानवी (६/१८/१२)"
जो पुराण नहीं पढ़ने के साथ उसके विरोध करने के लिए अर्थ का अनर्थ कर उसे नैरुक्त प्रक्रिया कहता है, उसका कैसा ज्ञान होगा?
(५) वेद संहिता का रचना क्रम, ऋषियों का परिचय और उनका काल केवल पुराणों से ही पता चलता है। स्वायम्भुव मनु (२९१०० ईपू) से कृष्ण द्वैपायन व्यास (३२०० ईपू) तक २८ व्यासों ने वेद संहिता का संकलन किया। इनकी सूची कूर्म पुराण, अध्याय (१/५२), देवी भागवत (अध्याय १/२-३), ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/३५), लिंग पुराण (१/७/११, १/२४), वायु पुराण (१/२३/११६-२१८), विष्णु पुराण (३/३), शिव पुराण (अध्याय ३/४-६) में है।
ऋषभदेव ११वें व्यास थे, जिनका सूक्त ऋग्वेद (१०/१६६) है। स्पष्टतः उनके पूर्व व्यासों की संहिताओं में यह सूक्त सम्भव नहीं है। इसी प्रकार विश्वामित्र, वसिष्ठ, भरद्वाज, दीर्घतमा आदि अधिकांश ऋषि स्वायम्भुव मनु के समय नहीं थे। इनके सूक्त मूल वेद में नहीं हो सकते जो एक ही संहिता थी। इसका ४ वेद और ६ अंगों में विभाजन आंगिरस भरद्वाज ने किया (मुण्डक उपनिषद्, १/१/१-५)।
(६) दिवोदास आदि के वर्णन पूर्ण रूप में पुराणों में ही हैं, जिनसे आयुर्वेद इतिहास का भी पता चलता है।
(७) शब्द वेद सृष्टि के आरम्भ में नहीं था। सृष्टि का आरम्भ अनिश्चित है, यह स्वयं नासदीय सूक्त (ऋक्, १०/१२९/१-७) में कहा गया है, जहां १० अनुमान किये गये हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने वस्तुओं के नाम रखे (ऋक्, १०/७१/१-४, महाभारत, १२/२३२/२४-२६, मनुस्मृति, १/२१)। उसके बाद उनका अक्षर में विभाजन हुआ (ऐन्द्रवायव व्याकरण, तैत्तिरीय सं, ६/४/७, मैत्रायणी सं, ४/५/८)। उसके बाद माहेश्वर सूत्र से व्याकरण परम्परा आरम्भ हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत आदि द्वारा लोकों की माप हुई, पृथु आदि के समय खनिजों का दोहन हुआ। इनके बाद ही विज्ञान सम्मत वेद सूक्त का दर्शन और कथन सम्भव है। सृष्टि के आरम्भ में जब पृथ्वी या मनुष्य नहीं थे तब कौन मनुष्य ऋषि हुआ और भाषा के अभाव में कैसे सूक्त का दर्शन किया?
४. पुराण समझने के लिए वेद-
वेद में कोई सूक्त विषय क्रम से नहीं है। उनको व्यवस्थित रूप में पुराण से ही समझा जा सकता है। पुराण के भी कई ऐसे प्रसंग हैं जिनका वास्तविक अर्थ वेद से ही स्पष्ट होता है।
(१) रास नृत्य- इस नृत्य में एक केन्द्रीय व्यक्ति के चारों तरफ अन्य व्यक्ति नृत्य करते हैं। गरबा में भी इसी प्रकार वृत्त में लोग घूमते हैं। यह सृष्टि क्रिया के विभिन्न स्तरों का प्रतीक है। आकाश में ब्रह्माण्ड अपने केन्द्र के चारों तरफ घूम रहा है। उसके १०० अरब ताराओं में एक सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी आदि ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी का अक्ष भी चन्द्र तथा सूर्य आकर्षण से लट्टू की तरह घूम रहा है। इन गतियों का उल्लेख वेद में है तथा उनकी चक्र गति की माप पुराणों में है। पुराण में भी मूल रास का ब्रह्माण्ड में ही वर्णन है।
तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् .... दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः।
तदिन्द्राग्नी कृणुतां तद्विशाखे, तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम्।
नक्षत्राणां अधिपत्नी विशाखे, श्रेष्ठाविन्द्राग्नी भुवनस्य गोपौ॥११॥
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तात्, उन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय।
तस्यां देवा अधिसंवसन्तः, उत्तमे नाक इह मादयन्ताम्॥१२॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१/१)
= देव कामना पूर्ण करते हैं, इन्द्राग्नि (कृत्तिका) से विशाखा (नक्षत्रों की पत्नी) तक बढ़ते हैं। तब वे पूर्ण होते हैं, जो पूर्णमासी है। तब विपरीत गति आरम्भ होती है। यह गति नाक के चारो तरफ है।
इसे ब्रह्माण्ड पुराण में मन्वन्तर काल कहा है, जो इतिहास का मन्वन्तर है।
ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/९)-स वै स्वायम्भुवः पूर्वम् पुरुषो मनुरुच्यते॥३६॥ तस्यैक सप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥३७॥
ब्रह्माण्ड पुराण (१/२/२९)-त्रीणि वर्ष शतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु। दिव्यः संवत्सरो ह्येष मानुषेण प्रकीर्त्तितः॥१६॥
त्रीणि वर्ष सहस्राणि मानुषाणि प्रमाणतः। त्रिंशदन्यानि वर्षाणि मतः सप्तर्षिवत्सरः॥१७॥
षड्विंशति सहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु। वर्षाणां युगं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः॥१९॥
पृथ्वी पर भी वार्षिक रास कार्त्तिक पूर्णिमा से आरम्भ होता है। यह ऋतु चक्र का वह समय है जब सभी समुद्री तूफान शान्त हो जाते हैं और समुद्री यात्रा आरम्भ हो सकती है। अतः सोमनाथ के समुद्र तट पर कार्त्तिकादि विक्रम सम्वत् का आरम्भ हुआ था।
देवी भागवत पुराण, स्कन्ध ९, अध्याय १-३ में सृष्टि प्रक्रिया के क्रमों के रूप में पार्वती (वेद वर्णित सृष्टि के ५ पर्व), महालक्ष्मी (दृश्य जगत्), सरस्वती (अदृश्य अप् या रस के स्तर), सावित्री (गायत्री माप अनुसार लोकों का क्रमशः बढ़ता आकार, विष्णु पुराण, २/७/३-४), राधा (५ तन्मात्रा रूप, ५ प्राणों की अधिष्ठात्री देवी), षडूर्वी या षष्ठी देवी (ऋक्, १०/१२८/२-५ आदि) का वर्णन है। षष्ठात् पञ्चाधिनिर्मिता (अथर्व, ८/९/४) = पञ्च-प्राणाधिदेवी के बाद षष्ठी निर्मिता। देवक्षेत्रं वै षष्टमहः (गोपथ ब्रा. उत्तर, ६/१०, ऐतरेय ब्रा, ५/९), पुरुष एव षष्टमहः (कौषीतकि ब्रा, २३/४)
वेद पुराण विरोधी इनको अश्लील नाच करने वाली कहते हैं।
(२) ब्रह्मा और सरस्वती-पुराणों का वर्णन अश्लील कह कर उसकी निन्दा की जाती है। ऋग्वेद (१०/६१/५-७) के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सहित सम्भोग किया। पुराणों से पता चलता है कि यह अश्लील नहीं है, बल्कि सृष्टि क्रिया है। प्रकृति ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई जिसमें ब्रह्म ने बीज वपन किया।
मम योनिर्महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्व भूतानां ततो भवति भारत॥३॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता॥४॥
(गीता, अध्याय १४)
पुराण में वर्णन-वामन पुराण (७१/२९-३६), गरुड़ पुराण (३/१६/८१-८२)-यहां सूर्य सिद्धान्त (१२/१२-१७) तथा पुरुष सूक्त क्रम के अनुसार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सृष्टि क्रम हैं, मनुष्यों के नाम नहीं। यह प्रसंग पुराण, शतपथ ब्राह्मण (२/१/२/६-१०), ऐतरेय ब्राह्मण (१३/९) को मिला कर स्पष्ट होता है।
(३) मृत्यु उपरान्त गति- इसको पौराणिक पाखण्ड कह कर गाली दी जाती है तथा श्राद्ध करने वाले को शव खाने वाला कहते हैं। गरुड़ (वेद का १, २, ३ सुपर्ण, गरुत्मान्, यजुर्वेद अध्याय १५ का मूर्धा वयः छन्द) आत्मा के वाहक हैं, जिनका लाक्षणिक रूप में गरुड़ पुराण में वर्णन है। पर उसकी विस्तृत व्याख्या अथर्व वेद, काण्ड १६ के ४ विस्तृत अध्यायों में ही है। उसमें सूक्ष्म आत्मा की गति को सूर्य किरण द्वारा कहा गया है। पृथ्वी कक्षा से बाहर की तरफ मंगल के २ उपग्रहों, अवान्तर ग्रह का वर्णन है। उसके बाद शनि वलय के ३ खण्डों को पीलुमती, उदन्वती, प्रद्यौ, कहा गया है (अथर्व, १८/२/४८)। सौर मण्डल से बाहर की गति के लिए गया श्राद्ध भी वेदों में ही वर्णित है।
(४) वेद सारांश को वेद विरुद्ध कहना- भागवत खण्डनम् (दयानन्द) में भागवत के प्रथम २ श्लोकों को वेद विरुद्ध और वेद निन्दा कहा गया है। स्पष्टतः यह वेद समझने की चेष्टा के बदले केवल निन्दा की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये श्लोक वेदों का सारांश कह रहे हैं। स्वयं वेद संकलन करने वाले कृष्ण द्वैपायन अपने प्रिय ग्रन्थ भागवत पुराण में वेद निन्दा कैसे कर सकते हैं?
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो ऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, सत्यं परं धीमहि॥१॥
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां,
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, ताप-त्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परैरीश्वरः,
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥२॥
निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।
पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥३॥
प्रथम मन्त्र का अर्थ-इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिस परमात्मा से है, जो कार्य प्रपञ्च में प्रविष्ट तथा उससे व्यतिरिक्त भी होने से स्वतः सिद्ध, सर्वज्ञ, स्वप्रकाश है; जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया, जिसमें विचारकुशल विद्वान् भी मोहित होते हैं; तेज, जल, मिट्टी का जैसे परस्पर विनिमय (आभास) होता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणात्मक जगत् सत्य जैसा दीखता है, अपने स्वरूप वैभव से माया को दूर हटाने वाले उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
ब्रह्म-सूत्र से समतुल्यता-
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (१/१/१) = निरस्त कुह कं सत्यं परं धीमहि।
जन्माद्यस्य यतः (१/१/२)= वही है।
तत्तु समन्वयात् (१/१/४) = (अर्थेषु) अन्वयात्।
ईक्षतेर्नाशब्दम् (१/१/५) = अर्थेष्वभिज्ञः।
एतेन सर्वे व्याख्याता (१/४/२९) आदि समन्वय नामक प्रथम अध्याय = मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तदनन्यत्वमा रम्भणशब्दादिभ्यः (२/१/१४) सूचित द्वितीय अविरोध अध्याय = तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।
सह कार्यान्तर विधिः वक्षेण तद्वतो विध्यादिवत् (३/४/४७) सूचित तृतीय साधनाध्याय = सत्यं परं धीमहि।
परं जैमिनिर्मुख्यत्वात् (४/३/१२) सूचित चतुर्थ फलाध्याय = धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुह कं सत्यं परं।
गायत्री मन्त्र से समतुल्यता-
तत् सवितुः देवस्य = जन्माद्यस्य यतः।
भर्गो देवस्य = अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
धियो यो नः प्रचोदयात् = सत्यं परं धीमहि (ध्यायेम)
५. पुराण संकलन-२८ व्यासों ने वेदों के साथ पुराणों का भी संकलन किया था।
द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा। वेदमेकं स बहुधा कुरुते हित काम्यया॥१९॥
अल्पायुषोऽल्पबुद्धींश्च विप्राञ्ज्ञात्वा कलावथ। पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे॥२०॥
(देवीभागवत पुराण, १/३)-(यहां वेद और पुराण को सम्बन्धित या पूरक कहा है।)
महाभारत के बाद ज्ञान लुप्त होने के कारण वेद संकलन बन्द हो गया। किन्तु नैमिषारण्य में पुराण संकलन १००० वर्ष चला और उसके बाद विक्रमादित्य काल में बेताल भट्ट की अध्यक्षता में संकलन हुआ। अतः पुराणों में उत्तरायण आदि क्रम उसी काल का है तथा उसके पूर्व तक के राजाओं का ही वर्णन है।
नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः।
सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत॥ (भागवत पुराण, १/१/४)
कलौ सहस्रमब्दानामधुना प्रगतं द्विज। परीक्षितो जन्मकालात् समाप्तिं नीयतां मखः॥
(पद्म पुराण, उत्तर खण्ड, १९६/७२)
एवं द्वापरसन्ध्याया अन्ते सूतेन वर्णितम्। सूर्यचन्द्रान्वयाख्यानं तन्मया कथितम् तव॥१॥
विशालायां पुनर्गत्वा वैतालेन विनिर्मितम्। कथयिष्यति सूतस्तमितिहाससमुच्चयम्॥२॥
तन्मया कथितं सर्वं हृषीकोत्तम पुण्यदम्। पुनर्विक्रमभूपेन भविष्यति समाह्वयः॥३॥
नैमिषारण्यमासाद्य श्रावयिष्यति वै कथाम्। पुनरुक्तानि यान्येव पुराणाष्टादशानि वै।।४॥
तानि चोपपुराणानि भविष्यन्ति कलौ युगे। तेषां चोपपुराणानां द्वादशाध्यायमुत्तमम्॥५॥
(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व ४, अध्याय १)
हर शास्त्र में यही होता है। नयी खोज होने पर कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं। इतिहास में अधिक पुरानी घटनायें संक्षिप्त या लुप्त हो जाती हैं, नयी घटनाओं का विस्तार से वर्णन होता है। किन्तु पुराणों में या सूर्य सिद्धान्त आदि ज्योतिष ग्रन्थों में सृष्टि वर्णन महाभारत के बहुत पूर्व का है। महाभारत के बाद अमेरिका से कोई सम्पर्क नहीं था पर पुराण और ज्योतिष ग्रन्थों में अमेरिका तथा पश्चिम अफ्रीका के स्थानों के देशान्तर दिये हैं तथा आकाश के ग्रहों, गैलेक्सी आदि की सही माप दी है जो महाभारत के बाद सम्भव नहीं था।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.