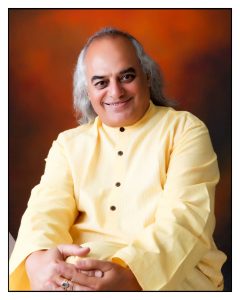- ज्योतिष विज्ञान
- |
-
31 October 2024
- |
- 0 Comments
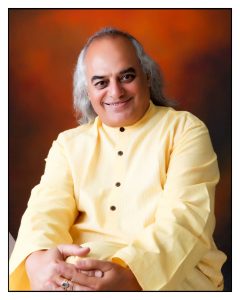
डॉ. अजय भांबी- महर्षि पतंजलि ने अपने विशिष्ट ग्रंथ पतंजलि योगसूत्र-योगदर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया है। वे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के अभ्यास से आत्मा अपने पड़ाव के दौरान जिन अशुद्धियों को अज्ञानवश जमा कर लेती है उनसे वह मुक्त हो जाती है, अंधकार के बादल छंट जाते हैं, आलोक फैल जाता है, ज्ञानोदय हो जाता है और आत्मा ज्ञान से आलोकित हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा को विश्व के साथ एकाकार होने का अनुभव होने लगता है और मनुष्य जिसके भीतर आत्मा निवास करती है, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों और उन तमाम गतिविधियों के बारे में सचेत हो जाता है जिनके कारण वह पदार्थ या प्रकृति का अंग बना होता है। अष्टांग योग के अभ्यास से मनुष्य का अज्ञान मिट जाता है और वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अंत में मात्र सत्य, प्रकाश या ज्ञान ही शेष रहता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी चेतना का अनुभव करने लगता है और शुद्ध हो जाता है और इसी शुद्धता से वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यहाँ पतंजलि के अष्टांग योग का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है:
https://mysticpower.in/ashparsh-yog/
यम
यम अष्टांग योग का पहला अंग है, जिसमें पतंजलि बताते हैं कि मनुष्य को बाहरी प्रभाव से अपने-आपको मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। वे आगे बताते हैं कि जैसे-जैसे मनुष्य का आचरण शुद्ध होता जाता है उसका मन भी शुद्ध होता चला जाता है और वह अच्छे मूल्यों को प्राप्त करने लगता है।
यम पाँच प्रकार के हैं:
अहिंसा : अहिंसा को कई तरीकों से बताया जा सकता है, लेकिन पतंजलि इसकी व्याख्या बिल्कल ही अलग तरीके से करते हैं। उनका कहना है कि किसी की हत्या न करनामात्र ही अहिंसा नहीं है, बल्कि मन में हत्या का विचार आना या वाणी से उसका उच्चारण भी हिंसा ही है। इसलिए साधक को इस स्तर पर पहुँचने के लिए प्रयास करना होगा।
सत्य : योगी को सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपनी इंद्रियों या मन से वह जो कुछ भी देखता, सुनता या अनुभव करता है, उसमें सत्य प्रतिबिम्बित होना चाहिए। यदि सत्य अप्रिय है या इससे कोई आहत होता है तो उसे संयम से काम लेना होगा और मौन का पालन करना होगा। उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे लोग अविधा महसूस करने लगे और उसके काम भी हिंसक नहीं होने चाहिए।
अस्तेय अर्थात् चोरी न करना : अस्तेय की व्याख्या करते हए पतंजलि कहते हैं कि किसी के माल को हड़पने के लिए किसी भी प्रकार का धोखा, कपट या बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भी चोरी है। जो कुछ कानूनी तौर पर आपका नहीं है, उसे हासिल करना भी चोरी है। उदाहरण के लिए रिश्वत लेना, निधि का दुरुपयोग करना, टैक्स की चोरी करना या गलत बिलिंग भी चोरी है।
ब्रह्मचर्य : ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से बना है। ब्रह्म और चर्य, अर्थात् ब्रह्म का आचरण करना या शुद्धता के पथ पर चलना। ब्रह्मचर्य का एक और अर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और विचारों और वाणी में भी इसका पालन करना। अष्टांग योग का पालन करते हुए शारीरिक संसर्ग से भी बचना, क्योंकि परमात्मा के साथ एकाकार होने की यात्रा में यह बाधक बन सकता है।
अपरिग्रह : साधक या योगी को शुद्धता के पथ पर चलना चाहिए और शुद्ध जीवन ही बिताना चाहिए। उसे किसी अन्य व्यक्ति से केवल उतना ही लेना चाहिए जिसकी उस। जरूरत हो। उससे अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसका मन एकाग्रता से भटक जाता है।
जब साधक इनका आचरण करता है तो वह अपने-आपको बाहरी प्रभावों से मुक्त कर लेता है और साधना के पथ पर अग्रसर होने लगता है।
नियम : नियम या शौच अष्टांग योग का दूसरा अंग है। नियम के अंतर्गत योगी को पाँच कर्तव्यों का पालन करना होता है। ये हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान।
शौच : हर साधक को तन, मन और वाणी से शुद्धता और शौच का पालन करना चाहिए। ये नियम हैं: शरीर, कपड़े, घर, धनार्जन के तरीकों और रसोई व खान-पान में भी शौच अर्थात् सफ़ाई का ध्यान करना चाहिए। नियमों के अंतर्गत तो यह भी व्यवस्था है कि आपसी लेन-देन में भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। साधक को विचारों में भी शुद्धता रखनी चाहिए और दूसरों के साथ व्यवहार भी मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साधक को राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। ये सभी नकारात्मक उद्वेग या आतंरिक मलिनताएँ हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए। संस्कृत में इसे शौच कहते हैं।
संतोष : दसरा नियम है, संतोष। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि साधक को पूरे संतोष के साथ अपनी चादर के अंदर ही रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद हर हाल में साधक को संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अंधाधुंध अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए और साथ ही उन्हें सीमाओं के भीतर ही रखना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए। कामना या तृष्णा के लिए कोई गंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दूसरों के माल पर नज़र नहीं डालनी चाहिए और अपनी संपत्ति से संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष का पालन करने से इच्छाएँ शांत हो जाती हैं।
तप : तप का अर्थ है आत्मशुद्धि। तप का पालन करने से योगी अपनी गंदगी से छुटकारा पा लेता है और सूक्ष्म स्तर पर उसका शरीर पवित्र हो जाता है। मन शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं का नियामक हो जाता है। मन बेचैन हो तो उसका परिणाम मनुष्य की क्रियाओं और इंद्रियों पर दिखाई पड़ने लगता है। यदि मन स्थिर हो जाए तो शरीर और इंद्रियाँ भी शांत हो जाती हैं। जब योगी तप करता है तो उसकी प्रतिक्रिया मन पर होती है और शरीर और इंद्रियों के स्तर पर कष्ट अनुभव करता है। इन कष्टों को सहना ही तप कहलाता है। पतंजलि के अनुसार, तप यदि स्वाभाविक रूप में होगा तभी मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई साधक शरीर और इंद्रियों की परवाह किये बिना तप के मार्ग पर चलता है तभी कुछ अलग ढंग से उसका शरीर शुद्ध होता जाएगा। यही कारण है कि योगी के शरीर का अनुपात सही होता है, वह स्वस्थ रहता है, साफ़-सुथरा रहता है और उसमें खास तरह की चमक होती है।योग साधना करते हए साधक तन और मन को शद्ध कर सकता है; शरीर के सभी विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। इन सभी कष्टों को शांति से सहने की क्रिया को ही तप कहा जाता है। इसका पालन करने से इंद्रियाँ और शरीर नियंत्रण में रहते हैं और योगी नई ऊँचाइयों पर पहुँच जाता है।
स्वाध्याय : यह चौथा नियम है। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है पाठ का ज्ञान, स्वयं को जानना और मंत्रपाठ करना. जप करना, मंत्रोच्चार करना और ईश्वर और देवी-देवताओं का स्मरण करना। इनका निरंतर पालन करने से योगी अपने ईश्वर और देवी-देवताओं की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है, जो उसे मुक्ति के पथ पर ले जाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। यद्यपि मुक्ति का अनुभव स्वतः अर्जित अनुभव होता है, लेकिन गुरू या ईश्वर की मदद से आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ईश्वर के साथ निकटता का अनुभव करते हए योगी अपने मार्ग पर और भी उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। सभी साधकों, भक्तों और योगियों को आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ईश्वर की मदद की ज़रूरत पड़ती है।
https://mysticpower.in/ashparsh-yog/
ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वर के प्रति समर्पण : यह पाँचवाँ नियम है। इसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात की गई है और इसके बदले में ईश्वर साधक को पूरी तरह अपनी शरण में ले लेता है। जब कोई साधक बिना किसी कामना के अपने आपको ईश्वर के प्रति पूर्णत: समर्पित कर देता है तो वह समाधि के लिए पात्र हो जाता है। समाधि की अवस्था में योगी इच्छाओं के बीज को नष्ट कर देता है और वह निर्बीज समाधि में पहुँच जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण यम और नियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।