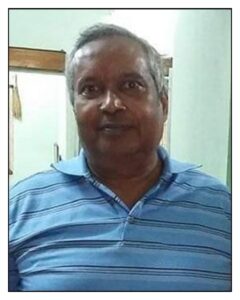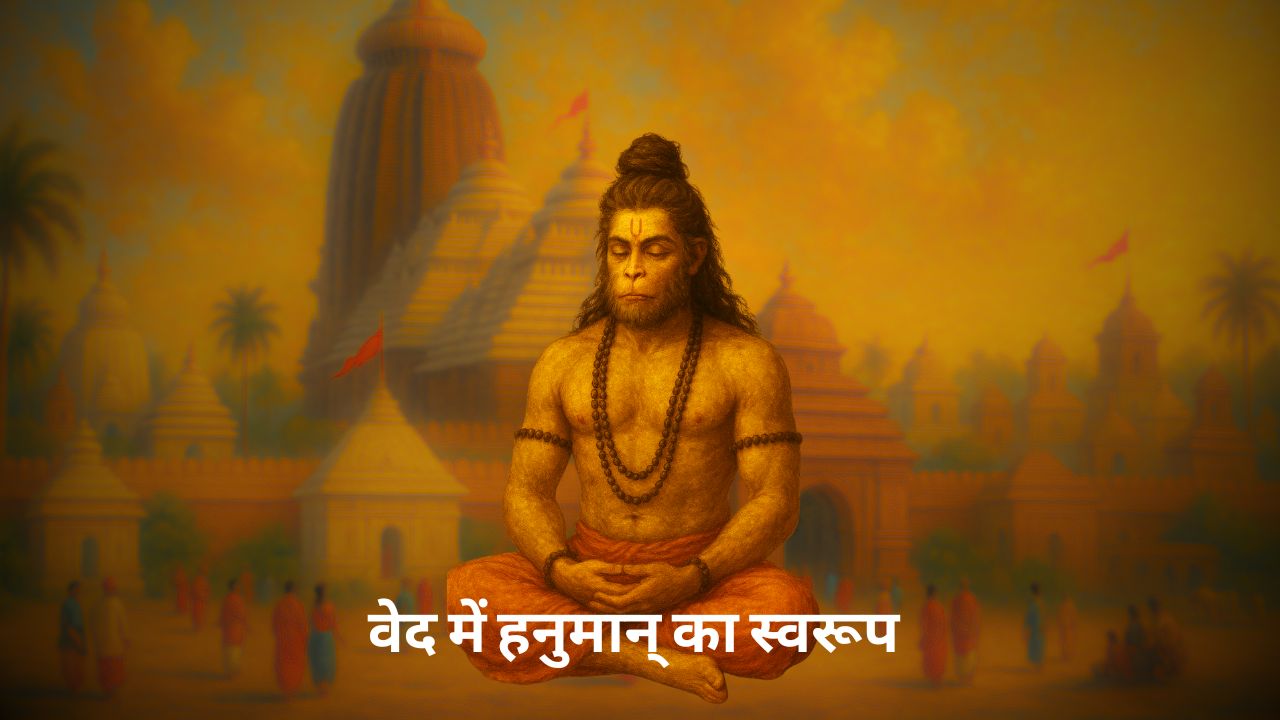- महापुरुष
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
१. बुद्ध का अर्थ और सूची –मनुष्य के विकास के भी ४ स्तर हैं जिसकी पूर्णता को बुद्ध कहा गया है-
(१) श्रावक-सामान्य मनुष्य जो अपनी उन्नति की इच्छा रखता है।
(२) बोधिसत्व-विकास की उच्च स्थिति।
(३) प्रत्येक बुद्ध-विकसित स्तर, मनुष्य रूप में बुद्ध।
(४) सम्यक् बुद्ध-क्षण मात्र के लिये ज्ञान की उच्चतम अवस्था। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार भी सम्यक् बुद्ध उच्चतम स्थिति होने के कारण एक ही हो सकता है।
प्रत्येक बुद्ध मनुष्य रूप में दीखता है। ७ लोक, २४ प्रकृति या बुद्धि के २८ अशक्ति के अनुसार ७, २४, या २८ मनुष्य बुद्ध हैं। स्तूप (थूप) वंश के अनुसार २८ बुद्धों के नाम हैं-
(१) तनहंकर, (२) मेधांकर, (३) शरणंकर, (४) दीपंकर, (५) कोण्डन्ना, (६) मंगल, (७) सुमना, (८) रेवत, (९) शोभित, (१०) अनोमदर्शी, (११) पद्म, (१२) नारद, (१३) पद्मोत्तर, (१४) सुमेधा, (१५) सुजाता, (१६) प्रियदर्शी, (१७) अन्तः दर्शी, (१८) धर्मदर्शी, (१९) सिद्धार्थ, (२०) तिष्य, (२१) पुष्य, (२२) विपश्यी, (२३) शिखी, (२४) विश्वभू, (२५) क्रकुच्छन्द, (२६) कनकमुनि, (२७) कश्यप, (२८) गौतम, (२९) मैत्रेय (भविष्य में)।
बोधिसत्त्व-यह बुद्धत्व प्राप्ति के निकट पूर्व की अवस्था है। चीनी, जापानी तथा तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर इनकी सूची है-
(१) आकाशगर्भ-आनन्द रूप जो सभी की सहायता करते हैं।
(२) अवलोकितेश्वर-कृपामूर्ति, महायान मार्ग के मुख्य बोधिसत्त्व।
(३) क्षितिगर्भ-नारकीय जीवों के लिये, दृढप्रतिज्ञ।
(४) महास्थानप्राप्त-बौद्धिक शक्ति, अमिताभ की बाईं तरफ स्थान।
(५) मैत्रेय-गौतम बुद्ध के बाद करुणामूर्ति के रूप में जन्म।
(६) मञ्जुश्री-प्रज्ञा तथा बुद्धि रूप में।
(७) नागार्जुन-महायान मार्ग की माध्यमक शाखा के संस्थापक।
(८) वज्रपाणि-बुद्ध के अंगरक्षक।
(९) पद्मसम्भव-तिब्बत के रिनपोछे।
(१०) समन्तभद्र-सभी बौद्धों की साधना तथा ध्यान रूप।
(११) संघाराम-बौद्ध मठों के रक्षक।
(१२) शान्तिदेव-बौद्ध विद्वान् जिन्होंने बोधिसत्वों के विषय में लिखा।
(१३) सितातपत्र-श्वेत वस्त्रधारी, अदृश्य विपत्तियों से रक्षा करने वाले।
(१४) स्कन्द-धर्मरक्षक, वज्रपाणि (इन्द्र) के सहायक।
(१५) सुपुष्पचन्द्र-शान्तिदेव की पुस्तक में लिखित।
(१६) सूर्यवैरोचन-भैषज्य गुरु बुद्ध के २ सहायकों में एक।
(१७) तारा-अवलोकितेश्वर का नारी रूप, तिब्बत में कार्यसिद्धि की देवी, चिकित्सा की देवी।
(१८) वज्रपाणि-महायान के प्राचीन बोधिसत्व।
(१९) वसुधर-सम्पत्ति तथा उत्पादन कारक, नेपाल में प्रचलित।
कालक्रम से मुख्य बुद्ध हैं-
(१) कश्यप-यह देवों तथा दैत्यों दोनों के गुरु थे तथा इनको ब्रह्मा भी कहा गया है। इनके काल के बाद १० युगों = ३६०० वर्ष तक दैत्यों का प्रभुत्व रहा जिसके बाद वैवस्वत मनु का काल (१३९०२ ईसा पूर्व) आरम्भ हुआ। अतः इनका काल १७,५०२ ईसा पूर्व है।
सख्यमासीत्परं तेषां देवनामसुरैः सह ।
युगाख्या दश सम्पूर्णा ह्यासीदव्याहतं जगत्॥६९॥
दैत्य संस्थमिदं सर्वमासीद्दश युगं किल ॥९२॥
अशपत्तु ततः शुक्रो राष्ट्रं दश युगं पुनः ॥९३॥ -ब्रह्माण्ड पुराण (२/३/७२) इनके समय पुनर्वसु नक्षत्र से वर्ष आरम्भ होता था जिसका देवता अदिति (कश्यप पत्नी है)-
अदितिर्जातम्, अदितिर्जनित्वम् (शान्ति पाठ, ऋक्, १/८९/१०)।
कैस्पियन सागर (झील) का नाम कश्यप जैसा होने से इसके निकट कुछ लोग कश्यप का स्थान मानते हैं। नीलमत पुराण तथा राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर ही पूर्व काल में कश्यप सागर था। फाहियान ने इनका स्थान श्रावस्ती के निकट लिखा है, जो उस समय ज्ञात रहा होगा। इनकी शिक्षा का वर्णन महाभारत, शान्ति पर्व अध्याय १२४ के प्रह्लाद-इन्द्र संवाद में है।
कश्यप को आयुर्वेद का भी आचार्य कहा गया है, जिनके नाम पर अगद-तन्त्र (विष विज्ञान) है। चीन में इनको फान या मञ्जुश्री बुद्ध कहते हैं, जिन्होंने हर वस्तु का नाम या चिह्न दिया। यह चीनी लिपि है, जिसमें हर शब्द के लिए अलग-अलग चिह्न हैं। वेद में इनको बृहस्पति कहा गया है, जिनको ब्रह्मा ने लिपि बनाने के अधिकृत किया। उनसे इन्द्र ने व्याकरण सीखा।
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत् नामधेयं दधानाः।
यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥ (ऋक् १०/७१/१)
बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यवर्ष सहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दपारायणं प्रोवाच। (पतञ्जलि-व्याकरण महाभाष्य १/१/१)
(२) अमिताभ बुद्ध-यह चीन में थे। इनको भारत में काक-भुशुण्डि कहा गया है। योगवासिष्ठ, निर्वाण खण्ड, भाग १, अध्याय १४-१७ में इनका स्थान मेरु पर्वत (पामीर) के उत्तर पूर्व कहा गया है। इनसे शिक्षा लेने गरुड़ गये थे जिनका भवन इण्डोनेसिया में था (रामायण, किष्किन्धा काण्ड, ४०/३९, में यवद्वीप सहित सप्तद्वीप)।
(३) सुमेधा बुद्ध-यह दुर्गा सप्तशती के सुमेधा ऋषि हैं। रामायण बालकाण्ड के अनुसार धनुष यज्ञ के बाद परशुराम ने शार्ङ्ग धनुष राम को दे दिया तथा उसके बाद वे तपस्या के लिये महेन्द्र पर्वत पर गये। ओडिशा के राजाओं को महेन्द्र राज कहा जाता था तथा यहां का सबसे ऊंचा पर्वत महेन्द्र गिरि (कन्धमाल जिला) है। यहां सुमेधा ने परशुराम को दीक्षा तथा उपदेश दिया था जिसका विस्तृत वर्णन त्रिपुरा रहस्य है जिसके २ विशाल खण्ड ज्ञान तथा माहात्म्य प्रायः ४००० पृष्ठों में उपलब्ध हैं। परशुराम के निधन पर ६१७७ ईसा पूर्व में कलम्ब (कोल्लम्) सम्वत् आरम्भ हुआ, जो केरल में अभी भी चल रहा है। सुमेधा ने शक्ति के रूपों की १० महाविद्या के रूप में व्याख्या की, जिनको बौद्ध ग्रन्थों में १० प्रज्ञा-पारमिता कहा गया है। महाविद्या या प्रज्ञा-पारमिता-दोनों का अर्थ है विद्या की सीमा। इनका स्थान आज भी बौध कहा जाता है (एक जिला)।
(४) दीपंकर बुद्ध-इन्होंने राजा सुचन्द्र को वज्र-योग का उपदेश दिया था। यह मार्ग वज्रयान कहा जाता है जिसमें उच्च कोटि की योग साधना की जाती है। इनके बुद्ध-तन्त्र का प्रचार हेवज्र ने किया तथा उस परम्परा में पद्म (सरोरुह) , वज्र, आनन्द-वज्र, अनङ्ग-वज्र हुये। अनङ्ग-वज्र का शिष्य ओडिशा का राजा इन्द्रभूति था जिसकी बहन लक्ष्मीङ्करा ने उनकी शिक्षा को गीतों के रूप में प्रचलित किया जिनको बंगाल में बाउल गीत कहा जाता है। इन्द्रभूति के पुत्र पद्मसम्भव ने तिब्बत में लामा परम्परा का आरम्भ किया। जो अ से ल तक (संस्कृत में अलम्) का ज्ञान रखता है, उसे लामा कहते हैं। लामा लोगों का प्रधान दलई-लामा है। दलई या दलवाइ ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्णाटक में प्रचलित है।
(५) शाक्यसिंह बुद्ध-यह महाभारत काल में नेपाल के किरात राजा जितेदस्ती के काल में गये थे (कोटा वेङ्कटाचलम की नेपाल वंशावली)। यह राजा महाभारत युद्ध में मारा गया था। इसके पिता हुमति के काल में पाण्डव अर्जुन नेपाल गये थे जिनके साथ किरात युद्ध तथा बाद में मित्रता की कहानी महाभारत, वन पर्व के कैरात पर्व, अध्याय ३८-४४ में वर्णित है तथा इस पर दण्डी का किरातार्जुनीयम् महाकाव्य है।
सिद्धार्थ को भी शाक्यमुनि इसलिये कहते थे क्योंकि उनका वंश साल (शक = सखुआ) वन के क्षेत्र में राज्य करता था। शाक्यसिंह भी इसी या निकटवर्त्ती अन्य शाक्यवंश के होंगे। इनकी शिक्षा महाभारत, शान्ति पर्व अध्याय ३०७-३०८ में है।
(६) सिद्धार्थ बुद्ध-महाभारत युद्ध में मारे गये सूर्यवंशी राजा बृहद्बल की २४ पीढ़ी बाद सिद्धार्थ का जन्म शुद्धोदन के पुत्र के रूप में हुआ। इनका उल्लेख सभी पुराणों में है। इनके जन्म की सभी मुख्य घटनायें वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) को हुयीं- जन्म ३१-३-१८८६ ईसा पूर्व, शुक्रवार, वैशाख शुक्ल १५ (पूर्णिमा), ५९-२४ घटी तक। कपिलवस्तु के लिये प्रस्थान २९-५-१८५९ ईसा पूर्व, रविवार, आषाढ़ शुक्ल १५। बुद्धत्व प्राप्ति ३-४-१८५१ ईसा पूर्व, वैशाख पूर्णिमा सूर्योदय से ११ घटी पूर्व तक। शुद्धोदन का देहान्त २५-६-१८४८ ईसा पूर्व, शनिवार, श्रावण पूर्णिमा। बुद्ध निर्वाण २७-३-१८०७ ईसा पूर्व, मंगलवार, वैशाख पूर्णिमा, सूर्योदय से कुछ पूर्व। इनकी जन्म कुण्डली-लग्न ३-१अंश-२’, सूर्य ०-४ अं-५४’, चन्द्र ६-२८अं-६’, मंगल ११-२८अं-२४’, बुध ११-१०अं-३०’, गुरु ५-८अं-१२’, शुक्र ०-२३अं-२४’, शनि १-१६अं-४८’, राहु २-१५अं-३८’, केतु ८-१५अं-३८’। ये सभी तिथि-नक्षत्र-वार बुद्ध की जीवनी से हैं।
(७) मैत्रेय बुद्ध-फाहियान के अनुसार यह बुद्ध निर्वाण के १५० वर्ष बाद (१६५७ ई.पू.) में धान्यकटक में हुए थे। यह प्राचीन सातवाहन राज्य की राजधानी थी, जिसके अवशेष आन्ध्र प्रदेश के गुण्टूर जिले के अमरावती मण्डल में है। अभी इसे आन्ध्र राजधानी क्षेत्र में रखा गया है। ओड़िशा में भी कटक को धान्य कटक कहते थे जिसके निकट धानमण्डल, साले (शालि) पुर, चाउलियागंज आदि हैं। दोनों क्षेत्र प्राचीन कलिंग में थे तथा धान उत्पादन के केन्द्र थे।
(८) लोकधातु बुद्ध-राजतरंगिणी के अनुसार यह गोनन्द वंश के ४८ वें राजा अशोक (१४४८-१४०० ईसा पूर्व) के समय थे। इनके द्वारा बौद्ध मत के प्रचार के कारण मध्य एसिआ बौद्ध घुस गये तथा उन्होंने कश्मीर का राज्य नष्ट कर दिया। राजतरंगिणी के इस श्लोक (१/१०१-१०२) के आधार पर मद्रास के अभिलेख अधिकारी हुल्ज ने कहानी गढ़ी कि मौर्य अशोक (कश्मीर अशोक नहीं) के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण राज्य नष्ट हो गया। ५१वें गोनन्द राजा कनिष्क (१२६४-१२३४ ईसा पूर्व) के काल में भी एक लोकधातु बुद्ध थे।
(९) गौतम बुद्ध-सामान्यतः ४८३ ईसा पूर्व में जिस बुद्ध का निर्वाण कहा जाता है, वह यही बुद्ध हैं जिनका काल कलि की २७ वीं शताब्दी (५०० ईसा पूर्व से आरम्भ) है। इन्होंने गौतम के न्याय दर्शन के तर्क द्वारा अन्य मतों का खण्डन किया तथा वैदिक मार्ग के उन्मूलन के लिये तीर्थों में यन्त्र स्थापित किये। गौतम मार्ग के कारण इनको गौतम बुद्ध कहा गया, जो इनका मूल नाम भी हो सकता है। स्वयं सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था कि उनका मार्ग १००० वर्षों तक चलेगा पर मठों में स्त्रियों के प्रवेश के बाद कहा कि यह ५०० वर्षों तक ही चलेगा। आज की धार्मिक संस्थाओं जैसा भ्रष्टाचार उनकी नजर में था। गौतम बुद्ध के काल में मुख्य धारा से द्वेष के कारण तथा सिद्धार्थ द्वारा दृष्ट दुराचारों के कारण इसका प्रचार शंकराचार्य (५०९-४७६ ईसा पूर्व) में कम हो गया। चीन में भी इसी काल में कन्फ्युशस तथा लाओत्से ने सुधार किये।
भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व ४, अध्याय २१-
सप्तविंशच्छते भूमौ कलौ सम्वत्सरे गते॥२९॥
शाक्यसिंह गुरुर्गेयो बहु माया प्रवर्तकः॥३०॥
स नाम्ना गौतमाचार्यो दैत्य पक्षविवर्धकः।
सर्वतीर्थेषु तेनैव यन्त्राणि स्थापितानि वै॥ ३१॥
(१०) मैत्रेय बुद्ध-एक अन्य मैत्रेय बुद्ध अभी होने वाले हैं, जिनके बारे में थियोसोफिकल सोसाइटी ने बहुत लिखा है। ये लोग आशा कर रहे थे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ही मैत्रेय बुद्ध होंगे, पर वह चूक गये। पता नहीं उनकी साधना में कमी थी या सत्ता का सहयोग नहीं मिला।
२. विष्णु अवतार बुद्ध- यह २००० कलि के कुछ बाद मगध (कीकट) में अजिन ब्राह्मण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुये। दैत्यों का विनाश इन्होंने ही किया, सिद्धार्थ तथा गौतम मुख्यतः वेद मार्ग के विनाश में तत्पर थे। इसका मुख्य कारण था प्रायः ८०० ईसा पूर्व में असीरिया में असुर बनिपाल के नेतृत्व में असुर शक्ति का उदय। उसके प्रतिकार के लिये आबू पर्वत पर यज्ञ कर ४ शक्तिशाली राजाओं का संघ बना। ये राजा देश-रक्षा में अग्रणी या अग्री होने के कारण अग्निवंशी कहे गये-प्रमर (परमार-सामवेदी ब्राह्मण), प्रतिहार (परिहार), चाहमान (चौहान), चालुक्य (शुक्ल यजुर्वेदी, सोलंकी, सालुंखे)।
इस संघ के नेता होने के कारण ब्राह्मण इन्द्राणीगुप्त को सम्मान के लिये शूद्रक ( ४ वर्णों या राआओं का समन्वय) कहा गया तथा इस समय आरम्भ मालव-गण-सम्वत् (७५६ ईसा पूर्व) को कृत-सम्वत् कहा गया। ६१२ ईसा पूर्व में इस संघ के चाहमान ने असीरिया की राजधानी निनेवे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसका उल्लेख बाइबिल में कई स्थानों पर है। http://bible.tmtm.com/wiki/NINEVEH_%28Jewish_Encyclopedia%29 http://www.biblewiki.be/wiki/Medes चाहमान को मध्यदेश (मेडेस) का राजा कहा गया है। विन्ध्य तथा हिमालय के बीच का भाग अभी भी मधेस कहा जाता है-नेपाल में मैदानी भाग के लोगों को मधेस कहते हैं। रघुवंश (२/४२) में भी अयोध्या के राजा दिलीप को मध्यम-लोक-पाल कहा गया है। इस दिन चाहमान या शाकम्भरी शक आरम्भ हुआ, जिसका प्रयोग वराहमिहिर (बृहत् संहिता १३/३) तथा ब्रह्मगुप्त ने किया है।
भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व (१/६)-
एतस्मिन्नेवकाले तु कान्यकुब्जो द्विजोत्तमः।
अर्बुदं शिखरं प्राप्य ब्रह्म होममथाकरोत्॥४५॥
वेदमन्त्रप्रभावाच्च जाताश्चत्वारि क्षत्रियाः।
प्रमरस्सामवेदी च चपहानिर्यजुर्विदः॥४६॥
त्रिवेदी च तथा शुक्लोऽथर्वा स परिहारकः॥४७॥
अवन्ते प्रमरो भूपश्चतुर्योजन विस्तृता।।४९॥
भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व, ४/३- व्यतीते द्विसहस्राब्दे किञ्चिज्जाते भृगूत्तम॥१९॥
अग्निद्वारेण प्रययौ स शुक्लोऽर्बुद पर्वते। जित्वा बौद्धान् द्विजैः सार्धं त्रिभिरन्यैश्च बन्धुभिः॥२०॥
भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व, (४/१२)- बौद्धरूपः स्वयं जातः कलौ प्राप्ते भयानके।
अजिनस्य द्विजस्यैव सुतो भूत्वा जनार्दनः॥२७॥
वेद धर्म परान् विप्रान् मोहयामास वीर्यवान्।॥२८॥
षोडषे च कलौ प्राप्ते बभूवुर्यज्ञवर्जिताः॥२९॥
भागवत पुराण १/३/२४-
ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्।
बुद्धो नाम्नाजिनसुतः कीकटेषु भविष्यति॥
वराहमिहिर-बृहत् संहिता (१३/३)- आसन् मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ। षड्-द्विक-पञ्च-द्वि (२५२६) युतः शककालस्तस्य राज्ञस्य॥
३. बौद्ध मार्ग तथा शंकराचार्य – सिद्धार्थ बुद्ध के पूर्व ७ मुख्य बुद्ध थे, जिनका वर्णन सप्ततथागत में है-विपश्यि, शिखि, विश्वभू, क्रकुच्छन्द, कनकमुनि, कश्यप (द्वितीय), गौतम। इनमें ४ बुद्धों की शिक्षा लिखित रूप में नहीं रहेने के कारण नष्ट हो गयी
अतीत बुद्धानं जिनानं देसितं।
निकीलितं बुद्ध परम्परागतं।
पुब्बे निवासा निगताय बुद्धिया।
पकासमी लोकहितं सदेवके॥ (बुद्ध वंश, १/७९)
इन ४ बुद्धों की शिक्षा लिखित उपदेश के अभाव में नष्ट हो गयी-
विपश्यि, शिखि, विश्वभू, तिष्य।
अन्य ३ बुद्धों के ३ दर्शन मार्ग थे-वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार।
सिद्धार्थ बुद्ध द्वारा चतुर्थ माध्यमिक दर्शन आरम्भ हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध ने मगध के राजा बिम्बिसार से मिल कर अपने मत का प्रचार किया। अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर शासन पर अधिकार किया और सिद्धार्थ की सहायता से उत्तर बिहार के गणतन्त्रों पर अधिकार किया। उस काल में काशी क्षेत्र में वहां के पूर्व राजा पार्श्वनाथ (युधिष्ठिर की ८वीं पीढ़ी के निचक्षु के समकालीन) के कारण बहुत से जैन मठ थे। उन पर बौद्धों ने कब्जा किया। कपासिय मठ में जैन लोगों को नात-पुत्त कह कर गाली देते थे। यह गाली (नतिया के बेटा) आज भी रोहतास जिले के कपसिया थाना क्षेत्र में प्रचलित है।
वेद मार्ग के विरोध के कारण आज भी मगध पर संस्कार हीनता का प्रभाव दीखता है।
सिद्धार्थ बुद्ध का प्रभाव गोरखपुर से गया तह ही था। मध्य और उत्तर भारत में इसका प्रचार गौतम बुद्ध (५६३ ईपू) तथा उनके शिष्यों द्वारा हुआ। ये लोग गिरोह बना कर चलते थे तथा राजाओं को प्रभावित कर वैदिक मन्दिरों मठों पर अधिकार करते थे। उस समय वेद मार्ग के नष्ट होने पर एक राजकुमारी रो रही थी, तो कुमारिल भट्ट (५५७-४९३ ईपू-ओड़िशा में महानदी के दक्षिण तट पर जय मंगला ग्राम में यज्ञेश्वर-चन्द्रगुणा के पुत्र) ने वेद मार्ग की पुनः स्थापना की प्रतिज्ञा की। उन्होंने उज्जैन के जैन मुनि कालकाचार्य (वीर, ५९९-५२७ ईपू) के पास २ वर्ष शिक्षा ली। कालकाचार्य जानते थे कि वह जैन नहीं है और कुमारिल उनके प्रिय शिष्य थे। उनकी मृत्यु के ३४ वर्ष बाद जब कुमारिल भट्ट ने वेद मार्ग का प्रचार किया, तब उन पर जैन लोगों ने आक्षेप किया कि वे गुरु द्रोही हैं, तो उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए प्रयाग संगम पर ४९३ ईपू में आत्मदाह किया।
उस समय शंकराचार्य उनसे मिले और आत्मदाह रोकने की प्रार्थना की। उस समय शंकराचार्य १५ वर्ष की आयु में ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार रूप में विख्यात हो चुके थे। कुमारिल ने कहा कि उनके शिष्य विश्वरूप (शोण नद के तट पर तत्कालीन मगध में) से मिल कर वेद मार्ग की स्थापना करें।
शंकराचार्य खण्डन करते थे, विश्वरूप मण्डन करते थे अतः मण्डन मिश्र नाम से विख्यात थे। धर्म स्थापना के लिए खण्डन-मण्डन दोनों आवश्यक हैं।
मण्डन मिश्र (५४८-४४७ ईपू) ने अपने पुत्र आयु के शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया यद्यपि १७ दिनों तक शास्त्रार्थ में तर्क द्वारा उनकी पराजय नहीं हुई थी। एक सन्त का समाज में अधिक सम्मान होता है, गृहस्थ कितना भी विद्वान् हो उसकी आज्ञा समाज नहीं मानता है। अतः अंग्रेजों ने भी गान्धी माध्यम से अपना प्रचार कराने के लिए उनको पहले वकील, सेना में सार्जेण्ट बनाने के बाद अन्त में साधु वेष में रखा।
शंकराचार्य ने अपनी बृहदारण्यक पद्धति तथा मण्डन मिश्र की छान्दोग्य पद्धति के समन्वय के लिए सम्बन्ध वार्त्तिक लिखने को कहा। यह मण्डन मिश्र माध्यम से मण्डन कार्य हुआ।
शंकराचार्य ने नास्तिक दर्शनों का खण्डन किया, यद्यपि राजनीति, कृषि, वाणिज्य के लिए चार्वाक को भी उपयोगी माना है। जैन दर्शन गौतम न्याय शास्त्र पर आधारित है, जिसमें २ ही विकल्प हैं-सत्य, असत्य। इसका सुधार जैन लोगों ने सप्तभंगी न्याय या अनेकान्त वाद से किया। पर सबके समन्वय रूप में वेदान्त दर्शन ही सर्वोच्च है। इसे समझने में पूर्व मीमांसा आदि अन्य आस्तिक दर्शन सहायक हैं।
दर्शनों का क्रम माधवीय सर्वदर्शन संग्रह में समझाया गया है। वेद मार्ग की स्थापना के लिये चाहमान वंश के राजा सुधन्वा की सहायता से भारत के ४ पीठों की स्थापना की। सामान्य लोगों के लिए दैनिक पञ्चदेव पूजा का विधान किया तथा तन्त्र मार्ग के भी शिष्य बनाये।
४. शंकराचार्य काल-आदि शंकर के सहपाठी चित्सुखाचार्य का बृहत् शंकर दिग्विजय सबसे प्रामाणिक है।
इसके अनुसार- तिष्ये (कलौ) प्रयात्यनल-शेवधि-बाण-नेत्रे (२५९३) ऽब्दे नन्दने दिनमणावुदगध्वभजि। राधे (वैशाखे) ऽदितेरुडु (पुनर्वसु नक्षत्रे) विनिर्गत मङ्ग (धनु) लग्नेऽस्याहूतवान् शिवगुरुः (पिता) स च शङ्करेति॥
दिनमणावुदगध्वभाजि का अर्थ है सूर्य उदग् = उत्तर मार्ग के उत्तर भाग में हैं। उदग अध्व का अर्थ मध्याह्न मान कर उनका मध्याह्न जन्म बाद के लेखकों ने मान लिया, किन्तु बाकी काल वही रखा।
कलि संवत् २५९३ के बदले युधिष्ठिर शक २६३१ लिखा है।
द्वारका पीठ के द्वितीय शंकराचार्य लिखित शंकर दिग्विजय में-
ततः सा दशमे मासि सम्पूर्ण शुभलक्षणे।
षड्विंशशतके श्रीमद् युधिष्ठिर शकस्य वै॥
एकत्रिंशेऽथ वर्षे तु हायने नन्दने शुभे मेषराशिं गते सूर्ये वैशाखे मासि शोभने॥
शुक्ले पक्षे (च) पञ्चम्यां तिथौ भास्कर वासरे।
पुनर्वसु गते चन्द्रे (सु) लग्ने कर्कटाह्वये॥
मध्याह्ने चाभिजिन्नाम मुहूर्ते शुभवीक्षिते।
स्वोच्चस्थे केन्द्रस्थे च गुरौ मन्दे कुजे रवौ॥
निजतुङ्गगते (शुक्रे) रविणा संगते बुधे।
प्रासूत तनयं साध्वी गिरिजेव षडाननम्॥
दोनों लेखों के अनुसार शङ्कराचार्य का जन्म नन्दन वर्ष में ही हुआ था। दक्षिण भारत में पितामह सिद्धान्त पद्धति से कलियुग का आरम्भ १३ वें प्रमाथी वर्ष से हुआ था। इसमें सौर वर्ष को ही गुरु वर्ष मानते हैं, अतः ६० वर्षों के ४३ चक्र ६० x ४३ = २५८० कलि वर्ष में पूरे हुए। उसके १३ वर्ष बाद २५९३ कलि या ५०९ ई.पू. में ही नन्दन वर्ष होगा।
७८८ ई. में ३८८९ कलि वर्ष होगा जिसमें ६४ चक्र पूरा हो कर ४९ वर्ष बचेंगे, अर्थात् १३वें प्रमाथी के ४९ वर्ष बाद द्वितीय विभव वर्ष होगा। जन्म स्थान-केरल के पूर्णा नदी तट पर, १०अं ४०’ उत्तर, ७६ अं पूर्व। ४-४-५०९ ई.पू. मंगलवार, २२५२ बजे, प्राणपद लग्न के अनुसार।
सौर वर्ष का आरम्भ ९.५३४८ मार्च ५०९ ई.पू. (९ मार्च उज्जैन मध्य सूर्योदय ६ बजे के ०.५३४८ दिन बाद), वैशाख शुक्ल १ का आरम्भ मार्च २०.७६२३४ को।
वैशाख शुक्ल पञ्चमी ३-४-५०९ ई.पू. ०९३४ बजे से, ४-४-५०९ ई. पू. ११३२ तक।
पुनर्वसु नक्षत्र ४-४-५०९ ई.पू. ०१३९ से ५-४-५०९, ०४०६ तक।
अहर्गण-सृष्टि ७,१४,४०,३२,४३,९६३ (रविवार =१), जुलियन १-१-४७१३ से (मंगलवार = १) १५,३५,६०५,
कलि (गुरु वार =१)-९,४७,१४७। ४-४-५०९ ई.पू. को कालटी में सूर्योदय ६-२७-३७ बजे भारतीय समय।
२२५२ बजे-लग्न ८-२१ अं -२४’, प्राणपद लग्न ८-२१ अं -२३’ , दशम भाव ५-२६ अं -४३’। अयनांश = -१० अं ५८’९”, सूर्य सिद्धान्त से = -१६ अं ५०’। ग्रह मध्य (अंश) स्पष्ट मन्दोच्च सूर्य २३.६२ २५.३८ — चन्द्र —- ९०.६८ — मंगल २७०.४८ ३०५.१९ १३०.०२ बुध १२८.६३ ४४.३४ २२०.३९ गुरु २४४.५३ २४७.४५ १७१.१८ शुक्र १७८.५१ ६७.५३ ७९.७८ शनि ३४६.४१ ३४३.२२ २३६.६२ राहु ३१.४७ —- —-
इस कुण्डली के अनुसार उनके बालारिष्ट तथा चक्रवर्त्ती संन्यासी का योग भी बनता है।
५. कुमारिल भट्ट-चित्सुखाचार्य ने इनको शङ्कर से ४८ वर्ष बड़ा कहा है।
अष्टचत्वारि वर्षाणि जन्मकालाद्गतानि वै।
प्रादुर्भावः शङ्करस्य ततो जातोऽतिवादिनः॥ (संस्कृत चन्द्रिका, खण्ड २, पृष्ठ ६) जिनविजय महाकाव्य में भी यही काल जैन युधिष्ठिर शक (२६३४ ई.पू. से) में दिया है-
ऋषि (७) र्वार (७) स्तथा पूर्णः (०) मर्त्याक्षौ (२) वाममेलनात्।
एकीकित्य लभेताङ्क क्रोधी स्यात् तत्र वत्सरः॥
भट्टाचार्य कुमारस्य कर्मकाण्डैकवादिनः।
ज्ञेयः प्रादुर्भावस्तस्मिन् वत्सरे यौधिष्ठिरे शके॥ २०७७ युधिष्ठिर शक = २६३४-२०७७ = ५५७ ईपू. इनका जन्म स्थान महानदी के दक्षिण जयमङ्गला (वर्तमान काकटपुर मंगला?)
कहा है-
आन्ध्रोत्कलानां संयोगे पवित्रे जयमङ्गले।
ग्रामे तस्मिन् महानद्यां भट्टाचार्य कुमारकः॥
आन्ध्रजातिस्तैत्तिरीयो माता चन्द्रगुणा सती।
यज्ञेश्वरः पिता यस्य—॥ इसी ग्रन्थ में शङ्कराचार्य का मृत्यु काल २१५७ जैन युधिष्ठिर शक अर्थात् ४७७ ईपू दिया है- ऋषि (७) र्बाण (५) स्तथा भूमि (१) र्मर्त्याक्षौ (२) वाम मेलनात्। एकत्वेन लभेताङ्कस्ताम्राक्षा तत्र वत्सरः॥
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.