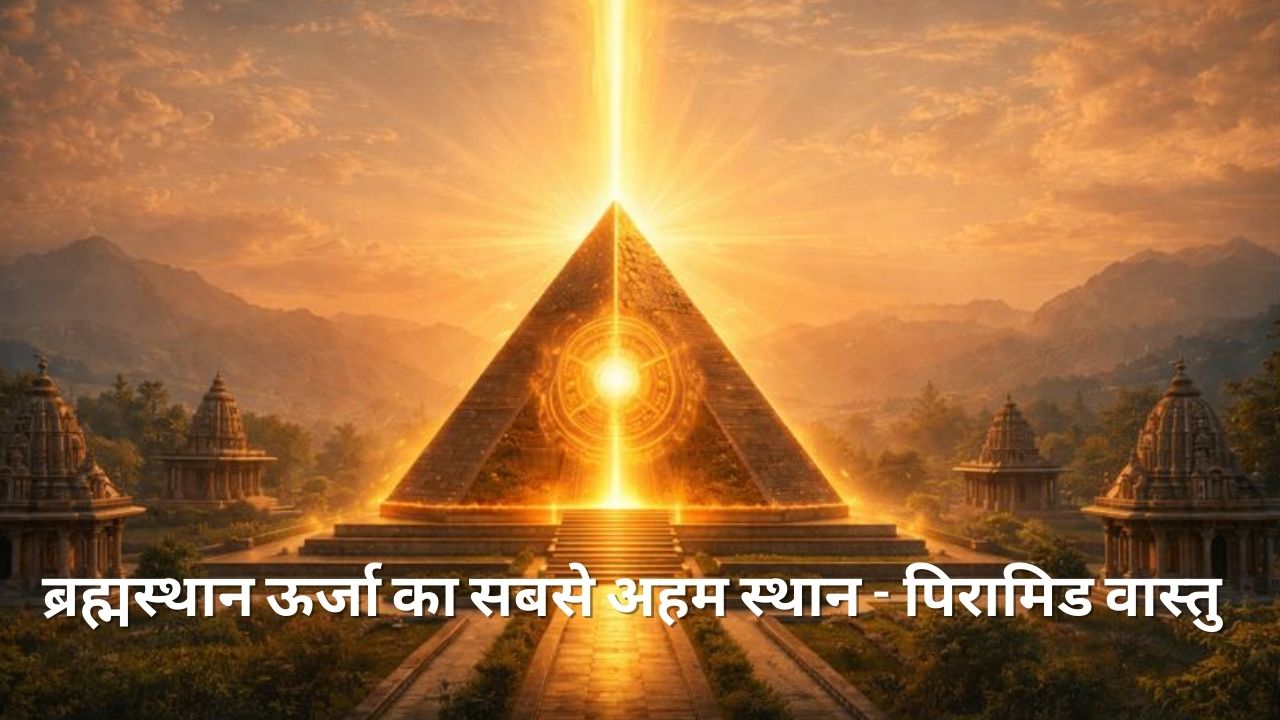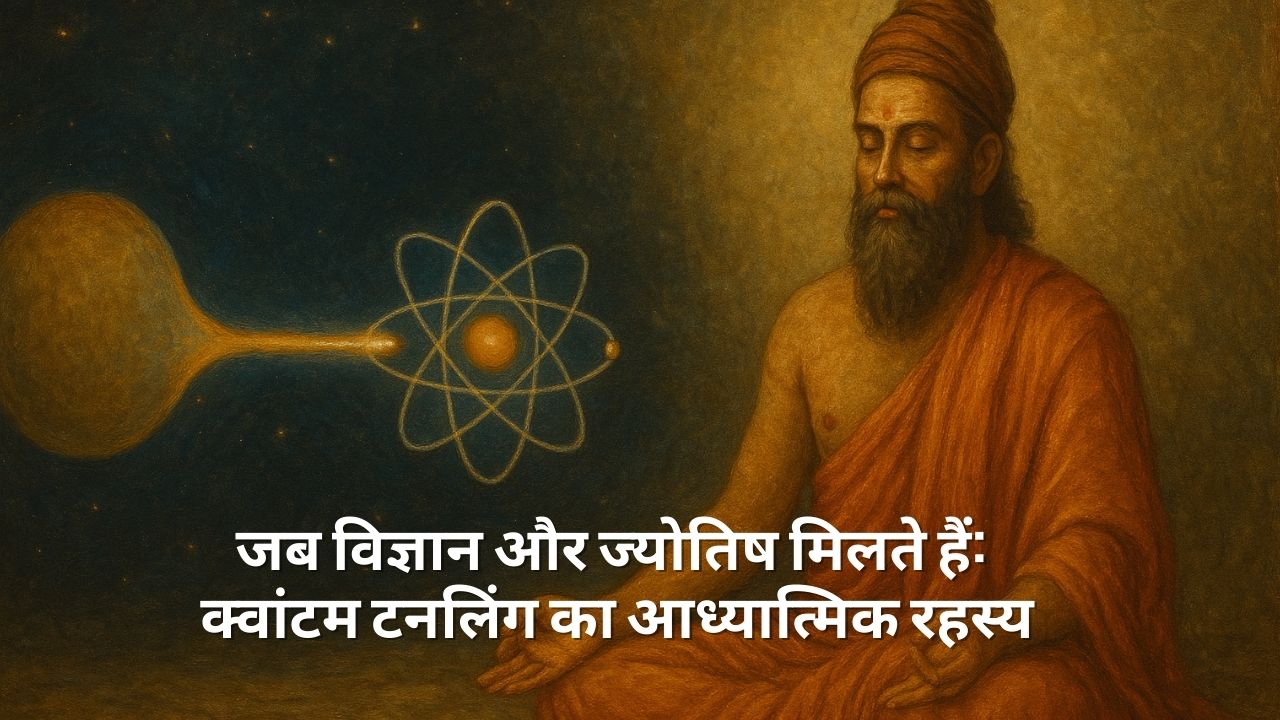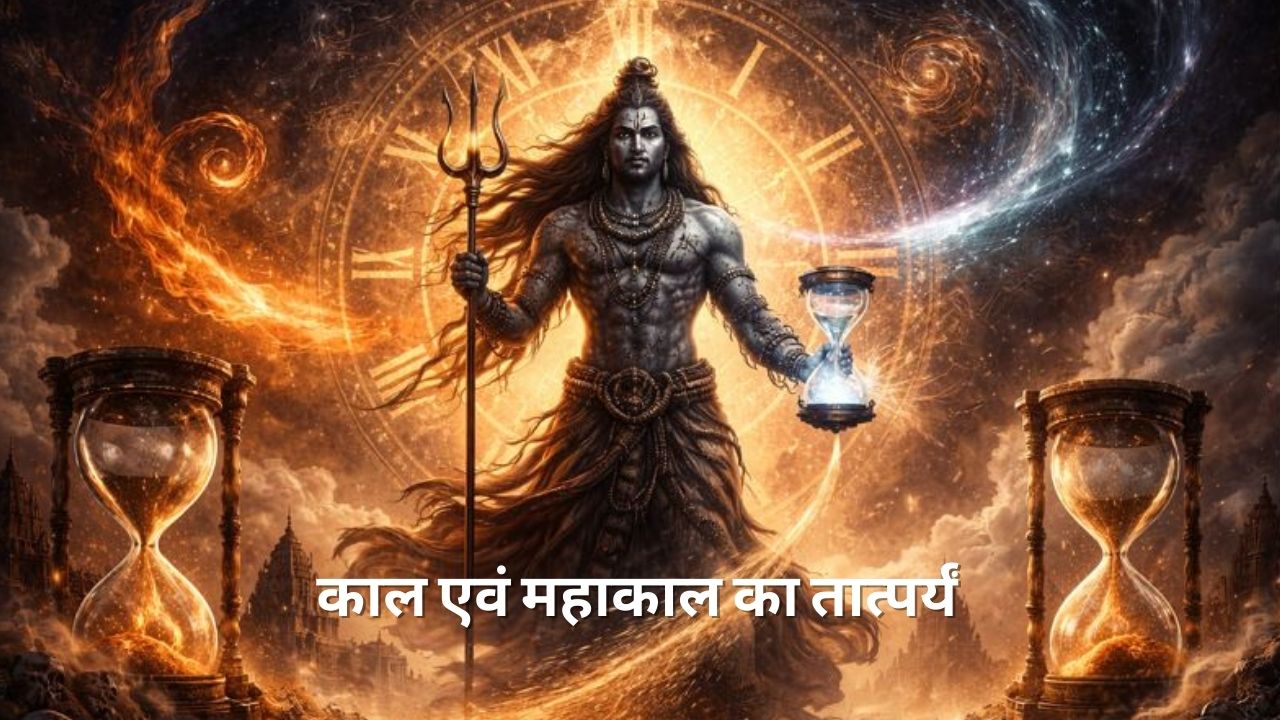- ज्योतिष विज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 श्री शशांक शेखर शुल्ब (धर्मज्ञ )-
Mystic Power- अनेक रहस्यों से युक्त ज्योतिषशास्त्र ज्ञान का महासमुद्र है। ब्रह्माण्ड के अनेक तत्त्वों के रहस्योद्घाटन में प्रवृत्त ज्योतिषशास्त्र में ग्रह-नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापात आदि ज्योति: पदार्थों के स्वरूप, गति एवं स्थित्यादि का निरीक्षण करने पर ये तारे क्या वस्तु हैं? इनमें पूर्व की ओर गतिमान् ज्योतिःपुंज क्या हैं? चन्द्रका स्वरूप प्रतिदिन क्यों बदलता रहता है ? स्वच्छ पूर्णिमा की रात्रि को कभी चन्द्र धूमिल या कुछ देर के लिये अदृश्य-सा क्यों हो जाता है ? स्वच्छ दिन में कभी-कभी सूर्य की प्रभा क्षीण क्यों पड़ जाती है ? ऋतुओं के आवागमन का चक्र कैसे चलता है ? इत्यादि क्या? क्यों? और कैसे ?
-जैसे प्रश्नों ने मानव-मन को उद्वेलित किया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की चाहने ज्योतिष शास्त्र की नींव रखी। हमारे ऋषि महर्षियों एवं पूर्वाचार्यों ने भी ज्योति: पदार्थों की गति-स्थित्यादि के अतिरिक्त आकाश में घटने वाली ग्रहण- जैसी आश्चर्यजनक घटनाओं का भी सतत निरीक्षण करके प्राणियों पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव का विश्लेषणकर ज्योतिषशास्त्र के मानक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा रचित ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तरूपी अनमोल रत्न ज्योतिष शास्त्र की अमूल्य धरोहर हैं। वैदिक दर्शन की अवधारणा पर आधारित ज्योतिषशास्त्र वेदांग के नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। वेदांग ज्योतिष में सभी वेदांगों में इसकी प्रधानता स्वीकार की गयी है-
श्री शशांक शेखर शुल्ब (धर्मज्ञ )-
Mystic Power- अनेक रहस्यों से युक्त ज्योतिषशास्त्र ज्ञान का महासमुद्र है। ब्रह्माण्ड के अनेक तत्त्वों के रहस्योद्घाटन में प्रवृत्त ज्योतिषशास्त्र में ग्रह-नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापात आदि ज्योति: पदार्थों के स्वरूप, गति एवं स्थित्यादि का निरीक्षण करने पर ये तारे क्या वस्तु हैं? इनमें पूर्व की ओर गतिमान् ज्योतिःपुंज क्या हैं? चन्द्रका स्वरूप प्रतिदिन क्यों बदलता रहता है ? स्वच्छ पूर्णिमा की रात्रि को कभी चन्द्र धूमिल या कुछ देर के लिये अदृश्य-सा क्यों हो जाता है ? स्वच्छ दिन में कभी-कभी सूर्य की प्रभा क्षीण क्यों पड़ जाती है ? ऋतुओं के आवागमन का चक्र कैसे चलता है ? इत्यादि क्या? क्यों? और कैसे ?
-जैसे प्रश्नों ने मानव-मन को उद्वेलित किया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की चाहने ज्योतिष शास्त्र की नींव रखी। हमारे ऋषि महर्षियों एवं पूर्वाचार्यों ने भी ज्योति: पदार्थों की गति-स्थित्यादि के अतिरिक्त आकाश में घटने वाली ग्रहण- जैसी आश्चर्यजनक घटनाओं का भी सतत निरीक्षण करके प्राणियों पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव का विश्लेषणकर ज्योतिषशास्त्र के मानक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा रचित ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तरूपी अनमोल रत्न ज्योतिष शास्त्र की अमूल्य धरोहर हैं। वैदिक दर्शन की अवधारणा पर आधारित ज्योतिषशास्त्र वेदांग के नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। वेदांग ज्योतिष में सभी वेदांगों में इसकी प्रधानता स्वीकार की गयी है-
 "यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा ।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम् ॥"
(आर्चज्योतिष ३५)
'ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम्' ज्योतिषशास्त्र की इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिषशास्त्र कहते हैं। वस्तुतः ग्रह-नक्षत्रों की गतिविधि एवं प्रभाव के विषय में जो कुछ भी ज्ञान है, वह सब ज्योतिष ही है। प्राणियों पर ग्रहादिकों के प्रभाव का अध्ययन कर उसके अनुसार शुभाशुभ-फल कथन ही ज्योतिषका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि भास्कराचार्यजी ने कहा है-
"यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा ।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम् ॥"
(आर्चज्योतिष ३५)
'ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम्' ज्योतिषशास्त्र की इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिषशास्त्र कहते हैं। वस्तुतः ग्रह-नक्षत्रों की गतिविधि एवं प्रभाव के विषय में जो कुछ भी ज्ञान है, वह सब ज्योतिष ही है। प्राणियों पर ग्रहादिकों के प्रभाव का अध्ययन कर उसके अनुसार शुभाशुभ-फल कथन ही ज्योतिषका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि भास्कराचार्यजी ने कहा है-
 'ज्योतिःशास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते।'
(सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय गोलप्रशंसा ६)
ज्योतिषशास्त्र के मुख्यतया सिद्धान्त, होरा एवं संहिता - ये तीन स्कन्ध हैं। सिद्धान्तस्कन्ध गणितात्मक है। इसमें मुख्यतया ग्रहों की गति, स्थिति, दिग्देश एवं कालगणन विषय की विवेचना प्राप्त होती है। ग्रहों के प्रभाव का अध्ययनकर शुभाशुभफल निरूपण होरा एवं संहिता का वर्ण्य विषय है।
मुख्यतया काल को आधार बनाकर फलविवेचना के लिये जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुण्डली का निर्माण किया जाता है। जन्मकुण्डली के द्वादश भावों में स्थित ग्रहों के परस्पर सम्बन्धादि का विचारकर वैयक्तिक फल का विवेचन होरास्कन्ध में किया जाता है। समष्टिगत फल का विवेचन संहितास्कन्ध में प्राप्त होता है। संहितास्कन्ध में शकुन, वास्तुप्रभृति विषय भी आते हैं। इस प्रकार मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर समुचित मार्गदर्शन देना ज्योतिषशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है।
होरास्कन्ध - अर्थ एवं प्रयोजन - मानवजीवन के सुख-दुःख, इष्टानिष्ट आदि सभी शुभाशुभ विषयों का विवेचन करने वाला शास्त्र ही होरा शास्त्र है । होरा शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र शब्दसे हुई है। अहोरात्र शब्द के प्रथम एवं अन्तिम अक्षर का लोप करने पर 'होरा' शब्द निष्पन्न होता है। एक राशि में २ होराएँ होती हैं। सम्पूर्ण अहोरात्र में क्रान्तिवृत्तस्थ १२ राशियों का स्पर्श पूर्वक्षितिज में हो जाता है, जिस कारण १२ लग्न एक दिन-रात में होते हैं। अतः १२ लग्नों की २४ होराएँ होती हैं। वस्तुतः जन्मकुण्डली में लग्न का अत्यधिक महत्त्व है। साथ ही सूक्ष्म विवेचन हेतु होरा-कुण्डली का भी विचार किया जाता है। बृहज्जा तक की होराभिप्राय- निर्णयटीका के अनुसार अहोरात्र का - मेषादि राशि भेदों का अर्थात् सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांशादिकों की प्राणपर्यन्त होरा संज्ञा है। इसी आधार पर इसे होराशास्त्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। होराशास्त्र का दूसरा नाम जातकशास्त्र भी है।
वैदिक दर्शन की पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार मनुष्य निरन्तर शुभाशुभ कर्मों में निरत रहता है। 'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्' इस सूक्ति के अनुसार उसे कर्मों का फल अवश्य भोगना है, परंतु एक साथ ही या एक ही जन्म में समस्त कर्मों का फल मिलना सम्भव नहीं है, अतः उसे अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं, जिसमें वह अपने किये कर्मों का फल भोगता है। इस प्रकार कर्मों के विपाक के तीन भेद बन जाते हैं -संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण। किसी भी प्राणीद्वारा वर्तमान क्षण तक किया समस्त कर्म, चाहे वह इस जन्म का हो अथवा पूर्व जन्मों का, संचित कर्म है। इसका फलविवेचन जन्मकुण्डली में योगायोग विचार से किया जाता है। जैसे- राजयोग, दरिद्रयोग आदि । अनेक जन्म-जन्मान्तरों के संचित कर्मों का फल एक साथ भोगना सम्भव नहीं है।
अतः संचित कर्मों में से जितने कर्मों के फल को प्राणी पहले भोगना आरम्भ करता है, वह प्रारब्ध या भाग्य कहलाता है। इसका विवेचन ज्योतिष में दशाविचार से होता है। जो कर्म अभी हो रहा है या किया जा रहा है, इसका विवेचन अष्टकवर्गके आधारपर गोचर अथवा तात्कालिक ग्रहस्थित्यनुसार किया जाता है। इस प्रकार ज्योतिषशास्त्र का यह स्कन्ध जन्मकुण्डली की ग्रहस्थिति के आधार पर मनुष्य के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों में किये गये शुभाशुभ कर्मो के विपाक को जातक के शुभाशुभ फल के रूप में प्रकाशित करता है।
इसलिये आचार्य वराहमिहिरका कथन है कि यह शास्त्र मनुष्य के लिये उसी प्रकार पथनिर्देशन का कार्य करता है, जैसे गहन अन्धकारमें दीपक ।
अतः होराशास्त्रका प्रयोजन ग्रहनक्षत्रों की गति- स्थित्यनुसार कुण्डली का निर्माणकर जातक के जीवन में आने वाले सुख-दुःखादि का अनुमान कर उसे अपने कर्तव्यों द्वारा अपने अनुकूल बनाने के लिये प्रेरित करना है।
होरास्कन्ध का वर्ण्य - विषय - होरास्कन्ध में मुख्य- तया ग्रह एवं राशियों का स्वरूप वर्णन, ग्रहों की दृष्टि, उच्च-नीच, मित्रामित्र, बलाबल आदिका विचार, द्वादश भावों द्वारा विचारणीय विषय एवं उनमें स्थित ग्रहों का शुभाशुभ फलविवेचन, जातक का अरिष्टविचार, वियोनि- जन्मविचार, राजयोग, प्रव्रज्यायोग, दरिद्रयोग आदि अनेक विध शुभाशुभ योगविचार, सूर्यकृत योग, चन्द्रकृत योग, नाभसयोग, आयुर्दायविचार, अष्टकवर्ग विचार, होरा- सप्तमांशादि दशवर्ग-साधन, ग्रहविंशोपकादि बलसाधन, विंशोत्तरी आदि दशान्तर्दशादि का साधन, नक्षत्रादिजनन- फलविचार आदि विषय सम्मिलित हैं। वस्तुतः होराशास्त्र के विभिन्न मानक ग्रन्थों में एक समानरूप से उपर्युक्त सभी विषय न होकर न्यूनाधिक रूप में प्राप्त होते हैं। वर्ण्य-विषय में न्यूनाधिकत्व होते हुए भी सभी का मुख्य उद्देश्य व्यष्टिगत फलविवेचन अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं तदनुसार दशा इत्यादि के आधार पर शुभाशुभ फलकथन करना है। बृहत्संहिता के सांवत्सर- सूत्राध्याय में होराशास्त्र के वर्ण्य विषय विशद रूपसे वर्णित हैं।
होरास्कन्ध का उद्भव एवं विकास - भारतीय त्रिस्कन्धात्मक ज्योतिषशास्त्र की अवधारणा को वैदिक काल से ही अनुभव किया जा सकता है। वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं। यद्यपि इनका वर्ण्य विषय ज्योतिष नहीं है, परंतु इनमें प्रसंगवश उपलब्ध व्यावहारिक ज्योतिषीय वर्णन तत्कालीन उत्कृष्ट ज्योतिषीय ज्ञानका परिचायक है। 'प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शनम्' एवं 'यादसे गणकम्' - जैसे मन्त्र उस समय के ज्योतिर्विदों के महत्त्व को द्योतित करते हैं।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में कुछ ज्योतिर्विद् ऋषियों के नामों का वर्णन मिलता है। नारदसंहिता, कश्यपसंहिता आदि में वसिष्ठ, अत्रि, नारद, पराशर, कश्यप, गर्ग आदि ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक १८ ( मतान्तरसे १९) ऋषियों के नाम प्राप्त होते हैं।
ये सभी आचार्य त्रिस्कन्धज्योतिर्विद् थे। इनमें से कुछ आचार्यों के ग्रन्थ आज भी प्राप्त हैं। यथा-महर्षि पराशरकृत बृहत्पाराशरहोराशास्त्र, नारदकृत नारदसंहिता एवं नारदीय ज्योतिष, काश्यपसंहिता, वसिष्ठसंहिता, सूर्यसिद्धान्त इत्यादि, परंतु आश्चर्य है कि इनमें वेदांग- ज्योतिष के प्रणेता लगधमुनि का नाम नहीं है। इस प्रकार त्रिस्कन्धज्योतिषशास्त्र की प्राचीन वैदिक परम्परा अभिलक्षित होती है, परंतु यह परम्परा प्रायः आचार्य वराहमिहिर से पूर्व खण्डित एवं लुप्तप्राय अनुभूत होती है। यवनों ने भारतीय ज्योतिष के साथ अपनी पद्धति का समन्वयकर एक नयी पद्धति 'ताजिकशास्त्र' को प्रस्तुत किया, जिसमें जातक पद्धति के समान ही वर्ष प्रवेश लग्न के आधार पर वर्ष भर का शुभाशुभ फल विवेचित किया जाता है। आचार्य वराहमिहिर ने यवनों के ज्योतिषज्ञान की प्रशंसा में कहा है-
"म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम्।
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्दैवविद्विजः ॥"
(बृहत्संहिता २।१५)
वराहमिहिर एवं उनके पश्चाद्वर्ती जातकशास्त्र के मानक ग्रन्थोंमें यवनों का प्रभाव स्पष्टरूप से परिलक्षित होता है।
होराशास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं ग्रन्थ- होरास्कन्धपर ऋषि जैमिनिकृत 'जैमिनिसूत्रम्' ग्रन्थ है, जो अपनी सूत्रपद्धति के द्वारा फलकथन हेतु प्रसिद्ध है। पराशरमुनिकृत बृहत्पाराशर होरा शास्त्र को होरास्कन्ध का सम्पूर्ण ज्ञान कराने वाला ग्रन्थ कहा जा सकता है। इनका 'लघुपाराशरी' नामक अन्य ग्रन्थ भी समुपलब्ध है। आचार्य वराहमिहिररचित 'बृहज्जातक' एवं 'लघुजातक' अप्रतिम ग्रन्थ हैं। बृहज्जातक को होराशास्त्र का प्रतिनिधिभूत ग्रन्थ कहा जा सकता है, जिसपर भट्टोत्पल (नवीं शताब्दी शककाल ) - द्वारा की गयी टीका अत्यन्त उत्कृष्ट है। इनके ग्रन्थों में मय, यवन, शक्ति, जीवशर्मा, मणित्थ, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, सत्याचार्य आदि पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। आचार्य कल्याणवर्माकृत सारावली (५५७ ई०), आचार्य वराहमिहिर के पुत्र पृथुयशाकृत षट्पंचाशिका, चन्द्रसेनकृत केवल ज्ञान होरा, श्रीपतिविरचित श्रीपतिपद्धति, रत्नावली, रत्नमाला एवं रत्नसार; बल्लालसेनरचित अद्भुतसागर, पद्मसूरिकृत भुवनदीपक, केशवरचित जातकपद्धति एवं ताजिकपद्धति, ढुण्ढिराजविरचित जातका भरण, वैद्यनाथकृत जातकपारिजात, नीलकण्ठरचित ताजिकनीलकण्ठी, महिमोदयकृत ज्योतिषरत्नाकर, गणेशकृत जातकालंकार इत्यादि ग्रन्थ होराशास्त्रमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त भी फलितज्योतिषके कई प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती आचार्योंके मतानुसार नवीन प्रकारसे ग्रन्थोंकी रचना की।
होरास्कन्धकी आवश्यकता एवं लोकोप- योगिता - कुछ विद्वानोंका कथन है कि जब पूर्वजन्मार्जित शुभाशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति अवश्यम्भावी है तो उसका ज्ञान कराने वाले होरास्कन्ध की क्या आवश्यकता ? क्योंकि जो होना है, वह तो होकर ही रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। सम्पूर्णरूप से भाग्य के भरोसे बैठकर ही यदि कृषक खेती करना छोड़ दे तो अन्नादि की उत्पत्ति कैसे होगी? नीतिवचनों में भी कहा गया है- 'न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ।' होराशास्त्र तो कर्मप्रधान शास्त्र है, जो पूर्वजन्मार्जित कर्मों के फल को क्रियमाण कर्म के द्वारा न्यूनाधिक करने में विश्वास रखता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि यदि होराशास्त्र के द्वारा कर्मविपाक को न्यूनाधिक किया जा सकता है तो श्रीराम, युधिष्ठिर-जैसे शक्तिमान् एवं सामर्थ्यशाली व्यक्तियोंको दुःख नहीं भोगना पड़ता अथवा होराशास्त्र के द्वारा भविष्यफल जानकर किसी को भी कभी दुःख नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ कर्मों की विचित्रता को ध्यान में रखना होगा। कुछ कर्म दृढ़ या स्थिर होते हैं तथा कुछ शिथिलमूलक या उत्पातसंज्ञक ।
अतः जहाँपर जन्म पत्रिकादि से दशाफलकालक्रम द्वारा रोग सम्भावना या अरिष्ट की सम्भावना है अथवा जब सन्तान, विद्या, धनादिका अभाव होने का कारण प्रकट होता है, वहाँ ग्रहशान्ति, मणिधारण, मन्त्रजप, दान, औषधिधारण आदि उपचारों से प्रतिबन्धक योगों को शिथिल करनेका प्रयास किया जा सकता है। जिस प्रकार दृढमूलवृक्ष भी प्रबल झंझावात से हिलकर जीर्ण या कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार दृढ़कर्मों का अशुभ फल भी कम तो अवश्य किया जा सकता है। इसीलिये सूक्ति है- 'हन्यते दुर्बलं दैवं पौरुषेण विपश्चिता' (होरारत्न)। शुभाशुभफलप्रद भाग्य कब फलीभूत होगा ? अपना पूर्ण फल देगा अथवा कुछ कम ? इत्यादिका ज्ञान भी होराशास्त्र से ही सम्भावित है। यह शास्त्र शुभाशुभफल-विपाक को जन्मकुण्डली के लग्नादि द्वादशभावों में स्थित स्वोच्च, मूलत्रिकोण, स्वगृह, मित्रगृहादि शुभ स्थानों अथवा शत्रुगृह, नीचगृह, अस्तादि अशुभ स्थानों या स्थितियों में स्थित नवग्रहों के परस्पर शुभाशुभ सम्बन्धों क आधार पर दशान्तर्दशादि के माध्यम से दिन, पक्ष, मास, वर्षादि के रूप में सूचित करता है। इसके आधार पर शुभाशुभफल विपाक समय में मनुष्य यथासम्भव जागरूक होकर मणि, मन्त्र, औषधि आदि उपायों से अशुभफल को न्यून तथा शुभ ग्रह के बल में वृद्धि करके सत्फल प्राप्त कर सकता है। इसीलिये कल्याण वर्मा का देवलों के लिये निर्देश है-
"विधात्रा लिखिता यस्य ललाटेऽक्षरमालिका।
देवज्ञस्तां पठेत् प्राज्ञः होरानिर्मलचक्षुषा।।"
(सारावली २।१)
होराशास्वके जानसे मनुष्य भावी सुख-दुःखादिका ज्ञानकर अपने पौरुषसे उसे अनुकूल बना सकता है। यह शास्त्र मनोवैज्ञानिक रूपसे उसे दुःखादि अशुभ परिस्थितियोंको झेलनेमें सम्बल प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणिमात्रपर पड़नेवाले शुभाशुभ प्रभावका अध्ययनकर फलकथन करना एवं मानवजीवनसे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओंका अध्ययनकर उसे समुचित मार्गदर्शन देना ही होराशास्त्रकी लोकोपयोगिताको सिद्ध करता है यह शास्त्र रोगके साध्यासाध्यत्वादिका निर्णय करके एवं उसके सम्भावित कालका अनुमान प्रस्तुतकर आयुर्वेदकी महान् सहायता करता है। इसी प्रकार जातककी अभिरुचि, दक्षता, स्वभावादिका विश्लेषण करके उसे भावी जीवनमें अपने कार्यक्षेत्रका चुनाव करनेमें सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः जातकशास्त्रकी लोकोपयोगिताको द्योतित करते हुए आचार्य कल्याणवर्माका कथन है-
"अर्थार्जने सहायः पुरुषाणामापदर्णवे पोतः ।
यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः ।।"
(सारावलीर २/५)
भारतीय वैदिक दर्शनमें 'कर्मवाद' का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार संसारमें प्राणी अनवरत कर्ममें ही निरत रहता है। वह चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकता है। कर्म करनेपर उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। आत्मा अजर एवं अमर है, परंतु कर्मबन्धनके फलस्वरूप उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्मबन्धनसे मुक्ति केवल तभी मिल सकती है, जब मनुष्यको आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान हो जाता है। प्राणीके शुभाशुभकर्मो का फल उसे वर्तमान जीवनमें कब, कहाँ और किस रूपमें प्राप्त होगा, इत्यादि समस्त जिज्ञासाओंका उत्तर जाननेका एकमात्र उपकरण होराशास्त्र है। इसका मुख्य कार्य ग्रह- नक्षत्रोंकी गतिस्थित्यनुसार कुण्डलीका निर्माणकर जातकके जीवनमें आनेवाले सुख-दुःखादिका अनुमानकर उसे अपने कर्तव्योंद्वारा अपने अनुकूल बनानेके लिये प्रेरित करना है। यही प्रेरणा मानवके लिये दुःखविघातक एवं पुरुषार्थसाधक होती है ।
'ज्योतिःशास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते।'
(सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय गोलप्रशंसा ६)
ज्योतिषशास्त्र के मुख्यतया सिद्धान्त, होरा एवं संहिता - ये तीन स्कन्ध हैं। सिद्धान्तस्कन्ध गणितात्मक है। इसमें मुख्यतया ग्रहों की गति, स्थिति, दिग्देश एवं कालगणन विषय की विवेचना प्राप्त होती है। ग्रहों के प्रभाव का अध्ययनकर शुभाशुभफल निरूपण होरा एवं संहिता का वर्ण्य विषय है।
मुख्यतया काल को आधार बनाकर फलविवेचना के लिये जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुण्डली का निर्माण किया जाता है। जन्मकुण्डली के द्वादश भावों में स्थित ग्रहों के परस्पर सम्बन्धादि का विचारकर वैयक्तिक फल का विवेचन होरास्कन्ध में किया जाता है। समष्टिगत फल का विवेचन संहितास्कन्ध में प्राप्त होता है। संहितास्कन्ध में शकुन, वास्तुप्रभृति विषय भी आते हैं। इस प्रकार मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर समुचित मार्गदर्शन देना ज्योतिषशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है।
होरास्कन्ध - अर्थ एवं प्रयोजन - मानवजीवन के सुख-दुःख, इष्टानिष्ट आदि सभी शुभाशुभ विषयों का विवेचन करने वाला शास्त्र ही होरा शास्त्र है । होरा शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र शब्दसे हुई है। अहोरात्र शब्द के प्रथम एवं अन्तिम अक्षर का लोप करने पर 'होरा' शब्द निष्पन्न होता है। एक राशि में २ होराएँ होती हैं। सम्पूर्ण अहोरात्र में क्रान्तिवृत्तस्थ १२ राशियों का स्पर्श पूर्वक्षितिज में हो जाता है, जिस कारण १२ लग्न एक दिन-रात में होते हैं। अतः १२ लग्नों की २४ होराएँ होती हैं। वस्तुतः जन्मकुण्डली में लग्न का अत्यधिक महत्त्व है। साथ ही सूक्ष्म विवेचन हेतु होरा-कुण्डली का भी विचार किया जाता है। बृहज्जा तक की होराभिप्राय- निर्णयटीका के अनुसार अहोरात्र का - मेषादि राशि भेदों का अर्थात् सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांशादिकों की प्राणपर्यन्त होरा संज्ञा है। इसी आधार पर इसे होराशास्त्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। होराशास्त्र का दूसरा नाम जातकशास्त्र भी है।
वैदिक दर्शन की पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार मनुष्य निरन्तर शुभाशुभ कर्मों में निरत रहता है। 'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्' इस सूक्ति के अनुसार उसे कर्मों का फल अवश्य भोगना है, परंतु एक साथ ही या एक ही जन्म में समस्त कर्मों का फल मिलना सम्भव नहीं है, अतः उसे अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं, जिसमें वह अपने किये कर्मों का फल भोगता है। इस प्रकार कर्मों के विपाक के तीन भेद बन जाते हैं -संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण। किसी भी प्राणीद्वारा वर्तमान क्षण तक किया समस्त कर्म, चाहे वह इस जन्म का हो अथवा पूर्व जन्मों का, संचित कर्म है। इसका फलविवेचन जन्मकुण्डली में योगायोग विचार से किया जाता है। जैसे- राजयोग, दरिद्रयोग आदि । अनेक जन्म-जन्मान्तरों के संचित कर्मों का फल एक साथ भोगना सम्भव नहीं है।
अतः संचित कर्मों में से जितने कर्मों के फल को प्राणी पहले भोगना आरम्भ करता है, वह प्रारब्ध या भाग्य कहलाता है। इसका विवेचन ज्योतिष में दशाविचार से होता है। जो कर्म अभी हो रहा है या किया जा रहा है, इसका विवेचन अष्टकवर्गके आधारपर गोचर अथवा तात्कालिक ग्रहस्थित्यनुसार किया जाता है। इस प्रकार ज्योतिषशास्त्र का यह स्कन्ध जन्मकुण्डली की ग्रहस्थिति के आधार पर मनुष्य के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों में किये गये शुभाशुभ कर्मो के विपाक को जातक के शुभाशुभ फल के रूप में प्रकाशित करता है।
इसलिये आचार्य वराहमिहिरका कथन है कि यह शास्त्र मनुष्य के लिये उसी प्रकार पथनिर्देशन का कार्य करता है, जैसे गहन अन्धकारमें दीपक ।
अतः होराशास्त्रका प्रयोजन ग्रहनक्षत्रों की गति- स्थित्यनुसार कुण्डली का निर्माणकर जातक के जीवन में आने वाले सुख-दुःखादि का अनुमान कर उसे अपने कर्तव्यों द्वारा अपने अनुकूल बनाने के लिये प्रेरित करना है।
होरास्कन्ध का वर्ण्य - विषय - होरास्कन्ध में मुख्य- तया ग्रह एवं राशियों का स्वरूप वर्णन, ग्रहों की दृष्टि, उच्च-नीच, मित्रामित्र, बलाबल आदिका विचार, द्वादश भावों द्वारा विचारणीय विषय एवं उनमें स्थित ग्रहों का शुभाशुभ फलविवेचन, जातक का अरिष्टविचार, वियोनि- जन्मविचार, राजयोग, प्रव्रज्यायोग, दरिद्रयोग आदि अनेक विध शुभाशुभ योगविचार, सूर्यकृत योग, चन्द्रकृत योग, नाभसयोग, आयुर्दायविचार, अष्टकवर्ग विचार, होरा- सप्तमांशादि दशवर्ग-साधन, ग्रहविंशोपकादि बलसाधन, विंशोत्तरी आदि दशान्तर्दशादि का साधन, नक्षत्रादिजनन- फलविचार आदि विषय सम्मिलित हैं। वस्तुतः होराशास्त्र के विभिन्न मानक ग्रन्थों में एक समानरूप से उपर्युक्त सभी विषय न होकर न्यूनाधिक रूप में प्राप्त होते हैं। वर्ण्य-विषय में न्यूनाधिकत्व होते हुए भी सभी का मुख्य उद्देश्य व्यष्टिगत फलविवेचन अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं तदनुसार दशा इत्यादि के आधार पर शुभाशुभ फलकथन करना है। बृहत्संहिता के सांवत्सर- सूत्राध्याय में होराशास्त्र के वर्ण्य विषय विशद रूपसे वर्णित हैं।
होरास्कन्ध का उद्भव एवं विकास - भारतीय त्रिस्कन्धात्मक ज्योतिषशास्त्र की अवधारणा को वैदिक काल से ही अनुभव किया जा सकता है। वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं। यद्यपि इनका वर्ण्य विषय ज्योतिष नहीं है, परंतु इनमें प्रसंगवश उपलब्ध व्यावहारिक ज्योतिषीय वर्णन तत्कालीन उत्कृष्ट ज्योतिषीय ज्ञानका परिचायक है। 'प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शनम्' एवं 'यादसे गणकम्' - जैसे मन्त्र उस समय के ज्योतिर्विदों के महत्त्व को द्योतित करते हैं।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में कुछ ज्योतिर्विद् ऋषियों के नामों का वर्णन मिलता है। नारदसंहिता, कश्यपसंहिता आदि में वसिष्ठ, अत्रि, नारद, पराशर, कश्यप, गर्ग आदि ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक १८ ( मतान्तरसे १९) ऋषियों के नाम प्राप्त होते हैं।
ये सभी आचार्य त्रिस्कन्धज्योतिर्विद् थे। इनमें से कुछ आचार्यों के ग्रन्थ आज भी प्राप्त हैं। यथा-महर्षि पराशरकृत बृहत्पाराशरहोराशास्त्र, नारदकृत नारदसंहिता एवं नारदीय ज्योतिष, काश्यपसंहिता, वसिष्ठसंहिता, सूर्यसिद्धान्त इत्यादि, परंतु आश्चर्य है कि इनमें वेदांग- ज्योतिष के प्रणेता लगधमुनि का नाम नहीं है। इस प्रकार त्रिस्कन्धज्योतिषशास्त्र की प्राचीन वैदिक परम्परा अभिलक्षित होती है, परंतु यह परम्परा प्रायः आचार्य वराहमिहिर से पूर्व खण्डित एवं लुप्तप्राय अनुभूत होती है। यवनों ने भारतीय ज्योतिष के साथ अपनी पद्धति का समन्वयकर एक नयी पद्धति 'ताजिकशास्त्र' को प्रस्तुत किया, जिसमें जातक पद्धति के समान ही वर्ष प्रवेश लग्न के आधार पर वर्ष भर का शुभाशुभ फल विवेचित किया जाता है। आचार्य वराहमिहिर ने यवनों के ज्योतिषज्ञान की प्रशंसा में कहा है-
"म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम्।
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्दैवविद्विजः ॥"
(बृहत्संहिता २।१५)
वराहमिहिर एवं उनके पश्चाद्वर्ती जातकशास्त्र के मानक ग्रन्थोंमें यवनों का प्रभाव स्पष्टरूप से परिलक्षित होता है।
होराशास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं ग्रन्थ- होरास्कन्धपर ऋषि जैमिनिकृत 'जैमिनिसूत्रम्' ग्रन्थ है, जो अपनी सूत्रपद्धति के द्वारा फलकथन हेतु प्रसिद्ध है। पराशरमुनिकृत बृहत्पाराशर होरा शास्त्र को होरास्कन्ध का सम्पूर्ण ज्ञान कराने वाला ग्रन्थ कहा जा सकता है। इनका 'लघुपाराशरी' नामक अन्य ग्रन्थ भी समुपलब्ध है। आचार्य वराहमिहिररचित 'बृहज्जातक' एवं 'लघुजातक' अप्रतिम ग्रन्थ हैं। बृहज्जातक को होराशास्त्र का प्रतिनिधिभूत ग्रन्थ कहा जा सकता है, जिसपर भट्टोत्पल (नवीं शताब्दी शककाल ) - द्वारा की गयी टीका अत्यन्त उत्कृष्ट है। इनके ग्रन्थों में मय, यवन, शक्ति, जीवशर्मा, मणित्थ, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, सत्याचार्य आदि पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। आचार्य कल्याणवर्माकृत सारावली (५५७ ई०), आचार्य वराहमिहिर के पुत्र पृथुयशाकृत षट्पंचाशिका, चन्द्रसेनकृत केवल ज्ञान होरा, श्रीपतिविरचित श्रीपतिपद्धति, रत्नावली, रत्नमाला एवं रत्नसार; बल्लालसेनरचित अद्भुतसागर, पद्मसूरिकृत भुवनदीपक, केशवरचित जातकपद्धति एवं ताजिकपद्धति, ढुण्ढिराजविरचित जातका भरण, वैद्यनाथकृत जातकपारिजात, नीलकण्ठरचित ताजिकनीलकण्ठी, महिमोदयकृत ज्योतिषरत्नाकर, गणेशकृत जातकालंकार इत्यादि ग्रन्थ होराशास्त्रमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त भी फलितज्योतिषके कई प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती आचार्योंके मतानुसार नवीन प्रकारसे ग्रन्थोंकी रचना की।
होरास्कन्धकी आवश्यकता एवं लोकोप- योगिता - कुछ विद्वानोंका कथन है कि जब पूर्वजन्मार्जित शुभाशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति अवश्यम्भावी है तो उसका ज्ञान कराने वाले होरास्कन्ध की क्या आवश्यकता ? क्योंकि जो होना है, वह तो होकर ही रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। सम्पूर्णरूप से भाग्य के भरोसे बैठकर ही यदि कृषक खेती करना छोड़ दे तो अन्नादि की उत्पत्ति कैसे होगी? नीतिवचनों में भी कहा गया है- 'न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ।' होराशास्त्र तो कर्मप्रधान शास्त्र है, जो पूर्वजन्मार्जित कर्मों के फल को क्रियमाण कर्म के द्वारा न्यूनाधिक करने में विश्वास रखता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि यदि होराशास्त्र के द्वारा कर्मविपाक को न्यूनाधिक किया जा सकता है तो श्रीराम, युधिष्ठिर-जैसे शक्तिमान् एवं सामर्थ्यशाली व्यक्तियोंको दुःख नहीं भोगना पड़ता अथवा होराशास्त्र के द्वारा भविष्यफल जानकर किसी को भी कभी दुःख नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ कर्मों की विचित्रता को ध्यान में रखना होगा। कुछ कर्म दृढ़ या स्थिर होते हैं तथा कुछ शिथिलमूलक या उत्पातसंज्ञक ।
अतः जहाँपर जन्म पत्रिकादि से दशाफलकालक्रम द्वारा रोग सम्भावना या अरिष्ट की सम्भावना है अथवा जब सन्तान, विद्या, धनादिका अभाव होने का कारण प्रकट होता है, वहाँ ग्रहशान्ति, मणिधारण, मन्त्रजप, दान, औषधिधारण आदि उपचारों से प्रतिबन्धक योगों को शिथिल करनेका प्रयास किया जा सकता है। जिस प्रकार दृढमूलवृक्ष भी प्रबल झंझावात से हिलकर जीर्ण या कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार दृढ़कर्मों का अशुभ फल भी कम तो अवश्य किया जा सकता है। इसीलिये सूक्ति है- 'हन्यते दुर्बलं दैवं पौरुषेण विपश्चिता' (होरारत्न)। शुभाशुभफलप्रद भाग्य कब फलीभूत होगा ? अपना पूर्ण फल देगा अथवा कुछ कम ? इत्यादिका ज्ञान भी होराशास्त्र से ही सम्भावित है। यह शास्त्र शुभाशुभफल-विपाक को जन्मकुण्डली के लग्नादि द्वादशभावों में स्थित स्वोच्च, मूलत्रिकोण, स्वगृह, मित्रगृहादि शुभ स्थानों अथवा शत्रुगृह, नीचगृह, अस्तादि अशुभ स्थानों या स्थितियों में स्थित नवग्रहों के परस्पर शुभाशुभ सम्बन्धों क आधार पर दशान्तर्दशादि के माध्यम से दिन, पक्ष, मास, वर्षादि के रूप में सूचित करता है। इसके आधार पर शुभाशुभफल विपाक समय में मनुष्य यथासम्भव जागरूक होकर मणि, मन्त्र, औषधि आदि उपायों से अशुभफल को न्यून तथा शुभ ग्रह के बल में वृद्धि करके सत्फल प्राप्त कर सकता है। इसीलिये कल्याण वर्मा का देवलों के लिये निर्देश है-
"विधात्रा लिखिता यस्य ललाटेऽक्षरमालिका।
देवज्ञस्तां पठेत् प्राज्ञः होरानिर्मलचक्षुषा।।"
(सारावली २।१)
होराशास्वके जानसे मनुष्य भावी सुख-दुःखादिका ज्ञानकर अपने पौरुषसे उसे अनुकूल बना सकता है। यह शास्त्र मनोवैज्ञानिक रूपसे उसे दुःखादि अशुभ परिस्थितियोंको झेलनेमें सम्बल प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणिमात्रपर पड़नेवाले शुभाशुभ प्रभावका अध्ययनकर फलकथन करना एवं मानवजीवनसे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओंका अध्ययनकर उसे समुचित मार्गदर्शन देना ही होराशास्त्रकी लोकोपयोगिताको सिद्ध करता है यह शास्त्र रोगके साध्यासाध्यत्वादिका निर्णय करके एवं उसके सम्भावित कालका अनुमान प्रस्तुतकर आयुर्वेदकी महान् सहायता करता है। इसी प्रकार जातककी अभिरुचि, दक्षता, स्वभावादिका विश्लेषण करके उसे भावी जीवनमें अपने कार्यक्षेत्रका चुनाव करनेमें सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः जातकशास्त्रकी लोकोपयोगिताको द्योतित करते हुए आचार्य कल्याणवर्माका कथन है-
"अर्थार्जने सहायः पुरुषाणामापदर्णवे पोतः ।
यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः ।।"
(सारावलीर २/५)
भारतीय वैदिक दर्शनमें 'कर्मवाद' का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार संसारमें प्राणी अनवरत कर्ममें ही निरत रहता है। वह चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकता है। कर्म करनेपर उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। आत्मा अजर एवं अमर है, परंतु कर्मबन्धनके फलस्वरूप उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्मबन्धनसे मुक्ति केवल तभी मिल सकती है, जब मनुष्यको आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान हो जाता है। प्राणीके शुभाशुभकर्मो का फल उसे वर्तमान जीवनमें कब, कहाँ और किस रूपमें प्राप्त होगा, इत्यादि समस्त जिज्ञासाओंका उत्तर जाननेका एकमात्र उपकरण होराशास्त्र है। इसका मुख्य कार्य ग्रह- नक्षत्रोंकी गतिस्थित्यनुसार कुण्डलीका निर्माणकर जातकके जीवनमें आनेवाले सुख-दुःखादिका अनुमानकर उसे अपने कर्तव्योंद्वारा अपने अनुकूल बनानेके लिये प्रेरित करना है। यही प्रेरणा मानवके लिये दुःखविघातक एवं पुरुषार्थसाधक होती है ।
Related Posts
- ज्योतिष विज्ञान
- |
- 07 December 2025
जब विज्ञान और ज्योतिष मिलते हैं: क्वांटम टनलिंग का आध्यात्मिक रहस्य
0 Comments
Comments are not available.