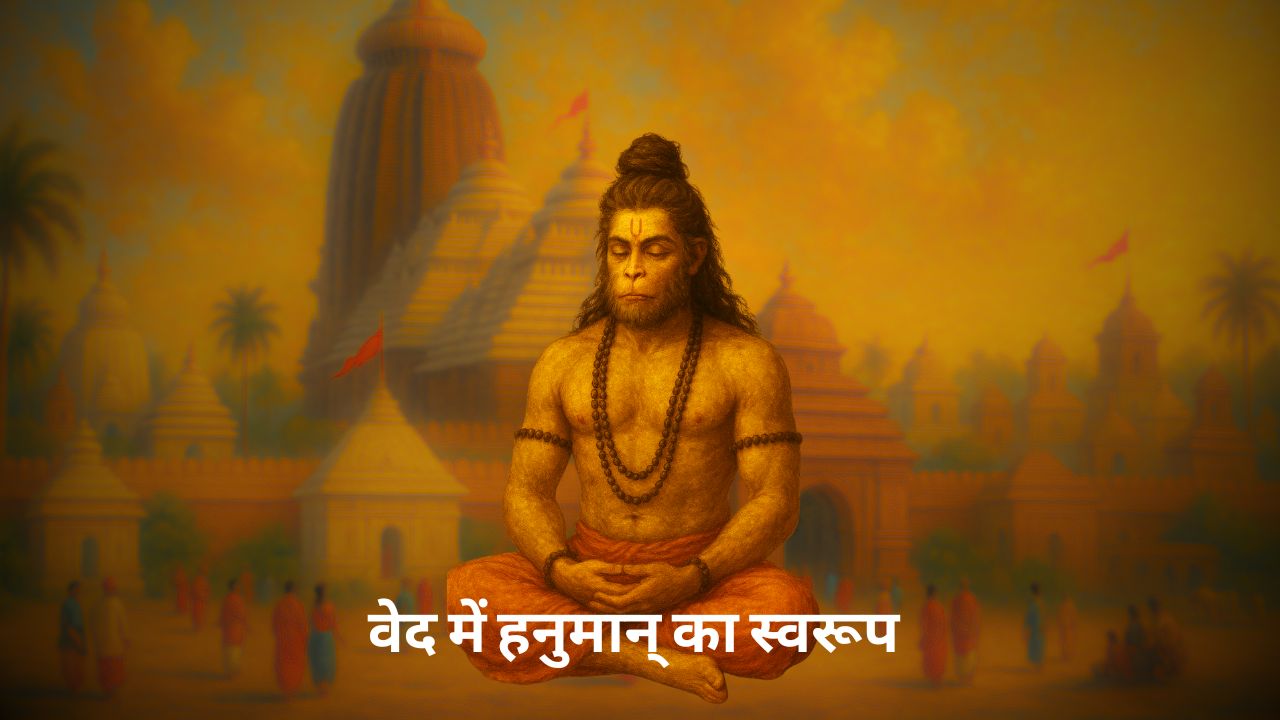- महापुरुष
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
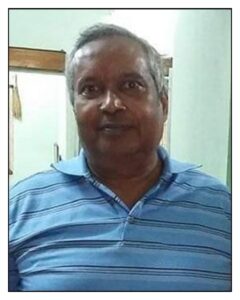
श्री अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)-
१. सृष्टि तत्त्व- काली कोई मनुष्य नहीं है, यह सृष्टि का तत्त्व है। इसे समझने के लिए रूप की कल्पना की गयी है। इसके रूपों का वर्णन महानिर्वाण तन्त्र में है- त्वं परा प्रकृतिः साक्षात् ब्रह्मणः परमात्मनः॥ (४/१०)
महत्तत्त्वादिभूतान्तं त्वया सृष्टमिदं जगत्। निमित्तमात्रं तद् ब्रह्म सर्वकारण कारणम्॥ (४/२६)
तस्येच्छा मात्रमालम्ब्य त्वं महायोगिनी परा। करोषि पासि हंस्यन्ते जगदेतच्चराचरम्॥ (४/२९)
कलनात् सर्वभूतानां महाकालः प्रकीर्त्तितः। महाकालस्य कलनात् त्वमाद्या कालिका परा॥ (४/३१
) कालत्वादादिभूतत्त्वादाद्या कालीति गीयते॥ (४/३२)
ध्यानं तु द्विविधं प्रोक्तं स्वरूपारूपभेदतः। स्वरूपं तव यद् ध्यानं अवाङ्-मनस-गोचरम्॥ (५/१३७)
मनसो धारणार्थाय शीघ्रं स्वाभीष्टसिद्धये। सूक्ष्मध्यान प्रबोधाय स्थूल ध्यानं वदामि ते॥(५/१३९)
अरूपायाः कालिकायाः काल मातुर्महा द्युतेः। गुण-क्रियानुसारेण क्रियते रूप कल्पना॥ (५/१४०)
उपासकानां कार्याय पुरैव कथितं प्रिये। गुण-क्रियानुसारेण रूपं देव्याः प्रकल्पितम्॥ (१३/४)
श्वेत-पीतादिको वर्णो यथा कृष्णे विलीयते। प्रविशन्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि शैलजे॥ (१३/५)
अतस्तस्याः कालशक्ते-र्निर्गुणाया निराकृतेः। हितायाः प्राप्तयोगानां वर्णः कृष्णो निरूपितः॥ (१३/६)
नित्यायाः कालरूपाया अव्ययायाः शिवात्मनः। अमृतत्त्वात् ललाटेऽस्याः शशिचिह्नं निरूपितम्॥ (१३/७)
शशिसूर्याग्निभिर्नित्यै-रखिलं कालिकं जगत्। सम्पश्यति यतस्तस्मात् कल्पितं नयनत्रयम्॥ (१३/८)
ग्रसनात् सर्व भूतानां कालदन्तेन चर्वणात्। तद्-रक्त संघो देवेश्या वासो रूपेण भाषितम्॥ (१३/९)
समये समये जीवरक्षणं विपदः शिवे। प्रेरणं स्वस्व कार्येषु वरश्चाभयमीरितम्॥ (१३/१०) (महानिर्वाण तन्त्र में शिव द्वारा पार्वती को उपदेश)
२. परा प्रकृति- यह महत्तत्त्व आदि क्रम से सृष्टि आरम्भ करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥ (गीता, ९/१०)
प्रकृति की इच्छा से सृष्टि तथा उसी में लय होता है। यही ब्रह्म की परिभाषा भी है कि जिससे जगत् की उत्पत्ति सृष्टि, लय आदि हो। जन्माद्यस्य यतः (ब्रह्म सूत्र, १/१/२)
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येने जातानि जीवन्ति। यत् प्रयन्त्यभिसंवसन्त्। तद् विजिज्ञासस्व। तद् ब्रह्मेति (तैत्तिरीय उपनिषद्, ३/१/१)
एक ही ब्रह्म सृष्टि के लिए २ भाग में बंट जाता है-पुरुष और प्रकृति। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्॥ (गीता, १३/१९)
द्विधा कृताऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्। अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः॥ (मनु स्मृति, १/३२) 
३. काली रूप- सभी भूतों का कलन (ग्रास) करने वाला महाकाल (शिव का एक रूप) है, उस महाकाल का भी जो कलन करे वह कालिका है (महानिर्वाण तन्त्र, ४/३१) ब्रह्म से सृष्टि का वर्णन हो चुका है। लय रूप में काली हैं। परिवर्तन का आभास काल है।
परिवर्तन क्या है- किसी स्थान पर एक वस्तु थी, वह अन्य स्थान पर चली गयी-यह गति या क्रिया है। एक वस्तु जिस रूप में थी, वह अन्य रूप में दीखती है। कई वस्तुओं का संग्रह एक स्थिति में था, अन्य स्थिति में दीखता है।
इनको परिणाम, पृथक् भाव या व्यवस्था क्रम कहा है-
परिणामः पृथग् भावो व्यवस्थाक्रमतः सदा। भूतैष्यद्वर्त्तमानात्मा कालरूपो विभाव्यते॥ (सांख्य कारिका, मृगेन्द्रवृत्ति दीपिका, १०/१४)
इस प्रकार देश-काल-पात्र या ज्योतिष में दिक्-देश-काल परस्पर सम्बन्धित हैं। दिक्कालावकाशादिभ्यः (कपिल सांख्य सूत्र, २/१२) सूर्य सिद्धान्त (१/१०) में २ प्रकार के काल कहे गये हैं-
अन्तकृत् या नित्य काल, कलनात्मक या जन्य। लोकानामन्तकृत् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते॥१०॥
नित्य काल लोकों का क्षय करता है तथा अन्त में समाप्त करता है। विश्व का स्थूल रूपों का सदा क्षय होता रहता है, उसे अक्षर पुरुष कहा है। इसका काल नित्य काल या मृत्यु है। कालोऽस्मि लोक क्षयकृत्प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिहप्रवृत्तः। (गीता, १०/३२)
यह कर्त्ता रूप या अक्षर पुरुष का काल है। काल की गणना सबसे कठिन है क्यों कि काल की गति दर्शक के अनुसार भिन्न भिन्न होती है (सापेक्षवाद, या योगवासिष्ठ में मण्डप उपाख्यान)।
एक बार जो चला गया, वह पुनः नहीं आता। किन्तु यज्ञ द्वारा उत्पादन क्रम चक्र में चलता है। प्राकृतिक चक्र हैं-दिन, मास, वर्ष जिनके अनुसार यज्ञ होते हैं। प्राकृतिक या यान्त्रिक चक्रों से काल की माप होती है। यह काल जन्य (जनन चक्र) तथा कलनात्मक (गणना योग्य) है। कालः कलयतामहम्। (गीता, १०/३०)
विश्व पुरुष या काल के २ अन्य रूप भी हैं- पूरे विश्व या उसके स्वतन्त्र भाग को देखें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता-भौतिक विज्ञान में ५ प्रकार के संरक्षण सिद्धान्त हैं। इसे अव्यय पुरुष कहते हैं, जिसे निर्माण चक्र के वृक्ष रूप में भी कहा है। इसका अक्षय काल है जो धाता तथा विश्व का स्रोत (मुख) है।
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः (गीता, १०/३३) बहुत सूक्ष्म विश्व या उसके परिवर्तन का आभास नहीं होता (भागवत पुराण, ३/११/२-३)।
यह परात्पर पुरुष का काल है, जिसका भेद रहित होने के कारण वर्णन सम्भव नहीं है। किसी भी विन्दु को देखने पर धीरे धीरे क्षय होते हुए समाप्त हो जाता है, वह नित्य काल या मृत्यु है। उसके महः (परिवेश) का काल महाकाल है जो ज्ञान रूप शिव का एक स्वरूप है। पूरे विश्व का लय होने पर कुछ पता नहीं चलता। वह परात्पर काल या महा-काली है। महाकाल जिस क्षेत्र में वर्तमान है, वह महाकाली है।
४. रूप कल्पना- विश्व के गुणों को समझने के लिए उसके अनुसार मूर्ति बनाते हैं। मनुष्य विश्व का प्रतिरूप है (बाइबिल, जेनेसिस, १/२७ में भी)। इसे वेद में कई प्रकार से समझाया गया है-आत्मा-परमात्मा का ऐक्य, विश्व तथा मनुष्य के समान अंग, ब्रह्माण्ड तथा मनुष्य के कणों की समान १०० अरब संख्या (शतपथ ब्राह्मण, १२/३/२/५, १०/४/४/२),
व्यक्ति-विश्व पुरुष (पुरुष सूक्त)। विश्व का स्रोत में लय होने पर अन्धकार होता है अतः इसे काली स्त्री के रूप में बनाते हैं।। काले रंग में सभी रंग भी लीन हो जाते हैं। आसीदिदं तमोभूतं-अप्रज्ञातं-अलक्षणम्। अप्रतर्क्यम्-अविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥ (मनु स्मृति, १/५)
तम आसीत्, तमसा गूळ्हमग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्व मा इदम्। (नासदीय सूक्त, ऋक्, १०/१२९/३)
बिना किसी आकार के उसका ध्यान नहीं होता, अतः विश्व की अपनी कल्पना अनुसार रूप कल्पना कर ध्यान करते हैं। रूपों के परिवर्तन या भेद के बीच में शून्य स्थिति आती है, जो निराकार ध्यान या निर्विकल्प समाधि है। विश्व का ग्रास करने वाले स्रोत की कल्पना के लिए काली का फैला हुआ मुख तथा लम्बी जिह्वा बनाते हैं।
४ दिशा या ४ वेद (मूर्ति रूप ऋक्, गति रूप यजु, महिमा रूप साम, ब्रह्म रूप अथर्व) रूप में काली के ४ हाथ बनाते हैं। विश्व का शब्द रूप में वर्णन शब्द वेद है जिसे चण्डी पाठ (४/५) में देवी रूप कहा है। शब्दों के लिए अ से क्ष तक के अक्षरों का प्रयोग है। अ से ह तक देवनागरी के ४९ अक्षर ४९ मरुत् हैं, इसके ३३ स्वर वर्ण ३३ देवों के चिह्न हैं, अतः यह चिह्न रूप में देवनगर है। ’अ’ से ह तक शरीर या विश्व हुआ, उसे जानने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जिसे अहं कहते हैं। अतः क्षेत्रज्ञ रूप में ’ह’ के बाद ३ अक्षर-क्ष, त्र, ज्ञ-जोड़ते हैं।
शरीर के सुषुम्ना के ६ चक्रों में ५० वर्ण अ से क्ष तक हैं। यह ’अक्ष-माला’ है। इसका अन्त मस्तिष्क केन्द्र आज्ञा-चक्र में होता है, अतः अक्ष माला रूप में काली ५० मुण्डों की माला पहनती हैं। विश्व के लय या समाप्ति रूप में उनको श्मशान वासिनी कहा गया है। कुछ दृश्य नहीं होने के कारण वे दिगम्बर हैं तथा ४ दिशायें उनके ४ हाथ हैं।
शवारूढां महाभीमां घोरदंष्ट्रां हसन्मुखीम्। चतुर्भुजां खड्गमुण्डवराभयकरां शिवाम्॥१॥
मुण्डमालाधरां देवीं ललज्जिह्वां दिगम्बराम्। एवं सञ्चिन्तयेत् कालीं श्मशानालय वासिनीम्॥२॥ (शाक्त प्रमोद, काली तन्त्र)
५. सौम्यरूप दक्षिणा काली- लय के बाद पुनः सृष्टि का आरम्भ होता है। उसके बाद वाक्-अर्थ (शब्द-विश्व) का विस्तार होता है, अतः चण्डी पाठ के महाकाली चरित्र के बाद ध्यान में अक्ष माला का उल्लेख है-
अक्ष-स्रक्-परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम्। महाकाली चरित्र में विश्व की लय स्थिति को सुप्त कहा गया है। उसके बाद निर्माण का आरम्भ शिव या कल्याणकारी रूप कहा गया है। इसके अनुसार योग-निद्रा में सुप्त देव रूप को विष्णु तथा जाग्रत रूप को जगन्नाथ कहा गया है। निर्माण या सौम्य रूप दक्षिणा काली है, उसका पुरुष रूप जगन्नाथ है।
(१) सुप्त रूप-महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः॥५४॥ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तदा विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्॥५६॥ उत्पन्नेति सदा लोके सानित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवी कृते॥६६॥ निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥७१॥
(२) जाग्रत रूप- यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत् पात्यत्ति यो जगत्॥८३॥
प्रबोधं च जगत् स्वामी नीयतां अच्युतो लघु॥८६॥
उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः॥९१॥
सौर मण्डल का केन्द्र सूर्य आकर्षण द्वारा ग्रहों को धारण करता है, जो विष्णु रूप है। उससे निर्गत ऊर्जा इन्द्र है जो शून्य में भी वर्तमान है। ऊर्जा द्वारा जीवन का पालन या जगत् की आत्मा रूप में जगन्नाथ है।
पृथिवी त्वया धृता लोका देवि! त्वं विष्णुना धृता। (भूमि पूजन मन्त्र)
नेन्द्रात् ऋते पवते धाम किं च न (ऋक्, ९/६९/६, सामवेद, २/७२०)
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (ऋक्, ६/४७/१८)
इन्द्रश्च विष्णो यद् अपस्पृधेथाम् (ऋक्, ६/६९/८, अथर्व, ७/४४/१)
-इन्द्र विष्णु की स्पर्धा, विष्णु आकर्षण करता है, इन्द्र के तेज का विकिरण होता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋक्, १/११५/१, अथर्व, १३/२/३५, २०/१०७/१४, वाज. यजु, ७/४२, १३/४६) (विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ३/३४/२०-२१) ६. सृष्टि नृत्य- (१) नृत्य अर्थ- सृष्टि का स्रोत अप् है जो समुद्र जैसा ३ धामों के आकाश मे फैला हुआ है। अप् में पदार्थों के मिश्रण से नये पदार्थ बनते हैं। मिश्रण की गति को मातरिश्वा वायु कहते हैं, क्योंकि यह माता समान गर्भ में सृष्टि करता है।
तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति (ईशावास्योपनिषद्, ४) मातरिश्वा का लय नृत्य है। उदुस्रिया जनिता यो जजाना-अपां गर्भो नृतमो यह्वो अग्निः (ऋक्, ३/१/१२) नृत्य की शक्ति का स्रोत आकाश में फैली इन्द्र शक्ति है- पपृक्षेण्यमिन्द्र त्वे ह्योजो नृम्णानि च नृतमानो अमर्तः (ऋक्, ५/३३/६) तवत्यं नर्यं नृतो अप (ऋक्, २/२२/४, साम, १/४६६) ईशे कृष्टीनां नृतुः (ऋक्, ८/६८/७) सांख्य में सृष्टि कार्य को प्रकृति का नृत्य कहा गया है- रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः॥ (सांख्य कारिका, ५९)
जिस प्रकार कोई नर्तकी रङ्गस्थ दर्शकों के समक्ष नृत्य करने के बाद पुनः नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकाशित करने के बाद निवृत्त हो जाती है।
(२) रास- सृष्टि नृत्य मुख्यतः २ प्रकार के हैं-जिनसे सम्भूति-असम्भूति होती है (ईशावास्योपनिषद्, ९-११) रास द्वारा निर्माण होता है। इससे यज्ञ चक्रों में सृष्टि होती है। कई प्रकार के चक्र हैं-मन्वन्तर काल में ब्रह्माण्ड का अक्ष भ्रमण, पृथ्वी अक्ष का अयन चक्र, सौर वर्ष, चान्द्र मास, दैनिक गति। समन्वित गति से निर्माण होता है। ब्रह्म-वैवर्त्त पुराण अध्याय (१/५) में रास मण्डल से सृष्टि का वर्णन है।
अन्य उदाहरण- तन्नोदेवासोअनुजानन्तुकामम् .... दूरमस्मच्छत्रवोयन्तुभीताः।
तदिन्द्राग्नी कृणुतां तद्विशाखे, तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम्। नक्षत्राणां अधिपत्नी विशाखे, श्रेष्ठाविन्द्राग्नी भुवनस्य गोपौ॥११॥
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तात्, उन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय।
तस्यां देवा अधिसंवसन्तः, उत्तमे नाक इह मादयन्ताम्॥१२॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१/१) =
देव कामना पूर्ण करते हैं, इन्द्राग्नि (कृत्तिका) से विशाखा (नक्षत्रों की पत्नी) तक बढ़ते हैं। तब वे पूर्ण होते हैं, जो पूर्णमासी है। तब विपरीत गति आरम्भ होती है। यह गति नाक कॆ चारो तरफ है। इसे ब्रह्माण्ड पुराण में मन्वन्तर काल कहा है, जो इतिहास का मन्वन्तर है।
स वै स्वायम्भुवः पूर्वम् पुरुषो मनुरुच्यते॥३६॥
तस्यैक सप्तति युगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥३७॥ (ब्रह्माण्ड पुराण, १/२/९)
पृथ्वी पर भी वार्षिक रास कार्त्तिक पूर्णिमा से आरम्भ होता है। इसके बाद भगवान् ४ मास शयन के बाद उठते हैं। भागवत:-इत्थं शरत्स्वच्छ जलं स गो गोपालकोऽच्युत: । (१०/२१/१) हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द व्रज कुमारिका:। (१०/२२/१) राधा-कृष्ण तत्त्व का यही वर्णन वेद में हैं। ऋग्वेद में परिभाषा है-
राध्नोति सकलान् कामान् तेन राधेति सा स्मृता स्तोत्रं राधानां पते। (ऋक्, १/३०/५) अन्य वर्णन हैं (ऋक्, १/१०/७, १/३२/११, ३/१५/३, ८/९३/१३, १०/२१/३, १/१५/५, १/४२/७, १/१७/१, १/१७/७, १/८/१८, १/१२१/५, १/६२/८, १/१४१/७,८; १/१४०/३; १/२२/७, १/१३४/४ आदि) पुराण तथा वेद में रास द्वारा सृष्टि वर्णन एक ही है, पुराणों में देश-काल की माप भी है। देवीभागवत पुराण, स्कन्ध ९, अध्याय २-
तदा वव्रे श्रमजलं तत्सर्वं विश्वगोलकम्॥४०॥
बभूवुरेषा तत्पुत्रा अधः प्राणाश्च पञ्च च॥४३॥
घर्मतोयाधिदेवश्च बभूव वरुणो महान्॥४४॥
शतमन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा॥४५॥
अध्याय३-तन्मध्ये शिशुरेकश्च शतकोटिरविप्रभः॥२॥
स्थूलात्स्थूलतमः सोऽपि नाम्ना देव् महाविराट्। परमाणुर्यथा सूक्ष्मात् परः स्थूलात्तथाप्यसौ॥४॥
प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च॥६॥
पुरुष सूक्त (यजु, ३१/१-१६, ऋक्, १०/९०/१-६) ततो विराट् अजायत, विराजो अधिपूरुषः (पुर से उसका अधिष्ठान पूरुष बड़ा है) गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, अध्याय १- तदैक्षत-द्वितीयं देव निर्माम् इति। -- सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदाद्र्यंम् अजायत --। (कण्डिका १)यत् समद्रवन्त तस्मात् समुद्र उच्यते। -- यच्च वृत्वा अतिष्ठन्तः-- एतं वरणं सन्तं वरुण इति आचक्षते। (कण्डिका ७)
(३) ताण्डव-ताण्डव नृत्य में समन्वय नहीं है, जिससे विनाश होता है। लिङ्ग पुराण, अध्याय (१/१०६) में असुर नाश के लिए शिव का ताण्डव वर्णन है। इसके लिए पार्वती का अंश उनके शरीर में प्रवेश कर विष ग्रहण कर नृत्य कर रहा था। स्कन्द पुराण, अध्याय (६/२५४) में आध्यात्मिक ताण्डव का वर्णन है जिससे शरीर के दोषों का नाश करते हैं। शत्रुनाश के लिए वीरभाव से ताण्डव होता है। शिव के ध्यान मन्त्र में इसे काल-आरभटी कहा गया है। तत् कालारभटी विजृम्भणपरित्रासादिवभ्रश्यता, वामार्धेन तदेकशेषकरणं बिभ्रद्वपुर्भैरवम्। तुल्यं चास्थिभुजङ्गभूषणमसौ भोगीन्द्रकङ्कालकै- -र्बिभ्राणः परमेश्वरो विजयते कल्पान्तमर्म्मान्तिकः॥ आरभट = वीर, साहसी। आरभटी = नाटक या नृत्य जिसके ४ प्रकार साहित्य दर्पण (४२०) में हैं- मायेन्द्र-जाल-संग्राम क्रोधोद्भ्रान्तादि चेष्टितैः। संयुक्ता वधबन्धनाद्यैरुद्धतारभटी मता। भास के स्वप्न वासवदत्ता नाटक में उदयन को छद्म हाथी द्वारा बान्धना भी आरभटी का उदाहरण कहा गया है। सदाशिव, अगस्त्य, परशुराम परम्परा से यह केरल में जीवित है, जिसे केरल युद्ध कला या कालारिपट्ट कहते हैं। यह कालारभट का अपभ्रंश है। केरल में प्रचलित होने के २ कारण हो सकते हैं-परशुराम का अन्तिम निवास स्थान शूर्पारक केरल-मंगलोर तट पर था, केरल का काली स्थान कालीकट (उच्चारण-कोझिकोड) है।
७. अग्नि-जिह्वा- प्रथम उत्पन्न (अग्रि) को परोक्ष में अग्नि कहा गया है। सृष्टि के लिए विरल पदार्थ घनीभूत होता है। घना पिण्ड या ऊर्जा (तीव्र ताप) अग्नि है।
अग्नि की ग्रास करने वाली ७ प्रकार की जिह्वा है जिनके नाम काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुची हैं। इनसे ही ७ लोक, ७ प्राण, शरीर के ७ गुहा आदि हुए हैं।
काली कराली च मनोजवा च, सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा।
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी, लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः॥ (१/२/४)
अग्नि-र्मूर्धा चक्षुषी चन्द्र-सूर्यौ, दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः।
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य, पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा॥ (२/१/४)
सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः।
सप्त इमे येषु चरन्ति प्राणा, गुहाशया निहिताः सप्त सप्त॥ (२/१/८) (मुण्डकोपनिषद्)
निकालने के लिए भी ७ जिह्वा है, जिनको अर्चि या अंगारा कहा है। दोनों मिला कर १४ जिह्वा हैं- अग्निजिह्वा मनवः (ऋक्, १/८९/७, वाज. यजु, २५/२०) मनु संख्या में १४ हैं। मन की भी १४ प्रवृत्ति हैं। योग सूत्र (२/२७) में ७ प्रज्ञा तथा अन्य में चित्त के उत्थान की ७ स्थिति कही गयी हैं।
८. त्रयी विद्या- (१) अज्ञेय ब्रह्म-अज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए उसे ३ भाग में समझते हैं-
ॐ तत्-सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः (गीता, १७/२३)
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च॥ (श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
पराशक्ति अज्ञेय है, उसे ज्ञान-बल-क्रिया रूपों में समझते हैं। हर त्रिवर्ग के बाद कुछ अविभक्त रह जाता है, अतः त्रयी का अर्थ ४ वेद है।
त्रयी विद्या हिङ्कारः, त्रय इमे लोकाः (छान्दोग्य उपनिषद्, २/२१/१) अविभक्तं विभक्तेषु (गीता, १८/२०)
त्रयी के नाम पर अंग्रेजों ने प्रचार किया कि पहले ३ वेद ऋक्-यजु-साम थे, बाद में अथर्व जोड़ा गया। किन्तु मूल वेद १ ही था जिसे अथर्व कहते थे। उसके मूर्ति-गति-महिमा रूप में ऋक्-यजु-साम विभाजन के बाद भी मूल बचा रहा, जिसे ब्रह्म या अथर्व वेद ही कहा गया। इसका प्रतीक पलास दण्ड है जिसका वेदारम्भ संस्कार में प्रयोग होता है-उसकी शाखा से ३ पत्ते निकलने के बाद शाखा भी बची रहती है।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठ- मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह॥१॥
द्वे विद्ये वेदितव्ये- ... परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डक उपनिषद्, १/१/१, ४, ५)
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः-(ऐतरेय ब्राह्मण, २/१)
(२) उदाहरण-ब्रह्म का वाचक ॐ है, जिसके ३ भाग हैं-अ, उ, म। उसके बाद पराशक्ति रूप अर्धमात्रा (अनुस्वार) बच जाती है। ॐ इति ब्रह्म (तैत्तिरीय उपनिषद्, १/८/१) ॐ इति तिस्रो मात्राः (मैत्रायणी उपनिषद्, ६/३) अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः (रात्रि सूक्त, ३, दुर्गा सप्तशती, १/७४) गायत्री मन्त्र के ३ पाद द्वारा ब्रह्म वर्णन के बाद भी अज्ञात परोरजा पद बच जाता है। परोरजसे असौ अदो मा प्रापत् इति (बृहदारण्यक उपनिषद्, ५/१४/७)
(३) देव या देवी-पिण्ड या विन्दु रूप पुरुष देव है, वह पुर या संरचना में रहता है। उसका क्षेत्र श्री या स्त्री रूप देवी है। यह मनुष्य याअन्य पशु में प्रजनन क्रिया के अर्थ का विस्तार है। जन्म माता के गर्भ में ही होता है, अतः क्षेत्र रूप स्त्री है। पुरुष का योगदान विन्दु मात्र है, अतः सीमाबद्ध पिण्ड रूप पुरुष है। दोनों के प्राण देव या देवी हैं। वेद में देवता शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि प्राण पिण्ड रूप में नहीं दीखता है। लोक भाषा में भी ऐसे ही लिंग विभाजन है-
१ केश पुल्लिंग है, उनका समूह या क्षेत्र चोटी, वेणी, मूंछ, दाढ़ी-ये सभी स्त्रीलिंग हैं। सैनिक पुल्लिंग है, किन्तु उनका समूह सेना, वाहिनी आदि स्त्रीलिंग हैं एक अन्य लक्षण है कि वृषा (वर्षा करने वाला, देने वाला जिससे विकिरण हो) वह पुरुष है। उसे ग्रहण करने वाला या युक्त होने वाला क्षेत्र योषा का अर्थ स्त्री है। अग्नि-सोम का भी ऐसा विभाजन है।
(४) त्रिवृत-३x३ भाग को त्रिवृत् या तिस्रस्त्रेधा कहा गया है। गायत्री मन्त्र के ३ पादों के पुनः ३-३ विभाग हैं। (१) भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ, (२) ऋक्, यजु, साम, (३) प्राण-अपान-व्यान। (बृहदारण्यक उपनिषद्, ५/१४/१-४) वेद में देवी के ३ रूपों का पुनः ३-३ विभाजन लिखा है- तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा। तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम्॥ (वाज. यजु, २०/६३) = सरस्वती, इळा, भारती (अश्विन् द्वारा)-ये ३ देवियां पुनः ३-३ में विभाजित हैं। इनको सोम अर्पण से इन्द्र (या इन्द्रिय) की पुष्टि होती है। इनको पुराण भाषा में काली, लक्ष्मी, सरस्वती कहा है। केवल ३ भाग होने पर इनको महा उपसर्ग से सूचित करते हैं। पुनः ३-३ भाग होने पर अव्यक्त स्रोत काली के साथ अन्य ९ महाविद्या हैं।
(५) गायत्री विभाग-गायत्री के ३ पाद कई प्रकार से त्रिभाग करते हैं- आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक ब्रह्मा-विष्णु-शिव (पलास-पिप्पल-वट) महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती ऋक्-यजु-साम अन्य भी प्रायः ५० विभाग वर्णित हैं। दुर्गा सप्तशती के ३ चरित्रों के अध्याय भी ३-३ भाग में हैं, १, ३, ९ अध्याय।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.