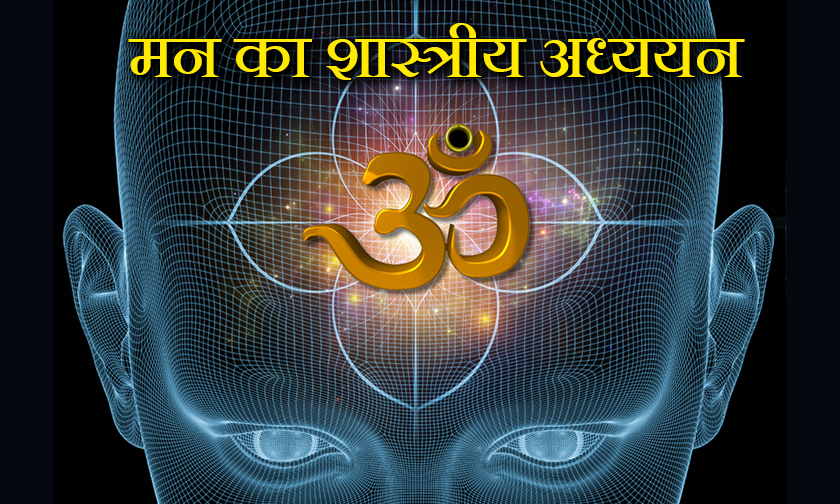- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
 श्री शशांक शेखर शुल्ब ( धर्मज्ञ )-
Mystic Power- मन की निरुक्ति...
" मन्यते बुध्यते अनेन इति मनः।"
अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वह 'मन' है। 'मन् ज्ञाने' धातु से मन शब्द निष्पन्न हुआ है। मन् धातु में असुन् प्रत्यय द्वारा मन या मनस् शब्द निर्मित होता है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान या बोधन क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु मन् से मन शब्द निर्मित हुआ है। मन की यह निरुक्ति उसके एकान्तिक कार्य ज्ञानोपलब्धि को रेखांकित करती है। आचार्य चरक ने 'जिसको उपस्थिति से ज्ञान का होना और अनुपस्थिति से ज्ञान का न होना' इस प्रकार मन का लक्षण वर्णित किया है।
"लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च।"
(च. शा. 1/18)
श्री शशांक शेखर शुल्ब ( धर्मज्ञ )-
Mystic Power- मन की निरुक्ति...
" मन्यते बुध्यते अनेन इति मनः।"
अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वह 'मन' है। 'मन् ज्ञाने' धातु से मन शब्द निष्पन्न हुआ है। मन् धातु में असुन् प्रत्यय द्वारा मन या मनस् शब्द निर्मित होता है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान या बोधन क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु मन् से मन शब्द निर्मित हुआ है। मन की यह निरुक्ति उसके एकान्तिक कार्य ज्ञानोपलब्धि को रेखांकित करती है। आचार्य चरक ने 'जिसको उपस्थिति से ज्ञान का होना और अनुपस्थिति से ज्ञान का न होना' इस प्रकार मन का लक्षण वर्णित किया है।
"लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च।"
(च. शा. 1/18)
 मन के पर्याय...
आयुर्वेदीय साहित्य में पर्यायों के द्वारा परिभाषा कथन की परम्परा है। जैसे- 'पर्यायैरायुरुच्यते', 'निदानमाहु पर्यायै' अथवा 'पर्यायैरुक्तमौषधम्' इत्यादि । मन के भी अनेक पर्याय आयुर्वेद एवं इतर प्राचीन वाङ्मय में वर्णित है। इन पर्यायों के स्वतन्त्र अर्थ भी है, परन्तु ये सब संयुक्त रूप से 'मन' के लिए प्रयुक्त है। आचार्य चरक ने अतीन्द्रिय, मन, सत्त्व, चेत आदि शब्द पर्याय रूप में उल्लिखित किये हैं।
"अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेत इत्याहुरेके ।"
(च. सू. 8/4)
अमरकोष में मन के पर्यायों में चित्त, चेत, हृदय, स्वान्त, हृद् मानस, मन आदि संगृहीत है-
"चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः।"
(अमरकोष)
इनके अतिरिक्त मनस्, अन्तःकरण, उभयेन्द्रिय, इन्द्रियातीत आदि पर्याय भी ( अमरकोष) मिलते है।
मन के पर्याय...
आयुर्वेदीय साहित्य में पर्यायों के द्वारा परिभाषा कथन की परम्परा है। जैसे- 'पर्यायैरायुरुच्यते', 'निदानमाहु पर्यायै' अथवा 'पर्यायैरुक्तमौषधम्' इत्यादि । मन के भी अनेक पर्याय आयुर्वेद एवं इतर प्राचीन वाङ्मय में वर्णित है। इन पर्यायों के स्वतन्त्र अर्थ भी है, परन्तु ये सब संयुक्त रूप से 'मन' के लिए प्रयुक्त है। आचार्य चरक ने अतीन्द्रिय, मन, सत्त्व, चेत आदि शब्द पर्याय रूप में उल्लिखित किये हैं।
"अतीन्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेत इत्याहुरेके ।"
(च. सू. 8/4)
अमरकोष में मन के पर्यायों में चित्त, चेत, हृदय, स्वान्त, हृद् मानस, मन आदि संगृहीत है-
"चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः।"
(अमरकोष)
इनके अतिरिक्त मनस्, अन्तःकरण, उभयेन्द्रिय, इन्द्रियातीत आदि पर्याय भी ( अमरकोष) मिलते है।
 मन की परिभाषा...
"सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः।"
(तर्कसंग्रह)
सुख, दुःख आदि की उपलब्धि का साधनभूत तत्त्व है-मन। दूसरे शब्दों में मन वह इन्द्रिय है जिससे सुख, दुःख आदि का ज्ञान होता है। सुख, दुःख की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने कहा है- 'अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्' अर्थात् जो भाव मन में अनुकूल है वह सुख और जो भाव मन के प्रतिकूल है वह दुःख । इससे स्पष्ट है कि सुख, दुःख आदि की प्रतीति मन द्वारा ही होती है; और जो सुख, दुःख आदि की उपलब्धि का साधन है वह मन है।
आचार्य चरक ने सुख, दुःख की बात न कर सम्पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि का साधन मन को माना है। उनके अनुसार जिसकी उपस्थिति से ज्ञान हो और अनुपस्थिति से ज्ञान न हो वही मन है। इस प्रकार ज्ञान का भाव (होना) और अभाव (न होना) मन के लक्षण हैं, उसके अस्तित्व की पहचान हैं। ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया के सम्पूर्ण साधन आत्मा, इन्द्रिय, अर्थ आदि की विद्यमानता रहते हुए भी मन का संयोग नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता है और संयोग होने पर ज्ञान होता है-
"लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च।
सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते।
वैवृत्त्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात् तच्च वर्तते ।"
(च. शा. 1/19)
मन इन्द्रियातीत है अर्थात् उसका प्रत्यक्षीकरण इन्द्रियों द्वारा नहीं होता है, अपितु उसके कार्यों से ही उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। इसलिए मन की सभी परिभाषाएँ उसके कार्यों पर आधारित है।
महर्षि चरक (च. शा. 2/31) के अनुसार मन की गति के कारण आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है—'मनोजवो देहमुपैति देहात्' । और मन के निकल जाने पर शील (स्वभाव) बदल जाता है, अभिरुचि नष्ट हो जाती है, सब इन्द्रियाँ कष्टपीड़ित होती है, बल का ह्रास हो जाता है, व्याधियाँ बढ़ जाती है, जिसके बिना प्राणों का त्याग हो जाता है और जो इन्द्रियों का अभिग्राहक प्रेरक है उसे मन कहते हैं-
"अस्ति खलु सत्त्वमौपपादुकं यज्जीवं स्पृक्शरीरेणाभिसम्बध्नाति, यस्मिन्नपगमन- पुरस्कृते शीलमस्य व्यावर्तते, भक्तिर्विपर्यस्यते, सर्वेन्द्रियाण्युपतप्यन्ते, बलं हीयते, व्याधय आप्यायन्ते यस्माद्धीनः प्राणाञ्जहाति, यदिन्द्रियाणामभिग्राहकं च 'मन' इत्यभिधी- यते; तत् त्रिविधमाख्यायते शुद्धं, राजसं, तामसमिति । येनास्य खलु मनो भूयिष्ठं, तेन द्वितीयायामाजातौ सम्प्रयोगो भवति यदा तु तेनैव शुद्धेन संयुज्यते, तदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति । स्मार्तं हि ज्ञानमात्मनस्तस्यैव मनसोऽनुबन्धादनुवर्तते, यस्यानुवृत्तिं पुरस्कृत्य पुरुषो 'जातिस्मर' इत्युच्यते । यानि खल्वस्य गर्भस्य सत्त्वजानि यान्यस्य सत्त्वतः सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः, तद्यथा-भक्तिः शीलं शौचं द्वेषः स्मृति- मोहस्त्यागो मात्सर्य शौर्य भयं क्रोधस्तन्द्रोत्साहस्तैक्ष्ण्यं मार्दवं गाम्भीर्यमनवस्थितत्वमित्येव- मादयश्चान्ये, ते सत्त्वविकारा, यानुत्तरकालं सत्त्वभेदमधिकृत्योपदेक्ष्यामः । नानाविधानि खलु सत्त्वानि तानि सर्वाण्येकपुरुषे भवन्ति, न च भवन्त्येककालम् एकं तु प्रायोवृत्त्याऽऽह ॥"
(च. शा. 3/13)
मन निश्चय शरीरान्तर के साथ सम्बन्ध करनेवाला है अर्थात् जीव के शरीरान्तर ग्रहण में मन ही साधकतम है; जो जीवात्मा के साथ नित्य रहता हुआ शरीर के साथ सम्बन्ध कराता है। जिससे देहान्तर में जाने को तैयार होने पर मुमूर्ष का स्वभाव विपरीत हो जाता है अर्थात् बदल जाता है। इच्छा बदल जाती है। सभी इन्द्रियाँ उपतप्त होती अर्थात् - दुःखी होती है। बल नष्ट हो जाता है। रोग भरपूर हो जाते हैं। जिससे हीन होने पर पुरुष प्राणों को छोड़ देता है। अर्थात् मन के न रहने पर मृत्यु हो जाती है, और जो इन्द्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करनेवाला मन है वह मन ही शरीरान्तर से जीवात्मा का सम्बन्ध कराता है। जीवात्मा स्वयं निष्क्रिय है। मन की क्रिया से क्रियावान् होकर उसका देहान्तर से सम्बन्ध होता है तभी गर्भोत्पत्ति होती है। इस प्रकार आत्मा से सचेतन हुआ मन ही आत्मा को शरीरान्तर हेतु तैय्यार करता है।
वह मन तीन प्रकार का है-
1. शुद्ध
2. राजस
3. तामस
जब मन सत्त्वप्रधान होता है तब शुद्ध कहलाता है, जब रजः प्रधान होता है तब राजस और जब तमः प्रधान होता है तब तामस कहलाता है। जो सत्त्व, रज वा तम गुण में जिसका आधिक्य इस जन्म में होता है, उसी गुण की अधिकतावाला मन ही द्वितीय जन्म में होता है । पूर्वजन्म में यदि मन शुद्ध (सत्त्वगुणाधिक) हो तो द्वितीय जन्म में भी मन शुद्ध होगा। यदि पुरुष का शुद्ध मन के साथ योग हुआ है तो वह व्यतीत जन्म का भी स्मरण कराता है । यदि राजस और तामस होगा तो पूर्वजन्म में अनुभूत सुना वा देखा हुआ उसे स्मरण नहीं होगा। सुश्रुत ने भी कहा है—
'भावितः पूर्वदेहेषु सततं शास्त्रबुद्धयः।
भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूर्वजातिस्मरा नराः।।"
(सु.शा. 2)
आत्मा का स्मृति सम्बन्धी ज्ञान उसी (शुद्ध) मन के अनुबन्ध (सहयोग) से ही इस जन्म में अनुवर्तन करता है अर्थात् आता है, जिसके अनुवर्तन से पुरुष 'जातिस्मर' कहलाता है अर्थात् पूर्वजन्म का स्मरण करनेवाला होता है।
जो इस गर्भ के सत्त्वज भाव है और जो मन से सम्भवतः उत्पन्न होते हैं, उनकी व्याख्या की जायेगी - भक्ति (इच्छा), शील (स्वभाव), पवित्रता, द्वेष, स्मृति, त्याग, मत्सरता (प्रमाद), मोह, शूरता, भय, क्रोध, तन्द्रा, उत्साह, तीक्ष्णता, मृदुता, गम्भीरता, चंचलता—ये और इस प्रकार के अन्य भाव सत्त्वज विकार है।
ब्रह्मसूत्र में मन की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गयी है। आत्मा, इन्द्रिय और विषयों के रहने पर भी जिसके अवधान से ज्ञान होता है और अनवधान से ज्ञान नहीं होता, उसे मन कहते है-
"नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ।"
(ब्रह्मसूत्र 2:3-32)
मन का स्वरूप...
मन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं हैं। परन्तु जो सूक्ष्म है, अणु है, एक है; स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से सर्वशरीर व्याप्त है, जो ज्ञान होने में प्रमुख हेतु है, शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर जाता है, स्वप्न और जाग्रत् दोनों अवस्थाओं में क्रियाशील रहता है, जो इन्द्रियों का नियामक है, जो गतिशील है—वह मन है । मन और बुद्धि को आत्मा के सदृश कहकर आचार्य चरक ने इसकी गूढ़ता प्रकट कर दी है।
"बुद्धिर्मनश्च निर्णीते यथैवात्मा तथैव च । (च. सू. 11/11)
इस वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मन मात्र क्रियास्वरूप है, रचनास्वरूप नहीं। किन्तु आयुर्वेद में मन को द्रव्य माना गया है—
"खादीनात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः।"
(च. सू. 1/48)
उसके गुण, कर्म, स्थान भी बताये है।
मन के विशिष्ट गुण...
आचार्यों ने मन के अणुत्व और एकत्व यह दो विशिष्ट गुण बताये हैं।
"अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ।'
(च. शा. 1/19)
अणुत्व गुण के कारण ही मन सम्पूर्ण शरीर में, सभी इन्द्रियों तक अव्याहत गति से सम्पर्क करता है। मन अणु (सूक्ष्म) तो है किन्तु असर्वव्यापक तथा एक है। यदि मन को अणु मानकर विभु (व्यापक) माना जाय तो मन सभी इन्द्रियों से एक साथ ही संयुक्त हो सकता था और इन्द्रियार्थी को एक साथ ही सम्पूर्ण ज्ञानोत्पत्ति हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार में एक ही इन्द्रियव्यापार सम्पन्न होता है। व्यवहार में कार्य करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक साथ देख-सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते है और कर्मेन्द्रिय से कार्य जैसे आँख, हाथ, पैर हिलाना आदि करते रहते हैं। वस्तुतः तब भी हमारा मन एक-एक इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ से क्रमशः ही सम्पर्क करता है। अतिक्षिप्रता के कारण ‘शतपत्रकमलभेदनवत्' हमें एक साथ हुआ प्रतीत होता है, जबकि वह कार्य एक एकश: ही होता है। अर्थात् कमल के सौ पत्तों को एक के ऊपर एक रख उनमें सहसा सुई छेदी जाय तो ऐसा लगता है कि एक साथ सभी को छेदा गया है जबकि सुई एक-एक का भेदन करती है।
मन को अपने अर्थ (चिन्त्य) आदि इन्द्रियार्थ और संकल्प आदि में संयुक्त होकर ज्ञानोत्पत्ति होती है। अतः पृथक्-पृथक् कार्य करने से यह भास होता है कि पृथक्- पृथक् कार्य करने वाले मन अनेक है, लेकिन यदि मन अनेक होता तो एक साथ ही अनेक प्रकार का ज्ञान हो सकता था। प्रत्यक्षतः देखा जाता है कि मन किसी एक इन्द्रिय या विषय से गम्भीर रूप से जुड़ा रहता है तो अन्य इन्द्रियार्थ के प्रत्यक्ष रहते हुए भी ज्ञान नहीं होता; यही मन के एकत्व का प्रबल प्रमाण है।
मन के सामान्य...
गुण सत्त्व, रज, तम ये मन के तीन सामान्य गुण है।
मन के दोष...
अति शुद्ध एवं प्रकाशक होने कारण सत्त्व सर्वदा गुणात्मक होता है, जबकि रज और तम दोष वैषम्य को प्राप्त कर मन को विकृति करने वाले होते हैं, इसलिए रज एवं तम मानस दोष माने गये हैं-
"मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च।"
(च. सू. 8/57)
मन के अर्थ...
ज्ञान की प्रक्रिया में मन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान की प्रक्रिया इन्द्रिय सापेक्ष और इन्द्रिय निरपेक्ष ऐसी दो प्रकार की होती है। जब मन इन्द्रियों के साथ प्रवृत्त होता है तो इन्द्रियार्थ को ग्रहण करवाकर ज्ञानोत्पत्ति करता है। लेकिन इन्द्रियों के बिना मन जिन विषयों को ग्रहण करता है वे शब्दादि रूप ही होते हैं, केवल इतना अन्तर रहता है कि शब्दादि का ग्रहण केवल मन के द्वारा इन्द्रियनिरपेक्ष होता है तो वे मनोऽर्थ कहलाते है। यह पूर्व स्मृति या अन्तःकरण के संयोग से सम्भव होता है। कल्पना या अनुमान के माध्यम से मन कुछ विषयों का ज्ञान करता है। महर्षि चरक ने मन के अर्थ चिन्त्य, विचार्य, उह्य, ध्येय, संकल्प और अन्यविषय माने हैं।
"चिन्त्यं विचार्यमूह्यं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च ।
यत्किञ्चिन्मनसो ज्ञेयं तत् सर्वं ह्यर्थसज्ञंकम् ।।"
(च. शा. 1/20)
1. चिन्त्य - किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति यह चिन्त्य करता है कि इसे किया जाय या नहीं, यही 'चिन्त्य' है।
2. विचार्य – किसी भी कार्य के करने से या न करने से क्या परिणाम होगा, क्या हानि-लाभ होगा यही विषय 'विचार्य' कहलाता है।
3. उह्य – किसी भी विषय के सम्बन्ध में जो सम्भावना व्यक्त की जाय वह उ है। जैसे इस प्रकार से होगा, यह ऐसा नहीं होगा इस प्रकार की ऊहापोहात्मक स्थिति को 'उह्य' कहा है।
4. ध्येय- जिसका ध्यान करके परिकल्प कल्पित रूप में जाना जाय जिसमें भावनात्मक ज्ञान निहित हो वह विषय 'ध्येय' कहलाता है।
5. संकल्प – यह गुणवान् और यह दोषवान् है इस तरह का निश्चय जहाँ किया जाय वह 'संकल्प' है ।
6. अन्य विषय - इसके अतिरिक्त अन्य जो भी विषय मन के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं वे सभी मन के अर्थ कहलाते हैं। यह ऐसी व्यापक परिकल्पना है कि सम्पूर्ण व्यापारों का इसमें समावेश सम्भव है।
मन के कर्म...
1. इन्द्रियाभिग्रह
2. स्वयं का निग्रह
3. उह्य
4. विचार
यह मन के कर्म है; यथा-
"इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्थ्य निग्रहः।
ऊहो विचारश्च ततः परं बुद्धिः प्रवर्तते ।।"
(च.शा. 1/21)
1. इन्द्रियाभिग्रह — इन्द्रियों को अपने वश में रखना अर्थात् इन्द्रियाँ किसी भी विषय को मन में अधिष्ठित कर ही उनके विषयों को ग्रहण करती है। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में तत्सम्बन्धी इन्द्रिय को प्रवृत्त करना यह भी मन का ही कर्म है। किसी ग्राह्य इन्द्रियार्थ को उस इन्द्रियविशेष से ग्रहण करा कर मन उस इन्द्रिय पर अभिग्रह करता है।
2. स्वयं का निग्रह — मन अपने आप पर भी नियन्त्रण करता है। किसी भी अनिष्ट विषय में मन प्रवृत्त हो रहा है तो उसे स्वयं मन ही रोकता है।
3. उह्य – उहा सम्भावना है। यह सम्भावना बाह्य इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित मन पूर्व स्मृतियों के साथ करता है। प्राप्त ज्ञान के स्वरूप का मन तर्क-वितर्क के माध्यम से विश्लेषण कर सम्भावित परिणाम को ज्ञात करता है। अतः उह्य को भी मन के कर्मों में समाविष्ट कर लिया गया है।
4. विचार - हेय और उपादेय की दृष्टि से कहीं विकल्पन किया जाय अर्थात् यह अनुपयोगी है यह उपयोगी है, ऐसा विचार करना; तो इसे विचार कहते हैं। द्विविधा पूर्ण विचार आदि मन का कार्य है। इससे परे बुद्धि की प्रवृत्ति होती है।
मन प्राप्त ज्ञान के विषय में यह मेरे लिये उचित होगा, हानिकारक होगा आदि ऊहापोह करता जरूर है परन्तु उस पर निर्णय लेने का कार्य बुद्धि करती है। मन यदि प्राकृत कार्य कर रहा है तो वह उन विकल्पों को बुद्धि की ओर प्रेषित कर देता है और उन पर बुद्धि जो निर्णय देती है तदनुरूप कार्य करता है।
मन का स्थान ...
मन के स्थान के विषय में आचार्यों में मत भिन्नता है।
"स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः ।
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः ।"
(तैतिरीय उपनिषद्, षष्ठ अनु.)
"तत् परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः । हृदयं महदर्थश्च तस्यादुक्तं चिकित्सकैः ।।"
(च. सू. 30/6-7)
"तद् (हृदयं) विशेषेणा चेतना स्थानम् ।'
(सु. शा. 4/31)
"हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम् ।
हृदयात् सम्प्रवर्तन्ते मनः पूर्वाणि देहिनाम् ।।"
(सु. शा. 4/34)
इन उपर्युक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि मन का स्थान हृदय है। किन्तु महर्षि भेल ने अपनी संहिता में मन का स्थान शिर में तालु के अन्तर्गत कहा है-
"शिरस्तात्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः ।
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान् ।।
समीपस्थान् विजानाति ।"
(भे.सं. चि. 8/2)
चरक ने अन्यत्र त्वचा को मन का स्थान माना है। इनकी एक एकशः चर्चा करना उचित होगा।
हृदय
मन के स्थान के रूप में हृदय को स्वीकार करते हुए अनेक उद्धरण आयुर्वेद साहित्य में उपलब्ध है। व्यवहार में भी इसीलिए हृदय मन के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। महर्षि चरक ने हृदय की प्रधानता मानकर इसे महत् तथा अर्थ आदि नाम से पुकारा है। चरक ने छः अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान, इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के विषय गुण, आत्मा और मन के चिन्त्य विषय, इन सबको हृदय के आश्रित बतलाया है-
"षडङ्गमङ्ग विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपञ्चकम् ।
आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम् ।।"
(च. सू. 30/4)
महर्षि सुश्रुत ने हृदय को चेतना का स्थान माना है-
"हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम् ।"
(सु.शा.4/13)
सुश्रुत ने कृतवीर्य ऋषि के मत का आधार लेकर शरीर में सर्वप्रथम हृदय उत्पन्न होता है' ऐसा मानकर हृदय को बुद्धि और मन का स्थान माना है-
"हृदयमिति कृतवीर्यो बुद्धेर्मनसश्च स्थानत्वात् ।"
(सु. शा. 3/32)
वाग्भट ने अष्टाङ्गहृदय में मन का स्थान हृदय माना है। सत्त्व (मन) आदि का निवास स्थान हृदय है जो स्तन एवं उरकोष्ठ के मध्य में रहता है-
"सत्त्वादिधाम हृदयं स्तनोरः कोष्ठमध्यगम् ।"
(अ. ह. शा. 4/13)
शिर
मन का स्थान शिर है। इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं में अनेकशः किया गया है। चरक सूत्रस्थान में इस विषय का उल्लेख है, जिसमें प्राण और समस्त इन्द्रियाँ आश्रित होती है और जो सब अंगों में उत्तमांग (श्रेष्ठ अंग) है, उसे शिर कहते है-
"प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च ।
यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ।।"
(च. सू. 17/12)
पुनः सिद्धिस्थान में चरकसंहिताकार कहते हैं कि शिर में इन्द्रियाँ और इन्द्रिय प्राणवह स्रोत उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार सूर्य में रश्मियाँ रहती हैं-
"शिरसि इन्द्रियाणि, इन्द्रियप्राणवहानि च स्त्रोतांसि सूर्यमिव गभस्तयः संश्रितानि ।"
(च. सि. 9/4)
इन्द्रियाँ ज्ञान और कर्म की साधन हैं। यहाँ इन्द्रियाँ कहने से मस्तिष्कगत ज्ञान और चेष्टा के केन्द्रों का इन्द्रियवह स्रोतों से ज्ञान संज्ञा लाने वाली नड़ियों का बोध होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की उपलब्धि के साधन मन का स्थान शिर है।
भेलसंहिता में शिर और हृदय को क्रमशः मन और चित्त का स्थान माना है। भेल के अनुसार शिर और तालु के बीच में मन रहता है। वहाँ रहते हुए समीपस्थ इन्द्रियों के रस आदि विषयों का ज्ञान करता है। उस मन के कारण ही सभी इन्द्रियों का बल रहता है। चित्त हृदय में रहता है और बुद्धियों का कारण बनता है। क्रियाओं का हेतु चित्त ही है-
"शिरस्तात्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः ।
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्।।
समीपस्थान् विजानाति त्रीन् भावांश्च नियच्छति ।
सुमनः प्रभवं चापि सर्वेन्द्रियमयं बलम् ॥
कारणं सर्वबुद्धीनां चित्तं हृदयसंश्रितम् ।
क्रियाणां चेतरासां च चित्तं सर्वत्र कारणम् ।।'
(भे.सं.चि. 8)
सर्वशरीर
सत्त्व (मन) आदि अतीन्द्रिय भावों का सम्पूर्ण सजीव शरीर ही अयनभूत और अधिष्ठान होता है—
"तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च ।।"
(च.वि. 5/6)
त्वगाश्रित मन
त्वचा ही वास्तविक इन्द्रिय है क्योंकि यह सभी इन्द्रियों में व्याप्त रहते हुए चित से जुड़ी रहती है-
"तत्रैकं स्पर्शनमिन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियव्यापकं चेतः समवायि ।"
(च. सू. 11/28)
इसी कारण त्वगाश्रित मन कहा गया है।
योगशास्त्र सम्मत मन का स्थान...
योगशास्त्र ने मन का स्थान मस्तिष्क में सहस्रार पद्म माना है, जिसमें मन निवास करता है-
"एतत्पद्यान्तराले निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम् ।"
(षट्चक्रनिरूपण 33)
उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकलता है कि मन का वास्तविक स्थान हृदय है, परन्तु उसकी विशिष्ट कार्यस्थली शिर है। इन्द्रियों और अधिष्ठानों में आवागमन के लिए मनोवह स्रोत हैं। वे सम्पूर्ण शरीर में (नख, लोम आदि छोड़कर) व्याप्त हैं। उनके माध्यम से सम्पूर्ण शरीर ही मन का कार्य क्षेत्र है।
मनोवह स्त्रोतम् ...
आयुर्वेदीय साहित्य में स्रोतसों की एक विशिष्ट परिकल्पना की गयी है। तदनुसार सम्पूर्ण शरीर को स्रोतसों का समूह माना गया है—
"अपि चैके स्त्रोतसामेव समुदयं पुरुषमिच्छन्ति ।"
(च. वि. 5:4)
शारीर-प्रसंग में जहाँ स्रोतसों का वर्णन है वहाँ मनोवह स्रोतस् का उल्लेख नहीं है। किन्तु अनेक मानस व्याधियों की सम्प्राप्ति वर्णन के प्रसंग में बार-बार मनोवह स्रोतस् का उल्लेख है। जैसे उन्माद की सम्प्राप्ति में प्रकुपित दोष मनोवह स्रोतसों में अधिष्ठत हो मनुष्य के चित्त को प्रभावित करते है-
"स्त्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ।"
(च. चि. 9/5)
चरक विमानस्थान के स्रोतोविमानीय नामक पंचम अध्याय में उन्होंने भिन्न-भिन्न स्रोतोसों का वर्णन किया है, किन्तु मनोवह स्रोतस् का उल्लेख नहीं है; वहीं टीका में आचार्य चक्रपाणि कहते हैं कि यद्यपि मन नित्य द्रव्य है इसलिए उसके पोषण के लिए किसी अन्य द्रव्य के संवहन की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए मनोवाही स्रोतस् नहीं कहा गया; तथापि मन को भिन्न-भिन्न इन्द्रिय प्रदेशों तक जाने के लिए स्रोतस् तो हैं ही; इसलिए अतीन्द्रिय मन का सम्पूर्ण शरीर ही स्रोतोरूप है-
"मनस्तु यद्यपि नित्यत्वेन न पोष्यं, तथापि तस्येन्द्रियप्रदेशगमनार्थं स्त्रोतोऽस्त्येव । तच्च मनः प्रभृतीनामतीन्द्रियाणां कृत्स्नमेव शरीरं स्त्रोतोरूपं वक्ष्यति ।"
(च. वि. 5/3 पर चक्रपाणि)
इसी प्रसंग में वे आगे कहते हैं कि यद्यपि मनोवाही स्रोतस् सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है या सम्पूर्ण शरीर मनोवह स्रोतस् का अवनभूत है फिर भी विशेष रूप से हृदयाश्रित मन का हृदय से सम्बन्ध ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्गामी दस धमनियाँ मनोवाही स्रोतस हैं-
"मनोवहानि स्त्रोतांसि यद्यपि पृथक्तोक्तानि तथापि मनसः 'केवलचेतनावत् शरीर- मयनभूत' इत्यभिधानात् सर्वशरीरस्त्रोतांसि गृह्यन्ते । विशेषेण तु हृदयाश्रितत्वान्मन- सस्तदाश्रिता दशधमन्यो मनोवहा अभिधीयन्ते ।"
(चक्रपाणि)
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर उरःस्थ हृदय की अपेक्षा शिरस्थ हृदय या मस्तिष्क तथा तत्सम्बन्धी नाड़ी संस्थान मनोवह स्रोतस् के वर्णन के ज्यादा अनुरूप है।
मानस रोगों की सम्प्राप्ति के सन्दर्भ में जिस प्रकार से आचार्यों ने मनोवाही स्रोतसों का वर्णन किया है उसकी नाड़ी संस्थान के साथ भी साम्यता नहीं है।
मन की परिभाषा...
"सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः।"
(तर्कसंग्रह)
सुख, दुःख आदि की उपलब्धि का साधनभूत तत्त्व है-मन। दूसरे शब्दों में मन वह इन्द्रिय है जिससे सुख, दुःख आदि का ज्ञान होता है। सुख, दुःख की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने कहा है- 'अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्' अर्थात् जो भाव मन में अनुकूल है वह सुख और जो भाव मन के प्रतिकूल है वह दुःख । इससे स्पष्ट है कि सुख, दुःख आदि की प्रतीति मन द्वारा ही होती है; और जो सुख, दुःख आदि की उपलब्धि का साधन है वह मन है।
आचार्य चरक ने सुख, दुःख की बात न कर सम्पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि का साधन मन को माना है। उनके अनुसार जिसकी उपस्थिति से ज्ञान हो और अनुपस्थिति से ज्ञान न हो वही मन है। इस प्रकार ज्ञान का भाव (होना) और अभाव (न होना) मन के लक्षण हैं, उसके अस्तित्व की पहचान हैं। ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया के सम्पूर्ण साधन आत्मा, इन्द्रिय, अर्थ आदि की विद्यमानता रहते हुए भी मन का संयोग नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता है और संयोग होने पर ज्ञान होता है-
"लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च।
सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते।
वैवृत्त्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात् तच्च वर्तते ।"
(च. शा. 1/19)
मन इन्द्रियातीत है अर्थात् उसका प्रत्यक्षीकरण इन्द्रियों द्वारा नहीं होता है, अपितु उसके कार्यों से ही उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है। इसलिए मन की सभी परिभाषाएँ उसके कार्यों पर आधारित है।
महर्षि चरक (च. शा. 2/31) के अनुसार मन की गति के कारण आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है—'मनोजवो देहमुपैति देहात्' । और मन के निकल जाने पर शील (स्वभाव) बदल जाता है, अभिरुचि नष्ट हो जाती है, सब इन्द्रियाँ कष्टपीड़ित होती है, बल का ह्रास हो जाता है, व्याधियाँ बढ़ जाती है, जिसके बिना प्राणों का त्याग हो जाता है और जो इन्द्रियों का अभिग्राहक प्रेरक है उसे मन कहते हैं-
"अस्ति खलु सत्त्वमौपपादुकं यज्जीवं स्पृक्शरीरेणाभिसम्बध्नाति, यस्मिन्नपगमन- पुरस्कृते शीलमस्य व्यावर्तते, भक्तिर्विपर्यस्यते, सर्वेन्द्रियाण्युपतप्यन्ते, बलं हीयते, व्याधय आप्यायन्ते यस्माद्धीनः प्राणाञ्जहाति, यदिन्द्रियाणामभिग्राहकं च 'मन' इत्यभिधी- यते; तत् त्रिविधमाख्यायते शुद्धं, राजसं, तामसमिति । येनास्य खलु मनो भूयिष्ठं, तेन द्वितीयायामाजातौ सम्प्रयोगो भवति यदा तु तेनैव शुद्धेन संयुज्यते, तदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति । स्मार्तं हि ज्ञानमात्मनस्तस्यैव मनसोऽनुबन्धादनुवर्तते, यस्यानुवृत्तिं पुरस्कृत्य पुरुषो 'जातिस्मर' इत्युच्यते । यानि खल्वस्य गर्भस्य सत्त्वजानि यान्यस्य सत्त्वतः सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः, तद्यथा-भक्तिः शीलं शौचं द्वेषः स्मृति- मोहस्त्यागो मात्सर्य शौर्य भयं क्रोधस्तन्द्रोत्साहस्तैक्ष्ण्यं मार्दवं गाम्भीर्यमनवस्थितत्वमित्येव- मादयश्चान्ये, ते सत्त्वविकारा, यानुत्तरकालं सत्त्वभेदमधिकृत्योपदेक्ष्यामः । नानाविधानि खलु सत्त्वानि तानि सर्वाण्येकपुरुषे भवन्ति, न च भवन्त्येककालम् एकं तु प्रायोवृत्त्याऽऽह ॥"
(च. शा. 3/13)
मन निश्चय शरीरान्तर के साथ सम्बन्ध करनेवाला है अर्थात् जीव के शरीरान्तर ग्रहण में मन ही साधकतम है; जो जीवात्मा के साथ नित्य रहता हुआ शरीर के साथ सम्बन्ध कराता है। जिससे देहान्तर में जाने को तैयार होने पर मुमूर्ष का स्वभाव विपरीत हो जाता है अर्थात् बदल जाता है। इच्छा बदल जाती है। सभी इन्द्रियाँ उपतप्त होती अर्थात् - दुःखी होती है। बल नष्ट हो जाता है। रोग भरपूर हो जाते हैं। जिससे हीन होने पर पुरुष प्राणों को छोड़ देता है। अर्थात् मन के न रहने पर मृत्यु हो जाती है, और जो इन्द्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करनेवाला मन है वह मन ही शरीरान्तर से जीवात्मा का सम्बन्ध कराता है। जीवात्मा स्वयं निष्क्रिय है। मन की क्रिया से क्रियावान् होकर उसका देहान्तर से सम्बन्ध होता है तभी गर्भोत्पत्ति होती है। इस प्रकार आत्मा से सचेतन हुआ मन ही आत्मा को शरीरान्तर हेतु तैय्यार करता है।
वह मन तीन प्रकार का है-
1. शुद्ध
2. राजस
3. तामस
जब मन सत्त्वप्रधान होता है तब शुद्ध कहलाता है, जब रजः प्रधान होता है तब राजस और जब तमः प्रधान होता है तब तामस कहलाता है। जो सत्त्व, रज वा तम गुण में जिसका आधिक्य इस जन्म में होता है, उसी गुण की अधिकतावाला मन ही द्वितीय जन्म में होता है । पूर्वजन्म में यदि मन शुद्ध (सत्त्वगुणाधिक) हो तो द्वितीय जन्म में भी मन शुद्ध होगा। यदि पुरुष का शुद्ध मन के साथ योग हुआ है तो वह व्यतीत जन्म का भी स्मरण कराता है । यदि राजस और तामस होगा तो पूर्वजन्म में अनुभूत सुना वा देखा हुआ उसे स्मरण नहीं होगा। सुश्रुत ने भी कहा है—
'भावितः पूर्वदेहेषु सततं शास्त्रबुद्धयः।
भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूर्वजातिस्मरा नराः।।"
(सु.शा. 2)
आत्मा का स्मृति सम्बन्धी ज्ञान उसी (शुद्ध) मन के अनुबन्ध (सहयोग) से ही इस जन्म में अनुवर्तन करता है अर्थात् आता है, जिसके अनुवर्तन से पुरुष 'जातिस्मर' कहलाता है अर्थात् पूर्वजन्म का स्मरण करनेवाला होता है।
जो इस गर्भ के सत्त्वज भाव है और जो मन से सम्भवतः उत्पन्न होते हैं, उनकी व्याख्या की जायेगी - भक्ति (इच्छा), शील (स्वभाव), पवित्रता, द्वेष, स्मृति, त्याग, मत्सरता (प्रमाद), मोह, शूरता, भय, क्रोध, तन्द्रा, उत्साह, तीक्ष्णता, मृदुता, गम्भीरता, चंचलता—ये और इस प्रकार के अन्य भाव सत्त्वज विकार है।
ब्रह्मसूत्र में मन की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गयी है। आत्मा, इन्द्रिय और विषयों के रहने पर भी जिसके अवधान से ज्ञान होता है और अनवधान से ज्ञान नहीं होता, उसे मन कहते है-
"नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ।"
(ब्रह्मसूत्र 2:3-32)
मन का स्वरूप...
मन का कोई निश्चित स्वरूप नहीं हैं। परन्तु जो सूक्ष्म है, अणु है, एक है; स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से सर्वशरीर व्याप्त है, जो ज्ञान होने में प्रमुख हेतु है, शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर जाता है, स्वप्न और जाग्रत् दोनों अवस्थाओं में क्रियाशील रहता है, जो इन्द्रियों का नियामक है, जो गतिशील है—वह मन है । मन और बुद्धि को आत्मा के सदृश कहकर आचार्य चरक ने इसकी गूढ़ता प्रकट कर दी है।
"बुद्धिर्मनश्च निर्णीते यथैवात्मा तथैव च । (च. सू. 11/11)
इस वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मन मात्र क्रियास्वरूप है, रचनास्वरूप नहीं। किन्तु आयुर्वेद में मन को द्रव्य माना गया है—
"खादीनात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः।"
(च. सू. 1/48)
उसके गुण, कर्म, स्थान भी बताये है।
मन के विशिष्ट गुण...
आचार्यों ने मन के अणुत्व और एकत्व यह दो विशिष्ट गुण बताये हैं।
"अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ।'
(च. शा. 1/19)
अणुत्व गुण के कारण ही मन सम्पूर्ण शरीर में, सभी इन्द्रियों तक अव्याहत गति से सम्पर्क करता है। मन अणु (सूक्ष्म) तो है किन्तु असर्वव्यापक तथा एक है। यदि मन को अणु मानकर विभु (व्यापक) माना जाय तो मन सभी इन्द्रियों से एक साथ ही संयुक्त हो सकता था और इन्द्रियार्थी को एक साथ ही सम्पूर्ण ज्ञानोत्पत्ति हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार में एक ही इन्द्रियव्यापार सम्पन्न होता है। व्यवहार में कार्य करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक साथ देख-सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते है और कर्मेन्द्रिय से कार्य जैसे आँख, हाथ, पैर हिलाना आदि करते रहते हैं। वस्तुतः तब भी हमारा मन एक-एक इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ से क्रमशः ही सम्पर्क करता है। अतिक्षिप्रता के कारण ‘शतपत्रकमलभेदनवत्' हमें एक साथ हुआ प्रतीत होता है, जबकि वह कार्य एक एकश: ही होता है। अर्थात् कमल के सौ पत्तों को एक के ऊपर एक रख उनमें सहसा सुई छेदी जाय तो ऐसा लगता है कि एक साथ सभी को छेदा गया है जबकि सुई एक-एक का भेदन करती है।
मन को अपने अर्थ (चिन्त्य) आदि इन्द्रियार्थ और संकल्प आदि में संयुक्त होकर ज्ञानोत्पत्ति होती है। अतः पृथक्-पृथक् कार्य करने से यह भास होता है कि पृथक्- पृथक् कार्य करने वाले मन अनेक है, लेकिन यदि मन अनेक होता तो एक साथ ही अनेक प्रकार का ज्ञान हो सकता था। प्रत्यक्षतः देखा जाता है कि मन किसी एक इन्द्रिय या विषय से गम्भीर रूप से जुड़ा रहता है तो अन्य इन्द्रियार्थ के प्रत्यक्ष रहते हुए भी ज्ञान नहीं होता; यही मन के एकत्व का प्रबल प्रमाण है।
मन के सामान्य...
गुण सत्त्व, रज, तम ये मन के तीन सामान्य गुण है।
मन के दोष...
अति शुद्ध एवं प्रकाशक होने कारण सत्त्व सर्वदा गुणात्मक होता है, जबकि रज और तम दोष वैषम्य को प्राप्त कर मन को विकृति करने वाले होते हैं, इसलिए रज एवं तम मानस दोष माने गये हैं-
"मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च।"
(च. सू. 8/57)
मन के अर्थ...
ज्ञान की प्रक्रिया में मन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान की प्रक्रिया इन्द्रिय सापेक्ष और इन्द्रिय निरपेक्ष ऐसी दो प्रकार की होती है। जब मन इन्द्रियों के साथ प्रवृत्त होता है तो इन्द्रियार्थ को ग्रहण करवाकर ज्ञानोत्पत्ति करता है। लेकिन इन्द्रियों के बिना मन जिन विषयों को ग्रहण करता है वे शब्दादि रूप ही होते हैं, केवल इतना अन्तर रहता है कि शब्दादि का ग्रहण केवल मन के द्वारा इन्द्रियनिरपेक्ष होता है तो वे मनोऽर्थ कहलाते है। यह पूर्व स्मृति या अन्तःकरण के संयोग से सम्भव होता है। कल्पना या अनुमान के माध्यम से मन कुछ विषयों का ज्ञान करता है। महर्षि चरक ने मन के अर्थ चिन्त्य, विचार्य, उह्य, ध्येय, संकल्प और अन्यविषय माने हैं।
"चिन्त्यं विचार्यमूह्यं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च ।
यत्किञ्चिन्मनसो ज्ञेयं तत् सर्वं ह्यर्थसज्ञंकम् ।।"
(च. शा. 1/20)
1. चिन्त्य - किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति यह चिन्त्य करता है कि इसे किया जाय या नहीं, यही 'चिन्त्य' है।
2. विचार्य – किसी भी कार्य के करने से या न करने से क्या परिणाम होगा, क्या हानि-लाभ होगा यही विषय 'विचार्य' कहलाता है।
3. उह्य – किसी भी विषय के सम्बन्ध में जो सम्भावना व्यक्त की जाय वह उ है। जैसे इस प्रकार से होगा, यह ऐसा नहीं होगा इस प्रकार की ऊहापोहात्मक स्थिति को 'उह्य' कहा है।
4. ध्येय- जिसका ध्यान करके परिकल्प कल्पित रूप में जाना जाय जिसमें भावनात्मक ज्ञान निहित हो वह विषय 'ध्येय' कहलाता है।
5. संकल्प – यह गुणवान् और यह दोषवान् है इस तरह का निश्चय जहाँ किया जाय वह 'संकल्प' है ।
6. अन्य विषय - इसके अतिरिक्त अन्य जो भी विषय मन के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं वे सभी मन के अर्थ कहलाते हैं। यह ऐसी व्यापक परिकल्पना है कि सम्पूर्ण व्यापारों का इसमें समावेश सम्भव है।
मन के कर्म...
1. इन्द्रियाभिग्रह
2. स्वयं का निग्रह
3. उह्य
4. विचार
यह मन के कर्म है; यथा-
"इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्थ्य निग्रहः।
ऊहो विचारश्च ततः परं बुद्धिः प्रवर्तते ।।"
(च.शा. 1/21)
1. इन्द्रियाभिग्रह — इन्द्रियों को अपने वश में रखना अर्थात् इन्द्रियाँ किसी भी विषय को मन में अधिष्ठित कर ही उनके विषयों को ग्रहण करती है। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में तत्सम्बन्धी इन्द्रिय को प्रवृत्त करना यह भी मन का ही कर्म है। किसी ग्राह्य इन्द्रियार्थ को उस इन्द्रियविशेष से ग्रहण करा कर मन उस इन्द्रिय पर अभिग्रह करता है।
2. स्वयं का निग्रह — मन अपने आप पर भी नियन्त्रण करता है। किसी भी अनिष्ट विषय में मन प्रवृत्त हो रहा है तो उसे स्वयं मन ही रोकता है।
3. उह्य – उहा सम्भावना है। यह सम्भावना बाह्य इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित मन पूर्व स्मृतियों के साथ करता है। प्राप्त ज्ञान के स्वरूप का मन तर्क-वितर्क के माध्यम से विश्लेषण कर सम्भावित परिणाम को ज्ञात करता है। अतः उह्य को भी मन के कर्मों में समाविष्ट कर लिया गया है।
4. विचार - हेय और उपादेय की दृष्टि से कहीं विकल्पन किया जाय अर्थात् यह अनुपयोगी है यह उपयोगी है, ऐसा विचार करना; तो इसे विचार कहते हैं। द्विविधा पूर्ण विचार आदि मन का कार्य है। इससे परे बुद्धि की प्रवृत्ति होती है।
मन प्राप्त ज्ञान के विषय में यह मेरे लिये उचित होगा, हानिकारक होगा आदि ऊहापोह करता जरूर है परन्तु उस पर निर्णय लेने का कार्य बुद्धि करती है। मन यदि प्राकृत कार्य कर रहा है तो वह उन विकल्पों को बुद्धि की ओर प्रेषित कर देता है और उन पर बुद्धि जो निर्णय देती है तदनुरूप कार्य करता है।
मन का स्थान ...
मन के स्थान के विषय में आचार्यों में मत भिन्नता है।
"स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः ।
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः ।"
(तैतिरीय उपनिषद्, षष्ठ अनु.)
"तत् परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः । हृदयं महदर्थश्च तस्यादुक्तं चिकित्सकैः ।।"
(च. सू. 30/6-7)
"तद् (हृदयं) विशेषेणा चेतना स्थानम् ।'
(सु. शा. 4/31)
"हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम् ।
हृदयात् सम्प्रवर्तन्ते मनः पूर्वाणि देहिनाम् ।।"
(सु. शा. 4/34)
इन उपर्युक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि मन का स्थान हृदय है। किन्तु महर्षि भेल ने अपनी संहिता में मन का स्थान शिर में तालु के अन्तर्गत कहा है-
"शिरस्तात्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः ।
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान् ।।
समीपस्थान् विजानाति ।"
(भे.सं. चि. 8/2)
चरक ने अन्यत्र त्वचा को मन का स्थान माना है। इनकी एक एकशः चर्चा करना उचित होगा।
हृदय
मन के स्थान के रूप में हृदय को स्वीकार करते हुए अनेक उद्धरण आयुर्वेद साहित्य में उपलब्ध है। व्यवहार में भी इसीलिए हृदय मन के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। महर्षि चरक ने हृदय की प्रधानता मानकर इसे महत् तथा अर्थ आदि नाम से पुकारा है। चरक ने छः अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान, इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के विषय गुण, आत्मा और मन के चिन्त्य विषय, इन सबको हृदय के आश्रित बतलाया है-
"षडङ्गमङ्ग विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपञ्चकम् ।
आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम् ।।"
(च. सू. 30/4)
महर्षि सुश्रुत ने हृदय को चेतना का स्थान माना है-
"हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम् ।"
(सु.शा.4/13)
सुश्रुत ने कृतवीर्य ऋषि के मत का आधार लेकर शरीर में सर्वप्रथम हृदय उत्पन्न होता है' ऐसा मानकर हृदय को बुद्धि और मन का स्थान माना है-
"हृदयमिति कृतवीर्यो बुद्धेर्मनसश्च स्थानत्वात् ।"
(सु. शा. 3/32)
वाग्भट ने अष्टाङ्गहृदय में मन का स्थान हृदय माना है। सत्त्व (मन) आदि का निवास स्थान हृदय है जो स्तन एवं उरकोष्ठ के मध्य में रहता है-
"सत्त्वादिधाम हृदयं स्तनोरः कोष्ठमध्यगम् ।"
(अ. ह. शा. 4/13)
शिर
मन का स्थान शिर है। इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं में अनेकशः किया गया है। चरक सूत्रस्थान में इस विषय का उल्लेख है, जिसमें प्राण और समस्त इन्द्रियाँ आश्रित होती है और जो सब अंगों में उत्तमांग (श्रेष्ठ अंग) है, उसे शिर कहते है-
"प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च ।
यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ।।"
(च. सू. 17/12)
पुनः सिद्धिस्थान में चरकसंहिताकार कहते हैं कि शिर में इन्द्रियाँ और इन्द्रिय प्राणवह स्रोत उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार सूर्य में रश्मियाँ रहती हैं-
"शिरसि इन्द्रियाणि, इन्द्रियप्राणवहानि च स्त्रोतांसि सूर्यमिव गभस्तयः संश्रितानि ।"
(च. सि. 9/4)
इन्द्रियाँ ज्ञान और कर्म की साधन हैं। यहाँ इन्द्रियाँ कहने से मस्तिष्कगत ज्ञान और चेष्टा के केन्द्रों का इन्द्रियवह स्रोतों से ज्ञान संज्ञा लाने वाली नड़ियों का बोध होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की उपलब्धि के साधन मन का स्थान शिर है।
भेलसंहिता में शिर और हृदय को क्रमशः मन और चित्त का स्थान माना है। भेल के अनुसार शिर और तालु के बीच में मन रहता है। वहाँ रहते हुए समीपस्थ इन्द्रियों के रस आदि विषयों का ज्ञान करता है। उस मन के कारण ही सभी इन्द्रियों का बल रहता है। चित्त हृदय में रहता है और बुद्धियों का कारण बनता है। क्रियाओं का हेतु चित्त ही है-
"शिरस्तात्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः ।
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्।।
समीपस्थान् विजानाति त्रीन् भावांश्च नियच्छति ।
सुमनः प्रभवं चापि सर्वेन्द्रियमयं बलम् ॥
कारणं सर्वबुद्धीनां चित्तं हृदयसंश्रितम् ।
क्रियाणां चेतरासां च चित्तं सर्वत्र कारणम् ।।'
(भे.सं.चि. 8)
सर्वशरीर
सत्त्व (मन) आदि अतीन्द्रिय भावों का सम्पूर्ण सजीव शरीर ही अयनभूत और अधिष्ठान होता है—
"तद्वदतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च ।।"
(च.वि. 5/6)
त्वगाश्रित मन
त्वचा ही वास्तविक इन्द्रिय है क्योंकि यह सभी इन्द्रियों में व्याप्त रहते हुए चित से जुड़ी रहती है-
"तत्रैकं स्पर्शनमिन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियव्यापकं चेतः समवायि ।"
(च. सू. 11/28)
इसी कारण त्वगाश्रित मन कहा गया है।
योगशास्त्र सम्मत मन का स्थान...
योगशास्त्र ने मन का स्थान मस्तिष्क में सहस्रार पद्म माना है, जिसमें मन निवास करता है-
"एतत्पद्यान्तराले निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धम् ।"
(षट्चक्रनिरूपण 33)
उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकलता है कि मन का वास्तविक स्थान हृदय है, परन्तु उसकी विशिष्ट कार्यस्थली शिर है। इन्द्रियों और अधिष्ठानों में आवागमन के लिए मनोवह स्रोत हैं। वे सम्पूर्ण शरीर में (नख, लोम आदि छोड़कर) व्याप्त हैं। उनके माध्यम से सम्पूर्ण शरीर ही मन का कार्य क्षेत्र है।
मनोवह स्त्रोतम् ...
आयुर्वेदीय साहित्य में स्रोतसों की एक विशिष्ट परिकल्पना की गयी है। तदनुसार सम्पूर्ण शरीर को स्रोतसों का समूह माना गया है—
"अपि चैके स्त्रोतसामेव समुदयं पुरुषमिच्छन्ति ।"
(च. वि. 5:4)
शारीर-प्रसंग में जहाँ स्रोतसों का वर्णन है वहाँ मनोवह स्रोतस् का उल्लेख नहीं है। किन्तु अनेक मानस व्याधियों की सम्प्राप्ति वर्णन के प्रसंग में बार-बार मनोवह स्रोतस् का उल्लेख है। जैसे उन्माद की सम्प्राप्ति में प्रकुपित दोष मनोवह स्रोतसों में अधिष्ठत हो मनुष्य के चित्त को प्रभावित करते है-
"स्त्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ।"
(च. चि. 9/5)
चरक विमानस्थान के स्रोतोविमानीय नामक पंचम अध्याय में उन्होंने भिन्न-भिन्न स्रोतोसों का वर्णन किया है, किन्तु मनोवह स्रोतस् का उल्लेख नहीं है; वहीं टीका में आचार्य चक्रपाणि कहते हैं कि यद्यपि मन नित्य द्रव्य है इसलिए उसके पोषण के लिए किसी अन्य द्रव्य के संवहन की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए मनोवाही स्रोतस् नहीं कहा गया; तथापि मन को भिन्न-भिन्न इन्द्रिय प्रदेशों तक जाने के लिए स्रोतस् तो हैं ही; इसलिए अतीन्द्रिय मन का सम्पूर्ण शरीर ही स्रोतोरूप है-
"मनस्तु यद्यपि नित्यत्वेन न पोष्यं, तथापि तस्येन्द्रियप्रदेशगमनार्थं स्त्रोतोऽस्त्येव । तच्च मनः प्रभृतीनामतीन्द्रियाणां कृत्स्नमेव शरीरं स्त्रोतोरूपं वक्ष्यति ।"
(च. वि. 5/3 पर चक्रपाणि)
इसी प्रसंग में वे आगे कहते हैं कि यद्यपि मनोवाही स्रोतस् सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है या सम्पूर्ण शरीर मनोवह स्रोतस् का अवनभूत है फिर भी विशेष रूप से हृदयाश्रित मन का हृदय से सम्बन्ध ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्गामी दस धमनियाँ मनोवाही स्रोतस हैं-
"मनोवहानि स्त्रोतांसि यद्यपि पृथक्तोक्तानि तथापि मनसः 'केवलचेतनावत् शरीर- मयनभूत' इत्यभिधानात् सर्वशरीरस्त्रोतांसि गृह्यन्ते । विशेषेण तु हृदयाश्रितत्वान्मन- सस्तदाश्रिता दशधमन्यो मनोवहा अभिधीयन्ते ।"
(चक्रपाणि)
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर उरःस्थ हृदय की अपेक्षा शिरस्थ हृदय या मस्तिष्क तथा तत्सम्बन्धी नाड़ी संस्थान मनोवह स्रोतस् के वर्णन के ज्यादा अनुरूप है।
मानस रोगों की सम्प्राप्ति के सन्दर्भ में जिस प्रकार से आचार्यों ने मनोवाही स्रोतसों का वर्णन किया है उसकी नाड़ी संस्थान के साथ भी साम्यता नहीं है।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.