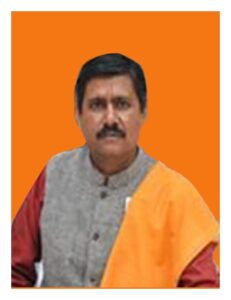- धर्म-पथ
- |
-
31 October 2024
- |
- 0 Comments
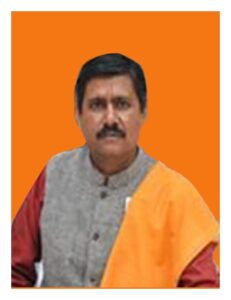
डॉ. दिलीप कुमार नाथाणी (विद्यावाचस्पति)-
शब्दकल्पद्रुम के अनुसार स्वयं देखी हुई बात को कहना आख्यान कहा गया है तथा सुनी बात को कहना उपाख्यान। जिन चरित्रों का कथन वंशक्रम से हो, वे वंशानुचरित नाम के प्रधान लक्षण में आ जाते हैं, तथा जिन चरित्रेां का वर्णन तत्तत् स्थलों में आदर्श के रूप में वंश के क्रम को छोड़कर दृष्टान्त के रूप में किया गया है, उनको यहाँ ‘आख्यान’ और ‘उपाख्यान’ नाम दिया गया है। जैसे महाभारत में नल का उपाख्यान, सावित्री का उपाख्यान आदि है। मार्कण्डेयपुराण में मदालसा का उपाख्यान इत्यादि ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं।
यह होने पर भी उपर्युक्त श्लोक में स्वयंदृष्ट कथन को ‘आख्यान’ और सुनी हुई बात के कथन को ‘उपाख्यान’ कहा गया है। कुछ विद्वानों ने ‘आख्यान’ और ‘उपाख्यान’ की व्याख्या में यह कहा है कि वेदों में जो आख्यायिकाएँ संकेत-रूप से आई हैं उनका विस्तार पुराणों में किया गया है। उन्हें ही ‘आख्यान’ कहना चाहिये। ‘उपाख्यान’ वे हैं, जो वेद या प्राचीन वाङ्मय में संकेतित नहीं हैं।
पुराणविद्या के अन्तर्गत पुराणकर्त्ता ने ही उनका संकलन किया है। नल आदि राजाओं के चरित्र ऐसे ही उपाख्यान हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि ‘वंश’ और ‘वंशानुचरित’ ये दो लक्षण अन्य वस्तु-वृत्तान्तों की अपेक्षा सर्वथा वैज्ञानिक हैं। मनुष्य विशेष राजाओं के जो चरित्र हैं, वे आख्यान ही हैं और प्रसंगागत जो चरित्र संगृहीत हुये हैं, वे ‘उपाख्यान’ हैं। अतिरिक्त विषयों में तृतीय स्थान ‘गाथा’ का है। ये गाथाएँ बहुत ही प्राचीन हैं। वेद के ब्राह्मण-भाग में भी बहुत सी गाथाएँ प्राप्त हेाती हैं। पुराणों के प्रतिपादन करने वाले श्रुतिवाक्यों में पुराण के साथ ‘गाथा’ का भी स्मरण किया गय ाहै। ‘गाथा’ का स्वरूप यह है कि किसी महामहिमशाली वर्तमान युग या युगान्तर में उत्पन्न होने वाले महापुरुष ने अपने अनुभवों का जिन शब्दों में प्रकाशन किया और शिष्ट पुरुषों ने जिन्हें सादर स्वीकार कर लिया, उन्हें ‘गाथा’ कहा जाता है। महाभारत में अपने पुत्र के यौवन को ग्रहण करके भी अतृप्त रहने वाले राजा ययाति ने अपने अनुभव को निम्नलिखित गाथा में प्रकाशित किया है-
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविशा कृष्णवर्त्तमेव भूय एवाभिवर्धते।।
अर्थात् कामनाओं के उपभोग से कभी काम शान्त नहीं होता, अपितु वह उसी प्रकार बढ़ जाता है, जिस प्रकार आहुति डालने पर अग्नि। ये गाथाएँ उपदेश के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती हैं, इसलिये पुराणों में स्थान-स्थान पर इस प्रकार की गाथाओं का संग्रह मिलता है। यदि सभी पुराणों से इस प्रकार की गाथाओं को कल्पशुद्धि से कल्पों की गाथा करने का अभिप्राय कुछ विद्वानों ने माना है। यह कल्पशुद्धि तो पुराणों के मुख्य लक्षणों में ही आ जाती है, इसलिये इनके अतिरिक्त विषयों में जो कल्पशुद्धि पद आया है, उसका अर्थ धर्मशास्त्र के कल्पसूत्रों में जो कर्मकाण्डों के विधान आते हैं और धर्मशास्त्रों में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के शुद्धियों के विचार मिलते हैं, उनका ही यहाँ कल्पशुद्धि पद से ग्रहण करना उचित होगा। (पुराणपरिशीलन, पं.गिरधर चतुर्वेदी, पृ. 57)
पुराणों का प्रयोजन
संस्कृत परम्परा के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिये उसके औचित्य को महत्त्व दिया जाता है। उसी प्रकार पुरणों के होने के सन्दर्भ में पुराणों के औचित्य पर धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों ने चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका के रचनाकार देवण्णभट्ट ने प्रमाण साधन के अन्तर्गत कहा है कि-वक्तृनपेक्षत्वेन वेदश्च प्रमाणम्। तन्मूलत्वेन स्मृत्याचारावपि। तन्मूलत्वं च तत्प्रतिपादितार्थाभिधायित्वात्। तथा च भृगुः
यःकश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे ब्रह्मज्ञानमयो हि सः।
इति। शंखोऽपि-‘तत्र वेदमूलास्स्मृतयः’इति एतदप्यदृष्टार्थनामेव, न पुनर्दृष्टार्थानाम्। तथा च पुराणम्-
सर्वा एता वेदमूला दृष्टार्थाः परिहृत्य तु।।
इति। ननु यदि स्मृतिशास्त्रस्य वेदप्रतिपादितार्थपरत्वेन वेदमूलत्वं तर्हि तेनैवालं किं धर्मशास्त्रेणेत्याशंक्याह मरीचिः-
दुर्बोधा वैदिकाश्शब्दाः प्रकीणत्वाच्च ये खिलाः।
तज्ज्ञैस्तु एव स्पष्टार्थाः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः।। (स्मृतिचन्द्रिका, प्रथम खण्ड, पृ. 2-3)
इति। एवं पुराणानामपि प्रामाण्यं प्रयोजनत्त्वं च सिद्धम्। सर्वाधिक प्रमाण हैं ‘वेद’ तथा वेदमूलकता होने के कारण प्रमाण साधन के रूप में स्मृतियों की भी प्रामाणिकता है। स्मृतियों की मूलकता को प्रमाणित करते हुये भृगु ने कहा कि जो भी कुछ भगवान् मनु के द्वारा कहा गया है वह सभी कुछ वेद में निहित है वेद में ब्रह्मज्ञान है वही मनु ने अपने धर्मशास्त्र में प्रकट किया है। शंख ऋषि ने भी स्पष्ट किया कि स्मृतियाँ वेदमूलक है। तब यदि वेद एवं स्मृति प्रमाण स्वरूप तो अन्य धर्मशोस्त्रों के होने का क्या प्रयोजन है इसी को स्पष्ट करते हुये मरीचि लिखते हैं कि वैदिक शब्द अत्यन्त दुर्बोध हैं अतः उन्हें प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता इसीलिये स्मृतितन्त्र की रचना हुई। इस पर स्मृतिचन्द्रिकाकार लिखते हैं कि यही पुराणों के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है-एवं पुराणानामपि प्रामाण्यं प्रयोजनत्वं च सिद्धम्। पुराणों की प्रासंगिकता को प्रकट करते हुये विष्णु स्मृति ने पुनः कहा है-
पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्सितम्।
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः। (स्मृतिचन्द्रिका, प्रथम खण्ड, पृ. 3, विश्णुस्मृति)
पुराण, मनु द्वारा कहा गया धर्म, छः अंग तथा वेद ये चार आज्ञासिद्ध प्रमाण है इनकी अनावश्यक तर्क के लिये अवहेलना नहीं करनी चाहिये।। पुराणों के प्रयोजन के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य याज्ञवल्क्य ने समझाया है। याज्ञवल्क्य ने धर्म के लिये प्रमाण रूप में कहा-
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रिताः
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश।
विद्या एवं धर्म के प्रमाण के हेतु हैं- पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, छः अंगों सहित चार वेद ये कुल चैदह विद्या व धर्म के लिये प्रमाण हैं। पुराणों के प्रयोजन अथवा औचित्य को प्रकट करते हुये जीवगोस्वामी ने अपने ग्रन्थ तत्त्वसन्दर्भ में कहा है-स्कान्दमाग्नेयमित्यादिसमाख्यास्तु प्रवचननिबन्धाः काठकादिवत्। आनुपूर्वीनिर्माणनिबन्धना वा। तस्मात् क्वचिदनित्यत्वश्रवणम् तु आविर्भावातिरोभावापेक्षया। तदेवमितिहासपुराणयोर्वेदत्वं सिद्धम्। (पुराण पत्रिका, अंक-जनवरी 1962, पृ. 182)
स्पष्ट है कि इनका काठक संहिता की तरह नित्य पठन करना आवश्यक है इसी से इतिहास पुराण का वेदत्व सिद्ध होता है।
क्रमश: