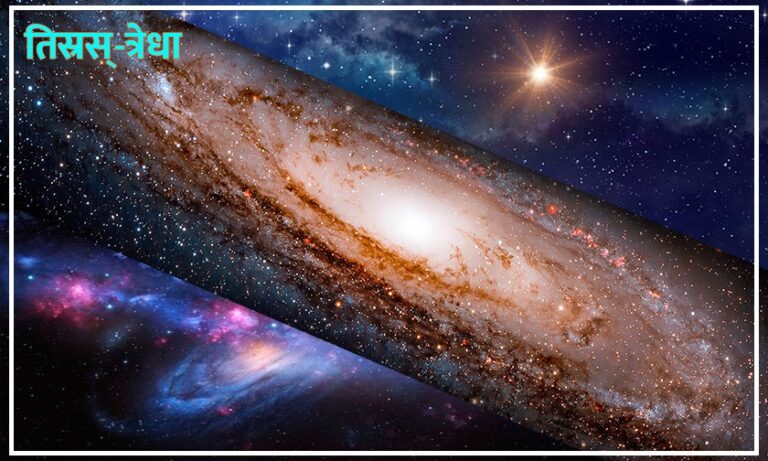- मिस्टिक ज्ञान
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
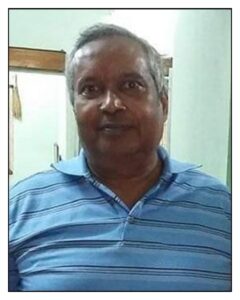 अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)–
१. अज्ञात के ज्ञान की विधि-विश्व या उसका चेतन रूप ब्रह्म अज्ञात है। विभिन्न दर्शनों या शास्त्रों में कई प्रकार के विभाजन द्वारा ही वह समझा जा सकता है।
नवैकादश पञ्च त्रीन् भावान् भूतेषु येन वै। ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्॥१४॥
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्। स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मकम्॥१५॥
(भागवत पुराण, ११/१९/१४-१५)
जगत् के अनन्त पदार्थों का ९, ११, ५, ३ में वर्गीकरण करना और अन्त में १ ही मूल तत्त्व देखना ज्ञान है। वर्गीकरण की पद्धति विज्ञान है। इसी को मुण्डक उपनिषद् (१/१/२) में परा-अपरा विद्या कहा है। परा विद्या को केवल विद्या तथा अपरा विद्या को अविद्या कहते हैं। यह विद्या का अभाव नहीं, उसका वर्गीकरण है। बिना सम्बन्ध समझे उनको भिन्न देखना भी विद्या का अभाव ही है।
वर्गीकरण के उदाहरण-न्याय वैशेषिक के ९ द्रव्य, ९ सर्ग, ९ दुर्गा, ५ महाभूत, विश्व के ५ पर्व, पञ्चाग्नि, ३ गुण, ३ लोक, ३ धाम, ॐ के ३ अक्षर, ११ रुद्र, मन सहित ११ इन्द्रियां, या सांख्य में प्रकृति-पुरुष के २५ तत्त्वों के अतिरिक्त शिव-शक्ति की ११ प्रत्यभिज्ञा।
२. त्रिविध विभाजन-अज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए उसे ३ भाग में समझते हैं-
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
= उस (ब्रह्म) का कार्य, करण आदि का पता नहीं चलता है, वैसा या अधिक कोई नहीं दीखता। हमारी कल्पना से परे है, अतः उसे ज्ञान-बल-क्रिया रूप में देखते हैं।
रामानुजाचार्य ने पुरी मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय यह मन्त्र कहा था जो महालक्ष्मी मन्दिर के मण्डप में आचार्य के चित्र के पास लिखा है। ज्ञान घन = जगन्नाथ, बल रूप = बलराम, क्रिया रूप = सुभद्रा।
३. तिस्रस्त्रेधा-वेद में देवी के ३ रूपों का पुनः ३-३ विभाजन लिखा है-
तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा। तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम्॥ (वाज. यजु. २०/६३)
=सरस्वती, इळा, भारती (अश्विन् द्वारा)-ये ३ देवियां पुनः ३-३ में विभाजित हैं। इनको सोम अर्पण से इन्द्र (या इन्द्रिय) की पुष्टि होती है।
अश्विनौ का सदा द्विवचन में प्रयोग है-नासिका के २ छिद्र, श्वास-प्रश्वास, विद्या-अविद्या, सम्भूति-विनाश (ईशावास्योपनिषद्, ९-११, १२-१४) आदि २ प्रकार से देखते हैं। पण्डित मधुसूदन ओझा ने इसे द्विनियति (दुनिया) कहा है (संशय तदुच्छेद वाद, १/१-२)। ऋग्वेद के सूक्त (१/३४) के देवता अश्विनौ हैं-उसमें ३३ प्रकार के ३ विभाजनों का उल्लेख है। अन्य स्थानों पर भी अश्विन् द्वारा त्रित उल्लेख हैं।
अश्विन् (प्राणायाम) द्वारा योग साधना होती है। इस आन्तरिक यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में है, अतः वहां अश्विन् शब्द का ही प्रयोग है।
देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरश्विनेळा सरस्वती। शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज। (वाज. यजु. २१/५४)
= शूष (सुषिर = छेद, सुषुम्ना) के मध्य के अनाहत चक्र में देवी का ध्यान होता है। अनाहत चक्र का चिह्न भी २ त्रिकोण युक्त है। अधोमुख त्रिकोण त्रिगुणात्मक शक्ति है। उसका ऊर्ध्वमुख त्रिकोण से पुनः विभाजन हुआ है। उससे नाभि के मणिपूर चक्र में इन्द्र की शक्ति धारण होती है। इसके केन्द्र में अधोमुख शक्ति त्रिकोण है, जिसमें अग्नि जल रही है। भौतिक रूप में यहां जठराग्नि है, जो अन्न का पाचन कर शरीर को शक्ति देता है।
ऋग्वेद में क्रिया या यज्ञ नहीं है। स्थिति रूप में वहां के ३ विभाजन हैं-भारती, इळा, सरस्वती।
(१) इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। (ऋक्, १/१३/९, ५/५/८, अथर्व, ५/२७९)
(२) भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये। (ऋक्, १/१८८/८)
(३) शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती। इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः (ऋक्, १/१४२/९)
(४) भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही। इमं नो यज्ञमा गमन् तिस्रो देवी सुपेशसः॥ (ऋक्, ९/५/८)
(५) सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः।
तिस्रो देवी स्वधया बर्हि रेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य॥ (ऋक्, २/३/८)
(६) आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः।
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। (ऋक्, ३/४/८, ७/२/८)
(७) तिस्रो देवीर्बर्हिरिदं वरीय आ सीदत चकृमा वः स्योनम्।
मनुष्वद् यज्ञं सुधिता हवींषीळा घृतपदी जुषन्त। (ऋक्, १०/७०/८)
(८) आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विळा मनुष्वदिह चेतयन्ती।
तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु। (ऋक्, १०/११०/८)
निरुक्त (८/१३) के अनुसार भरत आदित्य है, भारती उसकी भा (प्रकाश) है। आदित्य विश्व का वह रूप है, जिससे इस का आदि या आरम्भ हुआ है। इस का क्षेत्र भा या भारती है। स्वयम्भू मण्डल (पूर्ण विश्व), परमेष्ठी मण्डल (हमारा ब्रह्माण्ड, आकाशगंगा), तथा सौर मण्डल-इन ३ धामों के आदित्य हैं-अर्यमा, वरुण, मित्र। ये अभी खाली स्थान अन्तरिक्ष या व्रत में दीखते हैं।
तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीरुत द्यून्त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम्।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारु॥ (ऋक्, २/२७/८)
आदित्यों का प्रभाव क्षेत्र भारती है, जिसमें निर्माण हो रहा है, अतः इसे ब्राह्मी भी कहा है-ब्राह्मी तु भारती (अमरकोष, १/६/१)।
इळा दृश्य भूमि है जो सीमाबद्ध पिण्ड है। पिण्ड भू है, उस पर क्रिया या यज्ञ गो या इळा है-
गोभूवाचस्त्विडा इला (अमरकोष, ३/३/४२)।
सरस्वती ज्ञान का स्रोत है- सरस्वती साधयन्ती धियं (ऋक्, २/३/८)। शं सरस्वती सह धी भिरस्तु (ऋक्, ७/३५/११)। शं अर्थात् शान्त रहने से ही धी आती है तथा स्थिर रहती है।
४. चण्डी पाठ के त्रिक-चण्डी पाठ में परा अज्ञेय प्रकृति का वर्णन देवी-अथर्वशीर्ष में है। वहां भी अश्विन् या युग्मों द्वारा ही वर्णन है-
प्रकृति-पुरुष, आनन्द-अनानन्द, विज्ञान-अविज्ञान, ब्रह्म-अब्रह्म, पञ्चभूत-अपञ्च या अविभक्त भूत, वेद-अवेद, विद्या-अविद्या, अजा-अनजा आदि। उसके बाद अन्य वर्ग हैं।
कल्पना योग्य देवी का प्रथम रूप महाकाली है। महः का अर्थ त्रिलोकी या किसी पुर का आवरण है-महर् से महल हुआ है। उसमें परिवर्तन का आभास काल है। इसका अदृश्य कारण महाकाली है। यह मूल रूप अन्धकार में या परोक्ष है, अतः इसका कृष्ण वर्ण है।
महाकाली का १ अध्याय है। इसके त्रिविध विभाजन द्वारा महालक्ष्मी के ३ अध्याय हैं। दृश्य जगत् लक्ष्मी है। उसका तेज या प्रभाव श्री है जो दीखता नहीं है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ (वाज. यजु, ३१/२२)।
पुनः ३ विभाजन होने पर महा-सरस्वती चरित्र ९ अध्याय में है।
पिण्ड या विन्दु रूप पुरुष देव है, वह पुर या संरचना में रहता है। उसका क्षेत्र श्री या स्त्री रूप देवी है। यह मनुष्य याअन्य पशु में प्रजनन क्रिया के अर्थ का विस्तार है। जन्म माता के गर्भ में ही होता है, अतः क्षेत्र रूप स्त्री है। पुरुष का योगदान विन्दु मात्र है, अतः सीमाबद्ध पिण्ड रूप पुरुष है। दोनों के प्राण देव या देवी हैं। वेद में देवता शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि प्राण पिण्ड रूप में नहीं दीखता है। लोक भाषा में भी ऐसे ही लिंग विभाजन है-१ केश पुल्लिंग है, उनका समूह या क्षेत्र चोटी, वेणी, मूंछ, दाढ़ी-ये सभी स्त्रीलिंग हैं। सैनिक पुल्लिंग है, किन्तु उनका समूह सेना, वाहिनी आदि स्त्रीलिंग हैं एक अन्य लक्षण है कि वृषा (वर्षा करने वाला, देने वाला जिससे विकिरण हो) वह पुरुष है। उसे ग्रहण करने वाला या युक्त होने वाला क्षेत्र योषा का अर्थ स्त्री है। अग्नि-सोम का भी ऐसा विभाजन है।
चण्डी पाठ के महाकाली स्वरूप में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि आरम्भ का वर्णन है। इसमें विष्णु के जाग्रत रूप को जगन्नाथ कहा गया है। काली रूप में देवी ने रक्तबीजों (वायरस) का भक्षण किया था। प्रकृति में यह काम नीम करता है, जो काली का प्रतीक है। जगन्नाथ दक्षिणाकाली रूप होने के कारण उनकी मूर्त्ति भी नीम काष्ठ से बनती है। सूर्य विष्णु रूप में अपने आकर्षण से पृथ्वी का धारण करता है-पृथिवी त्वया धृता लोका, देवि त्वं विष्णुना धृता। उससे निकले इन्द्र रूपी प्रकाश द्वारा पृथ्वी कर जीवन चलता है। वह जगन्नाथ रूप है। विष्णु दृश्य रूप है, जगत् या जीवन क्रिया अदृश्य रूप है। जगदव्यक्तमूर्तिना (गीता ९/४) जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं (नारद परिव्राजक उपनिषद् ४/५०)
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥७१॥
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ॥९०॥
जाग्रत होने के बाद-उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तत्या मुक्तो जनार्दनः॥९१॥
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु॥८६॥
महालक्ष्मी चरित्र में विष्णु के तेज से शक्ति का निर्माण हुआ, तब अन्य देवों की शक्ति भी उसमें मिली।
महासरस्वती चरित्र में देवी के दूत रूप में शिव हैं। अतः इन ३ चरित्रों के ऋषि हैं-ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ऋक्-यजु-साम का रूप अग्नि-वायु या गति, महिमा या रवि है। अतः इन चरित्रों के स्वरूप ऋक्-यजु-साम तथा तत्त्व हैं-अग्नि, वायु, सूर्य।
३ चरित्रों के छन्द हैं-गायत्री (२४ अक्षर), उष्णिक् (२८ अक्षर), अनुष्टुप् (३२ अक्षर)। पाठ में अधिकांश छन्द अनुष्टुप् हैं, क्योंकि वाक् अनुष्टुप् है-हर अक्षर में ८ वर्ण तक हो सकते हैं, जो बीच के स्वर से जुड़े हैं। स्तुति के श्लोक (मुख्यतः ११ अध्याय में, या गीता के भी ११ अध्याय में) त्रिष्टुप् (११ x ४ अक्षर) में हैं, क्योंकि मनुष्य का मेरुदण्ड इसका ३ पाद (३३ भाग) है। इन छ्न्द अक्षरों के अनुसार श्लोक संख्या गिनने पर चण्डी पाठ में ७०० श्लोक होंगे। इसमें ३ एकाक्षर श्लोक-ऐं, ह्रीं, क्लीं परात्पर ॐ, तथा देव्यथर्वशीर्ष के २७ श्लोक मिलाने पड़ेंगे।
मध्यम चरित्र का आरम्भ ह्रीं से हुआ है जो महालक्ष्मी का मन्त्र है। यह हृदय स्थान है, जिसमें विष्णु रह कर भूतों को चला रहे हैं-
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ (गीता, १८/६१)
हृदय स्थान लक्ष्मी है (ह्रीं) उसमें कर्त्ता रूप ईश्वर है। हृदय की ३ क्रिया हैं-हृ = लेना, द = देना, य = नियमन। मनुष्य का हृदय रक्त लेता है, उसे नसों में भेज कर प्रवाहित करता है तथा हृदय गति के अनुसार चलता है। मस्तिष्क में भी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सूचना आती है, उससे कर्मेन्द्रियों को निर्देश जाता है, तथा नाड़ी गति से काम करता है। अतः यह भी हृदय है जिससे भावों का आदान-प्रदान होता है।
ऐं सरस्वती का बीज मन्त्र है। ऐं आश्चर्य प्रकट करता है, उससे जिज्ञासा होती है, जिसके बाद ज्ञान होता है। दुर्वासा के त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र, ३ के अनुसार यह ऋक्-यजु-साम के प्रथम अक्षरों अ, इ, अ का समन्वय है। अ+ (अ + इ) = अ + ए = ऐ।
क्लीं काली का बीज मन्त्र है। इसका एक स्वरूप कृष्ण का बीज मन्त्र क्रीं है। बीज मन्त्रों क्रीं, क्लीं के ही लौकिक रूप कृष्ण-काली हैं। इनमें र, ल का अन्तर है। र वायु या गति तत्त्व है, ल अग्नि तत्त्व है। माहेश्वर सूत्र में यह ऋलृक् है। अतः ऋत्, ऋतु आदि सोम का प्रवाह हैं। लृक् अग्नि प्रवाह है-लोक भाषा में लूक। सोम का विस्तार रूप काली है, उसका सघन या केन्द्र रूप कृष्ण है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो (ऋक्, १/३५/२, वाज, ३३/४३, ३४/३१ आदि)। अरबी में संयुक्त अक्षर नहीं होने से क्रीं, क्लीं, का करीम, कलीम हो गया है।
अन्य २ चरित्रों में बीज मन्त्रों का क्रम उलटा हो गया है। ज्ञान रूप शिव या सरस्वती के बाद विनाश क्रम आरम्भ होता है। ज्ञान पाने वाले में परिवर्तन होता है, जिसका निरीक्षण या प्रयोग करना है, उसमें भी परिवर्तन होता है। अतः शिव प्रलय के भी रूप हैं। प्रलय के बाद सृष्टि चक्र आरम्भ होने पर पुनः ज्ञान होता है। अतः महाकाली चरित्र में सरस्वती बीज और महासरस्वती चरित्र में काली बीज है।
मर्त्यानि हीमानि शरीराणीँ अमृतैषा देवता (प्राणः)-ऐतरेय आरण्यक (२/१/८)
अन्तरं मृत्योरमृतम्-इति। अवरं ह्येतन्मृत्योरमृतम्। मृत्यावमृतमाहितम्-इति। (शतपथ ब्राह्मण, १०/५/२/४)
अप् को अमृत और उससे जो मुक्त हुआ वह मृत्यु है। अलग होने को मुच्यु कहा है, मुच्यु से मृत्यु हुआ है-
स समुद्रादमुच्यत स मुच्युरभवत् तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते परोक्षेण। (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, १/७)
५. त्रयी विद्या- तीन विभाजन द्वारा ज्ञान होता है, अतः वेद को भी त्रयी कहते हैं। किसी भी प्रकार ३ का विभाजन करें, कुछ चीजें अविभाज्य रह जाती हैं। अविभाज्य तत्त्व को परात्पर ब्रह्म कहते हैं। यह हमारे किसी विभाजन में नहीं आता है, अतः इसके वर्णन को नेति कहते हैं। जैसे गजेन्द्र मोक्ष में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है-
स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः।
नायं गुणं कर्म न सन्न चासन्, निषेध-शेषो जयतादशेषः॥
(भागवत पुराण, ८/३/२४)
अविभक्त ब्रह्म रूप अथर्व वेद को मिला कर त्रयी का अर्थ ४ वेद होता है-१ मूल + ३ शाखा। इसका प्रतीक पलास दण्ड है जिसमें शाखा से ३ पत्ते निकलते हैं। इस प्रतीक का प्रयोग वेदारम्भ संस्कार में होता है।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठ- मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह॥१॥
द्वे विद्ये वेदितव्ये- … परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डक उपनिषद्, १/१/१, ४, ५)
यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः।
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति॥ (ऋक्, १०/१३५/१)
सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां योनिर्यत् पलासः। (स्वायम्भुव ब्रह्मरूपत्त्वात्)
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः-ऐतरेय ब्राह्मण, २/१)
वेद के ३ विभाजन इस प्रकार हैं-मूर्ति रूप ऋक्, गति रूप यजु, महिमा रूप साम, तथा अविभाज्य ब्रह्म रूप अथर्व।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
इसी प्रसंग में तैत्तिरीय ब्राह्मण में ५३ प्रकार का त्रयी विभाजन दिया है।
ज्ञान का क्रम भी वही है, मूर्त्ति या सत्ता रहने पर ही उसका ज्ञान होगा। उस वस्तु से प्रकाश, ध्वनि आदि द्वारा सूचना आनी चाहिये। यह गति रूप यजु है। वस्तु का प्रभाव क्षेत्र या साम जहां तक है, वहीं तक उसका ज्ञान हो सकता है। अतः भगवान् ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है (गीता, १०/२२)। वस्तु की पहचान के लिए वह परिवेश से भिन्न होना चाहिये, गति तथा महिमा भी परिवेश के सापेक्ष ही है। वह परिवेश या आधार अथर्व वेद है। इसी अनुसार विद् धातु के ४ अर्थ हैं-
ऋक्-विद् सत्तायाम् (धातुपाठ, ४/६०),
यजु-विद्लृ लाभे (६/१४१)
साम-विद् ज्ञाने (२/५७)
अथर्व-विद् विचारणे (७/१३) या विद् चेतनाख्यान निवासेषु (१०/१७७)।
६. गायत्री त्रिक-सभी छन्द ४ पाद के होते हैं, किन्तु ३ खण्ड में अर्थ होने के कारण गायत्री मन्त्र के ३ पाद हैं।
तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। (मीमांसा सूत्र, २/१/३५)
छन्द-पाद का अर्थ है, वाक्य तथा पद (वाक्यांश)।
मूल विन्दु से सृष्टि का आरम्भ हुआ। ३ गुण या ब्रह्मा-विष्णु-शिव रूप में विभाजन ॐ के ३ अक्षर हैं। मूल विन्दु अर्ध मात्रा रूप में बच जाता है जो चण्डी पाठ (१/७४) में परा प्रकृति का स्वरूप कहा है-
अर्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः।
गायत्री के भी ३ पाद विभाजन के बाद अव्यक्त अविभाज्य पद बच जाता है, जिसे परोरजा (लोकोत्तर) कहते हैं। विभाज्य पदों में भी प्रत्येक के पुनः ३-३ विभाग हैं-
(१) भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ, (२) ऋक्, यजु, साम, (३) प्राण-अपान-व्यान। (बृहदारण्यक उपनिषद्, ५/१४/१-४)
ॐ का विस्तार ३ लोकों में हुआ-भू, भुवः, स्वः। ३ धामों में ३-३ लोक होने से ७ लोक हुए, दो धामों के बीच के लोक समान हैं।
अवम लोक सौर मण्डल में-भू (पृथ्वी), भुवः (नेपचून तक ग्रह कक्षा), स्वः (३३ धाम तक सौर मण्डल)।
मध्यम धाम ब्रह्माण्ड का भू लोक अवम का स्वः लोक है। उसका भुवः महर्लोक तथा स्वः जनः लोक है।
परम धाम का भू लोक ब्रह्माण्ड या जनः लोक है। मध्यम तपः लोक है जहां तक का ताप या प्रकाश हम तक पहुंचता है। उसका स्वःलोक अनन्त सत्य लोक है।
गायत्री का प्रथम पद आकाश का आधिदैविक वर्णन है, मध्यम पाद दृश्य आधिभौतिक जगत् है, उत्तर पाद आध्यात्मिक या शरीर पर प्रभाव है।ये ब्रह्म के ३ वर्णनीय रूपों के विषय में हैं-स्रष्टा रूप ब्रह्मा, तेज या क्रिया रूप विष्णु, तथा ज्ञान रूप शिव।
ॐ भूर्भुवः स्वः/तत् सवितुर्वरेण्यं/भर्गो देवस्य धीमहि/धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी देव रूपों के भी ३ भाग इन ३ पादों से व्यक्त होते हैं-
(१) विष्णु-इक्षा या क्रियात्मक विचार, सूर्य, प्रत्येक व्यक्ति का मन। सृष्टि में हर व्यक्ति का मन या पिण्ड प्रायः स्वतन्त्र हैं, इसी कारण सबका स्वतन्त्र अस्तित्व है। इसका प्रतीक पीपल है जिसके पत्ते मनुष्य के मन जैसे डोलते हैं।
(२) शिव-परमेश्वर जिसके मन में प्रथम विचार उत्पन्न हुआ, तेज के विभिन्न क्षेत्र-रुद्र, शिव (शतरुद्र, सहस्र रुद्र, लक्ष रुद्र), शिवतर, शिवतम, सदाशिव, आदिगुरु रूप शिव। गुरु परम्परा का प्रतीक वट वृक्ष है जिसकी हवाई जड़ जमीन से लग कर वैसा ही वृक्ष बन जाती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य को ज्ञान दे कर अपने जैसा मनुष्य बना देता है।
(३) ब्रह्मा-मूल रस रूप पदार्थ, ५ पर्वों के पिण्ड (स्वयम्भू, ब्रह्माण्ड, तारा, ग्रह, तथा ग्रहों के जीव), ज्ञान संहति के रूप में वेदत्रयी। त्रयी का अर्थ ४ वेद होता है १ मूल (अथर्व) तथा ३ शाखा-ऋक्, यजु, साम (मुण्डकोपनिषद् १/१/१-५)। इसका प्रतीक पलास वृक्ष है, जिसकी शाखा से ३ पत्ते निकलते हैं पर मूल भी बचा रहता है।
(४) हनुमान्-स्रष्टा रूप वृषाकपि है, जो पहले जैसी सृष्टि करता है (सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्-ऋग्वेद १०/१९०/३)। तेज या गति रूप मारुति है। मन को प्रेरित करने वाला रूप मनोजव है (योगसूत्र ३/४९, ऋग्वेद १०/७१/७-८)। इसका प्रतीक मूल वट की शाखाओं से बने वृक्ष हैं जिनको लोकभाषा में दुमदुमा (द्रुम से द्रुम) कहते हैं।
(५) देवी रूप में वैदिक भाषा में भारती, इला, सरस्वती है तथा पौराणिक भाषा में महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती हैं (दुर्गा सप्तशती के ३ चरित्र)।
इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः (ऋक्, १/१३/९, ५/११/८)
भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे (ऋक्, १/१८८/८)
(६) गणेश रूप में प्रथम पाद उच्छिष्ट गणपति (१ पाद से विश्व बनने के बाद बचा मूल स्रोत) है, दृश्य जगत् के पिण्डों का समूह महा गणपति, तथा लोकों का गण या उसका मुख्य गणेश है। पुरुष सूक्त (वाजसनेयि यजु, अध्याय, ३१/३)-
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥३
अथर्व, शौनक, ११/७ उच्छिष्ट सूक्त-
उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः।
उच्छिष्टे इन्द्राग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम्॥१॥
उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्।
आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः॥२॥
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ (२१-२७)
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे (ऋक्, २/२३/१, वाज. सं. २३/१९, तै. सं. २/३/१४/३, मै. सं. १६६/११, काण्व. सं. ४/१)
गणनात्मक ज्ञान या शब्दों में प्रकट ज्ञान गणेश है-
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं —त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। (गणेश अथर्वशीर्ष, ४)
(७) इसी प्रकार कार्तिकेय (सुब्रह्म) सरस्वती, काली, लक्ष्मी के भी ३ रूप किये जा सकते हैं।
कार्तिकेय (सुब्रह्म)-मूल सरिर् या सलिल रूप, तारा संहति को ब्रह्माण्ड रूप में देखना, कणों का समूह पिण्ड रूप में देखना।
वातस्य जूतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये। (वा॰ यजुर्वेद, १३/४२)
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य उप प्र याहि दिव्यानि धाम ।(वा॰ यजुर्वेद, १५/५२)
ब्रह्म से सुब्रह्म-
ॐ ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत् स्वयं त्वेकमेव तदैक्षत महद्वै यक्षं तदेकमेवास्मि हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति तदभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत् तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य ललाटे स्नेहो यदार्द्र्यमाजायत तेनानन्दत् तमब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदामह इति । तद्यदब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदामह इति तस्मात् सुवेदोऽभवत्तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते॥ (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व १/१/१)
(८) सरस्वती-रस समुद्र का अनन्त विस्तार, ब्रह्माण्ड का सरस्वान् समुद्र, मस्तिष्क के भीतर समुद्र (मानसरोवर)।
यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति। (तैत्तिरीय उपनिषद् २/७)
मनो वै सरस्वान् (शतपथ ब्राह्मण, ७/५/१/३१, ११/२/४/९)
स्वर्गो लोकः सरस्वान् (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १६/५/१५)
वाक् सरस्वती (शतपथ ब्राह्मण, ७/५/१/३१, ११/२/४/९, १२/९/१/१३)
(९) काली-मूल अव्यक्त अज्ञात विश्व, व्यक्त विश्व में नित्य काल से परिवर्तन रूप जिसके बाद मूल रूप कभी वापस नहीं आता, काल का अनुभव या ज्ञान।
सप्त चक्रान् वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः।
सा इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत् कालः स ईषते प्रथमो नु देवः॥
(अथर्व, शौनक शाखा, १९/५३/२)
(१०) लक्ष्मी-अव्यक्त से दृश्य जगत् की उत्पत्ति, आकाश में अलग अलग रूप या आकार के पिण्ड, निकट की दृश्य वतुओं का ज्ञान, दृश्य वाक् या लिपि।
ततो विराडजायत, विराजो अधिपूरुषः।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः॥
(विराट् = दृश्य जगत्) (पुरुष सूक्त, ५)
यद्वै नास्ति तदलक्षणम् (शतपथ ब्राह्मण, ७/२/१/७)
तस्माद्यस्य सर्वतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते। (शतपथ ब्राह्मण, ८/५/४/३)
देवलक्ष्मं वै त्र्यालिखितं तामुत्तर लक्ष्माण देवा उपादधत (तैत्तिरीय सं. ५/२/८/३)
उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् (ऋक्, १०/७१/४)
अरुण कुमार उपाध्याय (धर्मज्ञ)–
१. अज्ञात के ज्ञान की विधि-विश्व या उसका चेतन रूप ब्रह्म अज्ञात है। विभिन्न दर्शनों या शास्त्रों में कई प्रकार के विभाजन द्वारा ही वह समझा जा सकता है।
नवैकादश पञ्च त्रीन् भावान् भूतेषु येन वै। ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्॥१४॥
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्। स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मकम्॥१५॥
(भागवत पुराण, ११/१९/१४-१५)
जगत् के अनन्त पदार्थों का ९, ११, ५, ३ में वर्गीकरण करना और अन्त में १ ही मूल तत्त्व देखना ज्ञान है। वर्गीकरण की पद्धति विज्ञान है। इसी को मुण्डक उपनिषद् (१/१/२) में परा-अपरा विद्या कहा है। परा विद्या को केवल विद्या तथा अपरा विद्या को अविद्या कहते हैं। यह विद्या का अभाव नहीं, उसका वर्गीकरण है। बिना सम्बन्ध समझे उनको भिन्न देखना भी विद्या का अभाव ही है।
वर्गीकरण के उदाहरण-न्याय वैशेषिक के ९ द्रव्य, ९ सर्ग, ९ दुर्गा, ५ महाभूत, विश्व के ५ पर्व, पञ्चाग्नि, ३ गुण, ३ लोक, ३ धाम, ॐ के ३ अक्षर, ११ रुद्र, मन सहित ११ इन्द्रियां, या सांख्य में प्रकृति-पुरुष के २५ तत्त्वों के अतिरिक्त शिव-शक्ति की ११ प्रत्यभिज्ञा।
२. त्रिविध विभाजन-अज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए उसे ३ भाग में समझते हैं-
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
= उस (ब्रह्म) का कार्य, करण आदि का पता नहीं चलता है, वैसा या अधिक कोई नहीं दीखता। हमारी कल्पना से परे है, अतः उसे ज्ञान-बल-क्रिया रूप में देखते हैं।
रामानुजाचार्य ने पुरी मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय यह मन्त्र कहा था जो महालक्ष्मी मन्दिर के मण्डप में आचार्य के चित्र के पास लिखा है। ज्ञान घन = जगन्नाथ, बल रूप = बलराम, क्रिया रूप = सुभद्रा।
३. तिस्रस्त्रेधा-वेद में देवी के ३ रूपों का पुनः ३-३ विभाजन लिखा है-
तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा। तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम्॥ (वाज. यजु. २०/६३)
=सरस्वती, इळा, भारती (अश्विन् द्वारा)-ये ३ देवियां पुनः ३-३ में विभाजित हैं। इनको सोम अर्पण से इन्द्र (या इन्द्रिय) की पुष्टि होती है।
अश्विनौ का सदा द्विवचन में प्रयोग है-नासिका के २ छिद्र, श्वास-प्रश्वास, विद्या-अविद्या, सम्भूति-विनाश (ईशावास्योपनिषद्, ९-११, १२-१४) आदि २ प्रकार से देखते हैं। पण्डित मधुसूदन ओझा ने इसे द्विनियति (दुनिया) कहा है (संशय तदुच्छेद वाद, १/१-२)। ऋग्वेद के सूक्त (१/३४) के देवता अश्विनौ हैं-उसमें ३३ प्रकार के ३ विभाजनों का उल्लेख है। अन्य स्थानों पर भी अश्विन् द्वारा त्रित उल्लेख हैं।
अश्विन् (प्राणायाम) द्वारा योग साधना होती है। इस आन्तरिक यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में है, अतः वहां अश्विन् शब्द का ही प्रयोग है।
देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरश्विनेळा सरस्वती। शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज। (वाज. यजु. २१/५४)
= शूष (सुषिर = छेद, सुषुम्ना) के मध्य के अनाहत चक्र में देवी का ध्यान होता है। अनाहत चक्र का चिह्न भी २ त्रिकोण युक्त है। अधोमुख त्रिकोण त्रिगुणात्मक शक्ति है। उसका ऊर्ध्वमुख त्रिकोण से पुनः विभाजन हुआ है। उससे नाभि के मणिपूर चक्र में इन्द्र की शक्ति धारण होती है। इसके केन्द्र में अधोमुख शक्ति त्रिकोण है, जिसमें अग्नि जल रही है। भौतिक रूप में यहां जठराग्नि है, जो अन्न का पाचन कर शरीर को शक्ति देता है।
ऋग्वेद में क्रिया या यज्ञ नहीं है। स्थिति रूप में वहां के ३ विभाजन हैं-भारती, इळा, सरस्वती।
(१) इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। (ऋक्, १/१३/९, ५/५/८, अथर्व, ५/२७९)
(२) भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये। (ऋक्, १/१८८/८)
(३) शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती। इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः (ऋक्, १/१४२/९)
(४) भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही। इमं नो यज्ञमा गमन् तिस्रो देवी सुपेशसः॥ (ऋक्, ९/५/८)
(५) सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः।
तिस्रो देवी स्वधया बर्हि रेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य॥ (ऋक्, २/३/८)
(६) आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः।
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। (ऋक्, ३/४/८, ७/२/८)
(७) तिस्रो देवीर्बर्हिरिदं वरीय आ सीदत चकृमा वः स्योनम्।
मनुष्वद् यज्ञं सुधिता हवींषीळा घृतपदी जुषन्त। (ऋक्, १०/७०/८)
(८) आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विळा मनुष्वदिह चेतयन्ती।
तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु। (ऋक्, १०/११०/८)
निरुक्त (८/१३) के अनुसार भरत आदित्य है, भारती उसकी भा (प्रकाश) है। आदित्य विश्व का वह रूप है, जिससे इस का आदि या आरम्भ हुआ है। इस का क्षेत्र भा या भारती है। स्वयम्भू मण्डल (पूर्ण विश्व), परमेष्ठी मण्डल (हमारा ब्रह्माण्ड, आकाशगंगा), तथा सौर मण्डल-इन ३ धामों के आदित्य हैं-अर्यमा, वरुण, मित्र। ये अभी खाली स्थान अन्तरिक्ष या व्रत में दीखते हैं।
तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीरुत द्यून्त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम्।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारु॥ (ऋक्, २/२७/८)
आदित्यों का प्रभाव क्षेत्र भारती है, जिसमें निर्माण हो रहा है, अतः इसे ब्राह्मी भी कहा है-ब्राह्मी तु भारती (अमरकोष, १/६/१)।
इळा दृश्य भूमि है जो सीमाबद्ध पिण्ड है। पिण्ड भू है, उस पर क्रिया या यज्ञ गो या इळा है-
गोभूवाचस्त्विडा इला (अमरकोष, ३/३/४२)।
सरस्वती ज्ञान का स्रोत है- सरस्वती साधयन्ती धियं (ऋक्, २/३/८)। शं सरस्वती सह धी भिरस्तु (ऋक्, ७/३५/११)। शं अर्थात् शान्त रहने से ही धी आती है तथा स्थिर रहती है।
४. चण्डी पाठ के त्रिक-चण्डी पाठ में परा अज्ञेय प्रकृति का वर्णन देवी-अथर्वशीर्ष में है। वहां भी अश्विन् या युग्मों द्वारा ही वर्णन है-
प्रकृति-पुरुष, आनन्द-अनानन्द, विज्ञान-अविज्ञान, ब्रह्म-अब्रह्म, पञ्चभूत-अपञ्च या अविभक्त भूत, वेद-अवेद, विद्या-अविद्या, अजा-अनजा आदि। उसके बाद अन्य वर्ग हैं।
कल्पना योग्य देवी का प्रथम रूप महाकाली है। महः का अर्थ त्रिलोकी या किसी पुर का आवरण है-महर् से महल हुआ है। उसमें परिवर्तन का आभास काल है। इसका अदृश्य कारण महाकाली है। यह मूल रूप अन्धकार में या परोक्ष है, अतः इसका कृष्ण वर्ण है।
महाकाली का १ अध्याय है। इसके त्रिविध विभाजन द्वारा महालक्ष्मी के ३ अध्याय हैं। दृश्य जगत् लक्ष्मी है। उसका तेज या प्रभाव श्री है जो दीखता नहीं है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ (वाज. यजु, ३१/२२)।
पुनः ३ विभाजन होने पर महा-सरस्वती चरित्र ९ अध्याय में है।
पिण्ड या विन्दु रूप पुरुष देव है, वह पुर या संरचना में रहता है। उसका क्षेत्र श्री या स्त्री रूप देवी है। यह मनुष्य याअन्य पशु में प्रजनन क्रिया के अर्थ का विस्तार है। जन्म माता के गर्भ में ही होता है, अतः क्षेत्र रूप स्त्री है। पुरुष का योगदान विन्दु मात्र है, अतः सीमाबद्ध पिण्ड रूप पुरुष है। दोनों के प्राण देव या देवी हैं। वेद में देवता शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि प्राण पिण्ड रूप में नहीं दीखता है। लोक भाषा में भी ऐसे ही लिंग विभाजन है-१ केश पुल्लिंग है, उनका समूह या क्षेत्र चोटी, वेणी, मूंछ, दाढ़ी-ये सभी स्त्रीलिंग हैं। सैनिक पुल्लिंग है, किन्तु उनका समूह सेना, वाहिनी आदि स्त्रीलिंग हैं एक अन्य लक्षण है कि वृषा (वर्षा करने वाला, देने वाला जिससे विकिरण हो) वह पुरुष है। उसे ग्रहण करने वाला या युक्त होने वाला क्षेत्र योषा का अर्थ स्त्री है। अग्नि-सोम का भी ऐसा विभाजन है।
चण्डी पाठ के महाकाली स्वरूप में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि आरम्भ का वर्णन है। इसमें विष्णु के जाग्रत रूप को जगन्नाथ कहा गया है। काली रूप में देवी ने रक्तबीजों (वायरस) का भक्षण किया था। प्रकृति में यह काम नीम करता है, जो काली का प्रतीक है। जगन्नाथ दक्षिणाकाली रूप होने के कारण उनकी मूर्त्ति भी नीम काष्ठ से बनती है। सूर्य विष्णु रूप में अपने आकर्षण से पृथ्वी का धारण करता है-पृथिवी त्वया धृता लोका, देवि त्वं विष्णुना धृता। उससे निकले इन्द्र रूपी प्रकाश द्वारा पृथ्वी कर जीवन चलता है। वह जगन्नाथ रूप है। विष्णु दृश्य रूप है, जगत् या जीवन क्रिया अदृश्य रूप है। जगदव्यक्तमूर्तिना (गीता ९/४) जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं (नारद परिव्राजक उपनिषद् ४/५०)
विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥७१॥
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ॥९०॥
जाग्रत होने के बाद-उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तत्या मुक्तो जनार्दनः॥९१॥
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु॥८६॥
महालक्ष्मी चरित्र में विष्णु के तेज से शक्ति का निर्माण हुआ, तब अन्य देवों की शक्ति भी उसमें मिली।
महासरस्वती चरित्र में देवी के दूत रूप में शिव हैं। अतः इन ३ चरित्रों के ऋषि हैं-ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ऋक्-यजु-साम का रूप अग्नि-वायु या गति, महिमा या रवि है। अतः इन चरित्रों के स्वरूप ऋक्-यजु-साम तथा तत्त्व हैं-अग्नि, वायु, सूर्य।
३ चरित्रों के छन्द हैं-गायत्री (२४ अक्षर), उष्णिक् (२८ अक्षर), अनुष्टुप् (३२ अक्षर)। पाठ में अधिकांश छन्द अनुष्टुप् हैं, क्योंकि वाक् अनुष्टुप् है-हर अक्षर में ८ वर्ण तक हो सकते हैं, जो बीच के स्वर से जुड़े हैं। स्तुति के श्लोक (मुख्यतः ११ अध्याय में, या गीता के भी ११ अध्याय में) त्रिष्टुप् (११ x ४ अक्षर) में हैं, क्योंकि मनुष्य का मेरुदण्ड इसका ३ पाद (३३ भाग) है। इन छ्न्द अक्षरों के अनुसार श्लोक संख्या गिनने पर चण्डी पाठ में ७०० श्लोक होंगे। इसमें ३ एकाक्षर श्लोक-ऐं, ह्रीं, क्लीं परात्पर ॐ, तथा देव्यथर्वशीर्ष के २७ श्लोक मिलाने पड़ेंगे।
मध्यम चरित्र का आरम्भ ह्रीं से हुआ है जो महालक्ष्मी का मन्त्र है। यह हृदय स्थान है, जिसमें विष्णु रह कर भूतों को चला रहे हैं-
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ (गीता, १८/६१)
हृदय स्थान लक्ष्मी है (ह्रीं) उसमें कर्त्ता रूप ईश्वर है। हृदय की ३ क्रिया हैं-हृ = लेना, द = देना, य = नियमन। मनुष्य का हृदय रक्त लेता है, उसे नसों में भेज कर प्रवाहित करता है तथा हृदय गति के अनुसार चलता है। मस्तिष्क में भी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सूचना आती है, उससे कर्मेन्द्रियों को निर्देश जाता है, तथा नाड़ी गति से काम करता है। अतः यह भी हृदय है जिससे भावों का आदान-प्रदान होता है।
ऐं सरस्वती का बीज मन्त्र है। ऐं आश्चर्य प्रकट करता है, उससे जिज्ञासा होती है, जिसके बाद ज्ञान होता है। दुर्वासा के त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र, ३ के अनुसार यह ऋक्-यजु-साम के प्रथम अक्षरों अ, इ, अ का समन्वय है। अ+ (अ + इ) = अ + ए = ऐ।
क्लीं काली का बीज मन्त्र है। इसका एक स्वरूप कृष्ण का बीज मन्त्र क्रीं है। बीज मन्त्रों क्रीं, क्लीं के ही लौकिक रूप कृष्ण-काली हैं। इनमें र, ल का अन्तर है। र वायु या गति तत्त्व है, ल अग्नि तत्त्व है। माहेश्वर सूत्र में यह ऋलृक् है। अतः ऋत्, ऋतु आदि सोम का प्रवाह हैं। लृक् अग्नि प्रवाह है-लोक भाषा में लूक। सोम का विस्तार रूप काली है, उसका सघन या केन्द्र रूप कृष्ण है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो (ऋक्, १/३५/२, वाज, ३३/४३, ३४/३१ आदि)। अरबी में संयुक्त अक्षर नहीं होने से क्रीं, क्लीं, का करीम, कलीम हो गया है।
अन्य २ चरित्रों में बीज मन्त्रों का क्रम उलटा हो गया है। ज्ञान रूप शिव या सरस्वती के बाद विनाश क्रम आरम्भ होता है। ज्ञान पाने वाले में परिवर्तन होता है, जिसका निरीक्षण या प्रयोग करना है, उसमें भी परिवर्तन होता है। अतः शिव प्रलय के भी रूप हैं। प्रलय के बाद सृष्टि चक्र आरम्भ होने पर पुनः ज्ञान होता है। अतः महाकाली चरित्र में सरस्वती बीज और महासरस्वती चरित्र में काली बीज है।
मर्त्यानि हीमानि शरीराणीँ अमृतैषा देवता (प्राणः)-ऐतरेय आरण्यक (२/१/८)
अन्तरं मृत्योरमृतम्-इति। अवरं ह्येतन्मृत्योरमृतम्। मृत्यावमृतमाहितम्-इति। (शतपथ ब्राह्मण, १०/५/२/४)
अप् को अमृत और उससे जो मुक्त हुआ वह मृत्यु है। अलग होने को मुच्यु कहा है, मुच्यु से मृत्यु हुआ है-
स समुद्रादमुच्यत स मुच्युरभवत् तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते परोक्षेण। (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, १/७)
५. त्रयी विद्या- तीन विभाजन द्वारा ज्ञान होता है, अतः वेद को भी त्रयी कहते हैं। किसी भी प्रकार ३ का विभाजन करें, कुछ चीजें अविभाज्य रह जाती हैं। अविभाज्य तत्त्व को परात्पर ब्रह्म कहते हैं। यह हमारे किसी विभाजन में नहीं आता है, अतः इसके वर्णन को नेति कहते हैं। जैसे गजेन्द्र मोक्ष में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है-
स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यङ्, न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः।
नायं गुणं कर्म न सन्न चासन्, निषेध-शेषो जयतादशेषः॥
(भागवत पुराण, ८/३/२४)
अविभक्त ब्रह्म रूप अथर्व वेद को मिला कर त्रयी का अर्थ ४ वेद होता है-१ मूल + ३ शाखा। इसका प्रतीक पलास दण्ड है जिसमें शाखा से ३ पत्ते निकलते हैं। इस प्रतीक का प्रयोग वेदारम्भ संस्कार में होता है।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठ- मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह॥१॥
द्वे विद्ये वेदितव्ये- … परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डक उपनिषद्, १/१/१, ४, ५)
यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः।
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति॥ (ऋक्, १०/१३५/१)
सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां योनिर्यत् पलासः। (स्वायम्भुव ब्रह्मरूपत्त्वात्)
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः-ऐतरेय ब्राह्मण, २/१)
वेद के ३ विभाजन इस प्रकार हैं-मूर्ति रूप ऋक्, गति रूप यजु, महिमा रूप साम, तथा अविभाज्य ब्रह्म रूप अथर्व।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
इसी प्रसंग में तैत्तिरीय ब्राह्मण में ५३ प्रकार का त्रयी विभाजन दिया है।
ज्ञान का क्रम भी वही है, मूर्त्ति या सत्ता रहने पर ही उसका ज्ञान होगा। उस वस्तु से प्रकाश, ध्वनि आदि द्वारा सूचना आनी चाहिये। यह गति रूप यजु है। वस्तु का प्रभाव क्षेत्र या साम जहां तक है, वहीं तक उसका ज्ञान हो सकता है। अतः भगवान् ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है (गीता, १०/२२)। वस्तु की पहचान के लिए वह परिवेश से भिन्न होना चाहिये, गति तथा महिमा भी परिवेश के सापेक्ष ही है। वह परिवेश या आधार अथर्व वेद है। इसी अनुसार विद् धातु के ४ अर्थ हैं-
ऋक्-विद् सत्तायाम् (धातुपाठ, ४/६०),
यजु-विद्लृ लाभे (६/१४१)
साम-विद् ज्ञाने (२/५७)
अथर्व-विद् विचारणे (७/१३) या विद् चेतनाख्यान निवासेषु (१०/१७७)।
६. गायत्री त्रिक-सभी छन्द ४ पाद के होते हैं, किन्तु ३ खण्ड में अर्थ होने के कारण गायत्री मन्त्र के ३ पाद हैं।
तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। (मीमांसा सूत्र, २/१/३५)
छन्द-पाद का अर्थ है, वाक्य तथा पद (वाक्यांश)।
मूल विन्दु से सृष्टि का आरम्भ हुआ। ३ गुण या ब्रह्मा-विष्णु-शिव रूप में विभाजन ॐ के ३ अक्षर हैं। मूल विन्दु अर्ध मात्रा रूप में बच जाता है जो चण्डी पाठ (१/७४) में परा प्रकृति का स्वरूप कहा है-
अर्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः।
गायत्री के भी ३ पाद विभाजन के बाद अव्यक्त अविभाज्य पद बच जाता है, जिसे परोरजा (लोकोत्तर) कहते हैं। विभाज्य पदों में भी प्रत्येक के पुनः ३-३ विभाग हैं-
(१) भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ, (२) ऋक्, यजु, साम, (३) प्राण-अपान-व्यान। (बृहदारण्यक उपनिषद्, ५/१४/१-४)
ॐ का विस्तार ३ लोकों में हुआ-भू, भुवः, स्वः। ३ धामों में ३-३ लोक होने से ७ लोक हुए, दो धामों के बीच के लोक समान हैं।
अवम लोक सौर मण्डल में-भू (पृथ्वी), भुवः (नेपचून तक ग्रह कक्षा), स्वः (३३ धाम तक सौर मण्डल)।
मध्यम धाम ब्रह्माण्ड का भू लोक अवम का स्वः लोक है। उसका भुवः महर्लोक तथा स्वः जनः लोक है।
परम धाम का भू लोक ब्रह्माण्ड या जनः लोक है। मध्यम तपः लोक है जहां तक का ताप या प्रकाश हम तक पहुंचता है। उसका स्वःलोक अनन्त सत्य लोक है।
गायत्री का प्रथम पद आकाश का आधिदैविक वर्णन है, मध्यम पाद दृश्य आधिभौतिक जगत् है, उत्तर पाद आध्यात्मिक या शरीर पर प्रभाव है।ये ब्रह्म के ३ वर्णनीय रूपों के विषय में हैं-स्रष्टा रूप ब्रह्मा, तेज या क्रिया रूप विष्णु, तथा ज्ञान रूप शिव।
ॐ भूर्भुवः स्वः/तत् सवितुर्वरेण्यं/भर्गो देवस्य धीमहि/धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी देव रूपों के भी ३ भाग इन ३ पादों से व्यक्त होते हैं-
(१) विष्णु-इक्षा या क्रियात्मक विचार, सूर्य, प्रत्येक व्यक्ति का मन। सृष्टि में हर व्यक्ति का मन या पिण्ड प्रायः स्वतन्त्र हैं, इसी कारण सबका स्वतन्त्र अस्तित्व है। इसका प्रतीक पीपल है जिसके पत्ते मनुष्य के मन जैसे डोलते हैं।
(२) शिव-परमेश्वर जिसके मन में प्रथम विचार उत्पन्न हुआ, तेज के विभिन्न क्षेत्र-रुद्र, शिव (शतरुद्र, सहस्र रुद्र, लक्ष रुद्र), शिवतर, शिवतम, सदाशिव, आदिगुरु रूप शिव। गुरु परम्परा का प्रतीक वट वृक्ष है जिसकी हवाई जड़ जमीन से लग कर वैसा ही वृक्ष बन जाती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य को ज्ञान दे कर अपने जैसा मनुष्य बना देता है।
(३) ब्रह्मा-मूल रस रूप पदार्थ, ५ पर्वों के पिण्ड (स्वयम्भू, ब्रह्माण्ड, तारा, ग्रह, तथा ग्रहों के जीव), ज्ञान संहति के रूप में वेदत्रयी। त्रयी का अर्थ ४ वेद होता है १ मूल (अथर्व) तथा ३ शाखा-ऋक्, यजु, साम (मुण्डकोपनिषद् १/१/१-५)। इसका प्रतीक पलास वृक्ष है, जिसकी शाखा से ३ पत्ते निकलते हैं पर मूल भी बचा रहता है।
(४) हनुमान्-स्रष्टा रूप वृषाकपि है, जो पहले जैसी सृष्टि करता है (सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्-ऋग्वेद १०/१९०/३)। तेज या गति रूप मारुति है। मन को प्रेरित करने वाला रूप मनोजव है (योगसूत्र ३/४९, ऋग्वेद १०/७१/७-८)। इसका प्रतीक मूल वट की शाखाओं से बने वृक्ष हैं जिनको लोकभाषा में दुमदुमा (द्रुम से द्रुम) कहते हैं।
(५) देवी रूप में वैदिक भाषा में भारती, इला, सरस्वती है तथा पौराणिक भाषा में महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती हैं (दुर्गा सप्तशती के ३ चरित्र)।
इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः (ऋक्, १/१३/९, ५/११/८)
भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे (ऋक्, १/१८८/८)
(६) गणेश रूप में प्रथम पाद उच्छिष्ट गणपति (१ पाद से विश्व बनने के बाद बचा मूल स्रोत) है, दृश्य जगत् के पिण्डों का समूह महा गणपति, तथा लोकों का गण या उसका मुख्य गणेश है। पुरुष सूक्त (वाजसनेयि यजु, अध्याय, ३१/३)-
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥३
अथर्व, शौनक, ११/७ उच्छिष्ट सूक्त-
उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः।
उच्छिष्टे इन्द्राग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम्॥१॥
उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्।
आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः॥२॥
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥ (२१-२७)
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे (ऋक्, २/२३/१, वाज. सं. २३/१९, तै. सं. २/३/१४/३, मै. सं. १६६/११, काण्व. सं. ४/१)
गणनात्मक ज्ञान या शब्दों में प्रकट ज्ञान गणेश है-
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं —त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। (गणेश अथर्वशीर्ष, ४)
(७) इसी प्रकार कार्तिकेय (सुब्रह्म) सरस्वती, काली, लक्ष्मी के भी ३ रूप किये जा सकते हैं।
कार्तिकेय (सुब्रह्म)-मूल सरिर् या सलिल रूप, तारा संहति को ब्रह्माण्ड रूप में देखना, कणों का समूह पिण्ड रूप में देखना।
वातस्य जूतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये। (वा॰ यजुर्वेद, १३/४२)
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य उप प्र याहि दिव्यानि धाम ।(वा॰ यजुर्वेद, १५/५२)
ब्रह्म से सुब्रह्म-
ॐ ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत् स्वयं त्वेकमेव तदैक्षत महद्वै यक्षं तदेकमेवास्मि हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति तदभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत् तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य ललाटे स्नेहो यदार्द्र्यमाजायत तेनानन्दत् तमब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदामह इति । तद्यदब्रवीत् महद्वै यक्षं सुवेदमविदामह इति तस्मात् सुवेदोऽभवत्तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते॥ (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व १/१/१)
(८) सरस्वती-रस समुद्र का अनन्त विस्तार, ब्रह्माण्ड का सरस्वान् समुद्र, मस्तिष्क के भीतर समुद्र (मानसरोवर)।
यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति। (तैत्तिरीय उपनिषद् २/७)
मनो वै सरस्वान् (शतपथ ब्राह्मण, ७/५/१/३१, ११/२/४/९)
स्वर्गो लोकः सरस्वान् (ताण्ड्य महाब्राह्मण, १६/५/१५)
वाक् सरस्वती (शतपथ ब्राह्मण, ७/५/१/३१, ११/२/४/९, १२/९/१/१३)
(९) काली-मूल अव्यक्त अज्ञात विश्व, व्यक्त विश्व में नित्य काल से परिवर्तन रूप जिसके बाद मूल रूप कभी वापस नहीं आता, काल का अनुभव या ज्ञान।
सप्त चक्रान् वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः।
सा इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत् कालः स ईषते प्रथमो नु देवः॥
(अथर्व, शौनक शाखा, १९/५३/२)
(१०) लक्ष्मी-अव्यक्त से दृश्य जगत् की उत्पत्ति, आकाश में अलग अलग रूप या आकार के पिण्ड, निकट की दृश्य वतुओं का ज्ञान, दृश्य वाक् या लिपि।
ततो विराडजायत, विराजो अधिपूरुषः।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः॥
(विराट् = दृश्य जगत्) (पुरुष सूक्त, ५)
यद्वै नास्ति तदलक्षणम् (शतपथ ब्राह्मण, ७/२/१/७)
तस्माद्यस्य सर्वतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते। (शतपथ ब्राह्मण, ८/५/४/३)
देवलक्ष्मं वै त्र्यालिखितं तामुत्तर लक्ष्माण देवा उपादधत (तैत्तिरीय सं. ५/२/८/३)
उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् (ऋक्, १०/७१/४)
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.