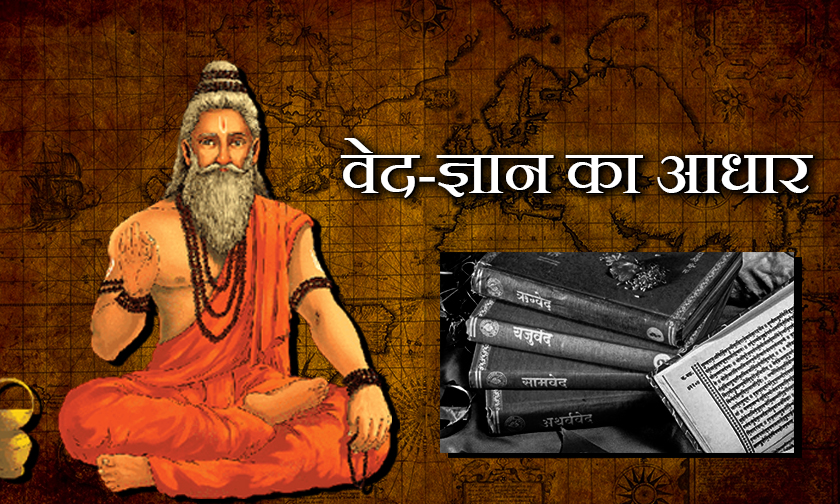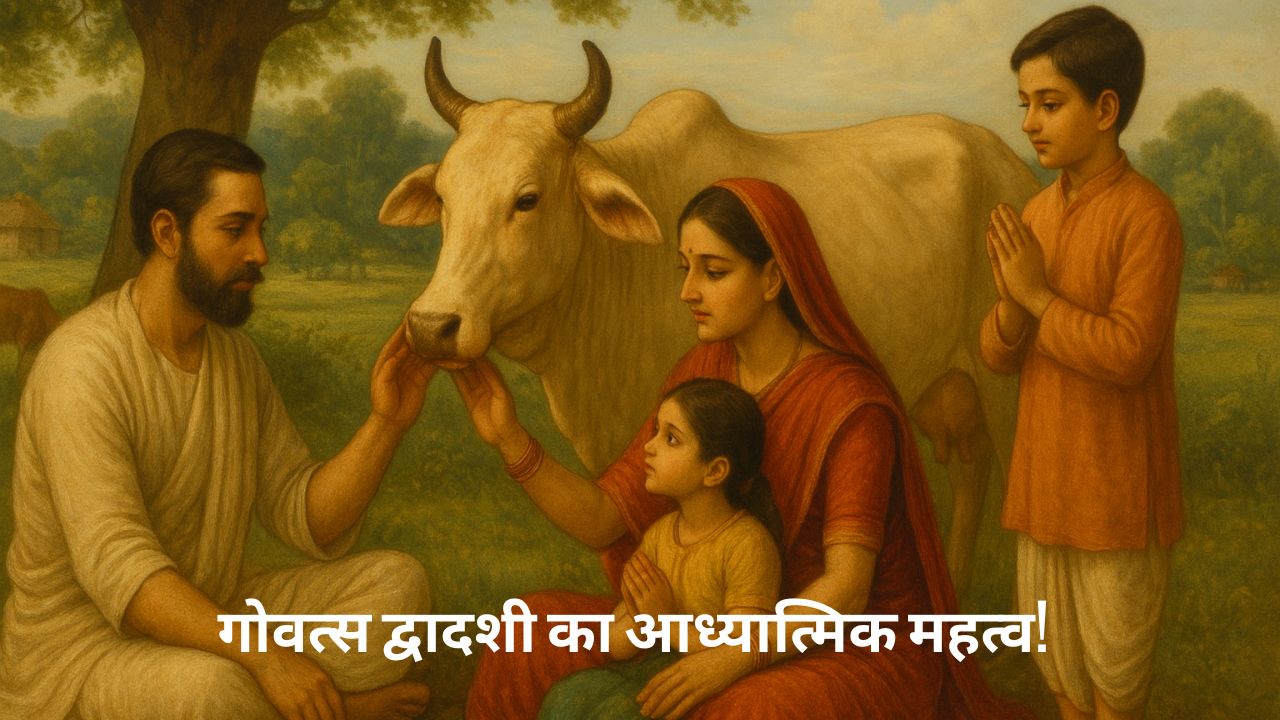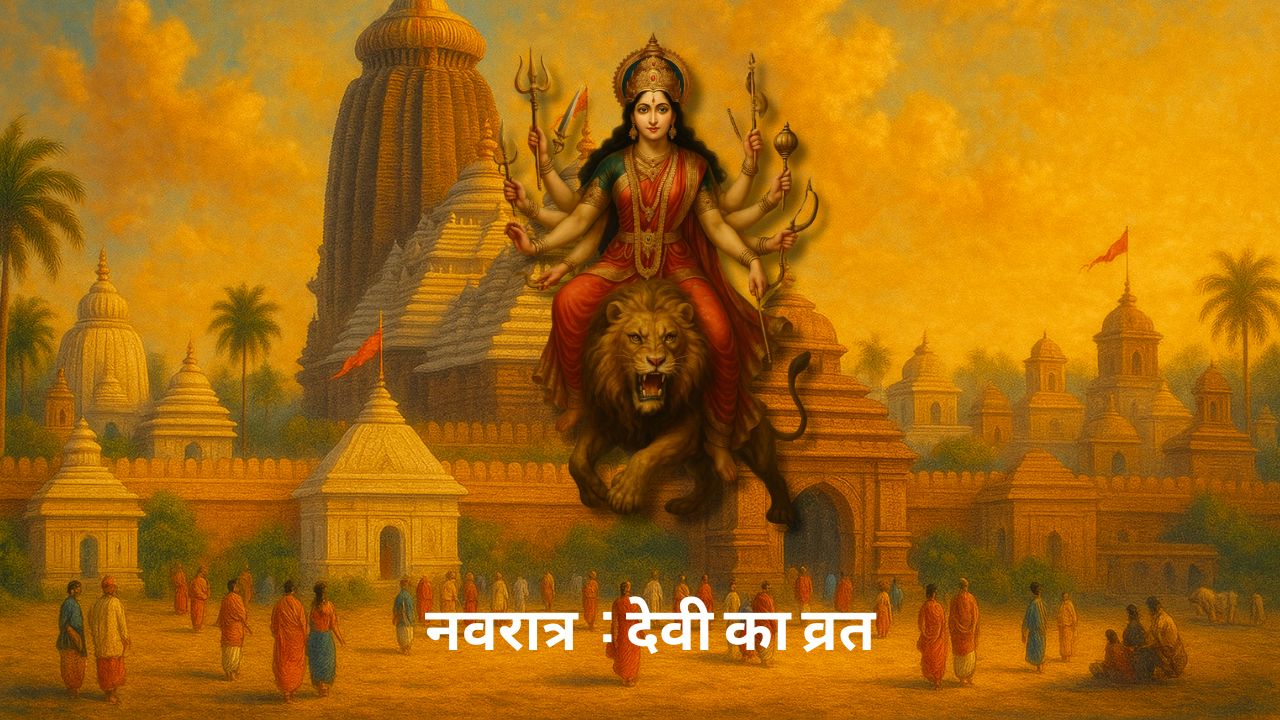- धर्म-पथ
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments
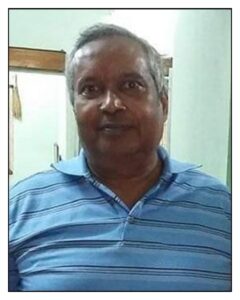 श्री अरुण कुमार उपाध्याय धर्मज्ञ
Mystic Power - १. विश्व स्रोत-
यह मनु स्मृति का कथन है। न केवल ज्ञान, बल्कि विश्व, ३ लोक ४ वर्ण और आश्रम, भूत और भविष्य का विश्व, धर्म-इन सबका स्रोत वेद को कहा है।
(१) धर्म स्रोत-
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ (मनु स्मृति, १/६)
धर्म के मूल ये हैं-अखिल वेद, उन पर आधारित स्मृति (मनु स्मृति, २/१३-१४ के अनुसार वेद आधारित स्मृति ही मान्य है), स्मृति के ज्ञाता, महापुरुषों के आचार (यत् यत् आचरति श्रेष्ठः, तत् तत् एव इतरो जनाः -गीता, ३/२१), और आत्म-तुष्टि।
श्री अरुण कुमार उपाध्याय धर्मज्ञ
Mystic Power - १. विश्व स्रोत-
यह मनु स्मृति का कथन है। न केवल ज्ञान, बल्कि विश्व, ३ लोक ४ वर्ण और आश्रम, भूत और भविष्य का विश्व, धर्म-इन सबका स्रोत वेद को कहा है।
(१) धर्म स्रोत-
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ (मनु स्मृति, १/६)
धर्म के मूल ये हैं-अखिल वेद, उन पर आधारित स्मृति (मनु स्मृति, २/१३-१४ के अनुसार वेद आधारित स्मृति ही मान्य है), स्मृति के ज्ञाता, महापुरुषों के आचार (यत् यत् आचरति श्रेष्ठः, तत् तत् एव इतरो जनाः -गीता, ३/२१), और आत्म-तुष्टि।
 (२) धर्म तथा ज्ञान-
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ (मनु स्मृति, १/७)
मनु (स्वायम्भुव) ने जिस किसी का जैसा धर्म कहा है, वह सभी वेदों में कहा गया है। मनु (अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित वेद) सभी ज्ञान का स्वरूप है। (२८ व्यासों में स्वायम्भुव मनु प्रथम थे, जिन्होंने मनुष्य ब्रह्मा रूप में वेदों को प्रकट किया-विष्णु पुराण, ३/३/११ आदि)।
(२) धर्म तथा ज्ञान-
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ (मनु स्मृति, १/७)
मनु (स्वायम्भुव) ने जिस किसी का जैसा धर्म कहा है, वह सभी वेदों में कहा गया है। मनु (अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित वेद) सभी ज्ञान का स्वरूप है। (२८ व्यासों में स्वायम्भुव मनु प्रथम थे, जिन्होंने मनुष्य ब्रह्मा रूप में वेदों को प्रकट किया-विष्णु पुराण, ३/३/११ आदि)।
 (३) तीन कालों का विश्व, ३ लोक, ३ वर्ण और आश्रम-
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति॥ (मनु स्मृति, १२/९७)
चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र), ३ लोक (भू, भुवः, स्वः-ये अभी ३ धामों में हैं-परम या पूर विश्व, मध्यम = ब्रह्माण्ड, अवम = सौर मण्डल), ४ आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास), भूत, भविष्य,
वर्तमान काल- ये सभी वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं।
यह वेद के पुरुष सूक्त में भी कहा है। यहां पुरुष का अर्थ चेतन विश्व तथा उसके सभी स्तर हैं। जो पुरुष द्वारा हुआ, वही वेद द्वारा हुआ। अतः जगत् ही वेद पुरुष है।
पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम॥२॥
तस्माद् विराट् अजायत, विराजो अधिपूरुषः।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिं अथो पुरः॥५॥
(भूमि तथा अन्य पुर या लोक, विराट् = दृश्य पिण्ड, अधिपूरुष = दृश्य ग्रह, नक्षत्रों के बीच के स्थान में विरल पदार्थ)
(४) पञ्च तन्मात्रा-
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः।
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूति गुणकर्मतः॥ (मनु स्मृति, १२/९८)
वेद में सृष्टि के ५ पर्व (स्तर) ५ महाभूत रूप हैं-स्वायम्भुव = पूर्ण आकाश, प्रायः खाली या आकाश, ब्रह्माण्ड = गति, वायु, सौर मण्डल = तेज, चान्द्र मण्डल - शान्त, जल, पृथ्वी = ठोस या भूमि तत्त्व। इनकी ५ तन्मात्रा हैं- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-ये सभी तथा प्रसूति या सृष्टि करने वाले गुण (सत्त्व, रज, तम)-ये सभी वेद से ही उत्पन्न हैं।
(५) भूतों का धारण-
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्।
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्॥ (मनु स्मृति, १२/९९)
वेद शास्त्र सनातन है। सृष्टि तथा उसका ज्ञान रूप वेद सदा था, तथा रहेगा। कुछ भाग नष्ट होता रहता है, तो उस स्थान पर नये निर्माण भी होते है। ज्ञान रूप वेद भी सनातन है, पर यह हर कल्प में ब्रह्मा द्वारा प्रकट होता है।
नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रविद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो। मा मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रविदः प्राहु (दु) र्दैवी वाचमुद्यासम्॥ (वरदापूर्वतापिनी उपनिषद्, तैत्तिरीय आरण्यक, ४/१/१, मैत्रायणी संहिता, ४/९/२)
यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिण अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण।
तां दैवी वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, २/८/८/१४)
प्रति मन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते। ऋचो यजूंषि सामानि यथावत् प्रतिदैवतम्॥५८॥
विधिहोत्रं तथा स्तोत्रं पूर्ववत् सम्प्रवर्तते। द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च॥५९॥
तथैवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम्। मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथाभेदा भवन्ति हि॥६०॥
प्रवर्तयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तोत्रं पुनः पुनः। एवं मन्त्रगुणानां तु समुत्पत्तिश्चतुर्विधम्॥६१॥
(मत्स्य पुराण, अध्याय १४५)
२. ज्ञान स्रोत-
वेद किसी ज्ञान-विज्ञान शाखा की पाठ्य पुस्तक नहीं है। यह उनका आधार या सर्व-विद्या प्रतिष्ठा है।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह।
(मुण्डकोपनिषद्,१/१/१)
जिन अर्थों में वेद विद्या की प्रतिष्ठा है, उन अर्थों में इसे अपौरुषेय कहा जाता है।
(१) ३ विश्वों का मिलन-आकाश में पृथ्वी की सृष्टि हुई, पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि। अतः ये ३ विश्व परस्पर की प्रतिमा हैं-
(क) आधिदैविक = आकाश की सृष्टि (इसका एक भेद अधिज्योतिष है),
(ख) आधिभौतिक = पृथ्वी पर का विश्व-इसकी ५ संस्थायें हैं-भौगोलिक, ऐतिहासिक, समाज संस्था, राष्ट्र संस्था, विज्ञान संस्था।
(ग) आध्यात्मिक = मनुष्य शरीर के भीतर का विश्व। आयुर्वेद, योग, तन्त्र द्वारा व्याख्या।
यह तर्क संगत है। किन्तु यदि ये परस्पर को अधिक प्रभावित करने लगें, तो कोई सृष्टि स्थायी नहीं रह सकेगी। अतः इनका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि सबकी क्रिया चलती रहती है। पृथ्वी पर एक मनुष्य की भावना दूसरे को प्रभावित करती है, पर उससे किसी की श्वास या नाड़ी गति बन्द नहीं होती। पृथ्वी पर सौर मण्डल के सभी ग्रहों के आकर्षण का प्रभाव होता है। पर उससे बहुत कम तात्कालिक विचलन होता है (ग्रह वक्री होने के समय), पृथ्वी की कक्षा अरबों वर्षों से वैसी ही है। इसी तरह सौर मण्डल के अन्य तारा इतनी दूर हैं कि उनके कारण सौर मण्डल के ग्रहों की कक्षा प्रभावित नही हुई है।
प्रतिमा के वैदिक उदाहरण-(क) आकाश में ब्रह्माण्ड संख्या = हमारे ब्रह्माण्ड में तारा संख्या = मनुष्य मस्तिष्क में कलल (सेल, न्यूरोन) संख्या = १०० अरब (शतपथ ब्राह्मण, १२/३/२/५, १०/४/४/२)। यह हर स्तर की कण संख्या है जो चूर्ण रूप में होता है, अतः १०० अरब को खर्व (चूर्ण करना) कहते हैं।
(ख) आकाश के २ अव्यक्त पर्व तथा ५ व्यक्त पर्वों के अनुसार मनुष्य मस्तिष्क और मेरुदण्ड में ७ चक्र हैं जो मनुष्य के ७ प्रकार के कोषों के केन्द्र हैं।
आकाश के पर्व चिह्न तत्त्व शरीर के चक्र चिह्न-
१. अव्यक्त अनन्त एक ॐ अव्यक्त सहस्रार एक ॐ
२. हिरण्यगर्भ विभक्त ॐ पदार्थ-ऊर्जा आज्ञा विभक्त ॐ
३. स्वयम्भू मण्डल अ आकाश विशुद्धि ह
४. ब्रह्माण्ड इ वायु अनाहत य
५. सौरमण्डल उ तेज स्वाधिष्ठान व
६. चान्द्र मण्डल ऋ अप् मणिपूर र
७. भूमण्डल लृ भूमि मूलाधार ल
इनकी प्रतिमा रूप पृथ्वी के उत्तर गोल के भारत पाद में ७ लोक है। उत्तर गोल के अन्य ३ पाद तथा दक्षिण गोल के ४ पाद - ये ७ तल हैं।
(ग) आधुनिक विज्ञान में प्रतिमा रूप-इन सिद्धान्तों को गोत्र सिद्धान्त (Anthropic Principle) कहते हैं। मनुष्य की आंख प्रकाश का वही भाग देखती है, जो पृथ्वी के वातावरण में सबसे कम अवशोषित होता है। मनुष्य शरीर के जल भाग (रक्त, प्लाज्मा) में लवणों का अनुपात वही है, जो समुद्र जल में है।
अपौरुषेयता-वेद इन ३ अर्थों में ही अपौरुषेय है-(क) ५ ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त ऋषि और परोरजा प्राण से अतीन्द्रिय ज्ञान। (ख) तीन विश्वों का समन्वय-जो अपने साथ महः (बाह्य विश्व) का सम्बन्ध देख सकता है, उसे महर्षि कहा गया है (वायु पुराण, ५९/८१-८२)। (ग) कई ऋषियों के मन्त्रों का संकलन करने से व्यक्तिगत आग्रह या कमी दूर हो जाती है।
३. तत्त्व वेद की अपौरुषेयता-
तत्त्व रूप में पूरा विश्व तथा उसके सभी स्तर ही पुरुष है जिसकी व्याख्या फुरुष सूक्त में की गयी है। जिस वेद से भूत, भविष्य, वर्तमान के विश्व और ३ लोकों की उत्पत्ति कही गयी है, वह तत्त्व वेद है। इस वेद से पुरुष की उत्पत्ति हुई अतः तत्त्व वेद भी अपौरुषेय है।
व्यक्त विश्व में प्रथम मण्डल के ३ मनोता (संकल्प का क्रिया रूप) थे-वेद, सूत्र, नियति।
इसका वेद तत्त्व है कि प्रत्येक विन्दु अन्य विन्दुओं से प्रभावित हो कर उनके बारे में जानता है। यह मूर्ति गति, महिमा-३ प्रकार का है जिनको ऋक्-यजु-साम कहा है।
सूत्र द्वारा २ या अधिक पिण्ड परस्पर सम्बन्धित होते हैं। इसके ३ प्रकार हैं-सत्य (सीमाबद्ध), ऋत (सीमाहीन), ऋत-सत्य (सीमा हीन किन्तु केन्द्र विन्दु)।
नियति सृष्टि या परिवर्तन की दिशा है। सांख्य में इसे सञ्चर-प्रतिसञ्चर कहा है, ईशावास्योपनिषद् में सम्भूति-असम्भूति (विनाश) कहा है। यथास्थिति या सन्तुलन इनकी बराबर स्थिति है।
पुरुष के ४ भागों में १ ही भाग व्यक्त विश्व है। ३ अव्यक्त भाग सदा रहते हैं (त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त, ३)। इस अव्यक्त भाग का वेद शून्य या अज्ञात है। व्यक्त भाग का अनन्त वेद है (भरद्वाज को इन्द्र द्वारा कथन-तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१०/११)-अनन्ताः वै वेदाः। यहां कई प्रकार के अनन्त हैं, ऋक का मूर्ति रूप संख्येय अनन्त है, यजुः का गति रूप असंख्येय अनन्त है, साम की महिमा अप्रमेय अनन्त है। अथर्व अज्ञेय अनन्त है। इस रूप में सृष्टि रूप पुरुष या अव्यक्त रूप पूरुष के लिए भी वेद अपौरुषेय हैं। विष्णु सहस्रनाम में ये शब्द हैं-अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय, अमेयात्मा।
वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुमः (भागवत पुराण, ६/१/४०)
आद्यं त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयो यस्मिन्प्रतिष्ठिता ।
स गुह्योऽन्यस्त्रिविद्वेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥ (मनु स्मृति, १२/२६५)
ब्रह्माण्ड में वेद का स्वरूप भृगु रूप आकर्षण तथा अङ्गिरा रूप विकिरण है।
आपो भृग्वङ्गिरो रूपमापो भृग्वङ्गिरोमयं सर्वमापोमयं भूतं सर्वं भृग्वङ्गिरोमयमन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसोऽनुगाः (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, १/३९)
इसमें अङ्गिरा के ३ स्तर हैं-केन्द्र में अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद प्रभाव सीमा तक आदित्य। ये ऋक्, यजु, साम वेद हैं।
तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यस्त्रीन् देवान्निरमिमीत--अग्निं वायुमादित्यमिति---स खलु पृथिव्या एवाग्निं निरमिमीतान्तरिक्षाद्वायुं दिव आदित्यम्--अग्नेर्ऋग्वेदं वायोर्यजुर्वेदं आदित्यात्सामवेदम् (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, १/६)
भृगु (आकर्षण जनित पिण्डों की स्थिति) से अथर्व हुआ।
ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यो यद्रेत आसीत्तदभृज्ज्यत, तस्माद्भृगुः समभवत्--भृगुरिव वै स सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद। (गोपथ पूर्व, १/३)
अथर्वाणश्च ह वा अङ्गिरसश्च भृगुचक्षुषी तद्ब्रह्माभिव्यपश्यन् (गोपथ पूर्व, १/२२)
सौर मण्डल के भीतर भी भृगु-अङ्गिरा के कारण वेद हैं। सम्पूर्ण सौर मण्डल की स्थिति भृगु या अथर्व वेद (सनातन ब्रह्म) है। अग्नि (११ अहर्गण-पृथ्वी तक), वायु (२२ अहर्गण-यूरेनस तक), रवि या आदित्य (सौर मण्डल की सीमा-३३ अहर्गण तक) क्रमशः ऋक्, यजु, साम वेद हैं।
अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम्॥ (मनु स्मृति, १/२३)
यही यज्ञ के लिए वसु, रुद्र, आदित्य क्षेत्र हैं, जो यज्ञ या उत्पादन रूपी गौ से सम्बन्धित हैं-
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्यानां अमृतस्य नाभिः।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥ (ऋक्, ८/१०१/१५)
केवल सूर्य पिण्ड देखने से इसका पिण्ड (मूर्त्ति) ऋक् है, इसका शरीर यजु है (भीतरी क्रिया कृष्ण, बाहरी कम्पन अङ्गार् शुक्ल यजु), तथा इसके तेज, आकर्षण, वायु का प्रसार (त्रिसामा) सामवेद है।
यदेतन्मण्डलं तपति। तन्महदुक्थं ताऽऋचः सऽऋचां लोकोऽथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ यऽएष ऽएतस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजूंषि स यजुषां लोकः॥ (शतपथ ब्राह्मण, १०/५/२/१)
चान्द्र मण्डल के मनोता हैं-रेत (सोम कण), श्रद्धा (कणों के बीच सम्बन्ध), यश (महिमा)। यही ३ वेदों के रूप हैं।
पृथ्वी से देखने पर वाक्, गौ, द्यौ-३ मनोता हैं, जो ३ वेदों के स्वरूप हैं। वाक् ३ प्रकार की पृथ्वी की माप है-२४ अहर्गण (गायत्री) पृथ्वी ग्रह है, त्रिष्टुप् (४४ अहर्गण) सूर्य का क्षेत्र महर्लोक तक, जगती (४८ अहर्गण) ब्रह्माण्ड।
जब तक स्वयम्भू, ब्रह्माण्ड, सौर मण्डल, चान्द्र मण्डल तथा पृथ्वी है, तब तक ये तत्त्व वेद सनातन हैं। ये सभी अपने पुर के पुरुषों से परे हैं।
४. ज्ञान प्राप्ति का क्रम-
निसर्ग से प्राप्त ज्ञान विद्या है, अतः इसे निगम (वेद) कहते हैं। वेद के कई अर्थ हैं-तत्त्व वेद को वेद पुरुष कहते हैं। विश्व का शब्द रूप में वर्णन श्री वेद है-
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्।
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ (मैत्रायणी उपनिषद्, ६/२२)
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
ब्रह्म या पुरुष वेद का ३ प्रकार विभाजन है-मूर्ति तत्त्व ऋक् है, गति यजुर्वेद है (शुक्ल-कृष्ण गति के अनुसार २ प्रकार का), महिमा या प्रभाव साम वेद है तथा स्थिर सनातन आधार ब्रह्म या अथर्व वेद है, (थर्व = थरथराना, अथर्व = स्थिर) शब्द रूप वेद श्री का रूप है-
शब्दात्मिकां सुविमलर्ग्यजुषां निधानमुद्गीथ रम्य पद-पाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमार्ति हन्त्री॥ (दुर्गा सप्तशती, ४/१०)
वेद में पुरुष रूप का वर्णन पुरुष सूक्त तथा श्री रूप का वर्णन श्री सूक्त, रात्रि सूक्त आदि में है।
४ प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के कारण विद् धातु के ४ अर्थ तथा ४ वेद हैं। पहले किसी वस्तु की सत्ता होनी चाहिए, अर्थात् मूर्त्त रूप जिसका वर्णन ऋग्वेद करता है। उस मूर्त्ति से कोई ध्वनि, प्रकाश, गन्ध आदि प्रभाव आना चाहिए। यह गति रूप यजुर्वेद है। उसकी प्रभाव सीमा या महिमा के भीतर ही उसका ज्ञान हो सकता है। महिमा सामवेद है। महिमा क्षेत्र में ही ज्ञान हो सकता है, अतः भगवान् ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
वेदानां सामवेदोऽस्मि (गीता, १०/२२)
तत्त्व वेद विद धातु का अर्थ
मूर्ति ऋक् सत्ता (विद् सत्तायाम्, धातुपाठ, ४/६०)
गति यजु लाभ, प्राप्ति-विद्लृ लाभे (६/१४१)
ज्ञान साम विद् ज्ञाने (२/५७)
आधार अथर्व विद् विचारणे (७/१३), चेतनाख्यान निवासेषु (१०/१७७)
प्रकृति या निसर्ग के जिस क्षेत्र की महिमा हम तक पहुंचती है वह महः है। उससे प्राप्त विद्या वेद है। उस ज्ञान का प्रयोग महः पर किया जाय तो वह महाविद्या है।
निसर्ग से प्राप्त ज्ञान ३ प्रकार का है। यह जैन दर्शन के शब्द हैं।
श्रुति ज्ञान-जितना हम निकट क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं। यह वेद हुआ, अतः इसे श्रुति कहते हैं।
अवधि ज्ञान-प्रकृति में परिवर्तन या गति जानने के लिए कुछ समय बाद पुनः देखना पड़ता है कि कितना अन्तर हुआ। पुरा का नवीन रूप देखने की पद्धति पुराण (पुरा + नवति) है।
केवल ज्ञान-ज्ञान पूरे विश्व में फैला है। उसका कुछ ही भाग ज्ञेय है। ज्ञेय भाग भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं। उस वस्तु की पूरी सूचना नहीं आती है, उसका कुछ ज्ञान कुछ अनुमान मिल कर परिज्ञान है।
अतः ज्ञान प्राप्ति का कर्म ३ प्रकार का है-
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना। (गीता, १८/१८)
५. अपरा विद्या-
विश्व या उसका चेतन रूप ब्रह्म अज्ञात है। विभिन्न दर्शनों या शास्त्रों में कई प्रकार के विभाजन द्वारा ही वह समझा जा सकता है।
नवैकादश पञ्च त्रीन् भावान् भूतेषु येन वै। ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्॥१४॥
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्। स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मकम्॥१५॥
(भागवत पुराण, ११/१९/१४-१५)
जगत् के अनन्त पदार्थों का ९, ११, ५, ३ में वर्गीकरण करना और अन्त में १ ही मूल तत्त्व देखना ज्ञान है। वर्गीकरण की पद्धति विज्ञान है। इसी को मुण्डक उपनिषद् (१/१/२) में परा-अपरा विद्या कहा है। परा विद्या को केवल विद्या तथा अपरा विद्या को अविद्या कहते हैं। यह विद्या का अभाव नहीं, उसका वर्गीकरण है। बिना सम्बन्ध समझे उनको भिन्न देखना भी विद्या का अभाव ही है।
वर्गीकरण के उदाहरण-न्याय वैशेषिक के ९ द्रव्य, ९ सर्ग, ९ दुर्गा, ५ महाभूत, विश्व के ५ पर्व, पञ्चाग्नि, ३ गुण, ३ लोक, ३ धाम, ॐ के ३ अक्षर, ११ रुद्र, मन सहित ११ इन्द्रियां, या सांख्य में प्रकृति-पुरुष के २५ तत्त्वों के अतिरिक्त शिव-शक्ति की ११ प्रत्यभिज्ञा।
अज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए उसे ३ भाग में समझते हैं-
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
= उस (ब्रह्म) का कार्य, करण आदि का पता नहीं चलता है, वैसा या अधिक कोई नहीं दीखता। हमारी कल्पना से परे है, अतः उसे ज्ञान-बल-क्रिया रूप में देखते हैं।
अतः विद्या के २ रूप कहे गये हैं-परा विद्या (विद्या) = एकीकरण, अपरा विद्या (अविद्या) = वर्गीकरण।
द्वे विद्ये वेदितव्ये- ... परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।
(मुण्डक उपनिषद्, १/१/३-५)
इनको ज्ञान-विज्ञान भी कहा है-ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः (गीता, ७/२)।
विज्ञान का वही अर्थ है जो आधुनिक साइंस में है-मोक्षे धीः ज्ञानं अन्यत्र विज्ञानं शिल्प शास्त्रयोः (अमरकोष, १/५/९)। यहां विज्ञान में उसका प्रयोग या इंजीनियरिंग भी है।
आधुनिक विज्ञान में केवल एक परिभाषा है-वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसकी पद्धति है-विभिन्न घटनाओं में साम्य देख कर नियम बनाना। परीक्षण या प्रयोग द्वारा नियम में त्रुटि देखकर उसमें संशोधन करना।
योग सूत्र (२/३) में विद्या के अभाव को अविद्या कहा है तथा उसके ५ पर्व कहे हैं। इनका अपरा विद्या अर्थ में आधुनिक परिभाषा से अधिक व्यापक अर्थ है-
(१) अविद्या = विषयों या तथ्यों का विभाजन।
(२) अस्मिता = प्रति तत्त्व या वर्ग की अलग अलग परिभाषा और व्याख्या।
(३) राग = अलग अलग तथ्यों में समानता खोज कर एक वर्ग में करना (Generalization)।
(४) द्वेष = अन्य वर्ग के तथ्यों से भेद दिखाना।
(५) अभिनिवेश = सिद्धान्त स्थिर करना, जिसके अनुसार नये तथ्यों को प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है।
वैदिक साहित्य इसी क्रम में है-
(१) संहिता = ऋषियों के मन्त्रों का संकलन।
(२) ब्राह्मण = सूतों की विषय अनुसार व्याख्या-वर्गी करण।
(३) आरण्यक = प्रयोग।
(४) उपनिषद् = स्थिर सिद्धान्त, निष्कर्ष।
वेदस्योपनिषत् सत्यम्, सत्यस्योपनिषद् दमः आदि (महाभारत, शान्ति पर्व, २५१/११-१२)
तस्माद् वा अप उपस्पृशति-इति उपनिषत् (शतपथ ब्राह्मण, १/१/१/१)
६. वर्णाश्रम और धर्म का स्रोत-
आधुनिक शिक्षा में इसकी कमी है। कई पन्थ बहुत इश्वरों को मान कर केवल अपने ईश्वर को सही मानते हैं तथा अन्य की हत्या करते है। उनके अनुसार उस पुस्तक का पालन ही धर्म है। वेद में धर्म का एक अर्थ प्राकृतिक गुण है (वैशेषिक दर्शन)। सामान्यतः धर्म का अर्थ है कि इससे प्रजा (व्यक्ति, समाज) का धारण होता है-
धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ (महाभारत, शान्ति पर्व, १०९/१२)
संहिता भाग में केवल ऋषियों द्वारा मन्त्र का दर्शन है। उसमें कर्तव्य नही लिखा है, जिसे विधि (कर्तव्य), निषेध (वर्जित) कहते हैं। इसके लिये वेद आधारित स्मृति ग्रन्थ है (मनुस्मृति, २/१२)। ब्राह्मण भाग में वेद व्याख्या है जिनके अनुसार कल्प सूत्र में विधि-निषेध का वर्णन है। ६ वेदाङ्गों में कल्प भी है।
इन ग्रन्थों में ४ वर्ण तथा ४ आश्रमों के कर्तव्य का वर्णन है। इस अर्थ में वेद से ही धर्म और वर्णाश्रम की उत्पत्ति हुई है। यह समझने के लिए वेद में संहिता के साथ तीनों ब्राह्मण भाग (ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्), ६ अंग तथा स्मृति को भी वेद मानना होगा।
(३) तीन कालों का विश्व, ३ लोक, ३ वर्ण और आश्रम-
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति॥ (मनु स्मृति, १२/९७)
चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र), ३ लोक (भू, भुवः, स्वः-ये अभी ३ धामों में हैं-परम या पूर विश्व, मध्यम = ब्रह्माण्ड, अवम = सौर मण्डल), ४ आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास), भूत, भविष्य,
वर्तमान काल- ये सभी वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं।
यह वेद के पुरुष सूक्त में भी कहा है। यहां पुरुष का अर्थ चेतन विश्व तथा उसके सभी स्तर हैं। जो पुरुष द्वारा हुआ, वही वेद द्वारा हुआ। अतः जगत् ही वेद पुरुष है।
पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम॥२॥
तस्माद् विराट् अजायत, विराजो अधिपूरुषः।
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिं अथो पुरः॥५॥
(भूमि तथा अन्य पुर या लोक, विराट् = दृश्य पिण्ड, अधिपूरुष = दृश्य ग्रह, नक्षत्रों के बीच के स्थान में विरल पदार्थ)
(४) पञ्च तन्मात्रा-
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः।
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूति गुणकर्मतः॥ (मनु स्मृति, १२/९८)
वेद में सृष्टि के ५ पर्व (स्तर) ५ महाभूत रूप हैं-स्वायम्भुव = पूर्ण आकाश, प्रायः खाली या आकाश, ब्रह्माण्ड = गति, वायु, सौर मण्डल = तेज, चान्द्र मण्डल - शान्त, जल, पृथ्वी = ठोस या भूमि तत्त्व। इनकी ५ तन्मात्रा हैं- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-ये सभी तथा प्रसूति या सृष्टि करने वाले गुण (सत्त्व, रज, तम)-ये सभी वेद से ही उत्पन्न हैं।
(५) भूतों का धारण-
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्।
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्॥ (मनु स्मृति, १२/९९)
वेद शास्त्र सनातन है। सृष्टि तथा उसका ज्ञान रूप वेद सदा था, तथा रहेगा। कुछ भाग नष्ट होता रहता है, तो उस स्थान पर नये निर्माण भी होते है। ज्ञान रूप वेद भी सनातन है, पर यह हर कल्प में ब्रह्मा द्वारा प्रकट होता है।
नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रविद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो। मा मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रविदः प्राहु (दु) र्दैवी वाचमुद्यासम्॥ (वरदापूर्वतापिनी उपनिषद्, तैत्तिरीय आरण्यक, ४/१/१, मैत्रायणी संहिता, ४/९/२)
यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिण अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण।
तां दैवी वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, २/८/८/१४)
प्रति मन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते। ऋचो यजूंषि सामानि यथावत् प्रतिदैवतम्॥५८॥
विधिहोत्रं तथा स्तोत्रं पूर्ववत् सम्प्रवर्तते। द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तथैव च॥५९॥
तथैवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम्। मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथाभेदा भवन्ति हि॥६०॥
प्रवर्तयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तोत्रं पुनः पुनः। एवं मन्त्रगुणानां तु समुत्पत्तिश्चतुर्विधम्॥६१॥
(मत्स्य पुराण, अध्याय १४५)
२. ज्ञान स्रोत-
वेद किसी ज्ञान-विज्ञान शाखा की पाठ्य पुस्तक नहीं है। यह उनका आधार या सर्व-विद्या प्रतिष्ठा है।
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह।
(मुण्डकोपनिषद्,१/१/१)
जिन अर्थों में वेद विद्या की प्रतिष्ठा है, उन अर्थों में इसे अपौरुषेय कहा जाता है।
(१) ३ विश्वों का मिलन-आकाश में पृथ्वी की सृष्टि हुई, पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि। अतः ये ३ विश्व परस्पर की प्रतिमा हैं-
(क) आधिदैविक = आकाश की सृष्टि (इसका एक भेद अधिज्योतिष है),
(ख) आधिभौतिक = पृथ्वी पर का विश्व-इसकी ५ संस्थायें हैं-भौगोलिक, ऐतिहासिक, समाज संस्था, राष्ट्र संस्था, विज्ञान संस्था।
(ग) आध्यात्मिक = मनुष्य शरीर के भीतर का विश्व। आयुर्वेद, योग, तन्त्र द्वारा व्याख्या।
यह तर्क संगत है। किन्तु यदि ये परस्पर को अधिक प्रभावित करने लगें, तो कोई सृष्टि स्थायी नहीं रह सकेगी। अतः इनका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि सबकी क्रिया चलती रहती है। पृथ्वी पर एक मनुष्य की भावना दूसरे को प्रभावित करती है, पर उससे किसी की श्वास या नाड़ी गति बन्द नहीं होती। पृथ्वी पर सौर मण्डल के सभी ग्रहों के आकर्षण का प्रभाव होता है। पर उससे बहुत कम तात्कालिक विचलन होता है (ग्रह वक्री होने के समय), पृथ्वी की कक्षा अरबों वर्षों से वैसी ही है। इसी तरह सौर मण्डल के अन्य तारा इतनी दूर हैं कि उनके कारण सौर मण्डल के ग्रहों की कक्षा प्रभावित नही हुई है।
प्रतिमा के वैदिक उदाहरण-(क) आकाश में ब्रह्माण्ड संख्या = हमारे ब्रह्माण्ड में तारा संख्या = मनुष्य मस्तिष्क में कलल (सेल, न्यूरोन) संख्या = १०० अरब (शतपथ ब्राह्मण, १२/३/२/५, १०/४/४/२)। यह हर स्तर की कण संख्या है जो चूर्ण रूप में होता है, अतः १०० अरब को खर्व (चूर्ण करना) कहते हैं।
(ख) आकाश के २ अव्यक्त पर्व तथा ५ व्यक्त पर्वों के अनुसार मनुष्य मस्तिष्क और मेरुदण्ड में ७ चक्र हैं जो मनुष्य के ७ प्रकार के कोषों के केन्द्र हैं।
आकाश के पर्व चिह्न तत्त्व शरीर के चक्र चिह्न-
१. अव्यक्त अनन्त एक ॐ अव्यक्त सहस्रार एक ॐ
२. हिरण्यगर्भ विभक्त ॐ पदार्थ-ऊर्जा आज्ञा विभक्त ॐ
३. स्वयम्भू मण्डल अ आकाश विशुद्धि ह
४. ब्रह्माण्ड इ वायु अनाहत य
५. सौरमण्डल उ तेज स्वाधिष्ठान व
६. चान्द्र मण्डल ऋ अप् मणिपूर र
७. भूमण्डल लृ भूमि मूलाधार ल
इनकी प्रतिमा रूप पृथ्वी के उत्तर गोल के भारत पाद में ७ लोक है। उत्तर गोल के अन्य ३ पाद तथा दक्षिण गोल के ४ पाद - ये ७ तल हैं।
(ग) आधुनिक विज्ञान में प्रतिमा रूप-इन सिद्धान्तों को गोत्र सिद्धान्त (Anthropic Principle) कहते हैं। मनुष्य की आंख प्रकाश का वही भाग देखती है, जो पृथ्वी के वातावरण में सबसे कम अवशोषित होता है। मनुष्य शरीर के जल भाग (रक्त, प्लाज्मा) में लवणों का अनुपात वही है, जो समुद्र जल में है।
अपौरुषेयता-वेद इन ३ अर्थों में ही अपौरुषेय है-(क) ५ ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त ऋषि और परोरजा प्राण से अतीन्द्रिय ज्ञान। (ख) तीन विश्वों का समन्वय-जो अपने साथ महः (बाह्य विश्व) का सम्बन्ध देख सकता है, उसे महर्षि कहा गया है (वायु पुराण, ५९/८१-८२)। (ग) कई ऋषियों के मन्त्रों का संकलन करने से व्यक्तिगत आग्रह या कमी दूर हो जाती है।
३. तत्त्व वेद की अपौरुषेयता-
तत्त्व रूप में पूरा विश्व तथा उसके सभी स्तर ही पुरुष है जिसकी व्याख्या फुरुष सूक्त में की गयी है। जिस वेद से भूत, भविष्य, वर्तमान के विश्व और ३ लोकों की उत्पत्ति कही गयी है, वह तत्त्व वेद है। इस वेद से पुरुष की उत्पत्ति हुई अतः तत्त्व वेद भी अपौरुषेय है।
व्यक्त विश्व में प्रथम मण्डल के ३ मनोता (संकल्प का क्रिया रूप) थे-वेद, सूत्र, नियति।
इसका वेद तत्त्व है कि प्रत्येक विन्दु अन्य विन्दुओं से प्रभावित हो कर उनके बारे में जानता है। यह मूर्ति गति, महिमा-३ प्रकार का है जिनको ऋक्-यजु-साम कहा है।
सूत्र द्वारा २ या अधिक पिण्ड परस्पर सम्बन्धित होते हैं। इसके ३ प्रकार हैं-सत्य (सीमाबद्ध), ऋत (सीमाहीन), ऋत-सत्य (सीमा हीन किन्तु केन्द्र विन्दु)।
नियति सृष्टि या परिवर्तन की दिशा है। सांख्य में इसे सञ्चर-प्रतिसञ्चर कहा है, ईशावास्योपनिषद् में सम्भूति-असम्भूति (विनाश) कहा है। यथास्थिति या सन्तुलन इनकी बराबर स्थिति है।
पुरुष के ४ भागों में १ ही भाग व्यक्त विश्व है। ३ अव्यक्त भाग सदा रहते हैं (त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त, ३)। इस अव्यक्त भाग का वेद शून्य या अज्ञात है। व्यक्त भाग का अनन्त वेद है (भरद्वाज को इन्द्र द्वारा कथन-तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१०/११)-अनन्ताः वै वेदाः। यहां कई प्रकार के अनन्त हैं, ऋक का मूर्ति रूप संख्येय अनन्त है, यजुः का गति रूप असंख्येय अनन्त है, साम की महिमा अप्रमेय अनन्त है। अथर्व अज्ञेय अनन्त है। इस रूप में सृष्टि रूप पुरुष या अव्यक्त रूप पूरुष के लिए भी वेद अपौरुषेय हैं। विष्णु सहस्रनाम में ये शब्द हैं-अनन्त, असंख्येय, अप्रमेय, अमेयात्मा।
वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुमः (भागवत पुराण, ६/१/४०)
आद्यं त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयो यस्मिन्प्रतिष्ठिता ।
स गुह्योऽन्यस्त्रिविद्वेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥ (मनु स्मृति, १२/२६५)
ब्रह्माण्ड में वेद का स्वरूप भृगु रूप आकर्षण तथा अङ्गिरा रूप विकिरण है।
आपो भृग्वङ्गिरो रूपमापो भृग्वङ्गिरोमयं सर्वमापोमयं भूतं सर्वं भृग्वङ्गिरोमयमन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसोऽनुगाः (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, १/३९)
इसमें अङ्गिरा के ३ स्तर हैं-केन्द्र में अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद प्रभाव सीमा तक आदित्य। ये ऋक्, यजु, साम वेद हैं।
तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यस्त्रीन् देवान्निरमिमीत--अग्निं वायुमादित्यमिति---स खलु पृथिव्या एवाग्निं निरमिमीतान्तरिक्षाद्वायुं दिव आदित्यम्--अग्नेर्ऋग्वेदं वायोर्यजुर्वेदं आदित्यात्सामवेदम् (गोपथ ब्राह्मण, पूर्व, १/६)
भृगु (आकर्षण जनित पिण्डों की स्थिति) से अथर्व हुआ।
ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यो यद्रेत आसीत्तदभृज्ज्यत, तस्माद्भृगुः समभवत्--भृगुरिव वै स सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद। (गोपथ पूर्व, १/३)
अथर्वाणश्च ह वा अङ्गिरसश्च भृगुचक्षुषी तद्ब्रह्माभिव्यपश्यन् (गोपथ पूर्व, १/२२)
सौर मण्डल के भीतर भी भृगु-अङ्गिरा के कारण वेद हैं। सम्पूर्ण सौर मण्डल की स्थिति भृगु या अथर्व वेद (सनातन ब्रह्म) है। अग्नि (११ अहर्गण-पृथ्वी तक), वायु (२२ अहर्गण-यूरेनस तक), रवि या आदित्य (सौर मण्डल की सीमा-३३ अहर्गण तक) क्रमशः ऋक्, यजु, साम वेद हैं।
अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम्॥ (मनु स्मृति, १/२३)
यही यज्ञ के लिए वसु, रुद्र, आदित्य क्षेत्र हैं, जो यज्ञ या उत्पादन रूपी गौ से सम्बन्धित हैं-
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्यानां अमृतस्य नाभिः।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥ (ऋक्, ८/१०१/१५)
केवल सूर्य पिण्ड देखने से इसका पिण्ड (मूर्त्ति) ऋक् है, इसका शरीर यजु है (भीतरी क्रिया कृष्ण, बाहरी कम्पन अङ्गार् शुक्ल यजु), तथा इसके तेज, आकर्षण, वायु का प्रसार (त्रिसामा) सामवेद है।
यदेतन्मण्डलं तपति। तन्महदुक्थं ताऽऋचः सऽऋचां लोकोऽथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ यऽएष ऽएतस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजूंषि स यजुषां लोकः॥ (शतपथ ब्राह्मण, १०/५/२/१)
चान्द्र मण्डल के मनोता हैं-रेत (सोम कण), श्रद्धा (कणों के बीच सम्बन्ध), यश (महिमा)। यही ३ वेदों के रूप हैं।
पृथ्वी से देखने पर वाक्, गौ, द्यौ-३ मनोता हैं, जो ३ वेदों के स्वरूप हैं। वाक् ३ प्रकार की पृथ्वी की माप है-२४ अहर्गण (गायत्री) पृथ्वी ग्रह है, त्रिष्टुप् (४४ अहर्गण) सूर्य का क्षेत्र महर्लोक तक, जगती (४८ अहर्गण) ब्रह्माण्ड।
जब तक स्वयम्भू, ब्रह्माण्ड, सौर मण्डल, चान्द्र मण्डल तथा पृथ्वी है, तब तक ये तत्त्व वेद सनातन हैं। ये सभी अपने पुर के पुरुषों से परे हैं।
४. ज्ञान प्राप्ति का क्रम-
निसर्ग से प्राप्त ज्ञान विद्या है, अतः इसे निगम (वेद) कहते हैं। वेद के कई अर्थ हैं-तत्त्व वेद को वेद पुरुष कहते हैं। विश्व का शब्द रूप में वर्णन श्री वेद है-
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्।
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ (मैत्रायणी उपनिषद्, ६/२२)
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
ब्रह्म या पुरुष वेद का ३ प्रकार विभाजन है-मूर्ति तत्त्व ऋक् है, गति यजुर्वेद है (शुक्ल-कृष्ण गति के अनुसार २ प्रकार का), महिमा या प्रभाव साम वेद है तथा स्थिर सनातन आधार ब्रह्म या अथर्व वेद है, (थर्व = थरथराना, अथर्व = स्थिर) शब्द रूप वेद श्री का रूप है-
शब्दात्मिकां सुविमलर्ग्यजुषां निधानमुद्गीथ रम्य पद-पाठवतां च साम्नाम्।
देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमार्ति हन्त्री॥ (दुर्गा सप्तशती, ४/१०)
वेद में पुरुष रूप का वर्णन पुरुष सूक्त तथा श्री रूप का वर्णन श्री सूक्त, रात्रि सूक्त आदि में है।
४ प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के कारण विद् धातु के ४ अर्थ तथा ४ वेद हैं। पहले किसी वस्तु की सत्ता होनी चाहिए, अर्थात् मूर्त्त रूप जिसका वर्णन ऋग्वेद करता है। उस मूर्त्ति से कोई ध्वनि, प्रकाश, गन्ध आदि प्रभाव आना चाहिए। यह गति रूप यजुर्वेद है। उसकी प्रभाव सीमा या महिमा के भीतर ही उसका ज्ञान हो सकता है। महिमा सामवेद है। महिमा क्षेत्र में ही ज्ञान हो सकता है, अतः भगवान् ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है।
ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजं सामरूप्यं ह शश्वत्, सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३/१२/८/१)
वेदानां सामवेदोऽस्मि (गीता, १०/२२)
तत्त्व वेद विद धातु का अर्थ
मूर्ति ऋक् सत्ता (विद् सत्तायाम्, धातुपाठ, ४/६०)
गति यजु लाभ, प्राप्ति-विद्लृ लाभे (६/१४१)
ज्ञान साम विद् ज्ञाने (२/५७)
आधार अथर्व विद् विचारणे (७/१३), चेतनाख्यान निवासेषु (१०/१७७)
प्रकृति या निसर्ग के जिस क्षेत्र की महिमा हम तक पहुंचती है वह महः है। उससे प्राप्त विद्या वेद है। उस ज्ञान का प्रयोग महः पर किया जाय तो वह महाविद्या है।
निसर्ग से प्राप्त ज्ञान ३ प्रकार का है। यह जैन दर्शन के शब्द हैं।
श्रुति ज्ञान-जितना हम निकट क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं। यह वेद हुआ, अतः इसे श्रुति कहते हैं।
अवधि ज्ञान-प्रकृति में परिवर्तन या गति जानने के लिए कुछ समय बाद पुनः देखना पड़ता है कि कितना अन्तर हुआ। पुरा का नवीन रूप देखने की पद्धति पुराण (पुरा + नवति) है।
केवल ज्ञान-ज्ञान पूरे विश्व में फैला है। उसका कुछ ही भाग ज्ञेय है। ज्ञेय भाग भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं। उस वस्तु की पूरी सूचना नहीं आती है, उसका कुछ ज्ञान कुछ अनुमान मिल कर परिज्ञान है।
अतः ज्ञान प्राप्ति का कर्म ३ प्रकार का है-
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना। (गीता, १८/१८)
५. अपरा विद्या-
विश्व या उसका चेतन रूप ब्रह्म अज्ञात है। विभिन्न दर्शनों या शास्त्रों में कई प्रकार के विभाजन द्वारा ही वह समझा जा सकता है।
नवैकादश पञ्च त्रीन् भावान् भूतेषु येन वै। ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्॥१४॥
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्। स्थित्युत्पत्तिलयान् पश्येद् भावानां त्रिगुणात्मकम्॥१५॥
(भागवत पुराण, ११/१९/१४-१५)
जगत् के अनन्त पदार्थों का ९, ११, ५, ३ में वर्गीकरण करना और अन्त में १ ही मूल तत्त्व देखना ज्ञान है। वर्गीकरण की पद्धति विज्ञान है। इसी को मुण्डक उपनिषद् (१/१/२) में परा-अपरा विद्या कहा है। परा विद्या को केवल विद्या तथा अपरा विद्या को अविद्या कहते हैं। यह विद्या का अभाव नहीं, उसका वर्गीकरण है। बिना सम्बन्ध समझे उनको भिन्न देखना भी विद्या का अभाव ही है।
वर्गीकरण के उदाहरण-न्याय वैशेषिक के ९ द्रव्य, ९ सर्ग, ९ दुर्गा, ५ महाभूत, विश्व के ५ पर्व, पञ्चाग्नि, ३ गुण, ३ लोक, ३ धाम, ॐ के ३ अक्षर, ११ रुद्र, मन सहित ११ इन्द्रियां, या सांख्य में प्रकृति-पुरुष के २५ तत्त्वों के अतिरिक्त शिव-शक्ति की ११ प्रत्यभिज्ञा।
अज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए उसे ३ भाग में समझते हैं-
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च॥
(श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/८)
= उस (ब्रह्म) का कार्य, करण आदि का पता नहीं चलता है, वैसा या अधिक कोई नहीं दीखता। हमारी कल्पना से परे है, अतः उसे ज्ञान-बल-क्रिया रूप में देखते हैं।
अतः विद्या के २ रूप कहे गये हैं-परा विद्या (विद्या) = एकीकरण, अपरा विद्या (अविद्या) = वर्गीकरण।
द्वे विद्ये वेदितव्ये- ... परा चैव, अपरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।
(मुण्डक उपनिषद्, १/१/३-५)
इनको ज्ञान-विज्ञान भी कहा है-ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः (गीता, ७/२)।
विज्ञान का वही अर्थ है जो आधुनिक साइंस में है-मोक्षे धीः ज्ञानं अन्यत्र विज्ञानं शिल्प शास्त्रयोः (अमरकोष, १/५/९)। यहां विज्ञान में उसका प्रयोग या इंजीनियरिंग भी है।
आधुनिक विज्ञान में केवल एक परिभाषा है-वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसकी पद्धति है-विभिन्न घटनाओं में साम्य देख कर नियम बनाना। परीक्षण या प्रयोग द्वारा नियम में त्रुटि देखकर उसमें संशोधन करना।
योग सूत्र (२/३) में विद्या के अभाव को अविद्या कहा है तथा उसके ५ पर्व कहे हैं। इनका अपरा विद्या अर्थ में आधुनिक परिभाषा से अधिक व्यापक अर्थ है-
(१) अविद्या = विषयों या तथ्यों का विभाजन।
(२) अस्मिता = प्रति तत्त्व या वर्ग की अलग अलग परिभाषा और व्याख्या।
(३) राग = अलग अलग तथ्यों में समानता खोज कर एक वर्ग में करना (Generalization)।
(४) द्वेष = अन्य वर्ग के तथ्यों से भेद दिखाना।
(५) अभिनिवेश = सिद्धान्त स्थिर करना, जिसके अनुसार नये तथ्यों को प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है।
वैदिक साहित्य इसी क्रम में है-
(१) संहिता = ऋषियों के मन्त्रों का संकलन।
(२) ब्राह्मण = सूतों की विषय अनुसार व्याख्या-वर्गी करण।
(३) आरण्यक = प्रयोग।
(४) उपनिषद् = स्थिर सिद्धान्त, निष्कर्ष।
वेदस्योपनिषत् सत्यम्, सत्यस्योपनिषद् दमः आदि (महाभारत, शान्ति पर्व, २५१/११-१२)
तस्माद् वा अप उपस्पृशति-इति उपनिषत् (शतपथ ब्राह्मण, १/१/१/१)
६. वर्णाश्रम और धर्म का स्रोत-
आधुनिक शिक्षा में इसकी कमी है। कई पन्थ बहुत इश्वरों को मान कर केवल अपने ईश्वर को सही मानते हैं तथा अन्य की हत्या करते है। उनके अनुसार उस पुस्तक का पालन ही धर्म है। वेद में धर्म का एक अर्थ प्राकृतिक गुण है (वैशेषिक दर्शन)। सामान्यतः धर्म का अर्थ है कि इससे प्रजा (व्यक्ति, समाज) का धारण होता है-
धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ (महाभारत, शान्ति पर्व, १०९/१२)
संहिता भाग में केवल ऋषियों द्वारा मन्त्र का दर्शन है। उसमें कर्तव्य नही लिखा है, जिसे विधि (कर्तव्य), निषेध (वर्जित) कहते हैं। इसके लिये वेद आधारित स्मृति ग्रन्थ है (मनुस्मृति, २/१२)। ब्राह्मण भाग में वेद व्याख्या है जिनके अनुसार कल्प सूत्र में विधि-निषेध का वर्णन है। ६ वेदाङ्गों में कल्प भी है।
इन ग्रन्थों में ४ वर्ण तथा ४ आश्रमों के कर्तव्य का वर्णन है। इस अर्थ में वेद से ही धर्म और वर्णाश्रम की उत्पत्ति हुई है। यह समझने के लिए वेद में संहिता के साथ तीनों ब्राह्मण भाग (ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्), ६ अंग तथा स्मृति को भी वेद मानना होगा।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.