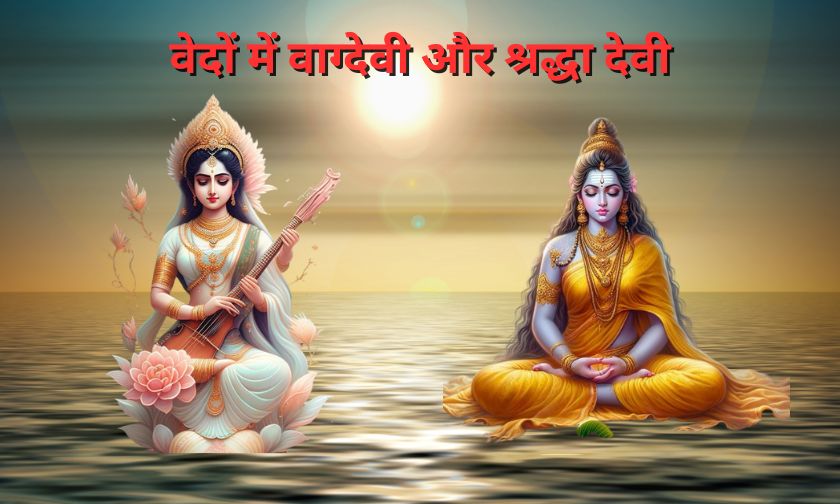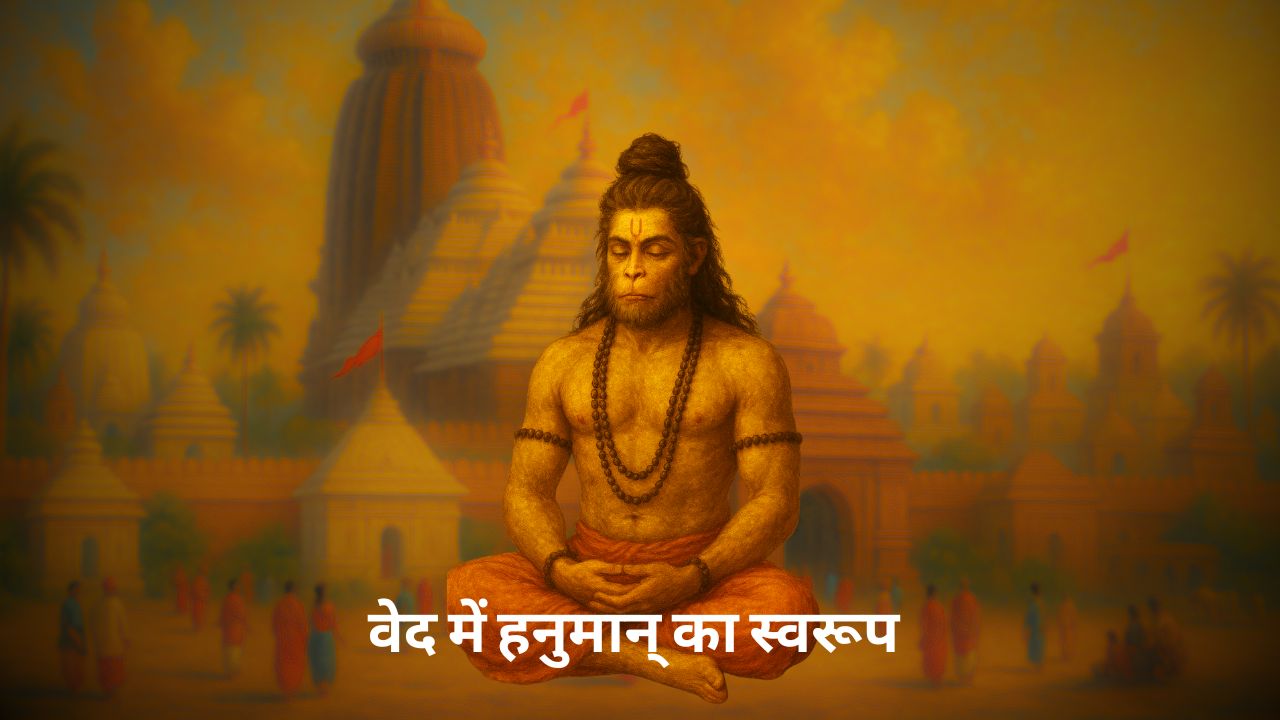- महापुरुष
- |
- 31 October 2024
- |
- 0 Comments

श्री शशांक शेखर शुल्ब (धर्मज्ञ )- Mystic Power- ऋग्वेद के अतिमहत्त्वपूर्ण सूक्तों में वाग्देवी और श्रद्धादेवी से सम्बद्ध दो सूक्त (ऋगू० १०.१२५.१ से ८ और ऋ० १०.१५१.१ से ५) हैं। इनमें वाग्देवी और श्रद्धादेवी के स्वरूप, कार्य और महत्त्व का वर्णन है।
(क) वाग्देवी :- ऋग्वेद के १०.१२५ सूक्त के आठ मंत्रों का ऋषि 'वाग् आम्भृणी' है। इसका देवता या वर्ण्य विषय आत्मा या वाक्तत्त्व है। इन आठ मंत्रों में वाग्देवी उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करती है ।
इस सूक्त का महत्त्व इस बात से प्रकट होता है कि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भाषाविज्ञान के प्रोफेसर सईस (Prof. Sayce) ने अपने ग्रन्थ 'Science of Lan- guage' भाग १ के पृष्ठ १ पर भाषाशास्त्रियों का ध्यान इस सूक्त की ओर आकृष्ट किया है। प्रो० सईस का कथन है कि इन आठ मंत्रों में वैदिक ऋषि का वाक्तत्त्व के विषय में जो वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर, विचारपूर्ण, भाषाविज्ञान के दृष्टि से सत्य तथा बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। इन आठ मन्त्रों में वाग्देवी का महत्त्व इस रूप में वर्णन किया गया है :
१. मैं (वाग्देवी) रुद्रों (प्राणतत्त्व, एकादश रुद्र), वसुओं (पृथिवी आदि आठ वसुओं, आदित्यों (१२ आदित्य, सूर्य) तथा विश्वदेवों (सभी देवों, सभी दिव्य विभूतियों) के साथ विचरण करती मैं मित्र और वरुण (सौर तत्त्व और जलीय तत्त्व) तथा इन्द्र और अग्नि (सौर तत्त्व और अग्नि तत्त्व) को धारण करती हूँ। मैं दोनों अश्विनीकुमारों (प्राण और अपान तत्त्व) को धारण करती हूँ । ऋग्वेद के १०.१२५ सूक्त के आठ मंत्रों का ऋषि 'वाग् आम्भृणी' है। इसका देवता या वर्ण्य विषय आत्मा या वाक्तत्त्व है। इन आठ मंत्रों में वाग्देवी उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करती है । "अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि-अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ।।" ( मंत्र १ )
२. मैं (वाग्वेदी) सोमतत्त्व की पालक और रक्षक हूँ। मैं त्वष्टा (विश्लेषक तत्त्व), पूषन् (पोषक तत्त्व) और भग (ऐश्वर्य) की पालक हूँ। मैं यज्ञकर्ताओं को ऐश्वर्य से समृद्ध करती हूँ। "अहं सोममाहनसं बिभर्मि अहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् । अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ।।" ( मंत्र २ )
३.मै राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ। मैं वसुओं (पृथ्वी आदि आठ वसुओं) को संबद्ध करने वाली हूँ। मैं विज्ञानमय हूँ। मैं पूजनीयों में अग्रगण्य हूँ। देवों (विद्वानों, भाषाशास्त्रियों) ने मुझे नाना (भाषाओं का) रूप देकर नाना प्रकार से प्रतिष्ठित किया है । "अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा, भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ।।" ( मंत्र ३)
४. जो मेरा (वाग्देवी या प्रतिभा) का साक्षात्कार करता है, जो मुझको हृदय में धारण करता है और मेरे कथन को सुनता हूँ, वह भौतिक जगत् का उपभोग करता है। दो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। मैं श्रद्धा के योग्य इस वचन को स्वयं कहती हूँ । "मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति या ई शृणोत्युक्तम् । अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रधिवं ते वदामि।।" ( मंत्र४)
५. मैं स्वयं यह कहती हूँ कि देवता और मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं। मेरी जिस पर दयादृष्टि होती है, उसको मैं उग्र (तेजस्वी) बना देती हूँ । उसको ब्रह्म (ब्रह्मवेत्ता, आत्मतत्त्वज्ञ) बना देती हूँ। उसको ऋषि और मेधावी बना देती हैं। "अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ।।" (मंत्र ५ )
६. मैं ब्रह्मद्वेषी के विनाश के लिए रुद्र को धनुष से सुसज्जित करती हूँ। मैं जन- कल्याण के लिए युद्ध करती हूँ। मैं द्युलोक और पृथिवी में सर्वत्र व्याप्त हूँ। "अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । अहं जनाय समदं कृणोमि-अहं द्यावापृथिवी आ विवेश ।।" ( मंत्र६)
७. मैं (वाग्देवी) इस संसार के शिरोभाग में चुलोक को उत्पन्न करती हैं। बुद्धिरूपी समुद्र के अन्तस्तल (ईश्वरीय ज्ञान) में मेरा निवास स्थान है। उसी स्थान से में सारे विश्व में व्याप्त हूँ। मैं अपने शरीर से द्युलोक को स्पर्श करती हूँ । "अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ।।" ( मंत्र ७)
८. मैं ही वायु के तुल्य सर्वत्र बह रही (व्याप्त) हूँ। मैं सारे संसार का निर्माण करती हूँ। मैं द्युलोक और पृथिवी से परे हैं, अर्थात् इनमें अलिप्त होकर रहती हूँ। मैं अपने सामर्थ्य से ही प्रकट होती हूँ। "अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव ।।" ( मंत्र ८)
इन मंत्रों में वाग्देवी के इन गुणों का विशेषरूप से उल्लेख है :-
१. वाग्देवी रुद्र, आदित्य, वसु आदि सभी देवों की रक्षक और पालक है।
२. वाग्देवी सोम्य गुणों की दात्री है।
३. वह भक्तों को सभी ऐश्वर्य प्रदान करती है।
४. वाग्देवी राष्ट्रीय भावना प्रदान करती है। इसमें संगठन की शक्ति है। वाग्देवी (भाषा) को ही विविध रूप देकर विद्वानों ने विश्व की समस्त भाषाओं को जन्म दिया है।
५. जो वाग्देवी को प्रसन्न कर लेता है, वह संसार के सारे सुख भोगता है। जो वाग्देवी का निरादर करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है ।
६. वाग्देवी के अनुग्रह से ही मनुष्य ब्रह्मर्षि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी और मेधावी होता है।
७. वाग्देवी निरादर करने वाले को समाप्त कर देती हैं। वह लोकहित के लिए संघर्ष करती हैं और सारे संसार में व्याप्त है।
८. वाग्देवी सारे संसार की निर्मात्री है।
९. सृष्टि निर्माण वाग्देवी का कार्य है। वह सर्वत्र व्याप्त होने पर भी निर्लेप, निरंजन और निष्काम है।
ब्राह्मण ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में वाग्देवी (विद्या, सरस्वती) के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।
१. वाग्देवी ब्रह्म स्वरूप है। वह ब्रह्म का विराट् रूप है। वह समुद्र की तरह अनन्त और अक्षय है। वह कभी नष्ट नहीं होती। (
क) "वाग् ब्रह्म ।" ( गोपथ ब्रा० १.२.१०) (ख) "वाग् वै ब्रह्म ।" ( ऐत०ब्रा० ६.३ । शत०ब्रा० २.१.४-१० ) (ग) "वाग् वै विराट् ।" (शत० ब्रा० ३.५.१.३४ ) (घ) "वाग् वै समुद्रो न वै वाक् क्षीयते न समुद्रः ।" ( ऐत० ब्रा० ५.१६)
२. वाग्देवी ही विद्या, बुद्धि और सरस्वती है। (क)" वाग् वै धिषणा ।" (शत० ब्रा० ६.५.४.५) (ख) "वाग् वै मतिः ।" ( शत०ब्रा० ८.१.२.७) (ग) "वागेव सरस्वती ।" ( ऐत०ब्रा० २.२४)
३. वाग्देवी कामधेनु है । वह सभी कामनाएं पूर्ण करती है । (क)"वाग् वै धेनुः (कामधेनुः) ।" ( गोपथ० १.२.२१ ) (ख) 'वाचं धेनुम् उपासीत ।" ( शत०ब्रा० १४.८.९.१)
४. वाग्देवी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रप्रेम देती है। "वाग्वै राष्ट्री ।" ( ऐत० १.१९)
५. वाग्देवी विश्वकर्मा है। वह सब कुछ बना और बिगाड़ सकती है। "वाग्वै विश्वकर्मा ऋषिः। वाचा हीदं सर्वं कृतम् ।" ( शत० ८.१.२.९)
६. वाग्देवी सारे देवों की प्रतिनिधि है। (क) "वागिति सर्वे देवाः ।" ( जैमि० उप०ब्रा० १.९.२) (ख) "वागेव देवाः ।" ( शत० १४.४.३.१३)
७. वाक और मन दोनों संबद्ध हैं। मन के भावों की अभिव्यक्ति का साधन वाणी है। (क) "वाक् च वै मनश्च देवानां मिथुनम्।" ( ऐत०ब्रा० ५.२३) (ख)" तस्य (मनसः ) एषा कुल्या यद् वाक्।" ( जैमि० उप०ब्रा०१.५८.३)
८. मन, वाक् (वाणी) और प्राण अमर हैं। ये प्रजापति के अमर रूप हैं। "अथैता अमृता मनो वाक् प्राणः ।" (शत० १०.१.३.४)
९. वाक् आग्नेय तत्त्व है। इसमें आग्नेय गुण दाहकता, शोधकता आदि है। "वागेवाग्निः ।" ( शत० ३.२.२.१३ )
१०. वाक् ओषधि है। यह सब रोगों की चिकित्सा है। मधुर और सान्त्वनापूर्ण वाणी रोगी का कष्ट दूर करती है। मन्त्र-चिकित्सा का आधार वाक्तत्त्व ही है। "वागु सर्व भेषजम् ।" (शत० ७.२.४.२८)
श्रद्धा श्रद्धा एक सात्त्विक भावना है। किसी महापुरुष के उत्कृष्ट गुणों के आधार पर यह श्रद्धा की भावना जागृत होती है और उसके गुणों को अपनाने की कामना जागृत करती है। यह उत्कृष्ट गुणों की आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। श्रद्धा का सामान्यतया अर्थ होता है- 'श्रत् सत्यं धीयते यत्र सा श्रद्धा' हृदय में सत्य की स्थापना करना श्रद्धा है। असत्य को हटाकर सत्य को प्रतिष्ठित करना श्रद्धा है। यजुर्वेद में श्रद्धा का महत्त्व बताते हुए कहा गया है कि व्रत धारण करने से मनुष्य दीक्षित होता है, दीक्षा से उसे दाक्षिण्य (दक्षता, निपुणता प्राप्त होता है दक्षता की प्राप्ति से श्रद्धा का भाव जागृत होता है और श्रद्धा से सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
"व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम् । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ।।" ( यजु० १९.३० )
भाषाविज्ञान की दृष्टि से श्रद्धा का मौलिक अर्थ ज्ञात होता है। संस्कृत का श्रद शब्द और लेटिन का हृदय वाचक Cord (कॉर्ड) शब्द मूलरूप में एक ही शब्द हैं। लेटिन के हृदय-वाचक Cord शब्द से अंग्रेजी के Cordial (कॉर्डियल, हार्दिक ), Cor date (कॉर्बेट, हृदयाकार) आदि शब्द बने हैं। अतः श्रद्धा का मौलिक अर्थ है 'अतु हृदयं धीयते यत्र सा श्रद्धा' जिसमें अपने हृदय को लगाते हैं या जिसके प्रति अपने हृदय को समर्पित करते हैं, वह श्रद्धा है। श्रद्धास्पद व्यक्ति को हम अपना हृदय समर्पित करते हैं। यह समर्पण गुणों के आधार पर सात्त्विक भाव से किया जाता हैं - | ऋग्वेद में एक महत्त्वपूर्ण सूक्त श्रद्धा सूक्त (ऋग्० १०.१५१/१ से ५) है। इस सूक्त की द्रष्टा 'श्रद्धा कामायनी' है। कामायनी का अर्थ है-काम अर्थात् कामनाओं या सात्त्विक विचारों का आश्रय स्थान तैत्तिरीय ब्राह्मण में कामायनी का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि श्रद्धा कामनाओं की माता या सदविचारों की जन्मदात्री है।
"श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वर्धयामसि ।" ( तै०ब्रा० २.८.८८)
हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने ऋग्वेद के इस सूक्त को आधार बनाकर हिन्दी में अपनी अमर काव्य-कृति 'कामायनी' की रचना की है।
ऋग्वेद में श्रद्धा का गुणगान करते हुए वर्णन किया गया है।
१. श्रद्धा से ही यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। श्रद्धा से अग्नि में हव्य पदार्थ डालते हैं। श्रद्धा सर्वोत्तम विभूति है। उसे हम प्रणाम करते हैं। "श्रद्धयाऽग्निः समिध्यते, श्रद्धया हूयते हविः । श्रद्धां भगस्य मूर्धनि, वचसा वेदयामसि ।।" ( ऋग्०१०.१५१.१)
२. हे श्रद्धा ! तू दान देने वाले को अभीष्ट फल दे । तू दान देने की इच्छा करने वाले का भी प्रिय कर। तू दानदाताओं और यज्ञकर्ताओं का प्रिय कर । "प्रियं श्रद्धे ददतः, प्रियं श्रद्धे दिदासतः । प्रियं भोजेषु यज्वसु-इदं म उदितं कृधि ।।" ( मंत्र २)
३. जिस प्रकार देवों ने उग्र असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने में श्रद्धा की, उसी प्रकार हे श्रद्धा ! तुम दाताओं और यज्ञकर्ताओं का प्रिय करो । "यथा देवा असुरेषु, श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । एवं भोजेषु यज्वसु- अस्माकमुदितं कृधि ।।" ( मंत्र ३)
४. देवगण और यज्ञकर्ता मनुष्य प्राणविद्या से सुरक्षित होकर श्रद्धा की उपासना करते हैं। वे हार्दिक संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं। श्रद्धा से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। "श्रद्धां देवा यजमाना, वायुगोपा उपासते । श्रद्धां हृदय्ययाऽऽकृत्या, श्रद्धया विन्दते वसु ।।" ( मंत्र ४ )
५. हम प्रातः, मध्याह्न और सायं श्रद्धा का आवाहन करते हैं। हे श्रद्धा ! तुम हमें श्रद्धावान् करो। "श्रद्धां प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यंदिनं परि । श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि, श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ।।" ( मंत्र ५ )
इन पांच मंत्रों में श्रद्धा देवी के इन गुणों का विशेषरूप से उल्लेख है :-
१. सभी धार्मिक कृत्यों के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है।
२. श्रद्धा सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य है।
३. दान और यज्ञ श्रद्धापूर्वक करने पर ही पूर्ण सफल होते हैं।
४. गुणों में उच्चता और उत्कृष्टता ही व्यक्ति को श्रद्धास्पद बनाती है ।
५. श्रद्धा देवी को प्रसन्न करने के लिए हृदय के विचारों की पवित्रता अनिवार्य है। श्रद्धा वैभव की दात्री है।
६. हृदय की पवित्रता से ही श्रद्धा हृदय में प्रतिष्ठित होती है।
ब्राह्मणग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में श्रद्धा देवी के विषय में ये विचार मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं ।
१. श्रद्धा के साथ सत्य का समन्वय होना चाहिए। अतः सत्य को यजमान (पति) और श्रद्धा को पत्नी कहा गया है। "श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः ।" ( ऐत० ७.१० १)
२. श्रद्धा सद्विचारों की जननी है। उसे निरन्तर बढ़ावें । "श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वर्धयामसि ।" ( तैत्ति० २.८.८.८ )
३. सत्कर्मों में प्रवृत्ति के लिए श्रद्धा की भावना आवश्यक है। अतः किसी प्रकार की दीक्षा के लिए श्रद्धा का होना अनिवार्य है। "एतद् दीक्षायै (रूपं) यत् श्रद्धा ।" (शत० १२.८.२.४)
४. श्रद्धा से तेजस्विता आती है। "तेज एव श्रद्धा ।" ( शत० ११.३.१.१)
५. श्रद्धा से मनोरथ की पूर्ति अवश्य होती है। जितनी अधिक श्रद्धा होगी, उतनी ही सफलता शीघ्र प्राप्त होगी। "श्रद्धैव सकृद् इष्टस्याक्षितिः । स यः श्रद्दधानो यजते, तस्येष्टं न क्षीयते ।" ( कौषीतकि० ७.४ )
६. श्रद्धा तेजोरूप है। वह सूर्य की पुत्री है। उसमें सूर्य के गुण है। "श्रद्धा वै सूर्यस्य दुहिता ।" ( शत० १२.७.३.११ ) इस प्रकार ज्ञात होता है कि वाग्देवी और श्रद्धादेवी की उपासना सर्वदा सफल होती है और वे सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। साथ ही यह उपासना भगवत्प्रेम की अभिवृद्धि में पूर्ण सहायक होती है ।
Related Posts
0 Comments
Comments are not available.